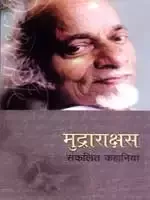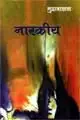|
कहानी संग्रह >> मुद्राराक्षस संकलित कहानियां मुद्राराक्षस संकलित कहानियांमुद्राराक्षस
|
2 पाठक हैं |
||||||
कथाकार द्वारा चुनी गई सोलह कहानियों का संकलन...
संकलन की कहानियां
| १. | फरार मल्लावां माई राजा से बदला लेगी |
| २. | जले मकान के कैदी |
| ३. | एहसास |
| ४. | एक बंदर की मौत |
| ५. | दिव्य दाह |
| ६. | प्रतिहिंसा |
| ७. | यूसुफ मियां की मृत्यु और प्रधानमंत्री का पानी |
| ८. | विस्थापित |
| ९. | पैशाचिक |
| १॰. | मुजरा |
| ११. | दुर्घटना |
| १२. | हीराबाई नाचेगी |
| १३. | निहत्थे |
| १४. | कटोरी देवी |
| १५. | चिरकुट |
| १६. | मुठभेड़ |
भूमिका
लगभग दस साल पहले की बात है। जाड़ों के दिन थे। सबाल्टर्न-पंथी इतिहासकारों
का सालाना जलसा उस बार लखनऊ में लगा था। देश-विदेश से आयी विद्वानों की एक
पूरी जमात वहां इकट्ठी थी। इतिहास, संस्कृति और सिद्धांत को लेकर चलने वाली
एक लंबी बहस ठंड और कोहरे के साथ शहर को अपने आगोश में लिए हुए थी।
तीसरे दिन आयोजन खत्म हुआ। मैं घर लौटा ही था कि घंटी बजी। दरवाजे पर
मुद्राराक्षस खड़े थे। "तुमसे बातें करनी है। जो कुछ तुम वहां कह रहे थे उसके
बारे में। इनको लेता आया। तुम्हारा घर इन्हीं को पता था।" शहर में ही रहने
वाले एक प्रसिद्ध आलोचक की ओर इशारा करते हुए मुद्राजी अंदर दाखिल हुए। उनसे
मेरी बाकायदा जान-पहचान का यह पहला दिन था।
पहली नजर में तो यही लगा कि सहमति की बजाय असहमति के बिंदु अधिक निकलेंगे और
हमारी बहस ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। मातहत जनों और दबी-कुचली जातियों के साथ
पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े मुद्राजी सबाल्टर्निस्ट इतिहास-दृष्टि के करीब
पड़ेंगे। ऐसी प्रतिबद्धता मेरी भी थी लेकिन इस किस्म के इतिहास-दर्शन को लेकर
मेरे सवाल थे। मुझे लगता था कि सबाल्टर्नी लोग उत्तर-आधुनिक किस्म के रवैये
से ग्रस्त थे। इतिहास के 'महाख्यान' का विखण्डन उनकी वैचारिक परियोजना का
केन्द्रीय तत्त्व प्रतीत होता था। वृहत्-रूप कर्ता का विसर्जन कर वे समतल
बिछे आम जनों में सूक्ष्म-रूप कर्तृत्व के बीज ऐसे बिखेर देना चाहते थे कि
इतिहास की फसल चौरस उगे। उसमें कोई बड़ी लहर न हो, चढ़ने और उतरने वाले
रास्ते न हों, प्रगति-अवनति की युगीन धारणाएं न हों, अंतरिक्ष के शून्य में
स्थित प्राकृतिक दिक-काल की भांति समय की कोई दिशा न हो। सबाल्टर्नी
विद्वत-जनों से मेरा मुख्य प्रश्न यही था-आप के इतिहास में समय की अवधारणा
है? गति की अवधारणा है? दीर्घस्तरीय और वृहत्-रूप कार्य-कारणता की अवधारणा
है? मानव प्रजाति के 'है' (being) से आगे ‘होने' (becoming) की भी अवधारणा है
या नहीं?
मुश्किलें और भी थीं। सबाल्टर्नी इतिहास-दर्शन की उत्तर औपनिवेशिकता के
सिद्धांत से गहरी सांठ-गांठ लगती थी। औपनिवेशिकता की दशा ही मानो अंतिम
निर्धारक दशा हो जिसने गुलाम मुल्कों का उत्तर काण्ड हमेशा के लिए लिख दिया
हो। अतीत मुग्ध अवस्थाओं के खतरे भी मौजूद थे। पहले के समुदाय, जन और
जीवन-रूप बेशक औपनिवेशिकता की हिंसा और विध्वंस के खेल का मैदान बने, लेकिन
अपने-आप में क्या वे ऐसे थे कि उनकी ओर वापस लौटने को उत्तर-औपनिवेशिक समय का
युगीन उपक्रम बना दिया जाए? और समय का पहिया मोड़ा न जा सके तो औपनिवेशिकता
को शाप देने का बौद्धिक कर्मकाण्ड अनन्त काल तक चले?
मुद्रा जी के साथ चलने वाली बहस उस अंदेशे के साथ शुरू हुई कि लोकवाद और
सामुदायिकतावाद के हिन्दी-साहित्य-सुलभ किसी पापुलिस्ट संस्करण से मुठभेड़
होगी और इस उम्मीद के साथ कि विचारधारात्मक कहा-सुनी के बहुत गर्म होने से
पहले ही हम एक दूसरे से विदा लेंगे। यह अंदेशा कितना बेबुनियाद था इसका
अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब से अब तक के लगभग दस वर्षों में,
यात्राओं और बीमारियों जैसी विघ्न-बाधाओं को छोड़ दें तो, लगभग हर हफ्ते या
दो हफ्ते में कम से कम एक शाम हम जरूर साथ बैठे हैं। इन हजार-बारह सौ घंटों
की वैचारिक कुश्ती सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, धर्म, साहित्य,
सिद्धांत, विज्ञान और दर्शन के अखाड़े में ही लड़ी गई है। बिला-शुबहा इस
कुश्ती से हम दोनों की सेहत अच्छी हुई है।
ऐसा नहीं है कि इन बहसों ने कभी उग्र रूप धारण न किया हो। इन वर्षों में एक
परम्परा यह भी बन गयी है कि इन शामों की समाप्ति मुद्राजी को अशोक मार्ग तक
छोड़ने की पैदल यात्रा के साथ होती है जहां से वे घर जाने के लिए कोई वाहन
पकड़ते हैं। बहसों का 'स्पिल-ओवर' मेरे घर से अशोक मार्ग तक जाने वाली इस
सड़क पर तो हुआ ही है, यदा-कदा ऐसा भी हुआ है कि यह किलोमीटर हम दोनों ने
बिना एक भी शब्द बोले तय किया हो। ऐसी मूक यात्राओं की शुरुआत प्रायः
मुद्राजी के बीच बहस में अचानक उठ खड़े होने से होती है-“बस! बहुत हो गया। अब
बातचीत का कोई फायदा नहीं है।" हम बोलते नहीं लेकिन अशोक मार्ग तक का सफर
जरूर साथ पूरा करते हैं।
हम दोनों अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर लड़ते हैं। इसका दोनों में से किसी को
अफसोस नहीं है। फिर अपनी अपनी जगहों से कुछ खिसकते भी हैं। इसका भी अफसोस
नहीं हैं एक अच्छा-खासा सफर इसी तरह पूरा हुआ है। लेकिन, बहुत बाद में, मुझे
एक बात का अफसोस जरूर हुआ। मुझे लगा कि इन बहसों में उग्र रूप धारण करने से
पहले मुझे उनका साहित्य पढ़ लेना चाहिए था।
हैरत की बात यह नहीं है कि कई वर्षों की अंतरंगता के बावजूद मैंने मुद्राजी
का साहित्य पढ़ा नहीं था। हिन्दी साहित्य की मेरी लगभग अनपढ़ता मित्रों को
मालूम है और हिन्दी कथा-साहित्य को लेकर मेरी अरुचि और पूर्वाग्रह उनकी
आलोचना का विषय भी रहे हैं। हैरत वाली बात यह थी मुद्राजी ने खुद मुझसे कभी
भी अपना साहित्य पढ़ने को नहीं कहा। बल्कि मैंने कभी इच्छा जाहिर भी की तो
उन्होंने हतोत्साहित किया। कहा-क्यों वक्त बरबाद करोगे। ये साहित्य-वाहित्य
भी कोई पढ़ने की चीज़ है। तुम विचार की दुनिया के आदमी हो। उसी में समय लगाओ
तो अच्छा है।
मुद्रा जी के लेख मैंने पढ़े थे। लगभग उन सभी विषयों पर बहस तो की ही थी।
मुझे लगता था कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की बेबाक समीक्षा उनकी भारी
उपलब्धि है, लेकिन नतीजों तक पहुंचने की जल्दबाजी भी दिखाई पड़ती है। इसी वजह
से रुख, रवैय्ये और विश्लेषण में संश्लिष्टता और जरूरी जटिलता की कमी लगती
है। लेकिन यह मेरी भूल थी, जिसकी जड़ में मेरी जानकारी का अधूरापन था। उनके
कथा-साहित्य से अपरिचय इसका मुख्य कारण था।
अपने लेखों में मुद्राजी युद्धरत विश्लेषक हैं। वे पोजीशन लेते हैं, तर्क
करते हैं, एक पक्ष में खड़े होते हैं और हमला बोलते हैं। वहां सब कुछ
बहिर्मुख हैं। लेकिन उनके कथा-साहित्य की बात और है। सभ्यता-समीक्षा वहां भी
है, पोजीशन वहां भी है, और हमला भी हैं लेकिन वहां एक संस्कृति का अपने आप से
जूझना भी है, एक शापग्रस्त सभ्यता का आत्मसंघर्ष भी हैं उदाहरण के लिए,
संघी-बजरंगी किस्म की राजनीति और विचारधारा की तीखी आलोचना उनकी कहानियों में
है ('जले मकान के कैदी', 'दिव्य दाह') लेकिन उन्हीं आमजनों में, जिनके पक्ष
में मुद्राजी खड़े हैं, इस विचारधारा की स्वीकार्यता उनकी कहानियों को
सामाजिक यथार्थ की उन गहरी परतों तक ले जाती है जहां सभ्यता-समीक्षा एक
अंतःसंघर्ष का अपने आप से जूझने का-रूप-ग्रहण करती है। जाति, वर्ग, जेण्डर की
सामाजिक-सभ्यतात्मक समस्याओं से रूबरू उनकी कहानियों में भी ये गुण मौजूद
हैं। सामाजिक और वैयक्तिक मनोविज्ञान के संधि-देश में स्थित उनकी कहानियों की
संश्लिष्टता और एहसास की जटिलता तो और भी बेजोड़ है।
बहस करने की बजाय मुद्राजी ने अपनी कहानियां सुनायी होती तो हमारी शामें
बेहतर गुजरी होतीं। ऐसा न समझें कि हमारी शामें बेहतर नहीं गुजरी। खूब गुजरी
और खूब गुजरेंगीं। लेकिन कहानियों वाली शामें कभी भी उन निश्शब्द यात्राओं
में नहीं खत्म होतीं जिनमें अशोक मार्ग तक हमारी बोलचाल बंद रही। आप खुश
किस्मत हैं कि उनकी कहानियों से रूबरू हैं।
- रवि सिन्हा
|
|||||