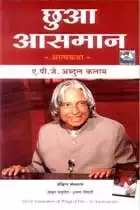|
जीवनी/आत्मकथा >> छुआ आसमान छुआ आसमानए. पी. जे. अब्दुल कलाम
|
410 पाठक हैं |
||||||
छुआ आसमान साहस और विश्वास की एक सशक्त कहानी, और इससे भी ज़्यादा यह स्वतंत्र भारत की विज्ञान और तकनीकी आत्मनिर्भरता की खोज की गाथा है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘‘उनके एकमात्र उत्साहित संदेश से ही उनकी आत्मकथा सैकड़ों मैनेजमेंट पुस्तकों से भी ज़्यादा मूल्यवान है।’’
–द हिन्दु
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा उनके अद्भुत
जीवन का वर्णन करती है : तमिलनाडु स्थित एक छोटे से तीर्थ-गाँव रामेश्वरम् में
नौका-मालिकों के अल्प-शिक्षित परिवार में जन्मा एक बालक, जिसने भारत के
प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल विकास कार्यक्रम की नींव रखी, और जो
हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक-नेता के रूप में उभरा।
छुआ आसमान साहस और विश्वास की एक सशक्त कहानी है, और इससे भी ज़्यादा यह स्वतंत्र भारत की विज्ञान और तकनीकी आत्मनिर्भरता की खोज की गाथा है। साथ ही यह अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा की कहानी भी है।
यह सरल और संक्षिप्त संस्करण डॉ. कलाम की प्रेरक कहानी को सभी पाठकों के लिए उपलब्ध कराएगा। साथ ही अनुवाद में प्रयुक्त तकनीकी एवं अँग्रेज़ी शब्दों के शब्दार्थ उन्हें विस्तार से समझने में सहायक होंगे।
छुआ आसमान साहस और विश्वास की एक सशक्त कहानी है, और इससे भी ज़्यादा यह स्वतंत्र भारत की विज्ञान और तकनीकी आत्मनिर्भरता की खोज की गाथा है। साथ ही यह अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा की कहानी भी है।
यह सरल और संक्षिप्त संस्करण डॉ. कलाम की प्रेरक कहानी को सभी पाठकों के लिए उपलब्ध कराएगा। साथ ही अनुवाद में प्रयुक्त तकनीकी एवं अँग्रेज़ी शब्दों के शब्दार्थ उन्हें विस्तार से समझने में सहायक होंगे।
1. मजबूत नींव
मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में,
द्वीप-नगर
रामेश्वरम् में हुआ। यह 1931 का वर्ष था और रामेश्वरम् ब्रिटिश भारत में
मद्रास (चेन्नई) राज्य का एक भाग था। मैं कई बच्चों में से एक था,
ऊँचे-पूरे एवं सुंदर माता-पिता का छोटे क़द और अपेक्षतया साधारण
चेहरे-मोहरे वाला लड़का।
मेरे पिता जैनुलआबदीन न तो बहुत उच्च-शिक्षित थे और न ही धनी, लेकिन ये कोई बड़ी कमियाँ नहीं थीं, क्योंकि वे बुद्धिमान और वास्तव में एक उदार मन वाले व्यक्ति थे। मेरा माँ आशियम्मा, एक विशिष्ट परिवार से थीं–उनके पूर्वजों में से एक को अँग्रेज़ों ने ‘बहादुर’ की उपाधि प्रदान की थी। वे भी पिता की ही तरह उदारमना थीं–मुझे याद नहीं कि वे रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थीं, लेकिन यह मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे भरे-पूरे परिवार में कुल मिलाकर जितने सदस्य थे, उनसे कहीं अधिक बाहरी लोग हमारे साथ भोजन करते थे ! मेरे माता-पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में सम्मान दिया जाता था। मेरे बचपन भौतिक और भावनात्मक रूप से भी, अत्यंत सुरक्षित था। मेरे पिता अपने सादगीपूर्ण सिद्धांतों के अनुरूप, सीधा-सादा जीवन जीते थे। उनका दिन सुबह की नमाज़ से शुरू होता था, जो वे सूर्योदय से पहले ही अता करते थे। वे ऐश-ओ-आराम की उन चीज़ों से दूर रहते थे, जो उनकी नज़र मैं ग़ैर-ज़रूरी थीं। भोजन, दवाएँ और कपड़े जैसी जीवन की ज़रूरी चीज़ों की कमी नहीं थी। मैं आम तौर पर माँ के साथ रसोईघर के फ़र्श पर बैठकर खाना खाता था। वे मेरे सामने एक केले का पत्ता बिछा देती थीं, जिस पर चावल और मुँह में पानी ला देने वाला गर्मागर्म साँभर, घर में बने हुए अचार और चम्मच-भर ताज़ा नारियल की चटनी परोस देती थीं।
हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो उन्नीसवीं सदी के मध्य में, चूना-पत्थर और ईंटों से बना था। यह मकान काफी बड़ा था और रामेश्वरम् में मस्जिद वाली गली में स्थित था। प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम् एक पवित्र तीर्थ-स्थल बना, हमारे घर से लगभग दस मिनट की पैदल-दूरी पर था। हमारा मुहल्ला मुस्लिम-बहुल था और इसका मस्जिद वाली गली नाम, यहाँ की एक बहुत पुरानी मस्जिद पर रखा गया था। मुहल्ले में दोनों धर्मों के पूजा-स्थल अग़ल-बग़ल होने की वजह से हिंदू-मुस्लिम बड़े प्यार से, पड़ोसियों की तरह मिल-जुलकर रहते थे।
मंदिर के बड़े पुजारी पक्षि लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की सबसे ताज़ा याद मुझे इन दोनों की है। दोनों अपने पारंपरिक पहनावे में आध्यात्मिक चर्चाएँ करते रहते थे। दोनों की सोच में समानता उनके भजन-पूजन के रीति-रिवाज की भिन्नता से कहीं ऊपर थी।
बचपन में, मेरे पिता मुझे अपने साथ शाम की नमाज़ के लिए मस्जिद ले जाते थे। ज़रा भी भाव और अर्थ जाने बग़ैर मैं अरबी में अता की जाने वाली नमाज़ सुनता रहता था। लेकिन मैं इतना समझता था कि ये नमाज़ें ईश्वर तक पहुँचती हैं। जब मैं सवाल करने लायक़ हुआ, तो मैंने पिताजी से नमाज़ के बारे में और ख़ुदा से संवाद बनाने में इसकी प्रासंगिकता के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे समझाया कि नमाज़ में रहस्य और पेचीदगी जैसा कुछ भी नहीं है।
‘जब तुम नमाज़ पढ़ते हो’, उन्होंने कहा–‘तुम शरीर और उसके सांसारिक जुड़ाव से परे पहुँच जाते हो। तुम उस ब्रह्माण्ड का एक हिस्सा बन जाते हो, जहाँ धन-दौलत, उम्र, जाति और नस्ल लोगों में फ़र्क करने के पैमाने नहीं होते।’
अक्सर, नमाज़ के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से निकलते, तो विभिन्न धर्मों के लोग उनके इंतज़ार में बाहर बैठे मिलते थे। उनमें से कई लोग पानी के कटोरे उनके आगे कर देते कि वे अपनी उँगलियाँ उनमें डालकर दुआ पढ़ दें। इसके बाद यह पानी घर ले जाकर मरीज़ों को दिया जाता। मुझे यह भी याद है कि फिर लोग मरीज़ के स्वस्थ होने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे घर आते थे, लेकिन वे अपने सहज अंदाज़ में अल्लाह का शुक्रिया करने को कहते, जो सबका भला करने वाला और दयालु है।
वे जटिल आध्यात्मिक बातों को भी इतनी सरल भाषा में समझाते थे कि मेरे जैसा छोटा बच्चा भी उन्हें समझ सकता था। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि हर एक इंसान अपने ख़ुद के वक़्त, जगह और हालत में–वह अच्छी हो या बुरी–दैवी शक्ति का हिस्सा बन जाता है, जिसे हम ख़ुदा कहते हैं। दुख-तकलीफ़ें हमें सबक़ देने और अति-आनंद तथा अहंकार की स्थिति से बाहर निकालने के लिए झटका देने आती हैं।
मैंने पिताजी से पूछा, ‘आप ये सब बातें उन लोगों को क्यों नहीं बताते, जो आपके पास मदद और सलाह माँगने आते हैं ?’ कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे यह जाँच रहे हों कि मैं किस हद तक उनकी बात समझने में सक्षम हूँ। जब उन्होंने उत्तर दिया, तो वह बड़े धीमे और शांत स्वर में था और उनके शब्दों में मैंने ख़ुद को ग़ज़ब की शक्ति से भरा महसूस किया।
उन्होंने कहा कि इंसान जब कभी भी अपने-आप को एकदम अकेला या हताश पाता है, तो उसे किसी तरह की मदद और दिलासे के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। हर एक दुःख या इच्छा, दर्द या उम्मीद एक ख़ास मददगार पा ही लेते हैं। मेरे पिता ख़ुद को केवल एक ऐसा मददगार, एक ऐसा मध्यस्थ मानते थे, जो नमाज़, इबादत या मन्नतों की ताक़त का इस्तेमाल शैतान, आत्मनाशी ताक़तों को हराने के लिए करता है। लेकिन वे मानते थे कि दिक़्क़तें सुलझाने का यह तरीक़ा ग़लत है, क्योंकि इस तरह की प्रार्थना डर से पैदा होती है। उनका मानना था कि व्यक्ति का प्रारब्ध ख़ुद के वास्तविक ज्ञान से उपजी दृष्टि होना चाहिए। डर अक्सर व्यक्ति की उम्मीदों को पूरा होने से रोक देता है। उन्हें सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि वाक़ई मैं किस्मत वाला इंसान हूँ, जिसे उन्होंने यह सब समझाया।
मैं अपने पिता के दर्शन से बेहद प्रभावित था। आज मैं यक़ीन करता हूँ और जब बच्चा था, तब भी करता था कि जब कोई व्यक्ति उन भावनात्मक रिश्तों से मुक्त हो जाता है, जो उसकी राह रोकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता की राहें सिर्फ एक छोटे से क़दम की दूरी पर रह जाती हैं। दिमाग़ी शांति और ख़ुशी हमें ख़ुद के भीतर ही मिलती है, न कि किसी बाहरी तरीक़े से। जब एक इंसान इस सच को समझ जाता है, तो उसके लिए असफलताएँ और बाधाएँ अस्थायी बन जाती हैं।
मैं बहुत छोटा था–सिर्फ़ छह साल का–जब मैंने पिताजी को अपना फ़लसफ़ा ज़िंदगी में उतारते देखा। उन्होंने तीर्थ-यात्रियों को रामेश्वरम् से धनुषकोडि ले जाने और वापस लाने के लिए एक नाव बनाने का फ़ैसला किया। मैंने लकड़ी की इस नाव को समुद्र तट पर आकार लेते देखा। लकड़ी को आग पर तपाकर नाव का पेंदा और बाहरी दीवारें बनाने के लिए तैयार किया गया था। नाव को आकार लेते देखना वाक़ई बड़ी सम्मोहक था।
जब नाव बनकर तैयार हुई, तो पिताजी ने बड़ी ख़ुशी-ख़ुशी धंधा शुरू किया। कुछ समय बाद रामेश्वरम् तट पर एक भयंकर चक्रवात आया। तुफ़ानी हवाओं में हमारी नाव टूट गई। पिताजी ने अपना नुक़सान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया–हक़ीक़त में वे तूफ़ान के कारण घटित एक बड़ी त्रासदी को लेकर ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि, चक्रवार्ती तूफ़ान में पामबान पुल उस वक़्त ढह गया था, जब यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी उसके ऊपर से गुज़र रही थी।
मैंने अपने पिताजी के नज़रिए और असली तबाही, दोनों से काफ़ी कुछ सीखा। तब तक मैंने समुद्र की सिर्फ़ सुंदरता ही देखी थी। अब इसकी ता़क़त और अनियंत्रित ऊर्जा भी प्रकट हो गई।
मेरे पिता जैनुलआबदीन न तो बहुत उच्च-शिक्षित थे और न ही धनी, लेकिन ये कोई बड़ी कमियाँ नहीं थीं, क्योंकि वे बुद्धिमान और वास्तव में एक उदार मन वाले व्यक्ति थे। मेरा माँ आशियम्मा, एक विशिष्ट परिवार से थीं–उनके पूर्वजों में से एक को अँग्रेज़ों ने ‘बहादुर’ की उपाधि प्रदान की थी। वे भी पिता की ही तरह उदारमना थीं–मुझे याद नहीं कि वे रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थीं, लेकिन यह मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे भरे-पूरे परिवार में कुल मिलाकर जितने सदस्य थे, उनसे कहीं अधिक बाहरी लोग हमारे साथ भोजन करते थे ! मेरे माता-पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में सम्मान दिया जाता था। मेरे बचपन भौतिक और भावनात्मक रूप से भी, अत्यंत सुरक्षित था। मेरे पिता अपने सादगीपूर्ण सिद्धांतों के अनुरूप, सीधा-सादा जीवन जीते थे। उनका दिन सुबह की नमाज़ से शुरू होता था, जो वे सूर्योदय से पहले ही अता करते थे। वे ऐश-ओ-आराम की उन चीज़ों से दूर रहते थे, जो उनकी नज़र मैं ग़ैर-ज़रूरी थीं। भोजन, दवाएँ और कपड़े जैसी जीवन की ज़रूरी चीज़ों की कमी नहीं थी। मैं आम तौर पर माँ के साथ रसोईघर के फ़र्श पर बैठकर खाना खाता था। वे मेरे सामने एक केले का पत्ता बिछा देती थीं, जिस पर चावल और मुँह में पानी ला देने वाला गर्मागर्म साँभर, घर में बने हुए अचार और चम्मच-भर ताज़ा नारियल की चटनी परोस देती थीं।
हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो उन्नीसवीं सदी के मध्य में, चूना-पत्थर और ईंटों से बना था। यह मकान काफी बड़ा था और रामेश्वरम् में मस्जिद वाली गली में स्थित था। प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम् एक पवित्र तीर्थ-स्थल बना, हमारे घर से लगभग दस मिनट की पैदल-दूरी पर था। हमारा मुहल्ला मुस्लिम-बहुल था और इसका मस्जिद वाली गली नाम, यहाँ की एक बहुत पुरानी मस्जिद पर रखा गया था। मुहल्ले में दोनों धर्मों के पूजा-स्थल अग़ल-बग़ल होने की वजह से हिंदू-मुस्लिम बड़े प्यार से, पड़ोसियों की तरह मिल-जुलकर रहते थे।
मंदिर के बड़े पुजारी पक्षि लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की सबसे ताज़ा याद मुझे इन दोनों की है। दोनों अपने पारंपरिक पहनावे में आध्यात्मिक चर्चाएँ करते रहते थे। दोनों की सोच में समानता उनके भजन-पूजन के रीति-रिवाज की भिन्नता से कहीं ऊपर थी।
बचपन में, मेरे पिता मुझे अपने साथ शाम की नमाज़ के लिए मस्जिद ले जाते थे। ज़रा भी भाव और अर्थ जाने बग़ैर मैं अरबी में अता की जाने वाली नमाज़ सुनता रहता था। लेकिन मैं इतना समझता था कि ये नमाज़ें ईश्वर तक पहुँचती हैं। जब मैं सवाल करने लायक़ हुआ, तो मैंने पिताजी से नमाज़ के बारे में और ख़ुदा से संवाद बनाने में इसकी प्रासंगिकता के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे समझाया कि नमाज़ में रहस्य और पेचीदगी जैसा कुछ भी नहीं है।
‘जब तुम नमाज़ पढ़ते हो’, उन्होंने कहा–‘तुम शरीर और उसके सांसारिक जुड़ाव से परे पहुँच जाते हो। तुम उस ब्रह्माण्ड का एक हिस्सा बन जाते हो, जहाँ धन-दौलत, उम्र, जाति और नस्ल लोगों में फ़र्क करने के पैमाने नहीं होते।’
अक्सर, नमाज़ के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से निकलते, तो विभिन्न धर्मों के लोग उनके इंतज़ार में बाहर बैठे मिलते थे। उनमें से कई लोग पानी के कटोरे उनके आगे कर देते कि वे अपनी उँगलियाँ उनमें डालकर दुआ पढ़ दें। इसके बाद यह पानी घर ले जाकर मरीज़ों को दिया जाता। मुझे यह भी याद है कि फिर लोग मरीज़ के स्वस्थ होने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे घर आते थे, लेकिन वे अपने सहज अंदाज़ में अल्लाह का शुक्रिया करने को कहते, जो सबका भला करने वाला और दयालु है।
वे जटिल आध्यात्मिक बातों को भी इतनी सरल भाषा में समझाते थे कि मेरे जैसा छोटा बच्चा भी उन्हें समझ सकता था। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि हर एक इंसान अपने ख़ुद के वक़्त, जगह और हालत में–वह अच्छी हो या बुरी–दैवी शक्ति का हिस्सा बन जाता है, जिसे हम ख़ुदा कहते हैं। दुख-तकलीफ़ें हमें सबक़ देने और अति-आनंद तथा अहंकार की स्थिति से बाहर निकालने के लिए झटका देने आती हैं।
मैंने पिताजी से पूछा, ‘आप ये सब बातें उन लोगों को क्यों नहीं बताते, जो आपके पास मदद और सलाह माँगने आते हैं ?’ कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे यह जाँच रहे हों कि मैं किस हद तक उनकी बात समझने में सक्षम हूँ। जब उन्होंने उत्तर दिया, तो वह बड़े धीमे और शांत स्वर में था और उनके शब्दों में मैंने ख़ुद को ग़ज़ब की शक्ति से भरा महसूस किया।
उन्होंने कहा कि इंसान जब कभी भी अपने-आप को एकदम अकेला या हताश पाता है, तो उसे किसी तरह की मदद और दिलासे के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। हर एक दुःख या इच्छा, दर्द या उम्मीद एक ख़ास मददगार पा ही लेते हैं। मेरे पिता ख़ुद को केवल एक ऐसा मददगार, एक ऐसा मध्यस्थ मानते थे, जो नमाज़, इबादत या मन्नतों की ताक़त का इस्तेमाल शैतान, आत्मनाशी ताक़तों को हराने के लिए करता है। लेकिन वे मानते थे कि दिक़्क़तें सुलझाने का यह तरीक़ा ग़लत है, क्योंकि इस तरह की प्रार्थना डर से पैदा होती है। उनका मानना था कि व्यक्ति का प्रारब्ध ख़ुद के वास्तविक ज्ञान से उपजी दृष्टि होना चाहिए। डर अक्सर व्यक्ति की उम्मीदों को पूरा होने से रोक देता है। उन्हें सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि वाक़ई मैं किस्मत वाला इंसान हूँ, जिसे उन्होंने यह सब समझाया।
मैं अपने पिता के दर्शन से बेहद प्रभावित था। आज मैं यक़ीन करता हूँ और जब बच्चा था, तब भी करता था कि जब कोई व्यक्ति उन भावनात्मक रिश्तों से मुक्त हो जाता है, जो उसकी राह रोकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता की राहें सिर्फ एक छोटे से क़दम की दूरी पर रह जाती हैं। दिमाग़ी शांति और ख़ुशी हमें ख़ुद के भीतर ही मिलती है, न कि किसी बाहरी तरीक़े से। जब एक इंसान इस सच को समझ जाता है, तो उसके लिए असफलताएँ और बाधाएँ अस्थायी बन जाती हैं।
मैं बहुत छोटा था–सिर्फ़ छह साल का–जब मैंने पिताजी को अपना फ़लसफ़ा ज़िंदगी में उतारते देखा। उन्होंने तीर्थ-यात्रियों को रामेश्वरम् से धनुषकोडि ले जाने और वापस लाने के लिए एक नाव बनाने का फ़ैसला किया। मैंने लकड़ी की इस नाव को समुद्र तट पर आकार लेते देखा। लकड़ी को आग पर तपाकर नाव का पेंदा और बाहरी दीवारें बनाने के लिए तैयार किया गया था। नाव को आकार लेते देखना वाक़ई बड़ी सम्मोहक था।
जब नाव बनकर तैयार हुई, तो पिताजी ने बड़ी ख़ुशी-ख़ुशी धंधा शुरू किया। कुछ समय बाद रामेश्वरम् तट पर एक भयंकर चक्रवात आया। तुफ़ानी हवाओं में हमारी नाव टूट गई। पिताजी ने अपना नुक़सान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया–हक़ीक़त में वे तूफ़ान के कारण घटित एक बड़ी त्रासदी को लेकर ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि, चक्रवार्ती तूफ़ान में पामबान पुल उस वक़्त ढह गया था, जब यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी उसके ऊपर से गुज़र रही थी।
मैंने अपने पिताजी के नज़रिए और असली तबाही, दोनों से काफ़ी कुछ सीखा। तब तक मैंने समुद्र की सिर्फ़ सुंदरता ही देखी थी। अब इसकी ता़क़त और अनियंत्रित ऊर्जा भी प्रकट हो गई।
2. शुरुआती असर
हमारे एक रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन ने नाव
बनाते वक़्त
पिताजी की काफ़ी मदद की थी। बाद में, उन्होंने मेरी बहन ज़ोहरा से निकाह
कर लिया। नाव बनाने और उसके समुद्र में चलने के दौरान ज़्यादातर समय
साथ-साथ रहने से मैं और जलालुद्दीन उम्र के बड़े फ़ासले के बावजूद अच्छे
दोस्त बन गए थे। वे मुझसे पंद्रह साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहते थे।
हर शाम हम दोनों साथ-साथ दूर घूमने निकल जाते थे। आमतौर पर हम आध्यात्मिक मुद्दों पर बात करते थे। इस विषय में संभवतः रामेश्वरम् के महौल ने हमारी रुचि बढ़ाई थी, जहाँ रोज़ाना असंख्य तीर्थ-यात्री इबादत करने आते हैं। हमारी पहली नज़र अक्सर विशाल, भव्य शिव मंदिर पर पड़ती थी। हम उतनी श्रद्धा से ही मंदिर की परिक्रमा करते थे, जितनी कि दूर-दराज़ जगहों से आने वाले यात्री करते थे।
मुझे लगता था कि जलालुद्दीन ख़ुदा से सीधे संवाद करने में समर्थ थे, तक़रीबन इस तरह, जैसे वे दोनों साथ-साथ काम करने वाले जोड़ीदार हों। वे ख़ुदा से अपनी तमाम शंकाओं के बारे में ऐसे बात करते थे, जैसे कि वे ठीक उनके बाज़ू में खड़े हों और सुन रहे हों। मैंने संवाद का यह तरीक़ा अद्भुत पाया। मैं समुद्र में डुबकी लगाकर अपनी प्राचीन प्रार्थनाएँ उच्चारित करते और पारंपरिक संस्कार पूरे करते तीर्थ-यात्रियों को भी ग़ौर से देखा करता था। एक अज्ञात और अदृश्य शक्ति के प्रति सम्मान का भाव–उनमें और जलालुद्दीन में, साफ़ दिखाई देता था।
जलालुद्दीन स्कूली शिक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि उनका परिवार शिक्षा का ख़र्च उठाने में असमर्थ था। शायद यही कारण था कि वे हमेशा मुझे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे और मेरी सफलताओं से बेहद ख़ुशी महसूस करते थे। प्रसंगवश, उस ज़माने में पूरे टापू में जलालुद्दीन अकेले आदमी थे, जो अँग्रेज़ी में लिख सकते थे। वे हर उस व्यक्ति के लिए पत्र लिखते थे, जिसे ज़रूरत होती थी–अर्ज़ी, कामकाजी या निजी ख़त। आसपास के इलाक़े में बहुत कम लोग ही थे, जो हमारे छोटे से क़स्बे से बाहर की दुनिया की जानकारी या ज्ञान में उनकी बराबरी पर आते हों।
ज़िंदगी के उस पड़ाव पर जलालुद्दीन ने मुझ पर गहरा असर डाला। वे मुझसे तमाम विषयों पर बात करते थे–वैज्ञानिक खोजें, समकालीन लेखन और साहित्य यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान और उसकी नई उपलब्धियों के बारे में भी। वे ही थे, जिन्होंने अपने सीमित संसार से बाहर की दुनिया की ओर देख पाने में मेरी सबसे ज़्यादा मदद की।
उस वक़्त मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू था अध्ययन से बढ़ता लगाव, यानी वह आदत, जो ताउम्र मेरे साथ बनी रही है। हमारे जैसी घरेलू जीवन शैली में किताबें दुर्लभ थीं और मुश्किल से ही मिल पाती थीं–सिवाय एस.टी.आर. मानिकम के विशाल निजी पुस्तकालय के। मानिकम एक उग्र राष्ट्रवादी थे, जो अहिंसा के गाँधीवादी तरीक़े से इतर साधनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। मैं अक्सर किताबें उधार लेने के लिए उनके घर जाया करता था। वे मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक और शख़्स भी थे, जिन्होंने मेरे बचपन को गढ़ने में सहायता की–मेरे चचेरे भाई, शम्सुद्दीन। उस वक़्त रामेश्वरम् में वे अकेले अख़बार वितरक थे। पामबान से सुबह आने वाली ट्रेन रामेश्वरम् के पाठकों के लिए तमिल अख़बार लेकर आती थी। उन दिनों अख़बार आज़ादी की लड़ाई के ताज़ा-तरीन हालात की जानकारी से पटे पड़े रहते थे, जिनमें ज़्यादातर पाठक गहरी रुचि लेते थे।
हर शाम हम दोनों साथ-साथ दूर घूमने निकल जाते थे। आमतौर पर हम आध्यात्मिक मुद्दों पर बात करते थे। इस विषय में संभवतः रामेश्वरम् के महौल ने हमारी रुचि बढ़ाई थी, जहाँ रोज़ाना असंख्य तीर्थ-यात्री इबादत करने आते हैं। हमारी पहली नज़र अक्सर विशाल, भव्य शिव मंदिर पर पड़ती थी। हम उतनी श्रद्धा से ही मंदिर की परिक्रमा करते थे, जितनी कि दूर-दराज़ जगहों से आने वाले यात्री करते थे।
मुझे लगता था कि जलालुद्दीन ख़ुदा से सीधे संवाद करने में समर्थ थे, तक़रीबन इस तरह, जैसे वे दोनों साथ-साथ काम करने वाले जोड़ीदार हों। वे ख़ुदा से अपनी तमाम शंकाओं के बारे में ऐसे बात करते थे, जैसे कि वे ठीक उनके बाज़ू में खड़े हों और सुन रहे हों। मैंने संवाद का यह तरीक़ा अद्भुत पाया। मैं समुद्र में डुबकी लगाकर अपनी प्राचीन प्रार्थनाएँ उच्चारित करते और पारंपरिक संस्कार पूरे करते तीर्थ-यात्रियों को भी ग़ौर से देखा करता था। एक अज्ञात और अदृश्य शक्ति के प्रति सम्मान का भाव–उनमें और जलालुद्दीन में, साफ़ दिखाई देता था।
जलालुद्दीन स्कूली शिक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि उनका परिवार शिक्षा का ख़र्च उठाने में असमर्थ था। शायद यही कारण था कि वे हमेशा मुझे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे और मेरी सफलताओं से बेहद ख़ुशी महसूस करते थे। प्रसंगवश, उस ज़माने में पूरे टापू में जलालुद्दीन अकेले आदमी थे, जो अँग्रेज़ी में लिख सकते थे। वे हर उस व्यक्ति के लिए पत्र लिखते थे, जिसे ज़रूरत होती थी–अर्ज़ी, कामकाजी या निजी ख़त। आसपास के इलाक़े में बहुत कम लोग ही थे, जो हमारे छोटे से क़स्बे से बाहर की दुनिया की जानकारी या ज्ञान में उनकी बराबरी पर आते हों।
ज़िंदगी के उस पड़ाव पर जलालुद्दीन ने मुझ पर गहरा असर डाला। वे मुझसे तमाम विषयों पर बात करते थे–वैज्ञानिक खोजें, समकालीन लेखन और साहित्य यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान और उसकी नई उपलब्धियों के बारे में भी। वे ही थे, जिन्होंने अपने सीमित संसार से बाहर की दुनिया की ओर देख पाने में मेरी सबसे ज़्यादा मदद की।
उस वक़्त मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू था अध्ययन से बढ़ता लगाव, यानी वह आदत, जो ताउम्र मेरे साथ बनी रही है। हमारे जैसी घरेलू जीवन शैली में किताबें दुर्लभ थीं और मुश्किल से ही मिल पाती थीं–सिवाय एस.टी.आर. मानिकम के विशाल निजी पुस्तकालय के। मानिकम एक उग्र राष्ट्रवादी थे, जो अहिंसा के गाँधीवादी तरीक़े से इतर साधनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। मैं अक्सर किताबें उधार लेने के लिए उनके घर जाया करता था। वे मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक और शख़्स भी थे, जिन्होंने मेरे बचपन को गढ़ने में सहायता की–मेरे चचेरे भाई, शम्सुद्दीन। उस वक़्त रामेश्वरम् में वे अकेले अख़बार वितरक थे। पामबान से सुबह आने वाली ट्रेन रामेश्वरम् के पाठकों के लिए तमिल अख़बार लेकर आती थी। उन दिनों अख़बार आज़ादी की लड़ाई के ताज़ा-तरीन हालात की जानकारी से पटे पड़े रहते थे, जिनमें ज़्यादातर पाठक गहरी रुचि लेते थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book