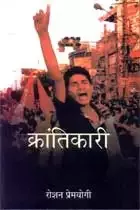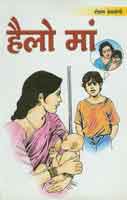|
उपन्यास >> क्रांतिकारी क्रांतिकारीरोशन प्रेमयोगी
|
330 पाठक हैं |
||||||
क्रांतिकारी में इक्कीसवीं सदी का गाँव, दलित उभार और जातीय संघर्ष है। यह पूरी तरह युवाओं का उपन्यास है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘क्रांतिकारी’ में इक्कीसवीं सदी का गाँव, दलित उभार
और जातीय संघर्ष है। इसलिए इसे मैं मुंशी प्रेमचंद के
‘गोदान’ से आगे की रचना कहना चाहूँगा। यह पूरी तरह से
युवाओं का उपन्यास है, जिसमें लड़कियों को महत्त्व नहीं दिया गया है।
संध्या को चंद्रशेखर के प्यार में पागल दिखाया गया है। पोस्टग्रेजुएट माला
को भी लेखक ने गृहिणी से ऊपर नहीं उठने दिया है। परंतु यह नहीं कहा जा
सकता कि यह पुरुष-प्रधान उपन्यास है। अनपढ़ सुन्नरी देवी, राजेश्वरी देवी
और शारदा देवी का रोल छोटा जरूर है, लेकिन वे अन्य सभी पात्रों पर भारी
पड़ती हैं। तीन दोस्त सामाजिक संघर्ष की अलख ही जगाते रह जाते हैं और
सुन्नरी देवी राजेंद्रनाथ के साथ मिलकर क्रांति की सूत्रधार बन जाती हैं।
–स्व. डॉ. रमाशंकर तिवारी
दलित समाज की संवेदना, उत्पीड़न, समाजिक-आर्थिक दशा तथा उनके संघर्षों पर
केंद्रित ‘क्रांतिकारी’ की स्क्रिप्ट पढ़ते समय मुझे
अपनी पुलिस कप्तानी के दौर की बहुत याद आई। दलितों पर होने वाले जिस तरह
के अत्याचारों को मैंने देखा और अफसर होने के नाते जिनका निदान ढूँढ़ने का
अथक प्रयास किया, उसी तरह के संघर्ष और उत्पीड़न की कथा इस उपन्यास में भी
है। इसके कुछ सवर्ण पात्र दलितों के पक्ष में खड़े हैं। उनका संघर्ष नकली
नहीं लगता। दो सवर्ण और एक दलित युवक मिलकर अपने गाँव-क्षेत्र की राजनीति
बदल देते हैं।
–जंगी सिंह
दलित परिवार में जन्म लेने के कारण सामाजिक अस्पृश्यता और उत्पीड़न का दंश
मैंने भी सहा है, इसलिए ‘क्रांतिकारी’ को पढ़ते हुए
यह सवाल मेरे मन में कई बार उठा कि जिस तरह इस उपन्यास में चंद्रशेखर और
केवलानंद जैसे सचेत सवर्ण लड़के दलित रामकरन के साथ खड़े हैं, मेरे साथ
क्यों नहीं खड़े हुए ?
चंद्रशेखर मुख्य पात्र है, जो चाहता है कि हमारे इलाके के गाँवों में दलितों का जीवन-स्तर ऊँचा उठे, वे संगठित हों और बराबरी पर आने के लिए लड़ें। उसके संघर्षों को याद करते ही मेरे शरीर में झुरझुरी-सी होने लगती है। दलितों की लड़ाई में वह अपना एक हाथ गँवा बैठता है। अंत में उसके विचारी की विजय होती है। विजय इस तरह कि दे मेधावी युवा अपने-अपने गाँव यह सोचकर आए थे कि यहीं पर रोजगार करेंगे और अपने साथ दलित समाज का भी जीवन-स्तर ऊँचा उठाएँगे। उनकी राह में क्षेत्रीय विधायक काँटा बोते हैं, इसलिए कि यदि रामकरन जैसे हरिजन दलितों के सर्वमान्य नेता बन जाएँगे तो हम सवर्णों का वोट बैंक टूट जाएगा। उधर चंद्रशेखर और रामकरन मिलकर दलितों को यह अहसास कराते हैं कि यदि संगठित और शिक्षित बनोगे तो कोई भी तुम्हारा उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। मछली शहर के निकट मेरे गाँव में कोई भी सवर्ण हम दलितों के घर की चाय नहीं पीता, जबकि इस उपन्यास में दलित रामकरन ब्राह्मणों के घर हवन-पूजन करवाता है।
ईशावस्या, माला और संध्या जैसे स्त्री-पात्र को उपन्यास में महत्त्व नहीं मिली है, लेकिन सबकी कमी पूरी कर देती है सुन्नरी देवी। उनका संघर्ष समूची दलित स्त्री जाति का संघर्ष है। वे किसी देवी की तरह समाजियों का नेतृत्व सँभालती हैं। दरअसल दलित क्रांति की मशक्कत तीन युवा मिलकर करते हैं, लेकिन जब क्रांति होती है तो वे युवा पीछे रह जाते हैं और सुन्नरी देवी विजय का परचम लहरा देती हैं।
चंद्रशेखर मुख्य पात्र है, जो चाहता है कि हमारे इलाके के गाँवों में दलितों का जीवन-स्तर ऊँचा उठे, वे संगठित हों और बराबरी पर आने के लिए लड़ें। उसके संघर्षों को याद करते ही मेरे शरीर में झुरझुरी-सी होने लगती है। दलितों की लड़ाई में वह अपना एक हाथ गँवा बैठता है। अंत में उसके विचारी की विजय होती है। विजय इस तरह कि दे मेधावी युवा अपने-अपने गाँव यह सोचकर आए थे कि यहीं पर रोजगार करेंगे और अपने साथ दलित समाज का भी जीवन-स्तर ऊँचा उठाएँगे। उनकी राह में क्षेत्रीय विधायक काँटा बोते हैं, इसलिए कि यदि रामकरन जैसे हरिजन दलितों के सर्वमान्य नेता बन जाएँगे तो हम सवर्णों का वोट बैंक टूट जाएगा। उधर चंद्रशेखर और रामकरन मिलकर दलितों को यह अहसास कराते हैं कि यदि संगठित और शिक्षित बनोगे तो कोई भी तुम्हारा उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। मछली शहर के निकट मेरे गाँव में कोई भी सवर्ण हम दलितों के घर की चाय नहीं पीता, जबकि इस उपन्यास में दलित रामकरन ब्राह्मणों के घर हवन-पूजन करवाता है।
ईशावस्या, माला और संध्या जैसे स्त्री-पात्र को उपन्यास में महत्त्व नहीं मिली है, लेकिन सबकी कमी पूरी कर देती है सुन्नरी देवी। उनका संघर्ष समूची दलित स्त्री जाति का संघर्ष है। वे किसी देवी की तरह समाजियों का नेतृत्व सँभालती हैं। दरअसल दलित क्रांति की मशक्कत तीन युवा मिलकर करते हैं, लेकिन जब क्रांति होती है तो वे युवा पीछे रह जाते हैं और सुन्नरी देवी विजय का परचम लहरा देती हैं।
–डॉ.चंदन भारती
क्रांतिकारी
तुम घरों में लगाते हो ताले
फिर क्यों चाहते हो
हम जुबान पर लगाएँ ?
तुम खाते हो गेहूँ की रोटी, अरहर की दाल
फिर क्यों चाहते हो
हम सावाँ-कोदौ-करेमुआ के साग पर जिंदगी बिताएँ ?
तुम पढ़ते हो वेद-पुराण-रामायण
फिर क्यों चाहते हो
हम अक्षर को भैंस मान जाएँ ?
तुम देते हो अर्घ्य, मिलाते हो सूर्य से आँखें
फिर क्यों चाहते हो
हम तुम्हारी परछाईं देख दुबक जाएँ ?
तुम्हारे घरों में हैं पीतल-सोने के हत्थों वाले सिंहासन
फिर क्यों चाहते हो
हम मचिया-बिड़वा-पीढ़े पर भी न बैठने पाएँ ?
ऐ स्वतंत्र भारत के सवर्णो !
15 अगस्त, 1947 को
स्वतंत्रता हमें भी मिली है
अब भारत पर मनुस्मृति नहीं
अंबेडकर के संविधान का राज है
त्याग दो उच्चता का अहंकार
आओ मानवता की बात करें !
फिर क्यों चाहते हो
हम जुबान पर लगाएँ ?
तुम खाते हो गेहूँ की रोटी, अरहर की दाल
फिर क्यों चाहते हो
हम सावाँ-कोदौ-करेमुआ के साग पर जिंदगी बिताएँ ?
तुम पढ़ते हो वेद-पुराण-रामायण
फिर क्यों चाहते हो
हम अक्षर को भैंस मान जाएँ ?
तुम देते हो अर्घ्य, मिलाते हो सूर्य से आँखें
फिर क्यों चाहते हो
हम तुम्हारी परछाईं देख दुबक जाएँ ?
तुम्हारे घरों में हैं पीतल-सोने के हत्थों वाले सिंहासन
फिर क्यों चाहते हो
हम मचिया-बिड़वा-पीढ़े पर भी न बैठने पाएँ ?
ऐ स्वतंत्र भारत के सवर्णो !
15 अगस्त, 1947 को
स्वतंत्रता हमें भी मिली है
अब भारत पर मनुस्मृति नहीं
अंबेडकर के संविधान का राज है
त्याग दो उच्चता का अहंकार
आओ मानवता की बात करें !
ट्रिन-ट्रिन-ट्रिन-ट्रिन...नऽऽ नऽऽ...ट्रिनऽऽ
‘‘श्रीमान् जी ! अभी सात मिनट पूरे कहाँ हुए हैं ?’’
‘‘मंच से नीचे जाओ, रामकरन ! सांप्रदायिकता और वर्ग-संघर्ष फैलाने वाली कविता पढ़नी है तो बसपा जैसी कोई पार्टी ज्वॉइन कर लो। चलो, नीचे जाओ। रोवर्स ! रेंजर्स ! अपने साथी के लिए तालियाँ बजा दीजिए।’’ मंच संचालन कर रहे स्काउट एंड गाइड्स शिविर के अधिकारी डॉ. दयानंद मिश्र तिरछी दृष्टि से रामकरन को देखते हैं।
‘‘ताली क्यों, विसिल न बजा दें ?’’ अगली पंक्ति में बैठे छात्र भीम सिंह ने अनुमति चाही।
‘‘विसिल क्यों, ऐसे घटिया कविता पर तो हूटिंग होनी चाहिए।’’ दूसरे छात्र ने जोड़ा।
इसके बाद तो सीटियाँ, तालियाँ और नाक एक साथ बजने लगती हैं, दर्जनों छात्र व्यंग्य-बाण छोड़ते हुए उद्दंडता पर उतारू। मुख्य अतिथि कुलपति डॉ. राजदेव पांडेय तथा दूसरे प्राध्यापक लड़कियों की तरह एक चुप हजार चुप।
रामकरन अब भी मंच पर खड़ा है, इस उम्मीद में कि कुलपति उसका साथ देंगे। वह कभी मंच पर उपस्थित गण्यमान्यों को देखता है तो कभी उद्दंडता कर रहे छात्रों की ओर। उसे आश्चर्य होता है कि कक्षा के कई सहपाठी भी खिल्ली उड़ाने और अपशब्द कहने वालों में सम्मिलित हैं। शिविर अधिकारी पुनः मंच से उतरने के लिए कहते हैं तो निराशा-मिश्रित आक्रोश ओढ़कर रामकरन नीचे की ओर कदम बढ़ाता है। उतर पाता उससे पहले ही एक सुदर्शन युवक बुलंद आवाज में चेतावनी देता है, ‘‘माइक पर वापस जाओ, रामकरन ! पूरी कविता पढ़े बिना नीचे उतरे तो तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा।’’
सारे स्टाउट्स व अतिथिगण मेज पर चढ़ गए उस युवक की ओर देखते हैं। वह दाँत पीसते हुए मंच संचालक की ओर रुख करता है, ‘‘डॉ. दयानंद जी। ! क्रांति की बात कभी राजनीतिक मंच से नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर ज्यादातर थके-बूढ़े-कुंठित-कूपमंडूप नेताओं का कब्जा है। यहाँ युवा शक्ति उपस्थित है, गुरुजन भी हैं, इसलिए यह मंच सबसे उपयुक्त है। कविता पढ़ो, रामकरन ! हम सुनने के लिए तैयार हैं, ताली भी बजाएँगे, जिसे न सुनना हो वह खिसक ले।’’
डॉ. दयानंद और उनके सहयोगी असहाय। छात्रों में बाता-कही शुरू हो जाती है। आश्चर्य ! लड़कियाँ फिर भी बैठी रहती हैं। कूद-फाँद करते हुए आगे आ पहुँचा एक युवक चिघाड़ता है, ‘‘माइक पर वापस जाओ राम !’’
‘‘यह तुम्हारा नहीं, पूर्वांचल का अपमान है, रामकरन ! चंद्रशेखर भइया का मैं भी समर्थन करता हूँ।’’ यह आवाज केवलानंद द्विवेदी की होती है तो अब चंद्रशेखर की बगल में खड़ा है।
‘‘यह अकोढ़ी की चमरउटिया नहीं है, चंद्रशेखर ! हम नहीं सुनना चाहते रामकरन की कविता।’’ दीपक नाम का युवक खुला विरोध करता है।
‘‘हम नहीं, मैं कहो, दीपक !’’ चंद्रशेखर उसकी ओर उँगली उठाता है।
‘‘कुचकुचवा की तरह घूर क्या रहे हो, नहीं सुनना है तो बाहर चले जाओ।’’ केवलानंद सिताररूपी चंद्रशेखर का तानपूरा लगता है।
‘‘तुम दोनों जाओ, हम सब नहीं सुनना चाहते।’’ लगभग सभी छात्र खड़े हो जाते हैं।
‘‘तो सारे चले जाओ बाहर। कविता पूरी हो जाने के बाद अंदर आ जाना।’’ चंद्रशेखर सहजता का परिचय देता है।
‘‘भइया जी ! जाने दीजिए, अब मैं खुद नहीं सुनाना चाहता।’’ रामकरन उसके करीब आता है।
‘‘कविता नहीं पढ़ोगे तो माइक के डंडे से पीटूँगा तुमको।’’ शेखर उसके धक्का देकर पुनः मंच पर चढ़ा देता है।
सारे प्राध्यापकों की तरह कुलपति भी चुप हैं।
‘‘बड़े भइया चंद्रशेखर को मेरा अभिवादन ! मित्र केवलानंद द्विवेदी और सभी सहपाठियों को हाय, मेरी कविता पहले पूरी हो गई है, इसलिए आप सब लोग शालीनता का परिचय दीजिए। दयानंद गुरुजी, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए।’’ रामकरन सम्मान-भरी आँखों से कुलपति को भी देखता है।
पीछे शुरू हो चुकी गड़का-गड़की के बीच चंद्रशेखर ताली बजाता है तो लड़कियाँ उसका साथ देती हैं। रामकरन लड़कियों की ओर अभिभूत नजरों से देखते हुए सिर झुकाता है। अब प्राध्यापक, कुलपति और मंच संचालक खिसियाहट ओढ़ लेते हैं।
चंद्रशेखर सहपाठी छात्राओं को धन्यवाद भी नहीं कह पाता, उससे पहले ही केवलानंद से कुछ छात्र हाथापाई करने लगते हैं। शेखर पीछे मुड़कर यह देख पाता कि उससे पहले ही एक युवक उसके बाल पकड़कर खींचता है, वह सँभलने का प्रयास करते हुए एक युवक को लंगी मार देता है, ‘‘साले ! बारह साल अखाड़े की मिट्टी इसलिए नहीं खोदा हूँ कि कोई मेरे बाल पकड़ ले !’’ उसकी आँखों में क्रोध उमड़ता है तो जीभ बाहर निकल आती है।
फर्श पर गिरा युवक उठने का प्रयास करता है। उठ पाता उससे पहले ही रामकरन उस पर चढ़ बैठता है, ‘‘भइया पर हाथ उठा दिए, भूसी छुड़ा दूँगा तेरी !’’
कई छात्रों को एक साथ परास्त कर रहा केवलानंद अब तक एक कुर्सी का गोड़ा तोड़ चुका है। वह गोड़ा तानकर नीचे गिरे युवक की ओर लपकता है तो डॉ. दयानंद हाथ फैलाकर आगे आ खड़े होते हैं, ‘‘केवलानंद ! गुरु का अनुरोध मान लो। तुम चाहोगे तो मारपीट रुक जाएगी।’’
वह गोड़ा नीचे करते हुए क्रोध का घूँट पीता है। डॉ. दयानंद बाहर से आकर स्काउट्स छात्रों की पटाई कर रहे युवकों को रोकने का प्रयास करते हैं, ‘‘यह ठीक नहीं हो रहा है चंद्रशेखर ! छोटी-सी बात पर तुम्हारी इस प्रकार गुंडई बर्दाश्त के बाहर है। भरपूर सज्जनता का परिचय दे रहे हैं तुम्हारे समर्थक !!’’
‘‘चुप रहिए, गुरु जी ! गिरगिरट की तरह रंग बदलते हो आप। यह सूअर की थूथन जैसा मुँह वाला दीपक सिंह तुम्हारा ही चिंटू है। पूछिए इससे, ठहरे हुए पानी में क्यों पत्थर उछाला इसने।’’ शेखर रुई की तरह धुने गए युवक की ओर उँगली उठाता है तो उसे नदारद पाता है। अब उसका क्रोध और भड़त उठता है, ‘‘आप गुरु हैं तो क्या लोकतंत्र की टाँग को नीचे दबाकर रखेंगे ! किसी से मन की वेदना सुनाने का अधिकार छीन लेंगे, किसी को बिना शिविर में आए ही प्रमाणपत्र दे देंगे ? आप और पहाड़ सिंह ने महाविद्यालय में जंगल राज फैला रखा है। जिसे आप लोग चाहते हैं, छात्रसंघ-अध्यक्ष चुना जाता है, जिसका खिलाफ हो जाते हैं, वह परिसर में घुसने नहीं पाता। तीन वर्श से अपकी निरंकुशता देख रहा था, आज पहली बार चुनौती दिया हूँ, चलो फैसला हो ही जाए। बताइए, कितने बड़े गुंडे हैं आप ? आपका इलाज क्या है ?
तेवरदार चंद्रशेखर कठफोड़वा पक्षी की चोंच की तरह उँगली उठाए जिसने कदम आगे बढ़ता है, दयानंद मिश्र पीछे हटते हैं। सभागार में चंद्रशेखर समर्थक छात्रों का कब्जा होने से उनके चेहरे पर बेइज्जती का भाव छाने लगता है। पीछे कदम हटाते हुए एक समय ऐसा आता है जब उनकी पीठ दीवार से सट जाती है और चंद्रशेखर की उँगली उनके सीने पर होती है, ‘‘कैसे कहा आपने रामकरन को सांप्रदायिक ? उत्तर दीजिए अन्यथा अपना सिर आपके सिर से लड़ा दूँगा... रिवॉल्वर निकालने का प्रयास किए तो हाथ मरोड़कर सीने पर चढ़ बैठूँगा। बोलिए !’’
‘‘चंद्रशेखर ! अपनी सीमा मत भूलो।’’
वह पीछे मुड़ता है तो सामने डॉ. ईशावस्या को खड़ी पाता है। कुछ कहता उससे पहले ही मैडम की फटकार उभरती है, ‘‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र पढ़ लिए तो क्या क्रांतिकारी हो गए ? सहन करने की भी एक सीमा होती है। पहले कार्यक्रम भरमंड करते हुए दीपक को अधमरा कर दिया, अब दयानंद जी के सिर पर हाथ उठाकर क्या साबित करना चाहते हो ? भरी सभा में एक तुम सत्यवादी हो, दूसरा तुम्हारा भाई रामकरन ?’’ वे भाई शब्द पर जोर देती हैं।
‘‘जी मैडम ! रामकरन सत्यवादी है और मैं उसका पक्षधर।’’
‘‘यदि हो तो क्या गुंडई के जरिए साबित करोगे ? यदि हां तो मैं तुम्हें अनर्थकारी और गुंडा कह रही हूँ। आओ, लड़ाओ मेरे सिर से अपना सिर। फाड़ो मेरे कपड़े, करो मुझे बेइज्जत।’’ उनकी दुबली, किंतु सुंदर काया क्रोध से काँपने लगती है
‘‘अऽऽ आप, रुक जाइए मैडम ! ऐ केवला ! तू हमारे बीच में न आ। मैं बात कर रहा हूँ, मैडम को समझा रहा हूँ।’’ शेखर हड़बड़ाकर दो कदम पीछे हटता है, साथ ही चभुरी बाँधे आगे आए केवलानंद का कॉलर पकड़कर खींचता है,
‘‘मैडम ! मैं क्षमा माँगता हूँ आपसे, धृतराष्ट्र की तरह काइयाँ और युधिष्ठिर की तरह ढोंगी डॉ. दयानंद मिश्र से भी। परंतु क्या बताएँगी, जब इन पर दबाव बढ़ा तो आप बीच में कूद पड़ीं, रामकरन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई तो आप चुप थीं ?’’
‘‘मैं चुप अवश्य थी परंतु डॉ. दयानंद जी के पक्ष में नहीं थी, और अब भी उनकी समर्थक नहीं हूँ। यदि तुमको रोकने के लिए आगे आई हूँ तो केवल इसलिए कि कल अखबारों में यह न छपे कि छात्रों ने प्राध्यापक की पिटाई की।’’
‘‘आपकी ही तरह यहाँ के अखबार वाले भी हैं, यह तो छाप देंगे कि प्राध्यापक के साथ अभद्रता हुई, यह नहीं लिखेंगे कि शुरुआत प्राध्यापक की ओर से हुई, जैसे कि आप मानने को नहीं तैयार हैं।’’
‘‘मैं मानती हूँ।’’ डॉ. ईशा अपने को अकेली अनुभव करती हैं।
‘‘फिर क्यों चुप रहीं, क्या आपको नहीं मालूम, यह मौन पक्षपात की श्रेणी में आता है ?’’
‘‘तुम बताओगे तब जानूँगी पक्षपात और निष्पक्षता का अर्थ !’’ साड़ी का पल्लू कमर में खोंसते हुए डॉ. ईशा पुनः आक्रोशित होती हैं, ‘‘आँख क्यों दिखा रहे हो, सोच रहे हो मैं तुमसे डर जाऊँगी ?’’
‘‘आँख तो आप दिखा रही हैं मैडम ! मनमाने ढंग से पहले किसी का पक्ष लेना और फिर लड़ने पर उतारू होना ‘उत्तर आधुनिक मनुवाद’ है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुँह पर टेप चिपकाकर हाथ पीछे की ओर बाँध देते हैं, आप जैसे लोग।’’ शेखर की आवाज में प्रतिरोध का भाव है।
‘‘जहाँ तक आँख दिखाने की बात है तो यह मेरा अधिकार है, शेखर ! रहा मनुवादी होने का आरोप तो तुमको समझाया नहीं जा सकता। जिस दिन व्यावहारिक समझ और परिपक्व ज्ञान तुम्हारे पास होगा, जवानी के जोस में गढ़ी गई परिभाषाएँ निरर्थक लगेंगी।’’
‘‘श्रीमान् जी ! अभी सात मिनट पूरे कहाँ हुए हैं ?’’
‘‘मंच से नीचे जाओ, रामकरन ! सांप्रदायिकता और वर्ग-संघर्ष फैलाने वाली कविता पढ़नी है तो बसपा जैसी कोई पार्टी ज्वॉइन कर लो। चलो, नीचे जाओ। रोवर्स ! रेंजर्स ! अपने साथी के लिए तालियाँ बजा दीजिए।’’ मंच संचालन कर रहे स्काउट एंड गाइड्स शिविर के अधिकारी डॉ. दयानंद मिश्र तिरछी दृष्टि से रामकरन को देखते हैं।
‘‘ताली क्यों, विसिल न बजा दें ?’’ अगली पंक्ति में बैठे छात्र भीम सिंह ने अनुमति चाही।
‘‘विसिल क्यों, ऐसे घटिया कविता पर तो हूटिंग होनी चाहिए।’’ दूसरे छात्र ने जोड़ा।
इसके बाद तो सीटियाँ, तालियाँ और नाक एक साथ बजने लगती हैं, दर्जनों छात्र व्यंग्य-बाण छोड़ते हुए उद्दंडता पर उतारू। मुख्य अतिथि कुलपति डॉ. राजदेव पांडेय तथा दूसरे प्राध्यापक लड़कियों की तरह एक चुप हजार चुप।
रामकरन अब भी मंच पर खड़ा है, इस उम्मीद में कि कुलपति उसका साथ देंगे। वह कभी मंच पर उपस्थित गण्यमान्यों को देखता है तो कभी उद्दंडता कर रहे छात्रों की ओर। उसे आश्चर्य होता है कि कक्षा के कई सहपाठी भी खिल्ली उड़ाने और अपशब्द कहने वालों में सम्मिलित हैं। शिविर अधिकारी पुनः मंच से उतरने के लिए कहते हैं तो निराशा-मिश्रित आक्रोश ओढ़कर रामकरन नीचे की ओर कदम बढ़ाता है। उतर पाता उससे पहले ही एक सुदर्शन युवक बुलंद आवाज में चेतावनी देता है, ‘‘माइक पर वापस जाओ, रामकरन ! पूरी कविता पढ़े बिना नीचे उतरे तो तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा।’’
सारे स्टाउट्स व अतिथिगण मेज पर चढ़ गए उस युवक की ओर देखते हैं। वह दाँत पीसते हुए मंच संचालक की ओर रुख करता है, ‘‘डॉ. दयानंद जी। ! क्रांति की बात कभी राजनीतिक मंच से नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर ज्यादातर थके-बूढ़े-कुंठित-कूपमंडूप नेताओं का कब्जा है। यहाँ युवा शक्ति उपस्थित है, गुरुजन भी हैं, इसलिए यह मंच सबसे उपयुक्त है। कविता पढ़ो, रामकरन ! हम सुनने के लिए तैयार हैं, ताली भी बजाएँगे, जिसे न सुनना हो वह खिसक ले।’’
डॉ. दयानंद और उनके सहयोगी असहाय। छात्रों में बाता-कही शुरू हो जाती है। आश्चर्य ! लड़कियाँ फिर भी बैठी रहती हैं। कूद-फाँद करते हुए आगे आ पहुँचा एक युवक चिघाड़ता है, ‘‘माइक पर वापस जाओ राम !’’
‘‘यह तुम्हारा नहीं, पूर्वांचल का अपमान है, रामकरन ! चंद्रशेखर भइया का मैं भी समर्थन करता हूँ।’’ यह आवाज केवलानंद द्विवेदी की होती है तो अब चंद्रशेखर की बगल में खड़ा है।
‘‘यह अकोढ़ी की चमरउटिया नहीं है, चंद्रशेखर ! हम नहीं सुनना चाहते रामकरन की कविता।’’ दीपक नाम का युवक खुला विरोध करता है।
‘‘हम नहीं, मैं कहो, दीपक !’’ चंद्रशेखर उसकी ओर उँगली उठाता है।
‘‘कुचकुचवा की तरह घूर क्या रहे हो, नहीं सुनना है तो बाहर चले जाओ।’’ केवलानंद सिताररूपी चंद्रशेखर का तानपूरा लगता है।
‘‘तुम दोनों जाओ, हम सब नहीं सुनना चाहते।’’ लगभग सभी छात्र खड़े हो जाते हैं।
‘‘तो सारे चले जाओ बाहर। कविता पूरी हो जाने के बाद अंदर आ जाना।’’ चंद्रशेखर सहजता का परिचय देता है।
‘‘भइया जी ! जाने दीजिए, अब मैं खुद नहीं सुनाना चाहता।’’ रामकरन उसके करीब आता है।
‘‘कविता नहीं पढ़ोगे तो माइक के डंडे से पीटूँगा तुमको।’’ शेखर उसके धक्का देकर पुनः मंच पर चढ़ा देता है।
सारे प्राध्यापकों की तरह कुलपति भी चुप हैं।
‘‘बड़े भइया चंद्रशेखर को मेरा अभिवादन ! मित्र केवलानंद द्विवेदी और सभी सहपाठियों को हाय, मेरी कविता पहले पूरी हो गई है, इसलिए आप सब लोग शालीनता का परिचय दीजिए। दयानंद गुरुजी, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए।’’ रामकरन सम्मान-भरी आँखों से कुलपति को भी देखता है।
पीछे शुरू हो चुकी गड़का-गड़की के बीच चंद्रशेखर ताली बजाता है तो लड़कियाँ उसका साथ देती हैं। रामकरन लड़कियों की ओर अभिभूत नजरों से देखते हुए सिर झुकाता है। अब प्राध्यापक, कुलपति और मंच संचालक खिसियाहट ओढ़ लेते हैं।
चंद्रशेखर सहपाठी छात्राओं को धन्यवाद भी नहीं कह पाता, उससे पहले ही केवलानंद से कुछ छात्र हाथापाई करने लगते हैं। शेखर पीछे मुड़कर यह देख पाता कि उससे पहले ही एक युवक उसके बाल पकड़कर खींचता है, वह सँभलने का प्रयास करते हुए एक युवक को लंगी मार देता है, ‘‘साले ! बारह साल अखाड़े की मिट्टी इसलिए नहीं खोदा हूँ कि कोई मेरे बाल पकड़ ले !’’ उसकी आँखों में क्रोध उमड़ता है तो जीभ बाहर निकल आती है।
फर्श पर गिरा युवक उठने का प्रयास करता है। उठ पाता उससे पहले ही रामकरन उस पर चढ़ बैठता है, ‘‘भइया पर हाथ उठा दिए, भूसी छुड़ा दूँगा तेरी !’’
कई छात्रों को एक साथ परास्त कर रहा केवलानंद अब तक एक कुर्सी का गोड़ा तोड़ चुका है। वह गोड़ा तानकर नीचे गिरे युवक की ओर लपकता है तो डॉ. दयानंद हाथ फैलाकर आगे आ खड़े होते हैं, ‘‘केवलानंद ! गुरु का अनुरोध मान लो। तुम चाहोगे तो मारपीट रुक जाएगी।’’
वह गोड़ा नीचे करते हुए क्रोध का घूँट पीता है। डॉ. दयानंद बाहर से आकर स्काउट्स छात्रों की पटाई कर रहे युवकों को रोकने का प्रयास करते हैं, ‘‘यह ठीक नहीं हो रहा है चंद्रशेखर ! छोटी-सी बात पर तुम्हारी इस प्रकार गुंडई बर्दाश्त के बाहर है। भरपूर सज्जनता का परिचय दे रहे हैं तुम्हारे समर्थक !!’’
‘‘चुप रहिए, गुरु जी ! गिरगिरट की तरह रंग बदलते हो आप। यह सूअर की थूथन जैसा मुँह वाला दीपक सिंह तुम्हारा ही चिंटू है। पूछिए इससे, ठहरे हुए पानी में क्यों पत्थर उछाला इसने।’’ शेखर रुई की तरह धुने गए युवक की ओर उँगली उठाता है तो उसे नदारद पाता है। अब उसका क्रोध और भड़त उठता है, ‘‘आप गुरु हैं तो क्या लोकतंत्र की टाँग को नीचे दबाकर रखेंगे ! किसी से मन की वेदना सुनाने का अधिकार छीन लेंगे, किसी को बिना शिविर में आए ही प्रमाणपत्र दे देंगे ? आप और पहाड़ सिंह ने महाविद्यालय में जंगल राज फैला रखा है। जिसे आप लोग चाहते हैं, छात्रसंघ-अध्यक्ष चुना जाता है, जिसका खिलाफ हो जाते हैं, वह परिसर में घुसने नहीं पाता। तीन वर्श से अपकी निरंकुशता देख रहा था, आज पहली बार चुनौती दिया हूँ, चलो फैसला हो ही जाए। बताइए, कितने बड़े गुंडे हैं आप ? आपका इलाज क्या है ?
तेवरदार चंद्रशेखर कठफोड़वा पक्षी की चोंच की तरह उँगली उठाए जिसने कदम आगे बढ़ता है, दयानंद मिश्र पीछे हटते हैं। सभागार में चंद्रशेखर समर्थक छात्रों का कब्जा होने से उनके चेहरे पर बेइज्जती का भाव छाने लगता है। पीछे कदम हटाते हुए एक समय ऐसा आता है जब उनकी पीठ दीवार से सट जाती है और चंद्रशेखर की उँगली उनके सीने पर होती है, ‘‘कैसे कहा आपने रामकरन को सांप्रदायिक ? उत्तर दीजिए अन्यथा अपना सिर आपके सिर से लड़ा दूँगा... रिवॉल्वर निकालने का प्रयास किए तो हाथ मरोड़कर सीने पर चढ़ बैठूँगा। बोलिए !’’
‘‘चंद्रशेखर ! अपनी सीमा मत भूलो।’’
वह पीछे मुड़ता है तो सामने डॉ. ईशावस्या को खड़ी पाता है। कुछ कहता उससे पहले ही मैडम की फटकार उभरती है, ‘‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र पढ़ लिए तो क्या क्रांतिकारी हो गए ? सहन करने की भी एक सीमा होती है। पहले कार्यक्रम भरमंड करते हुए दीपक को अधमरा कर दिया, अब दयानंद जी के सिर पर हाथ उठाकर क्या साबित करना चाहते हो ? भरी सभा में एक तुम सत्यवादी हो, दूसरा तुम्हारा भाई रामकरन ?’’ वे भाई शब्द पर जोर देती हैं।
‘‘जी मैडम ! रामकरन सत्यवादी है और मैं उसका पक्षधर।’’
‘‘यदि हो तो क्या गुंडई के जरिए साबित करोगे ? यदि हां तो मैं तुम्हें अनर्थकारी और गुंडा कह रही हूँ। आओ, लड़ाओ मेरे सिर से अपना सिर। फाड़ो मेरे कपड़े, करो मुझे बेइज्जत।’’ उनकी दुबली, किंतु सुंदर काया क्रोध से काँपने लगती है
‘‘अऽऽ आप, रुक जाइए मैडम ! ऐ केवला ! तू हमारे बीच में न आ। मैं बात कर रहा हूँ, मैडम को समझा रहा हूँ।’’ शेखर हड़बड़ाकर दो कदम पीछे हटता है, साथ ही चभुरी बाँधे आगे आए केवलानंद का कॉलर पकड़कर खींचता है,
‘‘मैडम ! मैं क्षमा माँगता हूँ आपसे, धृतराष्ट्र की तरह काइयाँ और युधिष्ठिर की तरह ढोंगी डॉ. दयानंद मिश्र से भी। परंतु क्या बताएँगी, जब इन पर दबाव बढ़ा तो आप बीच में कूद पड़ीं, रामकरन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई तो आप चुप थीं ?’’
‘‘मैं चुप अवश्य थी परंतु डॉ. दयानंद जी के पक्ष में नहीं थी, और अब भी उनकी समर्थक नहीं हूँ। यदि तुमको रोकने के लिए आगे आई हूँ तो केवल इसलिए कि कल अखबारों में यह न छपे कि छात्रों ने प्राध्यापक की पिटाई की।’’
‘‘आपकी ही तरह यहाँ के अखबार वाले भी हैं, यह तो छाप देंगे कि प्राध्यापक के साथ अभद्रता हुई, यह नहीं लिखेंगे कि शुरुआत प्राध्यापक की ओर से हुई, जैसे कि आप मानने को नहीं तैयार हैं।’’
‘‘मैं मानती हूँ।’’ डॉ. ईशा अपने को अकेली अनुभव करती हैं।
‘‘फिर क्यों चुप रहीं, क्या आपको नहीं मालूम, यह मौन पक्षपात की श्रेणी में आता है ?’’
‘‘तुम बताओगे तब जानूँगी पक्षपात और निष्पक्षता का अर्थ !’’ साड़ी का पल्लू कमर में खोंसते हुए डॉ. ईशा पुनः आक्रोशित होती हैं, ‘‘आँख क्यों दिखा रहे हो, सोच रहे हो मैं तुमसे डर जाऊँगी ?’’
‘‘आँख तो आप दिखा रही हैं मैडम ! मनमाने ढंग से पहले किसी का पक्ष लेना और फिर लड़ने पर उतारू होना ‘उत्तर आधुनिक मनुवाद’ है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुँह पर टेप चिपकाकर हाथ पीछे की ओर बाँध देते हैं, आप जैसे लोग।’’ शेखर की आवाज में प्रतिरोध का भाव है।
‘‘जहाँ तक आँख दिखाने की बात है तो यह मेरा अधिकार है, शेखर ! रहा मनुवादी होने का आरोप तो तुमको समझाया नहीं जा सकता। जिस दिन व्यावहारिक समझ और परिपक्व ज्ञान तुम्हारे पास होगा, जवानी के जोस में गढ़ी गई परिभाषाएँ निरर्थक लगेंगी।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book