|
विविध उपन्यास >> अप्सरा का शाप अप्सरा का शापयशपाल
|
378 पाठक हैं |
||||||
कुटिया से मेनका के लोप हो जाने पर जब तक शिशु कन्या महर्षि विश्वामित्र की गोद में किलकती-हुमकती रही, वे शिशु में मग्न रह कर सब कुछ भूले रहे...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
अनसूया क्षोभ से अधीर हो परन्तु विनय से अंजलि-बद्ध हो
बोली–‘‘महाराज, विशालमति नीतिज्ञों की ऐसा
विस्मृति से तो माया का भ्रम होता है। हम तीनों अल्पमति जो महाराज के रूप
में, मुद्रा, कंठस्वर, सब कुछ पहचान रहे हैं और महाराज को, आश्रम कन्या के
प्रति अनुराग की अधीरता में कूप से स्वयं जल कलश खींचकर वाटिका सींचने की
इच्छा, शकुन्तला के स्नेह के लिए आश्रम के पोष्य कुरंग से स्पर्धा,
शकुन्तला के पाणिग्रहण की इच्छा से माता गौतमी के सम्मुख प्रार्थना,
शकुन्तला के गर्भ से अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकार देने की
प्रतिज्ञा, इसके साथ अनेक दिवा-रात्रि का सहवास, इसे सम्मानपूर्वक राज
प्रासाद में बुला लेने का आश्वासन, सब कुछ विस्मृत हो गया
!’’
दुष्यन्त भृकुटी उठाकर विचार में मौन रहा और उसने अनुसूया से प्रश्न किया–‘‘देवी का क्या अभिप्राय है ? देवी किस प्रसंग का संकेत कर रही हैं !’’
स्वातन्त्रयोत्तर भारत के शिखरस्थ लेखकों में प्रमुख, यशपाल ने अपने प्रत्येक उपन्यास को पाठक के मन-रंजन से हटाकर उसकी वैचारिक समृद्धि को लक्षित किया है। विचारधारा से उनकी प्रतिबद्धता ने उनकी रचनात्मकता को हर बार एक नया आयाम दिया, और उनकी हर रचना एक नए तेवर के साथ सामने आई।
‘अप्सरा का शाप’ में उन्होंने दुष्यन्त-शकुन्तला के पौराणिक आख्यान को आधुनिक संवेदना और तर्कणा के आधार पर पुनराख्यायित किया है। यशपाल के शब्दों में : ‘शकुन्तला की कथा पतिव्रत धर्म में निष्ठा की पौराणिक कथा है। महाभारत के प्रणेता तथा कालिदास ने उस कथा का उपयोग अपने-अपने समय की भावनाओं, मान्यताओं तथा प्रयोजनों के अनुसार किया है। उन्हीं के अनुकरण में ‘अप्सरा का शाप’ के लेखक ने भी अपने युग की भावना तथा दृष्टि के अनुसार शकुन्तला के अनुभवों की कल्पना की है।’’
उपन्यास की केन्द्रीय वस्तु दुष्यन्त का शकुन्तला से अपने प्रेम सम्बन्ध को भूल जाना है, इसी को अपने नजरिए से देखते हुए लेखक ने इस उपन्यास में नायक ‘दुष्यन्त’ की पुनर्स्थापना की है और बताया है कि नायक ने जो किया, उसके आधार पर आज के युग में उसे धीरोदत्त की पदवी नहीं दी जा सकती।
दुष्यन्त भृकुटी उठाकर विचार में मौन रहा और उसने अनुसूया से प्रश्न किया–‘‘देवी का क्या अभिप्राय है ? देवी किस प्रसंग का संकेत कर रही हैं !’’
स्वातन्त्रयोत्तर भारत के शिखरस्थ लेखकों में प्रमुख, यशपाल ने अपने प्रत्येक उपन्यास को पाठक के मन-रंजन से हटाकर उसकी वैचारिक समृद्धि को लक्षित किया है। विचारधारा से उनकी प्रतिबद्धता ने उनकी रचनात्मकता को हर बार एक नया आयाम दिया, और उनकी हर रचना एक नए तेवर के साथ सामने आई।
‘अप्सरा का शाप’ में उन्होंने दुष्यन्त-शकुन्तला के पौराणिक आख्यान को आधुनिक संवेदना और तर्कणा के आधार पर पुनराख्यायित किया है। यशपाल के शब्दों में : ‘शकुन्तला की कथा पतिव्रत धर्म में निष्ठा की पौराणिक कथा है। महाभारत के प्रणेता तथा कालिदास ने उस कथा का उपयोग अपने-अपने समय की भावनाओं, मान्यताओं तथा प्रयोजनों के अनुसार किया है। उन्हीं के अनुकरण में ‘अप्सरा का शाप’ के लेखक ने भी अपने युग की भावना तथा दृष्टि के अनुसार शकुन्तला के अनुभवों की कल्पना की है।’’
उपन्यास की केन्द्रीय वस्तु दुष्यन्त का शकुन्तला से अपने प्रेम सम्बन्ध को भूल जाना है, इसी को अपने नजरिए से देखते हुए लेखक ने इस उपन्यास में नायक ‘दुष्यन्त’ की पुनर्स्थापना की है और बताया है कि नायक ने जो किया, उसके आधार पर आज के युग में उसे धीरोदत्त की पदवी नहीं दी जा सकती।
अप्सरा का शाप
इस देश को भारत नाम महाराज भरत के प्रताप से मिला है। प्रतापी भरत की माता
सती शकुन्तला महाराज दुष्यंत की रानी थी। शकुन्तला राजर्षि विश्वामित्र और
अप्सरा मेनका की सन्तान थी।
भरत की माता शकुन्तला के जन्म तथा जीवन के प्रसंग पुराणों, महाभारत तथा प्राचीन काव्यों में यत्र-तत्र मिलते हैं परन्तु ये वर्णन स्फुट हैं। शकुन्तला के जीवन-वृत्तान्त के अनेक व्यौरे ऐसे थे जिनका महत्व सम्भवतः तत्कालीन समाज की दृष्टि में विशेष नहीं था। अतः उस समय के इतिहासकारों और कवियों ने भी उन घटनाओं का वर्णन नहीं किया है। आधुनिक समाज की परिस्थितियों, समस्याओं और चिन्तन की दृष्टि से शकुन्तला के जीवन के, तत्कालीन लेखकों द्वारा उपेक्षित अनुभवों पर भी विचार करना उपयोगी होगा।
पौराणिक वर्णन के अनुसार शकुन्तला की माता मेनका इस लोक की नारी नहीं, देवलोक की अप्सरा थी। एक समय देवताओं पर विकट संकट आ गया था। उस संकट का उपाय करने के लिये देवराज इन्द्र ने मेनका को कुछ समय के लिये नारी शरीर धारण कर मर्त्यलोक में रहने का आदेश दिया था। उस प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार है :–
महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना चाहते थे। विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व के अधिकार और पद को पाने के लिये घोर तप किया। ब्राह्मणों और देवताओं ने विश्वामित्र के तप की श्लाघा से उन्हें महर्षि से ऊँचा, राजर्षि पद देना स्वीकार कर लिया परन्तु विश्वामित्र के क्षत्रिय कुलोद्भव होने के कारण देवताओं और ब्राह्मणों ने उन्हें समाज के विधायक ब्रह्मर्षि का पद देना स्वीकार न किया।
विश्वामित्र देवताओं और ब्राह्मणों की व्यवस्था और शासन में ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात देखकर देवताओं की सृष्टि और ब्राह्मणों की व्यवस्था से असंतुष्ट हो गये। उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित तथा शासित सृष्टि और व्यवस्था की प्रतिद्वन्द्विता में नयी सृष्टि तथा नयी व्यवस्था की रचना का निश्चय कर लिया। देवताओं और ब्राह्मणों ने सृष्टि की व्यवस्था पर अपने अधिकार के प्रति विश्वामित्र की इस चुनौती को क्षुद्र मानव का क्षुब्ध अहंकार ही समझा परन्तु विश्वामित्र दृढ़ निश्चय से नयी सृष्टि की व्यवस्था की रचना के लिये तप में लग गये।
कुछ समय पश्चात् देवलोक में नारद मुनि तथा अग्नि, वरुण, पवन आदि देवों के गणों द्वारा, विश्वामित्र के नवीन सृष्टि रचना के तप की सफलता के समाचार पहुँचने लगे। देवराज इन्द्र ने सुना–विश्वामित्र ने विरंचि द्वारा विरचित सृष्टि से भिन्न नये वनस्पति और जीवों के निर्माण में सफलता प्राप्त कर ली है। विश्वामित्र ने मरुस्थल में भी पनप सकने वाले वनस्पति नागफनी, मदार, एरण्ड आदि वृक्षों की जामुन, कटहल, नारियल, गेहूँ आदि फलों तथा धान्यों की रचना कर ली है। देवताओं और ब्राह्मणों को प्यारी दुग्धामृत देने वाली गाय की अपेक्षा अधिक दूध देने वाले भैंस नाम के जीव तथा देवों के प्रिय वाहन अश्व से भी अधिक समर्थ उष्ट्र की सृष्टि कर ली है। इन समाचारों से देवराज इन्द्र ने आशंका अनुभव की–क्षुद्र जान पड़ने वाला, मर्त्यलोक का मानव यदि दृढ़ निश्चय से प्रयत्न में कटिबद्ध हो जाय तो वह विरंचि की सृष्टि की व्यवस्था में भी हस्तक्षेप कर सकता है, वह दैवी विधान को भी हिला दे सकता है, उसके लिये सभी कुछ संभव है। देवराज इन्द्र देवों की सत्ता के प्रति मानव की स्पर्धा से अति आशंकित हो उठे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के, नयी सृष्टि-रचना के लिये प्रयत्न के तप को येन-केन प्रकारेण स्खलित कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया।
देवराज इन्द्र जानते थे कि परंतप महर्षि विश्वामित्र का निश्चय भंग कर देना अत्यन्त कठिन था। वे जानते थे, किसी भी शक्ति का भय अथवा सम्पदा का प्रलोभन विश्वामित्र को अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता था। इन्द्र ने विश्वामित्र का तप स्खलित करने के लिये, स्वयं उनकी ही शक्ति–विश्वामित्र के मानव शरीर की कार्य-कारण भूत प्राणशक्ति, सृजन-शक्ति–का ही उपयोग करने का निश्चय किया। देवराज ने विश्वामित्र के अस्तित्व अथवा शरीर में व्याप्त सृजन-शक्ति को वश में कर, उन्हें तप के लक्ष्य से विमुख करने का उत्तरदायित्व देवलोक की प्रुमख अप्सरा मेनका को सौंपा।
अप्सरा मेनका देवराज इन्द्र के आदेश से महर्षि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिये मर्त्यलोक में आयी। महर्षि को वश में करने के लिए मेनका ने इन्द्र से परामर्श से उस कामशक्ति का प्रयोग किया जो शरीर मात्र के उद्भव और क्रम का निमित्त होती है और प्राण तथा जीवन के गुण के रूप में जीव मात्र में समाहित रहती है। मेनका ने विश्वामित्र के शरीर में व्याप्त उस शक्ति का उद्बबोधन करने के लिये अप्सरा के गुण स्वभाव त्याग कर नारी प्रकृति ग्रहण कर ली और महर्षि विश्वामित्र के सामीप्य में प्रत्यक्ष हो गयी। विश्वामित्र का ध्यान आकर्षित करने के लिये मेनका को सूक्ष्म भाव-भंगिमा तथा संकेतों द्वारा अनेक प्रयत्न करने पड़े। वह अवसर पाकर महर्षि की दृष्टि में पड़ जाती और उनकी दृष्टि से संकोच प्रकट कर छिप जाने का यत्न करती। वह सयत्न असावधानी में अपने कमनीय शरीर पर से वायु द्वारा सहसा वस्त्र उड़ जाने देती और फिर महर्षि की दृष्टि के भय और लाज से कच्छप के समान अपने में ही सिमट जाती।
प्रज्वलित अग्नि का सामीप्य अन्य पदार्थो में समाहित सुषुप्त अग्नि का उद्बबोधन किये बिना नहीं रहता। महर्षि विश्वामित्र का शरीर कठिन तप से शुष्क काष्ठवत् हो गया था, परन्तु कामाग्नि की प्रतीक मेनका के सामीप्य और संगति से महर्षि के शरीर में कामशक्ति के स्फुलिंग स्फुरित होने लगे। उनका शरीर जीवन की उमंग से सिरहन और स्पन्दन अनुभव करने लगा। महर्षि की तप में लगी हुई प्राणशक्ति मेनका के लावण्यमय शरीर के अवलम्ब से सार्थक होने के लिये व्याकुल हो गयी। महर्षि के चित्त में मेनका की संगति को अधिकाधिक चरितार्थ करने के अतिरिक्त अन्य विचार का अवकाश न रहा। काम की एकाग्रता में विश्वामित्र को देवत्व तथा ब्रह्मत्व की स्पर्धा और प्रतिद्वन्द्वी सृष्टि की रचना का ध्यान न रहा। विश्वामित्र, नारी रूप मेनका के समर्पण के परिरम्भ में विवश हो गये।
मेनका विश्वामित्र का ध्यान नवसृष्टि रचना से स्खलित करने में सफल हो गयी परन्तु विश्वामित्र तप पुनः आरम्भ न कर दें, इस चिन्ता में वह कितने समय तक मर्त्यलोक में बनी रहती ! मेनका को मर्त्यलोक में देवलोक के कर्म तथा फल से उन्मुक्त, अबाध सुख का संतोष प्राप्त न था। उसे देवलोक में अपनी स्थित तथा अधिकार की भी चिन्ता थी। उसकी प्रतिद्वन्द्विनी अप्सरायें उर्वशी, रम्भा आदि देवलोक में उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठा सकती थीं।
अप्सरा मेनका ने मर्त्यलोक में जीवन के धर्म और नियम जान लिये थे :–जीव अपने शरीरों के प्रकृति और गुण से काम-प्रवृत्ति का धर्म पूरा करते हैं। जीव इसी धर्म की पूर्ति अथवा कर्म के फलस्वरूप सन्तान प्राप्त करते हैं और वे सन्तान के पालन-रक्षा आदि के धर्म अथवा कर्म में बंध जाते हैं। यही मर्त्यलोक में जीवन का धर्म अथवा लोकधर्म है। इस लोकधर्म की परम्परा से ही सृष्टि की व्यवस्था का चक्र चलता रहता है। जीवों में व्याप्त काम प्रवृत्ति अथवा सृजनधर्म की परम्परा ही सृष्टि के अनन्त चक्र की गति का कारण है। मेनका ने निश्चय किया देवराज द्वारा निर्दिष्ट उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र को लोकधर्म की परम्परा में बाँध देना आवश्यक होगा। मेनका ने विश्वामित्र को अपनी संगति से दिये आनन्द और सन्तोष का मूर्त्त, एक शिशु-कन्या उनके लिए प्रसव कर दी।
महर्षि विश्वामित्र रूप-लावण्य की पुंज मेनका में अपने परिणय के परिपाक का प्रतीक शिशु पाकर गद्गद हो गये। मेनका की गोद में वह नवजात कन्या केवल सजीव मांसपिण्ड के समान थी। उसके शरीर के नखशिख नारी शरीर की आकृति के संकेत मात्र ही थे। शिशु में आकृति की पूर्णता का कोई सौष्ठव नहीं होता। कच्ची कोमलता और अपूर्णता ही उस शिशु का भी सौंदर्य था। पिलपिले से सिर पर काले कोमल रोयें केशों के संकेत में, छोटे-छोटे नीले वन्य पुष्पों की भाँति दो नेत्र, नासा का छोटा-सा छिद्र मात्र और दंतहीन, प्रायः खुला रहने वाला मुख, मांस में कटे ताजे घाव सा लाल। कन्या-शिशु अपने छोटे-छोटे, नितान्त अक्षम पंगु हाथ-पांव केवल निरुद्देश्य हिलाडुला सकती थी। वह अपनी इच्छा और प्रयोजन को केवल किलक और क्रन्दन द्वारा ही प्रकट कर सकती थी परन्तु महर्षि इस सौंदर्य को निहार-निहार कर विभोर होते रहते। शिशु के किलकने और रोने में भी महर्षि को रोमहर्षक संगीत की झंकार की अनुभूति होती। वे उस नारी शरीर के अंकुर को स्नेह से निहारते और संतोष के लिए पुचकारते रहते। शिशु का हंसना देखने औऱ उसकी किलक सुन पाने के लिए उसे दोनों हाथों से उछालने लगते। उसे पुलकाने और किलकाने के लिए अपने घने श्मश्रु से घिरे ओठों को गोल बनाकर शिशु स्वर के अनुकरण में ‘‘ऊ, ई’’ शब्द करने लगते। मेनका उनके सामने बैठी सन्तोष से मुस्कराती रहती और शिशु के क्षुधा से ठुनकने पर उसे अपनी गोद में ले लेती।
महर्षि के सम्मुख समीप बैठी मेनका वक्ष से कंचुकी हटाकर गौर, सुगोल, उन्नत स्तन का श्याम ऊर्ध्व चंचु शिशु के मुख में दे देती। शिशु, सेवती की फैली हुई पंखुड़ियों के समान अपने नन्हें-नन्हें हाथ आश्रय के लिए माता के गौर वक्ष और स्तन पर रख, स्तनाग्र को अपने दंतहीन मुख में ले हुमक-हुमक कर घूँट भरने लगती तो महर्षि एकटक उसे देखते रहते। मेनका महर्षि के संतोष की श्लाघा में मुस्कराकर उनकी ओर देख लेती। मेनका की उस मुस्कान और उसकी आंखों की ज्योति से महर्षि ऐसे परमानन्द में तन्मय हो जाते जो उन्होंने तप करते समय अपने शरीर को विस्मृत कर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में भी अनुभव न किया था।
महर्षि और मेनका अपने आहार के लिए वन्य-प्रदेश में प्राप्य पदार्थों का उत्साह से संग्रह करते। वे इस तत्परता में नयी सृष्टि के लिए वनस्पति और जीवों का निर्माण करने की सफलता से भी अधिक उत्साह और सन्तोष अनुभव करते। वे ब्रह्मा की सृष्टि की प्रतिद्वन्द्विता में नव-सृष्टि निर्माण की प्रतिज्ञा भूल गये थे।
मेनका महर्षि को सन्तुष्ट देखकर अनुभव कर रही थी कि देवराज इन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो गया है। वह मानव के असामर्थ्य से सीमित, सुख-दुख संकुल संसार में क्यों बंधी रहे। उसके लिए देवलोक लौट जाने का अवसर आ गया था परन्तु मर्त्यलोक में निवास करके तथा जीवों के समान अपने शरीर से सन्तान प्रसव करके इस लोक के शरीरियों की भाँति वह सन्तान के मोह का अनुभव करने लगी थी। उसे आशंका थी कि देवलोक लौट जाने पर भी वह मर्त्यलोक के गुण-स्वभाव-सन्तान के मोह का परिचय पाकर उस आकर्षण को सदा अनुभव करती रहेगी।
एक प्रातः सूर्योदय के कुछ समय पश्चात् मेनका महर्षि के समीप बैठी शिशु-कन्या को दिवस का प्रथम दुग्धपान करा रही थी। कन्या ने सन्तुष्ट होकर माता के स्तन से मुख फेर लिया और समीप बैठे पिता की ओर देखा। माता के दूध के बूंद शिशु के ओठ से चिबुक पर ढरक आयी थी। पिता को स्नेह के आह्वान में दोनों हाथ बढ़ाये देख कर शिशु क्रीड़ा के लिए किलक उठी। विश्वामित्र ने शिशु को अपने हाथों में ले लिया और उसे हंसाने-किलकाने के लिए अपनी नासा उसके शरीर पर छुला-छुला कर उसे गुदगुदाने लगे। जिस समय विश्वामित्र शिशु से क्रीड़ा में आत्मविस्मृत थे मेनका उठ कर कुटिया से बाहर चली गयी और फिर नहीं लौटी।
महर्षि विश्वामित्र का-प्रतिद्वन्द्वी सृष्टि निर्माण का–तप भंग करने में सफल होकर मेनका देवलोक लौटी तो वहां उकी कामोद्दीपक शक्ति और कलात्मक सामर्थ्य की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई और देवसभा में उसका आदर बहुत बढ़ गया। मेनका के मर्त्यलोक प्रवास के समय देवसभा में सभी कलात्मक कार्यों के अनुष्ठान के अवसर, उर्वशी तथा उसकी अनुवर्ती अप्सराओं और गन्धर्वों को ही मिलते थे। परिणाम में उर्वशी के दल की कलात्मक क्षमता और प्रभाव भी बहुत बढ़ गये थे। मेनका की अनुपस्थिति में उसकी अनुवर्ती अप्सराओं और गन्धर्वों के दल में अनुशासन की शिथिलता आ गयी थी। प्रमाद और अनभ्यास के कारण उसके दल की अप्सराओं और गन्धर्वों की कला प्रवीणता का ह्रास हो गया था। देवलोक में लौटकर मेनका को अपने दल की क्षमता और प्रभाव की पुनर्स्थापना के लिए बहुत यत्न करना पड़ा। उस चिन्ता में भी मेनका का मन कबी-कभी अपनी मानवी संतान की स्मृति में भटक जाता।
मेनका ने देवलोक लौटकर अप्सरा के गुण तथा स्वभाव पुनः पा लिये थे। वह मर्त्यलोक की प्रवृत्तियों से विमुक्त हो गयी थी परन्तु इस लोक में रहने का कुछ न कुछ प्रभाव शेष था ही। वह अपनी मानवी सन्तान का मोह विस्मृत न कर सकी। उसके मन में अपनी कन्या की चिन्ता सिर उठा लेती परन्तु अपनी सन्तान के समाचारों के लिए मर्त्यलोक की ओर ध्यान का अवसर और सुविधा उसे कहां थी। उसने भी इस लोक में अपनी सन्तान की अवस्था तथा गतिविधि की ओर ध्यान रखने का कार्य अपनी अनुवर्ती अप्सरा सानुमती को सौंप दिया था।
सानुमती ने मेनका को समाचार दिया:–
कुटिया से मेनका के लोप हो जाने पर जब तक शिशु कन्या महर्षि विश्वामित्र की गोद में किलकती-हुमकती रही, वे शिशु में मग्न रह कर सब कुछ भूले रहे। मेनका के जाने के पश्चात् दो घड़ी में ही शिशु असुविधा और आवश्यकता से ठुनकने लगी और पिता के स्नेह से पुचकारने और बहलाने पर भी क्रन्दन से असुविधा प्रकट करती रही। महर्षि नितान्त असहाय शिशु को सम्भाल सकने में अपनी अक्षमता अनुभव करने लगे। शिशु की माता के लौटने में विलम्ब से वे खिन्न होने लगे। अन्ततः अधीर हो गये। दिन का तीसरा पहर बीतते-बीतते महर्षि ने समझ पाया–नवजात, नितान्त असमर्थ, असहाय शिशु को सम्भाल सकना नवीन सृष्टि से भी अधिक कठिन था। कन्या का रोना ही समाप्त न होता था और महर्षि उसे सन्तुष्ट औऱ प्रसन्न न कर सकते थे। उनका यह असामर्थ्य असीम क्षोभपूर्ण वेदना बन रहा था। इस संकट से महर्षि के ज्ञान-चक्षु खुल गये, समझ गये–वे मेह जाल में फंस कर लक्ष्य-भ्रष्ट हो गये थे। उन्होंने विचार किया–मैं देवत्व और ब्रह्मत्व की प्राप्ति की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर मोह आविष्ट हो रहा हूँ। सहसा उन्हें भास हो गया, यह तो उनका तप भ्रष्ट करने के लिए देवताओं का छल था।
विश्वामित्र ने निश्चय किया–मैं छला गया हूँ परन्तु छल को जान गया हूँ। छल के जाल में बंधा नहीं रहूँगा। क्या मेरे ज्ञान के सामर्थ्य तथा तप की शक्ति का प्रयोजन अंडे से तुरन्त निकले पक्षी-शावक के समान असहाय, क्षुद्र मानव जीव का वहन तथा पालन करना ही है ? इस उत्तरदायित्व को वही सम्भाले जिसने मुझे झेलने के लिए इसे अपने गर्भ से जन्म दिया है। महर्षि क्षुधा की असुविधा से क्रन्दन करती हुई शिशु-कन्या को गोद में लिये, क्षोभ में अपने तपोभंग के लिए पश्चाताप करते रहे। एक पहर रात्रि बीतने पर उन्होंने निश्चय कर लिया, वे मोहजाल के बन्धन से मुक्त हो जायेंगे।
महर्षि क्षुधा और असुविधा से निरन्तर रोती शिशु कन्या को गोद में लिये धैर्य से शिशु के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिशु रो-रो कर क्लान्त हो गयी और क्लान्ति से सो गयी। महर्षि ने कुटिया की अलगनी पर से मेनका का छोड़ा हुआ शाटक वस्त्र उतार लिया। सुषुप्त शिशु को शाटक-वस्त्र में लपेट लिया। शाटक में लिपटे शिशु को सावधानी से उठाकर वे अपनी कुटिया से बहुत दूर, ऋषि कण्व के आश्रम की दिशा में चल दिये। नवजात शिशु के उत्तरदायित्व से मुक्ति की चिंता में महर्षि को सूझ गया–ऋषि कण्व और गौतमी ज्ञानार्जन के लिए गृहस्थ त्याग, तपोवन का जीवन अपना कर भी करुणा के मोह जाल से मुक्त नहीं हो पाये हैं। वे असहाय असमर्थ त्यक्त शिशु की अवहेलना नहीं कर सकेंगे।
भरत की माता शकुन्तला के जन्म तथा जीवन के प्रसंग पुराणों, महाभारत तथा प्राचीन काव्यों में यत्र-तत्र मिलते हैं परन्तु ये वर्णन स्फुट हैं। शकुन्तला के जीवन-वृत्तान्त के अनेक व्यौरे ऐसे थे जिनका महत्व सम्भवतः तत्कालीन समाज की दृष्टि में विशेष नहीं था। अतः उस समय के इतिहासकारों और कवियों ने भी उन घटनाओं का वर्णन नहीं किया है। आधुनिक समाज की परिस्थितियों, समस्याओं और चिन्तन की दृष्टि से शकुन्तला के जीवन के, तत्कालीन लेखकों द्वारा उपेक्षित अनुभवों पर भी विचार करना उपयोगी होगा।
पौराणिक वर्णन के अनुसार शकुन्तला की माता मेनका इस लोक की नारी नहीं, देवलोक की अप्सरा थी। एक समय देवताओं पर विकट संकट आ गया था। उस संकट का उपाय करने के लिये देवराज इन्द्र ने मेनका को कुछ समय के लिये नारी शरीर धारण कर मर्त्यलोक में रहने का आदेश दिया था। उस प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार है :–
महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना चाहते थे। विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व के अधिकार और पद को पाने के लिये घोर तप किया। ब्राह्मणों और देवताओं ने विश्वामित्र के तप की श्लाघा से उन्हें महर्षि से ऊँचा, राजर्षि पद देना स्वीकार कर लिया परन्तु विश्वामित्र के क्षत्रिय कुलोद्भव होने के कारण देवताओं और ब्राह्मणों ने उन्हें समाज के विधायक ब्रह्मर्षि का पद देना स्वीकार न किया।
विश्वामित्र देवताओं और ब्राह्मणों की व्यवस्था और शासन में ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात देखकर देवताओं की सृष्टि और ब्राह्मणों की व्यवस्था से असंतुष्ट हो गये। उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित तथा शासित सृष्टि और व्यवस्था की प्रतिद्वन्द्विता में नयी सृष्टि तथा नयी व्यवस्था की रचना का निश्चय कर लिया। देवताओं और ब्राह्मणों ने सृष्टि की व्यवस्था पर अपने अधिकार के प्रति विश्वामित्र की इस चुनौती को क्षुद्र मानव का क्षुब्ध अहंकार ही समझा परन्तु विश्वामित्र दृढ़ निश्चय से नयी सृष्टि की व्यवस्था की रचना के लिये तप में लग गये।
कुछ समय पश्चात् देवलोक में नारद मुनि तथा अग्नि, वरुण, पवन आदि देवों के गणों द्वारा, विश्वामित्र के नवीन सृष्टि रचना के तप की सफलता के समाचार पहुँचने लगे। देवराज इन्द्र ने सुना–विश्वामित्र ने विरंचि द्वारा विरचित सृष्टि से भिन्न नये वनस्पति और जीवों के निर्माण में सफलता प्राप्त कर ली है। विश्वामित्र ने मरुस्थल में भी पनप सकने वाले वनस्पति नागफनी, मदार, एरण्ड आदि वृक्षों की जामुन, कटहल, नारियल, गेहूँ आदि फलों तथा धान्यों की रचना कर ली है। देवताओं और ब्राह्मणों को प्यारी दुग्धामृत देने वाली गाय की अपेक्षा अधिक दूध देने वाले भैंस नाम के जीव तथा देवों के प्रिय वाहन अश्व से भी अधिक समर्थ उष्ट्र की सृष्टि कर ली है। इन समाचारों से देवराज इन्द्र ने आशंका अनुभव की–क्षुद्र जान पड़ने वाला, मर्त्यलोक का मानव यदि दृढ़ निश्चय से प्रयत्न में कटिबद्ध हो जाय तो वह विरंचि की सृष्टि की व्यवस्था में भी हस्तक्षेप कर सकता है, वह दैवी विधान को भी हिला दे सकता है, उसके लिये सभी कुछ संभव है। देवराज इन्द्र देवों की सत्ता के प्रति मानव की स्पर्धा से अति आशंकित हो उठे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के, नयी सृष्टि-रचना के लिये प्रयत्न के तप को येन-केन प्रकारेण स्खलित कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया।
देवराज इन्द्र जानते थे कि परंतप महर्षि विश्वामित्र का निश्चय भंग कर देना अत्यन्त कठिन था। वे जानते थे, किसी भी शक्ति का भय अथवा सम्पदा का प्रलोभन विश्वामित्र को अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता था। इन्द्र ने विश्वामित्र का तप स्खलित करने के लिये, स्वयं उनकी ही शक्ति–विश्वामित्र के मानव शरीर की कार्य-कारण भूत प्राणशक्ति, सृजन-शक्ति–का ही उपयोग करने का निश्चय किया। देवराज ने विश्वामित्र के अस्तित्व अथवा शरीर में व्याप्त सृजन-शक्ति को वश में कर, उन्हें तप के लक्ष्य से विमुख करने का उत्तरदायित्व देवलोक की प्रुमख अप्सरा मेनका को सौंपा।
अप्सरा मेनका देवराज इन्द्र के आदेश से महर्षि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिये मर्त्यलोक में आयी। महर्षि को वश में करने के लिए मेनका ने इन्द्र से परामर्श से उस कामशक्ति का प्रयोग किया जो शरीर मात्र के उद्भव और क्रम का निमित्त होती है और प्राण तथा जीवन के गुण के रूप में जीव मात्र में समाहित रहती है। मेनका ने विश्वामित्र के शरीर में व्याप्त उस शक्ति का उद्बबोधन करने के लिये अप्सरा के गुण स्वभाव त्याग कर नारी प्रकृति ग्रहण कर ली और महर्षि विश्वामित्र के सामीप्य में प्रत्यक्ष हो गयी। विश्वामित्र का ध्यान आकर्षित करने के लिये मेनका को सूक्ष्म भाव-भंगिमा तथा संकेतों द्वारा अनेक प्रयत्न करने पड़े। वह अवसर पाकर महर्षि की दृष्टि में पड़ जाती और उनकी दृष्टि से संकोच प्रकट कर छिप जाने का यत्न करती। वह सयत्न असावधानी में अपने कमनीय शरीर पर से वायु द्वारा सहसा वस्त्र उड़ जाने देती और फिर महर्षि की दृष्टि के भय और लाज से कच्छप के समान अपने में ही सिमट जाती।
प्रज्वलित अग्नि का सामीप्य अन्य पदार्थो में समाहित सुषुप्त अग्नि का उद्बबोधन किये बिना नहीं रहता। महर्षि विश्वामित्र का शरीर कठिन तप से शुष्क काष्ठवत् हो गया था, परन्तु कामाग्नि की प्रतीक मेनका के सामीप्य और संगति से महर्षि के शरीर में कामशक्ति के स्फुलिंग स्फुरित होने लगे। उनका शरीर जीवन की उमंग से सिरहन और स्पन्दन अनुभव करने लगा। महर्षि की तप में लगी हुई प्राणशक्ति मेनका के लावण्यमय शरीर के अवलम्ब से सार्थक होने के लिये व्याकुल हो गयी। महर्षि के चित्त में मेनका की संगति को अधिकाधिक चरितार्थ करने के अतिरिक्त अन्य विचार का अवकाश न रहा। काम की एकाग्रता में विश्वामित्र को देवत्व तथा ब्रह्मत्व की स्पर्धा और प्रतिद्वन्द्वी सृष्टि की रचना का ध्यान न रहा। विश्वामित्र, नारी रूप मेनका के समर्पण के परिरम्भ में विवश हो गये।
मेनका विश्वामित्र का ध्यान नवसृष्टि रचना से स्खलित करने में सफल हो गयी परन्तु विश्वामित्र तप पुनः आरम्भ न कर दें, इस चिन्ता में वह कितने समय तक मर्त्यलोक में बनी रहती ! मेनका को मर्त्यलोक में देवलोक के कर्म तथा फल से उन्मुक्त, अबाध सुख का संतोष प्राप्त न था। उसे देवलोक में अपनी स्थित तथा अधिकार की भी चिन्ता थी। उसकी प्रतिद्वन्द्विनी अप्सरायें उर्वशी, रम्भा आदि देवलोक में उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठा सकती थीं।
अप्सरा मेनका ने मर्त्यलोक में जीवन के धर्म और नियम जान लिये थे :–जीव अपने शरीरों के प्रकृति और गुण से काम-प्रवृत्ति का धर्म पूरा करते हैं। जीव इसी धर्म की पूर्ति अथवा कर्म के फलस्वरूप सन्तान प्राप्त करते हैं और वे सन्तान के पालन-रक्षा आदि के धर्म अथवा कर्म में बंध जाते हैं। यही मर्त्यलोक में जीवन का धर्म अथवा लोकधर्म है। इस लोकधर्म की परम्परा से ही सृष्टि की व्यवस्था का चक्र चलता रहता है। जीवों में व्याप्त काम प्रवृत्ति अथवा सृजनधर्म की परम्परा ही सृष्टि के अनन्त चक्र की गति का कारण है। मेनका ने निश्चय किया देवराज द्वारा निर्दिष्ट उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र को लोकधर्म की परम्परा में बाँध देना आवश्यक होगा। मेनका ने विश्वामित्र को अपनी संगति से दिये आनन्द और सन्तोष का मूर्त्त, एक शिशु-कन्या उनके लिए प्रसव कर दी।
महर्षि विश्वामित्र रूप-लावण्य की पुंज मेनका में अपने परिणय के परिपाक का प्रतीक शिशु पाकर गद्गद हो गये। मेनका की गोद में वह नवजात कन्या केवल सजीव मांसपिण्ड के समान थी। उसके शरीर के नखशिख नारी शरीर की आकृति के संकेत मात्र ही थे। शिशु में आकृति की पूर्णता का कोई सौष्ठव नहीं होता। कच्ची कोमलता और अपूर्णता ही उस शिशु का भी सौंदर्य था। पिलपिले से सिर पर काले कोमल रोयें केशों के संकेत में, छोटे-छोटे नीले वन्य पुष्पों की भाँति दो नेत्र, नासा का छोटा-सा छिद्र मात्र और दंतहीन, प्रायः खुला रहने वाला मुख, मांस में कटे ताजे घाव सा लाल। कन्या-शिशु अपने छोटे-छोटे, नितान्त अक्षम पंगु हाथ-पांव केवल निरुद्देश्य हिलाडुला सकती थी। वह अपनी इच्छा और प्रयोजन को केवल किलक और क्रन्दन द्वारा ही प्रकट कर सकती थी परन्तु महर्षि इस सौंदर्य को निहार-निहार कर विभोर होते रहते। शिशु के किलकने और रोने में भी महर्षि को रोमहर्षक संगीत की झंकार की अनुभूति होती। वे उस नारी शरीर के अंकुर को स्नेह से निहारते और संतोष के लिए पुचकारते रहते। शिशु का हंसना देखने औऱ उसकी किलक सुन पाने के लिए उसे दोनों हाथों से उछालने लगते। उसे पुलकाने और किलकाने के लिए अपने घने श्मश्रु से घिरे ओठों को गोल बनाकर शिशु स्वर के अनुकरण में ‘‘ऊ, ई’’ शब्द करने लगते। मेनका उनके सामने बैठी सन्तोष से मुस्कराती रहती और शिशु के क्षुधा से ठुनकने पर उसे अपनी गोद में ले लेती।
महर्षि के सम्मुख समीप बैठी मेनका वक्ष से कंचुकी हटाकर गौर, सुगोल, उन्नत स्तन का श्याम ऊर्ध्व चंचु शिशु के मुख में दे देती। शिशु, सेवती की फैली हुई पंखुड़ियों के समान अपने नन्हें-नन्हें हाथ आश्रय के लिए माता के गौर वक्ष और स्तन पर रख, स्तनाग्र को अपने दंतहीन मुख में ले हुमक-हुमक कर घूँट भरने लगती तो महर्षि एकटक उसे देखते रहते। मेनका महर्षि के संतोष की श्लाघा में मुस्कराकर उनकी ओर देख लेती। मेनका की उस मुस्कान और उसकी आंखों की ज्योति से महर्षि ऐसे परमानन्द में तन्मय हो जाते जो उन्होंने तप करते समय अपने शरीर को विस्मृत कर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में भी अनुभव न किया था।
महर्षि और मेनका अपने आहार के लिए वन्य-प्रदेश में प्राप्य पदार्थों का उत्साह से संग्रह करते। वे इस तत्परता में नयी सृष्टि के लिए वनस्पति और जीवों का निर्माण करने की सफलता से भी अधिक उत्साह और सन्तोष अनुभव करते। वे ब्रह्मा की सृष्टि की प्रतिद्वन्द्विता में नव-सृष्टि निर्माण की प्रतिज्ञा भूल गये थे।
मेनका महर्षि को सन्तुष्ट देखकर अनुभव कर रही थी कि देवराज इन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो गया है। वह मानव के असामर्थ्य से सीमित, सुख-दुख संकुल संसार में क्यों बंधी रहे। उसके लिए देवलोक लौट जाने का अवसर आ गया था परन्तु मर्त्यलोक में निवास करके तथा जीवों के समान अपने शरीर से सन्तान प्रसव करके इस लोक के शरीरियों की भाँति वह सन्तान के मोह का अनुभव करने लगी थी। उसे आशंका थी कि देवलोक लौट जाने पर भी वह मर्त्यलोक के गुण-स्वभाव-सन्तान के मोह का परिचय पाकर उस आकर्षण को सदा अनुभव करती रहेगी।
एक प्रातः सूर्योदय के कुछ समय पश्चात् मेनका महर्षि के समीप बैठी शिशु-कन्या को दिवस का प्रथम दुग्धपान करा रही थी। कन्या ने सन्तुष्ट होकर माता के स्तन से मुख फेर लिया और समीप बैठे पिता की ओर देखा। माता के दूध के बूंद शिशु के ओठ से चिबुक पर ढरक आयी थी। पिता को स्नेह के आह्वान में दोनों हाथ बढ़ाये देख कर शिशु क्रीड़ा के लिए किलक उठी। विश्वामित्र ने शिशु को अपने हाथों में ले लिया और उसे हंसाने-किलकाने के लिए अपनी नासा उसके शरीर पर छुला-छुला कर उसे गुदगुदाने लगे। जिस समय विश्वामित्र शिशु से क्रीड़ा में आत्मविस्मृत थे मेनका उठ कर कुटिया से बाहर चली गयी और फिर नहीं लौटी।
महर्षि विश्वामित्र का-प्रतिद्वन्द्वी सृष्टि निर्माण का–तप भंग करने में सफल होकर मेनका देवलोक लौटी तो वहां उकी कामोद्दीपक शक्ति और कलात्मक सामर्थ्य की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई और देवसभा में उसका आदर बहुत बढ़ गया। मेनका के मर्त्यलोक प्रवास के समय देवसभा में सभी कलात्मक कार्यों के अनुष्ठान के अवसर, उर्वशी तथा उसकी अनुवर्ती अप्सराओं और गन्धर्वों को ही मिलते थे। परिणाम में उर्वशी के दल की कलात्मक क्षमता और प्रभाव भी बहुत बढ़ गये थे। मेनका की अनुपस्थिति में उसकी अनुवर्ती अप्सराओं और गन्धर्वों के दल में अनुशासन की शिथिलता आ गयी थी। प्रमाद और अनभ्यास के कारण उसके दल की अप्सराओं और गन्धर्वों की कला प्रवीणता का ह्रास हो गया था। देवलोक में लौटकर मेनका को अपने दल की क्षमता और प्रभाव की पुनर्स्थापना के लिए बहुत यत्न करना पड़ा। उस चिन्ता में भी मेनका का मन कबी-कभी अपनी मानवी संतान की स्मृति में भटक जाता।
मेनका ने देवलोक लौटकर अप्सरा के गुण तथा स्वभाव पुनः पा लिये थे। वह मर्त्यलोक की प्रवृत्तियों से विमुक्त हो गयी थी परन्तु इस लोक में रहने का कुछ न कुछ प्रभाव शेष था ही। वह अपनी मानवी सन्तान का मोह विस्मृत न कर सकी। उसके मन में अपनी कन्या की चिन्ता सिर उठा लेती परन्तु अपनी सन्तान के समाचारों के लिए मर्त्यलोक की ओर ध्यान का अवसर और सुविधा उसे कहां थी। उसने भी इस लोक में अपनी सन्तान की अवस्था तथा गतिविधि की ओर ध्यान रखने का कार्य अपनी अनुवर्ती अप्सरा सानुमती को सौंप दिया था।
सानुमती ने मेनका को समाचार दिया:–
कुटिया से मेनका के लोप हो जाने पर जब तक शिशु कन्या महर्षि विश्वामित्र की गोद में किलकती-हुमकती रही, वे शिशु में मग्न रह कर सब कुछ भूले रहे। मेनका के जाने के पश्चात् दो घड़ी में ही शिशु असुविधा और आवश्यकता से ठुनकने लगी और पिता के स्नेह से पुचकारने और बहलाने पर भी क्रन्दन से असुविधा प्रकट करती रही। महर्षि नितान्त असहाय शिशु को सम्भाल सकने में अपनी अक्षमता अनुभव करने लगे। शिशु की माता के लौटने में विलम्ब से वे खिन्न होने लगे। अन्ततः अधीर हो गये। दिन का तीसरा पहर बीतते-बीतते महर्षि ने समझ पाया–नवजात, नितान्त असमर्थ, असहाय शिशु को सम्भाल सकना नवीन सृष्टि से भी अधिक कठिन था। कन्या का रोना ही समाप्त न होता था और महर्षि उसे सन्तुष्ट औऱ प्रसन्न न कर सकते थे। उनका यह असामर्थ्य असीम क्षोभपूर्ण वेदना बन रहा था। इस संकट से महर्षि के ज्ञान-चक्षु खुल गये, समझ गये–वे मेह जाल में फंस कर लक्ष्य-भ्रष्ट हो गये थे। उन्होंने विचार किया–मैं देवत्व और ब्रह्मत्व की प्राप्ति की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर मोह आविष्ट हो रहा हूँ। सहसा उन्हें भास हो गया, यह तो उनका तप भ्रष्ट करने के लिए देवताओं का छल था।
विश्वामित्र ने निश्चय किया–मैं छला गया हूँ परन्तु छल को जान गया हूँ। छल के जाल में बंधा नहीं रहूँगा। क्या मेरे ज्ञान के सामर्थ्य तथा तप की शक्ति का प्रयोजन अंडे से तुरन्त निकले पक्षी-शावक के समान असहाय, क्षुद्र मानव जीव का वहन तथा पालन करना ही है ? इस उत्तरदायित्व को वही सम्भाले जिसने मुझे झेलने के लिए इसे अपने गर्भ से जन्म दिया है। महर्षि क्षुधा की असुविधा से क्रन्दन करती हुई शिशु-कन्या को गोद में लिये, क्षोभ में अपने तपोभंग के लिए पश्चाताप करते रहे। एक पहर रात्रि बीतने पर उन्होंने निश्चय कर लिया, वे मोहजाल के बन्धन से मुक्त हो जायेंगे।
महर्षि क्षुधा और असुविधा से निरन्तर रोती शिशु कन्या को गोद में लिये धैर्य से शिशु के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिशु रो-रो कर क्लान्त हो गयी और क्लान्ति से सो गयी। महर्षि ने कुटिया की अलगनी पर से मेनका का छोड़ा हुआ शाटक वस्त्र उतार लिया। सुषुप्त शिशु को शाटक-वस्त्र में लपेट लिया। शाटक में लिपटे शिशु को सावधानी से उठाकर वे अपनी कुटिया से बहुत दूर, ऋषि कण्व के आश्रम की दिशा में चल दिये। नवजात शिशु के उत्तरदायित्व से मुक्ति की चिंता में महर्षि को सूझ गया–ऋषि कण्व और गौतमी ज्ञानार्जन के लिए गृहस्थ त्याग, तपोवन का जीवन अपना कर भी करुणा के मोह जाल से मुक्त नहीं हो पाये हैं। वे असहाय असमर्थ त्यक्त शिशु की अवहेलना नहीं कर सकेंगे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book









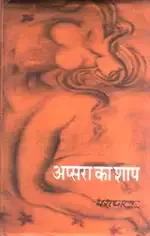


_s.webp)
