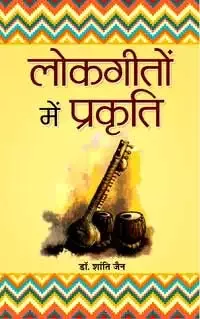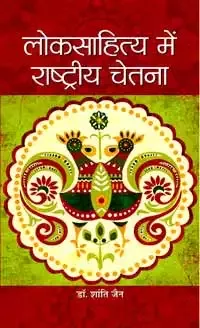|
संस्कृति >> लोकगीतों के संदर्भ और आयाम लोकगीतों के संदर्भ और आयामशान्ति जैन
|
291 पाठक हैं |
||||||
लोक जीवन तथा लोक संस्कृति पर आधारित लोकगीतों के विविध आयामों का अध्ययन...
Lokgeeton Ke Sandarbh Aur Ayam - A Hindi Book - by Shanti Jain
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
अछोर क्षितिज तक फैला अनन्त आकाश है–लोकगीतों का। अतल सागर जैसी गहराई है–लोकगीतों की। जंगल में उसे पेड़-पौधों की तरह अनादि है–इनका इतिहास। हृदय से निकले स्वर गीत बन गये, संगीत बन गये। समग्र जनजीवन के जीवन्त चित्र प्रस्तुत करते थे लोकगीत भारत की लोक संस्कृति के चित्रपट हैं।
लोकगीतों का संक्षिप्त परिचय, उसके प्रकार, विभिन्न प्रदेशों के संस्कार गीत, ऋतुओं के, व्रत-त्योहारों के, विभिन्न जातियों के, श्रमिकों के, बालक–बालिकाओं के, नृत्य के, विभिन्न रसों के, धार्मिक भावना के तथा किसी भी समय गाये जाने वाले गीतों का अध्ययन ग्यारह अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।
लोक जीवन तथा लोक संस्कृति पर आधारित लोकगीतों के विविध आयामों का अध्ययन इस ग्रन्थ की विशेषता है।
लोकगीतों का संक्षिप्त परिचय, उसके प्रकार, विभिन्न प्रदेशों के संस्कार गीत, ऋतुओं के, व्रत-त्योहारों के, विभिन्न जातियों के, श्रमिकों के, बालक–बालिकाओं के, नृत्य के, विभिन्न रसों के, धार्मिक भावना के तथा किसी भी समय गाये जाने वाले गीतों का अध्ययन ग्यारह अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।
लोक जीवन तथा लोक संस्कृति पर आधारित लोकगीतों के विविध आयामों का अध्ययन इस ग्रन्थ की विशेषता है।
कोश शैली में विवेचित माटी के गीत
भारतीय संस्कृति की अनूठी धरोहर–लोकगीत। काव्य रस से ओत-प्रोत, स्वर–सने, लय-लसे, हृदय तल से उभरे, सर्वथा मनोहारी। विविधता में एकता के साक्षात् प्रतीक। भाषाएँ भिन्न, बोलियाँ विभिन्न, किन्तु विषयवस्तु, स्वर-संयोजन तथा लय-प्रवाह में लगभग समानता। इनकी लघुकाय धुनों को सुनकर ‘बिहारी सतसई’ विषयक यह उक्ति सहज ही मानस में गूँज उठती है–
सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर,
देखन में छोटे लगैं, घाव करें गंभीर।
देखन में छोटे लगैं, घाव करें गंभीर।
परम्परा से प्राप्त और जन-जीवन से जुड़े इन लोकगीतों में निहित सरस साहित्य को उजाहर करने और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने का प्रथम श्रेय है–हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि पं० रामनरेश त्रिपाठी को। उन्हें इन गीतों के प्रति आकृष्ट किया एक रोचक घटना ने। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ ग्रामीण महिलाएँ, अपने परदेसी पतियों को विदा करने, रेलवे स्टेशन पर आई हुई थीं। ‘आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे’ इस वियोग व्यथा से आक्रान्त वे फूट-फूट कर रोये जा रही थीं। ट्रेन आई और उनके प्रियतमों को लिये आँखों से ओझल हो गई। कुछ देर तक तो वे महिलाएँ भींगी आँखों से उस भागती ट्रेन को निहारती रही, पर जब गाड़ी दृष्टि से परे हो गई तो उनका वह विलाप, आलाप में परिणत हो गया। वे गाने लगीं–‘रेलिया सवति, पिया को लिये जाय रे’। स्टेशन पर बैठे त्रिपाठीजी यह परिवर्तित परिदृश्य देख रहे थे। रेल से सौत की उपमा ? कितनी सटीक कितनी विमुग्धकारी ? त्रिपाठीजी का कवि हृदय इस अनुपम अभिव्यक्ति से अभिभूत हो उठा। उसी क्षण उन्होंने ठान लिया कि वे इन लोकगीतों का संग्रह एवं प्रकाशन कर जन-जन तक पहुँचाएँगे। उनका वह ऐतिहासिक संकल्प मूर्तिमान हुआ, उनकी ‘कविता कौमुदी’ के चौथे भाग में, लोकगीतों के संग्रह में। त्रिपाठीजी का वह अभिनव प्रयास, भावी शोधकों के लिये पथ का दीप बन गया–प्रेरक और मार्गदर्शक।
लोकगीतों में समाहित काव्य रस कितना मधुपगा, कितना विनोदात्मक होता है, इसकी कुछ झलकियाँ–
शाम हो चली है। एक युवक चरवाहा अपने ढेरों के साथ थका-माँदा जंगल से घर की ओर आ रहा है। दिन तो उसने रूखी-सूखी रोटियाँ खाकर बिता दिया था, किन्तु अब वह भूख से बेहाल हो उठा है। पास से गुजरती एक यौवनभार से बोझल सुन्दरी को देख वह कराह उठता है और फिर उसकी तड़प मुखर हो उठती है, उसके इस ‘बिरहा’ में–
लोकगीतों में समाहित काव्य रस कितना मधुपगा, कितना विनोदात्मक होता है, इसकी कुछ झलकियाँ–
शाम हो चली है। एक युवक चरवाहा अपने ढेरों के साथ थका-माँदा जंगल से घर की ओर आ रहा है। दिन तो उसने रूखी-सूखी रोटियाँ खाकर बिता दिया था, किन्तु अब वह भूख से बेहाल हो उठा है। पास से गुजरती एक यौवनभार से बोझल सुन्दरी को देख वह कराह उठता है और फिर उसकी तड़प मुखर हो उठती है, उसके इस ‘बिरहा’ में–
भुखिया क मारी विरहा बिसरिगा, भूलि गई कजरी कबीर,
देखि के गोरी क मोहनी मुरतिया, उठे न करेजवा में पीर।
देखि के गोरी क मोहनी मुरतिया, उठे न करेजवा में पीर।
भूख ने अब उसे बेसुध कर दिया है। न उसे मादक पावस में गाया जाने वाला ‘विरहा’ याद आ रहा है और न पावस की प्रियतमा ‘कजरी’। यही नहीं ‘फागुन मस्त महीना’ में गाया जाने वाला ‘कबीर’ भी वह भूल गया है। और तो और, चढ़ती जवानी में भी, उस चरवाहे को भूख ने इस कदर बेहाल कर दिया है कि गोरी की मोहनी मूरत देखकर भी उसके कलेजे में पीर नहीं उठती। ‘भूख’ का ऐसा सटीक, सार्थक और मर्मवेधी शब्द–चित्रण शायद ही अन्यत्र उपलब्ध हो।
युवती भी मनचली थी। चुटकी लेती हुई बोली– मरो तुम भूखे। मैं तो अपने प्रियतम को ऐसा भोजन कराऊँगी कि तुम उसका सपना भी नहीं देख सकते। जानते हो, वह क्या होगा ? और फिर नहले पर दहला जड़ते हुए गा उठी–
युवती भी मनचली थी। चुटकी लेती हुई बोली– मरो तुम भूखे। मैं तो अपने प्रियतम को ऐसा भोजन कराऊँगी कि तुम उसका सपना भी नहीं देख सकते। जानते हो, वह क्या होगा ? और फिर नहले पर दहला जड़ते हुए गा उठी–
तन मोरा अदहन, मन मोरा चाउर
नयन मूँग के दाल
अपने बलम के जेवना जेंवइबे
बिनू अदहन बिनू आग।
नयन मूँग के दाल
अपने बलम के जेवना जेंवइबे
बिनू अदहन बिनू आग।
मेरी दहकती देह उबाल खाता पानी है, मेरा मदभरा मन चावल है और मेरे नशीले नयन मूँग की दाल हैं। इन तीनों के मिश्रण से मैं अपने प्रियतम को ऐसा खाना खिलाऊँगी कि वह सर्वरूपेण तृप्त हो जायेगा। मुझे न तो आग की अपेक्षा है, न ही अदहन की। ठेठ बोली में उमड़ते यौवन का कितना मुग्धकारी शब्द चित्रण है, इस गीत में।
सावन–भादों की कजरारी भीगी रातें जब विरहदग्धा नायिका को नागिन-सी डँसने लगती हैं तो सूरदास की यह उक्ति साकार हो उठती है–प्रिय बिनु नागिन कारी रात’। और परदेसी प्रियतम की याद से आकुल वह विरहिणी उड़ेल देती है अपनी कसक, अपनी टीस, अपनी चिरसंगिनी इस कजली में–
सावन–भादों की कजरारी भीगी रातें जब विरहदग्धा नायिका को नागिन-सी डँसने लगती हैं तो सूरदास की यह उक्ति साकार हो उठती है–प्रिय बिनु नागिन कारी रात’। और परदेसी प्रियतम की याद से आकुल वह विरहिणी उड़ेल देती है अपनी कसक, अपनी टीस, अपनी चिरसंगिनी इस कजली में–
गरजे बरसे रे बादरवा, प्रिय बिन मोंहे ना सुहाय।
और मादक चैत ? उसकी तो कल्पना करके ही विरहिणी सिहर उठती है। उसके आगमन की आशंका से त्रस्त मनोव्यथा मुखरित हो उठती है इस ‘चैती’ में–
आयत चैत उतपतिया हो रामा, पिया घर नाहीं।
सच पूछा जाय तो ये लोकगीत हमारे साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उनके भीतर से हमारा इतिहास झाँकता है। वे सही अर्थो में हमारे सामाजिक जीवन के दर्पण हैं। इतिहास शोधक, यदि इन लोकगीतों में निहित सामग्री की छान-बीनकर, समुचित विश्लेषण चयन कर उनका अपेक्षित उपयोग करें तो हमारा इतिहास कहीं अधिक सजीव, संतुलित और सर्वांगीण बन जाएगा।
अब रही इन लोकगीतों के संगीत पक्ष की बात। वह भी कम रोचक नहीं। लोकगीतों की धुनों की, उनकी स्वर संरचना की तथा उनके लयप्रवाह की अपनी विशिष्टताएँ हैं। प्रथम, इनकी बंदिश प्रायः मध्यसप्तक में ही सीमित होती है, वह भी पूर्वार्ध में ही, उत्तरार्ध का स्पर्श यदा-कदा ही होता है। तार एवं मन्द्रसप्तक इनकी परिधि से बाहर ही रहते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसलिये इनका गायन श्रमसाध्य भी नहीं होता। यों तो इन बंदिशों से सभी बारह स्वरों का प्रयोग होता है, किन्तु बहुलता शुद्ध स्वरों की ही होती है।
दूसरे, अधिकांश लोकगीत कहरवा, दादरा जैसे छोटे, किन्तु प्रवाहमान तालों में निबद्ध होते हैं। चाल इनकी अक्सर मध्यलय में ही होती है; विलम्बित एवं द्रुतलय में बहुत कम लोकगीत गाए जाते हैं। तीसरे, इन लोकगीतों के स्वर विन्यास और लयदारी में सहज प्रवाह होता है, कोई बनावटीपन नहीं। उनकी सहजता, उनकी भावप्रवणता ही उन्हें इतना चुटीला, इतना मर्मभेदी बना देती है। और अन्तिम, कितने ही लोकगीतों की बन्दिशे कुछ गिने-चुने लोकप्रिय रागों पीलू, भैरवी, तिलक-कामोद आदि के मोहक स्वरगुच्छों में होती हैं।
मेरा अनुमान है कि राग रचना की प्रेरणा भी इन्हीं रंजक लोकगीतों के स्वरगुच्छों से मिली होगी। मतंग मुनि ने राग की जो व्याख्या की है, उससे इस अनुमान की पुष्टि होती है–
अब रही इन लोकगीतों के संगीत पक्ष की बात। वह भी कम रोचक नहीं। लोकगीतों की धुनों की, उनकी स्वर संरचना की तथा उनके लयप्रवाह की अपनी विशिष्टताएँ हैं। प्रथम, इनकी बंदिश प्रायः मध्यसप्तक में ही सीमित होती है, वह भी पूर्वार्ध में ही, उत्तरार्ध का स्पर्श यदा-कदा ही होता है। तार एवं मन्द्रसप्तक इनकी परिधि से बाहर ही रहते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसलिये इनका गायन श्रमसाध्य भी नहीं होता। यों तो इन बंदिशों से सभी बारह स्वरों का प्रयोग होता है, किन्तु बहुलता शुद्ध स्वरों की ही होती है।
दूसरे, अधिकांश लोकगीत कहरवा, दादरा जैसे छोटे, किन्तु प्रवाहमान तालों में निबद्ध होते हैं। चाल इनकी अक्सर मध्यलय में ही होती है; विलम्बित एवं द्रुतलय में बहुत कम लोकगीत गाए जाते हैं। तीसरे, इन लोकगीतों के स्वर विन्यास और लयदारी में सहज प्रवाह होता है, कोई बनावटीपन नहीं। उनकी सहजता, उनकी भावप्रवणता ही उन्हें इतना चुटीला, इतना मर्मभेदी बना देती है। और अन्तिम, कितने ही लोकगीतों की बन्दिशे कुछ गिने-चुने लोकप्रिय रागों पीलू, भैरवी, तिलक-कामोद आदि के मोहक स्वरगुच्छों में होती हैं।
मेरा अनुमान है कि राग रचना की प्रेरणा भी इन्हीं रंजक लोकगीतों के स्वरगुच्छों से मिली होगी। मतंग मुनि ने राग की जो व्याख्या की है, उससे इस अनुमान की पुष्टि होती है–
योऽयं ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषितः
रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः
रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः
लोकगीतों की विशिष्ट धुनों ने कलाकार की कल्पना को कुरेदा होगा और उसने ‘स्वर’ (आरोह-अवरोह), तथा वर्ण (रोचक गायन प्रक्रिया) से विभूषित कर उन्हें जनचित्तरंजक बनाकर ‘राग’ का जामा पहना दिया होगा। कुछ रागों के नाम जैसे भूपाली, जौनपुरी, पहाड़ी आदि इस तथ्य के स्पष्ट परिचायक हैं कि ये राग उन स्थानों की लोकप्रिय लोकधुनों से ही निर्मित और विकसित हुए होंगे।
पं० रामनरेश त्रिपाठी के ऐतिहासिक लोकगीत संग्रह के बाद से अब तक विभिन्न आंचलिक भाषाओं, बोलियों के लोकगीतों पर कितने शोधप्रबन्ध लिखे गये हैं किन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इन प्रबन्धों में मुख्यतः उनके साहित्य पक्ष का ही विश्लेषण, विवेचन हुआ है। उनका सांगीतिक पक्ष प्राय: अनछुआ ही रह गया है।
डॉ० शान्ति जैन ने अपनी प्रस्तुत पुस्तक ‘लोकगीतों के संदर्भ और आयाम’ में पहली बार इन गीतों के साहित्यक सौन्दर्य के विश्लेषण विवेचन के साथ उनके सांगीतिक पहलुओं पर भी समुचित प्रकाश डाला है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी शान्तिजी भाषाविद् और संगीत मर्मज्ञ दोंनो हैं। संस्कृत, हिन्दी तथा अनेक आंचलिक बोलियों पर इनका अच्छा अधिकार है। वह जानी मानी कवयित्री और गीतकार तो है ही, स्वयं एक उत्तम कोटि की गायिका भी है। अतः उन्होंने अपनी इस कृति में साहित्य और संगीत–लोकगीतों के दोनों पक्षों का समुचित, संतुलित और सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत किया है। विभिन्न क्षेत्रों के बिखरे-पसरे लोकगीतों के संग्रह और फिर उनके मनन मंथन में उन्होंने कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया है। फलतः उनका यह शोधपरक विश्लेषण और निरूपण हिन्दी भाषा में एक मील का पत्थर’ बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
कोश शैली मैं लिखी, ऐसी अनुपम उपलब्धि एवं सार्थक कृति के लिये शान्तिजी को मेरी हार्दिक बधाई और स्नेहाशीष भी।
पं० रामनरेश त्रिपाठी के ऐतिहासिक लोकगीत संग्रह के बाद से अब तक विभिन्न आंचलिक भाषाओं, बोलियों के लोकगीतों पर कितने शोधप्रबन्ध लिखे गये हैं किन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इन प्रबन्धों में मुख्यतः उनके साहित्य पक्ष का ही विश्लेषण, विवेचन हुआ है। उनका सांगीतिक पक्ष प्राय: अनछुआ ही रह गया है।
डॉ० शान्ति जैन ने अपनी प्रस्तुत पुस्तक ‘लोकगीतों के संदर्भ और आयाम’ में पहली बार इन गीतों के साहित्यक सौन्दर्य के विश्लेषण विवेचन के साथ उनके सांगीतिक पहलुओं पर भी समुचित प्रकाश डाला है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी शान्तिजी भाषाविद् और संगीत मर्मज्ञ दोंनो हैं। संस्कृत, हिन्दी तथा अनेक आंचलिक बोलियों पर इनका अच्छा अधिकार है। वह जानी मानी कवयित्री और गीतकार तो है ही, स्वयं एक उत्तम कोटि की गायिका भी है। अतः उन्होंने अपनी इस कृति में साहित्य और संगीत–लोकगीतों के दोनों पक्षों का समुचित, संतुलित और सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत किया है। विभिन्न क्षेत्रों के बिखरे-पसरे लोकगीतों के संग्रह और फिर उनके मनन मंथन में उन्होंने कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया है। फलतः उनका यह शोधपरक विश्लेषण और निरूपण हिन्दी भाषा में एक मील का पत्थर’ बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
कोश शैली मैं लिखी, ऐसी अनुपम उपलब्धि एवं सार्थक कृति के लिये शान्तिजी को मेरी हार्दिक बधाई और स्नेहाशीष भी।
समर बहादुर सिंह
अध्याय 1
लोकगीतों का संक्षिप्त परिचय
‘लोक’ शब्द संस्कृत के ‘लोकदर्शने’ धातु में ‘घञ्’ प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है–देखने वाला। साधारण जनता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है।
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में, ‘‘लोक हमारे जीवन का महासमुद्र हैं, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान संचित हैं। अर्वाचीन मानव के लिये लोक सर्वोच्च प्रजापति है।’’
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ‘लोक’ शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम से न लेकर नगरों व गाँवों में फैली उस समूची जनता से लिया है जो परिष्कृत, रुचिसंपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन की अभ्यस्त होती है।
डॉ० कुंजबिहारी दास ने लोकगीतों की परिभाषा देते हुए कहा है, ‘‘लोकसंगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है, जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक आदिम अवस्था में निवास करते हैं। यह साहित्य प्रायः मौखिक होता है और परम्परागत रूप से चला आ रहा है।’’
लोकगीतों को मात्र ग्रामगीत कहकर उनकी व्यापकता को कम नहीं किया जा सकता। ये गीत अब गाँव की चहारदीवारी को छोड़ नगरों और महानगरों की सीमा को छू रहे हैं। हिन्दी साहित्य कोश में ‘लोकगीत’ शब्द के तीन अर्थ किये गये हैं–
1. लोक में प्रचलित गीत,
2. लोकनिर्मित गीत तथा
3. लोकविषयक गीत।
किन्तु वास्तव में लोकगीत का तात्पर्य लोक में प्रचलित गीत ही है, जिसे दो अर्थ दिये जा सकते हैं–1. अवसरविशेष के प्रचलित गीत तथा 2. परम्परागत गीत।
लोक द्वारा निर्मित होने पर भी लोकगीत को किसी व्यक्तिविशेष से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि रचनाकार को उस गीत में समस्त लोक के व्यक्तित्व को उभारना होता है। लोकसाहित्य वस्तुतः जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा, जनता के लिये लिखा जाता है।
‘the poetry of the people, by the people, for the people.’’
अंग्रेजी में ‘फ़ोक’ का अर्थ है– लोक, राष्ट्र, जाति, सर्वसाधारण या वर्गविशेष।
इसीलिए folk song के अनुरूप हिन्दी में लोकसंज्ञा दी गई है। अंग्रेजी का folk song जर्मनी के volkslied का अपभंश है। समस्त मानव समाज में चेतन-अचेतन के रूप में जो भावनाएँ गीतबद्ध हुई हैं, उन्हें लोकगीत कहा जा सकता है। डॉ० बार्क ने ‘फ़ोक’ शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इससे सभ्यता के दूर रहने वाली किसी पूरी जाति का बोध होता है। ग्रिम का कथन है कि लोकगीत अपने आप बनते है–
‘‘a folk song composes itself.’’ –grimm
पेरी ने लिखा है कि लोकगीत आदिमानव का उल्लासमय संगीत है।
‘‘the primitive spontaneous music has been called folk-music.’’ –perey
राल्फ वी० विलियम्स का कथन है कि ‘‘लोकगीत न पुराना होता है न नया। वह तो जंगल के एक वृक्ष जैसा है, जिसकी जड़े तो दर ज़मीन से धँसी हुई हैं, परन्तु जिनमें निरन्तर नई-नई डालियाँ पल्लव और फल लगते हैं।’’
‘‘a folk song is neither new nor old, it is like a forest tree with its roots deeply buried in the past, but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits.’’
लोकगीत हमारे जीवन विकास की गाथा हैं। उनमें जीवन के सुख-दुःख मिलन-विरह, उतार-चढ़ाव की भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। सामाजिक रीति एवं कुरीतियों के भाव इन लोकगीतों में हैं। इनमें जीवन की सरल अनुभूतियों एवं भावों की गहराई है। श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का कहना है कि लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है।
लोकगीतों का विस्तार कहाँ तक है, इसे कोई नहीं बता सकता। किन्तु इनमें सदियों से चले आ रहे धार्मिक विश्वास एवं परम्पराएँ जीवित हैं। ये हृदय की गहराइयों से जन्मे हैं। श्रुतिपरम्परा से ये अपने विकास का मार्ग बनाते रहे हैं। अतः इनमें तर्क कम, भावना अधिक है। न इनमें छन्दशास्त्र की लौहश्रृंखला है, न अलंकारों की बोझिलता। इनमें तो लोकमानस का स्वच्छ और पावन गंगा-यमुना जैसा प्रवाह है। लोकगीतों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनमें सहज स्वाभाविकता एवं सरलता है। इनमें सुख-दुःख, प्रेम और करुणा के विविध रंग है। कहीं पुत्रजन्म के अवसर पर हर्ष-उल्लास के स्वर गूँजते हैं तो कहीं कन्या की विदाई या प्रियवियोग की बेला में करुणा के गीत मुखर होते हैं।
‘‘लोकगीतों में भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक और हृदय से निकली हुई लय के साथ होती है। हरे जंगलों में जैसे पंछी उन्मुक्त होकर गाते हैं, उसी प्रकार लोकगीत स्वाभाविक रीति से हृदय से फूटकर निकलते हैं। इनमें सरल काव्य होता है, भावों की खींचतान नहीं होती।’’
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में, ‘‘लोक हमारे जीवन का महासमुद्र हैं, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान संचित हैं। अर्वाचीन मानव के लिये लोक सर्वोच्च प्रजापति है।’’
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ‘लोक’ शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम से न लेकर नगरों व गाँवों में फैली उस समूची जनता से लिया है जो परिष्कृत, रुचिसंपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन की अभ्यस्त होती है।
डॉ० कुंजबिहारी दास ने लोकगीतों की परिभाषा देते हुए कहा है, ‘‘लोकसंगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है, जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक आदिम अवस्था में निवास करते हैं। यह साहित्य प्रायः मौखिक होता है और परम्परागत रूप से चला आ रहा है।’’
लोकगीतों को मात्र ग्रामगीत कहकर उनकी व्यापकता को कम नहीं किया जा सकता। ये गीत अब गाँव की चहारदीवारी को छोड़ नगरों और महानगरों की सीमा को छू रहे हैं। हिन्दी साहित्य कोश में ‘लोकगीत’ शब्द के तीन अर्थ किये गये हैं–
1. लोक में प्रचलित गीत,
2. लोकनिर्मित गीत तथा
3. लोकविषयक गीत।
किन्तु वास्तव में लोकगीत का तात्पर्य लोक में प्रचलित गीत ही है, जिसे दो अर्थ दिये जा सकते हैं–1. अवसरविशेष के प्रचलित गीत तथा 2. परम्परागत गीत।
लोक द्वारा निर्मित होने पर भी लोकगीत को किसी व्यक्तिविशेष से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि रचनाकार को उस गीत में समस्त लोक के व्यक्तित्व को उभारना होता है। लोकसाहित्य वस्तुतः जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा, जनता के लिये लिखा जाता है।
‘the poetry of the people, by the people, for the people.’’
अंग्रेजी में ‘फ़ोक’ का अर्थ है– लोक, राष्ट्र, जाति, सर्वसाधारण या वर्गविशेष।
इसीलिए folk song के अनुरूप हिन्दी में लोकसंज्ञा दी गई है। अंग्रेजी का folk song जर्मनी के volkslied का अपभंश है। समस्त मानव समाज में चेतन-अचेतन के रूप में जो भावनाएँ गीतबद्ध हुई हैं, उन्हें लोकगीत कहा जा सकता है। डॉ० बार्क ने ‘फ़ोक’ शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इससे सभ्यता के दूर रहने वाली किसी पूरी जाति का बोध होता है। ग्रिम का कथन है कि लोकगीत अपने आप बनते है–
‘‘a folk song composes itself.’’ –grimm
पेरी ने लिखा है कि लोकगीत आदिमानव का उल्लासमय संगीत है।
‘‘the primitive spontaneous music has been called folk-music.’’ –perey
राल्फ वी० विलियम्स का कथन है कि ‘‘लोकगीत न पुराना होता है न नया। वह तो जंगल के एक वृक्ष जैसा है, जिसकी जड़े तो दर ज़मीन से धँसी हुई हैं, परन्तु जिनमें निरन्तर नई-नई डालियाँ पल्लव और फल लगते हैं।’’
‘‘a folk song is neither new nor old, it is like a forest tree with its roots deeply buried in the past, but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits.’’
लोकगीत हमारे जीवन विकास की गाथा हैं। उनमें जीवन के सुख-दुःख मिलन-विरह, उतार-चढ़ाव की भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। सामाजिक रीति एवं कुरीतियों के भाव इन लोकगीतों में हैं। इनमें जीवन की सरल अनुभूतियों एवं भावों की गहराई है। श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का कहना है कि लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है।
लोकगीतों का विस्तार कहाँ तक है, इसे कोई नहीं बता सकता। किन्तु इनमें सदियों से चले आ रहे धार्मिक विश्वास एवं परम्पराएँ जीवित हैं। ये हृदय की गहराइयों से जन्मे हैं। श्रुतिपरम्परा से ये अपने विकास का मार्ग बनाते रहे हैं। अतः इनमें तर्क कम, भावना अधिक है। न इनमें छन्दशास्त्र की लौहश्रृंखला है, न अलंकारों की बोझिलता। इनमें तो लोकमानस का स्वच्छ और पावन गंगा-यमुना जैसा प्रवाह है। लोकगीतों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनमें सहज स्वाभाविकता एवं सरलता है। इनमें सुख-दुःख, प्रेम और करुणा के विविध रंग है। कहीं पुत्रजन्म के अवसर पर हर्ष-उल्लास के स्वर गूँजते हैं तो कहीं कन्या की विदाई या प्रियवियोग की बेला में करुणा के गीत मुखर होते हैं।
‘‘लोकगीतों में भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक और हृदय से निकली हुई लय के साथ होती है। हरे जंगलों में जैसे पंछी उन्मुक्त होकर गाते हैं, उसी प्रकार लोकगीत स्वाभाविक रीति से हृदय से फूटकर निकलते हैं। इनमें सरल काव्य होता है, भावों की खींचतान नहीं होती।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book