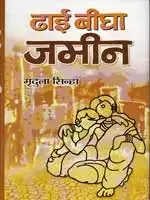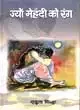|
कहानी संग्रह >> ढाई बीघा जमीन ढाई बीघा जमीनमृदुला सिन्हा
|
53 पाठक हैं |
||||||
समाज जीवन की ज्वलंत समस्याओं से रू-ब-रू कराती ये कहानियाँ पाठक की अंतःचेतना को झकझोरती हैं।
मनीष माँ के सुझाव पर आश्चर्य प्रकट कर गया।
‘‘हाँ, मैं ठीक कहती हूँ।’’
‘‘क्या ?’’ वह अनमना-सा बोला।
‘‘यही कि गाँव चलो। कम-से-कम तब तक जब तक मंदी रहे। देखना, फिर दिन बहुरेंगे तुम्हारे भी, पैकेट के भी। जिंदगी तो बितानी होती है, बेटा। पैकेज के सहारे या पुश्तैनी जमीन के सहारे, क्या फर्क पड़ता है।’’
मनीष ने हामी तो नहीं भरी थी, पर रात को माँ-बेटे दोनों को अच्छी नींद आई थी। सुबह का अखबार हाथ में लेकर मनीष गाँव जाने की योजना बना रहा था। उसके एक मित्र द्वारा आत्महत्या करने की खबर फोटो के साथ छपी थी। वह भी पैकेजवाला नौजवान था, शादीशुदा।
माँ चाय ले आई थी। मनीष लिपट गया माँ से। बोला, ‘‘माँ, चलो, अभी गाँव चलते हैं।’’
सुभद्रा बुदबुदाई थी, ‘‘कभी सुना था—जेवर संपत्ति का श्रृंगार और विपत्ति का आहार होता है। पर तुम्हारे लिए तो पुश्तैनी जमीन ही विपत्ति का आहार बन रही है। ढाई बीघा ही है तो क्या, तिनके का सहारा।’’
‘‘हाँ, मैं ठीक कहती हूँ।’’
‘‘क्या ?’’ वह अनमना-सा बोला।
‘‘यही कि गाँव चलो। कम-से-कम तब तक जब तक मंदी रहे। देखना, फिर दिन बहुरेंगे तुम्हारे भी, पैकेट के भी। जिंदगी तो बितानी होती है, बेटा। पैकेज के सहारे या पुश्तैनी जमीन के सहारे, क्या फर्क पड़ता है।’’
मनीष ने हामी तो नहीं भरी थी, पर रात को माँ-बेटे दोनों को अच्छी नींद आई थी। सुबह का अखबार हाथ में लेकर मनीष गाँव जाने की योजना बना रहा था। उसके एक मित्र द्वारा आत्महत्या करने की खबर फोटो के साथ छपी थी। वह भी पैकेजवाला नौजवान था, शादीशुदा।
माँ चाय ले आई थी। मनीष लिपट गया माँ से। बोला, ‘‘माँ, चलो, अभी गाँव चलते हैं।’’
सुभद्रा बुदबुदाई थी, ‘‘कभी सुना था—जेवर संपत्ति का श्रृंगार और विपत्ति का आहार होता है। पर तुम्हारे लिए तो पुश्तैनी जमीन ही विपत्ति का आहार बन रही है। ढाई बीघा ही है तो क्या, तिनके का सहारा।’’
—इसी संग्रह से
समाज जीवन की ज्वलंत समस्याओं से रू-ब-रू कराती ये कहानियाँ पाठक की
अंतःचेतना को झकझोरती हैं। ये व्यक्ति, परिवार और समाज को तोड़ती नहीं,
जोड़ती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जीवन-मंत्र लिये, संवेदना और मर्म से
भरपूर अत्यंत पठनीय कहानियाँ।
अनुक्रम
अक्षरा
फिर आज ढाढ़ मारकर किसी के रोने का करुण स्वर सुखिया की झुग्गी से मेरे
फ्लैट तक पहुँच ही गया। मैंने अपनी बालकनी से बगल की बालकनी में खड़ी
पड़ोसन की ओर प्रश्न उछाला, ‘‘अब क्या हुआ
?’’ प्रतिदिन चारों पहर झुग्गी से रोने-हँसने की आवाज
आती ही रहती है। दरअसल हमारे अपार्टमेंट के फ्लैटों से ऐसी कोई भी आवाज
झुग्गी तक क्या, अपने पड़ोस के फ्लैटों तक भी नहीं पहुँचती थी। यहाँ रुदन
और हँसी नितांत व्यक्तिगत ही होती है। कभी-कभी तो एक परिवार के बीच भी
नहीं बँटती। दुःख और सुख का आदान-प्रदान नहीं होता। एक स्थान पर जमा रहने
के कारण गहराई तक जाता है। घाव कर देता है, पर ये झुग्गियाँ हमें आज भी
सामाजिक प्राणी होने का एहसास कराती हैं, जहाँ दुःख और सुख सामूहिक होता
है, व्यक्तिगत नहीं।
‘‘होगा क्या, वही आपकी सुखिया है न, फिर नाटक कर रही है। मेरा शंभू दूध लेने गया था। सुखिया के घर के पास भीड़ देखकर रुक गया। लोग कह रहे थे—सुखिया ने फिर अपनी कोख पर मुक्के मारे हैं। वह मारती जा रही है, रोती जा रही है। न मुक्के मारना बंद करती है, न रोना। यह उसका नाटक नहीं तो और क्या है ?’’
मेरी पड़ोसन सुखिया पर उठी अपनी झल्लाहट मुझ पर उड़ेलती जा रही थी। पर मैं तो दस वर्ष पूर्व के कालखंड में पहुँच गई थी। तब मैं इस मुहल्ले में बसने आई ही थी। नया फ्लैट खरीदा था। इसलिए अपनी मित्रों के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने चली गई। वहाँ से लौटने पर जो शरीर की स्थिति सबकी होती है, मेरी भी हुई। मेरे साथ एक मास्टरजी रहते थे। मैंने कहा, ‘‘पास की झुग्गी-झोंपड़ी से किसी महिला को बुला लाइए। मुझे मालिश करवानी है।’’
वे झुग्गी के बाहर सड़क पर खड़े रहे। स्त्री, पुरुष और बच्चों का आना-जाना जारी था। शायद वे संकोच में थे कि अपने आमने-सामने और अगल-बगल से गुजरती महिलाओं से कैसे पूछें, ‘तुम मालिश कर सकती हो ?’
कहीं वे बुरा मान जाएँ ? फिर तो कहीं उनकी धुनाई हो जाए। वे इसी ऊहापोह में थे। एक महिला सिर पर घूँघट डाले खड़ी उनसे पूछ बैठी, ‘‘किसको खोज रहे हो, बाबू ? बहुत देर से खड़े हो।’’
‘‘मैं किसी को नहीं ढूँढ़ रहा। वह पास में जो नया फ्लैट बना है न, उसमें एक मैडम आई हैं। उन्हें मालिश करवानी है।’’
‘‘अरे, तो ऐसे बोलो न, चलो। मैं कर देती हूँ मालिश ! मुझे मालिश करनी आती है।’’
मास्टरजी खुश हो गए। उसे बुलाकर मेरे सामने खड़ा करते हुए एक जंग जीतने का ही एहसास छलका था उनके मुख पर। मैंने उसका नाम पूछा। उसने सुखिया बताया। मैंने अपना दर्द भरा शरीर उसके सुपुर्द कर दिया। उसने मालिश करते हुए अपना घूँघट थोडा सा ऊपर सरकाया।
काले रंग के कागज पर मानो किसी ने पतले कलम से आँख, भौंह, नाक और होंठों को उकेर दिया हो। लाल-लाल होठों के अंदर सुपुष्ट मक्के के बार पर जड़े सफेद-सफेद दाने। बदन के दर्द से परेशान मैं एक बार तो उसका पूरा चेहरा देख प्रफुल्ल हो उठी। रग-रग मे प्रफुल्लता फैलकर दर्द को दरकिनार कर गई। उसने भी मेरा भाव भाँप लिया। बोली, ‘‘क्या देखती हो, दीदी ?’’ प्रश्न इस लहजे में कि उसे ईश्वर द्वारा उकेरे अपने रूप और अपने द्वारा बड़ी बिंदी, सिंदूर, नाक में बड़े नग से सजे रंग के मिले-जुले प्रभाव का गुरूर नहीं तो अंदाज अवश्य था। मेरी सराहना के बाण रूपी नजरों से बिंधी वह अपना सुरूर प्रगट कर गई।
मैंने कहा, ‘‘कुछ नहीं। तुम मालिश करो।’’ उसे भी उस रूप-रंग से मेरे अभिभूत होने का अंदाजा लग गया था। उसने बड़े मनोयोग से मालिश प्रारंभ की। मुझे बड़ा सुखद लग रहा था। उसने बातों-बातों में बताया कि उसका एक पाँछ वर्ष का पप्पू है। वह झाँसी की रहनेवाली है। झुग्गी में उसके मायके के कई परिवार हैं। उसका आदमी उसे बहुत मानता है आदि-आदि। पहली भेंट में इतना परिचय काफी था। मालिश करनेवाली को बातों में उलझाए रखना भी एक विधा है। वरना मालिश जैसा बोझिल काम कोई क्यों करे ? पैसे के लिए पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी ब्यूटी पार्लर में मालिश करती हैं। सुखिया को भी बीस रुपए मिलने की उम्मीद थी।
उसके जाते समय मैंने कहा, ‘‘फिर कल इसी समय आना।’’
दूसरे दिन वह ठीक समय पर पहुँच गई। मेरे बदन पर उसके हाथ पड़ते ही मैंने पूछा, ‘‘तुम्हारा पप्पू कहाँ है ?’’
वह सुबकती हुई बोली, ‘‘आज फिर उसकी महतारी उठा ले गई। गाँव से उसका ससुर आया हुआ है।’’
‘‘क्या मतलब ? तुम अपने पप्पू की माँ नहीं हो ?’’ मैं चौंक गई थी।
‘‘हूँ न !’’
‘‘फिर उसकी महतारी उठा ले गई का क्या मतलब ?’’
‘‘दीदी ! अब मतलब-उतलब में मत फँसो। ईश्वर ने इस काया में सब अंग तो दिए। बस, कोख पत्थर की दे दी, जिसपर एक दूब भी न जमे। मेरी सास ने मुझे बाँझ कहकर उलाहना दिया। मैंने पास ही पड़े पत्थर उठाकर अपनी कोख पर मार लिया। फिर क्या था, दूसरे दिन दर्द शुरू हुआ। मेरा पति डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, ‘‘इसे बच्चा होने वाला है।’ उसने दवा भी दी। पर दवा खाने से पूर्व ही खून रिसना शुरू हो गया। बहुत रिसा। मैं बहुत रोती थी। मेरा पति मुझे दिल्ली ले आया। तब से यहीं कमाने-खाने लगी। बच्चा न होने की टीस तो मन में थी ही। एक वर्ष बाद अचानक एक दिन मेरी सास आ धमकी। फिर उलाहना, गाली ! मेरी भतीजी मेरे पास ही रहती थी। उसका दूसरा बेटा छह दिन का था। उसने मेरी सास के सामने मेरी गोद में बच्चा डालकर कहा, ‘‘लो बुआ, अपना पप्पू ! मैं गाँव जा रही हूँ।’’
मेरी सास आवाक् रह गई। अगर बुलाकर मेरी भतीजी ने मुझे अपने द्वारा गढ़ी कहानी सुनाई, ‘‘मेरा बच्चा हुआ। मेरी छाती में दूध नहीं उतरा। मेरी भतीजी का दो वर्ष का बच्चा भी अभी भी दूध पीता है। इसलिए छोटा भी उसे दे आई थी। अब उसको गाँव जाना है। मुझे ही रखना पड़ेगा।’’
मैंने शत-प्रतिशत सही शब्दों में उसके द्वारा गढ़ी कहानी अपनी सास को सुना दी। मेरा पति भी वहीं बैठा था। उसने भी सिर हिलाया। फिर तो मेरी झुग्गी पप्पू की किलकारियों से गूँज उठी। उसी रात हम मदनगीर से इस झोपड़ी में आ गए। बच्चा तो पल ही रहा था। पर मेरा कलेजा धक-धक करता रहता। कहीं रेशमा मुझसे छीनकर अपना बच्चा ले गई तो ?
यह विचार आते ही मैं अपने कलेजे से पप्पू को चिपका लेती। पप्पू हुँकारी भर देता। एक दिन ऐसा ही हुआ। रेशमा आ गई। बोली, ‘‘बुआ, मेरी बड़ी ननद दस दिनों के लिए आई हैं। उन्हें पता था कि मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था। वे इसे ढूँढ़ रही हैं। अब मैं यह तो नहीं कह सकती कि मेरा बच्चा नहीं रहा। ईश्वर करे मेरा बेटा मेरी भी आयु लेकर जीए। कोख तो मेरी ही है। बेटा भले तुम्हारा कहलाएगा। इसकी बुआ को दिखाना है। बुआ, मैं इसे ले जाती हूँ।’’ मैंने भी दे दिया। यह सिलसिला चलता रहा—उसके घर कोई गाँव से आए तो पप्पू उसका बेटा, मेरे घर कोई आए तो पप्पू मेरा बेटा !’’
लंबी कहानी कहती वह दोनों टाँगों की मालिश कर चुकी थी। पीठ की मालिश प्रारंभ करने के पूर्व वह रुकी। पीठ पर तेल डालते हुए बोली, ‘‘दीदीजी, अपनी कोख का जनमा तो अपना ही होता है। मैं अपने पप्पू को बड़े मन से रखती हूँ। दूध-फल भी खिलाती-पिलाती हूँ। दो घरों में चौका-बरतन करती हूँ। उनके घर भी बच्चे हैं। वे शर्ट-पैंट, जूते स्वेटर सब देती हैं। मैं भी होली-दिवाली पर पप्पू को नए कपड़े पहनाती रहती हूँ। पर बच्चा तो मेरी भतीजी का ही है न !’’
मेरी पीठ पर गरम जल की दो बूँद टपकीं। सुखिया ने बड़ी शीघ्रता से उन्हें अपनी साड़ी के आँचल से पोंछ दिया।
मैंने कहा, ‘‘सुखिया, तुम बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में जानती हो ?’’
उसने कहा, ‘‘हाँ ! किसी ने मुझे कहा था कि कागज बनवा लो। अब दीदीजी, आप ही सोचो। कागज पर लिख देने से मेरा बेटा कैसे होगा ? ईश्वर ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा। कोख में नहीं भरा तो मेरा बच्चा कैसे होगा ?’’ थोड़ा रुककर फिर बोली, ‘‘पर देखना दीदी, पप्पू उसके साथ नहीं रहेगा, कल ही भागकर आएगा। अपने प्यार से मैंने उसे बना लिया अपना बेटा, इसलिए लौट आएगा। देख लेना आप !’’
और उसने अपने अश्रुधार से ही अपने विश्वास को सींच लिया था। तभी तो दूसरे दिन घूँघट के नीचे से बत्तीसी झलकाती मेरे सामने खड़ी अपने विश्वास के फलित होने का इजहार कर रही थी। मेरी मालिश से प्रारंभ कर वह मेरे घर का झाड़ू-पोंछा भी करने लगी। कभी उसका रोना तो कभी हँसना जारी रहा। उसके भावों में उतार-चढ़ाव उसके पप्पू को लेकर ही होते थे।
उसका पप्पू विद्यालय जाने लगा। फिर तो पूछिए मत ! पप्पू को आज टिफिन में यह दिया, वह दिया। आज पप्पू का जुराब लेना है, आज जूते, कल स्कूल बैग तो स्कूल ड्रेस। मेरे घर का काम निबटाने की उसकी ड्यूटी थी, तो उसके पप्पू के बारे में कुछ-न-कुछ सुनना मेरा कर्तव्य। मेरी पोतियाँ भी बढ़ रही थीं। जब कभी अपनी पोती के बारे में कुछ बताऊँ, सुखिया के पप्पू की चर्चा प्रारंभ हो जाती। हमें सब मालूम था। सुखिया के पप्पू को अपनी माँ के हाथ की पूड़ियाँ पसंद थीं। सिलबट्टे पर पिसी धनिये की चटनी भी पप्पू को टिफिन में ब्रेड ले जाना अच्छा लगता था। दरअसल वह सपने में भी क्या बुदबुदाता था, हम सुनते रहते थे।
पर थोड़े ही दिनों में पप्पू अपने देवकी माँ के पास चला जाता। फिर लौट आता। उसके रहने, न रहने के अलग-अलग भाव सुखिया के मन और चेहरे पर अंकित रहते। उसके कार्य-कलापों में भी यह प्रकट होता। मालिश करते उसके हाथ की पकड़ बयाँ कर जाती कि, पप्पू उसके पास है या नहीं।
एक दिन सुखिया रोती-रोती कहने लगी, ‘‘दीदी ! अब तो बुढ़ापे की चिंता है। जीवन भर शरीर तोड़कर कमाया, मजदूरी भी की। दस-दस ईंट उठाकर चौथी मंजिल पर चढ़ जाती थी। अब तो घर का भी काम नहीं होता। शरीर गिरेगा तो कौन देखेगा ?’’
‘‘क्यों, पप्पू तो है न ! उसकी पत्नी देखेगी, और कौन ?’’
सुखिया चुप रही। पता नहीं क्या गुन-धुन रही होगी। मैंने भी नहीं छेड़ा। अपना काम समाप्त कर मेरे पास आई। बोली, ‘‘दीदी, बुढ़ापे की लाठी होते हैं बच्चे। पर अब तो आप लोगों के घर में भी बच्चे माँ-बाप के साथ नहीं रहते। आपका कमाया धन-जायदाद भी नहीं चाहिए उन्हें। मेरा पप्पू भी पढ़ रहा है। दसवीं पास कर गया है। पढ़-लिखकर तो मेरी झुग्गी में नहीं रहेगा। और मैं झुग्गी नहीं छोड़ूँगी, फिर मेरी सेवा कैसे करेगा ?’’
‘‘तुम इतना क्यों सोचती हो ? जो होगा, देखा जाएगा। मुझे देखो, मैं कहाँ चिंता करती हूँ !’’
‘‘आप क्यों करेंगी, दीदी ? आपके चार-चार बच्चे हैं, वे भी अपनी कोख-जाये। कोई-न-कोई देखेगा ही। मेरा तो एक ही है, वह भी कोख-जाया नहीं। दीदी ! अपनी कोख के ऊसर रह जाने की पीड़ा तो है ही। पप्पू के आ जाने के बाद भी यह पीड़ा नहीं जाती।’’
सुखिया को प्रसव-पीड़ा से वंचित रखकर ईश्वर का कुछ न बिगड़ा-बनता हो, मेरी सोच तो झकझोरी जाती थी। यह सच है कि एक बार प्रसव-पीड़ा झेल लेने पर उस पीड़ा की स्मृति जीवन भर सुखदायी ही होती है। किसी कुआँरी गर्भवती द्वारा गर्भपात करवाने की बात जब मेरी डॉक्टरनी पड़ोसन बताती, तो मैं बुदबुदाती, ‘‘हाय, वह बच्चा सुखिया की कोख में क्यों नहीं आया ?’’
उस दिन जब सुखिया आई, उसकी दोनों हथेलियाँ उसके पेड़ू पर थीं। वह मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं अखबार पढ़ रही थी। मैंने कहा, ‘‘खड़ी क्यों हो ? क्या आज काम नहीं करना ? फिर पप्पू के स्कूल जाना है ?’’
‘‘नहीं, ये खबर तो अखबार में नहीं छपी न, दीदी।’’
‘‘कौन सी खबर ?’’
‘‘होगा क्या, वही आपकी सुखिया है न, फिर नाटक कर रही है। मेरा शंभू दूध लेने गया था। सुखिया के घर के पास भीड़ देखकर रुक गया। लोग कह रहे थे—सुखिया ने फिर अपनी कोख पर मुक्के मारे हैं। वह मारती जा रही है, रोती जा रही है। न मुक्के मारना बंद करती है, न रोना। यह उसका नाटक नहीं तो और क्या है ?’’
मेरी पड़ोसन सुखिया पर उठी अपनी झल्लाहट मुझ पर उड़ेलती जा रही थी। पर मैं तो दस वर्ष पूर्व के कालखंड में पहुँच गई थी। तब मैं इस मुहल्ले में बसने आई ही थी। नया फ्लैट खरीदा था। इसलिए अपनी मित्रों के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने चली गई। वहाँ से लौटने पर जो शरीर की स्थिति सबकी होती है, मेरी भी हुई। मेरे साथ एक मास्टरजी रहते थे। मैंने कहा, ‘‘पास की झुग्गी-झोंपड़ी से किसी महिला को बुला लाइए। मुझे मालिश करवानी है।’’
वे झुग्गी के बाहर सड़क पर खड़े रहे। स्त्री, पुरुष और बच्चों का आना-जाना जारी था। शायद वे संकोच में थे कि अपने आमने-सामने और अगल-बगल से गुजरती महिलाओं से कैसे पूछें, ‘तुम मालिश कर सकती हो ?’
कहीं वे बुरा मान जाएँ ? फिर तो कहीं उनकी धुनाई हो जाए। वे इसी ऊहापोह में थे। एक महिला सिर पर घूँघट डाले खड़ी उनसे पूछ बैठी, ‘‘किसको खोज रहे हो, बाबू ? बहुत देर से खड़े हो।’’
‘‘मैं किसी को नहीं ढूँढ़ रहा। वह पास में जो नया फ्लैट बना है न, उसमें एक मैडम आई हैं। उन्हें मालिश करवानी है।’’
‘‘अरे, तो ऐसे बोलो न, चलो। मैं कर देती हूँ मालिश ! मुझे मालिश करनी आती है।’’
मास्टरजी खुश हो गए। उसे बुलाकर मेरे सामने खड़ा करते हुए एक जंग जीतने का ही एहसास छलका था उनके मुख पर। मैंने उसका नाम पूछा। उसने सुखिया बताया। मैंने अपना दर्द भरा शरीर उसके सुपुर्द कर दिया। उसने मालिश करते हुए अपना घूँघट थोडा सा ऊपर सरकाया।
काले रंग के कागज पर मानो किसी ने पतले कलम से आँख, भौंह, नाक और होंठों को उकेर दिया हो। लाल-लाल होठों के अंदर सुपुष्ट मक्के के बार पर जड़े सफेद-सफेद दाने। बदन के दर्द से परेशान मैं एक बार तो उसका पूरा चेहरा देख प्रफुल्ल हो उठी। रग-रग मे प्रफुल्लता फैलकर दर्द को दरकिनार कर गई। उसने भी मेरा भाव भाँप लिया। बोली, ‘‘क्या देखती हो, दीदी ?’’ प्रश्न इस लहजे में कि उसे ईश्वर द्वारा उकेरे अपने रूप और अपने द्वारा बड़ी बिंदी, सिंदूर, नाक में बड़े नग से सजे रंग के मिले-जुले प्रभाव का गुरूर नहीं तो अंदाज अवश्य था। मेरी सराहना के बाण रूपी नजरों से बिंधी वह अपना सुरूर प्रगट कर गई।
मैंने कहा, ‘‘कुछ नहीं। तुम मालिश करो।’’ उसे भी उस रूप-रंग से मेरे अभिभूत होने का अंदाजा लग गया था। उसने बड़े मनोयोग से मालिश प्रारंभ की। मुझे बड़ा सुखद लग रहा था। उसने बातों-बातों में बताया कि उसका एक पाँछ वर्ष का पप्पू है। वह झाँसी की रहनेवाली है। झुग्गी में उसके मायके के कई परिवार हैं। उसका आदमी उसे बहुत मानता है आदि-आदि। पहली भेंट में इतना परिचय काफी था। मालिश करनेवाली को बातों में उलझाए रखना भी एक विधा है। वरना मालिश जैसा बोझिल काम कोई क्यों करे ? पैसे के लिए पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी ब्यूटी पार्लर में मालिश करती हैं। सुखिया को भी बीस रुपए मिलने की उम्मीद थी।
उसके जाते समय मैंने कहा, ‘‘फिर कल इसी समय आना।’’
दूसरे दिन वह ठीक समय पर पहुँच गई। मेरे बदन पर उसके हाथ पड़ते ही मैंने पूछा, ‘‘तुम्हारा पप्पू कहाँ है ?’’
वह सुबकती हुई बोली, ‘‘आज फिर उसकी महतारी उठा ले गई। गाँव से उसका ससुर आया हुआ है।’’
‘‘क्या मतलब ? तुम अपने पप्पू की माँ नहीं हो ?’’ मैं चौंक गई थी।
‘‘हूँ न !’’
‘‘फिर उसकी महतारी उठा ले गई का क्या मतलब ?’’
‘‘दीदी ! अब मतलब-उतलब में मत फँसो। ईश्वर ने इस काया में सब अंग तो दिए। बस, कोख पत्थर की दे दी, जिसपर एक दूब भी न जमे। मेरी सास ने मुझे बाँझ कहकर उलाहना दिया। मैंने पास ही पड़े पत्थर उठाकर अपनी कोख पर मार लिया। फिर क्या था, दूसरे दिन दर्द शुरू हुआ। मेरा पति डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, ‘‘इसे बच्चा होने वाला है।’ उसने दवा भी दी। पर दवा खाने से पूर्व ही खून रिसना शुरू हो गया। बहुत रिसा। मैं बहुत रोती थी। मेरा पति मुझे दिल्ली ले आया। तब से यहीं कमाने-खाने लगी। बच्चा न होने की टीस तो मन में थी ही। एक वर्ष बाद अचानक एक दिन मेरी सास आ धमकी। फिर उलाहना, गाली ! मेरी भतीजी मेरे पास ही रहती थी। उसका दूसरा बेटा छह दिन का था। उसने मेरी सास के सामने मेरी गोद में बच्चा डालकर कहा, ‘‘लो बुआ, अपना पप्पू ! मैं गाँव जा रही हूँ।’’
मेरी सास आवाक् रह गई। अगर बुलाकर मेरी भतीजी ने मुझे अपने द्वारा गढ़ी कहानी सुनाई, ‘‘मेरा बच्चा हुआ। मेरी छाती में दूध नहीं उतरा। मेरी भतीजी का दो वर्ष का बच्चा भी अभी भी दूध पीता है। इसलिए छोटा भी उसे दे आई थी। अब उसको गाँव जाना है। मुझे ही रखना पड़ेगा।’’
मैंने शत-प्रतिशत सही शब्दों में उसके द्वारा गढ़ी कहानी अपनी सास को सुना दी। मेरा पति भी वहीं बैठा था। उसने भी सिर हिलाया। फिर तो मेरी झुग्गी पप्पू की किलकारियों से गूँज उठी। उसी रात हम मदनगीर से इस झोपड़ी में आ गए। बच्चा तो पल ही रहा था। पर मेरा कलेजा धक-धक करता रहता। कहीं रेशमा मुझसे छीनकर अपना बच्चा ले गई तो ?
यह विचार आते ही मैं अपने कलेजे से पप्पू को चिपका लेती। पप्पू हुँकारी भर देता। एक दिन ऐसा ही हुआ। रेशमा आ गई। बोली, ‘‘बुआ, मेरी बड़ी ननद दस दिनों के लिए आई हैं। उन्हें पता था कि मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था। वे इसे ढूँढ़ रही हैं। अब मैं यह तो नहीं कह सकती कि मेरा बच्चा नहीं रहा। ईश्वर करे मेरा बेटा मेरी भी आयु लेकर जीए। कोख तो मेरी ही है। बेटा भले तुम्हारा कहलाएगा। इसकी बुआ को दिखाना है। बुआ, मैं इसे ले जाती हूँ।’’ मैंने भी दे दिया। यह सिलसिला चलता रहा—उसके घर कोई गाँव से आए तो पप्पू उसका बेटा, मेरे घर कोई आए तो पप्पू मेरा बेटा !’’
लंबी कहानी कहती वह दोनों टाँगों की मालिश कर चुकी थी। पीठ की मालिश प्रारंभ करने के पूर्व वह रुकी। पीठ पर तेल डालते हुए बोली, ‘‘दीदीजी, अपनी कोख का जनमा तो अपना ही होता है। मैं अपने पप्पू को बड़े मन से रखती हूँ। दूध-फल भी खिलाती-पिलाती हूँ। दो घरों में चौका-बरतन करती हूँ। उनके घर भी बच्चे हैं। वे शर्ट-पैंट, जूते स्वेटर सब देती हैं। मैं भी होली-दिवाली पर पप्पू को नए कपड़े पहनाती रहती हूँ। पर बच्चा तो मेरी भतीजी का ही है न !’’
मेरी पीठ पर गरम जल की दो बूँद टपकीं। सुखिया ने बड़ी शीघ्रता से उन्हें अपनी साड़ी के आँचल से पोंछ दिया।
मैंने कहा, ‘‘सुखिया, तुम बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में जानती हो ?’’
उसने कहा, ‘‘हाँ ! किसी ने मुझे कहा था कि कागज बनवा लो। अब दीदीजी, आप ही सोचो। कागज पर लिख देने से मेरा बेटा कैसे होगा ? ईश्वर ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा। कोख में नहीं भरा तो मेरा बच्चा कैसे होगा ?’’ थोड़ा रुककर फिर बोली, ‘‘पर देखना दीदी, पप्पू उसके साथ नहीं रहेगा, कल ही भागकर आएगा। अपने प्यार से मैंने उसे बना लिया अपना बेटा, इसलिए लौट आएगा। देख लेना आप !’’
और उसने अपने अश्रुधार से ही अपने विश्वास को सींच लिया था। तभी तो दूसरे दिन घूँघट के नीचे से बत्तीसी झलकाती मेरे सामने खड़ी अपने विश्वास के फलित होने का इजहार कर रही थी। मेरी मालिश से प्रारंभ कर वह मेरे घर का झाड़ू-पोंछा भी करने लगी। कभी उसका रोना तो कभी हँसना जारी रहा। उसके भावों में उतार-चढ़ाव उसके पप्पू को लेकर ही होते थे।
उसका पप्पू विद्यालय जाने लगा। फिर तो पूछिए मत ! पप्पू को आज टिफिन में यह दिया, वह दिया। आज पप्पू का जुराब लेना है, आज जूते, कल स्कूल बैग तो स्कूल ड्रेस। मेरे घर का काम निबटाने की उसकी ड्यूटी थी, तो उसके पप्पू के बारे में कुछ-न-कुछ सुनना मेरा कर्तव्य। मेरी पोतियाँ भी बढ़ रही थीं। जब कभी अपनी पोती के बारे में कुछ बताऊँ, सुखिया के पप्पू की चर्चा प्रारंभ हो जाती। हमें सब मालूम था। सुखिया के पप्पू को अपनी माँ के हाथ की पूड़ियाँ पसंद थीं। सिलबट्टे पर पिसी धनिये की चटनी भी पप्पू को टिफिन में ब्रेड ले जाना अच्छा लगता था। दरअसल वह सपने में भी क्या बुदबुदाता था, हम सुनते रहते थे।
पर थोड़े ही दिनों में पप्पू अपने देवकी माँ के पास चला जाता। फिर लौट आता। उसके रहने, न रहने के अलग-अलग भाव सुखिया के मन और चेहरे पर अंकित रहते। उसके कार्य-कलापों में भी यह प्रकट होता। मालिश करते उसके हाथ की पकड़ बयाँ कर जाती कि, पप्पू उसके पास है या नहीं।
एक दिन सुखिया रोती-रोती कहने लगी, ‘‘दीदी ! अब तो बुढ़ापे की चिंता है। जीवन भर शरीर तोड़कर कमाया, मजदूरी भी की। दस-दस ईंट उठाकर चौथी मंजिल पर चढ़ जाती थी। अब तो घर का भी काम नहीं होता। शरीर गिरेगा तो कौन देखेगा ?’’
‘‘क्यों, पप्पू तो है न ! उसकी पत्नी देखेगी, और कौन ?’’
सुखिया चुप रही। पता नहीं क्या गुन-धुन रही होगी। मैंने भी नहीं छेड़ा। अपना काम समाप्त कर मेरे पास आई। बोली, ‘‘दीदी, बुढ़ापे की लाठी होते हैं बच्चे। पर अब तो आप लोगों के घर में भी बच्चे माँ-बाप के साथ नहीं रहते। आपका कमाया धन-जायदाद भी नहीं चाहिए उन्हें। मेरा पप्पू भी पढ़ रहा है। दसवीं पास कर गया है। पढ़-लिखकर तो मेरी झुग्गी में नहीं रहेगा। और मैं झुग्गी नहीं छोड़ूँगी, फिर मेरी सेवा कैसे करेगा ?’’
‘‘तुम इतना क्यों सोचती हो ? जो होगा, देखा जाएगा। मुझे देखो, मैं कहाँ चिंता करती हूँ !’’
‘‘आप क्यों करेंगी, दीदी ? आपके चार-चार बच्चे हैं, वे भी अपनी कोख-जाये। कोई-न-कोई देखेगा ही। मेरा तो एक ही है, वह भी कोख-जाया नहीं। दीदी ! अपनी कोख के ऊसर रह जाने की पीड़ा तो है ही। पप्पू के आ जाने के बाद भी यह पीड़ा नहीं जाती।’’
सुखिया को प्रसव-पीड़ा से वंचित रखकर ईश्वर का कुछ न बिगड़ा-बनता हो, मेरी सोच तो झकझोरी जाती थी। यह सच है कि एक बार प्रसव-पीड़ा झेल लेने पर उस पीड़ा की स्मृति जीवन भर सुखदायी ही होती है। किसी कुआँरी गर्भवती द्वारा गर्भपात करवाने की बात जब मेरी डॉक्टरनी पड़ोसन बताती, तो मैं बुदबुदाती, ‘‘हाय, वह बच्चा सुखिया की कोख में क्यों नहीं आया ?’’
उस दिन जब सुखिया आई, उसकी दोनों हथेलियाँ उसके पेड़ू पर थीं। वह मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं अखबार पढ़ रही थी। मैंने कहा, ‘‘खड़ी क्यों हो ? क्या आज काम नहीं करना ? फिर पप्पू के स्कूल जाना है ?’’
‘‘नहीं, ये खबर तो अखबार में नहीं छपी न, दीदी।’’
‘‘कौन सी खबर ?’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book