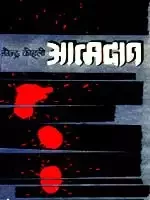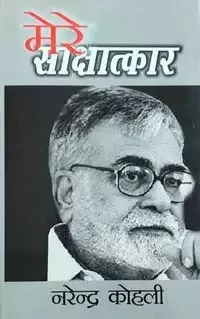|
उपन्यास >> आत्मदान आत्मदाननरेन्द्र कोहली
|
95 पाठक हैं |
||||||
आत्मदान
[१]
स्थाणीश्वर से अब वे बहुत दूर नहीं थे। यदि इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो
समय से स्थाणीश्वर पहुँच जाएँगे। मार्ग में रुकना पड़ा अथवा घोड़ा थक गया
तो विलंब होने की संभावना थी। अंधकार घिर आया तो इस गति से बढ़ना नहीं रह
जाएगा। राज्यवर्धन को देश के विरुद्ध ही नहीं काल के विरुद्ध भी दौड़ना
था।
सरपट भागते हुए घोड़े की गति को बिना धीमा किए, राज्यवर्धन ने पीछे मुड़ कर देखाः सेना और सेनापति पीछे छूट गये थे। पीछे तो वे बहुत पहले से ही छूटते जा रहे थे; क्रमशः अब वे इतनी दूर पीछे रह गए थे कि दिखाई भी नहीं दे रहे थे। आँखों पर बहुत बल देकर, दृष्टि को केंद्रित करने से, घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल की आँधी में छिटकी-छिटकी सी, धुंधली-धुंधली दो-एक आकृतियाँ अवश्य दिखाई पड़ती थीं, जो शायद खड्गग्राही और तांबूलिक की थीं....
पर राज्यवर्धन का मन गति को मंद करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं था। वह तो घोड़े से भी आगे उड़ा जा रहा था और घोड़े की मंद गति पर झुंझला रहा था। शायद ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य ने उड़न खटोले अथवा पुष्पक विमान जैसी चीजों की कल्पना की होगी-राज्यवर्धन सोच रहे थे-घोड़ों पर लंबी यात्राएँ सुखद नहीं हैं।...सुख ! व्यक्ति सुख की ओर भागता है; पर वे तो दुःख की ओर भाग रहे थे ! स्थाणीश्वर में क्या सुख शेष था अब ?....
सेना के पास बहुत सारा सामान था, शस्त्र थे, हाथी और बैल जैसे धीरे चलने वाले पशु थे। सेना उस गति से चल नहीं सकती थी, जिससे राज्यवर्धन चलना चाहते थे।............
उनकी स्थिति उस भारवाहक की-सी हो रही थी, जिसके सिर पर उसकी शारीरिक क्षमता से बहुत अधिक बोझ लाद दिया गया हो। उस बोझ के नीचे वह पिस रहा हो; किंतु भार उतारने की अनुमति उसे न हो। उस भारवाहक के पास अपनी पीड़ा कम करने का एक ही मार्ग था : वह अपनी यात्रा की अवधि को कम करे। अपनी गति को तेज से तेज करता चले, शीघ्र से शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुँच कर बोझ पटक दे........
पिता के देहांत की सूचना राज्यवर्धन के मन पर असह्य बोझ-सी चढ़ी बैठी थी, जैसे कोई विशालकाय हाथी उनके हृदय पर चारों पैर रख कर खड़ा हो गया हो...फिर मार्ग में ही माता के सती हो जाने की भी सूचना मिली थी।....हृदय पीड़ा के बोझ से दबा फट-सा रहा था। एक बार फट ही जाता तो इस यातना से तो मुक्ति मिलती। पर न वह फटा, न पीड़ा से निस्तार हुआ...वही बोझ राज्यवर्धन को भगाए लिए जा रहा था। बोझ का वह दबाव...फटता-सा हृदय...राज्यवर्धन मुक्ति के लिए लंबी साँस लेते। पर प्रत्येक साँस ही जैसे कशाघात करती, ‘भाग ! तेज ! और तेज !’...वे स्थाणीश्वर की ओर सरपट भागे जा रहे थे.............
.......पर स्थाणीश्वर जाकर ही क्या होगा? भार-वाहक तो अपने गंतव्य पर पहुँच कर, अपना भार पटक देता है। राज्यवर्धन अपनी पीड़ा कहाँ पटकेंगे ? हाँ ! हर्ष के कंधे पर अपना सिर टिका कर, खुल कर रो सकेंगे....निस्संकोच ! अपने छोटे भाई को अपनी बाँहों में भर कर, उसे अपने वक्ष से सटा, अपना बोझ हल्का करने के प्रयत्न करेंगे......
राज्यवर्धन ने एक ठंडी साँस छोड़ी।...घोड़ा वहशियों के समान भागा जा रहा था। उसकी गति भयंकर होती जा रही थी। तनिक सी भी अड़चन आने पर उसका संतुलन बिगड़ सकता था। ऐसी स्थिति में यदि राज्यवर्धन गिरे तो फिर जीवन की कोई आशा नहीं थी। घोड़ा क्षमता भर दौड़ने के पश्चात बेदम होकर भी गिर सकता था। ऐसे में घोड़े और सवार दोनों के ही प्राण जाएँगे।...पर क्या करना था राज्यवर्धन को इन प्राणों का। किसका भला हो रहा था इन प्राणों से। कष्ट ही तो पा रहे थे राज्यवर्धन। प्राण निकल जाएँ तो एक बार इस सारे कष्ट का अंत हो।...अच्छा है कि उनके साथ कोई नहीं है। अकेले थे तो घोड़ा इस प्रकार दौड़ाए लिए जा रहे थे। साथ कोई होता तो अवश्य ही उन्हें टोकता...पर ऐसे अवसर पर टोक-टाक उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें इस समय ऐसी ही गति चाहिए थी। मन से भी अधिक तीव्रगामी-अधिक हिंस्त्र, अधिक जोखिम वाली.......
राज्यवर्धन ने स्थाणीश्वर छोड़ा था तो पिता प्रभाकरवर्धन स्वस्थ और प्रसन्न थे। कितना उत्साह था उनमें पुत्र को रणक्षेत्र में भेजने का, जैसे यही उनके जीवन का लक्ष्य हो। कितने ओज भरे स्वर में उन्होंने कहा, ‘‘राज्यवर्धन !
पुत्र तुम्हारा शरीर अब कवच धारण करने योग्य हो गया है। इसका अर्थ समझते हो बेटा ?...क्षत्रिय-पुत्र का शरीर जब कवच धारण करने योग्य हो जाता है तो रणक्षेत्र ही उसका घर हो जाता है। स्थाणीश्वर में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम युद्धक्षेत्र में जाओ...’’
वे क्षण राज्यवर्धन के मन में आज भी पूरी तीव्रता से जीवित थे। समय का कुहरा उन्हें न फीका कर पाया था न धुँधला !...
पिता की बात सुनकर राज्वर्धन ने अपने मन को टटोला था। ...उन्हें कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि वे अब युद्ध के योग्य हो गए हैं। पिता के ओज ने भी उनके मन को तनिक नहीं छुआ था। शायद वह उत्साह उनमें था ही नहीं, जो उनके पिता और भाई के व्यक्तित्वों का केन्द्रबिन्दु था।...राज्यवर्धन का सारा संस्कार क्षत्रियों की भाँति हुआ था, किंतु उनमें क्षत्रिय-दर्प कभी नहीं जागा।...उनका शरीर सक्षम था और शस्त्र-विद्या भी उन्होंने सीखी थी, पर युद्ध में उनकी तनिक भी रूचि नहीं थी। युद्ध किसलिए ? कोई क्यों किसी को अपना शत्रु मानता है ? क्यों वह युद्धक्षेत्र में शवों का ढेर लगा देता है ? हत्या में भी कोई सुख होता है क्या ? किसी जीव का वध करने में क्या उपलब्धि है ? बहता हुआ रक्त देख कर राज्यवर्धन को कभी प्रसन्नता नहीं हुई।
तब भी उन्होंने अत्यन्त उदासीन भाव से पिता को निहारा था, ‘‘पिताजी ! यद्यपि आपने मेरा नाम राज्यवर्धन रखा है; किंतु मेरी न तो राज्य में कोई रुचि है, न राज्य के वर्धन में, युद्ध किसलिए पिताजी ? अपने ही जैसे मनुष्य के संहार के लिए ? क्षत्रिय किसलिए पिताजी ? क्षत्रिय का शरीर कवच धारण करने के योग्य क्या केवल इसलिए होता है कि वह युद्ध के नाम पर हत्याएँ करे ? जीवित मनुष्य को शवों अथवा पंगु, लुंज-पुंज, पीड़ित शरीरों में बदल दे।..नहीं पिताजी ! मनुष्यों के जीवन का, उसकी क्षमताओं का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए !’’
पिता ने पुत्र के चेहरे को क्षण भर देखा : हाँ ! उन्होंने ठीक ही समझा था। पुत्र वयस्क हो गया था। उसका शरीर कवच-धारण करने योग्य हो गया था तो उसका मस्तिष्क पिता से तर्क करने में भी समर्थ हो चुका था.....
पर इसकी प्रसन्नता नहीं हुई थी प्रभाकरवर्धन को। उन्होंने अपने पुत्रों की मानसिक परिपक्वता इस ओर नहीं चाही थी। यह मानसिकता क्षत्रियों के अनुकूल नहीं थी। कहीं बौद्ध भिक्षुओं का प्रभाव तो नहीं पड़ गया उनके पुत्र पर ! प्रभाकरवर्धन ने अपने बच्चों को शैव संस्कार दिए थे। अहिंसा में उनकी कोई निष्ठा नहीं थी।
‘‘नहीं !’’पिता का मुख तेज से तमतमा उठा था, ‘‘क्षत्रिय हत्या के लिए शस्त्र धारण नहीं करता। वह शस्त्र धारण करता है लोक-कल्याण के लिए, आर्त-त्राण के लिए, निर्बल की रक्षा के लिए।’’ उन्होंने राज्यवर्धन के कंधों पर हाथ रख सीधे उनकी आँखों में देखा, ‘‘पुत्र ! मैं तुम्हें अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध में नहीं भेज रहा हूँ। तुम्हें भेजा जा रहा है, हूणों के संहार के लिए। हूणों को अभी तुम नहीं जानते पुत्र ! वे बर्बरता और राक्षसत्व की सीमा हैं। मानव-पीड़न उनका मनोरंजन है।’’पिता रुक कर कुछ सोचते रहे थे, और तब आवेश के साथ उन्होंने कहा था, ‘‘प्रसिद्ध हूण मिहिरकुल का नाम तुमने सुना होगा पुत्र ! उसी की बात कहता हूँ........’’
पिता ने मिहिरकुल के विषय में अनेक घटनाएँ सुनाई थीं। वे घटनाएँ साधारण नहीं थीं : वे तो तपे हुए लोहे की सलाखें थीं, जिसे छू जाएँ उसकी त्वचा जला डालें; अपने ऐसे चिन्ह छोड़ जाएँ, जो कभी न मिटें। ...वे घटनाएँ आज भी राज्यवर्धन की आँखों के सम्मुख प्रत्यक्ष, जीवन्त घटनाओँ के समान दृश्यमान थीं.......
...मिहिरकुल अपनी विजय-वाहिनी के साथ उत्तर काश्मीर में पंचालधारा पर्वत-मार्ग पर हस्तिवंज पहुँचा था।
मार्ग सँकरा था, सेना विशाल थी। कुछ पशुओं में परस्पर भिड़ंत हो गई। किसी का ध्यान उस ओर नहीं था। साधारण-सी घटना थी। जहाँ इतने पशु एक साथ चल रहें हों, वहाँ एक का दूसरे के साथ भिड़ जाना बड़ी बात थी भी नहीं। किंतु वहाँ भाग-दौड़ के लिए अधिक स्थान नहीं था। महावत निकट थे नहीं और पशुओं की भिड़ंत उग्र हो उठी। अनेक भयंकर युद्घक-गज अपना संतुलन खो बैठे। पैर फिसला और वे सैकड़ों हाथ गहरे सीधे खड्ड में गिरे। हाथियों का भार अधिक था और खड्ड गहरी थी।
गिरने का वेग अद्भुत तीव्रता पकड़ गया, जैसे स्वयं न गिरे हों किसी असाधारण शक्तिशाली जीव ने उन्हें अपनी अलौकिक शक्ति से उठा कर पटक दिया हो। मार्ग की ऊबड़-खाबड़ चट्टानों से रगड़ खाते हाथियों के शरीर, चोट की पीड़ा और आसन्न मृत्यु के भय से उत्पन्न अपनी चिंघाड़ों से खड्ड के कण-कण को कँपा रहे थे...
हाथियों की देख-भाल करने वाले पशुओं की पीड़ा से विगलित और मिहिरकुल के भय से जड़ हो गए।
सेनापतियों ने भयभीत दृष्टि से मिहिरकुल की ओर देखा ! इस क्षति से जाने राजा कितना क्रुद्ध हो। संभव था, मिहिरकुल उन हाथियों के महावतों को, उनकी असावधानी का दंड देने के लिए, उसी खड्ड में पशुओं के ही समान, फिंकवा दे...
मिहिरकुल ने भी खड्ड में गिरे हाथियों का करुण आर्तनाद सुना। पीड़ा और मृत्यु का साक्षात नाद सुन कर उसकी आँखें विस्मय से कुछ बड़ी हो आईं। वह अद्भुत सुख से रोमांचित हो उठा। इतने विराट पशु इस प्रकार कष्ट से तड़प कर दिल दहला देने वाला शब्द करते हैं। उसे यह शब्द बहुत भाया था। सैकड़ों हाथ नीचे गर्त लुंज-पुंज, अंग-भंग, रक्त-लुंठित हाथियों का रुदन, उनका क्रंदन-चीत्कार, उनका अपने पैर तथा सूँड़ उठा-उठा कर पटकना, सूँड़ उठा कर सहायता के लिए चीत्कार करना-मिहिरकुल ने उनकी एक-एक प्रक्रिया को बड़ी सरस रुचि से आनन्दपूर्वक देखा था। उन दीर्घाकार प्राणियों की यातनामयी मृत्यु ने उसके लिए अच्छा मनोविनोद प्रस्तुत किया था। वे युद्धक-गज असह्य पीड़ा से मूर्च्छित हुए। उन्होंने अंतिम साँस ली, उनके चारों पैर और सूँड़ क्रमशः स्थिर और ठंडे हो गए। एक बार वे अंतिम रूप से काँपे और सदा के लिए शांत हो गए।
एक-एक कर, सारे हाथी यातना-भरी मृत्यु के पार उतरते गए। मिहिरकुल अपने मुख-मंडल पर क्रूर आनन्द के भाव लिए एकटक उनको देखता रहा।...आर्त ध्वनि जब एकदम शांत हो गई तो जैसे उसके हाथ में आई कोई चीज छिन गई। वह वंचित हो उठा। उसको कुछ ऐसी निराशा हुई, जैसे किसी बच्चे को अपना कोई आकर्षक खेल, अपेक्षा से बहुत पहले पूरा हो जाने से होती है...
पर वह बच्चा नहीं था। वह मिहिरकुल था : और समर्थ और शक्तिशाली। वह वंचित नहीं रह सकता था। वह अपनी इच्छाएँ पूरी करनी जानता था। आर्त ध्वनि सुनने की उसकी क्रूर कामना अतृप्त थी।
सरपट भागते हुए घोड़े की गति को बिना धीमा किए, राज्यवर्धन ने पीछे मुड़ कर देखाः सेना और सेनापति पीछे छूट गये थे। पीछे तो वे बहुत पहले से ही छूटते जा रहे थे; क्रमशः अब वे इतनी दूर पीछे रह गए थे कि दिखाई भी नहीं दे रहे थे। आँखों पर बहुत बल देकर, दृष्टि को केंद्रित करने से, घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल की आँधी में छिटकी-छिटकी सी, धुंधली-धुंधली दो-एक आकृतियाँ अवश्य दिखाई पड़ती थीं, जो शायद खड्गग्राही और तांबूलिक की थीं....
पर राज्यवर्धन का मन गति को मंद करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं था। वह तो घोड़े से भी आगे उड़ा जा रहा था और घोड़े की मंद गति पर झुंझला रहा था। शायद ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य ने उड़न खटोले अथवा पुष्पक विमान जैसी चीजों की कल्पना की होगी-राज्यवर्धन सोच रहे थे-घोड़ों पर लंबी यात्राएँ सुखद नहीं हैं।...सुख ! व्यक्ति सुख की ओर भागता है; पर वे तो दुःख की ओर भाग रहे थे ! स्थाणीश्वर में क्या सुख शेष था अब ?....
सेना के पास बहुत सारा सामान था, शस्त्र थे, हाथी और बैल जैसे धीरे चलने वाले पशु थे। सेना उस गति से चल नहीं सकती थी, जिससे राज्यवर्धन चलना चाहते थे।............
उनकी स्थिति उस भारवाहक की-सी हो रही थी, जिसके सिर पर उसकी शारीरिक क्षमता से बहुत अधिक बोझ लाद दिया गया हो। उस बोझ के नीचे वह पिस रहा हो; किंतु भार उतारने की अनुमति उसे न हो। उस भारवाहक के पास अपनी पीड़ा कम करने का एक ही मार्ग था : वह अपनी यात्रा की अवधि को कम करे। अपनी गति को तेज से तेज करता चले, शीघ्र से शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुँच कर बोझ पटक दे........
पिता के देहांत की सूचना राज्यवर्धन के मन पर असह्य बोझ-सी चढ़ी बैठी थी, जैसे कोई विशालकाय हाथी उनके हृदय पर चारों पैर रख कर खड़ा हो गया हो...फिर मार्ग में ही माता के सती हो जाने की भी सूचना मिली थी।....हृदय पीड़ा के बोझ से दबा फट-सा रहा था। एक बार फट ही जाता तो इस यातना से तो मुक्ति मिलती। पर न वह फटा, न पीड़ा से निस्तार हुआ...वही बोझ राज्यवर्धन को भगाए लिए जा रहा था। बोझ का वह दबाव...फटता-सा हृदय...राज्यवर्धन मुक्ति के लिए लंबी साँस लेते। पर प्रत्येक साँस ही जैसे कशाघात करती, ‘भाग ! तेज ! और तेज !’...वे स्थाणीश्वर की ओर सरपट भागे जा रहे थे.............
.......पर स्थाणीश्वर जाकर ही क्या होगा? भार-वाहक तो अपने गंतव्य पर पहुँच कर, अपना भार पटक देता है। राज्यवर्धन अपनी पीड़ा कहाँ पटकेंगे ? हाँ ! हर्ष के कंधे पर अपना सिर टिका कर, खुल कर रो सकेंगे....निस्संकोच ! अपने छोटे भाई को अपनी बाँहों में भर कर, उसे अपने वक्ष से सटा, अपना बोझ हल्का करने के प्रयत्न करेंगे......
राज्यवर्धन ने एक ठंडी साँस छोड़ी।...घोड़ा वहशियों के समान भागा जा रहा था। उसकी गति भयंकर होती जा रही थी। तनिक सी भी अड़चन आने पर उसका संतुलन बिगड़ सकता था। ऐसी स्थिति में यदि राज्यवर्धन गिरे तो फिर जीवन की कोई आशा नहीं थी। घोड़ा क्षमता भर दौड़ने के पश्चात बेदम होकर भी गिर सकता था। ऐसे में घोड़े और सवार दोनों के ही प्राण जाएँगे।...पर क्या करना था राज्यवर्धन को इन प्राणों का। किसका भला हो रहा था इन प्राणों से। कष्ट ही तो पा रहे थे राज्यवर्धन। प्राण निकल जाएँ तो एक बार इस सारे कष्ट का अंत हो।...अच्छा है कि उनके साथ कोई नहीं है। अकेले थे तो घोड़ा इस प्रकार दौड़ाए लिए जा रहे थे। साथ कोई होता तो अवश्य ही उन्हें टोकता...पर ऐसे अवसर पर टोक-टाक उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें इस समय ऐसी ही गति चाहिए थी। मन से भी अधिक तीव्रगामी-अधिक हिंस्त्र, अधिक जोखिम वाली.......
राज्यवर्धन ने स्थाणीश्वर छोड़ा था तो पिता प्रभाकरवर्धन स्वस्थ और प्रसन्न थे। कितना उत्साह था उनमें पुत्र को रणक्षेत्र में भेजने का, जैसे यही उनके जीवन का लक्ष्य हो। कितने ओज भरे स्वर में उन्होंने कहा, ‘‘राज्यवर्धन !
पुत्र तुम्हारा शरीर अब कवच धारण करने योग्य हो गया है। इसका अर्थ समझते हो बेटा ?...क्षत्रिय-पुत्र का शरीर जब कवच धारण करने योग्य हो जाता है तो रणक्षेत्र ही उसका घर हो जाता है। स्थाणीश्वर में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम युद्धक्षेत्र में जाओ...’’
वे क्षण राज्यवर्धन के मन में आज भी पूरी तीव्रता से जीवित थे। समय का कुहरा उन्हें न फीका कर पाया था न धुँधला !...
पिता की बात सुनकर राज्वर्धन ने अपने मन को टटोला था। ...उन्हें कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि वे अब युद्ध के योग्य हो गए हैं। पिता के ओज ने भी उनके मन को तनिक नहीं छुआ था। शायद वह उत्साह उनमें था ही नहीं, जो उनके पिता और भाई के व्यक्तित्वों का केन्द्रबिन्दु था।...राज्यवर्धन का सारा संस्कार क्षत्रियों की भाँति हुआ था, किंतु उनमें क्षत्रिय-दर्प कभी नहीं जागा।...उनका शरीर सक्षम था और शस्त्र-विद्या भी उन्होंने सीखी थी, पर युद्ध में उनकी तनिक भी रूचि नहीं थी। युद्ध किसलिए ? कोई क्यों किसी को अपना शत्रु मानता है ? क्यों वह युद्धक्षेत्र में शवों का ढेर लगा देता है ? हत्या में भी कोई सुख होता है क्या ? किसी जीव का वध करने में क्या उपलब्धि है ? बहता हुआ रक्त देख कर राज्यवर्धन को कभी प्रसन्नता नहीं हुई।
तब भी उन्होंने अत्यन्त उदासीन भाव से पिता को निहारा था, ‘‘पिताजी ! यद्यपि आपने मेरा नाम राज्यवर्धन रखा है; किंतु मेरी न तो राज्य में कोई रुचि है, न राज्य के वर्धन में, युद्ध किसलिए पिताजी ? अपने ही जैसे मनुष्य के संहार के लिए ? क्षत्रिय किसलिए पिताजी ? क्षत्रिय का शरीर कवच धारण करने के योग्य क्या केवल इसलिए होता है कि वह युद्ध के नाम पर हत्याएँ करे ? जीवित मनुष्य को शवों अथवा पंगु, लुंज-पुंज, पीड़ित शरीरों में बदल दे।..नहीं पिताजी ! मनुष्यों के जीवन का, उसकी क्षमताओं का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए !’’
पिता ने पुत्र के चेहरे को क्षण भर देखा : हाँ ! उन्होंने ठीक ही समझा था। पुत्र वयस्क हो गया था। उसका शरीर कवच-धारण करने योग्य हो गया था तो उसका मस्तिष्क पिता से तर्क करने में भी समर्थ हो चुका था.....
पर इसकी प्रसन्नता नहीं हुई थी प्रभाकरवर्धन को। उन्होंने अपने पुत्रों की मानसिक परिपक्वता इस ओर नहीं चाही थी। यह मानसिकता क्षत्रियों के अनुकूल नहीं थी। कहीं बौद्ध भिक्षुओं का प्रभाव तो नहीं पड़ गया उनके पुत्र पर ! प्रभाकरवर्धन ने अपने बच्चों को शैव संस्कार दिए थे। अहिंसा में उनकी कोई निष्ठा नहीं थी।
‘‘नहीं !’’पिता का मुख तेज से तमतमा उठा था, ‘‘क्षत्रिय हत्या के लिए शस्त्र धारण नहीं करता। वह शस्त्र धारण करता है लोक-कल्याण के लिए, आर्त-त्राण के लिए, निर्बल की रक्षा के लिए।’’ उन्होंने राज्यवर्धन के कंधों पर हाथ रख सीधे उनकी आँखों में देखा, ‘‘पुत्र ! मैं तुम्हें अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध में नहीं भेज रहा हूँ। तुम्हें भेजा जा रहा है, हूणों के संहार के लिए। हूणों को अभी तुम नहीं जानते पुत्र ! वे बर्बरता और राक्षसत्व की सीमा हैं। मानव-पीड़न उनका मनोरंजन है।’’पिता रुक कर कुछ सोचते रहे थे, और तब आवेश के साथ उन्होंने कहा था, ‘‘प्रसिद्ध हूण मिहिरकुल का नाम तुमने सुना होगा पुत्र ! उसी की बात कहता हूँ........’’
पिता ने मिहिरकुल के विषय में अनेक घटनाएँ सुनाई थीं। वे घटनाएँ साधारण नहीं थीं : वे तो तपे हुए लोहे की सलाखें थीं, जिसे छू जाएँ उसकी त्वचा जला डालें; अपने ऐसे चिन्ह छोड़ जाएँ, जो कभी न मिटें। ...वे घटनाएँ आज भी राज्यवर्धन की आँखों के सम्मुख प्रत्यक्ष, जीवन्त घटनाओँ के समान दृश्यमान थीं.......
...मिहिरकुल अपनी विजय-वाहिनी के साथ उत्तर काश्मीर में पंचालधारा पर्वत-मार्ग पर हस्तिवंज पहुँचा था।
मार्ग सँकरा था, सेना विशाल थी। कुछ पशुओं में परस्पर भिड़ंत हो गई। किसी का ध्यान उस ओर नहीं था। साधारण-सी घटना थी। जहाँ इतने पशु एक साथ चल रहें हों, वहाँ एक का दूसरे के साथ भिड़ जाना बड़ी बात थी भी नहीं। किंतु वहाँ भाग-दौड़ के लिए अधिक स्थान नहीं था। महावत निकट थे नहीं और पशुओं की भिड़ंत उग्र हो उठी। अनेक भयंकर युद्घक-गज अपना संतुलन खो बैठे। पैर फिसला और वे सैकड़ों हाथ गहरे सीधे खड्ड में गिरे। हाथियों का भार अधिक था और खड्ड गहरी थी।
गिरने का वेग अद्भुत तीव्रता पकड़ गया, जैसे स्वयं न गिरे हों किसी असाधारण शक्तिशाली जीव ने उन्हें अपनी अलौकिक शक्ति से उठा कर पटक दिया हो। मार्ग की ऊबड़-खाबड़ चट्टानों से रगड़ खाते हाथियों के शरीर, चोट की पीड़ा और आसन्न मृत्यु के भय से उत्पन्न अपनी चिंघाड़ों से खड्ड के कण-कण को कँपा रहे थे...
हाथियों की देख-भाल करने वाले पशुओं की पीड़ा से विगलित और मिहिरकुल के भय से जड़ हो गए।
सेनापतियों ने भयभीत दृष्टि से मिहिरकुल की ओर देखा ! इस क्षति से जाने राजा कितना क्रुद्ध हो। संभव था, मिहिरकुल उन हाथियों के महावतों को, उनकी असावधानी का दंड देने के लिए, उसी खड्ड में पशुओं के ही समान, फिंकवा दे...
मिहिरकुल ने भी खड्ड में गिरे हाथियों का करुण आर्तनाद सुना। पीड़ा और मृत्यु का साक्षात नाद सुन कर उसकी आँखें विस्मय से कुछ बड़ी हो आईं। वह अद्भुत सुख से रोमांचित हो उठा। इतने विराट पशु इस प्रकार कष्ट से तड़प कर दिल दहला देने वाला शब्द करते हैं। उसे यह शब्द बहुत भाया था। सैकड़ों हाथ नीचे गर्त लुंज-पुंज, अंग-भंग, रक्त-लुंठित हाथियों का रुदन, उनका क्रंदन-चीत्कार, उनका अपने पैर तथा सूँड़ उठा-उठा कर पटकना, सूँड़ उठा कर सहायता के लिए चीत्कार करना-मिहिरकुल ने उनकी एक-एक प्रक्रिया को बड़ी सरस रुचि से आनन्दपूर्वक देखा था। उन दीर्घाकार प्राणियों की यातनामयी मृत्यु ने उसके लिए अच्छा मनोविनोद प्रस्तुत किया था। वे युद्धक-गज असह्य पीड़ा से मूर्च्छित हुए। उन्होंने अंतिम साँस ली, उनके चारों पैर और सूँड़ क्रमशः स्थिर और ठंडे हो गए। एक बार वे अंतिम रूप से काँपे और सदा के लिए शांत हो गए।
एक-एक कर, सारे हाथी यातना-भरी मृत्यु के पार उतरते गए। मिहिरकुल अपने मुख-मंडल पर क्रूर आनन्द के भाव लिए एकटक उनको देखता रहा।...आर्त ध्वनि जब एकदम शांत हो गई तो जैसे उसके हाथ में आई कोई चीज छिन गई। वह वंचित हो उठा। उसको कुछ ऐसी निराशा हुई, जैसे किसी बच्चे को अपना कोई आकर्षक खेल, अपेक्षा से बहुत पहले पूरा हो जाने से होती है...
पर वह बच्चा नहीं था। वह मिहिरकुल था : और समर्थ और शक्तिशाली। वह वंचित नहीं रह सकता था। वह अपनी इच्छाएँ पूरी करनी जानता था। आर्त ध्वनि सुनने की उसकी क्रूर कामना अतृप्त थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book