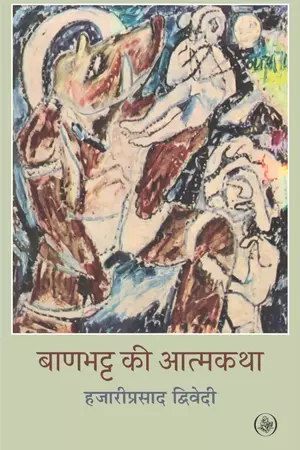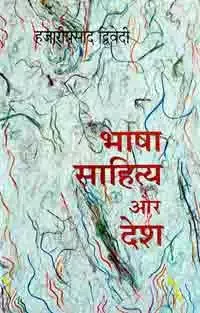|
उपन्यास >> बाणभट्ट की आत्मकथा (अजिल्द) बाणभट्ट की आत्मकथा (अजिल्द)हजारी प्रसाद द्विवेदी
|
356 पाठक हैं |
|||||||
बाणभट्ट द्वारा अपने महाकाव्य "हर्षचरित" में समाप्त भूमिका के रूप में दी गई है। इसमें वराह अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, जिसके द्वारा कवि अपने काव्य का समाप्ति करता है।
Banbhatt Ki Aatamkatha -A Hindi Book by Hazariprasad Dwivedi - बाणभट्ट की आत्मकथा - हजारीप्रसाद द्विवेदी
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथा-कृति होते हुए भी महाकाव्य की गरिमा से पूर्ण है। इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन-सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथा-भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रसमय साक्षात्कार कराती है। इसमें वह वाणी मुखरित है जो सामगान के समान पवित्र और अर्थपूर्ण है: ‘सत्य के लिए किसी न डरना, गुरू से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं।’
बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानायक कोरा भावुक कवि नहीं वरन् कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन-योद्धा है। उसके लिए ‘शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का एक ढेला नहीं, बल्कि ‘उससे बड़ा’ है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। ‘अपने को निशेष भाव से दे देने’ में जीवन की सार्थकता देखनेवाली निउनिया और ‘सबकुछ भूल जाने की साधना’ में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वरण कर लेता है तो यही गूँज अंत में रह जाती है-‘‘वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म कराके ही कवि गौरव का अनुभव करे।
बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानायक कोरा भावुक कवि नहीं वरन् कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन-योद्धा है। उसके लिए ‘शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का एक ढेला नहीं, बल्कि ‘उससे बड़ा’ है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। ‘अपने को निशेष भाव से दे देने’ में जीवन की सार्थकता देखनेवाली निउनिया और ‘सबकुछ भूल जाने की साधना’ में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वरण कर लेता है तो यही गूँज अंत में रह जाती है-‘‘वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म कराके ही कवि गौरव का अनुभव करे।
ततः समुत्क्षिप्य धरां स्वदंष्ट्रया
महावराहः स्फुट—पद्मलोचनः।
रसातलादुत्पल – पत्र- सन्निभः
समुत्थितो नील इवाचलो महान्।।
जलौघमग्ना सचराचरा धरा
विषाणकोट्याऽशिलविश्वमूर्त्तिना।
समुद्धृता येन वराहरूपिणा
स मे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु।।
महावराहः स्फुट—पद्मलोचनः।
रसातलादुत्पल – पत्र- सन्निभः
समुत्थितो नील इवाचलो महान्।।
जलौघमग्ना सचराचरा धरा
विषाणकोट्याऽशिलविश्वमूर्त्तिना।
समुद्धृता येन वराहरूपिणा
स मे स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु।।
बाणभट्ट की ‘आत्मकथा’ कथामुख
बाणभट्ट की ‘आत्मकथा’ के प्रकाशित होने के पूर्व उसका थोड़ा इतिहास जान लेना आवश्यक है। मिस कैथराइन आस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई-परिवार की कन्या है। यद्यपि वे अभी तक जीवित हैं; पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है, और पिछले पाँच वर्षों में मुझे उनकी केवल एक ही चिट्ठी मिली है, जो इस लेख से संबद्ध होने के कारण अंत में छाप दी गई है। मिस कैथराइन का भारती विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था अपने देश में रहते ही उन्होंने संस्कृत और ईसाई-हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। 68 वर्ष की उम्र में वे इस देश में आईं और अक्लांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का आठ वर्ष तक लगातार भ्रमण करती रहीं। यहाँ आकर उन्होंने बँगला का भी अभ्यास किया था !; पर इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई और आगे होने की कोई विशेष संभावना भी नहीं है। मिस कैथराइन को हम लोग ‘दीदी’ कहते थे —दीदी अर्थात् दादी। आगे जब कभी ‘दीदी’ शब्द का प्रयोग किया जाए, तो पाठक उन्ही से तात्पर्य समझें। बंगला में दादी के साथ मज़ाक करने का रिवाज है, दीदी इस बात को जानती थीं और कभी-कभी बड़ा करारा मजाक कर बैठती थीं। हम लोगों पर विशेषकर मेरे ऊपर—दीदी का स्नेह नाती के समान ही था। दीदी बहुत भोली थीं। अपनी कष्टसाध्य यात्राओं के बाद जब इधर लौटतीं तो हम लोगों के आमंद कता ठिकाना न रहता। नई बात सुनने के लिए या नई चीज देखने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक-एक करके, कभी कोई तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर की चित्रित काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकालकर हमारे हाथों पर रखती जातीं और उनका इतिहास सुनाती जातीं। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से् गद्गद होता और उनकी छोटी –छोटी नीली आँखें पानी से भरी होतीं फिर धीरे-से जेब से एक सफेद बिल्ली का बच्चा निकलता – बिलकुल सिकुड़ा हुआ। हम लोग इस मजाक से परिचित थे। दीदी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़ी उत्सुक्ता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता, मानो कोई बस्तलिखित पोथी ले रहा हो। और तब वह बिलौटा कूद जाता और हम लोग मानो अचकटाकर डर जाते। फिर दीदी इतना हँसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षातिरेक का परिणाम यह होता कि यार लोग संगृहीत बहुमूल्य वस्तुओं मे से कुछ को दबा जाते। (मैंने कभी ऐसा अपकर्म नहीं किया !) पर दीदी को पता भी नहीं चलता। कभी-कभी दीदी जब ध्यानावस्थ हो जातीं, तो इनका वलीकरुचित मुखमंडल बहुत ही आकर्षक होता। ऐसा जान पड़ता कि साक्षात् सरस्वती आविर्भूत हुई हैं। ऊधम करते हुए छोकरे पास से निकल जाते, धूल उड़ाती हुई बैलगाड़ियाँ चली जातीं, कुत्ते उछल-कूद से शुरू कर लड़ाई –झगड़े पर आमादा हो जाते ! पर दीदी कर्पूरृ-प्रतिमा की भाँति निर्वाक, निश्चल, निःस्पंद ही रहतीं ! जब उनकी समाधि टूटती, तब उनकी बातें सुनने लायक होतीं। अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी थीं। उनके चेहरे से ऐसा जान पड़ता था कि बुद्धदेव से उनकी जरूर भेंट हुई होगी। मैं जब मिलने गया, तो यद्यपि वे थकी हुयी थीं, पर यह कहना न भूलीं कि उन्हें रागृह में एक स्याल मिल गया था, जो उन्हें देखकर तीन बार ठिठक-टिठटककर खड़ा हउआ—जैसे कुछ कहना चाहता हो ! दीदी का विश्वास था कि बुद्धदेव का समसामयित था और उसी युग की कोई बात कहना चाहता था;! क्योंकि दीदी ने स्पष्ट ही उसके चेहरे पर एक निरीह करुण भाव देखा था। आहा, उस युग के स्यार भी कैसे करुणावान होते थे ! मैं समझ गया कि दीदी को अगर चूट दी जाए, तो उस घृंगाल के संबंध में एक पुराण हो जाएगा और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, ‘‘दादी, आजा न विश्राम करो, स्यार की बात कल होगी।’’ दीदी ने भाव-विह्वल हो कर कहा, ‘‘हाँ-’’ रे थक गई हूँ। जा, आज भाग जा। कल जरूर आना। देख, इस बार शोण नद के दोनों किनारों की पैदल यात्रा कर आई हूँ।’’ मैं जेसे अचरज में आ गया—‘‘सोण नद ?’’
‘‘हाँ रे, शोण नद।’’
‘‘कुछ मिला है, दीदी ?’’
‘‘बहुत-कुछ। कल आना।’’
मैं पचहत्तर वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और अध्यवसाय की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया। आहार के समय एक बार लौटकर फिर आया। सोचा, इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूँ। पर देखा, दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी हैं। आहा, चाँदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश घने नीलें-वर्ण के अच्छोद सरोवर की भाँति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ था। उसमें राजहंस की भाँति चंद्रमा धीरे-धीरे तैर रहा था। दूर कोने में एक –दो मेघ-शिशु दिन-भर के थके-माँदे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी-ही-चाँदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की अवस्था में बैठी थीं। पास ही खड़ा एक छोटा-सा खजूरी-वृक्ष सारी शून्यता को समता दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया।
दूसरे दिन मैं शाम को दीदी के स्थान पर पहुँचा। नौकर से् मालूम हुआ कि उस रात को दीदी दो बजे तक चुपचाप बैठी रहीं और फिर एकाएक अपनी टेबिल पर आकर लिखने लगीं, रात-भर लिखती रहीं और लिखने में ऐसी तन्मय थीं कि दूसरे दिन आठ बजे तक लालटेन बुझाये बिना लिखती ही रहीं फिर टेबिल पर ही सिर रखकर लेट गईं। और शाम के तीन बजे तक लेटी रहीं। फिर उन्होंने स्नान किया और अब चाय पीने जा रही हैं। चाय पीते-पीते दीदी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थीं। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुईं और बोलीं, ‘‘तुझे ही खोज रही थी। शोण-यात्रा में उपलब्ध सामग्री का हिंदी रुपांतर मैंने कर लिया है। तू इसे एक बार पढ़ तो भला। देख, मेरी हिंदी में जो गलती है, उसे सुधार दे और आनंद से इसका अँगरेजी में उल्था करा ले। ले भला !’’
यह ‘ले भला !’ दीदी का स्नेह-संभाषण था। जब वे अपने नातियों पर बहुत खुश होतीं, तो उन्हें कुछ देते समय कहती जातीं—‘ले भला।’ आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्कुट ही मिला करते थे; पर आज मिला कागज का एक बड़ा-सा पुलिंदाष। दीदी ने उसे देकर कहा कि यह उनकी दो सौ मील की पदल यात्रा का सुपरिणाम है। फिर कहने लगीं, ‘‘तु इसे आर्ज हगी रात को ठीक कर ले और कल पाँच बडे की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। परसों मुझे इसकी कापियाँ मिल जानी चाहिए।’’
मैंने सकुचाते हुए कहा, ‘‘दीदी, कोई पांडुलिपि मिली है क्या ?’’
दीदी ने डाटते हुए कहा, ‘‘एक बार पढ़के तो देख। इसका रहस्य फिर पूछना। तू बडा़ आलसी है। देख रे, बड़े दुःख की बात बता रही हूँ पुरुष का जन्म पाया है, आलस बड़कर काम कर। स्त्रियाँ चाहें भी तो आलस्यहीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं ? मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गये, जब काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में न तो उतना उत्साह रह गया है और न शक्ति ही। तू बड़ा आलसी है। बाद में पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं। तू समझता है, यूरोप की पराधीनता जरूर कम है; पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। आज देखती हूँ कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए।’’
मैंने देखा, दीदी की आँखें गीली हो गई हैं और उनका पोपला मुख कुछ कहने के लिए व्याकुल है; पर बात निकल नहीं रही है। जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। न जाने किस अतीत में उनका चित्त धीरे-धीरे डूब गया। और मैं चुप बैठा रहा, उस दिन दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ, तो उनकी आँखों से पानी की धारा झर रही थी ओर वे उसे पोंछने का प्रयत्न भी नहीं कर रही थीं।
मैंने अनुभव किया कि दीदी किसी बीती हुई घटना का ताना-बाना सुलझा रही हैं। उधर से ध्यान हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, ‘‘दीदी, आजकल, शोण में नावें चलती हैं ?’’ दीदी ने मुस्करा दिया। उसका भाव था कि ‘मैं समझ गई, तू मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है।’ फिर बोलीं, ‘‘देख, मैं यहाँ ज्यादा नहीं ठहर सकती। इस अनुवाद को तू ज़रा ध्यान से पढ़ और कल कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। दो-एक चित्र भी पुस्तक में देने होंगे। जा, जल्दी कर।’’
‘‘हाँ रे, शोण नद।’’
‘‘कुछ मिला है, दीदी ?’’
‘‘बहुत-कुछ। कल आना।’’
मैं पचहत्तर वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और अध्यवसाय की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया। आहार के समय एक बार लौटकर फिर आया। सोचा, इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूँ। पर देखा, दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी हैं। आहा, चाँदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश घने नीलें-वर्ण के अच्छोद सरोवर की भाँति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ था। उसमें राजहंस की भाँति चंद्रमा धीरे-धीरे तैर रहा था। दूर कोने में एक –दो मेघ-शिशु दिन-भर के थके-माँदे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी-ही-चाँदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की अवस्था में बैठी थीं। पास ही खड़ा एक छोटा-सा खजूरी-वृक्ष सारी शून्यता को समता दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया।
दूसरे दिन मैं शाम को दीदी के स्थान पर पहुँचा। नौकर से् मालूम हुआ कि उस रात को दीदी दो बजे तक चुपचाप बैठी रहीं और फिर एकाएक अपनी टेबिल पर आकर लिखने लगीं, रात-भर लिखती रहीं और लिखने में ऐसी तन्मय थीं कि दूसरे दिन आठ बजे तक लालटेन बुझाये बिना लिखती ही रहीं फिर टेबिल पर ही सिर रखकर लेट गईं। और शाम के तीन बजे तक लेटी रहीं। फिर उन्होंने स्नान किया और अब चाय पीने जा रही हैं। चाय पीते-पीते दीदी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थीं। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुईं और बोलीं, ‘‘तुझे ही खोज रही थी। शोण-यात्रा में उपलब्ध सामग्री का हिंदी रुपांतर मैंने कर लिया है। तू इसे एक बार पढ़ तो भला। देख, मेरी हिंदी में जो गलती है, उसे सुधार दे और आनंद से इसका अँगरेजी में उल्था करा ले। ले भला !’’
यह ‘ले भला !’ दीदी का स्नेह-संभाषण था। जब वे अपने नातियों पर बहुत खुश होतीं, तो उन्हें कुछ देते समय कहती जातीं—‘ले भला।’ आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्कुट ही मिला करते थे; पर आज मिला कागज का एक बड़ा-सा पुलिंदाष। दीदी ने उसे देकर कहा कि यह उनकी दो सौ मील की पदल यात्रा का सुपरिणाम है। फिर कहने लगीं, ‘‘तु इसे आर्ज हगी रात को ठीक कर ले और कल पाँच बडे की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। परसों मुझे इसकी कापियाँ मिल जानी चाहिए।’’
मैंने सकुचाते हुए कहा, ‘‘दीदी, कोई पांडुलिपि मिली है क्या ?’’
दीदी ने डाटते हुए कहा, ‘‘एक बार पढ़के तो देख। इसका रहस्य फिर पूछना। तू बडा़ आलसी है। देख रे, बड़े दुःख की बात बता रही हूँ पुरुष का जन्म पाया है, आलस बड़कर काम कर। स्त्रियाँ चाहें भी तो आलस्यहीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं ? मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गये, जब काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में न तो उतना उत्साह रह गया है और न शक्ति ही। तू बड़ा आलसी है। बाद में पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं। तू समझता है, यूरोप की पराधीनता जरूर कम है; पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। आज देखती हूँ कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए।’’
मैंने देखा, दीदी की आँखें गीली हो गई हैं और उनका पोपला मुख कुछ कहने के लिए व्याकुल है; पर बात निकल नहीं रही है। जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। न जाने किस अतीत में उनका चित्त धीरे-धीरे डूब गया। और मैं चुप बैठा रहा, उस दिन दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ, तो उनकी आँखों से पानी की धारा झर रही थी ओर वे उसे पोंछने का प्रयत्न भी नहीं कर रही थीं।
मैंने अनुभव किया कि दीदी किसी बीती हुई घटना का ताना-बाना सुलझा रही हैं। उधर से ध्यान हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, ‘‘दीदी, आजकल, शोण में नावें चलती हैं ?’’ दीदी ने मुस्करा दिया। उसका भाव था कि ‘मैं समझ गई, तू मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है।’ फिर बोलीं, ‘‘देख, मैं यहाँ ज्यादा नहीं ठहर सकती। इस अनुवाद को तू ज़रा ध्यान से पढ़ और कल कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। दो-एक चित्र भी पुस्तक में देने होंगे। जा, जल्दी कर।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book