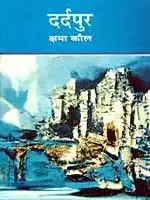|
सामाजिक >> दर्दपुर दर्दपुरक्षमा कौल
|
34 पाठक हैं |
||||||
धार्मिक उन्माद और आतंक के चलते कश्मीर के संस्कृतिमूलक समाज के भयावह विखण्डन तथा कश्मीरी हिन्दुओं और मुसलमानों के आपसी रिश्तों के संवेदन, द्वन्द्व एवं जटिलता को एक संवेगी रूप से उद्घाटित करने वाला सशक्त उपन्यास।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
धार्मिक उन्माद और आतंक के चलते कश्मीर के संस्कृतिमूलक समाज के भयावह
विखण्डन तथा कश्मीरी हिन्दुओं और मुसलमानों के आपसी रिश्तों के संवेदन,
द्वन्द्व एवं जटिलता को एक संवेगी रूप से उद् घाटित करने वाला सशक्त
उपन्यास।
दोद क्या ज़ाने यस नो बने,
गमुक्य जामु छिम वलिथ तने
गरु गरु फीरुस पेयम कने,
डयूठुम नु कांह ति पनुनि कने।
गमुक्य जामु छिम वलिथ तने
गरु गरु फीरुस पेयम कने,
डयूठुम नु कांह ति पनुनि कने।
-ललद्यद
(दर्द वह क्या जाने
जिस पर न बने
गम के वस्त्र हैं
मैंने पहने
घर घर घूमी
संगसार हुई
कोई नहीं था
मेरे कने (साथ)।)
जैसे माहौल में जिये हम लोग
आप होते तो खुदकुशी करते।
जिस पर न बने
गम के वस्त्र हैं
मैंने पहने
घर घर घूमी
संगसार हुई
कोई नहीं था
मेरे कने (साथ)।)
जैसे माहौल में जिये हम लोग
आप होते तो खुदकुशी करते।
-विद्यारत्न आसी
बम बचाएँगे
अपने बीज
और विरोध अपना
अपने बीज
और विरोध अपना
-अग्निशेखर
‘‘उनसे दो टूक कह देना है कि हम उनके लिए कोई आर्थिक
मदद लेकर नहीं आयी है।’’ सुमोना ने उसे समझाया।
‘‘हमें उनसे कहना है कि हम तुमसे मिलने आयी हैं। हम तुम्हारा दुःख बाँटने आयी हैं।’’ सुमोना ने फिर अपना सबक दोहराया ताकि कोई भी, किसी प्रकार की गलती न कर बैठे। खासकर सुधा।
‘‘पर हम दुःख किस रूप में बाँटेंगी ?’’ सुधा ने पूछा।
‘‘उनकी दुःखभरी कथाएँ सुन-सुन कर।’’
‘‘हम वहाँ कितने घण्टे रहेंगी।’’
‘‘डेढ़-दो से अधिक नहीं। वह गाँव खतरनाक नुक्ते पर कायम है। ठीक उसी दर्रे के पार पाकिस्तान है। और वही दर्रा आतंकवादियों का आवागमन का मार्ग भी।’’
‘‘हम कितना सुन पाएँगी इतने कम समय में ?’’
‘‘अब जितना भी।’’ समोना ने हल्की खीझ-सी दिखाते हुए ऐसी आवाज पैदी की, मानो कह रही हो हमारे मतलब की बात हमें एक मिनट में सुनाई देगी....फर्क यह है कि बात सुननी आए।
अब सुधा चुप हो गयी। आगे कोई प्रश्न नहीं। ‘उसे कम बोलना और कम प्रश्न, कम से कम सुमोना से करना, सीखना चाहिए’ सुधा स्वयं से मुखातिब हुई।
सर्दी तीखी होती जा रही थी। वह सोफे पर बैठ अविराम अश्रु बहा रही थी। कितने अश्रु स्थगित किये गये। कब-कब नहीं किये। क्योंकि फुर्सत नहीं थी और जीना था। आगे बढ़ना था। जीते हुए दिखाना था। बहादुर दिखना था। अश्रु बहाते हुए नहीं दिखना था। फलाँ...फलाँ...फलाँ...आदि...इत्यादि...वगैरा वगैरा। और कभी-कभी ऐसा भी हुआ दुःख की पराकाष्ठा में भी ये कमबख्त अश्रु निकले ही नहीं। आँखें सूख गयीं रेतीले खड्डों की तरह। होठों पर एक आँसुओं-सी गीली मुस्कान चिपकी रही। विचित्र-सी। हैरान कर देनेवाली। उसे खुद और औरों को भी।
उसकी इस मुस्कान को आँखें बाहर निकलकर हवा में उड़ती देख रही थीं...और कह रही थीं...‘नहीं भई होठो ! वह बात नहीं। यह मुस्कान वास्तविक अर्थ में किसकी समझ में आएगी। किसी को भी नहीं। शर्त लगाओ चाहो तो।’
हुआ भी था उन दिनों ऐसा ही। और वह उस दन्दाने की कथा खुद को सुनाये जा रही थी—बार-बार।
दन्दाना मर गया। बेचारे के दाँतों की आकृति ऐसी थी कि लगता था हर समय वह दाँत बाहर करके हँस रहा है। जब मर गया तो लोगों ने सोचा-मुआ दिल्लगी कर रहा है...मर कहाँ गया है...मुस्करा तो रहा है।
वह अपने पति के साथ लखनऊ से जम्मू आयी थी, आना आवश्यक था। अथाह दुःख, अनिश्चय उसके चेहरे पर ठहरा था और उसने उन्हीं, सदा बाहर हवा में उड़ते रहनेवाली आँखों से देखा था कि इस वक्त दन्दानी है। जम्मू पहुँच ज्यों-ज्यों घर निकट आता जा रहा था, उसकी निरीहता और बेबसी उसके अस्तित्व पर छाती जा रही थी। घनघोर। पता नहीं अन्दर क्या फैसला होगा। उसकी सास उसके पति को कहेगी—‘छोड़ दे इसे।’ वह छोड़ देगा। कहेगा—‘मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तू जाने, जैसे भी हो अपना चारा कर ले।’
गली के पहले मोड़ पर देखा सरदार सतवन्त सिंह गुजर गये हैं और उस दिन वहाँ ‘रस्म पगड़ी’ की गहमा-गहमी है। सरदार सतवन्त सिंह की बहू आँसू पोंछ रही थी। सतवन्त सिंह अक्सर धूप सेंकते, माला फेरते दुहाई देते रहते थे...कि उनकी बहू उनकी सेवा नहीं करती। दन्दानी ने खुद को कहा और कहीं तीसरी बनकर जरा सी मारक हँसी हँस भी ली। अदृश्य शरीर से। और खुद से कहा--‘‘कुछ नहीं कह सकते कि क्या है सरदार सतवन्त सिंह की बहू के इन अश्रुओं का अर्थ।’
आश्चर्य की बात है कि तत्काल उसके पति की निगाह उस पर पड़ी और कहा, ‘‘हँस रही हो ! यह हँसने की वेला है ?’’
वह समझाना चाहती थी उसे—‘पतिदेव ! मैं कतई नहीं हँस रही। किस बात पर हँसूँगी ? क्या कारण है कि मैं हँसूँगी ? मैं तो सतवन्त सिंह से ईर्ष्या करती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ...दिखाना चाहती हूँ कि बहू पर उसके लगाये सब लांछन गलत साबित हो रहे हैं...वह जार-जार रो रही है...मानो ससुर न होकर पिता हो...और सतवन्त सिंह तुम ? तुम क्या माला जपते थे...और सतवन्त सिंह तुम जीना चाहते जरजर देह के बावजूद...काश ! तुम मुझसे जीवन मृत्यु का विनिमय करते....क्योंकि जिन्दगी के दरवाजों पर मैं जी-तोड़ ठुक-ठुक लगा रही हूँ...कोई भी नहीं खुलता।’ और आश्चर्य की बात है। पर आश्चर्य की...कि आँखें, उसने देखा, उसकी फिर उदास माहौल में बाहर उड़ रही हैं...भिनभिना रही हैं...दुःखी करने वाली मक्खियों की तरह...और कह रही हैं—‘देखा न दन्दानी। दन्दानी कहीं की। मूर्ख दन्दानी औरत। अभी देख तेरा क्या हाल बनेगा। चल तो दन्दानी।’
‘‘मैं हँस नहीं रही थी। पीड़ा से मुख की मुद्रा विरूप हो उठी थी स्वामी।’’
वह चाहती है कि कहे अपने पति से जिसने उसकी डेढ़ वर्ष की बच्ची गोद में उठाकर उसे आभार-ग्रस्त कर लिया है। पर वह कहती नहीं। सिर्फ चौड़ा-लम्बा, आड़ा-तिरछा करके अपने चेहरे को वापस अपनी जगह पर लाना चाहती है और उन समानान्तर भिनभिना रही मक्खियों (आँखों) से पूछना चाहती है...‘क्या मैं....मेरा चेहरा ठीक लग रहा है अब....? अपनी जगह आ गया है क्या मेरा चेहरा ? ऐन मौके पर मक्खियाँ भी आँख मारती हैं...नहीं कहतीं कुछ साफ-साफ।
आज अश्रु थे कि आन पड़े थे चक्रवात की तरह। वह सोफे पर बैठी, चौकड़ी मार, अश्रुओं के साथ अनन्त की ओर बहना चाहती है। उसे, इत्मीनान है कि सुमोना और गुलशनआरा कम-से-कम उसके पति नहीं। आतंकवादी नहीं...या यों ही कोई गैर-पुरुष भी नहीं। उन्हें वह कतई दन्दानी नहीं दिखती होगी। या शायद वे दिन गये हैं, वे उसके दन्दानी होने के दिन या दन्दानी-सी दिखने के दिन।
उसने तुरन्त कान पकड़े।’ नहीं नहीं, मुझे इतना इत्मीनान नहीं लाना चाहिए भीतर। आखिर हूँ स्त्री ही।’
पर अश्रु ? क्या बात है अश्रु-बन्धुओं ? मैंने कोई आरजू मिन्नत नहीं की कि तुम कृपालू हो उठे। कृपा...अश्रुओ। कृपा। यह भगवान गणपति की कृपा है।
दोपहर के समय श्रीनगर पहुँचकर सुमोना और वह राउटर के दफ्तर पहुँच गये। उसने सुमोना से कह दिया था—‘आज गणपति के दर्शन करें सुमोना ?’ उसकी आवाज में प्रार्थना थी, अनुरोध था।
मुश्ताक ने सुमोना को देखते ही चाबियों का छ्ल्ला हाथ में उठाया और तेजी से बाहर आया। अर्थपूर्ण दृष्टि से उसे देखा। उसे भी मुश्ताक की दृष्टि का अर्थ बखूबी मालूम था...और उसकी इच्छा का अर्थ मुश्ताक समझता था। जरूर सुमोना और मुश्ताक के बीच टेलीफोन वार्ता हो चुकी थी उनके यहाँ पहुँचने से पहले।
‘‘हम सब शिव के पुजारी हैं, आदिकाल से। चलो गणपतियार के दर्शन कराएँ मैडम को।’’ मुश्ताक बोला और कार धीमी गति से चल पड़ी।
‘‘अजीब नागहानि हुई। अच्छे-भले हम तरक्की की राह पर चल रहे थे, क्या अल्लाह को मंजूर था।’’ वह फिर बोला। वह चुप थी और मुश्ताक के सर्वप्रथम वाक्य की ध्वनि और उस वाक्य को कहते हुए उसकी मुखमुद्रा उसके मन में तैर रही थी। सोच रही थी उसके सामने गाड़ी के और और आगे बढ़ते जाने के साथ-साथ ही आश्चर्यलोक खुलता जाएगा। एक अविश्वसनीय..अद्भुत आश्चर्यलोक...जो शायद उसने सपने में देखा था कभी...देखा है कभी...क्या कभी देखा भी है....?
अचानक सपने की धरती उपस्थित हुई। बदले हुए गली-कूचों में से गुजरी कार। उसने अपने साथ अहंकार कर लिया था—मैं पहचान लूँगी गणपति का भव्य द्वार जहाँ की ओर मुख करते हुए ही दृष्टि वितस्ता की मस्त लहरों पर नाव-सी सवार हो जाती...जहाँ से सूरज अपनी धूप की पतंगें भेजता और हम लूटते और काटते...मन की करते। तोबा, वह पहचान न कर पायी। कार आगे बढ़ गयी थी...फिर वापस आयी थी...क्योंकि आगे हब्बाकदल होने के निशान मिले थे जो मुश्ताक ने पुष्ट किये थे।
कड़ी काँटेदार तार को पार कर, फिर एक गुफानुमा बंकर पार कर, वह घुस आयी। अब आपा नहीं थी। वह वह नहीं थी। और नीचे से बह रही वितस्ता एक फव्वारा बनकर उसके भीतर चली आयी थी। उसे मालूम नहीं था कि वह दहाड़ भी मार सकती है। सन्न थी वह। आँखें अस्तित्व में खो गयी थीं। डूब गयी थीं। मक्खियों-सी भी बाहर, समानान्तर भिनभिना नहीं रही थीं। गुलशनआरा उदार—मना होना चाहती थी। उसके भीतर शायद एक ईमानदार इच्छा थी, इसलिए वह उसके साथ-साथ गर्भगृह तक चली आयी थी। सुधा पुरोहित मोहन बोय को ढूँढ़ रही थी। और गणपति के चरण छूती। बार-बार। मानो हाड़-मांस के चरण हों। उसने उस छुअन को जीना चाहा...और कह भी दिया...‘देखो छू रही हूँ आपको। सचमुच हूँ तुम्हारे सामने हे गणपति। हूँ न...? छू रही हूँ न तुम्हारे चरण...तुम भी छू रहे हो मुझे...और गणपति की मूर्ति अश्रुओं में डूबी है...वह दहाड़ों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही...सुरक्षाकर्मी अपनी-अपनी आँखें गीली पा रहे हैं...और मोहन बोय सामने प्रकट हो जाते हैं....’’...मैं खिड़की से कूद पड़ा, और आया। तुम्हें देखते ही....मानो तुम्हें नहीं, कोई सपना देख रहा होऊँ...।’’ यह कहते-कहते मोहन बोय ने देखा सुधा उसके चरण पागलों की तरह छू रही है और रो रही है...बेलगाम...मस्त। मानो रोने की मस्ती चढ़ी हो उस पर....जी भरकर रोने की....और मोहन बोय भी रो रहे हैं। वह उसे डूबी आँखों से एकटक देख रही है,....और अन्तर में कह रही है, ‘तुम ही गणपति हो..., सचमुच हो...देखो तुम्हारी नाक सूँड़ में बदल चुकी है...तुममें हवा पर सवार होने की सिद्धि है...तभी छलाँग मारकर आये हो...तुम देख सकते...तभी मैं आती दिखी...तुम ही गणपति हो।’’
मोहन बोय ने बताया, ‘‘...मैं दरवाजे से निकलूँ तो बहुत समय लगता...सुरक्षा के कारण मेरा दरवाजा भिन्न है...खिड़की से कूदना सुरक्षा नियमों के खिलाफ है, पर इस समय उन्होंने ने भी कुछ नहीं कहा...क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम आयी हो...तुम....तुम मतलब दिद्दा...और बताना जाकर प्रभु से कि यहाँ कि दीवार पर, यानी गणपति की दीवार पर, पीला रंग मिटाकर आतंकवादी हरा रंग पोतना चाहते थे....जिसमें सरकार और यहाँ के स्थानीय मुअतबरों की भी मसलहत थी...और उस रण्डी की औलाद और भट्टों के माथे के कलंक रैणा की भी, पर ऐसा हमने होने न दिया। एक सुबह जब देखा हरा रंग चढ़ा है...जमीन आसमान एक किया मैंने और दो दिन बाद फिर वापस अपना रंग पुतवाया---मरूँगा तो क्या बिगड़ेगा..मरूँगा...गणपति की भेंट चढ़ूँगा...अगले जन्म में कश्मीर का राजा बनकर आऊँगा....मगर तुम बहू-बेटियों का बचना जरूरी था। मेरी दोनों बेटियाँ फूला और सरला मिश्रीवाला कैम्प में रहती हैं...खैर...प्रभु से कहना....वहाँ से आवाज बुलन्द करें....कि यहाँ देवी-द्वार घोर असुरक्षित है....कोई सुरक्षा नहीं...’’
‘‘ठीक है। ठीक है। जरूर कहूँगी। जरूर।’’
गुलशनआरा जल्दी बाहर आकर कार में बैठ गयी थी। उससे एक सैनिक ने पूछा था—‘क्यों भगाया आपने इन्हें यहाँ से ? क्यों नहीं लाते हो इन्हें वापस ?’
गुलशनआरा स्त्री है। काश स्त्रियों के वश में होता कुछ। पुरुष ? पुरुष आतंकी। पुरुष ने तबाह किया...पूरा कायनात। स्त्री उसके पुरुषत्व की कालिख पर बराबर रो रही है। सोचा हो गुलशन ने। गुलशनआरा ने उसे कार में बैठकर बतायी थी सैनिक की कही बात और उसके बाद एक सूनापन छा गया था।
सोफे पर बैठे हुए बह रहे ये अश्रु उन्हीं की निरन्तरता है। वर्षों बाद वे उसकी आँखों के आसमान पर आच्छादित होकर अन्ततः बरस गये। मानो गणपति ने सारे विघ्न हटा दिये हों। सुमोना देख रही है और कुछ सोच रही है।
और सुधा नितान्त शिशिर में आ गयी वर्षा के झूले झूल रही है...परम आनन्द में। सद्-चिदानन्द में। बह रहे हैं अश्रु। बह ही रहे हैं...। ‘ देखूँगी कब रुकेंगे।’ वह सोचती है।
उसने उठकर धूपबत्ती जलायी और मन-ही-मन आँख मूँद कर गणेश जी और मोहन बोय को अर्पित की और टेबल पर स्थिर की।
‘‘मुझे एलर्जी होती है इस धुएँ से...यह धूप बत्ती बाहर रख दे...।’’ सुमोना ने कहा और रोक लगा दी। उसके भीतर फूट पड़े वर्षों बाद के आनन्द में।
वह चुप रही और सोचने लगी। देखा सुमोना अर्थपूर्ण ढंग से गुलशन से आँखें मिला रही थी। ‘अच्छा वह गुलशन की चिन्ता कर रही है।’ शायद उसकी धूप-बत्ती से कुफ्र का धुआँ फैल रहा है। जो कि गुलशन के धर्म को कदाचित् दूषित कर रहा है और सुमोना को चिन्तित। ‘मेरे धर्म और मेरी संवेदनशीलता की उसे कोई चिन्ता नहीं।’ कहती वह खुद से।
‘‘वह चाहती है कि गुलशनआरा का ख्याल रखने में मैं भी उसकी मदद करूँ। आखिर मैं भी हिन्दू हूँ...भट्टिनी।’’
‘‘भला क्या फर्क पड़ता है तेरे होने से या न होने से।’’ उसने ऐसा कहा मानो सुमोना बनकर वह सुधा से कह रही हो।
‘‘तुम धूप-बत्ती उठाकर रख आओ बाहर, अगर एलर्जी होती है।’’ सोफे पर बैठे-बैठे ही सुमोना की आपत्ति से अविचल रहने के भाव को अपने पर स्थिर किये उसने कहा।
वह चुप रही। उस पर एक नजर डालकर। शायद वह सोच रही थी कि इसकी इतनी हिम्मत ! कहती है, तुम रख आओ बाहर। बजाय एकदम बुझाने के...आखिर मैं...मैं...मैं सुमोना हूँ....यानी संस्था की प्रतिनिधि। एक अमीर-तरीन संस्था की प्रतिनिधि। यह क्या है ? क्या है यह ? एक ऐसे समुदाय की प्रतिनिधि जिसकी कोई हस्ती नहीं। जिसकी स्त्रियाँ ‘अच्छी बच्चियाँ’ हुआ करती हैं और पुरुष ‘अच्छे बच्चे’। अच्छे सुशील बेटे।
वह सुमोना को देख, फिर आँख मूँद अपने अन्तर्द्वन्द्व में लीन हो गयी। चाहा कि उन यन्त्र सरीखी आँखों को जादूगर के यन्त्र की तरह भीतर उपस्थित कर पूछे कि यह भला क्या माजरा ? हालाँकि उसे कुछ ज्यादा आश्चर्य नहीं है इस पर। तब भी वह कुछ ज्यादा विवरण जानना चाहती है।
कोई विवरण नहीं मिल रहा। बिलकिस के रोजे हैं। वह सुन रही है कि बैरे को आर्डर देकर सुमोना गुलशनआरा के इफ़्तार का इन्तजाम कर रही है। वह सोचती है कि शायद सुमोना उससे भी पूछेगी कि व शाम को भोजन में क्या लेना पसन्द करेगी। मगर सुमोना के चेहरे का माहौल ऐसी सम्भावना से दूर-दूर तक दूर प्रतीत हो रहा है। वह किसी भी प्राथमिकता में कहीं सम्मिलित नहीं कहीं।
इसलिए उसने सोचा कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में सोचे जो उसे खोने के बाद पुनः प्राप्त हुई। जैसे गणपति...या मोहन बोय...या उसके पाँव के नीचे की इस क्षण की ज़मीन ही।
आह ! कुछ ही मीलों पर उसकी माँ का घर है...फिर थोड़ा और आगे बढ़ो...तो उसका स्कूल। स्कूल ? हाँ हाँ स्कूल। बड़ा-सा, भव्य-सा स्कूल। स्कूल के ऐन सामने हाल। हाल ? वह हाल ? जहाँ सुबह प्रार्थना होती...‘सुजले, सुफले, सुजले, सुमने। जय भारत मातृ अनन्तगुणे..सुजले’ जब वह छोटी थी तो दसवीं की बड़ी-बड़ी लड़कियाँ मंच पर चढ़कर प्रार्थना करवातीं। उनमें दिलशाद हुआ करती। अज़रा हुआ करती। क्या यह सच है ? क्या वे संस्कृत भाषा में भारत का गुणगान करती थीं ?’ जय भारत मातृ अनन्तगुणे सुजले..., और मंच पर दिलशाद है। डॉ. दिलशाद और डॉ. अज़रा ज़ैदी ! कहाँ होंगी वे इस समय ? क्यों न मैं उनकी खोज करूँ ? हूँ...? कैसे...कहाँ...किससे पूछूँ...?
यदि वे कहेंगी—‘...हम वे नहीं...हमें कुछ नहीं याद...हम नहीं जानती...’
या कहें—‘....ओ...सुधा...हम नहीं जानती थीं कि हम कुफ्र कर रही थीं...खुदा हमें बख्श दें...या अल्लाह...हमारा वतन हमारे ही दीन के नाम से है...’
सुधा कुछ क्षण निर्जीव-सी हो उठी...दिलशाद और अज़रा के सामने...गाते हुए मन के अन्तिम प्रकोष्ठ के वाद्यवृन्द पर सुजले, सुफले, सुमने, सुवने...जय भारत मातृ अनन्तगुणे...चाहती है...सामने सुमोना भी यह गाए और गुलशन भी...।
यहाँ बगल में उसका कॉलेज है...इस डल के उस छोर पर वह विश्वविद्यालय जहाँ शिव और शक्ति (शंकराचार्य और हारीपर्वत) से रोज रूबरू होती और बीच में सतीसर का चिह्न डलझील।
शिव उठा और किया ताण्डव। पार्वती रोक न पायी।
और भरसक सुधा को राज्ञी की याद आयी। अकेली। उदास। वह काँटेदार तार और बंकर और पुलिस...वाले। और राज्ञी। विषण्ण। मनुष्य या भक्त के स्पर्श को तरसती सिन्धु। एक मन्त्र सुनने की ललकती सिन्धु।
फिर गणपति के काँटेदार तारों में वह फँस गयी। निकल ही नहीं पा रही उसने। मोहन बोय की काँगड़ी दहक रही थी और पुलिसकर्मियों की सिगड़ियाँ भी।
हमारे ईश्वर बन्दी बना लिये गये हैं ? क्या यह सच है ? क्या यह भी सच हो सकता है ? क्या वास्तव में बिलकिस का ईश्वर ईश्वर है ? और मेरा ईश्वर...?
उसने आँखें खोलीं। कमरे में सरसराहट हुई थी। सुमोना धूपबत्ती उठाकर बाहर ले जा रही थी। ‘देखो मेरे ईश्वर ! तुम ईश्वर नहीं...और मैं कुछ भी नहीं कर सकती...कोई तुम्हारी...मदद...हूँ हु कुछ भी नहीं।’’ उसने स्वयं से कहा और अविचलित रहने की कोशिश के सहारे रही भी।
सुमोना की तरफ कतई नहीं देखना चाहा। न गुलशन की तरफ ही। सिर्फ अपनी तरफ। अपने भीतर। मन्त्रों के माध्यम से अपने अन्तर्द्वन्द्वों की काँटेदार तार में उलझ उठी वह।
‘‘हमें उनसे कहना है कि हम तुमसे मिलने आयी हैं। हम तुम्हारा दुःख बाँटने आयी हैं।’’ सुमोना ने फिर अपना सबक दोहराया ताकि कोई भी, किसी प्रकार की गलती न कर बैठे। खासकर सुधा।
‘‘पर हम दुःख किस रूप में बाँटेंगी ?’’ सुधा ने पूछा।
‘‘उनकी दुःखभरी कथाएँ सुन-सुन कर।’’
‘‘हम वहाँ कितने घण्टे रहेंगी।’’
‘‘डेढ़-दो से अधिक नहीं। वह गाँव खतरनाक नुक्ते पर कायम है। ठीक उसी दर्रे के पार पाकिस्तान है। और वही दर्रा आतंकवादियों का आवागमन का मार्ग भी।’’
‘‘हम कितना सुन पाएँगी इतने कम समय में ?’’
‘‘अब जितना भी।’’ समोना ने हल्की खीझ-सी दिखाते हुए ऐसी आवाज पैदी की, मानो कह रही हो हमारे मतलब की बात हमें एक मिनट में सुनाई देगी....फर्क यह है कि बात सुननी आए।
अब सुधा चुप हो गयी। आगे कोई प्रश्न नहीं। ‘उसे कम बोलना और कम प्रश्न, कम से कम सुमोना से करना, सीखना चाहिए’ सुधा स्वयं से मुखातिब हुई।
सर्दी तीखी होती जा रही थी। वह सोफे पर बैठ अविराम अश्रु बहा रही थी। कितने अश्रु स्थगित किये गये। कब-कब नहीं किये। क्योंकि फुर्सत नहीं थी और जीना था। आगे बढ़ना था। जीते हुए दिखाना था। बहादुर दिखना था। अश्रु बहाते हुए नहीं दिखना था। फलाँ...फलाँ...फलाँ...आदि...इत्यादि...वगैरा वगैरा। और कभी-कभी ऐसा भी हुआ दुःख की पराकाष्ठा में भी ये कमबख्त अश्रु निकले ही नहीं। आँखें सूख गयीं रेतीले खड्डों की तरह। होठों पर एक आँसुओं-सी गीली मुस्कान चिपकी रही। विचित्र-सी। हैरान कर देनेवाली। उसे खुद और औरों को भी।
उसकी इस मुस्कान को आँखें बाहर निकलकर हवा में उड़ती देख रही थीं...और कह रही थीं...‘नहीं भई होठो ! वह बात नहीं। यह मुस्कान वास्तविक अर्थ में किसकी समझ में आएगी। किसी को भी नहीं। शर्त लगाओ चाहो तो।’
हुआ भी था उन दिनों ऐसा ही। और वह उस दन्दाने की कथा खुद को सुनाये जा रही थी—बार-बार।
दन्दाना मर गया। बेचारे के दाँतों की आकृति ऐसी थी कि लगता था हर समय वह दाँत बाहर करके हँस रहा है। जब मर गया तो लोगों ने सोचा-मुआ दिल्लगी कर रहा है...मर कहाँ गया है...मुस्करा तो रहा है।
वह अपने पति के साथ लखनऊ से जम्मू आयी थी, आना आवश्यक था। अथाह दुःख, अनिश्चय उसके चेहरे पर ठहरा था और उसने उन्हीं, सदा बाहर हवा में उड़ते रहनेवाली आँखों से देखा था कि इस वक्त दन्दानी है। जम्मू पहुँच ज्यों-ज्यों घर निकट आता जा रहा था, उसकी निरीहता और बेबसी उसके अस्तित्व पर छाती जा रही थी। घनघोर। पता नहीं अन्दर क्या फैसला होगा। उसकी सास उसके पति को कहेगी—‘छोड़ दे इसे।’ वह छोड़ देगा। कहेगा—‘मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तू जाने, जैसे भी हो अपना चारा कर ले।’
गली के पहले मोड़ पर देखा सरदार सतवन्त सिंह गुजर गये हैं और उस दिन वहाँ ‘रस्म पगड़ी’ की गहमा-गहमी है। सरदार सतवन्त सिंह की बहू आँसू पोंछ रही थी। सतवन्त सिंह अक्सर धूप सेंकते, माला फेरते दुहाई देते रहते थे...कि उनकी बहू उनकी सेवा नहीं करती। दन्दानी ने खुद को कहा और कहीं तीसरी बनकर जरा सी मारक हँसी हँस भी ली। अदृश्य शरीर से। और खुद से कहा--‘‘कुछ नहीं कह सकते कि क्या है सरदार सतवन्त सिंह की बहू के इन अश्रुओं का अर्थ।’
आश्चर्य की बात है कि तत्काल उसके पति की निगाह उस पर पड़ी और कहा, ‘‘हँस रही हो ! यह हँसने की वेला है ?’’
वह समझाना चाहती थी उसे—‘पतिदेव ! मैं कतई नहीं हँस रही। किस बात पर हँसूँगी ? क्या कारण है कि मैं हँसूँगी ? मैं तो सतवन्त सिंह से ईर्ष्या करती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ...दिखाना चाहती हूँ कि बहू पर उसके लगाये सब लांछन गलत साबित हो रहे हैं...वह जार-जार रो रही है...मानो ससुर न होकर पिता हो...और सतवन्त सिंह तुम ? तुम क्या माला जपते थे...और सतवन्त सिंह तुम जीना चाहते जरजर देह के बावजूद...काश ! तुम मुझसे जीवन मृत्यु का विनिमय करते....क्योंकि जिन्दगी के दरवाजों पर मैं जी-तोड़ ठुक-ठुक लगा रही हूँ...कोई भी नहीं खुलता।’ और आश्चर्य की बात है। पर आश्चर्य की...कि आँखें, उसने देखा, उसकी फिर उदास माहौल में बाहर उड़ रही हैं...भिनभिना रही हैं...दुःखी करने वाली मक्खियों की तरह...और कह रही हैं—‘देखा न दन्दानी। दन्दानी कहीं की। मूर्ख दन्दानी औरत। अभी देख तेरा क्या हाल बनेगा। चल तो दन्दानी।’
‘‘मैं हँस नहीं रही थी। पीड़ा से मुख की मुद्रा विरूप हो उठी थी स्वामी।’’
वह चाहती है कि कहे अपने पति से जिसने उसकी डेढ़ वर्ष की बच्ची गोद में उठाकर उसे आभार-ग्रस्त कर लिया है। पर वह कहती नहीं। सिर्फ चौड़ा-लम्बा, आड़ा-तिरछा करके अपने चेहरे को वापस अपनी जगह पर लाना चाहती है और उन समानान्तर भिनभिना रही मक्खियों (आँखों) से पूछना चाहती है...‘क्या मैं....मेरा चेहरा ठीक लग रहा है अब....? अपनी जगह आ गया है क्या मेरा चेहरा ? ऐन मौके पर मक्खियाँ भी आँख मारती हैं...नहीं कहतीं कुछ साफ-साफ।
आज अश्रु थे कि आन पड़े थे चक्रवात की तरह। वह सोफे पर बैठी, चौकड़ी मार, अश्रुओं के साथ अनन्त की ओर बहना चाहती है। उसे, इत्मीनान है कि सुमोना और गुलशनआरा कम-से-कम उसके पति नहीं। आतंकवादी नहीं...या यों ही कोई गैर-पुरुष भी नहीं। उन्हें वह कतई दन्दानी नहीं दिखती होगी। या शायद वे दिन गये हैं, वे उसके दन्दानी होने के दिन या दन्दानी-सी दिखने के दिन।
उसने तुरन्त कान पकड़े।’ नहीं नहीं, मुझे इतना इत्मीनान नहीं लाना चाहिए भीतर। आखिर हूँ स्त्री ही।’
पर अश्रु ? क्या बात है अश्रु-बन्धुओं ? मैंने कोई आरजू मिन्नत नहीं की कि तुम कृपालू हो उठे। कृपा...अश्रुओ। कृपा। यह भगवान गणपति की कृपा है।
दोपहर के समय श्रीनगर पहुँचकर सुमोना और वह राउटर के दफ्तर पहुँच गये। उसने सुमोना से कह दिया था—‘आज गणपति के दर्शन करें सुमोना ?’ उसकी आवाज में प्रार्थना थी, अनुरोध था।
मुश्ताक ने सुमोना को देखते ही चाबियों का छ्ल्ला हाथ में उठाया और तेजी से बाहर आया। अर्थपूर्ण दृष्टि से उसे देखा। उसे भी मुश्ताक की दृष्टि का अर्थ बखूबी मालूम था...और उसकी इच्छा का अर्थ मुश्ताक समझता था। जरूर सुमोना और मुश्ताक के बीच टेलीफोन वार्ता हो चुकी थी उनके यहाँ पहुँचने से पहले।
‘‘हम सब शिव के पुजारी हैं, आदिकाल से। चलो गणपतियार के दर्शन कराएँ मैडम को।’’ मुश्ताक बोला और कार धीमी गति से चल पड़ी।
‘‘अजीब नागहानि हुई। अच्छे-भले हम तरक्की की राह पर चल रहे थे, क्या अल्लाह को मंजूर था।’’ वह फिर बोला। वह चुप थी और मुश्ताक के सर्वप्रथम वाक्य की ध्वनि और उस वाक्य को कहते हुए उसकी मुखमुद्रा उसके मन में तैर रही थी। सोच रही थी उसके सामने गाड़ी के और और आगे बढ़ते जाने के साथ-साथ ही आश्चर्यलोक खुलता जाएगा। एक अविश्वसनीय..अद्भुत आश्चर्यलोक...जो शायद उसने सपने में देखा था कभी...देखा है कभी...क्या कभी देखा भी है....?
अचानक सपने की धरती उपस्थित हुई। बदले हुए गली-कूचों में से गुजरी कार। उसने अपने साथ अहंकार कर लिया था—मैं पहचान लूँगी गणपति का भव्य द्वार जहाँ की ओर मुख करते हुए ही दृष्टि वितस्ता की मस्त लहरों पर नाव-सी सवार हो जाती...जहाँ से सूरज अपनी धूप की पतंगें भेजता और हम लूटते और काटते...मन की करते। तोबा, वह पहचान न कर पायी। कार आगे बढ़ गयी थी...फिर वापस आयी थी...क्योंकि आगे हब्बाकदल होने के निशान मिले थे जो मुश्ताक ने पुष्ट किये थे।
कड़ी काँटेदार तार को पार कर, फिर एक गुफानुमा बंकर पार कर, वह घुस आयी। अब आपा नहीं थी। वह वह नहीं थी। और नीचे से बह रही वितस्ता एक फव्वारा बनकर उसके भीतर चली आयी थी। उसे मालूम नहीं था कि वह दहाड़ भी मार सकती है। सन्न थी वह। आँखें अस्तित्व में खो गयी थीं। डूब गयी थीं। मक्खियों-सी भी बाहर, समानान्तर भिनभिना नहीं रही थीं। गुलशनआरा उदार—मना होना चाहती थी। उसके भीतर शायद एक ईमानदार इच्छा थी, इसलिए वह उसके साथ-साथ गर्भगृह तक चली आयी थी। सुधा पुरोहित मोहन बोय को ढूँढ़ रही थी। और गणपति के चरण छूती। बार-बार। मानो हाड़-मांस के चरण हों। उसने उस छुअन को जीना चाहा...और कह भी दिया...‘देखो छू रही हूँ आपको। सचमुच हूँ तुम्हारे सामने हे गणपति। हूँ न...? छू रही हूँ न तुम्हारे चरण...तुम भी छू रहे हो मुझे...और गणपति की मूर्ति अश्रुओं में डूबी है...वह दहाड़ों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही...सुरक्षाकर्मी अपनी-अपनी आँखें गीली पा रहे हैं...और मोहन बोय सामने प्रकट हो जाते हैं....’’...मैं खिड़की से कूद पड़ा, और आया। तुम्हें देखते ही....मानो तुम्हें नहीं, कोई सपना देख रहा होऊँ...।’’ यह कहते-कहते मोहन बोय ने देखा सुधा उसके चरण पागलों की तरह छू रही है और रो रही है...बेलगाम...मस्त। मानो रोने की मस्ती चढ़ी हो उस पर....जी भरकर रोने की....और मोहन बोय भी रो रहे हैं। वह उसे डूबी आँखों से एकटक देख रही है,....और अन्तर में कह रही है, ‘तुम ही गणपति हो..., सचमुच हो...देखो तुम्हारी नाक सूँड़ में बदल चुकी है...तुममें हवा पर सवार होने की सिद्धि है...तभी छलाँग मारकर आये हो...तुम देख सकते...तभी मैं आती दिखी...तुम ही गणपति हो।’’
मोहन बोय ने बताया, ‘‘...मैं दरवाजे से निकलूँ तो बहुत समय लगता...सुरक्षा के कारण मेरा दरवाजा भिन्न है...खिड़की से कूदना सुरक्षा नियमों के खिलाफ है, पर इस समय उन्होंने ने भी कुछ नहीं कहा...क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम आयी हो...तुम....तुम मतलब दिद्दा...और बताना जाकर प्रभु से कि यहाँ कि दीवार पर, यानी गणपति की दीवार पर, पीला रंग मिटाकर आतंकवादी हरा रंग पोतना चाहते थे....जिसमें सरकार और यहाँ के स्थानीय मुअतबरों की भी मसलहत थी...और उस रण्डी की औलाद और भट्टों के माथे के कलंक रैणा की भी, पर ऐसा हमने होने न दिया। एक सुबह जब देखा हरा रंग चढ़ा है...जमीन आसमान एक किया मैंने और दो दिन बाद फिर वापस अपना रंग पुतवाया---मरूँगा तो क्या बिगड़ेगा..मरूँगा...गणपति की भेंट चढ़ूँगा...अगले जन्म में कश्मीर का राजा बनकर आऊँगा....मगर तुम बहू-बेटियों का बचना जरूरी था। मेरी दोनों बेटियाँ फूला और सरला मिश्रीवाला कैम्प में रहती हैं...खैर...प्रभु से कहना....वहाँ से आवाज बुलन्द करें....कि यहाँ देवी-द्वार घोर असुरक्षित है....कोई सुरक्षा नहीं...’’
‘‘ठीक है। ठीक है। जरूर कहूँगी। जरूर।’’
गुलशनआरा जल्दी बाहर आकर कार में बैठ गयी थी। उससे एक सैनिक ने पूछा था—‘क्यों भगाया आपने इन्हें यहाँ से ? क्यों नहीं लाते हो इन्हें वापस ?’
गुलशनआरा स्त्री है। काश स्त्रियों के वश में होता कुछ। पुरुष ? पुरुष आतंकी। पुरुष ने तबाह किया...पूरा कायनात। स्त्री उसके पुरुषत्व की कालिख पर बराबर रो रही है। सोचा हो गुलशन ने। गुलशनआरा ने उसे कार में बैठकर बतायी थी सैनिक की कही बात और उसके बाद एक सूनापन छा गया था।
सोफे पर बैठे हुए बह रहे ये अश्रु उन्हीं की निरन्तरता है। वर्षों बाद वे उसकी आँखों के आसमान पर आच्छादित होकर अन्ततः बरस गये। मानो गणपति ने सारे विघ्न हटा दिये हों। सुमोना देख रही है और कुछ सोच रही है।
और सुधा नितान्त शिशिर में आ गयी वर्षा के झूले झूल रही है...परम आनन्द में। सद्-चिदानन्द में। बह रहे हैं अश्रु। बह ही रहे हैं...। ‘ देखूँगी कब रुकेंगे।’ वह सोचती है।
उसने उठकर धूपबत्ती जलायी और मन-ही-मन आँख मूँद कर गणेश जी और मोहन बोय को अर्पित की और टेबल पर स्थिर की।
‘‘मुझे एलर्जी होती है इस धुएँ से...यह धूप बत्ती बाहर रख दे...।’’ सुमोना ने कहा और रोक लगा दी। उसके भीतर फूट पड़े वर्षों बाद के आनन्द में।
वह चुप रही और सोचने लगी। देखा सुमोना अर्थपूर्ण ढंग से गुलशन से आँखें मिला रही थी। ‘अच्छा वह गुलशन की चिन्ता कर रही है।’ शायद उसकी धूप-बत्ती से कुफ्र का धुआँ फैल रहा है। जो कि गुलशन के धर्म को कदाचित् दूषित कर रहा है और सुमोना को चिन्तित। ‘मेरे धर्म और मेरी संवेदनशीलता की उसे कोई चिन्ता नहीं।’ कहती वह खुद से।
‘‘वह चाहती है कि गुलशनआरा का ख्याल रखने में मैं भी उसकी मदद करूँ। आखिर मैं भी हिन्दू हूँ...भट्टिनी।’’
‘‘भला क्या फर्क पड़ता है तेरे होने से या न होने से।’’ उसने ऐसा कहा मानो सुमोना बनकर वह सुधा से कह रही हो।
‘‘तुम धूप-बत्ती उठाकर रख आओ बाहर, अगर एलर्जी होती है।’’ सोफे पर बैठे-बैठे ही सुमोना की आपत्ति से अविचल रहने के भाव को अपने पर स्थिर किये उसने कहा।
वह चुप रही। उस पर एक नजर डालकर। शायद वह सोच रही थी कि इसकी इतनी हिम्मत ! कहती है, तुम रख आओ बाहर। बजाय एकदम बुझाने के...आखिर मैं...मैं...मैं सुमोना हूँ....यानी संस्था की प्रतिनिधि। एक अमीर-तरीन संस्था की प्रतिनिधि। यह क्या है ? क्या है यह ? एक ऐसे समुदाय की प्रतिनिधि जिसकी कोई हस्ती नहीं। जिसकी स्त्रियाँ ‘अच्छी बच्चियाँ’ हुआ करती हैं और पुरुष ‘अच्छे बच्चे’। अच्छे सुशील बेटे।
वह सुमोना को देख, फिर आँख मूँद अपने अन्तर्द्वन्द्व में लीन हो गयी। चाहा कि उन यन्त्र सरीखी आँखों को जादूगर के यन्त्र की तरह भीतर उपस्थित कर पूछे कि यह भला क्या माजरा ? हालाँकि उसे कुछ ज्यादा आश्चर्य नहीं है इस पर। तब भी वह कुछ ज्यादा विवरण जानना चाहती है।
कोई विवरण नहीं मिल रहा। बिलकिस के रोजे हैं। वह सुन रही है कि बैरे को आर्डर देकर सुमोना गुलशनआरा के इफ़्तार का इन्तजाम कर रही है। वह सोचती है कि शायद सुमोना उससे भी पूछेगी कि व शाम को भोजन में क्या लेना पसन्द करेगी। मगर सुमोना के चेहरे का माहौल ऐसी सम्भावना से दूर-दूर तक दूर प्रतीत हो रहा है। वह किसी भी प्राथमिकता में कहीं सम्मिलित नहीं कहीं।
इसलिए उसने सोचा कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में सोचे जो उसे खोने के बाद पुनः प्राप्त हुई। जैसे गणपति...या मोहन बोय...या उसके पाँव के नीचे की इस क्षण की ज़मीन ही।
आह ! कुछ ही मीलों पर उसकी माँ का घर है...फिर थोड़ा और आगे बढ़ो...तो उसका स्कूल। स्कूल ? हाँ हाँ स्कूल। बड़ा-सा, भव्य-सा स्कूल। स्कूल के ऐन सामने हाल। हाल ? वह हाल ? जहाँ सुबह प्रार्थना होती...‘सुजले, सुफले, सुजले, सुमने। जय भारत मातृ अनन्तगुणे..सुजले’ जब वह छोटी थी तो दसवीं की बड़ी-बड़ी लड़कियाँ मंच पर चढ़कर प्रार्थना करवातीं। उनमें दिलशाद हुआ करती। अज़रा हुआ करती। क्या यह सच है ? क्या वे संस्कृत भाषा में भारत का गुणगान करती थीं ?’ जय भारत मातृ अनन्तगुणे सुजले..., और मंच पर दिलशाद है। डॉ. दिलशाद और डॉ. अज़रा ज़ैदी ! कहाँ होंगी वे इस समय ? क्यों न मैं उनकी खोज करूँ ? हूँ...? कैसे...कहाँ...किससे पूछूँ...?
यदि वे कहेंगी—‘...हम वे नहीं...हमें कुछ नहीं याद...हम नहीं जानती...’
या कहें—‘....ओ...सुधा...हम नहीं जानती थीं कि हम कुफ्र कर रही थीं...खुदा हमें बख्श दें...या अल्लाह...हमारा वतन हमारे ही दीन के नाम से है...’
सुधा कुछ क्षण निर्जीव-सी हो उठी...दिलशाद और अज़रा के सामने...गाते हुए मन के अन्तिम प्रकोष्ठ के वाद्यवृन्द पर सुजले, सुफले, सुमने, सुवने...जय भारत मातृ अनन्तगुणे...चाहती है...सामने सुमोना भी यह गाए और गुलशन भी...।
यहाँ बगल में उसका कॉलेज है...इस डल के उस छोर पर वह विश्वविद्यालय जहाँ शिव और शक्ति (शंकराचार्य और हारीपर्वत) से रोज रूबरू होती और बीच में सतीसर का चिह्न डलझील।
शिव उठा और किया ताण्डव। पार्वती रोक न पायी।
और भरसक सुधा को राज्ञी की याद आयी। अकेली। उदास। वह काँटेदार तार और बंकर और पुलिस...वाले। और राज्ञी। विषण्ण। मनुष्य या भक्त के स्पर्श को तरसती सिन्धु। एक मन्त्र सुनने की ललकती सिन्धु।
फिर गणपति के काँटेदार तारों में वह फँस गयी। निकल ही नहीं पा रही उसने। मोहन बोय की काँगड़ी दहक रही थी और पुलिसकर्मियों की सिगड़ियाँ भी।
हमारे ईश्वर बन्दी बना लिये गये हैं ? क्या यह सच है ? क्या यह भी सच हो सकता है ? क्या वास्तव में बिलकिस का ईश्वर ईश्वर है ? और मेरा ईश्वर...?
उसने आँखें खोलीं। कमरे में सरसराहट हुई थी। सुमोना धूपबत्ती उठाकर बाहर ले जा रही थी। ‘देखो मेरे ईश्वर ! तुम ईश्वर नहीं...और मैं कुछ भी नहीं कर सकती...कोई तुम्हारी...मदद...हूँ हु कुछ भी नहीं।’’ उसने स्वयं से कहा और अविचलित रहने की कोशिश के सहारे रही भी।
सुमोना की तरफ कतई नहीं देखना चाहा। न गुलशन की तरफ ही। सिर्फ अपनी तरफ। अपने भीतर। मन्त्रों के माध्यम से अपने अन्तर्द्वन्द्वों की काँटेदार तार में उलझ उठी वह।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book