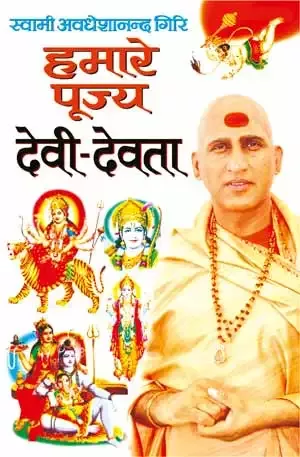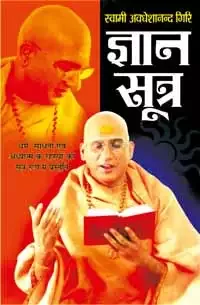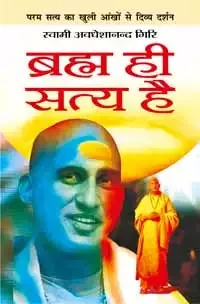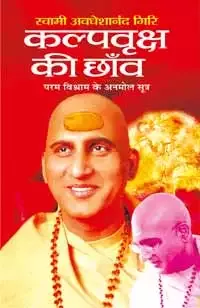|
धर्म एवं दर्शन >> हमारे पूज्य देवी-देवता हमारे पूज्य देवी-देवतास्वामी अवधेशानन्द गिरि
|
243 पाठक हैं |
||||||
’देवता’ का अर्थ दिव्य गुणों से संपन्न महान व्यक्तित्वों से है। जो सदा, बिना किसी अपेक्षा के सभी को देता है, उसे भी ’देवता’ कहा जाता है...
शंकराचार्य
जिस समय भगवान आद्यश्री शंकराचार्य आविर्भूत हुए थे, उस समय देश में सद्धर्म का अनुष्ठान प्रायः लुप्त हो गया था। केवल इतना ही नहीं, उसका स्वरूप ज्ञान भी उच्च कोटि के गिने-चुने महापुरुषों में ही सीमित रह गया था। परमात्मा की ज्ञान शक्ति ने ही उस अज्ञान प्रधान समय में श्री शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर देशव्यापक अज्ञानांधकार को दूर कर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक वैदिक धर्म-कर्म का एकछत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया था। 'शकरः शंकरः साक्षात्' इत्यादि वचनों के अनुसार आद्य शंकराचार्य लोकगुरु भगवान शंकर के अवतार थे—यह सर्वत्र प्रसिद्ध है।
कुछ लोगों को यह संदेह हो सकता है कि भगवान शंकराचार्य ने आविर्भूत होकर ऐसा कौन सा अभिनव सिद्धांत प्रकट किया तथा धर्म का प्रचार किया जिससे यह प्रतीत हो सके कि उन्होंने जगत का अवतारोचित अभूतपूर्व एवं लोकोत्तर कल्याण किया था? वस्तुतः अद्वैतवाद अनादिकाल से ही तत्-तत् अधिकारियों के अंदर प्रसिद्ध था। फिर उन्होंने 'प्रस्थानत्रय' पर भाष्य का निर्माण कर अथवा अपने और किसी व्यापार से कौन-सा विशेष कार्य सिद्ध किया?
इस शंका का समाधान यह है कि यद्यपि अधिकार भेद के अनुसार द्वैत, अद्वैत आदि मत अनादिकाल से ही प्रसिद्ध हैं तथापि विशुद्ध ब्रह्माद्वैतवाद अवैदिक दार्शनिक संप्रदाय के आविर्भाव से लुप्त सा हो गया था। योगाचार तथा माध्यमिक संप्रदाय एवं कुछ तांत्रिक संप्रदाय में अद्वैतवाद के नाम से जिस सिद्धांत का प्रचार हुआ था, वह विशुद्ध औपनिषद ब्रह्मवाद से अत्यंत भिन्न है।
वैदिक धर्म के प्रचार तथा प्रभाव के मंद हो जाने से समाज प्रायः श्रुतिसम्मत विशुद्ध ब्रह्मवाद को भूलकर अवैदिक संप्रदायों द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद को ग्रहण करने लगा था। हीनयान तथा महायान के अंतर्भूत अष्टादश संप्रदाय, शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख आदि माहेश्वर संप्रदाय, पंचरात्र, भागवत आदि वैष्णव संप्रदाय तथा गाणपत्य, सौर आदि विभिन्न धर्म-संप्रदाय भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में फैल गए थे। स्थान विशेष में आर्हत संप्रदाय का प्रभाव भी कम न था। देश के खंड-खंड में विभक्त होने तथा मनुष्यों की रुचि और प्रवृत्ति में कुछ विकार आ जाने के कारण श्रौत धर्मनिष्ठ एवं श्रौत धर्मसंरक्षक सार्वभौम चक्रवर्ती राजा भी कोई नहीं रह गया था जिसके प्रभाव और आदर्श से जनसमुदाय शुद्ध धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो सकता।
ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में वेदानुमत निर्विशेष अद्वैत वस्तु का शास्त्र तथा युक्ति के बल से दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन कर केवल विविध द्वैतवादों का ही नहीं, अपितु भ्रांत अद्वैतवाद का भी खंडन किया। शुद्ध वैदिक ज्ञानमार्ग का अन्वेषण करने वाले विरक्त-जिज्ञासु मुमुक्षु पुरुषों के लिए यही सर्व प्रधान उपकार माना जा सकता है, क्योंकि भगवान शंकर जैसे लोकोत्तर धीशक्ति संपन्न पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के लिए तत्कालीन दार्शनिकों के युक्तिजाल का खंडन करना सरल नहीं था। केवल इतना ही नहीं, अद्वैत सिद्धांत का अपरोक्षतया स्वानुभव करके जगत में उनके प्रचार के लिए तत्-तत् देश और काल के अनुसार मठादि स्थापन द्वारा ज्ञानोपदेश का स्थायी प्रबंध करना भी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं था।
पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेद में सत्ताभेदी की कल्पना करके भगवान शंकराचार्य ने एक विशाल समन्वय का मार्ग खोल दिया था। वह अपने-अपने अधिकार के अनुसार देवमार्गरत निष्ठावान साधन के लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यवहार भूमि में अनुभव के अनुसार अद्वैतवाद को अंगीकार करते हुए और तदनुरूप आचार, अनुष्ठान आदि का उपदेश देते हुए भगवान शंकराचार्य ने बताया कि वस्तुत: वेदांतोपदिष्ट अद्वैत भाव से शास्त्रानुमत द्वैत भाव का कोई विरोध नहीं है। क्योंकि शुद्ध ब्रह्मज्ञान के उदय से संस्कार या वासना की निवृत्ति, विविध प्रकार के कर्मों की निवृत्ति तथा चित्त का उपशम हो जाने पर अखिल द्वैत भावों का एक परमाद्वैत भाव में ही पर्यवसान हो जाता है। परंतु जब तक इस प्रकार परब्रह्म विद्या का उदय न हो तब तक द्वैत भाव को मिथ्या कहकर द्वैत भाव मूलक शास्त्रविहिंत उपासना आदि का त्याग करना उनके सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि जो अनधिकारी है अर्थात जिसको आत्मानात्म विवेक नहीं हुआ है, जिसके चित्त में पूर्ण रूप से वैराग्य का उदय नहीं हुआ है। और जिसमें मुक्ति की इच्छा तक उदित नहीं हुई है, उसके लिए वेदांत ज्ञान का अधिकार तक नहीं है।
कर्म से शुद्ध चित्त होकर उपासना में तत्पर होने से धीरे-धीरे ज्ञान की इच्छा तथा उसको अधिकार उत्पन्न हो जाता है। अतः व्यवहार भूमि में अपने-अपने प्राप्त संस्कारों के अनुसार जो जिस प्रकार के द्वैत अधिकार में रहता है, उसके लिए वही ठीक है। शंकराचार्य जी का कहना है कि वह शास्त्र संपन्न होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विपरीत पौरुष से उन्नति की आशा नहीं है।
वर्णाश्रम धर्म का लोप होने से समाज में धर्मविपर्यय अवश्यंभावी है। शंकराचार्य का सिद्धांत है कि वर्णाश्रम धर्म का संरक्षण करना ही परमेश्वर का नररूप में अवतीर्ण होने का मुख्य प्रयोजन है। शंकराचार्य के जीवन चरित, शिष्यों के प्रति उनके उपदेश तथा ग्रंथ आदि के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं भी वर्णाश्रम धर्म का उपकार करने के लिए समग्र जीवन एवं आत्म शक्ति का प्रयोग किया था, यह उनके अवतारत्व का ही द्योतक है। ये शंकर रूपी शंकरावतार वैदिक धर्म संस्थापक, परम ज्ञानमूर्ति, प्रज्ञा तथा करुणा के विग्रह स्वरूप महापुरुष वैदिक धर्मावलंबी मनुष्य मात्र के लिए सर्वदा प्रणम्य हैं।
|
|||||