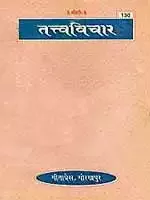|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> तत्त्व विचार तत्त्व विचारज्वाला प्रसाद कनोड़िया
|
440 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है तत्त्वविचार....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
।। श्रीहरि: ।।
निवेदन
‘‘तत्त्वविचार’’ मेरे सम्मान्य भाई
श्रीज्वालाप्रसादजी के कुछ लेखों का संग्रह है। मेरे ही आग्रह से अपने
प्राय: इन लेखों का लिखा था और अब मेरे ही आग्रह से बड़े संकोच में पड़कर
उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करने की आज्ञा देने के लिये आपको विवश होना
पड़ा है। श्रीज्वालाप्रसादजी अपने आपको लेखक नहीं मानते। और लेखक की
हैसियत से पाठकों के सामने उपस्थित होने में अपनी अयोग्यता प्रकट करते हुए
पाठकों से क्षमा चाहते हैं। यह बात सत्य भी है कि वे लेखक नहीं हैं, वे
विचारशील पुरुष हैं और मेरे मत से सुन्दर विचारों को पाकर कोई भी लेखक
सुलेखक बन सकता है। पाठक इस पुस्तक में प्रकाशित विचारों को पढ़कर लाभ
उठावें ऐसी मेरी प्रार्थना है।
मेरे कहने पर श्रीज्वालाप्रसादजी ने इसके लिये एक छोटी-सी संकोच भरी भूमिका लिख भेजी थी, परन्तु वह मुझको पसंद नहीं आयी। इसलिये उनके भावों के साथ कुछ अपने भाव मिलाकर मैंने ही उपर्युक्त परिचय लिख दिया है।
मेरे कहने पर श्रीज्वालाप्रसादजी ने इसके लिये एक छोटी-सी संकोच भरी भूमिका लिख भेजी थी, परन्तु वह मुझको पसंद नहीं आयी। इसलिये उनके भावों के साथ कुछ अपने भाव मिलाकर मैंने ही उपर्युक्त परिचय लिख दिया है।
हनुमानप्रसाद पोद्दार
श्रीहरि: तत्त्वविचार
ईश्वरतत्त्व
ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये
शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै।
रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव
तस्मात्त्वमेव शरणं मम चक्रपाणे।।
शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै।
रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव
तस्मात्त्वमेव शरणं मम चक्रपाणे।।
(श्रीहरिशरणाष्टकात्)
जगत् में प्राय: सभी ईश्वरवादी हैं। कुछ लोग तर्कवाद या विद्याबुद्धि के
गर्व से अनीश्वरवाद को सिद्ध करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। परन्तु
अन्त में ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है। यदि कोई कहे कि मेरे मुख में
जीभ नहीं है तो उसका यह कहना निराधार है, क्योंकि उसके बोलने से जीभ का
होना सिद्ध है। इसी प्रकार यदि कोई यह कहे पिता हुए ही नहीं तो उसका यह
कथन निराधार ही होगा; क्योंकि जब वह है तो अवश्य ही उसका जन्मदाता भी
स्वत: सिद्ध है, चाहे वह उसको जाने या न जाने। यही बात ईश्वर के संबंध में
है। जब कोई मनुष्य किसी घने जंगल में जाकर देखता है कि वहाँ एक सुन्दर
मन्दिर बना हुआ है और उसके समीप एक सुरम्य वाटिका लगी है, जिसमें नाना
प्रकार के फल-फूलों के वृक्ष यथास्थान सुव्यवस्थित हैं तथा जिसके एक ओर एक
चिड़ियाखाना भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी अलग-अलग विभागों
में पिंजड़ों में बंद हैं, ऐसी अवस्था में उसे यह मानना ही होगा कि इन
सबका बनानेवाला कोई अवश्य है। नियमित और सुव्यवस्थित कर्म के देखने से ही
कर्ता का अनुमान होता है, यह स्वाभाविक है।
प्राचीन वैदिक युग में एक समय इस जगत् को देखकर कुछ ऋषियों के मन में शंका हुई थी, उस समय उन्होंने जो निर्णय किया था, उसका वर्णन श्वेताश्वतर-उपनिषद् में इस प्रकार है-
प्राचीन वैदिक युग में एक समय इस जगत् को देखकर कुछ ऋषियों के मन में शंका हुई थी, उस समय उन्होंने जो निर्णय किया था, उसका वर्णन श्वेताश्वतर-उपनिषद् में इस प्रकार है-
ऊँ ब्रह्मवादिने वदन्ति-
किं कारणं ब्रह्म कुत: स्म जाता
जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा:।
अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्।।
किं कारणं ब्रह्म कुत: स्म जाता
जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा:।
अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्।।
(1/1)
अर्थात् ‘ब्रह्मवादी कहते हैं, क्या ब्रह्म कारण है ? हम किससे
जन्में हैं ? किससे जाते हैं ? और किसमें लीन होते हैं ? हे
ब्रह्मवेत्ताओं ! बताओ, वह कौन अधिष्ठाता है जिसकी व्यवस्था से हम
सुख-दु:ख में बर्तते हैं ?’ इसके बाद स्थूल दृष्टि से दीख पड़ने
वाले मूल कारणों को प्रश्नकर्ता स्वयं शंकायुक्त शब्दों में कहता है और
साथ ही उनका निराकरण भी करता है-
काल: स्वभावो नियतिर्यदृच्छा
भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्।
संयोग एषां न त्वात्मभावा-
दात्माप्यनीश: सुखदु: खहेतो:।।
भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्।
संयोग एषां न त्वात्मभावा-
दात्माप्यनीश: सुखदु: खहेतो:।।
(1/2)
अर्थात् ‘क्या काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा अथवा पंचभूत कारण
हैं,
या जीवात्मा कारण है ? यह बात विचारणीय है। इनका संयोग भी कारण नहीं हो
सकता, क्योंकि ये अनात्मपदार्थ जड़ हैं और जीवात्मा भी सुख-दु:ख में लिप्त
रहने के कारण सर्वशक्तिमान् नहीं है।’
‘काल’ शब्द का अभिप्राय यही है कि समस्त सृष्टि संबंधी क्रियाएँ कालविशेष में ही होती हैं; जैसे सभी वस्तुएँ अपनी ऋतु में ही उत्पन्न होती, फलती-फूलती और नष्ट होती हैं। इसीलिये कारण रूप में काल का अनुमान किया गया है।
पदार्थों के स्वभाव से ही जगत् में सारी क्रियाएँ होती देखी जाती हैं, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है और जल का गलाने का इत्यादि; अतएव स्वभाव का कारण रूप से अनुमान किया गया है।
‘नियति’ शब्द का अर्थ है होनहार। जैसे कोई मनुष्य पूर्ण सावधानी से चला जा रहा है, अचानक वज्रपात से उसकी मृत्यु हो जाती है और लोग कह उठते हैं- ‘होनहार ही ऐसी थी।’ इसी प्रकार अकारण ही नियति रूप में समस्त क्रियाएँ होती हैं, नियति को कारण कहनेवाले ऐसा बतलाते हैं।
बिना चेष्टा के जो काम अपने-आप हो जाय, उसे यदृच्छा कहते हैं, जैसे बिना किसी चेष्टा के किसी वस्तु का बीज किसी सुनसान स्थान में पहुँचकर वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार यदृच्छा से जगत् का अस्तित्व है। ऐसा यदृच्छा को कारण मानने वाले कहते हैं।’
‘भूतानि’ शब्द से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश-इन पंचमहाभूतों का ग्रहण होता है और ‘पुरुष’ शब्द जीवात्मा का द्योतक है।
इस प्रकार कालादि का कारण रूप से अनुमान करके उसका निराकरण भी इसी श्लोक में कर दिया गया है। अर्थात् ये सब जड़ होने के कारण कर्ता नहीं हो सकते तथा जीवात्मा चेतन होने पर भी अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् एवं सुख-दु:ख का भोक्ता होने के कारण कर्ता नहीं है। इस प्रकार मूल कारण का निश्चय न होते देख ऋषियों ने ध्यानमग्न होकर देखा-
‘काल’ शब्द का अभिप्राय यही है कि समस्त सृष्टि संबंधी क्रियाएँ कालविशेष में ही होती हैं; जैसे सभी वस्तुएँ अपनी ऋतु में ही उत्पन्न होती, फलती-फूलती और नष्ट होती हैं। इसीलिये कारण रूप में काल का अनुमान किया गया है।
पदार्थों के स्वभाव से ही जगत् में सारी क्रियाएँ होती देखी जाती हैं, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है और जल का गलाने का इत्यादि; अतएव स्वभाव का कारण रूप से अनुमान किया गया है।
‘नियति’ शब्द का अर्थ है होनहार। जैसे कोई मनुष्य पूर्ण सावधानी से चला जा रहा है, अचानक वज्रपात से उसकी मृत्यु हो जाती है और लोग कह उठते हैं- ‘होनहार ही ऐसी थी।’ इसी प्रकार अकारण ही नियति रूप में समस्त क्रियाएँ होती हैं, नियति को कारण कहनेवाले ऐसा बतलाते हैं।
बिना चेष्टा के जो काम अपने-आप हो जाय, उसे यदृच्छा कहते हैं, जैसे बिना किसी चेष्टा के किसी वस्तु का बीज किसी सुनसान स्थान में पहुँचकर वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार यदृच्छा से जगत् का अस्तित्व है। ऐसा यदृच्छा को कारण मानने वाले कहते हैं।’
‘भूतानि’ शब्द से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश-इन पंचमहाभूतों का ग्रहण होता है और ‘पुरुष’ शब्द जीवात्मा का द्योतक है।
इस प्रकार कालादि का कारण रूप से अनुमान करके उसका निराकरण भी इसी श्लोक में कर दिया गया है। अर्थात् ये सब जड़ होने के कारण कर्ता नहीं हो सकते तथा जीवात्मा चेतन होने पर भी अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् एवं सुख-दु:ख का भोक्ता होने के कारण कर्ता नहीं है। इस प्रकार मूल कारण का निश्चय न होते देख ऋषियों ने ध्यानमग्न होकर देखा-
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्।
य: कारणानि निखिलानि तानि
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक:।।
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्।
य: कारणानि निखिलानि तानि
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक:।।
(1/3)
अर्थात् ‘तब उन लोगों ने ध्यान योग में मग्न होकर अपने गुणों से
छिपी हुई परमात्मशक्ति को देखा, जो स्वयं काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा,
पंचभूत तथा आत्मारूप समस्त कारणों के एक ही कारण रूप में अधिष्ठित
है।’
इस प्रकार शास्त्रों में जगत् की उत्पत्ति में मूलभूत अन्य सब कारणों का निराकरण करके एकमात्र ईश्वर को आदि कारण सिद्ध किया है। इस पर यदि कोई कहे कि हम शास्त्री की बात नहीं मानना चाहते तो उसे तर्क और युक्ति द्वारा भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। जो नास्तिक विचारवाले जगत् की उत्पत्ति का मूलकारण प्रकृति (Nature) को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, उनसे यह पूछा जा सकता है कि ‘सृष्टि सुव्यवस्थित, नियमित और ज्ञानपूर्वक है अथवा अव्यवस्थित, और अनियमित और अज्ञानपूर्वक ?’
इस प्रकार शास्त्रों में जगत् की उत्पत्ति में मूलभूत अन्य सब कारणों का निराकरण करके एकमात्र ईश्वर को आदि कारण सिद्ध किया है। इस पर यदि कोई कहे कि हम शास्त्री की बात नहीं मानना चाहते तो उसे तर्क और युक्ति द्वारा भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। जो नास्तिक विचारवाले जगत् की उत्पत्ति का मूलकारण प्रकृति (Nature) को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, उनसे यह पूछा जा सकता है कि ‘सृष्टि सुव्यवस्थित, नियमित और ज्ञानपूर्वक है अथवा अव्यवस्थित, और अनियमित और अज्ञानपूर्वक ?’
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book