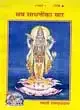|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> साधन के दो प्रधान सूत्र साधन के दो प्रधान सूत्रस्वामी रामसुखदास
|
131 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है साधन के दो प्रधान सूत्र.....
प्रस्तुत हैं इसी पुस्तक के कुछ अंश
।।श्रीहरिः।।
नम्र निवेदन
प्रायः सत्संग की मार्मिक बातों को गहराई से न समझने के कारण साधकों के
भीतर संशय रहता है कि जब हमें कुछ भी नहीं चाहिये, तो फिर साधन-भजन क्यों
करें ? जब कोई अपना ही नहीं है, तो फिर दूसरों की सेवा क्यों करें ?
आदि-आदि। वास्तव में ये शंकाएँ शरीर के साथ अपना सम्बन्ध मानने से ही
उत्पन्न होती हैं। इस विषय को प्रस्तुत पुस्तक ‘साधन के दो
प्रधान
सूत्र’ में बहुत सरल तथा सुन्दर रीति से समझाया गया है। सभी
साधकों
के लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। साधकों से नम्र निवेदन है कि इस पुस्तक
को मनोयोगपूर्वक पढ़ें और सच्ची बात को स्वीकार कर के लाभ उठायें।
प्रकाशक
1 साधन के दो प्रधान सूत्र
चौरासी लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परमपिता परमात्मा अपनी अहैतुकी
कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त
करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसलिये गोस्वामीजी महाराज ने
कहा है—
बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा।।
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परलोक सँवारा।।
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परलोक सँवारा।।
(मानस, उत्तर. 43/4)
भगवान् ने तो इसलिये मानवशरीर प्रदान किया कि जीव संसार-बन्धन से छूटकर
सदा के लिये कृत्यकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाय।
परन्तु दुःख की बात है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग तथा
संग्रह में लग गया ! कभी कोई मनुष्य संतकृपा अथवा भगवत्कृपा से साधन में
लग भी जाता है तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। दृढ़ निश्चचय के बिना
उसका जीवन साधनमय नहीं बन पाता। जीवन साधन मय न बनने के कारण वह कोरी
बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है, पर परमशान्ति नहीं प्राप्त कर
सकता। जीवन को साधनमय बनाने के लिये यह आवश्यक है कि साधक इन दो बातों को
दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले—
(1) मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिये और मेरा किसी से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।
(2) केवल भगवान् ही मेरे अपने हैं।
पहली बात संसार से सम्बन्ध-विच्छेद कराने वाली है और दूसरी बात भगवान् की प्राप्ति करनेवाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से ‘भक्ति’ की सिद्धि हो जाती है। अतः विवेकप्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करे। परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधन कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जायँगे। उनका मनुष्यजन्म सफल हो जायगा। इन बातों को सीखना नहीं है, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, परन्तु स्वीकार की गयी बात की विस्मृति नहीं होती।
अब यह शंका पैदा होती है कि जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर माता-पिता की सेवा क्यों करें ? वस्तुओं की रक्षा क्यों करें ? जब मेरे को कुछ नहीं चाहिये तो फिर अन्न-जल की क्या जरूरत है ? जब मेरा किसी से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है फिर दूसरे की सहायता क्यों करें ? सेवा क्यों करें ? जब केवल भगवान् ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करें ? इन सब शंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उपर्युक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकर करता है। शरीर के साथ में—मेरे सम्बन्ध (तादात्म्य) ही बन्धन का मूल कारण है। इसलिये हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है।
(1) मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिये और मेरा किसी से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।
(2) केवल भगवान् ही मेरे अपने हैं।
पहली बात संसार से सम्बन्ध-विच्छेद कराने वाली है और दूसरी बात भगवान् की प्राप्ति करनेवाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से ‘भक्ति’ की सिद्धि हो जाती है। अतः विवेकप्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करे। परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधन कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जायँगे। उनका मनुष्यजन्म सफल हो जायगा। इन बातों को सीखना नहीं है, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, परन्तु स्वीकार की गयी बात की विस्मृति नहीं होती।
अब यह शंका पैदा होती है कि जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर माता-पिता की सेवा क्यों करें ? वस्तुओं की रक्षा क्यों करें ? जब मेरे को कुछ नहीं चाहिये तो फिर अन्न-जल की क्या जरूरत है ? जब मेरा किसी से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है फिर दूसरे की सहायता क्यों करें ? सेवा क्यों करें ? जब केवल भगवान् ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करें ? इन सब शंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उपर्युक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकर करता है। शरीर के साथ में—मेरे सम्बन्ध (तादात्म्य) ही बन्धन का मूल कारण है। इसलिये हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है।
ईश्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी।।
(मानस, उत्तर. 117/1)
अब इस पर विचार करते हैं —
‘ईस्वर अंस जीव’—
जीव स्वयं अंश है और
परमात्मा अंशी
हैं। भगवान् ने भी कहा—‘ममैवांशो जीवलोके’
(गीता 15/7)।
जैसे भगवान् सत्-चित्-आनन्द स्वरूप हैं, ऐसे ही जीव भी
सत्-चित्-आनन्स्वरूप हैं जैसे सभी बेटों का माँ पर समान अधिकार होता है,
ऐसे ही परमपिता परमात्मा पर मानवमात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई
राजकुमार ‘मैं राजा का बेटा हूँ’—इस बात को
भूलकर भीख
माँगता है तो राजा को आश्चर्य के साथ-साथ बड़ा दुःख होता है, ऐसे ही
सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान् को बड़ा दुःख
होता है कि यह मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा
है
—‘मामप्राप्यैव कौन्तेय
ततो यान्त्यधमां
गतिम्’
(गीता 16/20।
साधक में इस बात का गर्व (स्वाभिमान) होना चाहिये कि भगवान् मेरे अपने
हैं, मैं भगवान् का हूँ—
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे।।
(मानस, अरण्य. 11 । 11)
हम त्रिलोकी के स्वामी परमपिता परमात्मा की सन्तान हैं, फिर हम तुच्छ
नाशवान संसार की ओर हाथ क्यों फैलायें ? जो संसार के सम्मुख होता है, उसको
संसार अपना दास बना लेता है। परन्तु जो भगवान् के सम्मुख होता है, स्वयं
भगवान् उसके दास बन जाते हैं—‘अहं
भक्तपराधीनः’
(श्रीमद्भा.9/4/63); ‘मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे
मुकुटमणि’! ऐसे परमसुहृदय प्रभु को छोड़कर संसार को चाहना कितनी
मूर्खता की बात है !
‘अबिनासी’—
परमात्मा अविनाशी हैं; अतः उनका
अंश जीव भी
अविनाशी है—‘अविनाशी तु तद्विद्धि’ (गीता
2/17)। परन्तु
स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान् शरीर-संसार के साथ सम्बन्ध जोड़ लेता
है—
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।।
(गीता 15/7)
इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है; परन्तु वह
प्रकृति में स्थित मन और पाँचों इन्द्रियों को आकर्षित करता है अर्थात्
अपना मान लेता है।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book