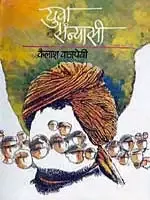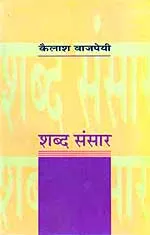|
नाटक-एकाँकी >> युवा संन्यासी युवा संन्यासीकैलाश बाजपेयी
|
216 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है युवा सन्यासी नाटक...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
स्वामी विवेकानन्द के बाल्यजीवन से लेकर उनकी समाधि-अवस्था तक की प्रमुख
घटनाओं का चित्रण करने वाली यह लघु नाट्य-कृति और कुछ नहीं,
अध्यात्मप्रेमी रचनाकार की अन्तर्मन की पीड़ा की सहज उद्भावना है। उनके ही
शब्द हैं-
‘‘आखिर इस सारी समृद्धि, भागदौड़ या ज्ञान का अर्थ क्या है ? हम जिसे विकास कहते हैं क्या वह सही विकास है ? हम सब दोहरी जिन्दगी जीते हैं। एक संसार है जो हमें मिला है-स्वयंभू सृष्टि।
इसी के समानान्तर एक और दुनिया है जो आदमी ने बनाई है-पंख और पहियों और तारों पर भागती, भोग के लिए उकसाती, परिचय को निर्वैयक्तिक करती, एक आयामवाले लोगों को जन्म देती, खाली और खोखली। सच है कि जिन्दगी आज जितनी सुविधापरक और रंगीन है पहले कभी नहीं थी, मगर इसी के साथ यह भी सच है कि आज आदमी जितना बेचारा और गम़गीन है पहले कभी नहीं था। कदाचर सहज और लड़ाई पहले से भी बहुत ज्यादा भोली मगर खूँख़्वार हो गई है। पूर्व हो या पश्चिम दुख लगातार बढ़ रहा है। कितने उपदेशक आये-गये, क्रान्तियाँ हुई लेकिन आदमी जहाँ था वहीं सड़ रहा है। ऐसे वक्त में विवेकानन्द जैसे संन्यासी, कर्मयोग बहुत अधिक प्रासंगिक ही जाते हैं।
दरअसल यह कृति एक नाटक भी है, जीवनवृत्त भी है और कुछ अर्थों में कहानी भी। एक रूपरेखा जिसका प्रारूप कुछ ऐसा है जो पाठकों से एक विशिष्ट मनोभूमि की अपेक्षा करता है। इसके रचना-शिल्प में एक अच्छी फिल्म के सूत्र निहित हैं। संभवत: यह कृति लिखी भी इसी उद्देश्य से गई है। आशा है, हिन्दी के सहृदय पाठकों एवं नाट्यकर्मियों को यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।
‘‘आखिर इस सारी समृद्धि, भागदौड़ या ज्ञान का अर्थ क्या है ? हम जिसे विकास कहते हैं क्या वह सही विकास है ? हम सब दोहरी जिन्दगी जीते हैं। एक संसार है जो हमें मिला है-स्वयंभू सृष्टि।
इसी के समानान्तर एक और दुनिया है जो आदमी ने बनाई है-पंख और पहियों और तारों पर भागती, भोग के लिए उकसाती, परिचय को निर्वैयक्तिक करती, एक आयामवाले लोगों को जन्म देती, खाली और खोखली। सच है कि जिन्दगी आज जितनी सुविधापरक और रंगीन है पहले कभी नहीं थी, मगर इसी के साथ यह भी सच है कि आज आदमी जितना बेचारा और गम़गीन है पहले कभी नहीं था। कदाचर सहज और लड़ाई पहले से भी बहुत ज्यादा भोली मगर खूँख़्वार हो गई है। पूर्व हो या पश्चिम दुख लगातार बढ़ रहा है। कितने उपदेशक आये-गये, क्रान्तियाँ हुई लेकिन आदमी जहाँ था वहीं सड़ रहा है। ऐसे वक्त में विवेकानन्द जैसे संन्यासी, कर्मयोग बहुत अधिक प्रासंगिक ही जाते हैं।
दरअसल यह कृति एक नाटक भी है, जीवनवृत्त भी है और कुछ अर्थों में कहानी भी। एक रूपरेखा जिसका प्रारूप कुछ ऐसा है जो पाठकों से एक विशिष्ट मनोभूमि की अपेक्षा करता है। इसके रचना-शिल्प में एक अच्छी फिल्म के सूत्र निहित हैं। संभवत: यह कृति लिखी भी इसी उद्देश्य से गई है। आशा है, हिन्दी के सहृदय पाठकों एवं नाट्यकर्मियों को यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।
प्राक्कथन
अपने पहले कविता-संग्रह ‘संक्रान्त’ के प्रकाशन के बाद से
लेकर पाँचवें संग्रह ‘सूफ़ीनामा’ के प्रकाशन तक, मैंने अपनी
रचनायात्रा के चार दशक पूरे किये। ‘सूफ़ीनामा’ तक आते-आते मन
में कविता की जो तस्वीर उभरती है उसे कम-से-कम शब्दों में कहूँ तो कहूँगा,
कविता वह अकेली और निराली अभिव्यक्ति है जो हर संकीर्णता का अतिक्रमण करती
हुई, अनय से लड़ती हुई, समता और लोकोपकार की चाह लिये एक ऐसे वलय का
निर्माण करती है जिसकी धुरी पर सत्य भासमान होता है। मैंने अब तक मुश्किल
से ढ़ाई सौ कविताएँ लिखी होंगी। जितना पढ़ा है उसकी तुलना में लेखन बहुत
कम हुआ। अगर पीछे मुड़कर देखूँ तो शायद डेढ़ सौ अप्रकाशित निबन्ध और
होंगे, जिनकी विषय विविधता से स्वयं मुझे ही अन्दाज़ नहीं लग पाता कि
मैंने कितना क्या-क्या पढ़ा या लिखा है। दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम तैयार
करने की प्रक्रिया में, ढेरों चिन्तक और महापुरुषों का कृतित्व और उनका
जीवन वृत्त मुझे तरह-तरह से उद्वेलित करता रहा।
मैं अगर अपने विद्यार्थी-जीवन से अब तक की अपनी जीवन-यात्रा के पृष्ठ पलटूँ तो लगता है मुझे संन्यासी हमेशा से आकर्षित करते रहे। प्रारम्भिक वर्षों में मेरे नाना जो खासे समृद्ध होने के बावजूद, तपस्वी जैसा जीवन जीते थे मेरा आदर्श रहे। उन्होंने अपने संरक्षण में मुझे तरह-तरह की सीख दी। लखनऊ विश्वविद्यालय में भर्ती होने से पहले का मेरा जीवन, जन्मजात आलसी होने के बावजूद, खासा संयत रहा। इस समय तक मैं वात्स्यायन और विवेकानन्द, गोर्की और प्रेमचन्द्र के ही साथ, (अगर मैं भूलता नहीं तो) खलील जिब्रान भी पड़ चुका था। आगे के वर्षों में मार्क्स, महावीर, धम्मपद, शंकर का वेदान्त, संक्षेप में कहूँ तो पश्चिम और पूर्व के सारे दार्शिनक निकाय, सभी उत्कृष्ट लेखक धीरे-धीरे मेरे अध्ययन की सरणि में आते और मेरी अन्त:चेतना में समाते चले गये। हालाँकि बचपन में पढ़ा यह सार- ‘जो पुरुष मन से इन्द्रयों को वश में करके अनासक्त हो कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है’-मुझे हमेशा याद रहा, मगर आचरण में मैं उसे आज तक न उतार सका। एक दृष्टि से मेरा जीवन ढेर सारे विरोधों का संगम बना रहा। शायद अब भी है, तो भी सौन्दर्य और संन्यास मुझे अब भी पराये नहीं लगते।
पिछले वर्षों में श्रीरामकृष्ण परमहंस का एक वृत्तचित्र बनाने के सिलसिले में दक्षिणेश्वर जाना हुआ। रहना भी। विद्यार्थी-जीवन में उनका जीवन-चरित्र पढ़ते हुए अक्सर समाधि के अनुभव के प्रति भी पर्यत्सुक हो जाया करता था। नाना जी ने माँ को बताया था कि कभी-कभी ‘मान्या’ (मेरा घर का नाम) इस अनुभव से गुज़रेगा। सम्प्रति यह बताना जरूरी नहीं कि कब कहाँ कैसे यह अनुभव हुआ। मगर समाधि निश्चय ही एक विरल घटना है। हमें नींद का पता है, हमें यह भी पता है कि कई बार आँख खुली होती है। दृश्य भी होता है तो भी देखना नहीं होता ! आवाज़ें आती हैं सुनना नहीं होता। जब मन में कोई याद नहीं होती तो अतीत नहीं होता। जब भीतर कोई योजना या विचार नहीं होता तो भविष्य नहीं होता। जब कोई शब्द, राग, विराग, विकार नहीं होता, सिर्फ़ एक कोरापन होता है, खालीपन-तो यह हुई Choiceless awareness। जे. कृष्णमूर्ति ने अपनी बात यहीं तक कही है मगर समाधि के बारे में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं-नमक से बनी एक गुड़िया को अगर समुद्र में छोड़ दिया जाय और कहा जाय कि लौटकर आना और गहराई के बारे में बताना, तो न वह कभी लौटेगी और न समाधि के अनुभव के बारे में कभी किसी को कुछ ज्ञात होगा।
जो भी हो, दक्षिणेश्वर में यह विचार मन में कभी आया कि कभी विवेकानन्द पर कुछ लिखा जा सकता है। सब लेखक किन्हीं अंशों तक चित्त की एकाग्रता को जानते हैं। असल में रचना होती ही तब है जब एकाग्रता केन्द्रीभूत होकर इतनी-प्रगाढ़ हो गई होती है कि स्वयं अपना होना भी याद नहीं रहता। इसलिए भीतर-ही-भीतर यह प्रतीक्षा फलती रही कि कभी-न-कभी जिन्दगी में एक अवधि ऐसी आयेगी जब इस युवा संन्यासी पर कुछ लिखना बन पायेगा। सबकुछ चलता रहा। समय के हिसाब से आयु सरकती रही, मगर विवेकानन्द पर लम्बी रचना लिखने की घड़ी नहीं आयी।
एक दिन सुबह-सुबह वासु भट्टाचार्य द्वार पर आ गये। शायद उन्होंने परमहंस रामकृष्ण पर बनाया वह वृत्तचित्र या तो दूरदर्शन पर देख लिया था या फिर उन्हें किसी ने वृत्तचित्र के बारे में बताया था। बड़ी देर तक उनसे विवेकानन्द जी के विषय में बातें होती रहीं, जिनसे निष्कर्ष यह निकला कि कहानी को नाटक और फ़िल्म-निर्माण विधि को ध्यान में रखकर लिखा जाये।
विवेकानन्द का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे साधक, चिन्तक, योगी, परिव्राजक, वेदान्ती सभी कुछ एक साथ हैं। वे शंकर से प्रेरित होते हुए भी शंकर जैसे नहीं। शंकर का ‘अद्वैत’ भी ठीक से समझा तभी जा सकता है जब द्वैत समझ में आ जाये। द्वैत का मतलब दूसरेपन की समझ या भाव। यानी एक ओर आप और दूसरी ओर कोई और। तो यह दूसरी ओर वाला अगर न रहे तो द्वैत गिर जाय। मगर दूसरा दूसरा लग ही तब सकता है जब आप में ‘मैं पन’ हो, लेकिन यदि किसी तरह ‘मैं पन’ न रहे, तिरोहित हो जाये तो दूसरा वहाँ कहाँ ठहरेगा ? क्योंकि दूसरा, दूसरा है ही इसलिए कि आपको अपने होने का एहसास है। तो अद्वैत की स्थापना में दूसरा तो ग़ायब होती ही है, आप भी नहीं रहते। यह एहसास, कहते हैं, सबसे पहले जनक को हुआ था। कोई भी दृश्य निरर्थक है अगर देखने वाला न हो। कोई भी देखनेवाला बेमानी है अगर दृश्य न हो। याकि दृश्य दृश्य कहलायेगा ही तब जब द्रष्टा हो। इसलिए जनक ने कहा-जो दिखाई दे रहा है और उसे जो देख रहा है दोनों के बीच जो संबंध है वह स्वप्न है और जागे हुए आदमी के लिए उतनी ही बेमानी है जितनी कि मुर्दें के लिए लोरी।
मगर विवेकाननेद का वेदान्त प्रत्येक जीव को ब्रह्य मानता हुआ भी, मानव विमुख नहीं। वह मानव-देह मन्दिर में प्रतिष्ठित मानव-आत्मा को ही एकमात्र पूजा की इकाई मानता है। उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। ग़रीब और दुखी लोग ही मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्गचिह्व हैं। विवेकानन्द का एक वाक्य मूल्यवान है। वे जब कहते हैं, ‘मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह दुरात्मा है’ तो एकाएक यह सत्य हर रचनाकार को सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर इस तमाम सारी समृद्धि, भागदौड़ या ज्ञान का अर्थ क्या है ?
हम जिसे विकास कहते हैं क्या वह सही विकास है ? हम सब दोहरी जिन्दगी जीते हैं। एक संसार वह है जो हमें मिला है-स्वयं सृष्टि। इसी के समानान्तर एक और दुनिया है जो आदमी ने बनाई है-पंख और पहियों और तारों पर भागती, भोग के लिए उकसाती, परिचय को निर्वैयक्तिक करती, एक आयामवाले लोगों को जन्म देती, खाली और खोखली। सच है कि जिन्दगी आज जितनी सुविधापरक और रंगीन है पहले कभी नहीं थी, मगर इसी के साथ यह भी सच है कि आज आदमी जितना बेचारा और गम़गीन है पहले कभी नहीं था। कदाचर सहज और लड़ाई पहले से भी बहुत ज्यादा भोली मगर खूँख़्वार हो गई है। पूर्व हो या पश्चिम दुख लगातार बढ़ रहा है। कितने उपदेशक आये-गये, क्रान्तियाँ हुई लेकिन आदमी जहाँ था वहीं सड़ रहा है। ऐसे वक्त में विवेकानन्द जैसे संन्यासी, कर्मयोगी, बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।
असल में यह कृति एक तरह की रूपरेखा है। इसका प्रारूप कुछ ऐसा है जो पाठकों से एक विशिष्ट मनोभूमि की अपेक्षा करता है। इसके रचना शिल्प में एक अच्छी फिल्म के सूत्र निहित हैं। यह कृति लिखी भी इसी उद्देश्य से गयी थी।
इस कृति का प्रकाशन कर इसे हमारे सहृदय पाठकों तक पहुँचाने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ।
मैं अगर अपने विद्यार्थी-जीवन से अब तक की अपनी जीवन-यात्रा के पृष्ठ पलटूँ तो लगता है मुझे संन्यासी हमेशा से आकर्षित करते रहे। प्रारम्भिक वर्षों में मेरे नाना जो खासे समृद्ध होने के बावजूद, तपस्वी जैसा जीवन जीते थे मेरा आदर्श रहे। उन्होंने अपने संरक्षण में मुझे तरह-तरह की सीख दी। लखनऊ विश्वविद्यालय में भर्ती होने से पहले का मेरा जीवन, जन्मजात आलसी होने के बावजूद, खासा संयत रहा। इस समय तक मैं वात्स्यायन और विवेकानन्द, गोर्की और प्रेमचन्द्र के ही साथ, (अगर मैं भूलता नहीं तो) खलील जिब्रान भी पड़ चुका था। आगे के वर्षों में मार्क्स, महावीर, धम्मपद, शंकर का वेदान्त, संक्षेप में कहूँ तो पश्चिम और पूर्व के सारे दार्शिनक निकाय, सभी उत्कृष्ट लेखक धीरे-धीरे मेरे अध्ययन की सरणि में आते और मेरी अन्त:चेतना में समाते चले गये। हालाँकि बचपन में पढ़ा यह सार- ‘जो पुरुष मन से इन्द्रयों को वश में करके अनासक्त हो कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है’-मुझे हमेशा याद रहा, मगर आचरण में मैं उसे आज तक न उतार सका। एक दृष्टि से मेरा जीवन ढेर सारे विरोधों का संगम बना रहा। शायद अब भी है, तो भी सौन्दर्य और संन्यास मुझे अब भी पराये नहीं लगते।
पिछले वर्षों में श्रीरामकृष्ण परमहंस का एक वृत्तचित्र बनाने के सिलसिले में दक्षिणेश्वर जाना हुआ। रहना भी। विद्यार्थी-जीवन में उनका जीवन-चरित्र पढ़ते हुए अक्सर समाधि के अनुभव के प्रति भी पर्यत्सुक हो जाया करता था। नाना जी ने माँ को बताया था कि कभी-कभी ‘मान्या’ (मेरा घर का नाम) इस अनुभव से गुज़रेगा। सम्प्रति यह बताना जरूरी नहीं कि कब कहाँ कैसे यह अनुभव हुआ। मगर समाधि निश्चय ही एक विरल घटना है। हमें नींद का पता है, हमें यह भी पता है कि कई बार आँख खुली होती है। दृश्य भी होता है तो भी देखना नहीं होता ! आवाज़ें आती हैं सुनना नहीं होता। जब मन में कोई याद नहीं होती तो अतीत नहीं होता। जब भीतर कोई योजना या विचार नहीं होता तो भविष्य नहीं होता। जब कोई शब्द, राग, विराग, विकार नहीं होता, सिर्फ़ एक कोरापन होता है, खालीपन-तो यह हुई Choiceless awareness। जे. कृष्णमूर्ति ने अपनी बात यहीं तक कही है मगर समाधि के बारे में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं-नमक से बनी एक गुड़िया को अगर समुद्र में छोड़ दिया जाय और कहा जाय कि लौटकर आना और गहराई के बारे में बताना, तो न वह कभी लौटेगी और न समाधि के अनुभव के बारे में कभी किसी को कुछ ज्ञात होगा।
जो भी हो, दक्षिणेश्वर में यह विचार मन में कभी आया कि कभी विवेकानन्द पर कुछ लिखा जा सकता है। सब लेखक किन्हीं अंशों तक चित्त की एकाग्रता को जानते हैं। असल में रचना होती ही तब है जब एकाग्रता केन्द्रीभूत होकर इतनी-प्रगाढ़ हो गई होती है कि स्वयं अपना होना भी याद नहीं रहता। इसलिए भीतर-ही-भीतर यह प्रतीक्षा फलती रही कि कभी-न-कभी जिन्दगी में एक अवधि ऐसी आयेगी जब इस युवा संन्यासी पर कुछ लिखना बन पायेगा। सबकुछ चलता रहा। समय के हिसाब से आयु सरकती रही, मगर विवेकानन्द पर लम्बी रचना लिखने की घड़ी नहीं आयी।
एक दिन सुबह-सुबह वासु भट्टाचार्य द्वार पर आ गये। शायद उन्होंने परमहंस रामकृष्ण पर बनाया वह वृत्तचित्र या तो दूरदर्शन पर देख लिया था या फिर उन्हें किसी ने वृत्तचित्र के बारे में बताया था। बड़ी देर तक उनसे विवेकानन्द जी के विषय में बातें होती रहीं, जिनसे निष्कर्ष यह निकला कि कहानी को नाटक और फ़िल्म-निर्माण विधि को ध्यान में रखकर लिखा जाये।
विवेकानन्द का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे साधक, चिन्तक, योगी, परिव्राजक, वेदान्ती सभी कुछ एक साथ हैं। वे शंकर से प्रेरित होते हुए भी शंकर जैसे नहीं। शंकर का ‘अद्वैत’ भी ठीक से समझा तभी जा सकता है जब द्वैत समझ में आ जाये। द्वैत का मतलब दूसरेपन की समझ या भाव। यानी एक ओर आप और दूसरी ओर कोई और। तो यह दूसरी ओर वाला अगर न रहे तो द्वैत गिर जाय। मगर दूसरा दूसरा लग ही तब सकता है जब आप में ‘मैं पन’ हो, लेकिन यदि किसी तरह ‘मैं पन’ न रहे, तिरोहित हो जाये तो दूसरा वहाँ कहाँ ठहरेगा ? क्योंकि दूसरा, दूसरा है ही इसलिए कि आपको अपने होने का एहसास है। तो अद्वैत की स्थापना में दूसरा तो ग़ायब होती ही है, आप भी नहीं रहते। यह एहसास, कहते हैं, सबसे पहले जनक को हुआ था। कोई भी दृश्य निरर्थक है अगर देखने वाला न हो। कोई भी देखनेवाला बेमानी है अगर दृश्य न हो। याकि दृश्य दृश्य कहलायेगा ही तब जब द्रष्टा हो। इसलिए जनक ने कहा-जो दिखाई दे रहा है और उसे जो देख रहा है दोनों के बीच जो संबंध है वह स्वप्न है और जागे हुए आदमी के लिए उतनी ही बेमानी है जितनी कि मुर्दें के लिए लोरी।
मगर विवेकाननेद का वेदान्त प्रत्येक जीव को ब्रह्य मानता हुआ भी, मानव विमुख नहीं। वह मानव-देह मन्दिर में प्रतिष्ठित मानव-आत्मा को ही एकमात्र पूजा की इकाई मानता है। उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। ग़रीब और दुखी लोग ही मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्गचिह्व हैं। विवेकानन्द का एक वाक्य मूल्यवान है। वे जब कहते हैं, ‘मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह दुरात्मा है’ तो एकाएक यह सत्य हर रचनाकार को सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर इस तमाम सारी समृद्धि, भागदौड़ या ज्ञान का अर्थ क्या है ?
हम जिसे विकास कहते हैं क्या वह सही विकास है ? हम सब दोहरी जिन्दगी जीते हैं। एक संसार वह है जो हमें मिला है-स्वयं सृष्टि। इसी के समानान्तर एक और दुनिया है जो आदमी ने बनाई है-पंख और पहियों और तारों पर भागती, भोग के लिए उकसाती, परिचय को निर्वैयक्तिक करती, एक आयामवाले लोगों को जन्म देती, खाली और खोखली। सच है कि जिन्दगी आज जितनी सुविधापरक और रंगीन है पहले कभी नहीं थी, मगर इसी के साथ यह भी सच है कि आज आदमी जितना बेचारा और गम़गीन है पहले कभी नहीं था। कदाचर सहज और लड़ाई पहले से भी बहुत ज्यादा भोली मगर खूँख़्वार हो गई है। पूर्व हो या पश्चिम दुख लगातार बढ़ रहा है। कितने उपदेशक आये-गये, क्रान्तियाँ हुई लेकिन आदमी जहाँ था वहीं सड़ रहा है। ऐसे वक्त में विवेकानन्द जैसे संन्यासी, कर्मयोगी, बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।
असल में यह कृति एक तरह की रूपरेखा है। इसका प्रारूप कुछ ऐसा है जो पाठकों से एक विशिष्ट मनोभूमि की अपेक्षा करता है। इसके रचना शिल्प में एक अच्छी फिल्म के सूत्र निहित हैं। यह कृति लिखी भी इसी उद्देश्य से गयी थी।
इस कृति का प्रकाशन कर इसे हमारे सहृदय पाठकों तक पहुँचाने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ।
नई
दिल्ली,
26 दिसम्बर, 1992
कैलाश वाजपेयी
दृश्य : एक
[कलकत्ता शहर की गौर मोहन स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन। बाहर
विश्वनाथ दत्त एडवोकेट लिखा है। भीतर आँगन में तुलसी का वृक्ष, शिव का
छोटा मन्दिर, अधेड़ दीख पड़ता। भुवनेश्वरी शिव के पास बैठी गा रही हैं-
नमामीशं ईशान-निर्वाणरूपम्
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद-स्वरूपम्।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।।
करालं महाकाल-कालं कृपालम्....]
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद-स्वरूपम्।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।।
करालं महाकाल-कालं कृपालम्....]
विश्वनाथ : भुवनेश्वरी, तुम्हारी शिवस्तुति अभी पूरी नहीं हुई ? रात गहरा
आयी है, अब सो भी जाओ।
भुवनेश्वरी : कोई प्रार्थना क्या कभी पूरी भी होती है ? वह भी आशुतोष की जिन्होंने हमें नरेन्द्र-सा बेटा दिया !
(पट बन्दकर उठती है। पास में रखा दिया लेकर आँगन पार करती हैं। बरामदे पर पहुँचकर द्वार खोलती हैं। दीये का प्रकाश जैसे-जैसे आगे बढ़ता है कमरा कुछ-कुछ साफ़ नज़र आता है। सामने पलँग पर पाँच-छह वर्ष की नरेन्द्र-बड़ी-बड़ी खुली हुई आँखें सामने टकटकी बाँधे देखती हुई)
(अकचकाकर) अरे बिले ! तू अभी तक सोया नहीं ?
नरेन्द्र : सोया होता तो जागता कैसे ?
भुवनेश्वरी : यही तो कह रही हूँ, सोया क्यों नहीं ?
नरेन्द्र : अँधेरे को देख रहा था, अँधेरा....इतना तमाम अँधेरा कहाँ से आ जाता है माँ!
भुवनेश्वरी : कोई प्रार्थना क्या कभी पूरी भी होती है ? वह भी आशुतोष की जिन्होंने हमें नरेन्द्र-सा बेटा दिया !
(पट बन्दकर उठती है। पास में रखा दिया लेकर आँगन पार करती हैं। बरामदे पर पहुँचकर द्वार खोलती हैं। दीये का प्रकाश जैसे-जैसे आगे बढ़ता है कमरा कुछ-कुछ साफ़ नज़र आता है। सामने पलँग पर पाँच-छह वर्ष की नरेन्द्र-बड़ी-बड़ी खुली हुई आँखें सामने टकटकी बाँधे देखती हुई)
(अकचकाकर) अरे बिले ! तू अभी तक सोया नहीं ?
नरेन्द्र : सोया होता तो जागता कैसे ?
भुवनेश्वरी : यही तो कह रही हूँ, सोया क्यों नहीं ?
नरेन्द्र : अँधेरे को देख रहा था, अँधेरा....इतना तमाम अँधेरा कहाँ से आ जाता है माँ!
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book