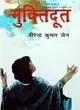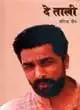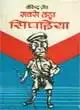|
कहानी संग्रह >> एक और नीलांजना एक और नीलांजनावीरेन्द्र जैन
|
140 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है एक आधुनिक प्रय़ोग एक और नीलांजना......
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
साहित्य के क्षेत्र में पुराकथा का वही स्थान और महत्व होता है जो काल के वर्तमान खण्ड के लिए अतीत का। कोई प्रयोगी प्रतिभा यदि पुराकथा की आज के साहित्य से समन्विति को उजागर कर दे तो वह प्रयत्न न केवल अपने में सार्थक बनता है बल्कि उपयोगिता की दृष्टि से सराहनीय भी माना जाता है।
द्वितीय संस्करण पर
‘एक और नीलांजना’ को निकले अभी पूरे दो वर्ष भी नहीं
हुए कि
उसका एक द्वितीय संस्करण आपके हाथ में है। ‘आम आदमी’
और
‘भोगा हुआ यथार्थ’ की नारे-बुलन्दी के आलम में इन
पुराकथाओं
के खो जाने का खतरा ही अधिक था। मगर हकीकत यह है कि आज के भीषण यथार्थ का
प्रतिक्षण भुक्त-भोगी आम आदमी ही इन कथाओं का सर्वोपरि पाठक है। और उसी
पाठक-वर्ग की माँग पर यह दूसरा संस्करण इतनी जल्दी सम्भव हुआ है। स्थापित
उच्चस्तरीय कहलाती हमारी समीक्षा के मानदण्ड तो इतने अवास्तविक घिसे-पिटे
और भोथरे हो चुके हैं कि वे आम आदमी के यथार्थ जीवन अनुभव संस्कार और समझ
से बहुत दूर पड़ गये हैं। आम आदमी को तो यह पता तक नहीं, उसकी चेतना और
पुकार की कैसी छदम अलगाववादी गलत और भ्रामक तसवीर साहित्य में पेश की जा
रही है।
पौराणिक रोमांस ‘मुक्तिदूत’, प्रस्तुत पुराकथा-संग्रह ‘एक और नीलांजना’ और उसके उपरान्त ‘अनुत्तर योगीः तीर्थकर महावीर’ सर्वसाधारण जागृत पाठक से लगाकर उच्चस्तरीय प्रबुद्ध भारतीय पाठक तक की चेतना में इतनी गहराई से व्यापते चले जा रहे हैं कि देखकर आश्चर्य होता है इसका कारण यह है कि बाह्म व्यवस्थागत सतही क्रान्ति इतनी अनिश्चित और विफल सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य उस ओर से निराश हो आया है। वह उसे अविश्वसनीय लगती है, उसमें उसे अब अपनी मुक्ति की सूरत और सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती। हर वाद, दल या राजसत्ता जिस इतिहास-व्यापी दुश्चक्र में फँसी है, उसका एक अवचेतनिक अहसास और साक्षात्कार मनुष्य को हो चुका है। उसे प्रतीति हो चुकी है कि राजनीति का लक्ष्य और जो कुछ भी हो, यह तो नहीं हो पा रहा कि समाज सुखी हो और व्यक्ति अपने को सार्थक होता पाये। यह एक ऐतिहासिक साक्षात्कार है जिसके साक्षात्कारी आम लोग है, साहित्यकार या अन्य विशेष वर्गों के लोग नहीं। बाहरी दुनिया की इस नग्न और कुरूप वास्तविकता को ठीक आँखों आगे पाकर, मनुष्य आपोआप भीतर की ओर मुड़ चला है। यह अब अपनी सुरक्षा और शान्ति, वास्तविक सुख की भूमि तक अपने ही भीतर खोजने को विवश हो गया है। आज का यह सर्वहारा मनुष्य अपनी आत्मा की तलाश में है। अब वह अपने ही अन्तरतम में कोई ऐसा निश्चल केन्द्र खोज रहा है, जिसके उजाले में वह अपनी सारी अन्तरबाह्य समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके।
मेरी ये पौराणिक कृतियाँ मानव इकाई की उसी सर्वथा स्वाधीन, भीतरी तलाश की प्रतीक-रूपकात्मक परिणतियाँ हैं। अपनी भीतरी अन्तरिक्ष और अनुभव-संसार की उसी अन्वेषण-यात्रा में से ये कथाएँ उतरी है। इसी से देखता हूँ कि आज का अभिनिवेशों और आरोपित धारणाओं से मुक्त सहज पाठक मेरी इन कृतियों की ओर मुग्ध मन से आकृष्ट हो रहा है। भीषण यथार्थ की त्रासदी को उलीचने वाले तथाकथित जनवादी और आम आदमी के साहित्य से वह अब ऊब गया है। उसे यह सब निरा पिष्टपेषण और दुहराव लगता है। उसकी आशा-आकांक्षा स्वप्नों और आत्मिक पुकार का अचूक उत्तर उसे इस कृत्रिम और सतही साहित्य में नहीं मिल रहा। वह उस साहित्य की तलाश में है जो उसकी निपीड़ित, गुमशुदा चेतना को अन्तश्चेतना के मौलिक जीवन-स्रोतों से जोड़ सके। बाहरी सामुदायिक प्रयत्नों के अनिश्चित और अविश्वसनीय कूटचक्रों से उसकी चेतना को उबारकर, जो उसे अपने ही भीतर स्वाधीन रूप से जीने को कोई अचूक ठौर, आधार या सहारा न दे सके।
मेरे पास आने वाले मेरे पाठकों के अनगिनत पत्रों से मुझे बारम्बार केवल यही प्रमाण मिला है कि मेरी इन मिथकीय कृतियों से उन्हें जीवन का अर्थ और प्रयोजन साक्षात्कृत होता है और जीने के लिए एक शक्ति और अवलम्ब प्राप्त होता है। उनकी अनेक उलझनें इन रचनाओं को पढ़ते हुए अनायास सुलझ जाती हैं। ‘एक और नीलांजना’ के इस द्वितीय संस्करण को प्रस्तुत करते हुए, मैं अपने ऐसे सच्चे भाविक पाठकों के प्रति अपनी आत्मिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।
पौराणिक रोमांस ‘मुक्तिदूत’, प्रस्तुत पुराकथा-संग्रह ‘एक और नीलांजना’ और उसके उपरान्त ‘अनुत्तर योगीः तीर्थकर महावीर’ सर्वसाधारण जागृत पाठक से लगाकर उच्चस्तरीय प्रबुद्ध भारतीय पाठक तक की चेतना में इतनी गहराई से व्यापते चले जा रहे हैं कि देखकर आश्चर्य होता है इसका कारण यह है कि बाह्म व्यवस्थागत सतही क्रान्ति इतनी अनिश्चित और विफल सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य उस ओर से निराश हो आया है। वह उसे अविश्वसनीय लगती है, उसमें उसे अब अपनी मुक्ति की सूरत और सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती। हर वाद, दल या राजसत्ता जिस इतिहास-व्यापी दुश्चक्र में फँसी है, उसका एक अवचेतनिक अहसास और साक्षात्कार मनुष्य को हो चुका है। उसे प्रतीति हो चुकी है कि राजनीति का लक्ष्य और जो कुछ भी हो, यह तो नहीं हो पा रहा कि समाज सुखी हो और व्यक्ति अपने को सार्थक होता पाये। यह एक ऐतिहासिक साक्षात्कार है जिसके साक्षात्कारी आम लोग है, साहित्यकार या अन्य विशेष वर्गों के लोग नहीं। बाहरी दुनिया की इस नग्न और कुरूप वास्तविकता को ठीक आँखों आगे पाकर, मनुष्य आपोआप भीतर की ओर मुड़ चला है। यह अब अपनी सुरक्षा और शान्ति, वास्तविक सुख की भूमि तक अपने ही भीतर खोजने को विवश हो गया है। आज का यह सर्वहारा मनुष्य अपनी आत्मा की तलाश में है। अब वह अपने ही अन्तरतम में कोई ऐसा निश्चल केन्द्र खोज रहा है, जिसके उजाले में वह अपनी सारी अन्तरबाह्य समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके।
मेरी ये पौराणिक कृतियाँ मानव इकाई की उसी सर्वथा स्वाधीन, भीतरी तलाश की प्रतीक-रूपकात्मक परिणतियाँ हैं। अपनी भीतरी अन्तरिक्ष और अनुभव-संसार की उसी अन्वेषण-यात्रा में से ये कथाएँ उतरी है। इसी से देखता हूँ कि आज का अभिनिवेशों और आरोपित धारणाओं से मुक्त सहज पाठक मेरी इन कृतियों की ओर मुग्ध मन से आकृष्ट हो रहा है। भीषण यथार्थ की त्रासदी को उलीचने वाले तथाकथित जनवादी और आम आदमी के साहित्य से वह अब ऊब गया है। उसे यह सब निरा पिष्टपेषण और दुहराव लगता है। उसकी आशा-आकांक्षा स्वप्नों और आत्मिक पुकार का अचूक उत्तर उसे इस कृत्रिम और सतही साहित्य में नहीं मिल रहा। वह उस साहित्य की तलाश में है जो उसकी निपीड़ित, गुमशुदा चेतना को अन्तश्चेतना के मौलिक जीवन-स्रोतों से जोड़ सके। बाहरी सामुदायिक प्रयत्नों के अनिश्चित और अविश्वसनीय कूटचक्रों से उसकी चेतना को उबारकर, जो उसे अपने ही भीतर स्वाधीन रूप से जीने को कोई अचूक ठौर, आधार या सहारा न दे सके।
मेरे पास आने वाले मेरे पाठकों के अनगिनत पत्रों से मुझे बारम्बार केवल यही प्रमाण मिला है कि मेरी इन मिथकीय कृतियों से उन्हें जीवन का अर्थ और प्रयोजन साक्षात्कृत होता है और जीने के लिए एक शक्ति और अवलम्ब प्राप्त होता है। उनकी अनेक उलझनें इन रचनाओं को पढ़ते हुए अनायास सुलझ जाती हैं। ‘एक और नीलांजना’ के इस द्वितीय संस्करण को प्रस्तुत करते हुए, मैं अपने ऐसे सच्चे भाविक पाठकों के प्रति अपनी आत्मिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।
1 जनवरी
वीरेन्द्र कुमार जैन
उद्भावना
प्रश्न उठता है, आज के जीवन-सन्दर्भ में पुराकथा की क्या सार्थकता है ?
क्या वह परम्परा की शाश्वती चैतन्यधारा में प्रतिष्ठित उदात्त और
ऊर्ध्वमुखी मानव-प्रतिभा की महत्ता को ध्वस्त करने के लिए, आज के
प्रतिवादी लेखक का प्रतीक-हथियार मात्र है ? या वह कोई चिरन्तन प्रगतिशील,
उन्नायक विधातृ शक्ति भी है ? उत्तर में मेरे
‘मुक्तिदूत’ की
एक चिन्मित पाठिका, ‘शोलापुर कॉलेज’ की प्राध्यापिका
कुमारी
मयूरी शाह के एक पत्र की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं :
‘‘आपका ‘मुक्तिदूत’ मेरी टेबल पर सदैव रहता है। फुरसत के समय चाहे जब पन्ना उलटती हूँ, और पढ़ती चली जाती हूँ। गत कई वर्षों में उसे कितनी बार पढ़ा होगा, कहना कठिन है।...पता नहीं कैसे, बचपन से ही मुक्तिदूत’ ने मेरे मन पर अमिट प्रभाव छोड़ा है. मेरा चैतन्य और जीवन उसी से मानो आकार लेता चला गया है। इसमें तिल मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है।....
‘‘लगता है ‘मुक्तिदूत’ ही मेरा जावीन-साथी है। मेरे सबसे भीतरी अकेलपन को उसने भरा है। ‘मुक्तिदूत’ की अंजना और वसन्त दीदी ही तो मेरी शास्वत सहेलियाँ हैं जीवन में आने वाली विपदाओं और समस्याओं का धीरज से सामना करने में, ‘मुक्तिदूत’ की अंजना ने ही तो मुझे सबसे अधिक शक्ति और सहारा दिया है।...मैं नृत्य करती हूँ निस्सन्देह। लेकिन कब ? जब ‘मुक्तिदूत’ का भावालोक बादल बनकर मेरे हृदय आकाश में छा जाता है, तो मेरे भीतर की मयूरी आनन्द-विभोर होकर नाचने लगती है। तब वह भरत नाट्यम होता है या और कोई नृत्य-प्रकार, मुझे नहीं मालूम।...
‘इसी प्रकार ‘तीर्थंकर’ मासिक में प्रकाशित आपकी कथाओं ने मेरे जीवन में कितना गहरा आध्यात्मिक रस सींचा है, कितनी आत्मिक शक्ति मुझे दी है, कह नहीं सकती। अब आपके उपन्यास ‘अनुत्तर योगी : तीर्थंकर महावीर’ की बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे निश्चित प्रतीति है कि आपका यह ग्रन्थ संसार-भर के साहित्य में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। वह अनन्त काल रहेगा। एक अज्ञात बहन की शुभेच्छा में यदि कोई शक्ति है, तो वह सदा मेरे भाई के पीछे खड़ी है, और झूठ नहीं होगी....।’’
बहन मयूरी का यह पत्र उन सैकड़ों पत्रों का प्रतिनिधि है, जो मुझे ‘मुक्तिदूत’ पर, ‘तीर्थंकर’ मासिक में प्रस्तुत कथाओं के प्रकाशन काल में मुझे मिलते रहे हैं। हजारों पाठकों को शक्ति और संबल देने वाली, साहित्य की इस उर्ध्वौमेषिनी, निर्मातृ, रूपान्तरकारी शक्ति का क्या कोई मूल्य नहीं ? क्या आज की जलती वास्तविकता का महज ज्वलन्त आलेखन ही साहित्य का एक मात्र ‘फंक्शन’ (कर्तृत्व’) है। सीमित देह मन की अज्ञानिनी भूमिका पर सदा घटित हो रही है, जीवन की ट्रेजडी, विषमता और कुरूपता को, एक ‘हॉण्टिंग’ सर्जनात्मक गुणवत्ता से नग्न करना ही, क्या साहित्य की एकमेव उपलब्धि है ? क्या अन्तिम प्रश्न-चिह्न आँकने और समस्याओं के जंगल खड़े कर देने पर ही साहित्य समाप्त है ?
क्या आत्म-द्रोह, लक्ष्यहीन विद्रोह, नाराबुलन्दी और पतन, पराजय, कुण्ठा की कलात्मक उलटबासियों से आगे साहित्य नहीं जाता ? कोई साहित्य यदि लक्ष-लक्ष मानव आत्माओं को संघर्ष करने की ताकत दे, उनके चिर निपीड़क प्रश्नों, समस्यों और उलझनों का समाधान करे, उन्हें उद्बुद्ध करे, जीवन और मुक्ति की कोई अचूक नयी राह उनके लिए खोल दे, तो क्या उसका कोई मूल्य नहीं ? क्या वह घटिया साहित्य है ? क्या उसकी कोई उच्च सृजनात्मक और कलात्मक उपलब्धि नहीं ? यदि है तो मेरे इस पौराणिक कथा-सृजन ने उसमें बेशक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, जिसका मुझे भी अभी पूरा अन्दाज नहीं है। निश्चय ही एक नित-नव्य, चिर प्रगतिमान नूतन चेतना और मनुष्य के सृजन की दिशा में मेरे इस विन्रम कृतित्व ने किस क़दर सफलता पायी है। आज का आलोचक चाहे तो इसे ही मेरे साहित्य की विफलता मानने को स्वतंत्र है। भावक तो मेरे इस सफलता के सचोट साक्षी हैं ही। लेकिन असलियत क्या है, उसका निर्णय तो महाकाल की धारा ही करेगी।
बेवजह बौद्धिक घुमाव-फिराव और उक्ति वैचित्र्य की कलाबाजारियों से बात को उलझाना मेरी आदत नहीं है, मेरे मन सृजन वह, जो भावक की अब तक की अस्पष्ट गहराइयों को हिला दे, उनमें निहित सम्भावनाओं को ऊपर ले आये, उनकी क्रिया-शक्ति को जीवन में संचरित कर दे; जो जीवन और जगत का एक ऊर्ध्वमुखी, प्रतिमान निर्माण करे; जो मनुष्य को उसकी अवचेतना के जन्मान्तव्यापी अन्धकारों, अराजकताओं और उलझनों से बाहर लाये; हर प्रतिकूलता के विरुद्ध अपराजेय आत्म-शक्ति के साथ जूझकर, अपने विकाश के लिए अनुकूल; सुखद-सुन्दर, आनन्दमय संवादी विश्व-रचना करने की सामर्थ्य उसे प्रदान करे।
बेशक, आज मनुष्य सर्वथा दिशाहारा हो गया है। वह सत्यानाश की कगार पर खड़ा है। अन्तहीन अन्धकार में भटकने को वह लाचार छूट गया है। लेकिन यही मनुष्य की अन्तिम नियति नहीं कि वह इन्हें अभीष्ट नहीं मानता। इस नकारात्मक परिबलों (फोर्सेज) को पराजित कर, पछाड़कर वह प्रकाश, सौन्दर्य, आनन्द, संवादिता के सुखी विश्व में जीने को बेताब है। अन्धकार कितना ही दुर्दान्त और सर्वग्रासी क्यों न हो, आखिर उसकी सीमा है। प्रकाश की कोई सीमा नहीं। वह सृष्टि की मौलिक और शाश्वती सत्ता है। अन्धकार एक सापेक्ष, नकारात्मक, अभावात्मक अवरोध मात्र है। हम उसे नहीं चाहते, यही प्रमाणित करता है कि वह अनिवार्य नहीं। उसे हट जाना होगा, उसे फट जाना पड़ेगा। अन्तिम सत्य, मृत्यु नहीं, जीवन है, अनन्त जीवन।
यह सच है कि मौजूदा प्रजातन्त्र सर्वत्र एक छलावा है। सच्चाई से उसका कोई सरोकार नहीं। वह एक मुखैटा है, खूबसूरत ओट है, कुछ समर्थों और शक्तिशालियों के न्यस्त-स्वार्थों, हितों की व्यवस्था को निर्बाध जारी रखने का सुरक्षा-दुर्ग है। माना कि आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था एवं तथाकथित धार्मिकता एवं नैतिकता कोटि-कोटि निर्बल मानवों के विरुद्ध, मुट्टीभर शक्तिमान् सत्ता-सम्पत्ति-स्वामियों का एक अमानुषिक षड्यन्त्र है। लेकिन क्या कविता में उसे कलात्मक गालियाँ देने से, और उस पर व्यंग्य-आक्रमण करने में सारी सृजनात्मकता को चुका देने से, उसका उन्मूलन हो जाएगा ? मौजूदा व्यवस्था का जो पैशाचिक पंजा, मानव की संन्तानों को निरा प्रेत बनाये दे रहा है, उनकी आत्माओं को असूझ अंधकार में भटकाए दे रहा है। उसका अपनी कला में सशक्त व्यंग्य-विद्रूपात्मक चित्रण मात्र ही क्या साहित्य की इति-श्री है ? वह भी ऐसा साहित्य, जिसे लेखक लिखे, और केवल लेखक बिरादरी पढ़े, और ‘अहो रूपमहो ध्वनि :’ करती रहे। इस बीभत्सता का वह सचोट अनावरण और सृजनात्मक बोध क्या उन मानवों तक पहुँच पाता है, जो सच्चे अर्थ में जीवन की नंगी और कुरूप धरती पर इस नरक को भोग रहे हैं ? बल्कि सच्चाई यह है कि जो सीधे भुक्तभोगी हैं, वे ही इस नर्मकदर्यता के सच्चे साक्षात्कारी हैं। हमारा यह तमाम कलात्मक अनावरण उसके आगे छोटा पड़ता है। उसके लिए उनका कष्ट निरा कला-विलास नहीं। उनके लिए वह मृत्यु की रक्ताक्त चट्टान है, और वही जिन्दा रहने के लिए सच्चे अर्थ में उससे जूझते हुए, अविश्रान्त युद्ध कर रहे हैं।
जड़त्व और अन्धकार की इन नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध सतत युद्ध जारी रखने के लिए, जो सर्जक आत्मज्ञान, आत्मप्रकाश और आत्मशक्ति का अचूक शस्त्र युगान्तरों में मानव प्रजाओं के दे गये हैं, उन्हीं का साहित्य चिरंजीवी और कालजयी होकर आज भी जीवित है। सहस्त्राब्दियों पूर्व लिखा जाकर भी वह आज भी वह मनुष्य को अपनी विरोधी आसुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अजस्त्र प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। वेद, उपनिष्द्, वाल्मीकि, वेदव्यास, जिनसेन, अश्वघोष, होमर, वर्जिल, दान्ते, कालिदास, तुलसीदास, कबीर और तमाम मध्यकालीन सन्तों का साहित्य आज भी इसीलिए जन हृदय में जीवन्त और संचारित है, क्योंकि वह मात्र समकालीन वस्तुस्थिति के ज्वलन्त चित्रण पर ही समाप्त नहीं, वह परिवर्तमान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुरूप हर युग में मनुष्य को अन्धकार, मृत्यु, अत्याचार और पीड़न के विरुद्ध जेहाद करके, स्वाधीन मुक्त जीवन जीने और तदनुरूप विश्व-रचना करने की शक्ति प्रदान करता है।
आज प्रश्न यह है कि सही प्रजातन्त्र, उत्तरदायी शासन, कल्याणी व्यवस्था कौन लाये ? क्या उसे कोई थाली में परोसकर हमारे सामने रख देगा ? क्या उसे लाने का दायित्व औरों पर डालकर केवल भोक्ता हो रहने की छुट्टी हमें है ? हर बुराई का दायित्व दूसरों पर टालकर उन्हें गरियाना और मात्र उनका शाब्दिक भंजन करने में व्यस्त रहना ही क्या सच्चा विद्रोह और क्रान्ति कही जा सकती है ? जो राज्य और अर्थ-सत्ता पर बैठें हैं, वे क्या आसमान से उतरे हैं ? वे भी मूलतः हमारी ही तरह कमजोर और सीमित इंसान हैं। उनकी कमजोरियों और तज्जन्य बलात्कारों को उलटने के लिए हम खुद पहले उनसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। उनके जैसी ही अपनी प्राणिक दुर्बलताओं और सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मशक्ति का स्वामित्व प्राप्त करना होगा।
एक सच्चा प्रजातन्त्र और सही व्यवस्था लाने के लिए, पहले हमें अपने भीतर ही एक आत्मतन्त्र स्थापित करना होगा। केवल सतही व्यवस्था में परिवर्तन से कोई अभीष्ट और स्थायी परिणाम नहीं आ सकता। सारी दुनिया को अपने अनुकूल बदल देने के लिए, पहले हमें खुद को बदलना होगा। एक सही व्यक्ति, इकाई ही सही व्यवस्था ला सकती है। यदि स्थापित और विस्थापक, दोनों वही पक्ष अपनी मूल प्रकृति में एक कमजोर और गलत हैं तो सही और आदर्श व्यवस्था आखिर लाये कौन ? यही तो आज प्रश्नों का एक प्रश्न है। पहल कौन करे और कैसे करे ?
इसी प्रश्न का कोई सम्भाव्य उत्तर खोजने और देने का एक अन्वेषक प्रयास हैं मेरी ये प्रस्तुत पुराकथाएँ, मेरा ‘मुक्तिदूत’, मेरी कविताएँ, मेरा समूचा कृतित्व। और सम्प्रति महावीर पर लिखे जा रहे मेरे उपन्यास में भी, इसी प्रश्न के एक मूर्तिमान् उत्तर के रूप में ‘अनुत्तरयोगी तीर्थंकर महावीर’ अवतरित हो रहे हैं।
उपनिषद् के ऋषि ने कहा था : ‘आत्मानं विद्धि’। डेल्फी के यूनानी देवालय के शीर्ष पर खुदा है : ‘नो दाइसेल्फ’। बुद्ध ने कहा था : ‘अप्प दीपो भव’। जिनेश्वरों की अनादिकालीन वाणी कहती है : ‘पूर्ण आत्मज्ञान ही केवल ज्ञान है : वही सर्वज्ञता है : वही अनन्त ऐश्वर्य-भोग है, वही मोक्ष है !’ आदि काल से आज तक के सभी पारद्रष्टाओं ने, जीवन के चरम लक्ष्य को इसी रूप में परिभाषित किया है। मानो यह कोई बौद्धिक सिद्धान्त-निर्णय नहीं, अनुभवगम्य सत्य-साक्षात्कार की ज्वलन्त वाणी है। देश कालातीत रूप से यह स्वयंसिद्ध हक़ीक़त है।
अपने को पूरा जानो, तो सबको सही और पूरा जान सकते हो। स्व और पर का सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान होने पर ही, स्व और पर के बीच सही सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। इस विज्ञान तक पहुँचे बिना, व्यक्ति-व्यक्ति, वस्तु-वस्तु और व्यक्ति तथा वस्तु के बीच सही संगति स्थापित नहीं हो सकती। व्यक्तियों, समाजों, वर्गों, जातियों, राष्ट्रों के बीच सम्यक् सम्बन्ध की स्थापना, इसी स्व-पर के सम्यक् ज्ञान के आधार पर हो सकती है। किसी भी सच्ची नैतिकता और चारित्रिकता का आधार भी यही हो सकता है। किसी भी मांगलिक समाज, राज्य, अर्थतन्त्र, प्रजातन्त्र और सर्वोदयी व्यवस्था की सही बुनियाद यही हो सकती है। इस उपलब्धि को स्थगित करके, इससे कमतर किसी भी ज्ञान-विज्ञान द्वारा निर्धारित व्यवस्था और चारित्रिकता, छद्म, पाखण्डी और शोषक ही हो सकती है।
स्व को सही जानना यानी व्यक्ति वस्तु के मौलिक स्व-भाव की, स्व-रूप को जानना है और स्व-भाव तथा स्व-रूप को जानकर, उसी में जीना सच्चा, और सार्थक और सुख-शान्तिपूर्वक जीना है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि की आचार संहिताएँ इसी स्वभावगत जीवन-स्थित को उपलब्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता में से निपजी हैं। स्वतन्त्र और शोषण-मुक्त जीवन और व्यवस्था की शर्त है, यह स्व-भाव में जीवन-धारण व्यक्ति से आरम्भ होकर ही विश्वव्यापी हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं स्वभाव और स्वरूप-ज्ञान में नहीं जीते, वे सारी दुनिया में सही जीवन-व्यवस्था लाने का दावा कैसे कर सकते हैं ? ऐसा दावा परिणाम में दाम्भिक, स्वार्थी और विकृत ही सिद्ध हो सकता है। व्यक्ति पहले स्वयं ही स्वभाव में अवस्थित हो, तभी वह सारे विश्व में अभीष्ट रूपान्तर या उत्क्रान्ति उपस्थित कर सकता है। यानी व्यक्ति की आत्मगत और स्वचेतनागत पहल ही सबसे बुनियादी और महत्त्वपूर्ण चीज़ है।
अटूट आत्मनिष्ठा और संचेतन, स्वैच्छिक आत्मदान ही इस पहल का तन्त्र हो सकता है। प्रतिपक्षी के अहंकार, राग-द्वेष, शोषण, अत्याचार के प्रत्युत्र में हमारे भीतर से प्रति-अहंकार, प्रतिराग-द्वेष, प्रतिशोषण, प्रति-अत्याचार न लौटे। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्याघात नहीं, प्रेम लौटे, प्रभुता लौटे। प्रतिक्रिया नहीं, चैतन्य की शुद्ध और नव्य क्रिया प्रवाहित हो, जिसके आत्म तेजस्वी संघात से विरोधी जड़-शक्ति की समूल विनाश हो जाए।
प्रस्तुत कहानियों की रचना में यही तत्त्व मौलिक रूप से अन्तर्निहित है। इनके पात्र प्रथमतः आत्मान्वेषी हैं, आत्मालोचक हैं, आत्मज्ञान के जिज्ञासु और खोजी है। उन्हें प्रथमतः अपनी स्वयं की, अपनी आत्मा की तलाश है। उनमें उत्कट पृच्छा है- कि क्या उनके भीतर कोई ऐसी अखण्ड अस्मिता या इयत्ता है जो क्षण-क्षण परिवर्तनशील मानसिक अवस्थाओं से परे, कोई ध्रुव, शाश्वत, समरस सत्ता रखती हो, जो तमाम बाहरी हालात चढ़ाव-उतार, संघर्षों, यन्त्रणाओं में स्वयं गुजरती हुई भी, कहीं उनसे अस्पृष्ट रहकर, उत्तीर्ण होकर, अपने साक्षी और द्रष्टाभाव में अविचल रह सकती हो; जो देह-मानसिक स्तर की अज्ञानी भूमिका पर गलत या विंसवादी हो गयी जीवन-व्यवस्था में, अपने भीतर के इस अखण्ड चैतन्य में से पहल करके, संवादिता ला सकती हो, नयी और कल्याणकारी सृष्टि रच सकती हो।
‘‘आपका ‘मुक्तिदूत’ मेरी टेबल पर सदैव रहता है। फुरसत के समय चाहे जब पन्ना उलटती हूँ, और पढ़ती चली जाती हूँ। गत कई वर्षों में उसे कितनी बार पढ़ा होगा, कहना कठिन है।...पता नहीं कैसे, बचपन से ही मुक्तिदूत’ ने मेरे मन पर अमिट प्रभाव छोड़ा है. मेरा चैतन्य और जीवन उसी से मानो आकार लेता चला गया है। इसमें तिल मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है।....
‘‘लगता है ‘मुक्तिदूत’ ही मेरा जावीन-साथी है। मेरे सबसे भीतरी अकेलपन को उसने भरा है। ‘मुक्तिदूत’ की अंजना और वसन्त दीदी ही तो मेरी शास्वत सहेलियाँ हैं जीवन में आने वाली विपदाओं और समस्याओं का धीरज से सामना करने में, ‘मुक्तिदूत’ की अंजना ने ही तो मुझे सबसे अधिक शक्ति और सहारा दिया है।...मैं नृत्य करती हूँ निस्सन्देह। लेकिन कब ? जब ‘मुक्तिदूत’ का भावालोक बादल बनकर मेरे हृदय आकाश में छा जाता है, तो मेरे भीतर की मयूरी आनन्द-विभोर होकर नाचने लगती है। तब वह भरत नाट्यम होता है या और कोई नृत्य-प्रकार, मुझे नहीं मालूम।...
‘इसी प्रकार ‘तीर्थंकर’ मासिक में प्रकाशित आपकी कथाओं ने मेरे जीवन में कितना गहरा आध्यात्मिक रस सींचा है, कितनी आत्मिक शक्ति मुझे दी है, कह नहीं सकती। अब आपके उपन्यास ‘अनुत्तर योगी : तीर्थंकर महावीर’ की बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे निश्चित प्रतीति है कि आपका यह ग्रन्थ संसार-भर के साहित्य में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। वह अनन्त काल रहेगा। एक अज्ञात बहन की शुभेच्छा में यदि कोई शक्ति है, तो वह सदा मेरे भाई के पीछे खड़ी है, और झूठ नहीं होगी....।’’
बहन मयूरी का यह पत्र उन सैकड़ों पत्रों का प्रतिनिधि है, जो मुझे ‘मुक्तिदूत’ पर, ‘तीर्थंकर’ मासिक में प्रस्तुत कथाओं के प्रकाशन काल में मुझे मिलते रहे हैं। हजारों पाठकों को शक्ति और संबल देने वाली, साहित्य की इस उर्ध्वौमेषिनी, निर्मातृ, रूपान्तरकारी शक्ति का क्या कोई मूल्य नहीं ? क्या आज की जलती वास्तविकता का महज ज्वलन्त आलेखन ही साहित्य का एक मात्र ‘फंक्शन’ (कर्तृत्व’) है। सीमित देह मन की अज्ञानिनी भूमिका पर सदा घटित हो रही है, जीवन की ट्रेजडी, विषमता और कुरूपता को, एक ‘हॉण्टिंग’ सर्जनात्मक गुणवत्ता से नग्न करना ही, क्या साहित्य की एकमेव उपलब्धि है ? क्या अन्तिम प्रश्न-चिह्न आँकने और समस्याओं के जंगल खड़े कर देने पर ही साहित्य समाप्त है ?
क्या आत्म-द्रोह, लक्ष्यहीन विद्रोह, नाराबुलन्दी और पतन, पराजय, कुण्ठा की कलात्मक उलटबासियों से आगे साहित्य नहीं जाता ? कोई साहित्य यदि लक्ष-लक्ष मानव आत्माओं को संघर्ष करने की ताकत दे, उनके चिर निपीड़क प्रश्नों, समस्यों और उलझनों का समाधान करे, उन्हें उद्बुद्ध करे, जीवन और मुक्ति की कोई अचूक नयी राह उनके लिए खोल दे, तो क्या उसका कोई मूल्य नहीं ? क्या वह घटिया साहित्य है ? क्या उसकी कोई उच्च सृजनात्मक और कलात्मक उपलब्धि नहीं ? यदि है तो मेरे इस पौराणिक कथा-सृजन ने उसमें बेशक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, जिसका मुझे भी अभी पूरा अन्दाज नहीं है। निश्चय ही एक नित-नव्य, चिर प्रगतिमान नूतन चेतना और मनुष्य के सृजन की दिशा में मेरे इस विन्रम कृतित्व ने किस क़दर सफलता पायी है। आज का आलोचक चाहे तो इसे ही मेरे साहित्य की विफलता मानने को स्वतंत्र है। भावक तो मेरे इस सफलता के सचोट साक्षी हैं ही। लेकिन असलियत क्या है, उसका निर्णय तो महाकाल की धारा ही करेगी।
बेवजह बौद्धिक घुमाव-फिराव और उक्ति वैचित्र्य की कलाबाजारियों से बात को उलझाना मेरी आदत नहीं है, मेरे मन सृजन वह, जो भावक की अब तक की अस्पष्ट गहराइयों को हिला दे, उनमें निहित सम्भावनाओं को ऊपर ले आये, उनकी क्रिया-शक्ति को जीवन में संचरित कर दे; जो जीवन और जगत का एक ऊर्ध्वमुखी, प्रतिमान निर्माण करे; जो मनुष्य को उसकी अवचेतना के जन्मान्तव्यापी अन्धकारों, अराजकताओं और उलझनों से बाहर लाये; हर प्रतिकूलता के विरुद्ध अपराजेय आत्म-शक्ति के साथ जूझकर, अपने विकाश के लिए अनुकूल; सुखद-सुन्दर, आनन्दमय संवादी विश्व-रचना करने की सामर्थ्य उसे प्रदान करे।
बेशक, आज मनुष्य सर्वथा दिशाहारा हो गया है। वह सत्यानाश की कगार पर खड़ा है। अन्तहीन अन्धकार में भटकने को वह लाचार छूट गया है। लेकिन यही मनुष्य की अन्तिम नियति नहीं कि वह इन्हें अभीष्ट नहीं मानता। इस नकारात्मक परिबलों (फोर्सेज) को पराजित कर, पछाड़कर वह प्रकाश, सौन्दर्य, आनन्द, संवादिता के सुखी विश्व में जीने को बेताब है। अन्धकार कितना ही दुर्दान्त और सर्वग्रासी क्यों न हो, आखिर उसकी सीमा है। प्रकाश की कोई सीमा नहीं। वह सृष्टि की मौलिक और शाश्वती सत्ता है। अन्धकार एक सापेक्ष, नकारात्मक, अभावात्मक अवरोध मात्र है। हम उसे नहीं चाहते, यही प्रमाणित करता है कि वह अनिवार्य नहीं। उसे हट जाना होगा, उसे फट जाना पड़ेगा। अन्तिम सत्य, मृत्यु नहीं, जीवन है, अनन्त जीवन।
यह सच है कि मौजूदा प्रजातन्त्र सर्वत्र एक छलावा है। सच्चाई से उसका कोई सरोकार नहीं। वह एक मुखैटा है, खूबसूरत ओट है, कुछ समर्थों और शक्तिशालियों के न्यस्त-स्वार्थों, हितों की व्यवस्था को निर्बाध जारी रखने का सुरक्षा-दुर्ग है। माना कि आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था एवं तथाकथित धार्मिकता एवं नैतिकता कोटि-कोटि निर्बल मानवों के विरुद्ध, मुट्टीभर शक्तिमान् सत्ता-सम्पत्ति-स्वामियों का एक अमानुषिक षड्यन्त्र है। लेकिन क्या कविता में उसे कलात्मक गालियाँ देने से, और उस पर व्यंग्य-आक्रमण करने में सारी सृजनात्मकता को चुका देने से, उसका उन्मूलन हो जाएगा ? मौजूदा व्यवस्था का जो पैशाचिक पंजा, मानव की संन्तानों को निरा प्रेत बनाये दे रहा है, उनकी आत्माओं को असूझ अंधकार में भटकाए दे रहा है। उसका अपनी कला में सशक्त व्यंग्य-विद्रूपात्मक चित्रण मात्र ही क्या साहित्य की इति-श्री है ? वह भी ऐसा साहित्य, जिसे लेखक लिखे, और केवल लेखक बिरादरी पढ़े, और ‘अहो रूपमहो ध्वनि :’ करती रहे। इस बीभत्सता का वह सचोट अनावरण और सृजनात्मक बोध क्या उन मानवों तक पहुँच पाता है, जो सच्चे अर्थ में जीवन की नंगी और कुरूप धरती पर इस नरक को भोग रहे हैं ? बल्कि सच्चाई यह है कि जो सीधे भुक्तभोगी हैं, वे ही इस नर्मकदर्यता के सच्चे साक्षात्कारी हैं। हमारा यह तमाम कलात्मक अनावरण उसके आगे छोटा पड़ता है। उसके लिए उनका कष्ट निरा कला-विलास नहीं। उनके लिए वह मृत्यु की रक्ताक्त चट्टान है, और वही जिन्दा रहने के लिए सच्चे अर्थ में उससे जूझते हुए, अविश्रान्त युद्ध कर रहे हैं।
जड़त्व और अन्धकार की इन नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध सतत युद्ध जारी रखने के लिए, जो सर्जक आत्मज्ञान, आत्मप्रकाश और आत्मशक्ति का अचूक शस्त्र युगान्तरों में मानव प्रजाओं के दे गये हैं, उन्हीं का साहित्य चिरंजीवी और कालजयी होकर आज भी जीवित है। सहस्त्राब्दियों पूर्व लिखा जाकर भी वह आज भी वह मनुष्य को अपनी विरोधी आसुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अजस्त्र प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। वेद, उपनिष्द्, वाल्मीकि, वेदव्यास, जिनसेन, अश्वघोष, होमर, वर्जिल, दान्ते, कालिदास, तुलसीदास, कबीर और तमाम मध्यकालीन सन्तों का साहित्य आज भी इसीलिए जन हृदय में जीवन्त और संचारित है, क्योंकि वह मात्र समकालीन वस्तुस्थिति के ज्वलन्त चित्रण पर ही समाप्त नहीं, वह परिवर्तमान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुरूप हर युग में मनुष्य को अन्धकार, मृत्यु, अत्याचार और पीड़न के विरुद्ध जेहाद करके, स्वाधीन मुक्त जीवन जीने और तदनुरूप विश्व-रचना करने की शक्ति प्रदान करता है।
आज प्रश्न यह है कि सही प्रजातन्त्र, उत्तरदायी शासन, कल्याणी व्यवस्था कौन लाये ? क्या उसे कोई थाली में परोसकर हमारे सामने रख देगा ? क्या उसे लाने का दायित्व औरों पर डालकर केवल भोक्ता हो रहने की छुट्टी हमें है ? हर बुराई का दायित्व दूसरों पर टालकर उन्हें गरियाना और मात्र उनका शाब्दिक भंजन करने में व्यस्त रहना ही क्या सच्चा विद्रोह और क्रान्ति कही जा सकती है ? जो राज्य और अर्थ-सत्ता पर बैठें हैं, वे क्या आसमान से उतरे हैं ? वे भी मूलतः हमारी ही तरह कमजोर और सीमित इंसान हैं। उनकी कमजोरियों और तज्जन्य बलात्कारों को उलटने के लिए हम खुद पहले उनसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। उनके जैसी ही अपनी प्राणिक दुर्बलताओं और सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मशक्ति का स्वामित्व प्राप्त करना होगा।
एक सच्चा प्रजातन्त्र और सही व्यवस्था लाने के लिए, पहले हमें अपने भीतर ही एक आत्मतन्त्र स्थापित करना होगा। केवल सतही व्यवस्था में परिवर्तन से कोई अभीष्ट और स्थायी परिणाम नहीं आ सकता। सारी दुनिया को अपने अनुकूल बदल देने के लिए, पहले हमें खुद को बदलना होगा। एक सही व्यक्ति, इकाई ही सही व्यवस्था ला सकती है। यदि स्थापित और विस्थापक, दोनों वही पक्ष अपनी मूल प्रकृति में एक कमजोर और गलत हैं तो सही और आदर्श व्यवस्था आखिर लाये कौन ? यही तो आज प्रश्नों का एक प्रश्न है। पहल कौन करे और कैसे करे ?
इसी प्रश्न का कोई सम्भाव्य उत्तर खोजने और देने का एक अन्वेषक प्रयास हैं मेरी ये प्रस्तुत पुराकथाएँ, मेरा ‘मुक्तिदूत’, मेरी कविताएँ, मेरा समूचा कृतित्व। और सम्प्रति महावीर पर लिखे जा रहे मेरे उपन्यास में भी, इसी प्रश्न के एक मूर्तिमान् उत्तर के रूप में ‘अनुत्तरयोगी तीर्थंकर महावीर’ अवतरित हो रहे हैं।
उपनिषद् के ऋषि ने कहा था : ‘आत्मानं विद्धि’। डेल्फी के यूनानी देवालय के शीर्ष पर खुदा है : ‘नो दाइसेल्फ’। बुद्ध ने कहा था : ‘अप्प दीपो भव’। जिनेश्वरों की अनादिकालीन वाणी कहती है : ‘पूर्ण आत्मज्ञान ही केवल ज्ञान है : वही सर्वज्ञता है : वही अनन्त ऐश्वर्य-भोग है, वही मोक्ष है !’ आदि काल से आज तक के सभी पारद्रष्टाओं ने, जीवन के चरम लक्ष्य को इसी रूप में परिभाषित किया है। मानो यह कोई बौद्धिक सिद्धान्त-निर्णय नहीं, अनुभवगम्य सत्य-साक्षात्कार की ज्वलन्त वाणी है। देश कालातीत रूप से यह स्वयंसिद्ध हक़ीक़त है।
अपने को पूरा जानो, तो सबको सही और पूरा जान सकते हो। स्व और पर का सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान होने पर ही, स्व और पर के बीच सही सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। इस विज्ञान तक पहुँचे बिना, व्यक्ति-व्यक्ति, वस्तु-वस्तु और व्यक्ति तथा वस्तु के बीच सही संगति स्थापित नहीं हो सकती। व्यक्तियों, समाजों, वर्गों, जातियों, राष्ट्रों के बीच सम्यक् सम्बन्ध की स्थापना, इसी स्व-पर के सम्यक् ज्ञान के आधार पर हो सकती है। किसी भी सच्ची नैतिकता और चारित्रिकता का आधार भी यही हो सकता है। किसी भी मांगलिक समाज, राज्य, अर्थतन्त्र, प्रजातन्त्र और सर्वोदयी व्यवस्था की सही बुनियाद यही हो सकती है। इस उपलब्धि को स्थगित करके, इससे कमतर किसी भी ज्ञान-विज्ञान द्वारा निर्धारित व्यवस्था और चारित्रिकता, छद्म, पाखण्डी और शोषक ही हो सकती है।
स्व को सही जानना यानी व्यक्ति वस्तु के मौलिक स्व-भाव की, स्व-रूप को जानना है और स्व-भाव तथा स्व-रूप को जानकर, उसी में जीना सच्चा, और सार्थक और सुख-शान्तिपूर्वक जीना है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि की आचार संहिताएँ इसी स्वभावगत जीवन-स्थित को उपलब्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता में से निपजी हैं। स्वतन्त्र और शोषण-मुक्त जीवन और व्यवस्था की शर्त है, यह स्व-भाव में जीवन-धारण व्यक्ति से आरम्भ होकर ही विश्वव्यापी हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं स्वभाव और स्वरूप-ज्ञान में नहीं जीते, वे सारी दुनिया में सही जीवन-व्यवस्था लाने का दावा कैसे कर सकते हैं ? ऐसा दावा परिणाम में दाम्भिक, स्वार्थी और विकृत ही सिद्ध हो सकता है। व्यक्ति पहले स्वयं ही स्वभाव में अवस्थित हो, तभी वह सारे विश्व में अभीष्ट रूपान्तर या उत्क्रान्ति उपस्थित कर सकता है। यानी व्यक्ति की आत्मगत और स्वचेतनागत पहल ही सबसे बुनियादी और महत्त्वपूर्ण चीज़ है।
अटूट आत्मनिष्ठा और संचेतन, स्वैच्छिक आत्मदान ही इस पहल का तन्त्र हो सकता है। प्रतिपक्षी के अहंकार, राग-द्वेष, शोषण, अत्याचार के प्रत्युत्र में हमारे भीतर से प्रति-अहंकार, प्रतिराग-द्वेष, प्रतिशोषण, प्रति-अत्याचार न लौटे। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्याघात नहीं, प्रेम लौटे, प्रभुता लौटे। प्रतिक्रिया नहीं, चैतन्य की शुद्ध और नव्य क्रिया प्रवाहित हो, जिसके आत्म तेजस्वी संघात से विरोधी जड़-शक्ति की समूल विनाश हो जाए।
प्रस्तुत कहानियों की रचना में यही तत्त्व मौलिक रूप से अन्तर्निहित है। इनके पात्र प्रथमतः आत्मान्वेषी हैं, आत्मालोचक हैं, आत्मज्ञान के जिज्ञासु और खोजी है। उन्हें प्रथमतः अपनी स्वयं की, अपनी आत्मा की तलाश है। उनमें उत्कट पृच्छा है- कि क्या उनके भीतर कोई ऐसी अखण्ड अस्मिता या इयत्ता है जो क्षण-क्षण परिवर्तनशील मानसिक अवस्थाओं से परे, कोई ध्रुव, शाश्वत, समरस सत्ता रखती हो, जो तमाम बाहरी हालात चढ़ाव-उतार, संघर्षों, यन्त्रणाओं में स्वयं गुजरती हुई भी, कहीं उनसे अस्पृष्ट रहकर, उत्तीर्ण होकर, अपने साक्षी और द्रष्टाभाव में अविचल रह सकती हो; जो देह-मानसिक स्तर की अज्ञानी भूमिका पर गलत या विंसवादी हो गयी जीवन-व्यवस्था में, अपने भीतर के इस अखण्ड चैतन्य में से पहल करके, संवादिता ला सकती हो, नयी और कल्याणकारी सृष्टि रच सकती हो।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book