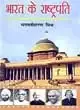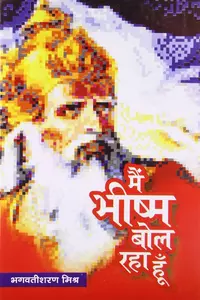|
पौराणिक >> पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमभगवतीशरण मिश्र
|
201 पाठक हैं |
||||||
ऐतिहासिक एवं पौराणिक गाथाओं को आधुनिक सन्दर्भ प्रदान करने में सिद्धहस्त, बहुचर्चित लेखक की नवीनतम औपन्यासिक कृति...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ऐतिहासिक एवं पौराणिक गाथाओं को आधुनिक सन्दर्भ प्रदान करने में सिद्धहस्त, बहुचर्चित लेखक की यह नवीनतम औपन्यासिक कृति अपनी भाषा के माधुर्य एवं शिल्पगत सौष्ठव द्वारा पाठक को मुग्ध किए बिना नहीं रहेगी।
‘पहला सूरज’, एवं ‘पवन पुत्र’ जैसी बहुचर्चित
कृतियों के पश्चात् श्रीकृष्ण जीवन के उत्तरार्ध पर आधारित यह बृहत्
उपन्यास डॉ. मिश्र की लेखकीय यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है जो केवल
अपनी आधुनिक दृष्टि ही नहीं अपितु विचारों की नवोन्मेषता और मौलिकता के
कारण भी विशिष्ट है।
डॉ. मिश्र शिल्पकार पहले हैं और उपन्यासकार बाद में, यही कारण है कि पुस्तक अथ से इति तक पाठक के मन को बाँधने में सक्षम है और श्रीकृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व के जटिलतम प्रसंग भी बोधगम्य एवं सहज सरल बन आए हैं।
श्रीकृष्ण को लेखक ने पुरुषोत्तम के रूप में ही देखा है और उसकी यह दृष्टि इस कृति को प्रासंगिक के साथ-साथ उपयोगी भी बना जाती है। विघटनशील मानवीय मूल्यों के इस काल में आदर्शों एवं मूल्यों की पुनर्स्थापना के सफल प्रयास का ही नाम है ‘पुरुषोत्तम’
डॉ. मिश्र शिल्पकार पहले हैं और उपन्यासकार बाद में, यही कारण है कि पुस्तक अथ से इति तक पाठक के मन को बाँधने में सक्षम है और श्रीकृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व के जटिलतम प्रसंग भी बोधगम्य एवं सहज सरल बन आए हैं।
श्रीकृष्ण को लेखक ने पुरुषोत्तम के रूप में ही देखा है और उसकी यह दृष्टि इस कृति को प्रासंगिक के साथ-साथ उपयोगी भी बना जाती है। विघटनशील मानवीय मूल्यों के इस काल में आदर्शों एवं मूल्यों की पुनर्स्थापना के सफल प्रयास का ही नाम है ‘पुरुषोत्तम’
यह पुस्तक
यद्यपि इस पुस्तक का लेखन प्रायः चार वर्षों में समाप्त हुआ क्योंकि 1987
में ही पवन पुत्र प्रकाशित हो गया था और उसके लेखन की समाप्ति के साथ ही
‘प्रथम पुरुष’ में हाथ लगा दिया गया था तथापि इस
उपन्यास के
लेखन में मात्र चार वर्ष लगे, ऐसा कहना उचित नहीं प्रतीत होता। इसका कारण
यह है कि कृष्ण के जीवन-चरित्र से सम्बन्धित पुस्तकों, विशेषकर
श्रीमद्भागवत, महाभारत तथा गीता से मेरा सम्बन्ध बाल्यकाल से ही रहा।
स्कूल के दिनों में जब संस्कृत पूरी तरह समझ में नहीं आती थी तब भी मैं इन
ग्रन्थों का संस्कृत श्लोकों के साथ-साथ हिन्दी टीका के साथ अध्ययन करता
था। बाद में तो भारत और गीता के अनुवादों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही,
फिर भी श्रीमद्भागवत के मूल पाठ से काम नहीं चलने को था और उसके अनुवाद के
साथ ही उसका अध्ययन सम्भव रहा क्योंकि श्रीमद्भागत की संस्कृत अन्य
ग्रन्थों की अपेक्षा कठिन है। कहा भी गया है कि विद्वानों की परीक्षा
श्रीमद्भागवत में ही होती है-
विद्यावताम् भागवते परीक्षा।
कहने का तात्पर्य यह कि कृष्ण-चरित्र बाल्यकाल से ही मेरे मन में बैठा था
और कृष्ण के व्यक्तित्व के प्रति एक विशेष आकर्षण बहुत पूर्व मेरे मन
मस्तिष्क में जड़ जमा चुका था। इसी के फलस्वरूप कृष्ण से सम्बन्धित जो कुछ
मिला, मैं पढ़ता गया।
इस पुस्तक के लेखन के पूर्व कृष्ण सम्बन्धी ग्रन्थों का विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ा। कृष्ण चरित्र मुख्यतः छह पुराणों में प्राप्त होता है-ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, महाभारत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण और श्रीमद्भागत पुराण। इनके अलावा गर्ग संहिता और पद्मपुराण में भी कृष्ण चरित्र विस्तार से मिलता है।
इन पुराणों में ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण में कथा प्रायः एक-सी है, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा श्रीमद्भागवत की कथा कुछ हद तक मिलती जुलती है।
पुराणों की कथाओं में भिन्नता होने के कारण किसी एक पुराण पर एक उपन्यास को आधृत करना कठिन था। ऐसी स्थिति में इन सारे ग्रन्थों के अध्ययन के पश्चात् मुझे बहुत हद तक अपना स्वतन्त्र विचार निर्धारित करने को बाध्य होना पड़ा।
पुराण और इतिहास में यद्यपि अन्तर नहीं है क्योंकि पुराणों का आधार भी इतिहास ही होता है किन्तु पुराणकारों की यह विशेषता होती है कि वे अति- शयोक्तियों और रूपकों का सहारा लेकर ऐतिहासिक गाथा को सामान्य जन के मध्य लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो पुराण जिस व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होता है उसी को वह सर्वोपरि मानता है और उसे ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
ऐसी स्थिति में अगर पुराणों को अतिशयोक्तियों और अनावश्यक रूपकों से मुक्त कर दिया जाए तो पौराणिक आख्यान भी इतिहास प्रामाणिकता प्राप्त कर सकते हैं और पौराणिक उपन्यास भी ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आ सकते हैं।
मैं यह कहने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा कि मैंने इस उपन्यास को पौराणिक कम और ऐतिहासिक अधिक बनाने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में मैं पौराणिक उपन्यास कहने के बदले ऐतिहासिक उपन्यास कहना अधिक पसन्द करूंगा।
मेरे उपर्युक्त कथन का कुछ आधार है। कृष्ण और उनके समय के अन्य व्यक्तियों की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिह्न लगाना आसान नहीं। उनके काल में मगध में जरासंध का राज्य रहा। राजगृह में जरासंध की राजधानी थी जिसके प्रमाण आज भी वहाँ कई रूपों में मिलते हैं। अगर जरासंध की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है तो कृष्ण की ऐतिहासिकता को संदिग्ध करने का हमें कोई अधिकार नहीं। सारे विद्वानों ने महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता को स्वीकारा है और माना है कि वह आज से प्रायः पांच हजार वर्ष पूर्व लड़ा गया।
आगे चलकर पुराणों ने विशेषकर श्रीमद्भागत ने कृष्ण-चरित्र को अति-शयोक्तियों चमत्कारों और रूपकों से भर दिया। इसके फलस्वरूप कृष्ण मनुष्य नहीं रहकर ईश्वर बन आए। भागवतकार ने स्पष्ट कहा है कि अन्य सारे अवतार तो अंशावतार मात्र थे, कृष्ण भगवान थे-
इस पुस्तक के लेखन के पूर्व कृष्ण सम्बन्धी ग्रन्थों का विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ा। कृष्ण चरित्र मुख्यतः छह पुराणों में प्राप्त होता है-ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, महाभारत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण और श्रीमद्भागत पुराण। इनके अलावा गर्ग संहिता और पद्मपुराण में भी कृष्ण चरित्र विस्तार से मिलता है।
इन पुराणों में ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण में कथा प्रायः एक-सी है, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा श्रीमद्भागवत की कथा कुछ हद तक मिलती जुलती है।
पुराणों की कथाओं में भिन्नता होने के कारण किसी एक पुराण पर एक उपन्यास को आधृत करना कठिन था। ऐसी स्थिति में इन सारे ग्रन्थों के अध्ययन के पश्चात् मुझे बहुत हद तक अपना स्वतन्त्र विचार निर्धारित करने को बाध्य होना पड़ा।
पुराण और इतिहास में यद्यपि अन्तर नहीं है क्योंकि पुराणों का आधार भी इतिहास ही होता है किन्तु पुराणकारों की यह विशेषता होती है कि वे अति- शयोक्तियों और रूपकों का सहारा लेकर ऐतिहासिक गाथा को सामान्य जन के मध्य लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो पुराण जिस व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होता है उसी को वह सर्वोपरि मानता है और उसे ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
ऐसी स्थिति में अगर पुराणों को अतिशयोक्तियों और अनावश्यक रूपकों से मुक्त कर दिया जाए तो पौराणिक आख्यान भी इतिहास प्रामाणिकता प्राप्त कर सकते हैं और पौराणिक उपन्यास भी ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आ सकते हैं।
मैं यह कहने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा कि मैंने इस उपन्यास को पौराणिक कम और ऐतिहासिक अधिक बनाने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में मैं पौराणिक उपन्यास कहने के बदले ऐतिहासिक उपन्यास कहना अधिक पसन्द करूंगा।
मेरे उपर्युक्त कथन का कुछ आधार है। कृष्ण और उनके समय के अन्य व्यक्तियों की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिह्न लगाना आसान नहीं। उनके काल में मगध में जरासंध का राज्य रहा। राजगृह में जरासंध की राजधानी थी जिसके प्रमाण आज भी वहाँ कई रूपों में मिलते हैं। अगर जरासंध की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है तो कृष्ण की ऐतिहासिकता को संदिग्ध करने का हमें कोई अधिकार नहीं। सारे विद्वानों ने महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता को स्वीकारा है और माना है कि वह आज से प्रायः पांच हजार वर्ष पूर्व लड़ा गया।
आगे चलकर पुराणों ने विशेषकर श्रीमद्भागत ने कृष्ण-चरित्र को अति-शयोक्तियों चमत्कारों और रूपकों से भर दिया। इसके फलस्वरूप कृष्ण मनुष्य नहीं रहकर ईश्वर बन आए। भागवतकार ने स्पष्ट कहा है कि अन्य सारे अवतार तो अंशावतार मात्र थे, कृष्ण भगवान थे-
कृष्णस्तु भगवान स्वयम्।
मैंने इस पुस्तक में कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखकर मनुष्य के रूप
में देखने का प्रयास किया है। यह बात पृथक् है कि यह मनुष्य शनैःशनै
मनुष्यत्व को लांघता हुआ देवत्व और अंततः ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है।
इस पुस्तक के प्रणयन के समय मेरा दृष्टिकोण स्पष्टतः यह रहा है कि भगवान
पैदा नहीं होता बल्कि बनता है। राम को भी भगवान मानें तो राम भगवान के रूप
में पैदा नहीं हुए थे किन्तु उनके कर्त्तव्यों उनकी वीरता, उनके शौर्य
उनका त्याग, उनके दैवी गुणों-ने उन्हें धीरे-धीरे भगवान बनाया। आज लोग
बुद्ध, महावीर जैन तथा ईसा (क्राइस्ट) को भी भगवान मानने लगे हैं।
भागवतकार ने भी बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना है। ये सारे ऐतिहासिक पुरुष
हैं और ये मनुष्य से भगवान बने न कि ये भगवान बनकर ही पैदा हुए।
इसी तथ्य को मैंने इस पुस्तक के लिखने के समय सतत् ध्यानगत रखा है। यही कारण है कि मैंने कृष्ण चरित्र से जुड़े चमत्कारों को ग्रहण करने में संकोच किया है और हर ऐसी घटना को जिसे पुराणकारों ने चमत्कार के रूप में लिया है, मैंने प्राकृतिक अथवा वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया है। यही कारण है कि मेरे कृष्ण के एक साधारण शिशु के रूप में पैदा होते ही कारागार के कपाट स्वयं नहीं खुल जाते और न भाद्रपद की उफनती यमुना केवल कृष्ण-चरणों का स्पर्श प्राप्त कर वसुदैव को मार्ग दे देती है। इसी रूप में अन्य बातों को भी लिया जा सकता है। द्रोपदी के चीर हरण की बात को भी उस अतिरंजना से मुक्त रखा है जिससे उसे पुराणकारों अथवा अन्य भक्त कवियों ने युक्त किया है।
इस सन्दर्भ में और कुछ कहने की आवश्यकता है। निश्चय ही कृष्ण चरित्र के साथ बहुत अन्याय हुआ है, विशेषकर कुछेक पुराणों एवं श्रृंगारिक कवियों द्वारा राधा का नाम कृष्ण के साथ जोड़ कर ऐसी-ऐसी कामुक रचनाओं का प्रणयन हुआ है कि बहुतों को कृष्ण को भगवान क्या एक शिष्ट मनुष्य कहने में भी शर्म आती है। निश्चय ही ऐसे लेखकों ने या तो अपनी दमित वासनाओं को ऐसे लेखन द्वारा उजागर किया है अथवा राधा-कृष्ण की लीला का सहारा ले अपने आश्रयदाताओं राजाओं, महाराजाओं, सामन्तों के मनोरंजन अथवा उनकी कामभावना को संतृप्त करने का प्रयास किया है।
मेरा उपर्युक्त आरोप निराधार नहीं है। श्रीमद्भागवत कृष्ण-चरित्र का प्रामाणिक और एक तरह से आद्यतन ग्रन्थ माना जाता है। यद्यपि मेरे विचार से ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना भागवत की रचना के पश्चात हुई फिर भी श्रीमद्भागवत को कृष्ण के सन्दर्भ में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वह किसी अन्य ग्रन्थ को नहीं उपलब्ध हो सकी। पाठकों को यह ज्ञात कर आश्चर्य होगा कि इस भागवत में राधा का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में राधा-कृष्ण की केलि-कीड़ाओं, प्रणय प्रसंगों आदि का वर्णन कृष्ण चरित्र के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है ? बात यहीं तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी। कहने वाले राधा को परकीया भी कह गए और प्रत्यक्षतः वह श्रीकृष्ण पर परस्त्री गमन का आरोप लगाने से भी नहीं चूके। ढूँढ़ने वालों ने अपनी कल्पना का कमाल दिखाया और राधा के पति का भी नाम ढूंढ़ निकाला। बंगला के एक उपन्यासकार ने तो जी भरकर इस परकीया से कृष्ण की केलि कराई। अब वह किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक तथ्य को उद्घाटित कर रहा था या अपनी दमित वासनाओं और कुण्ठाओं को खुल खेलने का अवसर दे रहा था, यह तो पाठक ही कहेंगे। श्रृंगारिक कवियों ने जो कमाल किया उसे कहने की आवश्यकता नहीं किन्तु राधा-कृष्ण को ढाल बनाकर इस खेल को खेलने का जो अक्षम्य अपराध उन्होंने किया उसका उदाहरण अन्यत्र ढूंढ़े नहीं मिलता।
पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का उल्लेख अवश्य आया है परन्तु भक्ति-प्रधान होने के कारण इस ग्रन्थ में राधा को कृष्ण की सहचरी होने के साथ-साथ सीता, पार्वती अथवा लक्ष्मी की तरह एक पूजनीया नारी के रूप में ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कृष्ण में इस ग्रन्थ में राधा को साध्वी संबोधन प्रदान करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि तुम श्री हो, तुम्हारे बिना मैं केवल कृष्ण होता हूं और जब तुम मुझसे संयुक्त हो जाती हो तो मैं श्रीकृष्ण बन जाता हूं।
इसी तथ्य को मैंने इस पुस्तक के लिखने के समय सतत् ध्यानगत रखा है। यही कारण है कि मैंने कृष्ण चरित्र से जुड़े चमत्कारों को ग्रहण करने में संकोच किया है और हर ऐसी घटना को जिसे पुराणकारों ने चमत्कार के रूप में लिया है, मैंने प्राकृतिक अथवा वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया है। यही कारण है कि मेरे कृष्ण के एक साधारण शिशु के रूप में पैदा होते ही कारागार के कपाट स्वयं नहीं खुल जाते और न भाद्रपद की उफनती यमुना केवल कृष्ण-चरणों का स्पर्श प्राप्त कर वसुदैव को मार्ग दे देती है। इसी रूप में अन्य बातों को भी लिया जा सकता है। द्रोपदी के चीर हरण की बात को भी उस अतिरंजना से मुक्त रखा है जिससे उसे पुराणकारों अथवा अन्य भक्त कवियों ने युक्त किया है।
इस सन्दर्भ में और कुछ कहने की आवश्यकता है। निश्चय ही कृष्ण चरित्र के साथ बहुत अन्याय हुआ है, विशेषकर कुछेक पुराणों एवं श्रृंगारिक कवियों द्वारा राधा का नाम कृष्ण के साथ जोड़ कर ऐसी-ऐसी कामुक रचनाओं का प्रणयन हुआ है कि बहुतों को कृष्ण को भगवान क्या एक शिष्ट मनुष्य कहने में भी शर्म आती है। निश्चय ही ऐसे लेखकों ने या तो अपनी दमित वासनाओं को ऐसे लेखन द्वारा उजागर किया है अथवा राधा-कृष्ण की लीला का सहारा ले अपने आश्रयदाताओं राजाओं, महाराजाओं, सामन्तों के मनोरंजन अथवा उनकी कामभावना को संतृप्त करने का प्रयास किया है।
मेरा उपर्युक्त आरोप निराधार नहीं है। श्रीमद्भागवत कृष्ण-चरित्र का प्रामाणिक और एक तरह से आद्यतन ग्रन्थ माना जाता है। यद्यपि मेरे विचार से ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना भागवत की रचना के पश्चात हुई फिर भी श्रीमद्भागवत को कृष्ण के सन्दर्भ में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वह किसी अन्य ग्रन्थ को नहीं उपलब्ध हो सकी। पाठकों को यह ज्ञात कर आश्चर्य होगा कि इस भागवत में राधा का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में राधा-कृष्ण की केलि-कीड़ाओं, प्रणय प्रसंगों आदि का वर्णन कृष्ण चरित्र के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है ? बात यहीं तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी। कहने वाले राधा को परकीया भी कह गए और प्रत्यक्षतः वह श्रीकृष्ण पर परस्त्री गमन का आरोप लगाने से भी नहीं चूके। ढूँढ़ने वालों ने अपनी कल्पना का कमाल दिखाया और राधा के पति का भी नाम ढूंढ़ निकाला। बंगला के एक उपन्यासकार ने तो जी भरकर इस परकीया से कृष्ण की केलि कराई। अब वह किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक तथ्य को उद्घाटित कर रहा था या अपनी दमित वासनाओं और कुण्ठाओं को खुल खेलने का अवसर दे रहा था, यह तो पाठक ही कहेंगे। श्रृंगारिक कवियों ने जो कमाल किया उसे कहने की आवश्यकता नहीं किन्तु राधा-कृष्ण को ढाल बनाकर इस खेल को खेलने का जो अक्षम्य अपराध उन्होंने किया उसका उदाहरण अन्यत्र ढूंढ़े नहीं मिलता।
पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का उल्लेख अवश्य आया है परन्तु भक्ति-प्रधान होने के कारण इस ग्रन्थ में राधा को कृष्ण की सहचरी होने के साथ-साथ सीता, पार्वती अथवा लक्ष्मी की तरह एक पूजनीया नारी के रूप में ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कृष्ण में इस ग्रन्थ में राधा को साध्वी संबोधन प्रदान करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि तुम श्री हो, तुम्हारे बिना मैं केवल कृष्ण होता हूं और जब तुम मुझसे संयुक्त हो जाती हो तो मैं श्रीकृष्ण बन जाता हूं।
आगच्छ शयने साध्वि कुरू वक्षः स्थलेहिमाम्।
स्वयं मे शोभास्वरूपाऽसि देहस्य भूषणं यथा।
कृष्ण वदन्ति मां लोकस्तवयैव रहितं यदा।
श्रीकृष्ण च तदा तेऽपित्वयैव सहितं परम्।
-ब्रह्मवैवर्त पुराणम् पंचदशो अध्यायः
स्वयं मे शोभास्वरूपाऽसि देहस्य भूषणं यथा।
कृष्ण वदन्ति मां लोकस्तवयैव रहितं यदा।
श्रीकृष्ण च तदा तेऽपित्वयैव सहितं परम्।
-ब्रह्मवैवर्त पुराणम् पंचदशो अध्यायः
स्पष्टतः राधा या तो एक काल्पनिक चरित्र है अथवा श्रीकृष्ण की एक ऐसी
सहचरी जो न तो उनकी परकीया थी न उनकी तथा कथित अविवाहिता प्रेमिका अथवा
प्रेयसी। कई पुराणों ने तो विशेषकर ब्रह्मवैवर्त पुराण ने राधा-कृष्ण के
विधिवत विवाह का भी वर्णन किया है और इसके अनुसार यह विवाह और किसी ने
नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा ने भांडीर वन में कराया है।
उपर्युक्त स्थिति में राधा की परकीया होने की बात तो पूर्णतया काल्पनिक और कामलोलुप कवियों की मनगढ़ंत कहानी से अधिक नहीं लगती।
एक उपन्यासकार इतिहासकार नहीं होता, न वह होता है कोई पुराणकार। पुराणों अथवा इतिहासों के अथाह सागर से चन्द मोतियों का अल्प सहारा ले उन्हें चमकदार बनाकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देना उसका कर्तव्य होता है उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। न तो वह इतिहास पुराण विशेषकर इतिहास को पूरी तरह नकार सकता है न अपनी कल्पना के पंखों को ही बेदर्दी से कुतरकर केवल तथ्यों को पाठकों के सामने परोस सकता है।
मैं इस भूमिका को अधिक लम्बा खींचना नहीं चाहता। किन्तु कुछ बातों को स्पष्ट कर देना आवश्यक था, अतः इतना दीर्घ पूर्व-कथन करना पड़ा। उपन्यासकार के रूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक में मैंने श्रीकृष्ण के जीवन के सभी पक्षों को पूरी ईमानदारी के साथ उद्घाटित करने का प्रयास किया है और मेरा लक्ष्य यह रहा है कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को इस ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय कि वह रोचक और विश्वसनीय होने के साथ-साथ प्रासंगिक भी हो।
पुस्तक की अथवा कृष्ण के जीवन की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता उपन्यास में स्वयं ही स्थान-स्थान पर प्रकट हुई है, अतः उस पर प्रकाश डालना मैं आवश्यक नहीं समझता।
जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया पुस्तक के दो खंडों में समाप्त हुई। पहले का नाम ‘प्रथम पुरुष’ और दूसरे का नाम ‘पुरुषोत्तम’ रखा गया। पर दोनों खंड़ अपने में पूर्ण हैं, अतः उन्हें दो पृथक-पृथक खण्डों में नहीं प्रस्तुत कर दो स्वतन्त्र पुस्तकों के रूप में ही प्रकाशित किया जा रहा है। ‘प्रथम पुरुष’ कंस-बध के साथ समाप्त होता है जो श्रीकृष्ण के जीवन की प्रथम सर्वोपरि उपलब्धि है।
‘पुरुषोत्तम’ में श्रीकृष्ण के शेष जीवन का वर्णन है और यह शेष जीवन उनकी मृत्यु-पर्यन्त विस्तृत है।
पुस्तक प्रणयन में शीघ्रता लाने हेतु जिन कुछेक शुभेच्छुओं की प्रेरणा रही है उनमें श्री कुणाल कुमार, श्री देवेन्द्र चौधरी, शिवनारायण एवं साहित्यमर्मज्ञ डा. माहेश्वरीसिंह ‘महेश’ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा यदि मेरा प्रयास युग-पुरुष श्रीकृष्ण को सही सन्दर्भ में प्रस्तुत करने में सफल हो पाता है।
उपर्युक्त स्थिति में राधा की परकीया होने की बात तो पूर्णतया काल्पनिक और कामलोलुप कवियों की मनगढ़ंत कहानी से अधिक नहीं लगती।
एक उपन्यासकार इतिहासकार नहीं होता, न वह होता है कोई पुराणकार। पुराणों अथवा इतिहासों के अथाह सागर से चन्द मोतियों का अल्प सहारा ले उन्हें चमकदार बनाकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देना उसका कर्तव्य होता है उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। न तो वह इतिहास पुराण विशेषकर इतिहास को पूरी तरह नकार सकता है न अपनी कल्पना के पंखों को ही बेदर्दी से कुतरकर केवल तथ्यों को पाठकों के सामने परोस सकता है।
मैं इस भूमिका को अधिक लम्बा खींचना नहीं चाहता। किन्तु कुछ बातों को स्पष्ट कर देना आवश्यक था, अतः इतना दीर्घ पूर्व-कथन करना पड़ा। उपन्यासकार के रूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक में मैंने श्रीकृष्ण के जीवन के सभी पक्षों को पूरी ईमानदारी के साथ उद्घाटित करने का प्रयास किया है और मेरा लक्ष्य यह रहा है कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को इस ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय कि वह रोचक और विश्वसनीय होने के साथ-साथ प्रासंगिक भी हो।
पुस्तक की अथवा कृष्ण के जीवन की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता उपन्यास में स्वयं ही स्थान-स्थान पर प्रकट हुई है, अतः उस पर प्रकाश डालना मैं आवश्यक नहीं समझता।
जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया पुस्तक के दो खंडों में समाप्त हुई। पहले का नाम ‘प्रथम पुरुष’ और दूसरे का नाम ‘पुरुषोत्तम’ रखा गया। पर दोनों खंड़ अपने में पूर्ण हैं, अतः उन्हें दो पृथक-पृथक खण्डों में नहीं प्रस्तुत कर दो स्वतन्त्र पुस्तकों के रूप में ही प्रकाशित किया जा रहा है। ‘प्रथम पुरुष’ कंस-बध के साथ समाप्त होता है जो श्रीकृष्ण के जीवन की प्रथम सर्वोपरि उपलब्धि है।
‘पुरुषोत्तम’ में श्रीकृष्ण के शेष जीवन का वर्णन है और यह शेष जीवन उनकी मृत्यु-पर्यन्त विस्तृत है।
पुस्तक प्रणयन में शीघ्रता लाने हेतु जिन कुछेक शुभेच्छुओं की प्रेरणा रही है उनमें श्री कुणाल कुमार, श्री देवेन्द्र चौधरी, शिवनारायण एवं साहित्यमर्मज्ञ डा. माहेश्वरीसिंह ‘महेश’ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा यदि मेरा प्रयास युग-पुरुष श्रीकृष्ण को सही सन्दर्भ में प्रस्तुत करने में सफल हो पाता है।
ऑफिसर फ्लैट
बेली रोड पटना,15
बेली रोड पटना,15
डॉ. भगवतीशरण मिश्र
पुरुषोत्तम
कंस-बंध से जहां सम्पूर्ण मथुरा नगरी उल्लसित थी और घर-घर में नित्य
दीपावली मनाई जा रही थी, देव-पूजन हो रहा था, मिष्टान्न बंट रहे थे, वहीं
इसी नगरी के राजमहल के एक कक्ष में दो ऐसी मानव-मूर्तियां भी थी जिनके
दुःख का कोई ओर-छोर नहीं था। भ्राद्रपद की अन्धकारपूर्ण रात्रि की तरह
उनका भविष्य भयावह और अन्धकारपूर्ण था। उनके जीवन में आशा की एक क्षीण लौ
भी नहीं जलने वाली थी और उनका शेष जीवन, वैधव्य, नैराश्य, दुर्भाग्य
पश्चात्ताप, पीड़ा और अन्धकार का वीभत्स सम्मिश्रण बना उनके समक्ष किसी
अछोर मरुकान्तार अथवा कंटक-कुश एवं हिंस्र वन्य जीवों से पूर्ण किसी
विस्तृत कानन की तरह फैला पड़ा था।
ये दो औरतें थीं-अस्ति और प्राप्ति। प्रतापी मगध-नरेश जरासंध की ये लावण्यवती पुत्रियां कंस से ब्याही गई थीं। उस समय शायद मगध नरेश को भी यह पता नहीं होगा कि कंस एक घोर अहंकारी व्यक्ति के रूप में विकसित होगा और उसका अहम एक दिन इस तरह आसमान छूने लगेगा कि वह उसके प्राणों के लिए ही संकट बन आयेगा और उसकी प्राण-प्रिय पुत्रियां उसके महल में अपनी सीमन्त-रेखा (मांग) को भले ही सिंदूर-चर्चित कर रही हैं किन्तु शीघ्र ही वे मथुरा से अपने पति की चिता की राख ही अपनी मुट्ठिइयों में भरकर लौटेंगी।
अस्ति और प्राप्ति की, इस विशाल महल में कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी।
ऐसा नहीं कि उन्होंने कंस को उसकी मनमानी से रोकना नहीं चाहा था या उसे अपार अहंकार पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया था, पर दोनों का या उसके अपार अहंकार पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया था, पर दोनों का सम्मिलित प्रयास भी अरण्यरोदन से कुछ अधिक नहीं सिद्ध हुआ था। आहुति पड़ी अग्नि की तरह उसके अत्याचार और अनाचार नित्य बढ़ते ही गए थे और उसने दोनों बहनों की बातों को कोई महत्त्व नहीं दिया अपितु कई बार तो उसने यहां तक कह दिया था कि वह जानता कि महाप्रतापी मगध-नरेश जरासंध की पुत्रियां ऐसी कायरता-ग्रस्त और भीरू होंगी तो वह भूलकर भी उन्हें अपने महल में स्थान नहीं देता।
पर अब तो अस्ति और प्राप्ति के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न था। सिंहासन पर महाराज उग्रसेन विराजमान हो गए थे, बलराम और श्रीकृष्ण उनके और उनके राज्य की सुरक्षा में तत्पर थे। नगर में नित्य और समारोह आयोजित हो रहे थे। लोग यह भी भूल गए थे कि आखिर मथुरा के एक गलत या सही राजा की मृत्यु हुई है, उसके लिए सप्ताह भर का औपचारिक शोक तो राज्य भर में मनाना ही चाहिए था। पर कौन शोक करने बैठा था कंस के नाम पर ? किसी तरह उसकी अन्तिम क्रिया कर दी गई थी। न राजकीय सम्मान, न कुछ विशेष औपचारिकता। जैसा किसी सामान्य शव को अग्नि की लपटों के हवाले कर दिया जाता है, उसी तरह कालिन्दी-कूल की एक चिता पर चढ़ा दिया गया था कंस के कुचले-मसले शव को। आखिर कृष्ण के साथ उस क्षणिक ही सही, मल्ययुद्ध और फिर मंच से नीचे उछाले जाने में उसकी देह की दुर्दशा तो हो ही गई थी।
बारह दिनों का अशौच का काल भी अस्ति-प्राप्ति के लिए ही था। राजभवन और नगर के कार्य यथावत् अपितु अब कुछ अधिक ही उत्साह और उमंग से सम्पन्न होते रहे थे। केवल दोनों बहनों के इर्द-गिर्द एक संत्रासक सन्नाटा लगातार बुनता रहा था उन दिनों। इस सन्नाटे को चीरे भी, ऐसा कोई नहीं था। दास-दासियां जो कंस के जीवित रहते हाथ बांधे डोलते रहते थे, उनमें से अब कभी-कभी ही कोई दिखाई पड़ जाता था। पिंड-दान आदि की औपचारिकता पूरी हो गई तो अस्ति प्राप्त को वहां रहना अब सर्वथा अनावश्यक व्यर्थ और त्रासद प्रतीत होने लगा।
उन्होंने महाराज उग्रसेन के यहाँ संवाद भिजवाया कि वे कुछ निवेदन करना चाहती हैं। कुछ वातावरण ही ऐसा रहा मथुरा का इन दिनों कि महाराज उग्रसेन भी प्रायः भूल ही बैठे थे कि पुत्र न रहा तो न रहा, दो पुत्र-बधुएं तो महल में हैं और उनकी सुधि भी लेनी है। उनका संवाद आते ही उन्हें अपने प्रमाद की ओर ध्यान गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि श्रीकृष्ण को ही भेजकर उनका मन्तव्य ज्ञात कर लें पर फिर उन्हें लगा कि ऐसा करना महान मूर्खता के सिवा और कुछ न होगा। श्रीकृष्ण ही तो उनके वैधव्य के कारण थे, उनके जीवन क्षितिज पर जो कभी नहीं निःशेष होने वाली तमिस्रा व्याप्त हो गई थी उसके एकमात्र जनक तो श्रीकृष्ण ही थे ! उनको सामने पाकर उनकी पुत्र बधुएं अपने में रह पायेंगी क्या ? उनके माध्यम से संवाद क्या जायेगा, कुछ ऐसा भी घट सकता है जो अप्रिय और अवांछित हो।
अन्ततः महाराज ने स्वयं अन्तःपुर में जाने का निर्णय लिया। पुत्र जैसा भी रहा हो, पुत्र बधुएं तो अपनी बेटियों की तरह थीं। भय यही था कि उनके आंसुओं का सामना वे कैसे कर पायेंगे ? वैधव्य नारी जीवन का महान अभिशाप है-सबसे भयावह दुःश्वप्न एक ऐसी काल रात्रि जिसका अन्त ही नहीं था, जिसमें प्रातः अथवा प्रत्यूष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वैधव्य-ग्रस्त जीवन के क्षितिज पर प्रसन्नता और उल्लास की लालिमा को कभी भूलकर भी छिटकना नहीं था। जिस नारी का सौभाग्य-सूर्य सदा के लिए अस्ताचलगामी हो जाय, उसके जीवन में किधर से एक प्रकाश-किरण को भी प्रवेश पाना था ?
महाराज उग्रसेन घबराए। अपने महल की ओर चल तो दिए पर पैर साथ नहीं दे रहे थे। वृद्धावस्था तो अभी वैसी नहीं उतरी थी पर वर्षों के कारावास ने तन और मन दोनों को जर्जर अवश्य कर दिया था। कुछ समय लगता उन्हें संतुलित और स्वस्थ होने में पर तब तक पुत्रबधुओं की पुकार को अनसुनी तो नहीं किया जा सकता था ?
दासियों ने अवसन्न पड़ी बहनों को महाराज के आगमन की सूचना दी। उन्हें अपने कानों पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। जिनके पति ने इस निर्दोष प्रजापालक को सिंहासन-च्युत कर कारागार का नारकीय जीवन भोगने को बाध्य किया था उनकी पुकार पर वे स्वयं उनसे मिलने आ जाएंगे, यह बात उनकी कल्पना के बाहर थी। वे दौड़ी थीं जैसी थीं वैसी ही उनके चरण स्पर्श को किन्तु श्वसुर को देखते ही कुछ उनके प्रेम-प्रदर्शन और कुछ अपने जीवन की व्यर्थता के बोध ने उन्हें उनकी आंखों को जल पूरित कर दिया और महाराज उग्रसेन के पैर जैसे तप्त जल बूंदों से ही पखार दिए गए।
नहीं रोक सके महाराज अपने को भी और जैसे पयोधर किसी पर्वत का स्पर्श पाते ही रीता होने लगता है वैसे ही उनकी आंखें भी बस पड़ीं। आंखें ही नहीं बरस पडीं, हृदय भी विगलित हो गया और उन्हें जैसे पहले-पहले एक कठोर, हृदयहीन यथार्थ से आमना-सामना हुआ। पुत्र-शोक की प्रतीति प्रथम- प्रथम ही हुई और राज्य और उससे जुड़े मान-सम्मान की निस्सारता का बोध भी प्रथम-प्रथम बार ही हुआ। क्या होता अगर वे कुछ दिन और कारागार में ही बन्द रहते ? क्या होता यदि सिंहासन पर उनकी मृत्यु-पर्यन्त कंस ही विराजमान रहता, अन्ततः था तो वह उनका पुत्र ही वे तो राज्य सुख भोग ही चुके थे। कंटक-निर्मित किरीट से अधिक क्या होता है राज-मुकुट ? समस्याओं और संकटों से नित्य निपटने को विवश होने की अपेक्षा तो कारागार का वह जीवन ही अधिक शान्तिप्रद और कहें तो सुखद और निरापद था। तब कम-से-कम ऐसी स्थिति का सामाना करने के लिए तो उन्हें नहीं विवश होना पड़ता।
देर तक पुत्रबधुएं पैरों पर निष्प्राण सी पड़ी रहीं तो महाराज उग्रसेन किसी तरह अपना खोया हुआ स्वर पा सके। अब तक वे पैरों को स्नात करते, चार चार- नेत्रों से निस्मृत जल से इस तरह अन्दर-ही-अन्दर उद्वेलित और अस्थिर हो आए थे कि स्वयं उनकी आंखों से भी अश्रुपात आरम्भ हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ भी बोलना कठिन था।
‘‘जो हो चुका उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर है। नियति का विधान मान उसे शिरोधार्य करने में ही बुद्धिमत्ता है।’’ उन्होंने पुत्रवधुओं को संबोधित किया था। ‘‘क्या समझती हो तुम, मैं सुखी हूं ? तुम्हारी पीड़ा से मेरी पीड़ा कुछ अधिक ही है। पुत्र, कुपुत्र ही सही पर होता है अपना अंश ही। व्यक्ति उसी में अपनी पूर्णता देखता है। पुत्र शोक से बड़ा इस लोक में कोई शोक नहीं होता, इस तथ्य को तुम नहीं जान सकती।
महाराज उग्रसेन इस समय सचमुच घोर पीड़ा से ग्रस्त थे। घोर उपेक्षा और अपमान के काल उन्होंने भले ही कंस की समाप्ति में अपनी सहमति दे दी हो पर अब उनके पश्चात्ताप के सागर का कोई अन्त नहीं था।
‘‘पुत्र-शोक की बात कह रहे हैं महाराज।’’ अन्ततः बड़ी बहन अस्ति ने ही अपना सिर उठाया था। अब शर्म और संकोच कैसा ? नियति के एक क्रूर झटके ने ही जिसका सब कुछ समाप्त कर दिया था, उसके लिए कहां का संकोच और कैसी शर्म ? आंचल सिर से सरक चुका था जिसे व्यवस्थित करने का भी उसने कोई प्रयास नहीं किया। चन्द्रमुख को काले भयावह मेघ-शावकों की तरह घेरे अव्यवस्थिति केश और सिन्दूर रहित सीमान्त तथा रोते-रोते सूज आई बड़ी-बड़ी अश्रुपूरित आंखों ने उग्रसेन को अब वास्तविकता से पूरी तरह परिचित करा दिया था। प्राप्ति यद्यपि सिर झुकाए ही बैठी रही पर उसकी स्थिति का अनुमान भी उग्रसेन सहज ही कर सकते थे।
उग्रसेन का अन्तर पूरी तरह द्रवित हो गया। कंस का दोष था, होगा, पर इन दो निरीह नारियों का क्या अपराध था ? इन्होंने तो जैसा उन्होंने सुन रखा था, अपने पति को सुमार्ग पर ही लाने का सतत प्रयास किया। पर अब तो उनका संसार पूरी तरह स्वाहा हो गया। जिसका श्वसुर जीवित हो उसे वैधव्य का वरण करना पडे़ यह कैसी बड़ी विडम्बना थी ? उग्रसेन सोचते जा रहे थे। इसी मध्य किसी ने उनके बैठने के लिए एक रजत-जटित मंचक रख दिया था। प्रांगण मध्य ही वे उसे मंचक पर बैठ गए थे। अधिक देर वे खड़ा भी तो नहीं रह सकते थे। कारा-जीवन ने उन्हें दुर्बल तो कर ही दिया था। अस्ति और प्राप्ति नीचे ही बैठी रहीं। उनकी आंखों से अक्षुपात जारी था, यह बात महाराज उग्रसेन से छिपी नहीं रह सकी। अस्ति तो पर्दा-विहीन हो ही गई थी, अतः उसकी स्थिति वे सहज ही अवलोकित कर रहे थे, प्राप्ति की सिसकियां और उसका गीला मुखावरण उसकी करुणा पूर्ण स्थिति का अभिज्ञान करा रहे थे।
ये दो औरतें थीं-अस्ति और प्राप्ति। प्रतापी मगध-नरेश जरासंध की ये लावण्यवती पुत्रियां कंस से ब्याही गई थीं। उस समय शायद मगध नरेश को भी यह पता नहीं होगा कि कंस एक घोर अहंकारी व्यक्ति के रूप में विकसित होगा और उसका अहम एक दिन इस तरह आसमान छूने लगेगा कि वह उसके प्राणों के लिए ही संकट बन आयेगा और उसकी प्राण-प्रिय पुत्रियां उसके महल में अपनी सीमन्त-रेखा (मांग) को भले ही सिंदूर-चर्चित कर रही हैं किन्तु शीघ्र ही वे मथुरा से अपने पति की चिता की राख ही अपनी मुट्ठिइयों में भरकर लौटेंगी।
अस्ति और प्राप्ति की, इस विशाल महल में कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी।
ऐसा नहीं कि उन्होंने कंस को उसकी मनमानी से रोकना नहीं चाहा था या उसे अपार अहंकार पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया था, पर दोनों का या उसके अपार अहंकार पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया था, पर दोनों का सम्मिलित प्रयास भी अरण्यरोदन से कुछ अधिक नहीं सिद्ध हुआ था। आहुति पड़ी अग्नि की तरह उसके अत्याचार और अनाचार नित्य बढ़ते ही गए थे और उसने दोनों बहनों की बातों को कोई महत्त्व नहीं दिया अपितु कई बार तो उसने यहां तक कह दिया था कि वह जानता कि महाप्रतापी मगध-नरेश जरासंध की पुत्रियां ऐसी कायरता-ग्रस्त और भीरू होंगी तो वह भूलकर भी उन्हें अपने महल में स्थान नहीं देता।
पर अब तो अस्ति और प्राप्ति के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न था। सिंहासन पर महाराज उग्रसेन विराजमान हो गए थे, बलराम और श्रीकृष्ण उनके और उनके राज्य की सुरक्षा में तत्पर थे। नगर में नित्य और समारोह आयोजित हो रहे थे। लोग यह भी भूल गए थे कि आखिर मथुरा के एक गलत या सही राजा की मृत्यु हुई है, उसके लिए सप्ताह भर का औपचारिक शोक तो राज्य भर में मनाना ही चाहिए था। पर कौन शोक करने बैठा था कंस के नाम पर ? किसी तरह उसकी अन्तिम क्रिया कर दी गई थी। न राजकीय सम्मान, न कुछ विशेष औपचारिकता। जैसा किसी सामान्य शव को अग्नि की लपटों के हवाले कर दिया जाता है, उसी तरह कालिन्दी-कूल की एक चिता पर चढ़ा दिया गया था कंस के कुचले-मसले शव को। आखिर कृष्ण के साथ उस क्षणिक ही सही, मल्ययुद्ध और फिर मंच से नीचे उछाले जाने में उसकी देह की दुर्दशा तो हो ही गई थी।
बारह दिनों का अशौच का काल भी अस्ति-प्राप्ति के लिए ही था। राजभवन और नगर के कार्य यथावत् अपितु अब कुछ अधिक ही उत्साह और उमंग से सम्पन्न होते रहे थे। केवल दोनों बहनों के इर्द-गिर्द एक संत्रासक सन्नाटा लगातार बुनता रहा था उन दिनों। इस सन्नाटे को चीरे भी, ऐसा कोई नहीं था। दास-दासियां जो कंस के जीवित रहते हाथ बांधे डोलते रहते थे, उनमें से अब कभी-कभी ही कोई दिखाई पड़ जाता था। पिंड-दान आदि की औपचारिकता पूरी हो गई तो अस्ति प्राप्त को वहां रहना अब सर्वथा अनावश्यक व्यर्थ और त्रासद प्रतीत होने लगा।
उन्होंने महाराज उग्रसेन के यहाँ संवाद भिजवाया कि वे कुछ निवेदन करना चाहती हैं। कुछ वातावरण ही ऐसा रहा मथुरा का इन दिनों कि महाराज उग्रसेन भी प्रायः भूल ही बैठे थे कि पुत्र न रहा तो न रहा, दो पुत्र-बधुएं तो महल में हैं और उनकी सुधि भी लेनी है। उनका संवाद आते ही उन्हें अपने प्रमाद की ओर ध्यान गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि श्रीकृष्ण को ही भेजकर उनका मन्तव्य ज्ञात कर लें पर फिर उन्हें लगा कि ऐसा करना महान मूर्खता के सिवा और कुछ न होगा। श्रीकृष्ण ही तो उनके वैधव्य के कारण थे, उनके जीवन क्षितिज पर जो कभी नहीं निःशेष होने वाली तमिस्रा व्याप्त हो गई थी उसके एकमात्र जनक तो श्रीकृष्ण ही थे ! उनको सामने पाकर उनकी पुत्र बधुएं अपने में रह पायेंगी क्या ? उनके माध्यम से संवाद क्या जायेगा, कुछ ऐसा भी घट सकता है जो अप्रिय और अवांछित हो।
अन्ततः महाराज ने स्वयं अन्तःपुर में जाने का निर्णय लिया। पुत्र जैसा भी रहा हो, पुत्र बधुएं तो अपनी बेटियों की तरह थीं। भय यही था कि उनके आंसुओं का सामना वे कैसे कर पायेंगे ? वैधव्य नारी जीवन का महान अभिशाप है-सबसे भयावह दुःश्वप्न एक ऐसी काल रात्रि जिसका अन्त ही नहीं था, जिसमें प्रातः अथवा प्रत्यूष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वैधव्य-ग्रस्त जीवन के क्षितिज पर प्रसन्नता और उल्लास की लालिमा को कभी भूलकर भी छिटकना नहीं था। जिस नारी का सौभाग्य-सूर्य सदा के लिए अस्ताचलगामी हो जाय, उसके जीवन में किधर से एक प्रकाश-किरण को भी प्रवेश पाना था ?
महाराज उग्रसेन घबराए। अपने महल की ओर चल तो दिए पर पैर साथ नहीं दे रहे थे। वृद्धावस्था तो अभी वैसी नहीं उतरी थी पर वर्षों के कारावास ने तन और मन दोनों को जर्जर अवश्य कर दिया था। कुछ समय लगता उन्हें संतुलित और स्वस्थ होने में पर तब तक पुत्रबधुओं की पुकार को अनसुनी तो नहीं किया जा सकता था ?
दासियों ने अवसन्न पड़ी बहनों को महाराज के आगमन की सूचना दी। उन्हें अपने कानों पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। जिनके पति ने इस निर्दोष प्रजापालक को सिंहासन-च्युत कर कारागार का नारकीय जीवन भोगने को बाध्य किया था उनकी पुकार पर वे स्वयं उनसे मिलने आ जाएंगे, यह बात उनकी कल्पना के बाहर थी। वे दौड़ी थीं जैसी थीं वैसी ही उनके चरण स्पर्श को किन्तु श्वसुर को देखते ही कुछ उनके प्रेम-प्रदर्शन और कुछ अपने जीवन की व्यर्थता के बोध ने उन्हें उनकी आंखों को जल पूरित कर दिया और महाराज उग्रसेन के पैर जैसे तप्त जल बूंदों से ही पखार दिए गए।
नहीं रोक सके महाराज अपने को भी और जैसे पयोधर किसी पर्वत का स्पर्श पाते ही रीता होने लगता है वैसे ही उनकी आंखें भी बस पड़ीं। आंखें ही नहीं बरस पडीं, हृदय भी विगलित हो गया और उन्हें जैसे पहले-पहले एक कठोर, हृदयहीन यथार्थ से आमना-सामना हुआ। पुत्र-शोक की प्रतीति प्रथम- प्रथम ही हुई और राज्य और उससे जुड़े मान-सम्मान की निस्सारता का बोध भी प्रथम-प्रथम बार ही हुआ। क्या होता अगर वे कुछ दिन और कारागार में ही बन्द रहते ? क्या होता यदि सिंहासन पर उनकी मृत्यु-पर्यन्त कंस ही विराजमान रहता, अन्ततः था तो वह उनका पुत्र ही वे तो राज्य सुख भोग ही चुके थे। कंटक-निर्मित किरीट से अधिक क्या होता है राज-मुकुट ? समस्याओं और संकटों से नित्य निपटने को विवश होने की अपेक्षा तो कारागार का वह जीवन ही अधिक शान्तिप्रद और कहें तो सुखद और निरापद था। तब कम-से-कम ऐसी स्थिति का सामाना करने के लिए तो उन्हें नहीं विवश होना पड़ता।
देर तक पुत्रबधुएं पैरों पर निष्प्राण सी पड़ी रहीं तो महाराज उग्रसेन किसी तरह अपना खोया हुआ स्वर पा सके। अब तक वे पैरों को स्नात करते, चार चार- नेत्रों से निस्मृत जल से इस तरह अन्दर-ही-अन्दर उद्वेलित और अस्थिर हो आए थे कि स्वयं उनकी आंखों से भी अश्रुपात आरम्भ हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ भी बोलना कठिन था।
‘‘जो हो चुका उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर है। नियति का विधान मान उसे शिरोधार्य करने में ही बुद्धिमत्ता है।’’ उन्होंने पुत्रवधुओं को संबोधित किया था। ‘‘क्या समझती हो तुम, मैं सुखी हूं ? तुम्हारी पीड़ा से मेरी पीड़ा कुछ अधिक ही है। पुत्र, कुपुत्र ही सही पर होता है अपना अंश ही। व्यक्ति उसी में अपनी पूर्णता देखता है। पुत्र शोक से बड़ा इस लोक में कोई शोक नहीं होता, इस तथ्य को तुम नहीं जान सकती।
महाराज उग्रसेन इस समय सचमुच घोर पीड़ा से ग्रस्त थे। घोर उपेक्षा और अपमान के काल उन्होंने भले ही कंस की समाप्ति में अपनी सहमति दे दी हो पर अब उनके पश्चात्ताप के सागर का कोई अन्त नहीं था।
‘‘पुत्र-शोक की बात कह रहे हैं महाराज।’’ अन्ततः बड़ी बहन अस्ति ने ही अपना सिर उठाया था। अब शर्म और संकोच कैसा ? नियति के एक क्रूर झटके ने ही जिसका सब कुछ समाप्त कर दिया था, उसके लिए कहां का संकोच और कैसी शर्म ? आंचल सिर से सरक चुका था जिसे व्यवस्थित करने का भी उसने कोई प्रयास नहीं किया। चन्द्रमुख को काले भयावह मेघ-शावकों की तरह घेरे अव्यवस्थिति केश और सिन्दूर रहित सीमान्त तथा रोते-रोते सूज आई बड़ी-बड़ी अश्रुपूरित आंखों ने उग्रसेन को अब वास्तविकता से पूरी तरह परिचित करा दिया था। प्राप्ति यद्यपि सिर झुकाए ही बैठी रही पर उसकी स्थिति का अनुमान भी उग्रसेन सहज ही कर सकते थे।
उग्रसेन का अन्तर पूरी तरह द्रवित हो गया। कंस का दोष था, होगा, पर इन दो निरीह नारियों का क्या अपराध था ? इन्होंने तो जैसा उन्होंने सुन रखा था, अपने पति को सुमार्ग पर ही लाने का सतत प्रयास किया। पर अब तो उनका संसार पूरी तरह स्वाहा हो गया। जिसका श्वसुर जीवित हो उसे वैधव्य का वरण करना पडे़ यह कैसी बड़ी विडम्बना थी ? उग्रसेन सोचते जा रहे थे। इसी मध्य किसी ने उनके बैठने के लिए एक रजत-जटित मंचक रख दिया था। प्रांगण मध्य ही वे उसे मंचक पर बैठ गए थे। अधिक देर वे खड़ा भी तो नहीं रह सकते थे। कारा-जीवन ने उन्हें दुर्बल तो कर ही दिया था। अस्ति और प्राप्ति नीचे ही बैठी रहीं। उनकी आंखों से अक्षुपात जारी था, यह बात महाराज उग्रसेन से छिपी नहीं रह सकी। अस्ति तो पर्दा-विहीन हो ही गई थी, अतः उसकी स्थिति वे सहज ही अवलोकित कर रहे थे, प्राप्ति की सिसकियां और उसका गीला मुखावरण उसकी करुणा पूर्ण स्थिति का अभिज्ञान करा रहे थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book