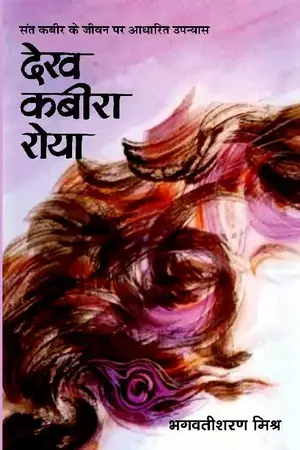|
जीवन कथाएँ >> देख कबीरा रोया देख कबीरा रोयाभगवतीशरण मिश्र
|
413 पाठक हैं |
|||||||
संत कबीर के जीवन पर एक प्रमाणिक एवं पठनीय उपन्यास....
Dekha Kabira Roya Bhagvati sharan Mishr
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तावना
कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर एक औपन्यासिक कृति प्रस्तुत करना बहुत आसान नहीं है।
इस प्रयास में मैं गत चार वर्षों से लगा रहा। 1992 में आरंभ हुई यह कृति, 1996 के अंत में पूर्ण हुई।
बीच में और उपन्यास आते रहे पर कबीर पर कार्य जारी रहा। उनसे संबंधित स्थानों के भ्रमण के अलावा उनके और उनके जीवन से संबंधित साहित्य के अध्ययन का क्रम चलता रहा।
काशी के कबीर-चौरे पर परामर्श विमर्श से प्रसन्नता हुई तो वहीं के लहर-तालाब (शिशु-कबीर का प्राप्ति स्थान) की दु:स्थिति को देखकर रुलाई भी आई। संगमरमर की चंद चट्टानें खड़ी कर देने और उन पर सरोवर निरंतर अतिक्रमण का आखेट होता जा रहा है। अनेक मठों में चलती मनमानी और अनेक मठाधीशों के कबीर-साहित्य संबंधी अज्ञान और दुराग्रह ने मन को मरोड़ा।
पंथ की विभिन्न शाखाओं-प्रशाखाओं के मध्य मूल-वृक्ष का अन्वेषण ही कठिन हो गया।
कबीर के जीवन को लेकर प्रामाणिक सूचनाओं के अभाव में आज से प्राय: साढ़े पांच सौ वर्ष पूर्व उत्पन्न संत कवि के जीवन को लेकर कथा बुनना एक चुनौती भरा कार्य था जिसे मैंने दायित्वपूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास किया है।
उनके साहित्य को लेकर डॉ.हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉ.रामकुमार वर्मा के अलावा दर्जनों शोधकर्ताओं की कृतियां उपलब्ध हैं पर उनके जीवन-पक्ष पर सामग्री प्रस्तुत करने का साहस किसी ने नहीं किया। किसी ने कुछ किया भी तो वह कई कबीर-पंथियों के कोप का शिकार भी बना। डॉ.रामकुमार वर्मा ने उनके जीवन के रहस्यों पर से कुछ पर्दा उठाने का प्रयास किया तो कुछ मठाधीशों द्वारा भरपूर गालियां खाईं।
कबीर के वैवाहिक जीवन को लेकर विशेष विवाद रहा। कुछ मान्य लेखक उन्हें विवाहित मानते हैं तो कुछ उनके साथ दो पत्नियों का भी नाम जोड़ते हैं-लोई और धनिया का।
कट्टर कबीरपंथी उन्हें बालब्रह्मचारी मानते हैं और वैवाहिक होने की बात को पंथ के लिए अपमानजनक समझते हैं। इसकी कोई तुक समझ में नहीं आती। विवाहित होने से भक्ति किधर से प्रभावित होती है ? अनेक संत-सुधारक गृहस्थ रहे हैं कि नहीं ?
मैंने इस विवाद और धनिया-लोई प्रकरण को एक तार्किक एवं विश्वसनीय स्वरूप दिया है। लोई को मैंने कबीर की विधिवत् विवाहिता पत्नी माना है और धनिया को एक ऐसे चरित्र के रूप में उभारा है जिससे कबीर के व्यक्तित्व को उदात्तता ही प्राप्त होती है। इस रहस्य को अभी रहस्य ही रहने देता हूं। पुस्तक के परायण के दौरान वह स्वत: स्पष्ट होता जाएगा।
कबीर के जीवन पर कबीरपंथियों द्वारा रचित पुस्तकें सूचनापूर्ण तो हैं नहीं आद्यन्त अविश्वसनीय और असंख्य चमत्कारों से भरी हैं। ‘कबीर मंसूर’ नामक महाग्रंथ तो इसमें सर्वाधिक अग्रणी भूमिका निभाता है। बिना अंदर देखे उस पुस्तक को खरीदकर मैं अपव्यय का ही दोषी हुआ।
‘कबीर-चौरा’ काशी के मठाधीश गंगाशरण शास्त्री की जीवनीपरक पुस्तक कुछ हद तक प्रामाणिक प्रतीत होती है पर उसमें भी चमत्कारों की अधिकता ने उसे अविश्वनसीय बना दिया है।
अंग्रेजी की एक पुस्तक मिली पर उससे कुछ हाथ नहीं लगा।
चमत्कारों से मुझे चिढ़ नहीं है। मैं उनका साक्षी भी रहा हूँ। मेरी एक सत्य घटनाओं पर आधारित पुस्तक भी है, ‘बंधक आत्माएं।
किंतु चमत्कारों की भी, विशेषकर, व्यक्ति-विशेष के जीवन में एक सीमा होती है। अब किसी मरणधर्मा व्यक्ति के समक्ष साक्षात् विष्णु को ही करबद्ध खड़ा कर देना कैसा लग सकता है ? अथवा जो कबीर जीवन-भर अवतारों को नकारता रहा उसे शिव का ही अवतार घोषित कर देना कौन-सा न्याय है ?
कबीर के जीवन को मैंने नितांत चमत्कारहीन ही नहीं माना है। जब अघोरी और सामान्य तांत्रिक चमत्कार कर सकते हैं तो एक परम समर्पित राम-भक्त चमत्कारी नहीं होगा, यह कैसे कह सकते हैं ?
मेरे पास चमत्कार बहुत चौंकाने वाले नहीं है। वे स्थान और व्यक्ति के सर्वथा अनुकूल हैं और उनका अस्तित्व इस पु्स्तक में दाल में नमक से अधिक है। पाठक इन्हें पढ़कर नाक-भौं सिकोड़ने की स्थिति में नहीं आएंगे, यह मैंने सुनिश्चित किया है। साथ ही इन एक-दो चमत्कारों के आधार भी हैं। वे नितांत कल्पना-प्रसूत नहीं है।
कबीर एक संत के अलावा एक महान् समाज सुधारक भी थे। जिस सामाजिक न्याय की बात आज की जाती है उसका प्रबल पक्षधर आज से साढ़े पांच सौ वर्षों से अधिक पूर्व ही पैदा हो चुका था। समानता और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रथम शंखनाद कबीर ने ही किया था।
उनके व्यक्तित्व के इन अनूठे पक्ष के साथ भी पुस्तक में पूर्ण न्याय किया गया है।
कबीर के व्यक्तित्व का सबलतम पक्ष है उनका कवि-रूप। इस आशु कवि की चेरी थी कविता। अनुचर थे इसके शब्द और अलंकार। यद्यपि जान-बूझकर अलंकारों का प्रयोग इसने कभी नहीं किया।
आशु कवि के साथ-साथ आम आदमी के कवि थे कबीर। आश्चर्य है कि आज आधे हजार वर्ष के अधिक के उपरांत भी प्राय: हर पढ़ा लिखा अथवा नितांत निरक्षर भट्टाचार्य भी कबीर की एक-दो साखियों को अवश्य जानता है, भले ही उसे यह ज्ञात नहीं हो कि वे कबीर की ही उक्ति हैं क्योंकि सबमें कबीर का नाम नहीं आता। उदाहरण के लिए-‘निंदक नियरे राखिए..।’ और ‘ढाई आखर प्रेम...।’ की उक्तियों से आज भी कौन परिचित नहीं ?
कबीर की प्रतिभा के इस पक्ष को भी पूर्णतया उजागर करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है।
कबीर की ‘साखियों’, ‘रमैनियों’ आदि के रूप निरंतर परिवर्तित होते गए हैं। यहां विशुद्ध प्रामाणिकता की अपेक्षा व्यर्थ है। कबीर की रचनाओं पर उपलब्ध अनेक संग्रहों में से जो सामग्री अधिकतम ग्राह्य लगी है उसी का उपयोग इस औपन्यासिक कृति में किया गया है।
‘बीजक’ की प्रामाणिकता अभी तक संदिग्ध ही है, अत: उसकी तरफ मैं बहुत मुखातिब नहीं हुआ हूं।
कबीर की उलटवांसियों से कौन परिचित नहीं-
इस प्रयास में मैं गत चार वर्षों से लगा रहा। 1992 में आरंभ हुई यह कृति, 1996 के अंत में पूर्ण हुई।
बीच में और उपन्यास आते रहे पर कबीर पर कार्य जारी रहा। उनसे संबंधित स्थानों के भ्रमण के अलावा उनके और उनके जीवन से संबंधित साहित्य के अध्ययन का क्रम चलता रहा।
काशी के कबीर-चौरे पर परामर्श विमर्श से प्रसन्नता हुई तो वहीं के लहर-तालाब (शिशु-कबीर का प्राप्ति स्थान) की दु:स्थिति को देखकर रुलाई भी आई। संगमरमर की चंद चट्टानें खड़ी कर देने और उन पर सरोवर निरंतर अतिक्रमण का आखेट होता जा रहा है। अनेक मठों में चलती मनमानी और अनेक मठाधीशों के कबीर-साहित्य संबंधी अज्ञान और दुराग्रह ने मन को मरोड़ा।
पंथ की विभिन्न शाखाओं-प्रशाखाओं के मध्य मूल-वृक्ष का अन्वेषण ही कठिन हो गया।
कबीर के जीवन को लेकर प्रामाणिक सूचनाओं के अभाव में आज से प्राय: साढ़े पांच सौ वर्ष पूर्व उत्पन्न संत कवि के जीवन को लेकर कथा बुनना एक चुनौती भरा कार्य था जिसे मैंने दायित्वपूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास किया है।
उनके साहित्य को लेकर डॉ.हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉ.रामकुमार वर्मा के अलावा दर्जनों शोधकर्ताओं की कृतियां उपलब्ध हैं पर उनके जीवन-पक्ष पर सामग्री प्रस्तुत करने का साहस किसी ने नहीं किया। किसी ने कुछ किया भी तो वह कई कबीर-पंथियों के कोप का शिकार भी बना। डॉ.रामकुमार वर्मा ने उनके जीवन के रहस्यों पर से कुछ पर्दा उठाने का प्रयास किया तो कुछ मठाधीशों द्वारा भरपूर गालियां खाईं।
कबीर के वैवाहिक जीवन को लेकर विशेष विवाद रहा। कुछ मान्य लेखक उन्हें विवाहित मानते हैं तो कुछ उनके साथ दो पत्नियों का भी नाम जोड़ते हैं-लोई और धनिया का।
कट्टर कबीरपंथी उन्हें बालब्रह्मचारी मानते हैं और वैवाहिक होने की बात को पंथ के लिए अपमानजनक समझते हैं। इसकी कोई तुक समझ में नहीं आती। विवाहित होने से भक्ति किधर से प्रभावित होती है ? अनेक संत-सुधारक गृहस्थ रहे हैं कि नहीं ?
मैंने इस विवाद और धनिया-लोई प्रकरण को एक तार्किक एवं विश्वसनीय स्वरूप दिया है। लोई को मैंने कबीर की विधिवत् विवाहिता पत्नी माना है और धनिया को एक ऐसे चरित्र के रूप में उभारा है जिससे कबीर के व्यक्तित्व को उदात्तता ही प्राप्त होती है। इस रहस्य को अभी रहस्य ही रहने देता हूं। पुस्तक के परायण के दौरान वह स्वत: स्पष्ट होता जाएगा।
कबीर के जीवन पर कबीरपंथियों द्वारा रचित पुस्तकें सूचनापूर्ण तो हैं नहीं आद्यन्त अविश्वसनीय और असंख्य चमत्कारों से भरी हैं। ‘कबीर मंसूर’ नामक महाग्रंथ तो इसमें सर्वाधिक अग्रणी भूमिका निभाता है। बिना अंदर देखे उस पुस्तक को खरीदकर मैं अपव्यय का ही दोषी हुआ।
‘कबीर-चौरा’ काशी के मठाधीश गंगाशरण शास्त्री की जीवनीपरक पुस्तक कुछ हद तक प्रामाणिक प्रतीत होती है पर उसमें भी चमत्कारों की अधिकता ने उसे अविश्वनसीय बना दिया है।
अंग्रेजी की एक पुस्तक मिली पर उससे कुछ हाथ नहीं लगा।
चमत्कारों से मुझे चिढ़ नहीं है। मैं उनका साक्षी भी रहा हूँ। मेरी एक सत्य घटनाओं पर आधारित पुस्तक भी है, ‘बंधक आत्माएं।
किंतु चमत्कारों की भी, विशेषकर, व्यक्ति-विशेष के जीवन में एक सीमा होती है। अब किसी मरणधर्मा व्यक्ति के समक्ष साक्षात् विष्णु को ही करबद्ध खड़ा कर देना कैसा लग सकता है ? अथवा जो कबीर जीवन-भर अवतारों को नकारता रहा उसे शिव का ही अवतार घोषित कर देना कौन-सा न्याय है ?
कबीर के जीवन को मैंने नितांत चमत्कारहीन ही नहीं माना है। जब अघोरी और सामान्य तांत्रिक चमत्कार कर सकते हैं तो एक परम समर्पित राम-भक्त चमत्कारी नहीं होगा, यह कैसे कह सकते हैं ?
मेरे पास चमत्कार बहुत चौंकाने वाले नहीं है। वे स्थान और व्यक्ति के सर्वथा अनुकूल हैं और उनका अस्तित्व इस पु्स्तक में दाल में नमक से अधिक है। पाठक इन्हें पढ़कर नाक-भौं सिकोड़ने की स्थिति में नहीं आएंगे, यह मैंने सुनिश्चित किया है। साथ ही इन एक-दो चमत्कारों के आधार भी हैं। वे नितांत कल्पना-प्रसूत नहीं है।
कबीर एक संत के अलावा एक महान् समाज सुधारक भी थे। जिस सामाजिक न्याय की बात आज की जाती है उसका प्रबल पक्षधर आज से साढ़े पांच सौ वर्षों से अधिक पूर्व ही पैदा हो चुका था। समानता और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रथम शंखनाद कबीर ने ही किया था।
उनके व्यक्तित्व के इन अनूठे पक्ष के साथ भी पुस्तक में पूर्ण न्याय किया गया है।
कबीर के व्यक्तित्व का सबलतम पक्ष है उनका कवि-रूप। इस आशु कवि की चेरी थी कविता। अनुचर थे इसके शब्द और अलंकार। यद्यपि जान-बूझकर अलंकारों का प्रयोग इसने कभी नहीं किया।
आशु कवि के साथ-साथ आम आदमी के कवि थे कबीर। आश्चर्य है कि आज आधे हजार वर्ष के अधिक के उपरांत भी प्राय: हर पढ़ा लिखा अथवा नितांत निरक्षर भट्टाचार्य भी कबीर की एक-दो साखियों को अवश्य जानता है, भले ही उसे यह ज्ञात नहीं हो कि वे कबीर की ही उक्ति हैं क्योंकि सबमें कबीर का नाम नहीं आता। उदाहरण के लिए-‘निंदक नियरे राखिए..।’ और ‘ढाई आखर प्रेम...।’ की उक्तियों से आज भी कौन परिचित नहीं ?
कबीर की प्रतिभा के इस पक्ष को भी पूर्णतया उजागर करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है।
कबीर की ‘साखियों’, ‘रमैनियों’ आदि के रूप निरंतर परिवर्तित होते गए हैं। यहां विशुद्ध प्रामाणिकता की अपेक्षा व्यर्थ है। कबीर की रचनाओं पर उपलब्ध अनेक संग्रहों में से जो सामग्री अधिकतम ग्राह्य लगी है उसी का उपयोग इस औपन्यासिक कृति में किया गया है।
‘बीजक’ की प्रामाणिकता अभी तक संदिग्ध ही है, अत: उसकी तरफ मैं बहुत मुखातिब नहीं हुआ हूं।
कबीर की उलटवांसियों से कौन परिचित नहीं-
‘‘कबीरदास की उलटा बानी, बरसै कंबल भीजैं पानी’’-
यह सामान्य जन भी बोलता है। इन उलटवांसियों का भी कुछ स्वाद यहां मिलेगा।
पुस्तक में यत्र-तत्र श्रीमद्भागवदगीता के उद्धरण मिलेंगे। यों तो कुरान-शरीफ के भी मिलेंगे पर गीता पर अधिक बल मिलेगा। इसका कारण गीता के प्रति मेरी विशेष दुर्बलता नहीं अपितु गीता और कबीर दोनों की, मेरी कुछ ही सही, जानकारी को जानना चाहिए। गीता भक्ति-योग, ज्ञान-योग और कर्म-योग तीनों का आदर्श संगम प्रस्तुत करती है तो कबीर भी एक श्रेष्ठ भक्त, अप्रतिम कर्म-योगी और अद्भुत ज्ञानी हैं। अगर किसी तरह वे गीता के सिद्धांतों से परिचित हो आए हों और उन्हें अपने व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में उतार दिया हो तो मैं गीता के प्रति पक्षपात का दोषी नहीं कहा जा सकता।
संक्षेपत: यह कि कबीर क्या-क्या थे, क्या नहीं थे इसका पता इस औपन्यासिक कृति से बहुत सीमा तक अवश्य मिलेगा।
इस पुस्तक की भाषा के संबंध में अंतिका के रूप में ‘कबीर-उवाच’ में कबीर स्वयं बोलते हैं। इस संबंध में उन्हीं का कथन ग्राह्य होना चाहिए।
मेरी अनेक औपन्यासिक कृतियों का शिल्प-विधान अपना है। मेरे शिल्प को पूर्णतया खुल खेलने का सुअवसर तो कबीर प्रदान करने से रहे फिर भी उसकी बानगी यत्र-तत्र मिल ही जाएगी।
अंत में, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि यह एक औपन्यासिक कृति है, ऐतिहासिक नहीं। ऐतिहासिकता चाहे इसमें जितनी उपलब्ध हो पर इसे इतिहास-ग्रंथ की संज्ञा तो नहीं ही दे सकते। फिर भी कबीर के संबंध में जो कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिल सकता था, आधार-सामग्री के रूप में उसी का प्रयोग हुआ है। औपन्यासिक पुस्तक की प्रामाणिकता पर जितना विश्वास उचित है इससे कम का दावा मैं नहीं करता पर पुस्तक की सफलता निहित है इसकी प्रासंगिकता में। आज साढ़े पांच सहस्र वर्ष बाद भी कबीर कितना प्रासंगिक हो उठे हैं, यह इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात् ही ज्ञात होगा।
राजपाल एंड संस के स्वत्वाधिकारी श्री विश्वनाथजी कबीर के अत्यंत प्रेमी हैं। स्व.अमृतलाल नागर से भी उन्होंने कबीर पर उपन्यास लिखने का आग्रह किया था पर उनके काल-कवलित हो जाने के कारण यह योजना धरी रह गई। पुन: मुझसे उन्होंने इस संबंध में बार-बार आग्रह किया। कोई चार वर्षों बाद ही सही, मैं उनकी अभिलाषा की पूर्ति कर सका, इसका मुझे हर्ष है।
इस पुस्तक के लिए सामग्री संयोजन में मु. नसीम, राजभाषा विभाग, पटना का विशेष सहयोग रहा। इस मज़हब-प्रेमी और धर्म-भीरू व्यक्ति की तत्परता का मैं कायल हूं।
भागनेय ‘धनु’ मेरा सबसे अल्प-वय पाठक है। मेरी कृतियों में उसकी अभिरुचि प्रशंसनीय रही है। बहन गीता और उनके पति श्री श्रीनिवास पांडेय की आत्मीयता मेरे साहित्यिक प्रयासों में सदा सहायक रही है।
डॉ.शिवनारायण आशीर्वादार्ह हैं।
इसकी पांडुलिपि के टंकक श्री त्रिपुरारी प्रसाद की त्वरा और तत्परता ने इस पुस्तक को शीघ्र प्रकाश्य बनाया। उनका साधुवाद।
अन्य बहुत सारे मेरे शुभेच्छुओं, जिनमें भागनेय वैजनाथ भी सम्मिलित हैं, के प्रति मेरा आभार। विशेषत: अपने पाठक-वर्ग के प्रति जो निरंतर मेरी नई कृति की आतुर प्रतीक्षा करता है, कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे।
अंत में उस राम के प्रति अपार श्रद्धा-समर्पण, जिस पर जितना कबीर का दावा था उससे कुछ कम मैं अपना नहीं मानता।
अस्तु
विजया दशमी, 1996
पुस्तक में यत्र-तत्र श्रीमद्भागवदगीता के उद्धरण मिलेंगे। यों तो कुरान-शरीफ के भी मिलेंगे पर गीता पर अधिक बल मिलेगा। इसका कारण गीता के प्रति मेरी विशेष दुर्बलता नहीं अपितु गीता और कबीर दोनों की, मेरी कुछ ही सही, जानकारी को जानना चाहिए। गीता भक्ति-योग, ज्ञान-योग और कर्म-योग तीनों का आदर्श संगम प्रस्तुत करती है तो कबीर भी एक श्रेष्ठ भक्त, अप्रतिम कर्म-योगी और अद्भुत ज्ञानी हैं। अगर किसी तरह वे गीता के सिद्धांतों से परिचित हो आए हों और उन्हें अपने व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में उतार दिया हो तो मैं गीता के प्रति पक्षपात का दोषी नहीं कहा जा सकता।
संक्षेपत: यह कि कबीर क्या-क्या थे, क्या नहीं थे इसका पता इस औपन्यासिक कृति से बहुत सीमा तक अवश्य मिलेगा।
इस पुस्तक की भाषा के संबंध में अंतिका के रूप में ‘कबीर-उवाच’ में कबीर स्वयं बोलते हैं। इस संबंध में उन्हीं का कथन ग्राह्य होना चाहिए।
मेरी अनेक औपन्यासिक कृतियों का शिल्प-विधान अपना है। मेरे शिल्प को पूर्णतया खुल खेलने का सुअवसर तो कबीर प्रदान करने से रहे फिर भी उसकी बानगी यत्र-तत्र मिल ही जाएगी।
अंत में, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि यह एक औपन्यासिक कृति है, ऐतिहासिक नहीं। ऐतिहासिकता चाहे इसमें जितनी उपलब्ध हो पर इसे इतिहास-ग्रंथ की संज्ञा तो नहीं ही दे सकते। फिर भी कबीर के संबंध में जो कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिल सकता था, आधार-सामग्री के रूप में उसी का प्रयोग हुआ है। औपन्यासिक पुस्तक की प्रामाणिकता पर जितना विश्वास उचित है इससे कम का दावा मैं नहीं करता पर पुस्तक की सफलता निहित है इसकी प्रासंगिकता में। आज साढ़े पांच सहस्र वर्ष बाद भी कबीर कितना प्रासंगिक हो उठे हैं, यह इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात् ही ज्ञात होगा।
राजपाल एंड संस के स्वत्वाधिकारी श्री विश्वनाथजी कबीर के अत्यंत प्रेमी हैं। स्व.अमृतलाल नागर से भी उन्होंने कबीर पर उपन्यास लिखने का आग्रह किया था पर उनके काल-कवलित हो जाने के कारण यह योजना धरी रह गई। पुन: मुझसे उन्होंने इस संबंध में बार-बार आग्रह किया। कोई चार वर्षों बाद ही सही, मैं उनकी अभिलाषा की पूर्ति कर सका, इसका मुझे हर्ष है।
इस पुस्तक के लिए सामग्री संयोजन में मु. नसीम, राजभाषा विभाग, पटना का विशेष सहयोग रहा। इस मज़हब-प्रेमी और धर्म-भीरू व्यक्ति की तत्परता का मैं कायल हूं।
भागनेय ‘धनु’ मेरा सबसे अल्प-वय पाठक है। मेरी कृतियों में उसकी अभिरुचि प्रशंसनीय रही है। बहन गीता और उनके पति श्री श्रीनिवास पांडेय की आत्मीयता मेरे साहित्यिक प्रयासों में सदा सहायक रही है।
डॉ.शिवनारायण आशीर्वादार्ह हैं।
इसकी पांडुलिपि के टंकक श्री त्रिपुरारी प्रसाद की त्वरा और तत्परता ने इस पुस्तक को शीघ्र प्रकाश्य बनाया। उनका साधुवाद।
अन्य बहुत सारे मेरे शुभेच्छुओं, जिनमें भागनेय वैजनाथ भी सम्मिलित हैं, के प्रति मेरा आभार। विशेषत: अपने पाठक-वर्ग के प्रति जो निरंतर मेरी नई कृति की आतुर प्रतीक्षा करता है, कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे।
अंत में उस राम के प्रति अपार श्रद्धा-समर्पण, जिस पर जितना कबीर का दावा था उससे कुछ कम मैं अपना नहीं मानता।
अस्तु
विजया दशमी, 1996
भगवतीशरण मिश्र
1
मैं कबीर, जाति-पांति का पता नहीं, धर्म-संप्रदाय में आस्था नहीं, जिह्वा पर लगाम नहीं, सीधे को उलटा और उलटे को सीधा कहने का आदी, उलटवांसियों के लिए ख्यात-कुख्यात आज चला हूं लिखने अपनी आत्मकथा-अपनी राम-कहानी।
आप पूछिएगा यह आत्मकथा है कि प्रेतकथा-भूतगाथा ? आज से साढ़े पांच सौ वर्षों से भी पूर्व इस धरा-धाम को छोड़ गया यह आदमी आज अपनी आत्मकथा कैसे लिखने लगा ?
सच पूछिए तो मैंने कभी लिखा नहीं-अपने जीवन काल में भी। ‘मसि कागद छुओ नहीं,’ इस मेरी प्रसिद्ध उक्ति से आप भी अनभिज्ञ नहीं। जब पढ़ा ही नहीं तो लिखता क्या ? जो स्याही, कागज से भी दूर रहा वह क्या खाक पढ़ता व लिखता ? ऐसे भी पढ़ाई के प्रति मेरी धारणा से बच्चा-बच्चा परिचित है, भले ही उस उक्ति का बहुतों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया हो-
आप पूछिएगा यह आत्मकथा है कि प्रेतकथा-भूतगाथा ? आज से साढ़े पांच सौ वर्षों से भी पूर्व इस धरा-धाम को छोड़ गया यह आदमी आज अपनी आत्मकथा कैसे लिखने लगा ?
सच पूछिए तो मैंने कभी लिखा नहीं-अपने जीवन काल में भी। ‘मसि कागद छुओ नहीं,’ इस मेरी प्रसिद्ध उक्ति से आप भी अनभिज्ञ नहीं। जब पढ़ा ही नहीं तो लिखता क्या ? जो स्याही, कागज से भी दूर रहा वह क्या खाक पढ़ता व लिखता ? ऐसे भी पढ़ाई के प्रति मेरी धारणा से बच्चा-बच्चा परिचित है, भले ही उस उक्ति का बहुतों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया हो-
पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय।
ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय।।
ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय।।
कहा न, इस उक्ति से बहुतों ने बहुत लाभ उठाया। अरे मैं, तो नैसर्गिक निर्गुण प्रेम की बात कर रहा था-इल्हामी मुहब्बत की, खुदा की इबादत की और बहुत सारे मन-चले अपने और औरों को भटकाने के लिए ढोल पीटते चले-चलो जब कबीर साहब ही ढाई अक्षर को इतना महत्व दे गए तो फेंको पोथी-पतरा और करो प्रेम। इस भौतिक, स्वार्थपरक, सांसारिक प्रेम में ये इतने डूबे-उतराए, मरे-मिटे कि अब लगता है व्यर्थ ही बोल गया (लिख गया नहीं) ये पंक्तियां ? पर अब पछताने से क्या होता है ? जीभ से फिसल गई बात और तरकश से निकल गए तीर को कब वापस आना है ?
खैर, बात कहां से कहां आ गई ? मैं कह रहा था आपको, लग रहा होगा कि यह मुर्दा किधर से और कैसे बोलने लगा। बोलना तो बोलना, लिखने भी लगा। जिसने जीवन-भर लिखने की हिमाकत नहीं कि वह मरने के आधे हजार वर्ष बाद कागज-कलम लेकर कैसे बैठ गया ? किस तन, किस हाथ से ?
तो भाई मेरे, यहां मरता कौन है ? मैंने कहा-‘ना मैं हिन्दू ना मुसलमान।’ मेरा यह कथन भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं; खैर, इस पर नहीं जाइए तो मेरी एक उक्ति को तो मानिएगा ? उन दिनों नाथ संप्रदायी जोगी (योगी) खूब होते थे। अत: मैंने अपने को सबसे काट लिया, योगियों से भी, हिन्दुओं से और मुसलमानों से भी और बोल पड़ा-
खैर, बात कहां से कहां आ गई ? मैं कह रहा था आपको, लग रहा होगा कि यह मुर्दा किधर से और कैसे बोलने लगा। बोलना तो बोलना, लिखने भी लगा। जिसने जीवन-भर लिखने की हिमाकत नहीं कि वह मरने के आधे हजार वर्ष बाद कागज-कलम लेकर कैसे बैठ गया ? किस तन, किस हाथ से ?
तो भाई मेरे, यहां मरता कौन है ? मैंने कहा-‘ना मैं हिन्दू ना मुसलमान।’ मेरा यह कथन भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं; खैर, इस पर नहीं जाइए तो मेरी एक उक्ति को तो मानिएगा ? उन दिनों नाथ संप्रदायी जोगी (योगी) खूब होते थे। अत: मैंने अपने को सबसे काट लिया, योगियों से भी, हिन्दुओं से और मुसलमानों से भी और बोल पड़ा-
जोगी गोरख-गोरख करैं, हिन्दू राम-नाम उच्चारैं।
मुसलमान कहैं एक खुदाई, कबीर को स्वामी, घट-घट बसाई।।
मुसलमान कहैं एक खुदाई, कबीर को स्वामी, घट-घट बसाई।।
हां, तो ‘ना मैं हिन्दू ना मुसलमान।’ हुआ न यह सिद्ध ? मुसलमान कह लो तब भी अच्छा, हिन्दू कह लो तब भी वाह-वाह। पर मरता पूरी तरह दोनों में कोई नहीं। हिन्दू कहते हैं मरना क्या है ? शरीर रहे न रहे, आत्मा कहीं जाती है ? वह जो अजर, अमर, अविनाशी और न जाने क्या-क्या है। उसे न हथियार काट सकते, न आग जलाकर खाक कर सकती, न पानी गला सकता, न वायु ही उसका बाल-बांका कर सकती। मुसलमान कहते हैं रूहें शरीर छोड़ने के बाद पड़ी रहती हैं उस अंतिम दिन की प्रतीक्षा में जब खुदा सबकी करनी-धरनी का हिसाब लेगा।
तो यही मान लीजिए कि मेरी यह रूह, मेरी यही अमर-अनश्वर आत्मा-सवार हो बैठी है एक बीसवीं सदी के मसि-जीवी-लेखक पर और उसी के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देने पर पिल पड़ा हूं। हां पीड़ा ही। अगर अंदर की पीड़ा मुझे अशांत और व्यग्र नहीं करती, मथ नहीं देती मेरे अंतस् को तो इतने दिनों तक शांत पड़ा रहा मैं क्यों कष्ट देने जाता बेचारे इस निरीह लेखक को ?
हां, मेरी पीड़ा कुछ कम नहीं है। अथाह है वह। जीवन-पर्यन्त मैं सांप्रदायिकता, धर्मांधता के प्रति विद्रोह करता रहा, मुल्लाओं-पंडितों से लोहा लेता रहा, आम आदमी को इस व्यर्थ के आपसी विद्रोह के विरुद्ध आगाह करता रहा और आज दुर्भाग्यवश उसी सांप्रदायिकता उसी धर्मांधता का नंगा नाच देखने को अभिशप्त हो गया हूं। रो रहा हूं मैं। सचमुच।
नहीं; आप मेरी भाषा पर नहीं जाइएगा। मेरी तो कोई खास भाषा रही नहीं। ठीक है पूरबिया था और बहुतों ने मेरी भाषा को भी पूरबिया कहा। पर कभी भी किसी बंधन का कायल नहीं रहनेवाला कबीर, भाषा के बंधन को ही कब अंगीकार करने वाला था ? अत: जब जो भाषा, जो शब्द जीभ पर चढ़ी उसे उगल गया। इस स्वतंत्रता, कह लीजिए स्वच्छंदता ही का अधिकार अब भी अपने पास सुरक्षित रखता हूं। अत: मेरी भाषा में कभी कोई खालिस उर्दू या फारसी का जुमला आ जाए या कभी संस्कृत के विशुद्ध तत्सम शब्द उतर पड़े तो दोष आप मात्र इस अभागे लेखक को नहीं दीजिएगा। सारी करनी मेरी ही होगी। ऐसे भी, जिसको अपनी आत्मकथा को लिपिबद्ध करने के लिए बाध्य कर रहा हूं, उसे थोड़ी स्वतंत्रता तो देनी ही होगी। उसको कुछ खास शब्दों, किसी विशेष शैली-शिल्प से मोह होगा तो तृप्त करता जाए वह अपनी इस लालसा को भी। मुझे कोई एतराज, कोई आपत्ति नहीं। अंतत: वह पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी का नहीं, बीसवीं सदी का प्रवक्ता है, अत: उसे तो आज की भाषा में, आपकी भाषा में ही बोलना-लिखना पड़ेगा ? यह बात पृथक् कि अगर वह इस कबीर पर नहीं लिखता होता, उसकी जीवन-गाथा को नहीं गाता होता तो वह भाषा के संबंध में दुराग्रही भी हो सकता था और मौज में आता तो मेरी वर्णसंकरी भाषा को तिलांजलि दे विशुद्ध तत्सम शब्दों से उर्दू-फारसी के शब्दों को कांटों की तरह चुन फेंकता। पर मुझे विश्वास है, वह ऐसा नहीं करेगा। मैं करने भी नहीं दूंगा। मुझे किसी खास जाति, किसी विशेष संप्रदाय, किसी भाषा-विशेष के प्रति राग-अनुराग नहीं रहा तो इसे भी इसकी इजाजत कैसे दूंगा ? अत: उसकी खिचड़ी भाषा को झेलने के लिए आपको प्रस्तुत रहना पड़ेगा। हां, वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि किस स्थान पर किस शब्द का और किस जगह पर किस शिल्प-शैली का प्रयोग करे। इतनी स्वतंत्रता तो उसे देनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं कितना भी अंकुश दूं, वह अपनी चलाने से बाज थोड़े ही आएगा ? कहा भी गया है न उस प्राचीन संस्कृत भाषा में कि कवि-लेखक निरंकुश होते हैं-निरंकुशा कवय:।
अब इस वाक्य को भी तूल नहीं दे बैठिएगा कि यह निरक्षर कबीर देव-भाषा (संस्कृत) में कैसे बोलने लगा। अगर ऐसी बात आपके मन में उठी तो इसके पहले का मेरा सारा तर्क पानी का बुलबुला ही सिद्ध होगा न ? अंतिम रूप में यह प्रकट ही कर दूं कि अंतत: इस आत्मकथा में मेरे तो विचार-मात्र ही होंगे, भाषा बहुत हद तक उसकी ही होगी न ? अब यह उसकी मुझ पर अतिरिक्त मेहरबानी होगी कि वह मेरी भावना मेरे विश्वास, मेरी आस्था की भी कद्र करे और किसी एक भाषा की भंगिमाओं के प्रति दुराग्रही न हो जाए।
खैर, मैं अपनी पीड़ा की बात कह रहा था। यह पीड़ा ही इस अनर्गल (?) गाथा को प्रासंगिकता भी प्रदान करती है, नहीं तो बीसवीं सदी के अंतिम चरण में पंद्रहवीं सदी के किसी पात्र को अपने उपन्यास का नायक बना डालने के लिए इसके समीक्षक इसे कच्चे ही चबा डालेंगे। प्रासंगिकता आपके समीक्षकों का अति प्रिय शब्द है। तो प्रासंगित है मेरी कहानी अपितु और ही अधिक प्रासंगिक हो आई है आज के परिवेश में-मेरी असह्य पीड़ा की पृष्ठभूमि में।
तो लड़ रहे हैं आज लोग। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजे और गुरुद्वारों के नाम पर। यहां तक की चमड़ी के रंग पर भी। अभी कुछ वर्ष ही पहले अमरीका के कई शहरों में श्वेतों और अश्वेतों का ऐसा संघर्ष हुआ जिसने तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति के भविष्य को ही अंधकार में झोंक दिया। अफ्रीका की बात क्या करें ? वहां तो काली चमड़ी, गोरी आँखों की लगातार भारी दुखदायी किरकिरी बनी रही।
खैर, विदेशों की बात छोड़िए। असल पीड़ा तो अपनी धरती, अपनी माटी को लेकर है। यों रूहों-आत्माओं के लिए कोई देश-विदेश नहीं होता। राष्ट्रों की सीमाएं-लकीरें आपकी खींची हुई हैं। एक अशरीरी आत्मा के लिए सारा विश्व ही अपना है पर फिर भी जहां पैदा हुआ, पला-पुसा बड़ा हुआ जिसे अपनी कर्मभूमि-रंगभूमि बनाया उसके प्रति कुछ विशेष राग तो स्वाभाविक है। मेरी इस दुर्बलता को आप अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, ऐसा विश्वास है मुझे।
हां, तो मैं अपने प्यारे देश के द्वारा दी जा रही पीड़ा की ही बात करूं। जिसने, हां जिसने ही मुझे अपनी आत्मकथा को लिखवाने को विवश किया है, लाचार कर दिया है।
कुछ इंगित तो ऊपर कर ही दिया है, पर पीड़ाएं अनेक हैं। आज की भाषा में कहूं तो विविध आयामी। अभी मैं सांप्रदायिकता की बात कर रहा था। इसे झेलता तो मैं विगत कई सौ वर्षों से आ रहा हूं, पर यह पीड़ा अब पराकाष्ठा छूने लगी है। उसका तो पहले ले-देकर एक स्वरूप था-तथाकथित हिन्दू और मुसलमान अल्ला-हो-अकबर और बजरंग बली का नारा दे तलवारें टकरा देते थे, लोगों के जिगरों पेटों में खंजरें उतार देते थे। जिस्मानी लहू की, शोणित की, नदियां बह चलती थी। रैन-बसेरों-झोपड़ियों और महलों-तक को आग की लपटों के हवाले कर उन्हें खाक में मिला दिया जाता था। बेकसूर बेगुनाह अबलाओं-माताओं और बहनों-बेटियों-की अस्मत-इज्जत को नाना प्रकार से, बेदर्दी से बर्बाद किया जाता था।
पर अब इस संप्रदायवाद के सर्प के कई मुख हो आए हैं। यह पौराणिक कालियनाग की तरह कई फनों का बन आया है। अब हिन्दू-मुसलमान ही आपस में लड़ते-कटते हों यह बात कहां रही ? कभी अपने को हिन्दुत्व के घोर समर्थक घोषित करने वाले, हिन्दुओं के लिए अनगिनत कुर्बानियां देनेवाले, अपने किशोरों तक को दीवारों में चुनवा देनेवाले मेरे परम श्रद्धास्पद नानक देव के शिष्य आज अपने को एक सर्वथा नई कौम मान उन्हीं हिन्दुओं को जिबह कर रहे हैं-गाजर-मूली की तरह काट रहे हैं। ए.के 47 (यह आपके युग का नायाब आविष्कार है) से एक साथ दर्जनों बेगुनाहों-बेपरवाहों बेगुनाहों के शरीर के टुकड़े कर रहे हैं ? प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की धज्जियाँ उड़ाने के साथ, उनके साथ लगे अनेकानेक निर्दोषों के जिस्मों की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये पागल हो गए हैं क्या-पूरी तरह विक्षिप्त ? मैं समझ नहीं पाता। आदमी, आदमी के लहू से प्यास बुझाए यह तो शायद सभ्यता के आदिम काल में भी कभी-कभी ही होता था। मैं सोचता हूं और कांप जाता हूं। मेरी रूह थर्रा जाती है। ऐसे भी, शरीर में भी रहता तो रूह ही थर्राती। भावना, संवेदना से संबंध तो उसी का होता है।
रूह थर्रा जाती है कि ऐसा तो पशु भी नहीं करते-चौपाये। अपनी जाति-प्रजाति की रक्षा में ये भी अक्सर तत्पर और सावधान रहते हैं। आपका ‘डार्विन’ कह गया आदमी बंदर से बना है। चलो, एक क्षण के लिए मान लो पर एक बंदर दूसरे बंदर की जान का दुश्मन कहां बनता है ? वे तो बड़े प्रेम से बैठकर एक-दूसरे की जुएं चुनते हैं-पारस्परिक स्नेह दर्शाते हैं। दूसरे जीव उन पर आक्रमण करें तो एकजुट हो उन पर हमला बोल अपने पूरे झुंड को ही बचा ले जाते हैं। कभी-कभी आपस में थोड़ा बहुत चीं-चपड़ कर लेते हों, वह अलग बात है, पर एक बंदर को छेड़ा नहीं कि बर्रे के छत्ते में हाथ दिया। सारे तुम्हारे पीछे पिल पड़ेंगे।
मैं सोचता हूं आदमी पशु से भी गया-बीता हो गया न ? कभी होते होंगे कुछ नरभक्षी, कुछ बियावानों घोर जंगलों में, पर अब तो ‘कंक्रीट’ के जंगलों-तथाकथित सभ्य नगरों-गांवों में रहने वाले भी नरभक्षी हो गए हैं। मेरी पीड़ा स्वाभाविक है, मनुष्य पशु (बंदर) से आदमी क्या बनेगा वह आदमी से पशु हो गया है-तमाशे का बंदर बन गया है।
इस संप्रदायवाद पर पुन: लौटूं इसके पूर्व प्रदेश-गत, राज्य-गत, भेद-भाव के आधार पर व्यर्थ में बहाए जा रहे खून के परनालों की बात कर लूं। मैंने कहा, मैं विदेशों के झंझट में नहीं पडूंगा अत: श्रीलंका और उसके जाफना और अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, उसकी बात नहीं करूंगा। अपनी धरती पर जो कुछ हो रहा है वह इतना त्रासद और पीड़ाप्रद है कि दूसरों का रोना कौन रोए ? मैं पूछता हूं क्या होता रहा अब तक प्रकृति के क्रोड़ में बसे, ब्रह्मपुत्र के समान महान् और पावन नद से पोषित अपने असम में ? क्यों वे कुछ लोग जो तुम्हारी जमीन पर शरण लेने आ गए वे आदमी नहीं रहे ? तुम्हारे बंधु-बांधव, तुम्हारे देशवासी होने से वे कैसे वंचित हो गए ? कोई असमी नहीं होकर बंगाली, बिहारी या बंगलादेशी हो गया तब भी आदमी होने से वह किधर रह गया ?
खैर, मेरी पीड़ा का सर्वाधिक कारण है कि जिस मंदिर-मस्जिद को मैं आजीवन अनावश्यक समझता रहा उसी को लेकर इस हिन्दुस्तान, इस भारतभूमि में विवाद की आंधी बहती रही। नर-संहार हुआ। किशोर और युवा तक अनावश्यक उत्साह में आ धर्मांधों के भाषणों के प्रवाह में आ अपना रक्त सरयू के पानी की तरह बहा गए। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध अब भी अड़ा है-दो अड़ियल सांडों की तरह। अब इस मूर्खता पर मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं ? अरे मैं तो ठहरा निर्गुणिया, मेरा निर्गुण राम, घट-घट वासी है। वह कहां किसी एक मंदिर, किसी एक पाषाण-मूर्ति में बसने-रमने गया ? क्या मैंने गलत कहा था अपने जीवन काल में-
तो यही मान लीजिए कि मेरी यह रूह, मेरी यही अमर-अनश्वर आत्मा-सवार हो बैठी है एक बीसवीं सदी के मसि-जीवी-लेखक पर और उसी के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देने पर पिल पड़ा हूं। हां पीड़ा ही। अगर अंदर की पीड़ा मुझे अशांत और व्यग्र नहीं करती, मथ नहीं देती मेरे अंतस् को तो इतने दिनों तक शांत पड़ा रहा मैं क्यों कष्ट देने जाता बेचारे इस निरीह लेखक को ?
हां, मेरी पीड़ा कुछ कम नहीं है। अथाह है वह। जीवन-पर्यन्त मैं सांप्रदायिकता, धर्मांधता के प्रति विद्रोह करता रहा, मुल्लाओं-पंडितों से लोहा लेता रहा, आम आदमी को इस व्यर्थ के आपसी विद्रोह के विरुद्ध आगाह करता रहा और आज दुर्भाग्यवश उसी सांप्रदायिकता उसी धर्मांधता का नंगा नाच देखने को अभिशप्त हो गया हूं। रो रहा हूं मैं। सचमुच।
नहीं; आप मेरी भाषा पर नहीं जाइएगा। मेरी तो कोई खास भाषा रही नहीं। ठीक है पूरबिया था और बहुतों ने मेरी भाषा को भी पूरबिया कहा। पर कभी भी किसी बंधन का कायल नहीं रहनेवाला कबीर, भाषा के बंधन को ही कब अंगीकार करने वाला था ? अत: जब जो भाषा, जो शब्द जीभ पर चढ़ी उसे उगल गया। इस स्वतंत्रता, कह लीजिए स्वच्छंदता ही का अधिकार अब भी अपने पास सुरक्षित रखता हूं। अत: मेरी भाषा में कभी कोई खालिस उर्दू या फारसी का जुमला आ जाए या कभी संस्कृत के विशुद्ध तत्सम शब्द उतर पड़े तो दोष आप मात्र इस अभागे लेखक को नहीं दीजिएगा। सारी करनी मेरी ही होगी। ऐसे भी, जिसको अपनी आत्मकथा को लिपिबद्ध करने के लिए बाध्य कर रहा हूं, उसे थोड़ी स्वतंत्रता तो देनी ही होगी। उसको कुछ खास शब्दों, किसी विशेष शैली-शिल्प से मोह होगा तो तृप्त करता जाए वह अपनी इस लालसा को भी। मुझे कोई एतराज, कोई आपत्ति नहीं। अंतत: वह पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी का नहीं, बीसवीं सदी का प्रवक्ता है, अत: उसे तो आज की भाषा में, आपकी भाषा में ही बोलना-लिखना पड़ेगा ? यह बात पृथक् कि अगर वह इस कबीर पर नहीं लिखता होता, उसकी जीवन-गाथा को नहीं गाता होता तो वह भाषा के संबंध में दुराग्रही भी हो सकता था और मौज में आता तो मेरी वर्णसंकरी भाषा को तिलांजलि दे विशुद्ध तत्सम शब्दों से उर्दू-फारसी के शब्दों को कांटों की तरह चुन फेंकता। पर मुझे विश्वास है, वह ऐसा नहीं करेगा। मैं करने भी नहीं दूंगा। मुझे किसी खास जाति, किसी विशेष संप्रदाय, किसी भाषा-विशेष के प्रति राग-अनुराग नहीं रहा तो इसे भी इसकी इजाजत कैसे दूंगा ? अत: उसकी खिचड़ी भाषा को झेलने के लिए आपको प्रस्तुत रहना पड़ेगा। हां, वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि किस स्थान पर किस शब्द का और किस जगह पर किस शिल्प-शैली का प्रयोग करे। इतनी स्वतंत्रता तो उसे देनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं कितना भी अंकुश दूं, वह अपनी चलाने से बाज थोड़े ही आएगा ? कहा भी गया है न उस प्राचीन संस्कृत भाषा में कि कवि-लेखक निरंकुश होते हैं-निरंकुशा कवय:।
अब इस वाक्य को भी तूल नहीं दे बैठिएगा कि यह निरक्षर कबीर देव-भाषा (संस्कृत) में कैसे बोलने लगा। अगर ऐसी बात आपके मन में उठी तो इसके पहले का मेरा सारा तर्क पानी का बुलबुला ही सिद्ध होगा न ? अंतिम रूप में यह प्रकट ही कर दूं कि अंतत: इस आत्मकथा में मेरे तो विचार-मात्र ही होंगे, भाषा बहुत हद तक उसकी ही होगी न ? अब यह उसकी मुझ पर अतिरिक्त मेहरबानी होगी कि वह मेरी भावना मेरे विश्वास, मेरी आस्था की भी कद्र करे और किसी एक भाषा की भंगिमाओं के प्रति दुराग्रही न हो जाए।
खैर, मैं अपनी पीड़ा की बात कह रहा था। यह पीड़ा ही इस अनर्गल (?) गाथा को प्रासंगिकता भी प्रदान करती है, नहीं तो बीसवीं सदी के अंतिम चरण में पंद्रहवीं सदी के किसी पात्र को अपने उपन्यास का नायक बना डालने के लिए इसके समीक्षक इसे कच्चे ही चबा डालेंगे। प्रासंगिकता आपके समीक्षकों का अति प्रिय शब्द है। तो प्रासंगित है मेरी कहानी अपितु और ही अधिक प्रासंगिक हो आई है आज के परिवेश में-मेरी असह्य पीड़ा की पृष्ठभूमि में।
तो लड़ रहे हैं आज लोग। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजे और गुरुद्वारों के नाम पर। यहां तक की चमड़ी के रंग पर भी। अभी कुछ वर्ष ही पहले अमरीका के कई शहरों में श्वेतों और अश्वेतों का ऐसा संघर्ष हुआ जिसने तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति के भविष्य को ही अंधकार में झोंक दिया। अफ्रीका की बात क्या करें ? वहां तो काली चमड़ी, गोरी आँखों की लगातार भारी दुखदायी किरकिरी बनी रही।
खैर, विदेशों की बात छोड़िए। असल पीड़ा तो अपनी धरती, अपनी माटी को लेकर है। यों रूहों-आत्माओं के लिए कोई देश-विदेश नहीं होता। राष्ट्रों की सीमाएं-लकीरें आपकी खींची हुई हैं। एक अशरीरी आत्मा के लिए सारा विश्व ही अपना है पर फिर भी जहां पैदा हुआ, पला-पुसा बड़ा हुआ जिसे अपनी कर्मभूमि-रंगभूमि बनाया उसके प्रति कुछ विशेष राग तो स्वाभाविक है। मेरी इस दुर्बलता को आप अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, ऐसा विश्वास है मुझे।
हां, तो मैं अपने प्यारे देश के द्वारा दी जा रही पीड़ा की ही बात करूं। जिसने, हां जिसने ही मुझे अपनी आत्मकथा को लिखवाने को विवश किया है, लाचार कर दिया है।
कुछ इंगित तो ऊपर कर ही दिया है, पर पीड़ाएं अनेक हैं। आज की भाषा में कहूं तो विविध आयामी। अभी मैं सांप्रदायिकता की बात कर रहा था। इसे झेलता तो मैं विगत कई सौ वर्षों से आ रहा हूं, पर यह पीड़ा अब पराकाष्ठा छूने लगी है। उसका तो पहले ले-देकर एक स्वरूप था-तथाकथित हिन्दू और मुसलमान अल्ला-हो-अकबर और बजरंग बली का नारा दे तलवारें टकरा देते थे, लोगों के जिगरों पेटों में खंजरें उतार देते थे। जिस्मानी लहू की, शोणित की, नदियां बह चलती थी। रैन-बसेरों-झोपड़ियों और महलों-तक को आग की लपटों के हवाले कर उन्हें खाक में मिला दिया जाता था। बेकसूर बेगुनाह अबलाओं-माताओं और बहनों-बेटियों-की अस्मत-इज्जत को नाना प्रकार से, बेदर्दी से बर्बाद किया जाता था।
पर अब इस संप्रदायवाद के सर्प के कई मुख हो आए हैं। यह पौराणिक कालियनाग की तरह कई फनों का बन आया है। अब हिन्दू-मुसलमान ही आपस में लड़ते-कटते हों यह बात कहां रही ? कभी अपने को हिन्दुत्व के घोर समर्थक घोषित करने वाले, हिन्दुओं के लिए अनगिनत कुर्बानियां देनेवाले, अपने किशोरों तक को दीवारों में चुनवा देनेवाले मेरे परम श्रद्धास्पद नानक देव के शिष्य आज अपने को एक सर्वथा नई कौम मान उन्हीं हिन्दुओं को जिबह कर रहे हैं-गाजर-मूली की तरह काट रहे हैं। ए.के 47 (यह आपके युग का नायाब आविष्कार है) से एक साथ दर्जनों बेगुनाहों-बेपरवाहों बेगुनाहों के शरीर के टुकड़े कर रहे हैं ? प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की धज्जियाँ उड़ाने के साथ, उनके साथ लगे अनेकानेक निर्दोषों के जिस्मों की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये पागल हो गए हैं क्या-पूरी तरह विक्षिप्त ? मैं समझ नहीं पाता। आदमी, आदमी के लहू से प्यास बुझाए यह तो शायद सभ्यता के आदिम काल में भी कभी-कभी ही होता था। मैं सोचता हूं और कांप जाता हूं। मेरी रूह थर्रा जाती है। ऐसे भी, शरीर में भी रहता तो रूह ही थर्राती। भावना, संवेदना से संबंध तो उसी का होता है।
रूह थर्रा जाती है कि ऐसा तो पशु भी नहीं करते-चौपाये। अपनी जाति-प्रजाति की रक्षा में ये भी अक्सर तत्पर और सावधान रहते हैं। आपका ‘डार्विन’ कह गया आदमी बंदर से बना है। चलो, एक क्षण के लिए मान लो पर एक बंदर दूसरे बंदर की जान का दुश्मन कहां बनता है ? वे तो बड़े प्रेम से बैठकर एक-दूसरे की जुएं चुनते हैं-पारस्परिक स्नेह दर्शाते हैं। दूसरे जीव उन पर आक्रमण करें तो एकजुट हो उन पर हमला बोल अपने पूरे झुंड को ही बचा ले जाते हैं। कभी-कभी आपस में थोड़ा बहुत चीं-चपड़ कर लेते हों, वह अलग बात है, पर एक बंदर को छेड़ा नहीं कि बर्रे के छत्ते में हाथ दिया। सारे तुम्हारे पीछे पिल पड़ेंगे।
मैं सोचता हूं आदमी पशु से भी गया-बीता हो गया न ? कभी होते होंगे कुछ नरभक्षी, कुछ बियावानों घोर जंगलों में, पर अब तो ‘कंक्रीट’ के जंगलों-तथाकथित सभ्य नगरों-गांवों में रहने वाले भी नरभक्षी हो गए हैं। मेरी पीड़ा स्वाभाविक है, मनुष्य पशु (बंदर) से आदमी क्या बनेगा वह आदमी से पशु हो गया है-तमाशे का बंदर बन गया है।
इस संप्रदायवाद पर पुन: लौटूं इसके पूर्व प्रदेश-गत, राज्य-गत, भेद-भाव के आधार पर व्यर्थ में बहाए जा रहे खून के परनालों की बात कर लूं। मैंने कहा, मैं विदेशों के झंझट में नहीं पडूंगा अत: श्रीलंका और उसके जाफना और अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, उसकी बात नहीं करूंगा। अपनी धरती पर जो कुछ हो रहा है वह इतना त्रासद और पीड़ाप्रद है कि दूसरों का रोना कौन रोए ? मैं पूछता हूं क्या होता रहा अब तक प्रकृति के क्रोड़ में बसे, ब्रह्मपुत्र के समान महान् और पावन नद से पोषित अपने असम में ? क्यों वे कुछ लोग जो तुम्हारी जमीन पर शरण लेने आ गए वे आदमी नहीं रहे ? तुम्हारे बंधु-बांधव, तुम्हारे देशवासी होने से वे कैसे वंचित हो गए ? कोई असमी नहीं होकर बंगाली, बिहारी या बंगलादेशी हो गया तब भी आदमी होने से वह किधर रह गया ?
खैर, मेरी पीड़ा का सर्वाधिक कारण है कि जिस मंदिर-मस्जिद को मैं आजीवन अनावश्यक समझता रहा उसी को लेकर इस हिन्दुस्तान, इस भारतभूमि में विवाद की आंधी बहती रही। नर-संहार हुआ। किशोर और युवा तक अनावश्यक उत्साह में आ धर्मांधों के भाषणों के प्रवाह में आ अपना रक्त सरयू के पानी की तरह बहा गए। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध अब भी अड़ा है-दो अड़ियल सांडों की तरह। अब इस मूर्खता पर मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं ? अरे मैं तो ठहरा निर्गुणिया, मेरा निर्गुण राम, घट-घट वासी है। वह कहां किसी एक मंदिर, किसी एक पाषाण-मूर्ति में बसने-रमने गया ? क्या मैंने गलत कहा था अपने जीवन काल में-
पाहन पूजे हरि मिलै, तो मैं पूजौं पहार।
ताते वह चाकी भली, पीस खाए संसार।।
ताते वह चाकी भली, पीस खाए संसार।।
और मस्जिदों को भी मैंने कहां बख्शा ? अरे खुदा हो या भगवान, वह तो सर्वत्र व्याप्त है- तुम्हारे भीतर भी है तुम्हारे बाहर भी। तुमने कुछ सोचा नहीं मांगा नहीं कि बात उस तक पहुंच गई। उसके लिए चिल्लाने की आवश्यकता है ? अजान की ?
मंदिर की, उसके अंदर की पाषाणी मूर्तियों की बात तो मैंने दोटूक कर दी ऊपर। रही मस्जिद की बात तो वह जग-जाहिर है। मुसलमानों ने विशेषकर मुल्लाओं-मौलवियों ने उस समय बहुत आग उगली मेरे विरूद्ध। बात ही चुभने वाली निकल गई थी मेरे मुख से। पर सच्ची बात, खरी उक्ति, कब मीठी और प्रिय होती है ? मुआफ करना मैं तुम्हारी देव-भाषा की इस उक्ति का कायल कभी नहीं रहा कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो लेकिन सत्य भी अगर प्रिय नहीं हो, मीठा नहीं हो, कड़वा हो तो नहीं बोलो-
मंदिर की, उसके अंदर की पाषाणी मूर्तियों की बात तो मैंने दोटूक कर दी ऊपर। रही मस्जिद की बात तो वह जग-जाहिर है। मुसलमानों ने विशेषकर मुल्लाओं-मौलवियों ने उस समय बहुत आग उगली मेरे विरूद्ध। बात ही चुभने वाली निकल गई थी मेरे मुख से। पर सच्ची बात, खरी उक्ति, कब मीठी और प्रिय होती है ? मुआफ करना मैं तुम्हारी देव-भाषा की इस उक्ति का कायल कभी नहीं रहा कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो लेकिन सत्य भी अगर प्रिय नहीं हो, मीठा नहीं हो, कड़वा हो तो नहीं बोलो-
सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्।
न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्।
न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्।
तो मैं तो सत्य ही बोलूंगा और खर ही बोलूंगा और आज जब तुम बाबरी मस्जिद के नाम पर बवेला खड़ा कर चुके हो, लहू के परनाले बहा चुके हो तो मैं मस्जिद को लेकर भी अपनी उस पुरानी उक्ति को ही दुहराऊँगा-
कंकड़ पाथर जोर के, मस्जिद लिया चुनाय।
ता चढ़ि मौला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय।।
ता चढ़ि मौला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय।।
-कंकड़-पत्थर से मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मौलवी मुर्गे की तरह बांग देता है। खुदा बहरा हो गया है क्या ?
ठीक ही कहा न ? पुकारो उसको जो तुमसे बाहर है। जो तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है तुम्हारी सांस-सांस में रचा-बसा है, उसको क्या पुकारना ? ठीक ही कहा उस कृष्ण ने न अपनी गीता में भले ही उसे मुसलमान काफिर कह लें और कुछ मनचले हिन्दू ‘छलिया’ और क्या-क्या, पर थी तो उसपर खुदाई रहमत-ईश्वरीय अनुकंपा ? ईश्वर ही तो था वह कि और क्या था ? हां, तो मैं कह रहा था कि उसने ठीक ही कहा कि उसी का (ईश्वर का, खुदा का) अंश सभी जीवों के अंदर बसा हुआ है-‘ममैवांशो जीव लोके जीव भूतों सनातन:।’
और कुरान (कुरआन मजीद) की ही बात करो तो वह कहां कहती हैं कि खुदा कहीं एक जगह, आसमान की किन्हीं बुलंदियों में छिपा बैठा है ?
ठीक ही कहा न ? पुकारो उसको जो तुमसे बाहर है। जो तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है तुम्हारी सांस-सांस में रचा-बसा है, उसको क्या पुकारना ? ठीक ही कहा उस कृष्ण ने न अपनी गीता में भले ही उसे मुसलमान काफिर कह लें और कुछ मनचले हिन्दू ‘छलिया’ और क्या-क्या, पर थी तो उसपर खुदाई रहमत-ईश्वरीय अनुकंपा ? ईश्वर ही तो था वह कि और क्या था ? हां, तो मैं कह रहा था कि उसने ठीक ही कहा कि उसी का (ईश्वर का, खुदा का) अंश सभी जीवों के अंदर बसा हुआ है-‘ममैवांशो जीव लोके जीव भूतों सनातन:।’
और कुरान (कुरआन मजीद) की ही बात करो तो वह कहां कहती हैं कि खुदा कहीं एक जगह, आसमान की किन्हीं बुलंदियों में छिपा बैठा है ?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book