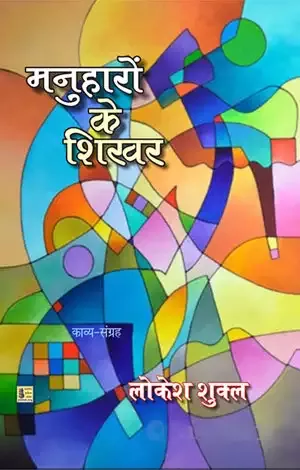|
नई पुस्तकें >> मनुहारों के शिखर मनुहारों के शिखरलोकेश शुक्ल
|
5 पाठक हैं |
|||||||||
लोकेश जी के गीतों का संग्रह
कविवर लोकेश शुक्ल की काव्य-कृति का अंतर्पाठ करते हुए....
वेदना के द्वार दस्तक देती मन की सुगंध
• श्याम सुन्दर निगम
कृतिकार लोकेश शुक्ल हिंदी गीत प्रेमियों के प्रिय गीतकार ही नहीं, वरन उनके अन्दर बैठा एक सौम्य व्यक्ति हर किसी को पुरानी चीन्ही-पहचानी, पढ़ी किताब का मुकम्मल आमुख/ उपसंहार लगता है। उनके मन में सुगंध है। व्यक्तित्व में दूध-मलाई मिठास है। इनसे तादात्म्य बैठा पाए कोई जिज्ञासु पाठक तो कुछ वैसी कसैली परतें भी खुल ही जाती हैं जिन्होंने कवि के व्यक्तित्व की निर्मित में ऊर्जा और ऊष्मा का काम किया है। सहज - संकोची लगता स्वभाव। कुलीन शालीनता भी है। गहराई सागर वाली है। शोध्य खारेपन के साथ यह कुरकुरा और सुस्वादयुत होने लग पड़ता है, उन आत्मीय क्षणों में, जब कभी वह किसी साहित्यिक रचना/कृति पर विमर्श कर रहे होते हैं या, और जब किसी को तटस्थ होकर सुन रहे होते हैं। लगता है कि वह स्वयं को भी भीतर-भीतर खंगाल रहे होते हैं, विश्लेषित कर रहे होते हैं। इसीलिये मेरा मानना है कि जब कोई मुझ जैसा 'अगीत' भी उनके गीत पढ़ेगा (और सोने में सुहागा अगर सौभाग्य से उनके सुकंठ से सुन सकेगा) तो गीतात्म हुए बिना नहीं रह सकता। यादें, यादों से लिपटकर मुस्करायेंगी और जब भी इस रचनाधर्मी शिखर के दूसरी ओर का परिदृश्य देख पायेगा कोई पाठक/श्रोता तो ऐसे 'हालमार्क' कवि से साक्षात् होगा जो त्योहारों के फीके हो जाने से गदमसा महसूस करता है, वहीं उतना ही तल्ख और तीता लगता है जब समाज के लिए नासूर बनती जारही राजनीति की विद्रूपताओं और विसंगतियों पर उंगली रखता है, समाज के बिखराव को अपनी रचनाओं में समेटने-सहजने के जतन करता है। इसी के चलते मुझे भरोसा है कि गीतकार लोकेश शुक्ल की 'कहन' और मेरे मन का 'अनुकथन' किसी दुविधा में पड़े बिना इस पार से उस पार की यात्रा में 'मनुहारों के शिखर' को सुधी पाठकों को शहद-संदल संयोग का सहज ही साझीदार बना लेगा।
कृति में के गीतों के शब्दों और लय की अनुगूंज बहुत देर तक पाठक में बसे रहने की तासीर रखती है। कहीं से भी पाठ प्रारंभ करे, कहीं से। मेरी मानसिक बुनावट की युति तो कुछ यूं बैठती है कि सुधियों के झुरमुट से मुलकना, मुलक-मुलक कर रतनारे नयनों की भाषा पढ़ना, और इस अनुक्रम में छुए-अनछुए तटों से नई पहचान, प्रेमगीतों के रचनाकार लोकेश शुक्ल की सृजनधर्मिता की पाकीजा आधारभूमि है। रचनाकार 'अनदेखा' देखते हुए बचपन के शरमाते दिनों में खो जाता है। कंचन हिरण हो जाती हैं किशोर यादें। कभी ओट ले लुकना-छिपना और कभी लौक पड़ना। इस 'कभी खो जाने' के और 'कभी खोजे जा पाने' का सुफलित ही है ये कि एक तरफ बरखा की बूंदों से मन पागल होता है, तो दूसरी तरफ बिन बातों के नयनों का काजल धुल रहा होता है - निष्कलुष प्रेम, अद्भुत चित्र !
'बिखरे तो पर बिखर न पाए निखरे छंट-छंट के'।
लोकेश जी की लेखनी की अद्भुत जादूगरी।
पागल-पागल मन को, काजल-काजल अपना बना लेना।
कमाल ! बरबस गीत फूट पड़ता है -
'ये कैसा दरपन दे दिया तुमने,
खुद को देखूँ तुमको पाऊँ'
ये एक तरफ, और दूसरी तरफ का भाव अनायास ही नहीं, प्रत्युत गीतकार के गरिमामय व्यक्तित्व से मुहाँ-चाई करता अपने समकालिक घटाघट को रेखांकित करता एक ऐसा सजग कलम का सिपाही है जो चिंता से चिंतन की राह निकाल लेता है। भूल जाता है अपने हृदय पर लगे नुकीले होगये प्यारे रिश्तों की चोट। भूल जाता है 'गैरों' जैसे आचरण करते 'अपनों' के भीतर छिपे खोट। ऐसा ही कुछ तो इलहाम भी हुआ होगा उन दिनों 'जब आस की छाँव में आस्था के कदम डगमगाए कभी तो मिली थी दुआ'। उतरी थी एक दिव्य-किरण संदेशा लेकर कि 'तुम कभी उस द्वार पर जाकर तो देखो, प्राण के बंधन तुम्हें छूटे मिलेंगे'। ये भी कि कदाचित् कवि का स्वाभिमान ही बेड़ियां बना ले और नहीं जा पा सके 'उस द्वार' तो न सही, अपनी प्रेमरस की उसी चितवनी गुनगुनाहट में लौट जाए जहाँ `नागफनी के जंगल-जंगल बोता रहा बीज फूलों के' उन्हीं फूलों की पंखुरी-पंखुरी महक बांचे कि... ; अपने पास ज़रा बैठो तुम / उतरो मन की गहराई में / मिल जाते प्रश्नों के उत्तर आसानी से तनहाई में'।
सहज अलभ्य इन्हीं 'दिशा देते' गुरु-चिंतन के निर्मोल क्षणों में कवि कभी अपने हिस्से आये ऊबड़-खाबड़ रहे आये जीवन के आध्यात्मिक खण्ड को अपने तईं जी लेता है और उन्हें स्थाई- भाव दे पाने के निमित्त लेखकीय अनुलोम-विलोम सा करने लगता है, नयी साँस भरता है। नयी ऊर्जा के साथ जीवन के नए पाठ खोलता है। अपने सुधी पाठकों के लिए पोर-पोर में भरे उमंग और जोश की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक उत्सवधर्मी उत्साह ! जैसे रेशम की डोर से ठुनकी दे-देकर, 'मैं' और 'तू' की रटन लगाये मन को खुशबू के आभास की ओर खींचता है, खोजता है मरुथली गाँव की बुलाहट वाली सुरीली बाँसुरी। जाने कहाँ खो गयी निगोड़ी, हृदय की पीर भी ले गयी। काश ! ऐसा हो जाए कि वही फागुन... जो आबाल-वृद्ध नर-नारियों के होश हर लेता था, लौट कर आ जाए, आज के अपरिचित से लगते मौसम में घुल जाये। एक अप्रतिम, उपमेय गीतकार की लेखनी से होली के रंग बनकर पूरी कायनात को भिगो जाए। कवि के साथ-साथ अमृत-पलों को न भुला पाने वाला समूचा परिवेश सराबोर हो जाए, ऐसे कि -
गुझिया सी फूली फिरे बरसाने की नार
घूंघट लंबा काढ़कर करे लठ्ठ की मार
अद्भुत है ये परिकल्पना, जहाँ गुझिया उत्सव बन गयी, बरसाना प्रेमोपहार हो गया, घूंघट मर्यादा, और लट्ठ की मार... मीठी छेड़-छाड़ ! इन सभी तत्त्वों में गीतकार लोकेश शुक्ल के सेमल-फाहे जैसे सुकोमल मन की भीनी-शबनमी तासीर सर्वनिष्ठ है।
सुगंध ! सुगंध के बीच आपस में फुसफुसाते मकरंदी तंतु, जो एक आयु पाकर शब्दों में गीतरूप धर लेते हैं। मोहक पल छीनकर गले आ मिलते हैं। सुधियों में लहरा जाता है कोई न कोई बिखरा स्वप्न, ऐसे कि किरण-किरण 'चाँद' खुशबू के अध्याय बाँचते हुए शरमा जाता है '। चाँद का शरमाना उधर, इधर मन के निराले ठौर, निराले ठौर पाकर मन में बौंसते बौर ! इन्हीं पूजिल पलों में जैसे एक अनुभूति उल्लसित हुयी-हुयी सी प्रत्यक्षा...
'सावन नभ का दामन निर्मल कर महकाता है,
वैसे तेरा रूप देखकर मन पवित्र हो जाता है'।
इन्हीं पंक्तियों में कवि लोकेश की असीम गीतमयता स्वयमेव शिखर हो जाती है। बावरी प्यास कोई सीख सुनने को तैयार नहीं। मृगतृष्णायें दुबक जाएँ तो केवल और केवल 'मनुहारों' का ही आसरा कि 'मेरे मीत! तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उसका मन बाँच कर तो देखो, फिर अपने भीतर से आती आवाज को सुनो, फिर तो तुम नहीं, शिखर स्वयं मनुहारों पर न्योछावर हो जाएगा, समर्पण की राह चल पड़ेगा, गुनगुनाहट और महामहाहट साथ मिलकर आवाज देंगे-
आओ हम जोड़ें बिखरे कोमल संबंधों को,
आओ भावों के गहने हम पहनायें रूठे छंदों को,
चलो चांदनी की राहों में फैलाएं रजनीगंधों को
आओ मीठे संबंधों से दूर करें सब कटु तटबंधों को
गीतकार ने 'मनुहारों के शिखर' के माध्यम से 'कैप्सूल प्रेमग्रंथ' लिख दिया जिसने बरबस बच्चन जी की अमर पंक्ति 'इस पार प्रिये मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा' का स्मरण करा दिया। यहाँ नहीं, तो फिर और कहाँ होगा कि हृदय की पीर वेदना के द्वार खड़ी पुकार लगाती है, और साँझ वेला है कि समय सापेक्षता को स्वर देती है, धूल उठती देखती है। फिर भी अपने अन्तस् में एक अटूट विश्वास जीती है कि 'जब हर तरफ सुगंधों के डेरे लगे हैं, तो भटके हुए मन को सहारा मिल ही जाएगा', बस इस 'दाह' को अपना बना कर देखना है, प्रेम की तपिश को आत्मसात करना है, कोखजायी कविता की तरह हौले-हौले सहलाना भी है, अपनाना भी है। यहीं मिलेगा खुशबू का संगम यहीं होंगी कस्तूरी की बातें, और होंगी संदली रातें। सुघर, लजीली। प्रीति की लताएँ झूलेंगी, आत्मिक ऊष्मा में प्रतीति अंकुवायेगी - आसक्ति के चरम क्षण...। किसे पता वन्दगी को किस धार बहा ले चले, किस बहार से भेंट कराये, जहाँ सिवाय इसके कुछ न सूझे कि प्यार में पूजा चढ़ी हर भावना महकी हुयी लगे। प्रेम ईश्वर की झाईं बना सामने ही दिपदिपाये, बाकी सारी छवियाँ इसी अद्भुत प्रेमपर्व का हिस्सा बन जायें।
बहुआयामी व्यक्तित्व के मालधनी हैं कविवर लोकेश शुक्ल जी। सौम्य, सुशील संस्कारवान। एक जुम्मेदार नागर भी हैं। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है और ये दोनों समेकित रूप में लोकेश जी के गीतों की निर्मित का बिन्दु भी हैं, परिधि भी।
साथ ही साथ विचार ये भी करना है कि इनकी रचनाधर्मिता का दूसरा ध्रुवांत भी है जहाँ अपने दंशों की गठरी सर पर लादे आज का मनुष्य है, क्रमश: छीजते जाते मानव-मूल्य हैं, व्यापक और वृहत्तर सन्दर्भों में निरंतर संवेदनाच्युत होता जा रहा समाज है। कवि को मानवीय जीवन की संरक्षा की चिंता है, जिसके लिए उनकी स्वयं की फूल-शूल-धूल वाली जीवनयात्रा 'मूल' मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित है। वह लम्बे अरसे तक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, किन्तु इस अहम् के पोषण से विरत रहे कि वह बड़े हिंदी समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' से जुड़े रहे। लोकेश जी तो चेहरों पर चस्पां चेहरों की परतें उचाड़ने के पक्षधर रहे। वह विस्मित होते हैं कि...
ये कैसा उजाला है चारों तरफ
आदमी डर रहा है परछाईं से
कवि के अंतस्तल में तो प्रेम के कोटर हैं, जिनके पार्श्व में ही घनी पीड़ा के प्रकोष्ठ अंत: निर्मित हैं। इन्हीं में वह पल-पल मरते - जीते आदमी को देखते हैं, टुकड़े-टुकड़े बंटते आदमी के बहुत नजदीक जाकर जीवन की माईक्रोस्कोपिक संवीक्षा करते हैं, और पाते हैं कि भाग रहा है मरुथल- मरुथल मिले न कोई ठौर है'। कवि को दुर्दिनों की पदचाप सुनाई पड़ने लगती है, किन्तु यहाँ भी मिलता है तो बस नकली आचरणों का मेला, अकुलाहट के घने अँधेरे। सुखों की सियने उखड़ी हुयी हैं, जीवन में ऐसी अजब-गजब आपा-धापी है कि पर्वत - पर्वत घाटी - घाटी, बादल - बादल छाती फाटी। नतीजतन, कवि बड़ी गंभीरता के साथ रेखांकित करता है कि-
टूट चले आँखों के रिश्ते अपने ही खारे जल से
नाता कोई नहीं रहा अब पुरवाई के आँचल से,
कोमल सपनों की सौगातें छीनी हैं इस मौसम ने
जीवन की बिसात उलटी है राजनीति के पासों ने...
सुख-दुःख के सभी ताने-बाने मन की तकली से कातने जब कभी बैठ जाता है कवि तो उसकी अन्तस्थ पीड़ा इतनी सघन हो जाती है कि जब कभी सामने कुछ ऐसा-वैसा देख लेता है तो सहसा बुदबुदा उठता है नौनिहाल कंधों को पर्वत ढोने की मजबूरी है...
अजीब दौर से गुजरना हो रहा है कि 'आँसू आँखों में ही सूख जा रहे हैं', निश्चित ही कवि, थोड़ी देर के लिए, इन शब्दों को समतुल्य भाव दे पाने में किंकर्त्तव्यविमूढ़ हुआ होगा। उसे अपनी लेखनी की रोशनाई ही सूख गयी सी लगी होगी। द्वन्द से जूझना पड़ा होगा... आखिर वह लिखे तो क्या लिखे, किस विधि लिखे, किसको लिखे...' आदमी' है कहाँ ! आदमी लाये कहाँ से !! वह तो तकनीकी विस्तार में मशीन बन गया है'। विकल्प्तः कवि कुछ पीछे लौटकर मानस यात्रा करता है। अपने खुद के जिए जीवन की उलटबांसी - पावस, गर्मी, होली के मौसम में -- बरास्ते राजनीति, धर्म, उन क्षणों को खोज पाने के जतन करता है जहाँ बूँदों की पायल बजती है, हठ की गांठें खुलती हैं, साँझ केश सँवारती है, मन सहज ही उस पार पहुँच जाता है जहाँ बादल आपस में बतियाते दिखते हैं। बादलों का बतियाना जैसे दूर कहीं टीले पर बैठे किसी अजाने बरेदी की गर्म साँसों से निकलती आती अलगोझे की गूँज... तभी तो सूरज भी अपनी तपन भूलकर अठखेलियाँ करता दिखता है।
कवि का आत्मबल उतना ही प्रबल है जितनी उसकी आस्तिकता। आस्थाजनित आश्वस्ति उसकी निजी पूँजी है। और विरासत भी। इन्हीं के चलते न उसका सोच डिगता है, न उसकी कलम रुकती है। उसे तो भरोसा है...
जीवन तम में दीपशिखा सा राम नाम उजियारा है / सब का यही सहारा है / जग का पालनहारा है / जन-जन का रखवारा है..
सीताराम की शक्ति से पर्वत सी विपदाए कटती हैं... एक भरोसो, एक बल... इस अनुशीलन में सृजन के अद्भुत क्षण अँकुवाते हैं। नए-नए रास्ते खुलते हैं, कवि स्वयं मशाल लेकर आगे खड़ा दिखता है समाज के प्रति एक साहित्यकार का इससे बेहतर प्रदेय क्या हो सकता है... शिखर पर खड़े होकर समय के बोल सुनता है। 'कल' की आवाज बनकर 'आज' का आवाहन करता है - 'संकट में हताश मत हो तुम, पलटो कुछ पन्ने अतीत के'।
नफ़रत कभी सर्जना नहीं होती, भूखे पेटों से मुंह मोड़ लेने से कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती। गहरे सागर में स्वयं ही उतरकर देखना है, सार्थक संवाद की पहल होगी, दुनिया के चीन्हे / अनचीन्हे तमाम चेहरे सामने होंगे। एक दूसरे से टकराती लहरों को आपस में बतियाते हुए पायेंगे। माटी के गीत गुनगुनायेंगे तो कुछ न कुछ सुवास होगा ही', कवि का दृढ़ विश्वास मुखरित होता है कि -
टूट गए सपने तो क्या हुआ...
आशा के दीप तो जलाओ,
कुछ न कुछ प्रकाश होगा।
अपने किरदार तो निभाओ,
कुछ न कुछ तो उजास होगा।
यह एक यथार्थ है। मनुष्य के जीवन में क्वचित् अपरिचित भाव जबरियां अपना डेरा डाल लेते हैं, रास्ते में डोर 'ढील-घसीट' करते हुए ले चलते हैं, पर किधर ! कुछ पता नहीं चलने देते...। वहीं दूसरा अवलम्ब है कि सहसा एक रूप-सरूप झिलमिल-झिलमिल करने लग जाता है। अलौकिक आभा, अकल्पनीय दीप्ति। कभी साक्षात् होने पर प्राण उमगते हैं लोचन में'। सुगंध की चादर सामने फ़ैली दिखती है, खुशियों की सौगातें उतार फेंकती हैं पीड़ा की छेदही पिछौरी। पतझर, सावन, बिजली, बादल गलबहियाँ डाले साझा-मखमली-ओढ़नी वाली बातें करने लगते हैं। यादों के घने कुहासे स्वयमेव छँटने लगते हैं, रेत के अधरों की प्यास बुझती है, अगन में सपन में मन के निराले बौर खिलते हैं। कवि इसके निमित्त मंत्रवत सूत्र छोड़ता है--
मन को ज़रा बदल कर देखो, घर चौबारे फिर महकेंगे
दिल के रोशनदान खुलें तो, ढाई आखर फिर चहकेंगे...
सिद्ध गीत-कवि लोकेश शुक्ल अपनी संजीदा और ईमानदार रचनाधर्मी साधना के चलते स्वयं शिखर हुए लगते हैं जब वह आत्म-संबोधन करते हैं -
ऐसा कोई गीत रचो मन
जिसकी गूँज नहीं मिट पाए
जन-जन की पीड़ा हर जाए
भटकों को रस्ता दिखलाए,
जो इकतारों पर लहराए,
जो सब के दिल को महकाए...
मेरी शुभकामनाएँ कि गीतकार लोकेश शुक्ल की मानव-कल्याण की कांक्षा सुफलित हो...
मुझे विश्वास है काव्य-कृति 'मनुहारों के शिखर' को विज्ञ पाठकों का भरपूर सम्मान मिलेगा।
- श्याम सुन्दर निगम
|
|||||