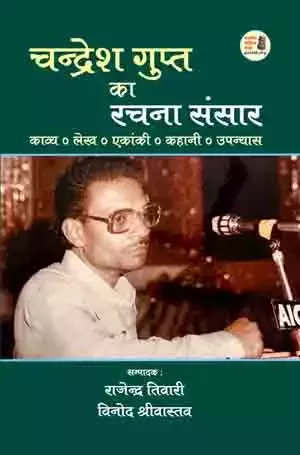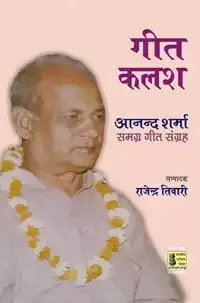|
संकलन >> चन्द्रेश गुप्त का रचना संसार चन्द्रेश गुप्त का रचना संसारराजेन्द्र तिवारीविनोद श्रीवास्तव
|
5 पाठक हैं |
||||||||||
विलक्षण साहित्यकार चन्द्रेश गुप्त का समग्र रटना संसार
ब-क़लम ख़ुद
चन्द्रेश की कहानी, उन्हीं की ज़बानी
नाम से किसी भी शख्स की पहचान एक सीमित दायरे में बनती है, फिर भी जरूरी है। क्योंकि शुरुआत इसी से होती है। रमेशचन्द्र गुप्त, कब चन्द्रेश रमेश चन्द्र गुप्त बने और फिर रमेश चन्द्र गुप्त चन्द्रेश से चन्द्रेश गुप्त हुए, यह तो याद नहीं, लेकिन नामों में परिवर्तन की यह उखाड़-पछाड़ ठीक वैसे ही हुई जैसे जिन्दगी में अन्य सारे कार्य होते हैं। अलबत्ता यह जरूर है कि चन्द्रेश गुप्त के जीवन में कभी कोई चीज क्रमशः नहीं हुई। सम्भवतः किसी-किसी के जीवन का क्रम व्यतिक्रम जैसा भी होता है। इसे समय का चक्कर और नियति का फेर भी कहा जा सकता है।
अब से 57 वर्ष पहले 2 अक्टूबर 1937 को पैदा हुए चन्द्रेश गुप्त ने ग्यारह-बारह वर्ष की उम्र में जो पहला झटका खाया तो अपने को एकदम तन्हा महसूस किया। सम्पन्नता और लाड़-प्यार में खुली आँखें, कम उम्र में ही अभाव तथा विपन्नता के रेगिस्तान को देखकर जीवन की जिजीविषा लिये अपने अस्तित्व की स्थापना में घूमने लगीं।
कानपुर तब छोटा था। शान्त, सुकून भरा। फिर भी जिन्दगी को जिन्दगी की तलाश ने दौड़ाया, भटकाया, परेशान किया और लड़ने की आदत दी जो आज तक उसी शिद्दत से बरकरार है। यह दौड़ शायद ता-उम्र चलेगी।
सम्भवतः किसी भी लेखक या रचनाकार की रचनात्मक ऊर्जा का उत्स उसका जीवन संघर्ष ही होता है। क्योंकि जो भीतर होता है, उसे बाहर लाने के लिए कागज और कलम का संयोजन अपने आप हो जाता है।
टुकड़े-टुकड़े करके पूरी हुई एम.ए.(हिन्दी), फिर साहित्यरत्न (हिन्दी), संस्कृत की शिक्षा, उपलब्धि कम एक झूठे आत्मतोष का कारण जरूर है कि रोजी-रोटी का जुगाड़ बनाने में सहायक हो गयी।
चन्द्रेश गुप्त सम्भव था, रचनाकार न होते तो संगीतकार या गायक होते लेकिन नियति ने मार्ग जो निर्धारित कर दिया था, सो लेखक और कवि हो गये। गद्य के साथ पद्य लेखन भी शुरू हुआ था सो सन् 1956 में ही प्रताप अखबार में पन्द्रह अगस्त के लिए कविता लिखकर भेज दी। हैरानी हुई। कविता छप गयी। छपने से उत्साह बना। कलकत्ता से निकलने वाली फिल्म-पत्रिका 'अभिनय' में कविता भेजी। वह भी छपी। फिर लिखने का क्रम चालू हो गया। अचानक एक दिन एक पैकेट डाक से आया। असमंजस, उत्सुकता से पैकेट खोला। देखकर उछल पड़ा। मेरी भेजी हुई पाण्डुलिपि छपे उपन्यास के रूप में सामने थी –'जहरीली गैस'
यह उत्साह बढ़ाने वाला प्रयास था। लेकिन अपरिपक्व मानसिकता यह नहीं देख सकी कि 'ट्रैक' गलत पकड़ लिया है। दूरगामी परिणाम क्या होंगे? बहरहाल जासूसी उपन्यासों के लिखने का चस्का लगा तो फिर लग ही गया। पैसा भी मिल रहा था और ख्याति भी। चूँकि इलाहाबाद प्रकाशन का केंद्र था इसलिए प्रकाशक भी दौड़ने लगे। कानपुर से उन दिनों प्रेम बाजपेयी ख्याति की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। लेकिन उनका लेखन जासूसी नहीं था।
एक अजीब संयोग था। गद्य में जासूसी और पद्य में गीत, कविता लेखन। कोई तालमेल नहीं था दोनों में मगर चला और खूब चला। सन् 1960 में विजय शंकर दीक्षित 'चंचल' के सहयोग से आचार्य वागीश शास्त्री के सान्निध्य में आया। आचार्य जी साप्ताहिक 'सहयोगी' पत्रिका का सम्पादन कर रहे थे और नई पीढ़ी के लिये प्रेरणा स्रोत भी। हास्य-व्यंग्य के स्तरीय कवि हैं। उनके साथ मंचों पर आना-जाना भी शुरू हुआ।
उन्हीं दिनों आचार्य किशोरी दास बाजपेयी और आचार्य वागीश का अंत: राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शब्द को लेकर शास्त्रार्थ हुआ। यह कानपुर के साहित्य जगत की ऐतिहासिक घटना थी। संस्कृत और हिन्दी के उद्भट विद्वानों का वाक् युद्ध। आचार्य बाजपेयी द्वारा पराजय की आत्म स्वीकृति, वागीश जी द्वारा विनम्र निवेदन, आचार्य जी की क्रुद्ध मुद्रा, सकपकाये विद्वान, अदभुत दृश्य।
उन्हीं दिनों कवि बच्चन के गीत में मयूरी के नाचने को गलत ठहराने की बहस। दरअसल 'सहयोगी' पत्रिका में एक स्थायी कालम था हिन्दी में बिंदी, इस कालम में वागीश जी हिन्दी में गलत प्रयोग करने वालों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। बहरहाल जीवन के वे सुनहरे दिन थे। सीखने, जानने, समझने का खूब मौका मिला। परिचय का दायरा भी बढ़ा। कानपुर से ही 'धर्मयुग' की टक्कर में 'मनु' साप्ताहिक का पं. शम्भू रतन त्रिपाठी के सम्पादन में निकलना, चर्चा होना कानपुर के साहित्य संसार में चहल-पहल मचाये था। उन्हीं दिनों पत्रकार पं. विष्णु त्रिपाठी द्वारा 'सोपान' पत्रिका का निकलना प्रमुख घटनाएँ थीं।
उन्हीं दिनों कलकत्ता से भोलानाथ 'बिंब' के सम्पादन में बेहद अच्छी पत्रिका 'बिंब' निकल रही थी। कलकत्ते के वरिष्ठ कथाकार छेदी लाल गुप्त एक कहानी पत्रिका से सम्बद्ध थे। उसमें भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ भी छपती थीं। विश्वामित्र, अभिनय, बिंब और कहानी पत्रिका में कविताएँ गीत व कहानियाँ छपीं। आगरा से 'युवक' पत्रिका और 'साहित्यालोक' निकलते थे। उनमें भी छपा। लेकिन तब तक चन्द्रेश गुप्त, रमेश चन्द्र गुप्त 'चन्द्रेश' थे। यही नाम जासूसी, फिर सामाजिक उपन्यासों में भी जा रहा था। पत्रकारिता का चस्का वागीश जी ने पैदा किया। हास्य पत्रिका 'चोंच' का प्रकाशन शुरू करवा कर। उसमें सह सम्पादक बना। प्रकाशक बने राम सेवक भारतीय, अब लखनऊ में हैं।
कविता का मंच भी सिर चढ़कर बोल रहा था। सो आचार्य सनेही, आचार्य बिहारी की मण्डली में भी धँसा। कंठ बहुत अच्छा है, सो कार्यक्रमों में खूब बुलाया जाता। सभी का स्नेह भरपूर मिला और मार्ग-दर्शन भी। आज जो भी हूँ उन्हीं दिनों की देन है।
लेखन के अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों में प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था 'वासंती' की स्थापना व नटराज संस्था की स्थापना में सहयोग तथा अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलनों का संयोजन, स्मारिकाओं का सम्पादन।
इसके अलावा 'चोंच' का सम्पादन। श्याम लाल गुप्त 'पार्षद' अभिनन्दन ग्रंथ का सम्पादन। डेढ़ साल तक 'नगरवधू' पत्रिका का सम्पादन। अब अनियतकालीन नवगीत पत्रिका 'गतिविधि' का सम्पादन-प्रकाशन।
सन् 1965-66 में साठोत्तरी कविता आन्दोलन से जुड़कर 'साठोत्तरी कविता' संकलन के एक कवि के रूप में चर्चा।
प्रकाशन- कई सौ उपन्यास, डेढ़ दर्जन कहानियाँ, फुटकर गीत, नवगीत व कविताएँ, समीक्षाएँ, लेख। 'नदी-नाव संयोग' तथा 'चिन्दी-चिन्दी जिन्दगी' उपन्यास प्रकाशित। 'चिन्दी-चिन्दी जिन्दगी' दैनिक जागरण में धारावाहिक रूप से छपा। सफर-दर-सफर और नवगीत संग्रह शीघ्र प्रकाश्य।
सम्मान के नाम पर सबसे बड़ा सम्मान आनन्दपुरी सिटीजन्स फोरम ने किया। सम्मान में अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन भी किया। प्रबुद्ध युवा भारती, सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी तथा पं. दुर्गा प्रसाद दुबे पुरस्कार समिति से सम्मानित।
साठोत्तरी कविता आन्दोलन से जुड़ने की कोशिश की मगर लगा कि आन्दोलन से जुड़ना रचनात्मकता कम राजनीति ज्यादा है सो पलायन कर दिया।
दरअसल साहित्य को किसी भी आन्दोलन की दरकार कभी नहीं होती। किसी भी आन्दोलन को बनाना या उससे जुड़ना केवल इस कारण होता है कि किसी प्रकार स्थापना हो जाय, मान्यता मिल जाय, लोगों की स्वीकृति मिल जाय। इस दृष्टि से देखा जाय तो कहानी, कविता और आलोचक - तीनों में जमकर वाद चले। लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात जैसी है। सार्थकता केवल रचनात्मकता में है। क्योंकि कोई भी रचना अपने आप में आन्दोलन हो सकती है, होती भी है। उसके लिये तर्क, बहस, गोष्ठियाँ किसी विचार विशेष का सम्प्रेषण करने वाली होती हैं। जबकि रचना सार्वभौमिक होती है। उसके लिये मैन्युफैस्टो या किसी फतवे की जरूरत नहीं। बैसाखी की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि सारी बहसें-मुबाहिसे, घोषणापत्र, रचना के संदर्भ में, समय के गर्त में चले गये। रचना केवल रचना होती है। जरूरत इस बात की है कि लेखन आदमी से आदमी तक हो। यही उसका कद भी है।
आज के रचनाकार के साथ एक दिक्कत यह है कि वह अपनी रचना के लिये तमाम अवलम्ब थामता है। जबकि यह काम उन पर छोड़ा जाना चाहिए जिनके लिये लिखा जा रहा है। चूँकि दूसरा पक्ष भी हमने थाम रखा है। जाहिर है कि जो काम हमारा नहीं है, वो भी किया जा रहा है। यही कारण है कि अनेक उपलब्धियाँ और अनेक राग होते हुए भी आम आदमी के नक्कारखाने में उसकी तूती नहीं सुनाई पड़ रही है। मियाँ मिट्ठू बनने का दम्भ, बुद्धिजीवी होने का भ्रम और रचनाकार होने का अहम् आम आदमी की पकड़ से बाहर रहता है। रचनाकार की त्रासदी यह भी है कि उसे अब खबरों, चित्रों की जरूरत रहती है। इस चक्कर में वह अपनी विरासत की भी उपेक्षा किये हुए है। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक विरासत से कटना, बृहत्तर लोक संस्कृति से भी कटना है। यह बात एकदम साफ है कि जमीन से कटकर न तो स्थायित्व मिलना है, न जीवन की बोधगम्यता। दरअसल जब हम यह मानकर चलते हैं कि साहित्य का केन्द्रबिन्दु मनुष्य है, तब यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि रचनाकर पहले आम आदमी है और यदि उसका बोध आम आदमी जैसा वास्तव में है, तब वह उस जमीन, समाज और देश की उपेक्षा कैसे कर सकता है - जिनके बीच में रहता है।
एक बेहद कटु सत्य है कि हिन्दी में जितने भी वाद पोषित किये गये हैं उन सबका मूल उद्देश्य आत्मस्थापना के सिवाय कुछ नहीं है। यह आत्मस्थापना वायवीय और आयातित विचारधारा है। रहना, खाना, पीना, जीना-मरना जब सब यहीं की जमीन पर है तब यहीं की विरासत हमारे लेखन की बुनियाद बन सकती है, और है भी। अपनों के बीच संघर्ष के लिये जाने-पहचाने हथियार काम देंगे। हम जीवन यहाँ का जियें और सोच आयातित हो, तो जाहिर है कि साहित्य अजनबी रहेगा। हिन्दी के साथ यह दुर्भाग्य व्यापक स्तर पर जुड़ा है। जीवन, रहन-सहन, भाषा और संस्कृति ही किसी विचार की जन्मदात्री होती हैं। इसे समूह स्तर पर एक षड़यंत्र के तहत काटा गया।
अक्सर चर्चा चलती है कि हिन्दी का साहित्य बिकता नहीं है। लेकिन क्या सदैव ही ऐसा रहा है। एक नहीं पचीसों उदाहरण हैं जब साहित्य, हिन्दी साहित्य को पाठकों ने अपनाया है। यहाँ तक कि अन्य हिन्दयेत्तर भाषा का अनुवाद तक हिन्दी में जमकर अधिकाधिक संख्या में बिका है, बिक रहा है। तब शुद्ध हिन्दी के बिकने में क्या दिक्कत?
चन्द्रेश गुप्त पुन: यह कहना चाहेंगे कि अपनों के बीच साहित्य को इतना चमत्कारिक और गूढ़ मत बनाइये कि अजनबी बनकर रह जाये। हमारे हिन्दी के स्वनामधन्य महिमामण्डितों ने अपनापन अपनों के ही बीच 'वाद' के कारण 'अजनबी' बनाकर परोस दिया। परिणाम यही होना था।
दर्जनों ऐसे नाम गिनाये जा सकते हैं जो बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू के हैं। लेकिन हिन्दी में वे अजनबी न होकर हिन्दी के ही लगते हैं। अपने लगते हैं। अपनी जमीन, अपनी जमात के लगते हैं। इस फर्क के बारे में सोचने की जरूरत है। हिन्दी का रचनाकार हिन्दी के लिये अजनबी और हिन्दयेत्तर भाषी हिन्दी का अपना? इसे दुरभिसंधि नहीं कहा जायेगा? और मजाक यह है कि इतना सब कुछ 'वाद' के चलते हुआ, हो रहा है। शायद आगे भी होगा। अपने-अपने वादों के कोटरों में बन्द हिन्दी के स्वनामधन्य रचनाकार अपनी ढपली बजाने में लगे हैं भले ही उनकी कोई सुने या न सुने।
यहाँ मैं दो प्रमुख नामों का उदाहरण देना चाहूँगा। एक पंडित बेचन शर्मा 'उग्र' और दूसरे हंसराज रहबर। इसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि इनके समकालीनों ने इनको इसलिए अस्वीकृत और उपेक्षित किया क्योंकि इन्होंने न 'वाद' के कोटर में अपने को बन्द किया और न किसी लादी गयी विचारधारा को स्वीकार किया। यह दोनों रचनाकार चले बेबाक कलम के दम पर। इन्होंने अपने चेले-चपाटी या पिष्टपेषण करने वाले भी नहीं तैयार किये।
निराला जी का नाम इसी प्रसंग में लेना अन्यथा नहीं होगा। उनके साथ कतिपय साहित्यकारों व समालोचकों ने क्या-क्या किया, इसे जानने वाले इक्का-दुक्का आज भी मौजूद हैं।
एक शख्स और स्मृति में है। कलम की दम पर अपना लोहा मनवाने की क्षमता रखनेवाले रचनाकार स्व. राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी के साथ साहित्य जगत ने जो दुर्व्यवहार किया, उनके जीवन में उसे 'घृणित' तक कहा जा सकता है, मेरी अपनी दृष्टि में, सम्भव है लोगों को गलत भी लगे, यदि स्व. चौधरी के सम्पूर्ण लेखन का ईमानदारी के साथ पुनर्मूल्यांकन किया जाय, तो उनके समकालीन अनेक स्थापित रचनाकार बौने साबित हो जायें तो आश्चर्य नहीं। दरअसल उनके जीवन में जान-बूझकर, पूरी ताकत के साथ उनको उपेक्षित करने का षड़यंत्र रचा गया।
यह सारी बातें खुलासा करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हिन्दी में विचारधारायें थोपना, 'वाद' चलाने, बढ़िया से बढ़िया साहित्यकार को गुमनामी के अन्धेरे में डालने, छोटा-बड़ा बनाने का कार्य कोई नया नहीं है। यह तो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के समय से शुरू हो गया था।
मेरा स्पष्ट मत है कि 'वाद' साहित्य की मारक क्षमता को कम करता है। अच्छे रचनाकार को भी अन्धेरे में धकेल देता है। साहित्य अच्छा-बुरा, कमजोर, सतही, उत्कृष्ट, पठनीय आदि तो हो सकता है, 'वाद' नहीं। अगर 'वाद' है तो वो साहित्य नहीं। पूछा जा सकता है कि किसी के भी लेखन की प्रासंगिकता या गैर प्रासंगिकता का फतवा देने वाले आप कौन हैं भाई? आप सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान् तो हैं नहीं - फिर आप फतवा देने वाले कौन हैं? अगर हैं तो आपकी रचनाओं की पठनीयता कितनी है? प्रेमचन्द्र को प्रासंगिक बताने वाले आप कौन और क्या हैं? अगर हैं तो आप प्रेमचंद को छोड़िये, उनके पासंग भी बनकर दिखाइये।
मैं 'वाद के खिलाफ सिर्फ इस कारण हूँ कि वर्तमान में हिन्दी साहित्य की पठनीयता को समाप्त करने, पाठक वर्ग को साहित्य से दूर करने, पुस्तकों की बिक्री कम करवाने, साहित्य के नाम पर गुरूडम फैलाने, दस रुपये की एक काफी पीकर सर्वहारा वर्ग की बात करने, एयरकंडीशन रूम में बैठकर आम आदमी के दुःख दर्द की बातें करने, पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिये गोटें बिठाने वाले ये साहित्यिक 'वादी' हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के लिये ऐसे सांप-बिच्छू और दीमक हैं, जिनसे अभी तक हिन्दी साहित्य को हानि ही हुई है। तुलनात्मक रूप से बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि भाषाओं का साहित्य फल-फूल रहा है। हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ अकारण मरती जा रही हैं जबकि अन्य भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बढ़ी है।
वास्तव में हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। 'वाद' कुछेक के लिये तो लाभप्रद हो सकता है लेकिन वे कुछेक ही हिन्दी साहित्य नहीं हैं। हमें अपनी सोचें, अपनी दृष्टि, अपनी मानसिकता, अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी। मैंने 'वाद' के प्रति अपनी खिलाफत का इजहार इसलिये किया है कि तीस-पैंतीस साल के रचनाकाल में काफी उतार-चढ़ाव देखा है, निष्कर्ष निकाले हैं और परिणाम सामने है। अन्तत: निष्कर्ष गलत भी नहीं हैं।
- चन्द्रेश गुप्त
स्वतंत्रता दिवस • 15 अगस्त, 2000
66/170, दानाखोरी
कानपुर - 208 001
|
|||||