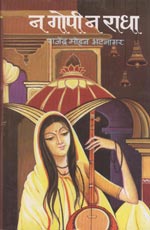|
जीवन कथाएँ >> न गोपी न राधा न गोपी न राधाराजेन्द्र मोहन भटनागर
|
84 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत पुस्तक में मीराबाई के जीवन पर प्रकाश डाला गया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
समर्पण सुरभि
यह क्यों संभव हुआ कि मैंने मीरा पर ‘पयस्विनी मीरा’,
‘जोगिन’, ‘श्यामप्रिया’,
‘प्रेम
दीवानी’ (उपन्यास) और ‘मीरा’ (नाटक) लिख
पाने के बाद भी
यह अनुभव किया कि अभी मीरा पर और अधिक लिखा जा सकता है ? मैंने मीरा पर
स्वलिखित प्रत्येक कृति को एक दूसरे से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है।
बहुत दिनों से यह इच्छा जोर पकड़ रही थी कि भक्ति के अनन्य भाव को मीरा के
माध्यम से प्रकट करूँ। एक भक्त की सामाजिक धार्मिकता को केंद्रबिंदु बनाकर
मीरा के संपूर्ण समर्पण की उदात्त मानसिकता की भागीरथी को आज के मतिभ्रमित
जनमानस को सौंप दूँ।
मीरा-मन मयूर बन नाच उठे, कोयल बन गा उठे और अनिंद्य रूप बन आलोकित हो उठे जगत् के मानस-मंदिर में। आज का अधार्मिक जन धर्म ध्वजाओं के अहं से अपने को मुक्त कर सहज अनाहत के सहचारी भाव में आलुप्त हो सके।
मैं वृंदावन गया, वहाँ रहा। उदयपुर चित्तौड़ में रमता रहा और फिर द्वारका में जा बैठा मीरा का अनुभवभूमि के अंतःस्पर्श के लिए। इन लीलास्थिलियों में लीलामय को ढूँढ़ता रहा मीरा के माध्य से। मीरा मिली। उसने बातचीत की। गीत गाए। नाची। उसमें आकर सारे भेद तिरोहित, सारे विरोधाभास शांत, समस्त वैभव संपन्नता की चकाचौंध का जादू अदृश्य हो गया। शेष-अशेष कुछ नहीं रहा।
वह मीरा नहीं, श्याम हो गई थी और उसने श्यामभाव को मीरा बन जिया था अनंत अक्षय आनंद के साथ। उसकी पीड़ा ही आनंद थी, सत्य थी और सुंदर थी।
मीरा ने श्याम को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते अपने को ही विस्मृत कर दिया था। वह कृष्ण ही हो गई थी। फिर उसे किससे शर्म लाज और किसका भय-आतंक सर्वेश्वर को जी लेने के बाद सांसारिक इयत्ताओं, भौतिक मिथकों और धार्मिक संकीर्णताओं का उसके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। वह तब साकार को निराकार में जी रहा होता है। निराकार में बाधा व्यथा कहाँ ? फिर वह सबसे प्रकट हो रहा होता है। बूँद का नदी बन जाना और नदी में गंगा-यमुना बन जाना हर बूँद से तभी संभव है, जब वह अपने में नदी के अनुभव से ओत-प्रोत हो।
कभी विचार आया कि अकेले में शिशु किसको लखकर मुसकान से भर उठता है ? अपनी नन्हीं-नन्हीं बाँहें नचा-नचाकर किसको रिझाता है और अपनी बड़ी-बड़ी अँखियन में वह किसको रचा-बसा लेता है ? क्यों वह किलकारी मारने लगता है ? क्यों तरह-तरह की कलोल कर उठता है और क्यों आनंद से सावन बन झूम उठता है ? तब क्या वह अपनी भक्ति को कृष्ण लला को अर्पित कर रहा होता है ? उसके साथ क्रीड़ा कर रहा होता है और स्वयं मोरपंखी जसोदा का प्यारा लाड़ला बन इठला रहा होता है ? जैसे-जैसे वह उसमें दूर होता जाता है वैसे-ही-वैसे उसका अक्षय आनंद, अमिट मुसकान अमर आकर्षण और कृष्णभाव लुप्त होता चला जाता है। वह मात्र आकार रह जाता है प्राणसत्ता के अभाव में। मीरा प्रारंभ से कृष्णा रही; गृहस्थिन होकर भी कृष्णा ही बनी रही और प्रौढ़ा होकर भी कृष्णा ही बनी रही। अंततोगत्वा वह कृष्णा ही रही और फिर स्वयं ही कृष्ण हो गई। कृष्ण रंग में रँगकर सदा के लिए रसराज में समा गई।
भक्ति शिशु है। शिशु को हर अवस्था में अपने में बनाए रखना ही भक्ति साधना है और अंत की अक्षय अनुभूति है। उस अनुभूति के बाद अनुभूति जगत् की वह स्वयं स्थायी अनुभूति बन जाती है। तब सुमन नहीं, उसका रंग नहीं, उसका आकार-आकर्षण नहीं और उसका रूप सौंदर्य नहीं होता; होता है उसका गंध-माधुर्य, जो चारों ओर उड़ा-उड़ा घूमता है सावन के सघन मेघ-सा झूमता-झुमाता नाचता-गाता, मोद मनाता हुआ।
मैं वृंदावन में रहा। व्रज की लीला गलियों में घूमा। रसेश्वर के रसराज में डूबा। कल-कल करती यमुना नदी के किनारे, गहरी चाँदनी चंदन निशीथ में अकेले बैठा हुआ प्राण प्यारे, बाँके बिहारी यशोदा लला और नवनीतप्रिय की मुरली सुनता रहा आँख बंद किए। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, तब मैं कहाँ था और क्यों झूम रहा था। कोटिशः बार मैंने उस पावन लीलाभूमि की मधुशाला बन जाना चाहा, करील के कुंजों पर पक्षी बन चहक जाना चाहा और यमुना बन बह लेना चाहा; परंतु वह पूर्णतया संभव नहीं हुआ। हाँ, उसके गंध-रूप की जितनी अनुभुति पा सका, उसे अवश्य अपने पाठकों में बाँटने का प्रयत्न करता रहा।
मीरा तो मीरा नहीं रही थी, अंततः वही बन गई थी जो वह स्वयं था। पूजा-प्रार्थना ही जब आराध्य बन जाए तब क्या बचता है द्वैत के लिए, पूजा के लिए, आराधना के और कर्म-अकर्म के लिए!
इस बार मेरा यही प्रयत्न रहा है। आकार से बाहर आकर निराकार जगत् में प्रवेश करने से पूर्व की अनंत मीरा-अनुभूतियों में से कुछ अनुभूतियों से अपने पाठकों को जोड़ सकूँ, ताकि उनका तन भीग उठे, उनका मन रीझ उठे और उनका तन-मन एकाकार हो सके। भिद्य कुछ नहीं रहे, सब अभिद्य हो जाए। मीराभाव यही तो था, जिसे कबीर ने यों कहा है-
मीरा-मन मयूर बन नाच उठे, कोयल बन गा उठे और अनिंद्य रूप बन आलोकित हो उठे जगत् के मानस-मंदिर में। आज का अधार्मिक जन धर्म ध्वजाओं के अहं से अपने को मुक्त कर सहज अनाहत के सहचारी भाव में आलुप्त हो सके।
मैं वृंदावन गया, वहाँ रहा। उदयपुर चित्तौड़ में रमता रहा और फिर द्वारका में जा बैठा मीरा का अनुभवभूमि के अंतःस्पर्श के लिए। इन लीलास्थिलियों में लीलामय को ढूँढ़ता रहा मीरा के माध्य से। मीरा मिली। उसने बातचीत की। गीत गाए। नाची। उसमें आकर सारे भेद तिरोहित, सारे विरोधाभास शांत, समस्त वैभव संपन्नता की चकाचौंध का जादू अदृश्य हो गया। शेष-अशेष कुछ नहीं रहा।
वह मीरा नहीं, श्याम हो गई थी और उसने श्यामभाव को मीरा बन जिया था अनंत अक्षय आनंद के साथ। उसकी पीड़ा ही आनंद थी, सत्य थी और सुंदर थी।
मीरा ने श्याम को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते अपने को ही विस्मृत कर दिया था। वह कृष्ण ही हो गई थी। फिर उसे किससे शर्म लाज और किसका भय-आतंक सर्वेश्वर को जी लेने के बाद सांसारिक इयत्ताओं, भौतिक मिथकों और धार्मिक संकीर्णताओं का उसके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। वह तब साकार को निराकार में जी रहा होता है। निराकार में बाधा व्यथा कहाँ ? फिर वह सबसे प्रकट हो रहा होता है। बूँद का नदी बन जाना और नदी में गंगा-यमुना बन जाना हर बूँद से तभी संभव है, जब वह अपने में नदी के अनुभव से ओत-प्रोत हो।
कभी विचार आया कि अकेले में शिशु किसको लखकर मुसकान से भर उठता है ? अपनी नन्हीं-नन्हीं बाँहें नचा-नचाकर किसको रिझाता है और अपनी बड़ी-बड़ी अँखियन में वह किसको रचा-बसा लेता है ? क्यों वह किलकारी मारने लगता है ? क्यों तरह-तरह की कलोल कर उठता है और क्यों आनंद से सावन बन झूम उठता है ? तब क्या वह अपनी भक्ति को कृष्ण लला को अर्पित कर रहा होता है ? उसके साथ क्रीड़ा कर रहा होता है और स्वयं मोरपंखी जसोदा का प्यारा लाड़ला बन इठला रहा होता है ? जैसे-जैसे वह उसमें दूर होता जाता है वैसे-ही-वैसे उसका अक्षय आनंद, अमिट मुसकान अमर आकर्षण और कृष्णभाव लुप्त होता चला जाता है। वह मात्र आकार रह जाता है प्राणसत्ता के अभाव में। मीरा प्रारंभ से कृष्णा रही; गृहस्थिन होकर भी कृष्णा ही बनी रही और प्रौढ़ा होकर भी कृष्णा ही बनी रही। अंततोगत्वा वह कृष्णा ही रही और फिर स्वयं ही कृष्ण हो गई। कृष्ण रंग में रँगकर सदा के लिए रसराज में समा गई।
भक्ति शिशु है। शिशु को हर अवस्था में अपने में बनाए रखना ही भक्ति साधना है और अंत की अक्षय अनुभूति है। उस अनुभूति के बाद अनुभूति जगत् की वह स्वयं स्थायी अनुभूति बन जाती है। तब सुमन नहीं, उसका रंग नहीं, उसका आकार-आकर्षण नहीं और उसका रूप सौंदर्य नहीं होता; होता है उसका गंध-माधुर्य, जो चारों ओर उड़ा-उड़ा घूमता है सावन के सघन मेघ-सा झूमता-झुमाता नाचता-गाता, मोद मनाता हुआ।
मैं वृंदावन में रहा। व्रज की लीला गलियों में घूमा। रसेश्वर के रसराज में डूबा। कल-कल करती यमुना नदी के किनारे, गहरी चाँदनी चंदन निशीथ में अकेले बैठा हुआ प्राण प्यारे, बाँके बिहारी यशोदा लला और नवनीतप्रिय की मुरली सुनता रहा आँख बंद किए। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, तब मैं कहाँ था और क्यों झूम रहा था। कोटिशः बार मैंने उस पावन लीलाभूमि की मधुशाला बन जाना चाहा, करील के कुंजों पर पक्षी बन चहक जाना चाहा और यमुना बन बह लेना चाहा; परंतु वह पूर्णतया संभव नहीं हुआ। हाँ, उसके गंध-रूप की जितनी अनुभुति पा सका, उसे अवश्य अपने पाठकों में बाँटने का प्रयत्न करता रहा।
मीरा तो मीरा नहीं रही थी, अंततः वही बन गई थी जो वह स्वयं था। पूजा-प्रार्थना ही जब आराध्य बन जाए तब क्या बचता है द्वैत के लिए, पूजा के लिए, आराधना के और कर्म-अकर्म के लिए!
इस बार मेरा यही प्रयत्न रहा है। आकार से बाहर आकर निराकार जगत् में प्रवेश करने से पूर्व की अनंत मीरा-अनुभूतियों में से कुछ अनुभूतियों से अपने पाठकों को जोड़ सकूँ, ताकि उनका तन भीग उठे, उनका मन रीझ उठे और उनका तन-मन एकाकार हो सके। भिद्य कुछ नहीं रहे, सब अभिद्य हो जाए। मीराभाव यही तो था, जिसे कबीर ने यों कहा है-
लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।।
लीलामय होकर फिर व्यक्ति संसारी नहीं रह सकता और लीलामयी अनुभूतियों की
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त उसके पास कुछ शेष भी नहीं बचता। यथार्थतः वह
निःशेष को जीता है और उसी का होकर रह जाता है। मीराभाव का संपूर्ण समर्पण
यही तो है कि वह आकार न रहकर स्वयं में लीलामय भाव बन गई। इस संस्थिति की
कल्पना करना भी अति कठिन है। फिर उसको लिपिबद्ध करना तो और भी कठिन व
दुर्लभ कार्य है। मीरा ने जो गाया वह लीलामय भाव, संबंध सहचरी अनुराग और
अनुतप्त वैरागी संचारीभाव उनकी संपूर्णता का ही प्रतीक है, जिसे मुझे
प्रस्तुत करना है मीरामय होकर। पहले जोगी होइए, जोगी रस में डूबिए और फिर
जोगिन को अपने में जी जाइए, तब मीराभाव मुखर होगा-मीरा होकर मीरामय जगत्
के लिए समग्र समर्पण के माध्यम से।
समग्र समर्पण के साथ अनेक सूर्य आलोक के सामने आकर, उसे आत्मसात् कर अपने से प्रकट करने का प्रयत्न अति दुर्लभ है। यथार्थतः वह प्रयत्न से नहीं, लीलामयी की कृपा से ही संभव है। पूजा के नितांत एकांत क्षणों में जब मौन भी निस्तब्ध होकर आत्मलीन हो जाता है तब हृदय के भाव जगत् में कृष्णानुराग भर उठता है। वह इंद्रधनुष बनाता है और रिमझिम अमृत बरसाता है। वही मीराभाव है। मुझे उसी भाव ने इस बार मीरा-हृदय के कपाट खोलने का आदेश दिया है। इस कृति के जन्म के पीछे वही अमृत निर्झर प्रेरणा संसार बना है। वह सदा ही विद्यमान है। गत और अनागत में नहीं। वर्तमान ही जिसका गत है और वर्तमान ही जिसका अनागत। उसमें कोई द्वैत नहीं भेद नहीं और काल का अंतराल नहीं : क्योंकि वही अद्वैत है, अभिद्य है और महाकाल है-मृत्युंजयी से आगे आदि, अनादि और अनंत-ही-अनंत है, अजन्मा है वह, निरापद है और निराकांक्षित है।
इस कृति के साथ मेरी यह यात्रा, जो पाँच वर्षों से अनवरत चल रही है, कभी रुकी थमी नहीं, सदा प्रवाहमयी बनी हुई है। यह कृति उसी का प्रतिफल है। उन क्षणों के अंतर्गत बहते हुए अनुक्षणों का संवाद है। अपने पाठकों को भी उस ओर ले चलने के लिए निमंत्रण भाव से अभिभूत कर यह कृति कुछ समय के लिए मीरामय हो जाने के मधुरोल्लासमय उमंगित महोत्सव की अनुभूति कराना चाहती है।
वह जो जगत का कार्य-कारण है, सूत्रधार व स्रष्टा है; जिसे मीरा ने भजा है और जिसमें वह अंतर्लीन हुई है, उसी मीरा को यहाँ मैंने भजने का प्रयास, किया है-इसी कृति में। कुछ नहीं कह सकता हूँ-और न कुछ कहने का मेरा मन ही है, सिवाय उन अनंत आनंदानुभूतियों के, जिनको मैंने इसको लिखते समय अनुभव किया है।
अंततः प्रो. भगवती लाल व्यास का मैं हृदय से आभारी हूँ, जो उस कृति के पहले भक्त पाठक व समीक्षक रहे हैं और जिन्होंने इस कृति के प्रति अपना अपार स्नेह व आदर प्रकट किया है।
अस्तु,
समग्र समर्पण के साथ अनेक सूर्य आलोक के सामने आकर, उसे आत्मसात् कर अपने से प्रकट करने का प्रयत्न अति दुर्लभ है। यथार्थतः वह प्रयत्न से नहीं, लीलामयी की कृपा से ही संभव है। पूजा के नितांत एकांत क्षणों में जब मौन भी निस्तब्ध होकर आत्मलीन हो जाता है तब हृदय के भाव जगत् में कृष्णानुराग भर उठता है। वह इंद्रधनुष बनाता है और रिमझिम अमृत बरसाता है। वही मीराभाव है। मुझे उसी भाव ने इस बार मीरा-हृदय के कपाट खोलने का आदेश दिया है। इस कृति के जन्म के पीछे वही अमृत निर्झर प्रेरणा संसार बना है। वह सदा ही विद्यमान है। गत और अनागत में नहीं। वर्तमान ही जिसका गत है और वर्तमान ही जिसका अनागत। उसमें कोई द्वैत नहीं भेद नहीं और काल का अंतराल नहीं : क्योंकि वही अद्वैत है, अभिद्य है और महाकाल है-मृत्युंजयी से आगे आदि, अनादि और अनंत-ही-अनंत है, अजन्मा है वह, निरापद है और निराकांक्षित है।
इस कृति के साथ मेरी यह यात्रा, जो पाँच वर्षों से अनवरत चल रही है, कभी रुकी थमी नहीं, सदा प्रवाहमयी बनी हुई है। यह कृति उसी का प्रतिफल है। उन क्षणों के अंतर्गत बहते हुए अनुक्षणों का संवाद है। अपने पाठकों को भी उस ओर ले चलने के लिए निमंत्रण भाव से अभिभूत कर यह कृति कुछ समय के लिए मीरामय हो जाने के मधुरोल्लासमय उमंगित महोत्सव की अनुभूति कराना चाहती है।
वह जो जगत का कार्य-कारण है, सूत्रधार व स्रष्टा है; जिसे मीरा ने भजा है और जिसमें वह अंतर्लीन हुई है, उसी मीरा को यहाँ मैंने भजने का प्रयास, किया है-इसी कृति में। कुछ नहीं कह सकता हूँ-और न कुछ कहने का मेरा मन ही है, सिवाय उन अनंत आनंदानुभूतियों के, जिनको मैंने इसको लिखते समय अनुभव किया है।
अंततः प्रो. भगवती लाल व्यास का मैं हृदय से आभारी हूँ, जो उस कृति के पहले भक्त पाठक व समीक्षक रहे हैं और जिन्होंने इस कृति के प्रति अपना अपार स्नेह व आदर प्रकट किया है।
अस्तु,
राजेंद्र मोहन भटनागर
एक
‘‘माता, वृदावन आने वाला है।’’
गाड़ीवान ने सहजभाव से कहा।
लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। गाड़ी चलती रही। बैलों के गले में बँधी घंटियाँ बजती रहीं। गाड़ी की गति से लग रहा था कि सुघड़ गैल पाकर बैल उत्साही मन से भागने लगे हैं, मानो उनका मन भी वृंदावन की गंधरज पाकर वृंदावनी हो उठा हो।
मीरा में ललक थी गहरी रची-पची। सारी रात वह सो नहीं पाई। नाम स्मरण करती रही कान्हा का और अनुभव करती रही लीलाधर की लीलाभूमि की रस किंवदंतियों का। उसके सामने करील के कुंज, निर्मल यमुना का तीर, चंदनमयी रज और बाल गोपाल कृष्ण मोर मुकुट पहने, हृदय-पटल पर बैजंती माला सुशोभित किए, ग्वालबालों के बीचोबीच आ खड़े हुए। ऐसी अनेक दृश्यावलियों को वह अपने सामने से गुजरते देखती रही ललचाई मधुर आँखों से। उसकी श्वास-श्वास में नवनीतप्रिय का वृंदावनी मधुमास फाग खेल उठा।
‘‘माता, आज आप रात भर नहीं सोईं।’’
‘‘तू सोया क्या ?’’
‘‘नहीं।’’
‘‘ये बलराम सोए क्या ?’’
‘‘नहीं।’’
‘‘फिर मैं कैसे सोती, धूपद !’’ मीरा में चाह की लाली पौ जैसी फैलने लगी हौले हौले और उसका अनुरागी मन सहस्रों नयन बन निहारने लगा वृंदावनी रज-उमंग को। उसके रंध्र-रंध्र में कृष्ण सुवास उत्सवी हो उठा।
गाड़ीवान धूपद स्वेच्छा से वृंदावन आया था कृष्ण-रज माथे पर लगाने और उसे हृदय में बसाने के लिए प्रफुल्ल मन से अति उत्साही होकर। वह मीरा के पद सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया था। ललिता को हलका सा ज्वर था। रात भर ‘कृष्ण’ नाम का जाप करते हुए उसने अपने मन को कृष्णमय रंग में रँग लिया था। मुँह अँधेरे, शीतल मलयानिल के झोंके खाकर उसके तंद्रिल नेत्र मुँद गए थे।
छन...छन-...छन, चक्की की गर्र-गर्र-गर्र, पनघट पर हँसी ठट्टा बैलों की घंटियाँ पायल की रुनझुन आदि ध्वनियाँ मंगलाचरण पढ़ रही थीं महाकाव्यमयी यात्रा के संदर्भ पर्यावरण में।
मीरा देख रही थी नीलांबर में शांतभाव से स्थित ध्रुव तारे को अचल मन से अपलक दृष्टि से। प्रकृति की रूप-छटा के विषय परिवर्तन प्रवर्तन को वह आत्मसात् कर रही थी कि तभी उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ा-‘जय राधे, जय गोविंद ! जय गोविंद हरे-हरे ! जय गोपाल, जय कन्हैया !’
कुछ देर बीत जाने पर एक जोर की आवाज में स्वर तरंगें थिरक उठीं-‘जय माखन चुरैया की ! जय कृष्ण कन्हैया की ! जय राधा रानी की ! जय गिरिधर गोपाल की !’
मीरा ने मन ही मन कृष्ण कन्हैया को नमन किया।
वह गाड़ीवान से बोली, ‘‘तनिक गाड़ी को रोको।’’
गाड़ीवान धूपद ने रास खींची। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। मीरा नीचे उतरी। सबसे पहले उसने वहाँ की माटी को उठाया, माथे से लगाया बारंबार नमन करते हुए कहा, ‘‘ए साँवरिया, नटनागर ! मैं तिहारी नगरी में आई हूँ तिहारे से मिलने। मिलोगे तो, प्रभु ! माखन चुराते हुए, मटकियाँ फोड़ते हुए, गैयाँ चराते हुए, मुरली बजाते हुए। बोलो मेरे गिरिधर गोपाल, क्या सोच में पड़ गए ? जनम-जनम की तुम्हारी दासी, लोक-लाज छोड़कर तुम्हारे पास आई है। जवाब दो या न दो, पर मेरी प्रतिज्ञा कान खोलकर सुन लो-मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। बिना मिले कदापि नहीं लौटूँगी। देखती हूँ, अब किसकी आन रहती है।’’
धूपद का मन गुलगुली मचाकर जाती हुई बयार से गद्गद हो उठा था। वह बोला, ‘‘माता, यहाँ की सुबह कितनी सुंदर है !’’
‘‘हाँ रे, यहां की भोर प्रतिदिन कान्हा से मिलने आती है, तब कहीं और जाती है।’’
‘‘सच, माता ?’’
‘‘झूठ कुछ नहीं होता रे ! जो होता है, वह सच होता है।’’ मीरा ने सहजभाव से समझाया।
‘‘फिर ‘झूठ मत बोलो’ क्यों कहा जाता है, माता ?’’ धूपद ने सहज जिज्ञासा प्रकट कर दी।
‘‘जो है, जब उसे छिपाया जाता है और जो नहीं है, उसे जताया जाता है तब वह झूठ होता है। हमें झूठ नहीं जानना। जिस गैल नहीं जाना, उसके बारे में कैसी पूछताछ ? उसके बारे में जिज्ञासा क्यों ? बोल रे, क्या समझा ?’’ मीरा ने उसे चेता दिया।
‘‘समझ गया, माता, उसके बारे में सोचना बंद। प्रश्न बंद।’’ धूपद ने धीरे से कहा।
मीरा कबूतरों की टोलियों को घेरा बनकर आकाश में जाते हुए अवलोकती रही। पेड़ों पर चिड़ियाँ चीं-चीं करने लगीं। कहीं से कोयल बोली, मोर बोला और गाय-भैंसे-रँभाने लगीं।
मीरा का मन गद्गद हो उठा था। उसके रोम-रोम में नंद के लला की माधुरी मूरत समा उठी थी। वह बोली, ‘‘यहाँ से हम पैदल चलेंगे, धूपद।’’
‘‘क्यों, माता ?’’
‘‘क्योंकि अब हम वृंदावन में आ चुके हैं। लीलाधारी कान्हा की क्रीड़ाभूमि की माटी का भरपूर आनंद लेंगे। आज भी इस माटी में बाँके बिहारी की सुगंध है। तभी तो यहाँ की भूमि चंदन-गुलाब है।’’ मीरा कहीं गहरे में डूबी बोले जा रही थी धीरे-धीरे अमृत रस घोलती हुई और मन ही मन उसकी भव्य छटा को नमन करती हुई। जाने कब से वृंदावन बँहियाँ उठा-उठाकर उसे बुला रहा था। जाने कब से वह स्वप्न में टेर रहा था। जाने कब से अपनी अलौकिक रूप छटा को दिखलाकर मन बाँध रहा था।
अब वह वृंदावन में है। उस वृंदावन में, जिसकी तृष्णा उसे बहुत दिनों से सता रही थी। क्या होगा कान्हा का वृंदावन ? क्या होगा गिरिधर का व्रज ? कैसा लगेगा अनुपम, अद्वितीय उसका हर पल और हर पल का हर अनुपल ? उसको यह सोच चैन नहीं लेने देता था। इतना उतावलापन ! इतना बालपन ! इतना भक्ति-समर्पण ! इतनी पूजा अर्चना ! ओह !
ठाकुर के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करती करती वह स्वयं प्रार्थना बन जाती थी-‘‘जा रे ठाकुर, तू बड़ा कठोर है, पत्थरदिल है ! ललचाता है, सैन बताता है, लुभाता है और अवसर आने पर लुका छिपी का खेल खेलने लगता है। बुलाता क्यों रहता है रे ? ले क्यों नहीं चलता ? अपना मानता भी है, पर अपनाने के बखत भाग खड़ा होता है रे, मेरे रनछोर मुकुंद। क्या-क्या कहूँ तुझसे ! कब तक कहती हूँ !’’
बाँके बिहारी ने उसकी सुन ली। धूपद मिल गया। अकेला। खेत-खलिहान, घर-जायदाद सब। पर कहीं मन नहीं। शादी हुई, नहीं के बराबर। डेढ़ बरस में जवान पत्नी की इहलीला समाप्त। तब से वैरागी। निठल्ला मन आता, गाता और मन आता, कहीं बिना किसी को बताए चला जाता। कुछ अता-पता नहीं चलता। अचानक लौट आता। किसी को कुछ नहीं बताता। पहली बात तो यह बोलता ही नहीं, गूँगा हो जाता है।
कैसा मलूक ! हट्टा-कट्टा साढ़े पाँच फीट का जवान। गोरा रंग। गठी देह। नाक नक्श सुघड़ लंबी बाँहें। होंठ पतले और लाल सुर्ख।
मीरा को उस गाँव में रुक जाना पड़ा। राजघराने की लाडली बहू। लोक-लाज तजकर संन्यासिनी बनी। महल छोड़ा। कँटीले रास्तों पर निकल पड़ी वह अकेली, साधु-संतों की मुँहबोली।
उसको देखने गाँव-गाँव की भीड़ उमड़ पड़ती। सब उसे रोकना चाहते। कहीं रुक जाती, कहीं नहीं वह अपने में नहीं होती। न रुकना होता तो वह कहती, रुकना बन नहीं रहा है, पुरजनो ! मेरे अपने से कैसा रुकना और कैसा चलना। वह तो किसन कन्हैया, मोरपंखी मुकुटधारी से है। वो रोके, रुक जाऊँ। वो चलने का सैन करे, चल पड़ूँ। अब वो बुला रहा है, न चलूँगी तो नाराज हो बैठेगा। सो जाना है। क्षमा करना। मैं आपके मान-मनुहार को मानना चाहकर भी नहीं मान सकती।’’
मीरा चलने को हुई तो उस गाड़ी के एक बैल को कुछ हो गया। वह कंधे डाल गया। मीरा को रुकना पड़ा। वह बीमार बैल को छोड़कर कैसे आगे बढ़ती। उस बैल के मन में भी तो रास रचैया बैठा हुआ था।
रात उगी। चौपाल जुड़ी। सारा गाँव आ बैठा। वहाँ धूपद भी था। वह हाथ जोड़कर बोला, ‘‘माता, आज्ञा हो तो हम भी कुछ सुनाएँ।’’
सबकी दृष्टि धूपद पर ठहर गई पल भर के लिए।
‘‘सुनाओ, भाई !’’
धूपद कुछ देर तक सोचने के बाद धीरे धीरे गा उठा-
लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। गाड़ी चलती रही। बैलों के गले में बँधी घंटियाँ बजती रहीं। गाड़ी की गति से लग रहा था कि सुघड़ गैल पाकर बैल उत्साही मन से भागने लगे हैं, मानो उनका मन भी वृंदावन की गंधरज पाकर वृंदावनी हो उठा हो।
मीरा में ललक थी गहरी रची-पची। सारी रात वह सो नहीं पाई। नाम स्मरण करती रही कान्हा का और अनुभव करती रही लीलाधर की लीलाभूमि की रस किंवदंतियों का। उसके सामने करील के कुंज, निर्मल यमुना का तीर, चंदनमयी रज और बाल गोपाल कृष्ण मोर मुकुट पहने, हृदय-पटल पर बैजंती माला सुशोभित किए, ग्वालबालों के बीचोबीच आ खड़े हुए। ऐसी अनेक दृश्यावलियों को वह अपने सामने से गुजरते देखती रही ललचाई मधुर आँखों से। उसकी श्वास-श्वास में नवनीतप्रिय का वृंदावनी मधुमास फाग खेल उठा।
‘‘माता, आज आप रात भर नहीं सोईं।’’
‘‘तू सोया क्या ?’’
‘‘नहीं।’’
‘‘ये बलराम सोए क्या ?’’
‘‘नहीं।’’
‘‘फिर मैं कैसे सोती, धूपद !’’ मीरा में चाह की लाली पौ जैसी फैलने लगी हौले हौले और उसका अनुरागी मन सहस्रों नयन बन निहारने लगा वृंदावनी रज-उमंग को। उसके रंध्र-रंध्र में कृष्ण सुवास उत्सवी हो उठा।
गाड़ीवान धूपद स्वेच्छा से वृंदावन आया था कृष्ण-रज माथे पर लगाने और उसे हृदय में बसाने के लिए प्रफुल्ल मन से अति उत्साही होकर। वह मीरा के पद सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया था। ललिता को हलका सा ज्वर था। रात भर ‘कृष्ण’ नाम का जाप करते हुए उसने अपने मन को कृष्णमय रंग में रँग लिया था। मुँह अँधेरे, शीतल मलयानिल के झोंके खाकर उसके तंद्रिल नेत्र मुँद गए थे।
छन...छन-...छन, चक्की की गर्र-गर्र-गर्र, पनघट पर हँसी ठट्टा बैलों की घंटियाँ पायल की रुनझुन आदि ध्वनियाँ मंगलाचरण पढ़ रही थीं महाकाव्यमयी यात्रा के संदर्भ पर्यावरण में।
मीरा देख रही थी नीलांबर में शांतभाव से स्थित ध्रुव तारे को अचल मन से अपलक दृष्टि से। प्रकृति की रूप-छटा के विषय परिवर्तन प्रवर्तन को वह आत्मसात् कर रही थी कि तभी उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ा-‘जय राधे, जय गोविंद ! जय गोविंद हरे-हरे ! जय गोपाल, जय कन्हैया !’
कुछ देर बीत जाने पर एक जोर की आवाज में स्वर तरंगें थिरक उठीं-‘जय माखन चुरैया की ! जय कृष्ण कन्हैया की ! जय राधा रानी की ! जय गिरिधर गोपाल की !’
मीरा ने मन ही मन कृष्ण कन्हैया को नमन किया।
वह गाड़ीवान से बोली, ‘‘तनिक गाड़ी को रोको।’’
गाड़ीवान धूपद ने रास खींची। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। मीरा नीचे उतरी। सबसे पहले उसने वहाँ की माटी को उठाया, माथे से लगाया बारंबार नमन करते हुए कहा, ‘‘ए साँवरिया, नटनागर ! मैं तिहारी नगरी में आई हूँ तिहारे से मिलने। मिलोगे तो, प्रभु ! माखन चुराते हुए, मटकियाँ फोड़ते हुए, गैयाँ चराते हुए, मुरली बजाते हुए। बोलो मेरे गिरिधर गोपाल, क्या सोच में पड़ गए ? जनम-जनम की तुम्हारी दासी, लोक-लाज छोड़कर तुम्हारे पास आई है। जवाब दो या न दो, पर मेरी प्रतिज्ञा कान खोलकर सुन लो-मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। बिना मिले कदापि नहीं लौटूँगी। देखती हूँ, अब किसकी आन रहती है।’’
धूपद का मन गुलगुली मचाकर जाती हुई बयार से गद्गद हो उठा था। वह बोला, ‘‘माता, यहाँ की सुबह कितनी सुंदर है !’’
‘‘हाँ रे, यहां की भोर प्रतिदिन कान्हा से मिलने आती है, तब कहीं और जाती है।’’
‘‘सच, माता ?’’
‘‘झूठ कुछ नहीं होता रे ! जो होता है, वह सच होता है।’’ मीरा ने सहजभाव से समझाया।
‘‘फिर ‘झूठ मत बोलो’ क्यों कहा जाता है, माता ?’’ धूपद ने सहज जिज्ञासा प्रकट कर दी।
‘‘जो है, जब उसे छिपाया जाता है और जो नहीं है, उसे जताया जाता है तब वह झूठ होता है। हमें झूठ नहीं जानना। जिस गैल नहीं जाना, उसके बारे में कैसी पूछताछ ? उसके बारे में जिज्ञासा क्यों ? बोल रे, क्या समझा ?’’ मीरा ने उसे चेता दिया।
‘‘समझ गया, माता, उसके बारे में सोचना बंद। प्रश्न बंद।’’ धूपद ने धीरे से कहा।
मीरा कबूतरों की टोलियों को घेरा बनकर आकाश में जाते हुए अवलोकती रही। पेड़ों पर चिड़ियाँ चीं-चीं करने लगीं। कहीं से कोयल बोली, मोर बोला और गाय-भैंसे-रँभाने लगीं।
मीरा का मन गद्गद हो उठा था। उसके रोम-रोम में नंद के लला की माधुरी मूरत समा उठी थी। वह बोली, ‘‘यहाँ से हम पैदल चलेंगे, धूपद।’’
‘‘क्यों, माता ?’’
‘‘क्योंकि अब हम वृंदावन में आ चुके हैं। लीलाधारी कान्हा की क्रीड़ाभूमि की माटी का भरपूर आनंद लेंगे। आज भी इस माटी में बाँके बिहारी की सुगंध है। तभी तो यहाँ की भूमि चंदन-गुलाब है।’’ मीरा कहीं गहरे में डूबी बोले जा रही थी धीरे-धीरे अमृत रस घोलती हुई और मन ही मन उसकी भव्य छटा को नमन करती हुई। जाने कब से वृंदावन बँहियाँ उठा-उठाकर उसे बुला रहा था। जाने कब से वह स्वप्न में टेर रहा था। जाने कब से अपनी अलौकिक रूप छटा को दिखलाकर मन बाँध रहा था।
अब वह वृंदावन में है। उस वृंदावन में, जिसकी तृष्णा उसे बहुत दिनों से सता रही थी। क्या होगा कान्हा का वृंदावन ? क्या होगा गिरिधर का व्रज ? कैसा लगेगा अनुपम, अद्वितीय उसका हर पल और हर पल का हर अनुपल ? उसको यह सोच चैन नहीं लेने देता था। इतना उतावलापन ! इतना बालपन ! इतना भक्ति-समर्पण ! इतनी पूजा अर्चना ! ओह !
ठाकुर के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करती करती वह स्वयं प्रार्थना बन जाती थी-‘‘जा रे ठाकुर, तू बड़ा कठोर है, पत्थरदिल है ! ललचाता है, सैन बताता है, लुभाता है और अवसर आने पर लुका छिपी का खेल खेलने लगता है। बुलाता क्यों रहता है रे ? ले क्यों नहीं चलता ? अपना मानता भी है, पर अपनाने के बखत भाग खड़ा होता है रे, मेरे रनछोर मुकुंद। क्या-क्या कहूँ तुझसे ! कब तक कहती हूँ !’’
बाँके बिहारी ने उसकी सुन ली। धूपद मिल गया। अकेला। खेत-खलिहान, घर-जायदाद सब। पर कहीं मन नहीं। शादी हुई, नहीं के बराबर। डेढ़ बरस में जवान पत्नी की इहलीला समाप्त। तब से वैरागी। निठल्ला मन आता, गाता और मन आता, कहीं बिना किसी को बताए चला जाता। कुछ अता-पता नहीं चलता। अचानक लौट आता। किसी को कुछ नहीं बताता। पहली बात तो यह बोलता ही नहीं, गूँगा हो जाता है।
कैसा मलूक ! हट्टा-कट्टा साढ़े पाँच फीट का जवान। गोरा रंग। गठी देह। नाक नक्श सुघड़ लंबी बाँहें। होंठ पतले और लाल सुर्ख।
मीरा को उस गाँव में रुक जाना पड़ा। राजघराने की लाडली बहू। लोक-लाज तजकर संन्यासिनी बनी। महल छोड़ा। कँटीले रास्तों पर निकल पड़ी वह अकेली, साधु-संतों की मुँहबोली।
उसको देखने गाँव-गाँव की भीड़ उमड़ पड़ती। सब उसे रोकना चाहते। कहीं रुक जाती, कहीं नहीं वह अपने में नहीं होती। न रुकना होता तो वह कहती, रुकना बन नहीं रहा है, पुरजनो ! मेरे अपने से कैसा रुकना और कैसा चलना। वह तो किसन कन्हैया, मोरपंखी मुकुटधारी से है। वो रोके, रुक जाऊँ। वो चलने का सैन करे, चल पड़ूँ। अब वो बुला रहा है, न चलूँगी तो नाराज हो बैठेगा। सो जाना है। क्षमा करना। मैं आपके मान-मनुहार को मानना चाहकर भी नहीं मान सकती।’’
मीरा चलने को हुई तो उस गाड़ी के एक बैल को कुछ हो गया। वह कंधे डाल गया। मीरा को रुकना पड़ा। वह बीमार बैल को छोड़कर कैसे आगे बढ़ती। उस बैल के मन में भी तो रास रचैया बैठा हुआ था।
रात उगी। चौपाल जुड़ी। सारा गाँव आ बैठा। वहाँ धूपद भी था। वह हाथ जोड़कर बोला, ‘‘माता, आज्ञा हो तो हम भी कुछ सुनाएँ।’’
सबकी दृष्टि धूपद पर ठहर गई पल भर के लिए।
‘‘सुनाओ, भाई !’’
धूपद कुछ देर तक सोचने के बाद धीरे धीरे गा उठा-
‘‘दुलहनी, गावहुँ मंगलाचार।
हम घरि आए हो राजा राम भरतार।
तन रति करि मैं मन रज करिहुँ, पंच तत बराती।
रामदेव मोरे पाँहुँने आए, मैं जोबन में माती...
हम घरि आए हो राजा राम भरतार।
तन रति करि मैं मन रज करिहुँ, पंच तत बराती।
रामदेव मोरे पाँहुँने आए, मैं जोबन में माती...
धूपद खूब जमा। उसने तल्लीन होकर गाया।
मीरा ने कहा, ‘‘कंठ मधुर है। अच्छा गाते हो।’’
‘‘जी, माता।’’ परंतु तुरंत ही सिर हिलाकर उसने कहा, ‘‘नहीं, माता।’’
इस पर सब हँस पड़े। मीरा मुसकराकर रह गई उस भोले मानुष के सरल चित्त को पढ़कर। कुछ समय अनबोला बीता। स्त्री पुरुष आपस में बतियाते रहे नदी के पानी की तरह।
मीरा ने कहा, ‘‘तुम धूपद हो ?’’
‘‘जी, माता।’’
‘‘तुम्हारा चित्त एक ठौर नहीं टिकता।’’
धूपद सोचता हुआ निरुत्तर रह गया।
‘‘बता सकते हो, ऐसा क्यों होता है ?’’ मीरा ने आगे पूछा।
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘इस ओर सोचते नहीं ?’’
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘फिर भागते क्यों हो ?’’
‘‘पता नहीं, माता।’’
‘‘तुम्हें पता क्या है, धूपद ?’’
‘‘कुछ नहीं, माता।’’
‘‘ऐसे कब तक, भागते रहोगे ?’’
‘‘नहीं मालूम।’’
‘‘भागकर जाते कहाँ हो ?’’
‘‘कहाँ जाऊँ ?’’
‘‘वहाँ चैन मिलता है ?’’
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘तुम जानना चाहते हो ?’’
‘‘क्या माता ?’’
‘‘जो तुम नहीं जानते।’’ मीरा ने गंभीर होकर कहा।
धूपद सोच में पड़ गया। वह क्या नहीं जानता ? उसे क्या जानना है ? क्यों जानना है ? पत्नी नहीं। माता पिता नहीं। चाचा ताऊ कोई नहीं। पत्नी के पक्षवाले उसके साथ अपनी छोटी लड़की को ब्याहना चाहते थे। लेकिन उसने उन्हें दो टूक उत्तर दे दिया-‘ससुरजी, ब्याह बार बार नहीं होता। वह एक बार हो चुका। अपने भाग्य में पत्नी का इतना ही साथ बदा था। अब और ब्याह नहीं।’ उसके बाद से उधर से चुप्पी।
‘‘क्या सोच में पड़ गए, धूपद ?’’ मीरा उसके मन की जन्मपत्री बाँचकर पूछ रही थी। उसे लग रहा था कि वह श्रीकृष्ण सेवा का सच्चा पात्र है। उसका मन शुद्ध है। उसके आचार-विचार में कोई खोट नहीं।
‘‘क्या सोचूँ, माता ! सोचना हम जैसे मूरख से कभी बना नहीं। सोचने को है भी क्या ! काला आखर कभी पढ़ा नहीं। सुना सुनाया भी कुछ नहीं। पत्नी स्वर्ग क्या सिधारी कि जग माटी हो गया। बेकार !’’ धूपद ने याद करते हुए अपनी कहानी के शीर्षक बाँचे और सोचता रह गया कि क्या उसे ऐसे सोचना चाहिए था ?
‘‘तुम कुछ मत सोचो। पर एक ठौर चित्त तो लगाओ। तुमने चित्तचोर का नाम सुना है ?’’
‘‘कौन चित्तचोर ?’’
‘‘वह दूसरों का चित्त चुराता है। तुम उसे नहीं जानते ?’’
धूपद ने सिर हिलाकर कहा, ‘‘नहीं।’’
‘‘अपना मोर मुकुटधारी, बाँके बिहारी, गोवर्धन गिरिधारी।’’
‘‘किसन कन्हैया ?’’
‘‘हाँ वही चित्तचोर है। वह जिसका चित्त चुरा ले वह जगत् की सारी आल-बाल से मुक्त। फिर चैन ही चैन।’’ मीरा ने सहजभाव से धूपद को समझाया। उसके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि धूपद सीधे ही किसन कन्हैया से जुड़ सकता है। एक बार उसके मन में टेढ़े होकर नटनागर ने स्थान बना लिया, फिर वह चाहे लाख प्रयत्न करे, तो भी वह नहीं निकलेगा। पर लगन तो लगे चिनगारी तो उठे।
‘‘उसके क्या कहने ! वह तो जगत् का पालनहार है। सारा जगत् उसी से है। पर वह हमारा चित्त क्यों चुराएगा ?’’ धूपद में सहज प्रश्न बुनावट डालने लगे।
‘‘क्यों नहीं चुराएगा ? वह तो जन्म का चोर है।’’ मीरा ने उसके मन को कुरेदा।
‘‘क्या कहती हैं, माता ! किसन और चोर।’’
‘‘क्यों, किसन चोर क्यों नहीं हो सकता ?’’
‘‘ना बाबा, ना ! कभी नहीं। भगवान् भी क्या कभी चोर हुए हैं ?’’ धूपद इतना कहकर मन ही मन जप करने लगा-‘‘हरे हरे हरे किसन, हरे-हरे !’’
‘‘क्यों नहीं हुए हैं ! माखन चुराया है न ! माखनचोर तभी तो उन्हें कहा जाता है। माखन चुराते हुए रँगे हाथ पकड़े गए तो क्या बोले, जानते हो तुम ?’’ मीरा ने उसके मन में झाँकने का प्रयत्न किया।
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘गोपियाँ जसोदा को लेकर आ गईं। किसन के मुँह पर माखन लगा हुआ था। उनके हाथ माखन से भरे हुए थे। एक गोपी बोली, ‘ये देख लो अपने लला की करतूत। आप तो मानती ही नहीं थी कि....’ इसपर किसन बोला, ‘‘मैया, तू इनकी बातों पर भरोसा न कर। यह सब इनकी ही चालाकी है। इन सबन ने मिलकर मेरे मुँह में माखन लिपटाया। मेरे हाथ में माखन दिया और बोलीं-लला, तू माखन चख। जासे हमारा माखन अमृत बन जाएगा। सो मैया। और अब जे तोहे लिवा लाईं। मेरी भोली मैया, जरा सोचतो-इत्ते ऊँचे छीके पर मेरी बँहियाँ कैसे पहुँच सकती हैं ! जे सब मुझे तेरी साँटी से पिटवाना चाहती हैं। मैया, जे बड़ी चतुर हैं-मुझे फुसलाती हैं और तोहे उकसाती हैं।’ जसोदा बोलीं, ‘जे बात है। निपूतियों, तुम मेरे लला को पिटवाना चाहती हो ! आ मेरे आँखों के तारे मेरे पास आ।’ ऐसा किया था उस किसन कन्हैया, माखन चुरैया ने।’’ मीरा ने सहज ढंग से सारा प्रसंग सुना दिया। धूपद की आँखें खुली की खुली रह गईं। मीरा आगे कह रही थी-‘‘वह चित्तचोर है, जगत् का सिरजनहार। वह चित्त एक बार चुरा ले तो फिर चित्त को भटकने का कोई ठौर ही न रहे। सब झंझट दूर। बोल तू चाहेगा कि वह तेरा चित्त चुराए ?’’
धूपद ने कुछ देर बाद कहा, ‘‘पर वह हमारा चित्त चुराएगा क्यों, माता ? उसे क्या पड़ी कि वह ऐसे वैसों का चित्त चुराए ?’’
‘‘तूने ठीक कहा है, धूपद, वह हर एक का चित्त नहीं चुराता। वह तो चुराने वालों का चित्त चुराता है।’’ मीरा ने समझाया।
मीरा ने कहा, ‘‘कंठ मधुर है। अच्छा गाते हो।’’
‘‘जी, माता।’’ परंतु तुरंत ही सिर हिलाकर उसने कहा, ‘‘नहीं, माता।’’
इस पर सब हँस पड़े। मीरा मुसकराकर रह गई उस भोले मानुष के सरल चित्त को पढ़कर। कुछ समय अनबोला बीता। स्त्री पुरुष आपस में बतियाते रहे नदी के पानी की तरह।
मीरा ने कहा, ‘‘तुम धूपद हो ?’’
‘‘जी, माता।’’
‘‘तुम्हारा चित्त एक ठौर नहीं टिकता।’’
धूपद सोचता हुआ निरुत्तर रह गया।
‘‘बता सकते हो, ऐसा क्यों होता है ?’’ मीरा ने आगे पूछा।
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘इस ओर सोचते नहीं ?’’
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘फिर भागते क्यों हो ?’’
‘‘पता नहीं, माता।’’
‘‘तुम्हें पता क्या है, धूपद ?’’
‘‘कुछ नहीं, माता।’’
‘‘ऐसे कब तक, भागते रहोगे ?’’
‘‘नहीं मालूम।’’
‘‘भागकर जाते कहाँ हो ?’’
‘‘कहाँ जाऊँ ?’’
‘‘वहाँ चैन मिलता है ?’’
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘तुम जानना चाहते हो ?’’
‘‘क्या माता ?’’
‘‘जो तुम नहीं जानते।’’ मीरा ने गंभीर होकर कहा।
धूपद सोच में पड़ गया। वह क्या नहीं जानता ? उसे क्या जानना है ? क्यों जानना है ? पत्नी नहीं। माता पिता नहीं। चाचा ताऊ कोई नहीं। पत्नी के पक्षवाले उसके साथ अपनी छोटी लड़की को ब्याहना चाहते थे। लेकिन उसने उन्हें दो टूक उत्तर दे दिया-‘ससुरजी, ब्याह बार बार नहीं होता। वह एक बार हो चुका। अपने भाग्य में पत्नी का इतना ही साथ बदा था। अब और ब्याह नहीं।’ उसके बाद से उधर से चुप्पी।
‘‘क्या सोच में पड़ गए, धूपद ?’’ मीरा उसके मन की जन्मपत्री बाँचकर पूछ रही थी। उसे लग रहा था कि वह श्रीकृष्ण सेवा का सच्चा पात्र है। उसका मन शुद्ध है। उसके आचार-विचार में कोई खोट नहीं।
‘‘क्या सोचूँ, माता ! सोचना हम जैसे मूरख से कभी बना नहीं। सोचने को है भी क्या ! काला आखर कभी पढ़ा नहीं। सुना सुनाया भी कुछ नहीं। पत्नी स्वर्ग क्या सिधारी कि जग माटी हो गया। बेकार !’’ धूपद ने याद करते हुए अपनी कहानी के शीर्षक बाँचे और सोचता रह गया कि क्या उसे ऐसे सोचना चाहिए था ?
‘‘तुम कुछ मत सोचो। पर एक ठौर चित्त तो लगाओ। तुमने चित्तचोर का नाम सुना है ?’’
‘‘कौन चित्तचोर ?’’
‘‘वह दूसरों का चित्त चुराता है। तुम उसे नहीं जानते ?’’
धूपद ने सिर हिलाकर कहा, ‘‘नहीं।’’
‘‘अपना मोर मुकुटधारी, बाँके बिहारी, गोवर्धन गिरिधारी।’’
‘‘किसन कन्हैया ?’’
‘‘हाँ वही चित्तचोर है। वह जिसका चित्त चुरा ले वह जगत् की सारी आल-बाल से मुक्त। फिर चैन ही चैन।’’ मीरा ने सहजभाव से धूपद को समझाया। उसके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि धूपद सीधे ही किसन कन्हैया से जुड़ सकता है। एक बार उसके मन में टेढ़े होकर नटनागर ने स्थान बना लिया, फिर वह चाहे लाख प्रयत्न करे, तो भी वह नहीं निकलेगा। पर लगन तो लगे चिनगारी तो उठे।
‘‘उसके क्या कहने ! वह तो जगत् का पालनहार है। सारा जगत् उसी से है। पर वह हमारा चित्त क्यों चुराएगा ?’’ धूपद में सहज प्रश्न बुनावट डालने लगे।
‘‘क्यों नहीं चुराएगा ? वह तो जन्म का चोर है।’’ मीरा ने उसके मन को कुरेदा।
‘‘क्या कहती हैं, माता ! किसन और चोर।’’
‘‘क्यों, किसन चोर क्यों नहीं हो सकता ?’’
‘‘ना बाबा, ना ! कभी नहीं। भगवान् भी क्या कभी चोर हुए हैं ?’’ धूपद इतना कहकर मन ही मन जप करने लगा-‘‘हरे हरे हरे किसन, हरे-हरे !’’
‘‘क्यों नहीं हुए हैं ! माखन चुराया है न ! माखनचोर तभी तो उन्हें कहा जाता है। माखन चुराते हुए रँगे हाथ पकड़े गए तो क्या बोले, जानते हो तुम ?’’ मीरा ने उसके मन में झाँकने का प्रयत्न किया।
‘‘नहीं, माता।’’
‘‘गोपियाँ जसोदा को लेकर आ गईं। किसन के मुँह पर माखन लगा हुआ था। उनके हाथ माखन से भरे हुए थे। एक गोपी बोली, ‘ये देख लो अपने लला की करतूत। आप तो मानती ही नहीं थी कि....’ इसपर किसन बोला, ‘‘मैया, तू इनकी बातों पर भरोसा न कर। यह सब इनकी ही चालाकी है। इन सबन ने मिलकर मेरे मुँह में माखन लिपटाया। मेरे हाथ में माखन दिया और बोलीं-लला, तू माखन चख। जासे हमारा माखन अमृत बन जाएगा। सो मैया। और अब जे तोहे लिवा लाईं। मेरी भोली मैया, जरा सोचतो-इत्ते ऊँचे छीके पर मेरी बँहियाँ कैसे पहुँच सकती हैं ! जे सब मुझे तेरी साँटी से पिटवाना चाहती हैं। मैया, जे बड़ी चतुर हैं-मुझे फुसलाती हैं और तोहे उकसाती हैं।’ जसोदा बोलीं, ‘जे बात है। निपूतियों, तुम मेरे लला को पिटवाना चाहती हो ! आ मेरे आँखों के तारे मेरे पास आ।’ ऐसा किया था उस किसन कन्हैया, माखन चुरैया ने।’’ मीरा ने सहज ढंग से सारा प्रसंग सुना दिया। धूपद की आँखें खुली की खुली रह गईं। मीरा आगे कह रही थी-‘‘वह चित्तचोर है, जगत् का सिरजनहार। वह चित्त एक बार चुरा ले तो फिर चित्त को भटकने का कोई ठौर ही न रहे। सब झंझट दूर। बोल तू चाहेगा कि वह तेरा चित्त चुराए ?’’
धूपद ने कुछ देर बाद कहा, ‘‘पर वह हमारा चित्त चुराएगा क्यों, माता ? उसे क्या पड़ी कि वह ऐसे वैसों का चित्त चुराए ?’’
‘‘तूने ठीक कहा है, धूपद, वह हर एक का चित्त नहीं चुराता। वह तो चुराने वालों का चित्त चुराता है।’’ मीरा ने समझाया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book