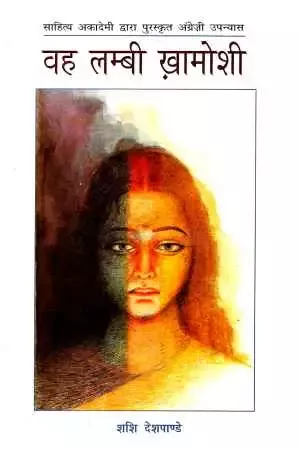|
स्त्री-पुरुष संबंध >> वह लम्बी खामोशी वह लम्बी खामोशीशशि देशपाण्डे
|
376 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है अंग्रेजी उपन्यास का हिन्दी अनुवाद....
Aawan
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
...मैं मोहन के लिए बनी बनायी तैयार थी-जैसा कि हमारी शादी के शीघ्र ही बाद मोहन ने मुझे बताया था-वह ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो अंग्रेजी बोल सके। उसके कथन से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था और दादा के उन शब्दों से भी जब उन्होंने पहली बार मोहन के विषय में मुझसे कहा था। दादा ने कहा था, ‘‘मेरा पक्का अनुमान है कि वह एक शिक्षित सुसंस्कृत पत्नी चाहता है। उसका कहना है कि उसे दान-दहेज, रुपये-पैसे आदि से कुछ मतलब नही है।’’
एक शिक्षित-सुसंस्कृत पत्नी...मुझे सन्देह हुआ कि क्या सब पुरुष इसी तरह के परिशुद्ध, निश्चित, सूक्ष्म विचार रखते हैं। लड़कियों के लिए कम-से-कम मेरे और उन बहुत सी मेरी जानी पहचानी लड़कियों के लिए यह खोज अस्पष्ट और धुँधली रही थी। हम भी किसी खोज में थे, पर किस चीज की खोज में थे, यह नहीं जानते थे। या अगर जानते भी थे तो उसे कोई विशेष नाम देने की इच्छा नहीं थी। यदि हमें नाम देने को विवश नहीं किया जाता, कि हम किस वस्तु की खोज में हैं, तो मेरा अनुमान है कि हम उसे, ‘प्रेम’ का नाम देते, जैसा चलचित्रों में नरगिस और राजकपूर के बीच, कैरी ग्राण्ट और डैबोरा केर के बीच होते देखा था। उसका अर्थ था, एक सुन्दर-सा युवा पुरुष यह कहता हुआ, ‘मैं तुमसे प्रेम करता हूँ’’-ऐसा सुन्दर युवा जो उन असली युवाओं से नितान्त भिन्न था जिसे हम प्रतिदन देखते थे। हमने प्रेम का यह वस्त्र उन सब युवा व्यक्तियों को पहनाकर देखा, जो हमारे सम्पर्क में आये, हर बार यह जानने को उत्सुकता से कि क्या यह ठीक बैठेगा ?
‘‘अगर मैं पुरुष होती, और मैं जिस दुनिया में रहती हूँ उसे जानने की चिन्ता करती तो मुझे लगता है कि उस आधी दुनिया की लम्बी ख़ामोशी का भार मुझे किंचित् बेचैन करता।’’
(एलिज़ाबैथ रॉबिन्स,-डब्ल्यू. डबल्यू. एस. एल. की 1907 की एक वार्ता का अंश)
एक शिक्षित-सुसंस्कृत पत्नी...मुझे सन्देह हुआ कि क्या सब पुरुष इसी तरह के परिशुद्ध, निश्चित, सूक्ष्म विचार रखते हैं। लड़कियों के लिए कम-से-कम मेरे और उन बहुत सी मेरी जानी पहचानी लड़कियों के लिए यह खोज अस्पष्ट और धुँधली रही थी। हम भी किसी खोज में थे, पर किस चीज की खोज में थे, यह नहीं जानते थे। या अगर जानते भी थे तो उसे कोई विशेष नाम देने की इच्छा नहीं थी। यदि हमें नाम देने को विवश नहीं किया जाता, कि हम किस वस्तु की खोज में हैं, तो मेरा अनुमान है कि हम उसे, ‘प्रेम’ का नाम देते, जैसा चलचित्रों में नरगिस और राजकपूर के बीच, कैरी ग्राण्ट और डैबोरा केर के बीच होते देखा था। उसका अर्थ था, एक सुन्दर-सा युवा पुरुष यह कहता हुआ, ‘मैं तुमसे प्रेम करता हूँ’’-ऐसा सुन्दर युवा जो उन असली युवाओं से नितान्त भिन्न था जिसे हम प्रतिदन देखते थे। हमने प्रेम का यह वस्त्र उन सब युवा व्यक्तियों को पहनाकर देखा, जो हमारे सम्पर्क में आये, हर बार यह जानने को उत्सुकता से कि क्या यह ठीक बैठेगा ?
‘‘अगर मैं पुरुष होती, और मैं जिस दुनिया में रहती हूँ उसे जानने की चिन्ता करती तो मुझे लगता है कि उस आधी दुनिया की लम्बी ख़ामोशी का भार मुझे किंचित् बेचैन करता।’’
(एलिज़ाबैथ रॉबिन्स,-डब्ल्यू. डबल्यू. एस. एल. की 1907 की एक वार्ता का अंश)
संकेत आरंभिक
पुस्तक में प्रयुक्त रिश्तों और नातों की भिन्न-भिन्न नाम-संज्ञाएँ पाठक को कठिनाई में डाल सकती हैं। अतः उनकी सुविधा के लिये यह संकेत दे रही हूं कि इस कथा को कहनेवाले जया के पिता ‘अप्पा’ और माँ ‘आई’ हैं। उसका बड़ा भाई दिनकर, ‘दादा’ और पिता की माँ (दादी) ‘अज्जी’ हैं। उसके पिता के सारे भाई ‘काका’ और उनकी पत्नियाँ ‘काकी’ हैं। जया की माँ की माँ (नानी) दूसरी ‘अज्जी’ हैं। उसके मामा हैं ‘चन्दूमामा’ और ‘मकरन्द मामा’। चन्दूमामा की पत्नी उसकी मामी ‘वनीता मामी’ है।
किसी प्रायोजन को सिद्ध करने और कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, तुम्हें कठोर और निष्ठुर बनना पड़ता है। हाँ, अगर तुम शान्त भी बनना चाहो, सारे विश्व को प्रेम करने की इच्छा करो, तो पहले तुम्हारे प्यार की सीमा में आए विशिष्ट व्यक्तियों से प्यार करना छोड़ना पड़ेगा। और जो तुम्हें प्यार करते हैं, उन्हें जब तुम यह जताते हो कि तुम उन्हें किसी विशेष रूप में प्यार नहीं करते, और वे इस बात से आहत होते हैं, तो यह और भी बुरा होता है। सन्त बनने का और कोई रास्ता है ही नहीं। न ही कोई चित्रकार या लेखक बनने का।
यह सब बातें मैं अब क्यों सोच रही हूँ ? क्या इसलिए कि मैं शब्दों की खोज में संघर्षरत हूँ ? है न विचित्र बात ! लेखन-क्रिया मेरे लिए हमेशा आसान रही है। उचित शब्दों तक इतने सुभीते से पहुँच जाना मुझे प्रसन्न कर देता था, कभी-कभी तो लजा भी देता है। ज़्यादा ही आसान लगता था। किन्तु अब तो, न मालूम क्या बात है, मुझे प्रसव पीड़ा का स्मरण हो जाता है। उसकी याद से अब भय लगता है। ‘भय’ कि मेरे अपने शरीर से मेरा नियन्त्रण छूटा जा रहा था। मैंने उसका अवरोध किया।
क्या मैं अब भी प्रतिरोध कर रही हूँ ? शायद ! क्योंकि मैं अब उन सब मासूम अबोध बालिकाओं का जिक्र नहीं कर रही हूँ, जिनकी बाबत अब तक मैंने लिखा है, वे लड़कियाँ जिन्होंने अपना गठबन्धन अनन्ततोगत्वा उपयुक्त पुरुषों से कर लिया।
न ही मैं किसी निर्दयी, भावशून्य पति और भावुकता से आक्रान्त पत्नी की कहानी लिख रही हूँ। मैं ‘हमारी’ कहानी लिख रही हूँ। मोहन की और अपनी भी। मैं यह भी जानती हूँ कि कोई कभी भी अपनी निजी कहानी की नायिका नहीं हो सकता। आत्माभिव्क्ति एक निर्मम प्रक्रिया है। ‘वह वास्तव चित्र’, ‘वास्तव तुम’ कभी प्रकट नहीं होता। उसकी खोज उतनी ही सभ्रम में डालनेवाली है, जितना यह जानने का प्रयत्न कि तुम वास्तव में कैसे दिखाई देते हो ? दस भिन्न-भिन्न दर्पण तुम्हें अपने दस भिन्न-भिन्न चेहरे दिखाते हैं।
कामत ने मुझसे कहा था, ‘‘तुम्हारा चेहरा तुम्हारे नाम जैसा है’’ और मैं मन्त्रमुग्ध हो गई थी। ‘‘कैसे ?’’ मैंने उससे पूछा था। मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई कि मैं औरों की आँखों को कैसी दिखती हूँ। दर्पण तो सदा धोखा देता है। दर्पण तो वही दर्शाता है जो तुम देखना चाहते हो और शायद दूसरे भी तुम्हारे चेहरे में वही देखते हैं, जो वह देखना चाहते हैं। पर फिर भी अपने आइने को देखने का आकर्षण और यह जानने की लालसा कि तुम औरों को कैसे दिखते हो, कभी नीरस नहीं होती।
शायद अपने को अन्दर रख कर लिखना ठीक नहीं है। सम्भवतया मुझे स्वयं को और ‘हम’ को एक फ़ासले पर खड़े होकर देखना होगा। मेरे साथ पहले भी हुआ है। ऐसे अवसर आए हैं जब मुझे अपने निज से विलग और दूर होने की विचित्र अनूभूति हुई। वे ऐसे अवसर थे, जब मैं दो स्पष्ट तत्त्वों को अलविदा कर सकी हूँ। अपने अनुभव को और उस अनुभव के बोध को। क्या ऐसा करने की आवश्यक निर्ममता मुझमें है ?
एक बार एक पत्रिका ने कहा था, ‘‘हमें अपना वैयक्तिक विवरण भेज दो’’ और इस सोच ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। मेरे जीवन में ऐसा क्या था, जो अर्थपूर्ण हो। अन्त में जब सारे जीवन में से मैंने अप्रासंगिक बातों को छान डाला, तो शेष रहीं केवल ये बातें :
मैं जन्मी। जब मैं पन्द्रह साल की थी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी शादी मोहन से हुई। मेरे दो बच्चे हैं और मैंने तीसरे को जीने नहीं दिया।
शुरू करने के लिए सम्भवतः इतना ही पर्याप्त है।
अब यहाँ से आगे बढ़ें !
किसी प्रायोजन को सिद्ध करने और कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, तुम्हें कठोर और निष्ठुर बनना पड़ता है। हाँ, अगर तुम शान्त भी बनना चाहो, सारे विश्व को प्रेम करने की इच्छा करो, तो पहले तुम्हारे प्यार की सीमा में आए विशिष्ट व्यक्तियों से प्यार करना छोड़ना पड़ेगा। और जो तुम्हें प्यार करते हैं, उन्हें जब तुम यह जताते हो कि तुम उन्हें किसी विशेष रूप में प्यार नहीं करते, और वे इस बात से आहत होते हैं, तो यह और भी बुरा होता है। सन्त बनने का और कोई रास्ता है ही नहीं। न ही कोई चित्रकार या लेखक बनने का।
यह सब बातें मैं अब क्यों सोच रही हूँ ? क्या इसलिए कि मैं शब्दों की खोज में संघर्षरत हूँ ? है न विचित्र बात ! लेखन-क्रिया मेरे लिए हमेशा आसान रही है। उचित शब्दों तक इतने सुभीते से पहुँच जाना मुझे प्रसन्न कर देता था, कभी-कभी तो लजा भी देता है। ज़्यादा ही आसान लगता था। किन्तु अब तो, न मालूम क्या बात है, मुझे प्रसव पीड़ा का स्मरण हो जाता है। उसकी याद से अब भय लगता है। ‘भय’ कि मेरे अपने शरीर से मेरा नियन्त्रण छूटा जा रहा था। मैंने उसका अवरोध किया।
क्या मैं अब भी प्रतिरोध कर रही हूँ ? शायद ! क्योंकि मैं अब उन सब मासूम अबोध बालिकाओं का जिक्र नहीं कर रही हूँ, जिनकी बाबत अब तक मैंने लिखा है, वे लड़कियाँ जिन्होंने अपना गठबन्धन अनन्ततोगत्वा उपयुक्त पुरुषों से कर लिया।
न ही मैं किसी निर्दयी, भावशून्य पति और भावुकता से आक्रान्त पत्नी की कहानी लिख रही हूँ। मैं ‘हमारी’ कहानी लिख रही हूँ। मोहन की और अपनी भी। मैं यह भी जानती हूँ कि कोई कभी भी अपनी निजी कहानी की नायिका नहीं हो सकता। आत्माभिव्क्ति एक निर्मम प्रक्रिया है। ‘वह वास्तव चित्र’, ‘वास्तव तुम’ कभी प्रकट नहीं होता। उसकी खोज उतनी ही सभ्रम में डालनेवाली है, जितना यह जानने का प्रयत्न कि तुम वास्तव में कैसे दिखाई देते हो ? दस भिन्न-भिन्न दर्पण तुम्हें अपने दस भिन्न-भिन्न चेहरे दिखाते हैं।
कामत ने मुझसे कहा था, ‘‘तुम्हारा चेहरा तुम्हारे नाम जैसा है’’ और मैं मन्त्रमुग्ध हो गई थी। ‘‘कैसे ?’’ मैंने उससे पूछा था। मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई कि मैं औरों की आँखों को कैसी दिखती हूँ। दर्पण तो सदा धोखा देता है। दर्पण तो वही दर्शाता है जो तुम देखना चाहते हो और शायद दूसरे भी तुम्हारे चेहरे में वही देखते हैं, जो वह देखना चाहते हैं। पर फिर भी अपने आइने को देखने का आकर्षण और यह जानने की लालसा कि तुम औरों को कैसे दिखते हो, कभी नीरस नहीं होती।
शायद अपने को अन्दर रख कर लिखना ठीक नहीं है। सम्भवतया मुझे स्वयं को और ‘हम’ को एक फ़ासले पर खड़े होकर देखना होगा। मेरे साथ पहले भी हुआ है। ऐसे अवसर आए हैं जब मुझे अपने निज से विलग और दूर होने की विचित्र अनूभूति हुई। वे ऐसे अवसर थे, जब मैं दो स्पष्ट तत्त्वों को अलविदा कर सकी हूँ। अपने अनुभव को और उस अनुभव के बोध को। क्या ऐसा करने की आवश्यक निर्ममता मुझमें है ?
एक बार एक पत्रिका ने कहा था, ‘‘हमें अपना वैयक्तिक विवरण भेज दो’’ और इस सोच ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। मेरे जीवन में ऐसा क्या था, जो अर्थपूर्ण हो। अन्त में जब सारे जीवन में से मैंने अप्रासंगिक बातों को छान डाला, तो शेष रहीं केवल ये बातें :
मैं जन्मी। जब मैं पन्द्रह साल की थी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी शादी मोहन से हुई। मेरे दो बच्चे हैं और मैंने तीसरे को जीने नहीं दिया।
शुरू करने के लिए सम्भवतः इतना ही पर्याप्त है।
अब यहाँ से आगे बढ़ें !
लम्बी ख़ामोशी
पहला भाग
जब मैं बच्चा थी, तो फ़िल्मी-संगीत इतना घटिया माना जाता था, कि अपने रेडियो पर उसे सुनने की मनाही थी। अब बीते दिनों में झाँककर देखती हूँ तो समझ में आता है कि यह धारणा उस समय की कृतिम अति नैतिकता का अंश थी। महात्मा गाँधी की मृत्यु के बाद यह झूमते-झामते गाने आनन्ददायक और हल्के-फुल्के माने जाते थे, और इसीलिए कुप्रभाव डालनेवाले। इसीलिए ‘रेडियो सीलोन’ से गाना सुनना शर्मानक और छिछोरापन था। छिछोरापन तो था ही—क्योंकि मेरे पिता की रुचि सदैव गम्भीर शास्त्रीय संगीत में रही थी। अतः उन्होंने उस तरह के गाने सुनने के मेरे व्यसन को सदा तुच्छ समझा था। और उसे वह विरक्तिमय भावुकता की लुगदी कहते थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि मैं रफ़ी और लता के बदले पलुस्कर और फ़य्याज ख़ाँ में रुचि लूँ। किन्तु वह असफल रहे।
मुझे याद है कि एक बार उन्होंने कहा था, ‘‘जया ! तुम्हारी रुचि कितनी घटिया है ?’’
उस समय जो शर्म मुझे लगी वह बहुत समय तक मेरे अन्दर ज़िन्दा रही। फ़िल्म देखने जाने के लिए तैयार होते समय मोहन अक्सर कहा करते, ‘‘जया ! जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यही होगा न कि हम विज्ञापन नहीं देख पाएंगे। ना सही उन्हें देखने की इच्छा होती ही किसे है ?’’
मुझे वह इच्छा रहती थी। किन्तु मैंने मोहन पर प्रकट नहीं होने देने का साहस नहीं किया। मान लो वह भी यही कहता, ‘‘कितनी घटिया रुचि है तुम्हारी जया ?’’ मैं, बल्कि झिझककर कहती, ‘‘हाँ-हाँ ! क्या जल्दी है ?’’....और साथ ही साथ समय से पहुँचने के प्रयत्न में छल से व्यग्रता से लगी रहती। शिशु के होंठों पर प्यार से चिपकी दूध की मूंछें, मुस्कराती माँ अपने बेटे की छाती पर विक्स मलती, उससे भी कम उम्र की माँ अपने बच्चे को फ़ैरेक्स पिलाती....हाथ में हाथ डाले भाई-बहन अपने चाव भरे मुस्कराते माता-पिता और चाकलेटों की तरफ़ दौड़ते। मुझे सब प्रिय लगते थे। वे आरामदेह, खिले हुए, प्रसन्न परिवार, अपने चमकते घरों में, मेरे लिए विशुद्ध कविता के दाने बिखरा देते थे। मेरे लिए वे, परियों की कहानी थे, जिनमें लोग ‘‘फिर, सदा ख़ुशी और आनन्द में मग्न रहते थे।’’
जिस शाम मैं और मोहन अपने दादर के फ़्लैट में आए और उसके लगभग दस दिन बाद से हम चारों का एक साथ खाने बैठना—उसी तरह एक रंगीन विज्ञापन की चमकती-दमकती तस्वीर-सा सामने आया। हम मुस्कराए, हँसे खिलखिलाए। मुझ ‘माँ’ ने उन्हें बड़ा प्यार और ध्यान से खिलाया। परिवार का प्रधान मोहन सन्तुष्टमन मुस्कुराया और बच्चे प्रफुल्ल और खेल में मस्त ! ‘दृश्य’—हाँ उसे दृश्य ही कहूँगी, क्योंकि उस चित्र से मेल खाता और कोई शब्द नहीं ढूँढ़ पाई। जब ढूँढ़ने की कोशिश की तो, तो हाथ आई रात के खाने पर होती तो वही साधारण बातचीत—विद्वेष का कूड़ा-कचरा तैरता हुआ ऊपर आकर एक शान्त, स्वच्छ सतह को गन्दला करता हुआ।
प्रसन्नता का भ्रम—हाँ उसे विलुप्त करना पड़ा। सच्चाई शायद यह है कि उस समय दृश्य से बहुत फ़ासले पर नहीं थी। उस भ्रम को मैं बनाए रखने की कल्पना कर रही थी। सम्भवतया कौन जानता है कि ऐसा हो कि तुच्छ ढंग की कहा-सुनी और भद्देपन का अपना खेल दिखाकर, समय अदृश्य हो जाए और एक रमणीय दृश्य छोड़ जाए। किन्तु उन क्षणों में मुझे अपने निज में यह सच्चाई स्वीकृत करनी पड़ी थी कि पारिवरिक जीवन जीना मुझे बहुधा असह्य लगता है। अधिक तंग करती थी वह ऊब, जो एक ही तरह के ढंग से जीने से होती थी और एक अन्तहीन नीरसता की अकुलाहट उत्पन्न करती थी। अब मुझे याद आता है कि मैंने कितनी आहें भरी थीं कि ऐसी सत्यानाशी दुर्घटना अकस्मात हो जो व्यक्तिगत रूप से तो न हो किन्तु ऐसी हो जो हमें अपनी इस उबाऊ स्थिति से हिलाकर रख दे।
एक बार आठ ग्रहों के संयुक्तमिलन ने जो किसी दुर्घटना का पूर्वाभास, होता है, मेरी इस आशा को उत्तेजित कर दिया था। मुझे आश्चर्य होता था कि युद्ध, भूचाल, ज्वार, तूफ़ान आदि दूर के अनजान देशों में क्यों होते हैं ? ख़ून-ख़राबा, व्यभिचार और वीरता का स्थान अन्य जनों के जीवन में क्यों है, हमारे में कभी क्यों नहीं ? ‘मुसीबतें’, ‘कुकर्म’, ‘दण्ड’ आदि शब्द हमारे जीवन में अप्रासंगिक लगते थे। ग्रीक नाटकों के कोरस की तरह, हम कष्टों से दूरी पर रहते थे—हमारे भाग्य में तो लगातार जीना ही जीना है। एक डग के बाद दूसरा डग भरना, जब तक मृत्यु स्वाभाविक रूप से हम तक पहुँचे।
किन्तु अन्त में, सबकुछ के बाद, वह आई है। मेरी अपनी विपत्ति; वह थी एक इनाम का पैकेट बनी, रंग-बिरंगे रेशमी फ़ीतों में बँधी, मेरे पति द्वारा दी गई मुझे एक भेंट के रूप में। और मैं चकरा गई। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी भेंट का मुझे क्या करना है ? मुझे वह असंभव लगा। मोहन से अवश्य कोई गलती हुई है। हमारा जीवन पहले की ही तरह ही चलेगा, बीच-बीच में होंगे नीरस झगड़े, बच्चों की सफलताएँ और असफलताएँ, उनका आपसी अलगाव, हमसे उदासीनता, हमारा रोष। हमारी कड़वाहट, हमारी वृद्धावस्था, शायद मेरे लिए वैधव्य—यही हमारा भविष्य था। हम जैसों के लिए और कुछ असंभव नहीं था।
‘‘हम जैसे’ अब यह वाक्य मुझे किस बात की याद दिलाता है ? अरे हाँ ! मोहन द्वार सुनाई गई उन स्त्रियों और बच्चों की कहानी जो दिल्ली की सड़कों पर चौकड़ी मारे बैठी थीं। शायद हमें उस कहानी को एक अपशकुन की तरह, अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए था, पर जब मैंने मोहन से वह गाथा सुनी थी, तो मेरे लिए भीतर कोई हलचल नहीं हुई थी। मैं नितान्त तटस्थ रही थी...बिलकुल अलग-थलग किन्तु यह भी स्वीकार करती हूँ कि उस समय मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि उस घटना से जिसका हमसे कोई सरोकार नहीं था और न ही कोई बहुत अजीबोगरीब घटना थी, मोहन के मन में इतनी बढ़ी-चढ़ी प्रतिक्रिया क्यों हुई थी ? मैंने शायद ही मोहन को ऐसी किसी घटना से प्रभावित होते देखा था, जिसका वास्ता उसका अपने से, अपने परिवार से अपनी नौकरी से न हो। मैं जानती हूँ वह कारण जिसने मोहन को इतने असंदिग्ध रूप से प्रभावित किया था—जो उसने देखा था उसने कहीं उसे भयभीत कर दिया था।
‘‘वे औरतें नंगी ज़मीन पर बैठी हुई थीं। और सोचो तो कि उसके नीचे न तो चटाई थी और न कोई अख़बार का टुकड़ा। एकदम ज़मीन पर ऐसी बैठी थीं जैसे भिखारिनें। जया ! कल्पना करो अगर हम जैसे लोग उस स्थिति में आ जाएँ ।’’
‘‘हम जैसे’’—इन शब्दों के अर्थ खोलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझ गई थी। अच्छी तरह पढ़े-लिखे, मेहनती, सुरक्षित नौकरियों में लगे इन्सान, इन्श्योरेंस और प्रोविडेण्ट फण्ड की आरामदेह गद्दियों पर टिके, दो स्वस्थ, पौष्टिक भोजन करते बढ़िया स्कूलों में जाते बच्चों समेत ! ‘‘वे लोग वहाँ चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक भी नहीं बोल रहा था।....बच्चे तक भी नहीं। हाँ...बच्चे तक नहीं ! ...इसी से मुझे धक्का लगा, जया ! कि उनके साथ उनके बच्चे भी थे। वे कुछ रंगीन तख्ते पकड़े हुए थे...बोर्ड....जिनपर घर में बैठकर रंग पोता होगा और लिखा होगा ! शायद कुछ बच्चों ने भी रंग भी लगाया हो। कुछ अक्षरों से रंग नीचे टपक आया था....वे बूँदें आँसू लग रही थीं।’’
अब मुझे याद आता है कि इस नुक़्ते पर मैं उठ बैठी थी और मोहन की बात पूरे ध्यान से सुनने लगी। नीचे टपकती रंग की बूँदें जो आँसुओं-सी लग रही थीं। और यह शब्द थे मोहन के उस उस मुँह के, जो कभी कल्पना की उड़ाने नहीं भरता था, जो अलंकृत या लच्छेदार भाषा का तिरस्कार करता था, जिसे जीवन की वास्तविकता में विश्वास रखने में अभिमान था।
सब पट्टे एक ही बात बोल रहे थे : ‘‘हमें न्याय चाहिए’’। औरतें और बच्चे उन पट्टों के लिए बैठे थे, और उनके चेहरे बता रहे थे कि वे जानते हैं कि सब कुछ निराशाजनक है। वे ऐसे दिखते थे जैसे ...वह आगे कहने के लिए शब्द ढूँढ़ने में अटक गया और अन्त में शब्द निकला भयावह’। लोग एक नज़र उन पर डालकर चलते बनते थे। जया ! क्या अजीब बात थी कि एक भी इन्सान न वहाँ ठहरा और न किसी ने गौर से देखा। लोगों ने एक उड़ती-सी नज़र उन पर डाली और झटपट वहाँ से आगे बढ़ गए। न किसी ने उनसे कुछ प्रश्न किया और न ही कुछ टिप्पणी की।
मुझे याद है कि एक बार उन्होंने कहा था, ‘‘जया ! तुम्हारी रुचि कितनी घटिया है ?’’
उस समय जो शर्म मुझे लगी वह बहुत समय तक मेरे अन्दर ज़िन्दा रही। फ़िल्म देखने जाने के लिए तैयार होते समय मोहन अक्सर कहा करते, ‘‘जया ! जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यही होगा न कि हम विज्ञापन नहीं देख पाएंगे। ना सही उन्हें देखने की इच्छा होती ही किसे है ?’’
मुझे वह इच्छा रहती थी। किन्तु मैंने मोहन पर प्रकट नहीं होने देने का साहस नहीं किया। मान लो वह भी यही कहता, ‘‘कितनी घटिया रुचि है तुम्हारी जया ?’’ मैं, बल्कि झिझककर कहती, ‘‘हाँ-हाँ ! क्या जल्दी है ?’’....और साथ ही साथ समय से पहुँचने के प्रयत्न में छल से व्यग्रता से लगी रहती। शिशु के होंठों पर प्यार से चिपकी दूध की मूंछें, मुस्कराती माँ अपने बेटे की छाती पर विक्स मलती, उससे भी कम उम्र की माँ अपने बच्चे को फ़ैरेक्स पिलाती....हाथ में हाथ डाले भाई-बहन अपने चाव भरे मुस्कराते माता-पिता और चाकलेटों की तरफ़ दौड़ते। मुझे सब प्रिय लगते थे। वे आरामदेह, खिले हुए, प्रसन्न परिवार, अपने चमकते घरों में, मेरे लिए विशुद्ध कविता के दाने बिखरा देते थे। मेरे लिए वे, परियों की कहानी थे, जिनमें लोग ‘‘फिर, सदा ख़ुशी और आनन्द में मग्न रहते थे।’’
जिस शाम मैं और मोहन अपने दादर के फ़्लैट में आए और उसके लगभग दस दिन बाद से हम चारों का एक साथ खाने बैठना—उसी तरह एक रंगीन विज्ञापन की चमकती-दमकती तस्वीर-सा सामने आया। हम मुस्कराए, हँसे खिलखिलाए। मुझ ‘माँ’ ने उन्हें बड़ा प्यार और ध्यान से खिलाया। परिवार का प्रधान मोहन सन्तुष्टमन मुस्कुराया और बच्चे प्रफुल्ल और खेल में मस्त ! ‘दृश्य’—हाँ उसे दृश्य ही कहूँगी, क्योंकि उस चित्र से मेल खाता और कोई शब्द नहीं ढूँढ़ पाई। जब ढूँढ़ने की कोशिश की तो, तो हाथ आई रात के खाने पर होती तो वही साधारण बातचीत—विद्वेष का कूड़ा-कचरा तैरता हुआ ऊपर आकर एक शान्त, स्वच्छ सतह को गन्दला करता हुआ।
प्रसन्नता का भ्रम—हाँ उसे विलुप्त करना पड़ा। सच्चाई शायद यह है कि उस समय दृश्य से बहुत फ़ासले पर नहीं थी। उस भ्रम को मैं बनाए रखने की कल्पना कर रही थी। सम्भवतया कौन जानता है कि ऐसा हो कि तुच्छ ढंग की कहा-सुनी और भद्देपन का अपना खेल दिखाकर, समय अदृश्य हो जाए और एक रमणीय दृश्य छोड़ जाए। किन्तु उन क्षणों में मुझे अपने निज में यह सच्चाई स्वीकृत करनी पड़ी थी कि पारिवरिक जीवन जीना मुझे बहुधा असह्य लगता है। अधिक तंग करती थी वह ऊब, जो एक ही तरह के ढंग से जीने से होती थी और एक अन्तहीन नीरसता की अकुलाहट उत्पन्न करती थी। अब मुझे याद आता है कि मैंने कितनी आहें भरी थीं कि ऐसी सत्यानाशी दुर्घटना अकस्मात हो जो व्यक्तिगत रूप से तो न हो किन्तु ऐसी हो जो हमें अपनी इस उबाऊ स्थिति से हिलाकर रख दे।
एक बार आठ ग्रहों के संयुक्तमिलन ने जो किसी दुर्घटना का पूर्वाभास, होता है, मेरी इस आशा को उत्तेजित कर दिया था। मुझे आश्चर्य होता था कि युद्ध, भूचाल, ज्वार, तूफ़ान आदि दूर के अनजान देशों में क्यों होते हैं ? ख़ून-ख़राबा, व्यभिचार और वीरता का स्थान अन्य जनों के जीवन में क्यों है, हमारे में कभी क्यों नहीं ? ‘मुसीबतें’, ‘कुकर्म’, ‘दण्ड’ आदि शब्द हमारे जीवन में अप्रासंगिक लगते थे। ग्रीक नाटकों के कोरस की तरह, हम कष्टों से दूरी पर रहते थे—हमारे भाग्य में तो लगातार जीना ही जीना है। एक डग के बाद दूसरा डग भरना, जब तक मृत्यु स्वाभाविक रूप से हम तक पहुँचे।
किन्तु अन्त में, सबकुछ के बाद, वह आई है। मेरी अपनी विपत्ति; वह थी एक इनाम का पैकेट बनी, रंग-बिरंगे रेशमी फ़ीतों में बँधी, मेरे पति द्वारा दी गई मुझे एक भेंट के रूप में। और मैं चकरा गई। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी भेंट का मुझे क्या करना है ? मुझे वह असंभव लगा। मोहन से अवश्य कोई गलती हुई है। हमारा जीवन पहले की ही तरह ही चलेगा, बीच-बीच में होंगे नीरस झगड़े, बच्चों की सफलताएँ और असफलताएँ, उनका आपसी अलगाव, हमसे उदासीनता, हमारा रोष। हमारी कड़वाहट, हमारी वृद्धावस्था, शायद मेरे लिए वैधव्य—यही हमारा भविष्य था। हम जैसों के लिए और कुछ असंभव नहीं था।
‘‘हम जैसे’ अब यह वाक्य मुझे किस बात की याद दिलाता है ? अरे हाँ ! मोहन द्वार सुनाई गई उन स्त्रियों और बच्चों की कहानी जो दिल्ली की सड़कों पर चौकड़ी मारे बैठी थीं। शायद हमें उस कहानी को एक अपशकुन की तरह, अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए था, पर जब मैंने मोहन से वह गाथा सुनी थी, तो मेरे लिए भीतर कोई हलचल नहीं हुई थी। मैं नितान्त तटस्थ रही थी...बिलकुल अलग-थलग किन्तु यह भी स्वीकार करती हूँ कि उस समय मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि उस घटना से जिसका हमसे कोई सरोकार नहीं था और न ही कोई बहुत अजीबोगरीब घटना थी, मोहन के मन में इतनी बढ़ी-चढ़ी प्रतिक्रिया क्यों हुई थी ? मैंने शायद ही मोहन को ऐसी किसी घटना से प्रभावित होते देखा था, जिसका वास्ता उसका अपने से, अपने परिवार से अपनी नौकरी से न हो। मैं जानती हूँ वह कारण जिसने मोहन को इतने असंदिग्ध रूप से प्रभावित किया था—जो उसने देखा था उसने कहीं उसे भयभीत कर दिया था।
‘‘वे औरतें नंगी ज़मीन पर बैठी हुई थीं। और सोचो तो कि उसके नीचे न तो चटाई थी और न कोई अख़बार का टुकड़ा। एकदम ज़मीन पर ऐसी बैठी थीं जैसे भिखारिनें। जया ! कल्पना करो अगर हम जैसे लोग उस स्थिति में आ जाएँ ।’’
‘‘हम जैसे’’—इन शब्दों के अर्थ खोलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझ गई थी। अच्छी तरह पढ़े-लिखे, मेहनती, सुरक्षित नौकरियों में लगे इन्सान, इन्श्योरेंस और प्रोविडेण्ट फण्ड की आरामदेह गद्दियों पर टिके, दो स्वस्थ, पौष्टिक भोजन करते बढ़िया स्कूलों में जाते बच्चों समेत ! ‘‘वे लोग वहाँ चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक भी नहीं बोल रहा था।....बच्चे तक भी नहीं। हाँ...बच्चे तक नहीं ! ...इसी से मुझे धक्का लगा, जया ! कि उनके साथ उनके बच्चे भी थे। वे कुछ रंगीन तख्ते पकड़े हुए थे...बोर्ड....जिनपर घर में बैठकर रंग पोता होगा और लिखा होगा ! शायद कुछ बच्चों ने भी रंग भी लगाया हो। कुछ अक्षरों से रंग नीचे टपक आया था....वे बूँदें आँसू लग रही थीं।’’
अब मुझे याद आता है कि इस नुक़्ते पर मैं उठ बैठी थी और मोहन की बात पूरे ध्यान से सुनने लगी। नीचे टपकती रंग की बूँदें जो आँसुओं-सी लग रही थीं। और यह शब्द थे मोहन के उस उस मुँह के, जो कभी कल्पना की उड़ाने नहीं भरता था, जो अलंकृत या लच्छेदार भाषा का तिरस्कार करता था, जिसे जीवन की वास्तविकता में विश्वास रखने में अभिमान था।
सब पट्टे एक ही बात बोल रहे थे : ‘‘हमें न्याय चाहिए’’। औरतें और बच्चे उन पट्टों के लिए बैठे थे, और उनके चेहरे बता रहे थे कि वे जानते हैं कि सब कुछ निराशाजनक है। वे ऐसे दिखते थे जैसे ...वह आगे कहने के लिए शब्द ढूँढ़ने में अटक गया और अन्त में शब्द निकला भयावह’। लोग एक नज़र उन पर डालकर चलते बनते थे। जया ! क्या अजीब बात थी कि एक भी इन्सान न वहाँ ठहरा और न किसी ने गौर से देखा। लोगों ने एक उड़ती-सी नज़र उन पर डाली और झटपट वहाँ से आगे बढ़ गए। न किसी ने उनसे कुछ प्रश्न किया और न ही कुछ टिप्पणी की।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book