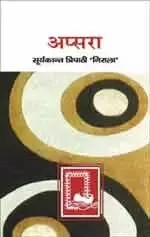|
नारी विमर्श >> अप्सरा अप्सरासूर्यकान्त त्रिपाठी निराला
|
278 पाठक हैं |
||||||
धरती पर उतरती अप्सरा-सी सुन्दर और कला-प्रेम में डूबी एक वीरांगना की यह कथा हमारे ह्रदय पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। अपने व्यवसाय से उदासीन होकर वह अपना ह्रदय एक कलाकार को दे डालती है और नाना दुष्चक्रों का सामना करती हुई अन्ततः अपनी पावनता को बनाए रख पाने में समर्थ होती है।
Apsara a hindi book by Suryakant Tripathi Nirala - अप्सरा - सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
आधुनिक हिन्दी कविता के सर्वाधिक तेजस्वी और युगांतरकारी व्यक्तित्व सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला एक समर्थ, सोद्देश्य कथाकार के नाते भी सुप्रतिष्ठित हैं। काव्य-रचना के साथ-साथ उन्होंने जिन कई उपन्यासों की रचना की, उनमें अप्सरा पहला है यानी ‘निराला’ की कथा-यात्रा का प्रथम सोपान।
धरती पर उतरती अप्सरा-सी सुन्दर और कला-प्रेम में डूबी एक वीरांगना की यह कथा हमारे ह्रदय पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। अपने व्यवसाय से उदासीन होकर वह अपना ह्रदय एक कलाकार को दे डालती है और नाना दुष्चक्रों का सामना करती हुई अन्ततः अपनी पावनता को बनाए रख पाने में समर्थ होती है। इस प्रक्रिया में उसकी नारी सुलभ कोमलताएँ तो उजागर होती ही हैं, उसकी चारित्रिक दृढ़ता भी प्रेरणा पद हो उठती है। इसके साथ ही इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय परवेश और स्वाधीनता-प्रेमी युवा-वर्ग की दृढ़ संकल्पित मानसिकता का चित्रण भी अत्यन्त सुन्दर ढंग से हुआ है, जो कि महाप्राण निराला की सामाजिक प्रतिबद्धता का एक ज्वलंत उदाहरण है।
अप्सरा को साहित्य में सबसे पहले मंद गति से सुंदर-सुकुमार कवि-मित्र सुमित्रानन्दन पंत की ओर बढ़ते हुए देखा, पंत की ओर नहीं। मैंने देखा, पंत जी की तरफ एक स्नेह-कटाक्ष कर, सहज फिरकर उसने मुझसे कहा, इन्हीं के पास बैठकर इन्हीं से मैं अपना जीवन रहस्य कहूँगी, फिर चली गई।
धरती पर उतरती अप्सरा-सी सुन्दर और कला-प्रेम में डूबी एक वीरांगना की यह कथा हमारे ह्रदय पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। अपने व्यवसाय से उदासीन होकर वह अपना ह्रदय एक कलाकार को दे डालती है और नाना दुष्चक्रों का सामना करती हुई अन्ततः अपनी पावनता को बनाए रख पाने में समर्थ होती है। इस प्रक्रिया में उसकी नारी सुलभ कोमलताएँ तो उजागर होती ही हैं, उसकी चारित्रिक दृढ़ता भी प्रेरणा पद हो उठती है। इसके साथ ही इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय परवेश और स्वाधीनता-प्रेमी युवा-वर्ग की दृढ़ संकल्पित मानसिकता का चित्रण भी अत्यन्त सुन्दर ढंग से हुआ है, जो कि महाप्राण निराला की सामाजिक प्रतिबद्धता का एक ज्वलंत उदाहरण है।
अप्सरा को साहित्य में सबसे पहले मंद गति से सुंदर-सुकुमार कवि-मित्र सुमित्रानन्दन पंत की ओर बढ़ते हुए देखा, पंत की ओर नहीं। मैंने देखा, पंत जी की तरफ एक स्नेह-कटाक्ष कर, सहज फिरकर उसने मुझसे कहा, इन्हीं के पास बैठकर इन्हीं से मैं अपना जीवन रहस्य कहूँगी, फिर चली गई।
वक्तव्य
अन्यान्य भाषाओं के मुकाबले हिंदी में उपन्यासों की संख्या थोड़ी है। साहित्य तथा समाज के गले पर मुक्ताओं की माला की तरह इने-गिने उपन्यास ही हैं। मैं श्री प्रेमचन्द जी के उपन्यासों के उद्देश्यों पर कह रहा हूँ। इनके अलावा और भी कई ऐसी रचनाएँ हैं, जो स्नेह तथा आदर-सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। इन बड़ी-बड़ी तोंदवाले औपन्यासिक सेठों की महफ़िल में मेरी दंशिताधरा अप्सरा उतरते हुए बिल्कुल संकुचित नहीं हो रही—उसे विश्वास है, वह एक ही दृष्टि से इन्हें अपना अनन्य भक्त कर लेगी। किसी दूसरी रूपवाली अनिंद्य सुंदरी से भी आँखें मिलाते हुए वह नहीं घबराती, क्योंकि वह स्पर्द्धा की एक ही सृष्टि, अपनी ही विद्युत् से चमकती हुई चिर-सौंदर्य के आकाश-तत्त्व में छिप गई है।
मैंने किसी विचार से अप्सरा नहीं लिखी, किसी उद्देश्य की पुष्टि भी इसमें नहीं। अप्सरा स्वयं मुझे जिस-जिस ओर ले गई, दीपक-पतंग की तरह मैं उसके साथ रहा। अपनी ही इच्छा से अपने मुक्त जीवन-प्रसंग का प्रांगण छोड़ प्रेम की सीमित, पर दृढ़ बाहों में सुरक्षित, बँध रहना उसने पसंद किया।
इच्छा न रहने पर भी प्रासंगिक काव्य, दर्शन, समाज राजनीति आदि की कुछ बातें चरित्रों के साथ व्यवहारिक जीवन की समस्या की तरह आ पड़ी हैं, वे अप्सरा के ही रूप-रुचि के अनुकूल हैं। उनसे पाठकों शिक्षा के तौर पर कुछ मिलता हो, अच्छी बात है; न मिलता हो, रहने दें; मैं अपनी तरफ़ से केवल अप्सरा उनकी भेंट कर रहा हूँ।
मैंने किसी विचार से अप्सरा नहीं लिखी, किसी उद्देश्य की पुष्टि भी इसमें नहीं। अप्सरा स्वयं मुझे जिस-जिस ओर ले गई, दीपक-पतंग की तरह मैं उसके साथ रहा। अपनी ही इच्छा से अपने मुक्त जीवन-प्रसंग का प्रांगण छोड़ प्रेम की सीमित, पर दृढ़ बाहों में सुरक्षित, बँध रहना उसने पसंद किया।
इच्छा न रहने पर भी प्रासंगिक काव्य, दर्शन, समाज राजनीति आदि की कुछ बातें चरित्रों के साथ व्यवहारिक जीवन की समस्या की तरह आ पड़ी हैं, वे अप्सरा के ही रूप-रुचि के अनुकूल हैं। उनसे पाठकों शिक्षा के तौर पर कुछ मिलता हो, अच्छी बात है; न मिलता हो, रहने दें; मैं अपनी तरफ़ से केवल अप्सरा उनकी भेंट कर रहा हूँ।
एक
इडेन-गार्डेन में, कृत्रिम सरोवर के तट पर, एक कुंज के बीच, शाम सात बजे के करीब, जलते हुए एक प्रकाश-स्तंभ के नीचे पड़ी हुई एक कुर्सी पर सत्रह साल की चंपे की कली-सी एक किशोरी बैठी सरोवर की लहरों पर चमकती चाँद की किरणें और जल पर खुले हुए, काँपते, बिजली की बत्तियों के कमल के फूल एकचित्त से देख रही थी। और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई थी, पर इसका उसे खयाल न था।
युवती एकाएक चौंककर काँप उठी। उसी बेंच पर एक गोरा बिलकुल सटकर बैठ गया। युवती एक बगल हट गई। फिर कुछ सोचकर, इधर-उधर देख, घबराई हुई, उठकर खड़ी हो गई। गोरे ने हाथ पकड़कर जबरन बेंच पर बैठा लिया। युवती चीख उठी।
बाग में उस समय इक्के-दुक्के आदमी रह गए थे। युवती ने इधर-उधर देखा, पर कोई नजर न आया। भय से उसका कंठ भी रुक गया। अपने आदमियों को पुकारना चाहा, पर आवाज न निकली। गोरे ने उसे कसकर पकड़ लिया।
गोरा कुछ निश्छल प्रेम की बात कह रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कालर में उँगलियाँ घुसेड़ दीं, और गर्दन के पास कोट के साथ पकड़कर साहब को एक बित्ता बेंच से ऊपर उठा लिया, जैसे चूहे को बिल्ली। साहब के कब्जे से युवती छूट गई। साहब ने सिर घुमाया। आगंतुक ने दूसरे हाथ से युवती की तरफ सिर फेर दिया, अब कैसी लगती है ?
साहब झपटकर खड़ा हो गया। युवक ने कालर छोड़ते हुए जोर से सामने रेल दिया। एक पेड़ के सहारे साहब सँभल गया, फिरकर उसने देखा, एक युवक अकेला खड़ा है। साहब को अपनी वीरता का खयाल आया। टुम पीछे से हमको पकड़ा। कहते-कहते वह यूवक की ओर लपका। तो अभी दिल की मुराद पूरी नहीं हुई ? युवक तैयार हो गया। साहब को वॉक्सिंग (घूसेबाजी) का अभिमान था, युवक को कुश्ती का। साहब के वार करते ही यूवक ने कलाई पकड़ ली, और वहीं से बाँधकर बहल्ले में दे मारा, और छाती पर बैठ कई रद्दे कस दिए। साहब बेहोश हो गया। युवती खड़ी सविनय ताकती रही। युवक ने रुमाल भिगोकर साहब का मुँह पोंछ दिया। फिर उसी के सिर पर रख दिया। जेब से कागज निकाल बेंच के सहारे एक चिट्ठी लिखी, और साहब की जेब में रख दी। फिर युवती से पूछा, ‘‘आपको कहाँ जाना है ?’’
‘‘मेरी मोटर सड़क पर खड़ी है। उस पर मेरा ड्राइवर और बूढ़ा अर्दली बैठा होगा। मैं हवाखोरी के लिए आई थी। आपने मेरी रक्षा की मैं सदैव-सदैव आपकी कृतज्ञ रहूँगी !’’
युवक ने सिर झुका लिया।
‘‘अपका शुभ नाम ?’’ युवती ने पूछा।
‘‘नाम बतलाना अनावश्यक समझता हूँ। आप जल्द यहाँ से चली जाएँ।’’
युवक को कृतज्ञता की सजल दृष्टि से देखती हुई युवती चल दी। रुककर कुछ कहना चाहा, पर कह न सकी। युवती फील्ड के फाटक की ओर चली, युवक हाईकोर्ट की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद युवती फिर लौटी। युवक नज़र से बाहर हो गया था। वह गई, और साहब की जेब से चिट्ठी निकालकर चुपचाप चली आई।
युवती एकाएक चौंककर काँप उठी। उसी बेंच पर एक गोरा बिलकुल सटकर बैठ गया। युवती एक बगल हट गई। फिर कुछ सोचकर, इधर-उधर देख, घबराई हुई, उठकर खड़ी हो गई। गोरे ने हाथ पकड़कर जबरन बेंच पर बैठा लिया। युवती चीख उठी।
बाग में उस समय इक्के-दुक्के आदमी रह गए थे। युवती ने इधर-उधर देखा, पर कोई नजर न आया। भय से उसका कंठ भी रुक गया। अपने आदमियों को पुकारना चाहा, पर आवाज न निकली। गोरे ने उसे कसकर पकड़ लिया।
गोरा कुछ निश्छल प्रेम की बात कह रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कालर में उँगलियाँ घुसेड़ दीं, और गर्दन के पास कोट के साथ पकड़कर साहब को एक बित्ता बेंच से ऊपर उठा लिया, जैसे चूहे को बिल्ली। साहब के कब्जे से युवती छूट गई। साहब ने सिर घुमाया। आगंतुक ने दूसरे हाथ से युवती की तरफ सिर फेर दिया, अब कैसी लगती है ?
साहब झपटकर खड़ा हो गया। युवक ने कालर छोड़ते हुए जोर से सामने रेल दिया। एक पेड़ के सहारे साहब सँभल गया, फिरकर उसने देखा, एक युवक अकेला खड़ा है। साहब को अपनी वीरता का खयाल आया। टुम पीछे से हमको पकड़ा। कहते-कहते वह यूवक की ओर लपका। तो अभी दिल की मुराद पूरी नहीं हुई ? युवक तैयार हो गया। साहब को वॉक्सिंग (घूसेबाजी) का अभिमान था, युवक को कुश्ती का। साहब के वार करते ही यूवक ने कलाई पकड़ ली, और वहीं से बाँधकर बहल्ले में दे मारा, और छाती पर बैठ कई रद्दे कस दिए। साहब बेहोश हो गया। युवती खड़ी सविनय ताकती रही। युवक ने रुमाल भिगोकर साहब का मुँह पोंछ दिया। फिर उसी के सिर पर रख दिया। जेब से कागज निकाल बेंच के सहारे एक चिट्ठी लिखी, और साहब की जेब में रख दी। फिर युवती से पूछा, ‘‘आपको कहाँ जाना है ?’’
‘‘मेरी मोटर सड़क पर खड़ी है। उस पर मेरा ड्राइवर और बूढ़ा अर्दली बैठा होगा। मैं हवाखोरी के लिए आई थी। आपने मेरी रक्षा की मैं सदैव-सदैव आपकी कृतज्ञ रहूँगी !’’
युवक ने सिर झुका लिया।
‘‘अपका शुभ नाम ?’’ युवती ने पूछा।
‘‘नाम बतलाना अनावश्यक समझता हूँ। आप जल्द यहाँ से चली जाएँ।’’
युवक को कृतज्ञता की सजल दृष्टि से देखती हुई युवती चल दी। रुककर कुछ कहना चाहा, पर कह न सकी। युवती फील्ड के फाटक की ओर चली, युवक हाईकोर्ट की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद युवती फिर लौटी। युवक नज़र से बाहर हो गया था। वह गई, और साहब की जेब से चिट्ठी निकालकर चुपचाप चली आई।
दो
कनक धीरे-धीरे अठारहवें वर्ष के पहले चरण में आ पड़ी। अपार अलौकिक सौंदर्य, एकांत में, कभी-कभी अपनी मनोहर रागिनी सुना जाता। वह कान लगा उसके अमृत-स्वर को सुनती पान किया करती। अज्ञात एक अपूर्व आनन्द का प्रवाह अंगों को अपाद-मस्तक नहला जाता। स्नेह की विद्युल्लता काँप उठती। उस अपरिचित कारण की तलाश में विस्मय से आकाश की ओर ताककर रह जाती। कभी-कभी खिले हुए अंगों के स्नेहभार में एक स्पर्श मिलता, जैसे अशरीर उसकी आत्मा में कोई प्रवेश कर रहा हो। उस गुदगुदी में उसके तमाम अंग काँपकर खिल उठते। अपनी देह के वृंत अपलक खिली हुई ज्योत्स्ना के चंद्र-पुष्प की तरह, सौंदर्योज्ज्वल पारिजात की तरह एक अज्ञात प्रणय की वायु डोल उठती। आँखों में प्रश्न फूट पड़ता, संसार के रहस्यों के प्रति विस्मय।
कनक गंधर्व-कुमारिका थी। उसकी माता सर्वेश्वरी बनारस की रहनेवाली थी। नृत्य-संगीत में वह भारत प्रसिद्ध हो चुकी थी। बड़े-बड़े राजे-महाराजे जल्से में उसे बुलाते, उसकी बड़ी आवभगत करते। इस तरह सर्वेश्वरी ने अपार संपत्ति एकत्र कर ली थी। उसने कलकत्ता-बहूबाजार में आलीशान अपना एक खास मकान बनवा लिया था, और व्यवसाय की वृद्धि के लिए, उपार्जन की सुविधा के विचार से, प्रायः वहीं रहती भी थी। सिर्फ बुढ़वा-मंगल के दिनों, तवायफों तथा रईसों पर अपने नाम की मुहर मार्जित कर लेने के विचार से, काशी-आवास करती थी। वहाँ भी उसकी एक कोठी थी।
सर्वेश्वरी की इस अथाह सम्पत्ति की नाव पर एकमात्र उसकी कन्या कनक ही कर्णधार थी, इसलिए कनक में सब तरफ से ज्ञान का थोड़ा-थोड़ा प्रकाश भर देना—भविष्य के सुखपूर्वक निर्वाह के लिए, अपनी नाव खेने की सुविधा के लिए, उसने आवश्यक समझ लिया था। वह जानती थी, कनक अब कली नहीं, उसके अंगों के कुल दल खुल गए हैं। उसके हृदय के चक्र में चारों ओर के सौंदर्य का मधु भर गया है। पर उसकी लक्ष्य उसकी शिक्षा की तरफ था। अभी तक उसने उसका जातीय शिक्षा का भार अपने हाथों में नहीं लिया। अभी दृष्टि से ही वह कनक को प्यार कर लेती, उपदेश दे देती थी। कार्यतः उसकी तरफ से अलग थी। कभी-कभी जब व्यवसाय और व्यवसायियों से फुर्सत मिलती, वह कुछ देर के लिए कनक को बुला लिया करती। और, हर तरफ से उसने कन्या के लिए स्वतंत्र प्रबंध कर रखा था। उसके पढ़ने का घर ही में इंतजाम कर दिया था। एक अँगरेज-महिला, श्रीमती कैथरिन, तीन घंटे उसे पढ़ा जाया करती थीं। दो घंटे के लिए एक अध्यापक आया करते थे।
इस तरह वह शुभ्र-स्वच्छ निर्झरिणी विद्या के ज्योत्स्ना-लोक के भीतर से मुखर शब्द-कलरव करती हुई ज्ञान के समुद्र की ओर अबाध बह चली। हिंदी के अध्यापक उसे पढ़ाते हुए अपनी अर्थ प्राप्ति की कलुषित कामना पर पश्चाताप करते, कुशाग्रबुद्धि शिष्या के भविष्य का पंकिल चित्र खींचते हुए मन-ही-मन सोचते, इसकी पढ़ाई ऊपर वर्षा है—तलवार में ज्ञान, नागिन का दूध पीना। इसका काटा हुआ एक कदम भी नहीं चल सकता। पर नौकरी छोड़ने की चिन्ता-मात्र से व्याकुल हो उठते थे। उसकी अँग्रेजी की आचार्या उसे बाइबिल पढ़ाती हुई बड़ी एकाग्रता से देखती, और मन-ही-मन निश्चय करती थी कि किसी दिन उसे प्रभु ईसा की शरण में लाकर कृतार्थ कर देगी। कनक भी अँग्रेजी में जैसी तेज थी, उसे अपनी सफलता पर जरा द्विधा न थी। उसकी माता सोचती, इसके हृदय को जिन तारों से बाँधकर मैं इसे सजाऊँगी, उनके स्वर-झंकार से एक दिन संसार के लोग चकित हो जाएँगे; इसके द्वारा अप्सरा-लोक में एक नया ही परिवर्तन कर दूँगी, और वह केवल एक ही अंग में नहीं, चारों तरफ; मकान के सभी शून्य छिद्रों को जैसे प्रकाश और वायु भरते रहते हैं, आत्मा का एक ही समुद्र जैसे सभी प्रवाहों का चरण परिणाम है।
इस समय कनक अपनी सुगंध से आप ही आश्चर्यचकित हो रही थी। अपने बालपन की बालिका तन्वी कवयित्री को चारों ओर केवल कल्पना का आलोक देख पड़ता था, उसने अभी उसकी किरण-तंतुओं से जाल बुनना नहीं सीखा था। काव्य था, पर शब्द-रचना नहीं—जैसे उस प्रकाश में उसकी तमाम प्रगतियाँ फँस गई हों, जैसे इस अवरोध से बाहर निकलने की वह राह न जानती हो। वहीं उसका सबसे बड़ा सौंदर्य उसमें एक अतुल नैसर्गिक विभूति थी। संसार के कुल मनुष्य और वस्तुएँ उसकी दृष्टि में मरीचिका के ज्योति-चित्रों की तरह आतीं, अपने यथार्थ स्वरूप में नहीं।
कनक की दिनचर्या बहुत साधारण थी। जो दासियाँ उसकी देख-रेख के लिए थीं, पर उन्हें प्रतिदिन दो बार उसे नहला देने और तीन-चार बार वस्त्र बदलवा देने के इंतजाम में ही जो कुछ थोड़ा-सा काम था, बाकी समय यों ही कटता था। कुछ समय साड़ियाँ चुनने में लग जाता था। कनक प्रतिदिन शाम को मोटर पर किले के मैदान की तरफ निकलती थी। ड्राइवर के बगल में एक अर्दली बैठता था। पीछे की सीट पर अकेली कनक। कनक प्रायः आभरण नहीं पहनती थी। कभी-कभी हाथों में सोने की चूड़ियाँ डाल लेती थी। गले में एक हीरे की कनी का जड़ाऊ हार। कानों में हीरे के दो चंपे पड़े रहते। संध्या-समय, सात बजे के बाद से दस बजे तक और दिन में भी इसी तरह सात से दस तक पढ़ती थी। भोजन-पान में बिलकुल सादगी, पर पुष्टिकारक भोजन उसे दिया जाता था।
कनक गंधर्व-कुमारिका थी। उसकी माता सर्वेश्वरी बनारस की रहनेवाली थी। नृत्य-संगीत में वह भारत प्रसिद्ध हो चुकी थी। बड़े-बड़े राजे-महाराजे जल्से में उसे बुलाते, उसकी बड़ी आवभगत करते। इस तरह सर्वेश्वरी ने अपार संपत्ति एकत्र कर ली थी। उसने कलकत्ता-बहूबाजार में आलीशान अपना एक खास मकान बनवा लिया था, और व्यवसाय की वृद्धि के लिए, उपार्जन की सुविधा के विचार से, प्रायः वहीं रहती भी थी। सिर्फ बुढ़वा-मंगल के दिनों, तवायफों तथा रईसों पर अपने नाम की मुहर मार्जित कर लेने के विचार से, काशी-आवास करती थी। वहाँ भी उसकी एक कोठी थी।
सर्वेश्वरी की इस अथाह सम्पत्ति की नाव पर एकमात्र उसकी कन्या कनक ही कर्णधार थी, इसलिए कनक में सब तरफ से ज्ञान का थोड़ा-थोड़ा प्रकाश भर देना—भविष्य के सुखपूर्वक निर्वाह के लिए, अपनी नाव खेने की सुविधा के लिए, उसने आवश्यक समझ लिया था। वह जानती थी, कनक अब कली नहीं, उसके अंगों के कुल दल खुल गए हैं। उसके हृदय के चक्र में चारों ओर के सौंदर्य का मधु भर गया है। पर उसकी लक्ष्य उसकी शिक्षा की तरफ था। अभी तक उसने उसका जातीय शिक्षा का भार अपने हाथों में नहीं लिया। अभी दृष्टि से ही वह कनक को प्यार कर लेती, उपदेश दे देती थी। कार्यतः उसकी तरफ से अलग थी। कभी-कभी जब व्यवसाय और व्यवसायियों से फुर्सत मिलती, वह कुछ देर के लिए कनक को बुला लिया करती। और, हर तरफ से उसने कन्या के लिए स्वतंत्र प्रबंध कर रखा था। उसके पढ़ने का घर ही में इंतजाम कर दिया था। एक अँगरेज-महिला, श्रीमती कैथरिन, तीन घंटे उसे पढ़ा जाया करती थीं। दो घंटे के लिए एक अध्यापक आया करते थे।
इस तरह वह शुभ्र-स्वच्छ निर्झरिणी विद्या के ज्योत्स्ना-लोक के भीतर से मुखर शब्द-कलरव करती हुई ज्ञान के समुद्र की ओर अबाध बह चली। हिंदी के अध्यापक उसे पढ़ाते हुए अपनी अर्थ प्राप्ति की कलुषित कामना पर पश्चाताप करते, कुशाग्रबुद्धि शिष्या के भविष्य का पंकिल चित्र खींचते हुए मन-ही-मन सोचते, इसकी पढ़ाई ऊपर वर्षा है—तलवार में ज्ञान, नागिन का दूध पीना। इसका काटा हुआ एक कदम भी नहीं चल सकता। पर नौकरी छोड़ने की चिन्ता-मात्र से व्याकुल हो उठते थे। उसकी अँग्रेजी की आचार्या उसे बाइबिल पढ़ाती हुई बड़ी एकाग्रता से देखती, और मन-ही-मन निश्चय करती थी कि किसी दिन उसे प्रभु ईसा की शरण में लाकर कृतार्थ कर देगी। कनक भी अँग्रेजी में जैसी तेज थी, उसे अपनी सफलता पर जरा द्विधा न थी। उसकी माता सोचती, इसके हृदय को जिन तारों से बाँधकर मैं इसे सजाऊँगी, उनके स्वर-झंकार से एक दिन संसार के लोग चकित हो जाएँगे; इसके द्वारा अप्सरा-लोक में एक नया ही परिवर्तन कर दूँगी, और वह केवल एक ही अंग में नहीं, चारों तरफ; मकान के सभी शून्य छिद्रों को जैसे प्रकाश और वायु भरते रहते हैं, आत्मा का एक ही समुद्र जैसे सभी प्रवाहों का चरण परिणाम है।
इस समय कनक अपनी सुगंध से आप ही आश्चर्यचकित हो रही थी। अपने बालपन की बालिका तन्वी कवयित्री को चारों ओर केवल कल्पना का आलोक देख पड़ता था, उसने अभी उसकी किरण-तंतुओं से जाल बुनना नहीं सीखा था। काव्य था, पर शब्द-रचना नहीं—जैसे उस प्रकाश में उसकी तमाम प्रगतियाँ फँस गई हों, जैसे इस अवरोध से बाहर निकलने की वह राह न जानती हो। वहीं उसका सबसे बड़ा सौंदर्य उसमें एक अतुल नैसर्गिक विभूति थी। संसार के कुल मनुष्य और वस्तुएँ उसकी दृष्टि में मरीचिका के ज्योति-चित्रों की तरह आतीं, अपने यथार्थ स्वरूप में नहीं।
कनक की दिनचर्या बहुत साधारण थी। जो दासियाँ उसकी देख-रेख के लिए थीं, पर उन्हें प्रतिदिन दो बार उसे नहला देने और तीन-चार बार वस्त्र बदलवा देने के इंतजाम में ही जो कुछ थोड़ा-सा काम था, बाकी समय यों ही कटता था। कुछ समय साड़ियाँ चुनने में लग जाता था। कनक प्रतिदिन शाम को मोटर पर किले के मैदान की तरफ निकलती थी। ड्राइवर के बगल में एक अर्दली बैठता था। पीछे की सीट पर अकेली कनक। कनक प्रायः आभरण नहीं पहनती थी। कभी-कभी हाथों में सोने की चूड़ियाँ डाल लेती थी। गले में एक हीरे की कनी का जड़ाऊ हार। कानों में हीरे के दो चंपे पड़े रहते। संध्या-समय, सात बजे के बाद से दस बजे तक और दिन में भी इसी तरह सात से दस तक पढ़ती थी। भोजन-पान में बिलकुल सादगी, पर पुष्टिकारक भोजन उसे दिया जाता था।
तीन
धीरे-धीरे, ऋतुओं के सोने के पंख फड़का, एक साल और उड़ गया। मन के खिलते हुए प्रकाश के अनेक झरने उसकी कमल-सी आँखों से होकर बह गए। पर अब उसके मुख से आश्चर्य की जग-ज्ञान की मुद्रा चित्रित हो जाती । वह स्वयं अब अपने भविष्य के तट पर तूलिका चला लेती है। साल-भर से माता के पास उसे नृत्य और संगीत की शिक्षा मिल रही है। इधर उसकी उन्नति के चपल क्रम को देख सर्वेश्वरी पहले की कल्पना की अपेक्षा शिक्षा के पथ पर उसे और दूर तक ले चलने का विचार करने लगी, और गंधर्व जाति के छूटे हुए पूर्व गौरव को स्पर्द्धा से प्राप्त करने के लिए उसे उत्साह भी दिया करती थी। कनक अपलक ताकती हुई माता के वाक्यों को सप्रमाण सिद्ध करने का मन-ही-मन निश्चय करती, पतिज्ञाएँ करती। माता ने उसे सिखलाया, ‘‘किसी को प्यार मत करना। हमारे लिए प्यार करना आत्मा की कमजोरी है, यह हमारा धर्म नहीं।’’
कनक ने अस्फुट वाणी में मन-ही-मन प्रतिज्ञा की, ‘‘किसी को प्यार नहीं करूँगी। यह हमारे लिए आत्मा की कमजोरी है, धर्म नहीं।’’
माता ने कहा, ‘‘संसार के और लोग भीतर से प्यार करते हैं, हम लोग बाहर से।’’
कनक ने निश्चय किया, ‘‘और लोग भीतर से प्यार करते हैं, मैं बाहर से करूँगी।’’
माता ने कहा, ‘‘हमारी जैसी स्थिति है, इस पर ठहरकर भी हम लोक में वैसी ही विभूति, वैसा ही ऐश्वर्य, वैसा ही सम्मान अपनी कला के प्रदर्शन से प्राप्त कर सकती है; साथ ही, जिस आत्मा को और लोग अपने सर्वस्व का त्याग कर प्राप्त करते हैं, उसे भी हम लोग अपनी कला के उत्कर्ष द्वारा, उसी में प्राप्त करती हैं उसी में लीऩ होना हमारी मुक्ति है। जो आत्मा सभी सृष्टियों का सूक्ष्मतम तंतु की तरह उनके प्राणों के प्रियतम संगीत को झंकृत करती, जिसे लोग बाहर के कुल संबंधों को छोड़, ध्वनि के द्वारा तन्मय हो प्राप्त करते, उसे हम अपने बाह्य यंत्र के तारों से झंकृत कर, मूर्ति में लगा लेतीं, फिर अपने जलते हुए प्राणों का गरल, उसी शिव को, मिलकर पिला देती हैं। हमारी मुक्ति इस साधना द्वारा होती है, इसीलिए ऐश्वर्य पर हमारा सदा ही अधिकार रहता है। हम बाहर से जितनी सुंदर, भीतर से उतनी ही कठोर इसीलिए हैं। और लोग बाहर से कठोर, पर भीतर से कोमल हुआ करते हैं, इसलिए वे हमें पहचान नहीं पाते और अपने सर्वस्व तक का दान कर हमें पराजित करना चाहते हैं। हमारे प्रेम को प्राप्त कर, जिस पर केवल हमारे कौशल के शिव का ही एकाधिकार है, जब हम लोग अपने इस धर्म के गर्त से, मौखरिए की रागिनी सुन मुग्ध हुई नागिन की तरह, निकल पड़ती हैं, तब हमारे महत्त्व के प्रति भी हमें कलंकित अहल्या की तरह शाप से बाँध, पतित कर चले जाते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के सुखमय विहार को छोड़ मौखरिए की संकीर्ण टोकरी में बंद हो जाती हैं, फिर वही हमें इच्छानुसार नचाता, अपनी स्वतंत्र इच्छा के वश में हमें गुलाम बना लेता है। अपनी बुनियाद पर इमारत की तरह तुम्हें अटल रहना होगा, नहीं तो फिर अपनी स्थिति से ढह जाओगी, बह जाओगी।’’
कनक के मन में होठ काँपकर रह गए, ‘‘अपनी बुनियाद में इमारत की तरह अटल रहूँगी !
कनक ने अस्फुट वाणी में मन-ही-मन प्रतिज्ञा की, ‘‘किसी को प्यार नहीं करूँगी। यह हमारे लिए आत्मा की कमजोरी है, धर्म नहीं।’’
माता ने कहा, ‘‘संसार के और लोग भीतर से प्यार करते हैं, हम लोग बाहर से।’’
कनक ने निश्चय किया, ‘‘और लोग भीतर से प्यार करते हैं, मैं बाहर से करूँगी।’’
माता ने कहा, ‘‘हमारी जैसी स्थिति है, इस पर ठहरकर भी हम लोक में वैसी ही विभूति, वैसा ही ऐश्वर्य, वैसा ही सम्मान अपनी कला के प्रदर्शन से प्राप्त कर सकती है; साथ ही, जिस आत्मा को और लोग अपने सर्वस्व का त्याग कर प्राप्त करते हैं, उसे भी हम लोग अपनी कला के उत्कर्ष द्वारा, उसी में प्राप्त करती हैं उसी में लीऩ होना हमारी मुक्ति है। जो आत्मा सभी सृष्टियों का सूक्ष्मतम तंतु की तरह उनके प्राणों के प्रियतम संगीत को झंकृत करती, जिसे लोग बाहर के कुल संबंधों को छोड़, ध्वनि के द्वारा तन्मय हो प्राप्त करते, उसे हम अपने बाह्य यंत्र के तारों से झंकृत कर, मूर्ति में लगा लेतीं, फिर अपने जलते हुए प्राणों का गरल, उसी शिव को, मिलकर पिला देती हैं। हमारी मुक्ति इस साधना द्वारा होती है, इसीलिए ऐश्वर्य पर हमारा सदा ही अधिकार रहता है। हम बाहर से जितनी सुंदर, भीतर से उतनी ही कठोर इसीलिए हैं। और लोग बाहर से कठोर, पर भीतर से कोमल हुआ करते हैं, इसलिए वे हमें पहचान नहीं पाते और अपने सर्वस्व तक का दान कर हमें पराजित करना चाहते हैं। हमारे प्रेम को प्राप्त कर, जिस पर केवल हमारे कौशल के शिव का ही एकाधिकार है, जब हम लोग अपने इस धर्म के गर्त से, मौखरिए की रागिनी सुन मुग्ध हुई नागिन की तरह, निकल पड़ती हैं, तब हमारे महत्त्व के प्रति भी हमें कलंकित अहल्या की तरह शाप से बाँध, पतित कर चले जाते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के सुखमय विहार को छोड़ मौखरिए की संकीर्ण टोकरी में बंद हो जाती हैं, फिर वही हमें इच्छानुसार नचाता, अपनी स्वतंत्र इच्छा के वश में हमें गुलाम बना लेता है। अपनी बुनियाद पर इमारत की तरह तुम्हें अटल रहना होगा, नहीं तो फिर अपनी स्थिति से ढह जाओगी, बह जाओगी।’’
कनक के मन में होठ काँपकर रह गए, ‘‘अपनी बुनियाद में इमारत की तरह अटल रहूँगी !
चार
अखबारों के बड़े-बड़े अक्षरों में सूचना निकली :
शकुंतला ! शकुंतला !! शकुंतला !!!
शकुंतला मिस कनक
दुष्यंत राजकुमार वर्मा, एम्. ए.
प्रशंसा में और भी बड़े-बड़े आकर्षक शब्द लिए हुए थे। थिएटर-शौकीनों को हाथ बढ़ाकर स्वर्ग मिला। वे लोग थिएटर का तमाम इतिहास कंठाग्र रखते थे। जितने भी ऐक्टर (अभिनेता) और छोटी-छोटी जितनी भी मशहूर ऐक्ट्रेस (अभिनेत्रियाँ) थीं, उन्हें सबके नाम मालूम थे, सबकी सूरतें पहचानते थे, पर यह मिस कनक अपरिचित थी। विज्ञापन के नीचे कनक की तारीफ भी खूब की गई थी। लोग टिकट खरीदने के लिए उतावले हो गए। टिकट-घर के सामने अपार भीड़ लग गई, जै़से आदमियों का सागर तरंगित हो रहा हो। एक-एक झोंके से बाढ़ के पानी की तरह वह जनसमुद्र इधर-से-उधर डोल उठता था। बॉक्स, आर्केस्ट्रा, फर्स्ट क्लास में भी और और दिनों से ज्यादा भीड़ थी।
विजयपुर के कुँअर साहब भी उन दिनों कलकत्ते की सैर कर रहे थे। इन्हें स्टेट से छः हजार मासिक जेब-खर्च मिलता था। वह सब नई रोशनी, नए फैशन में फूँककर ताप लेते थे। आपने भी एक बॉक्स किराए पर लिया। थिएटर की मिसों की प्रायः आपकी कोठी में दावत होती थी, और तरह-तरह के तोहफे आप उनके मकान पहुँचा दिया करते थे। संगीत का आपको अजहद शौक था। खुद भी गाते थे, पर आवाज जैसे ब्रह्मभोज के पश्चात कड़ाह रगड़ने की। लोग इस पर भी कहते थे, क्या मँजी हुई आवाज है ! आपको भी मिस कनक का पता मालूम न था। इससे और उतावले हो रहे थे। जैसे ससुराल जा रहे हों, और स्टेशन के पास गाड़ी पहुँच गई हो।
देखते-देखते संध्या के छः का समय हुआ। थियेटर-गेट के सामने पान खाते, सिगरेट पीते, हँसी-मजाक करते हुए बड़ी-बड़ी तोंदवाले सेठ छड़ियाँ चमकाते, सुनहली डंडी का चश्मा लगाए हुए कॉलेज के छोकरे, अंग्रेजी अखबारों की एक-एक प्रति लिए हुए हिंदी के संपादक सहकारियों पर अपने अपार ज्ञान का बुखार उतारते हुए, पहले ही से कला की कसौटी पर अभिनय की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हुए टहल रहे थे। इन सब बाहरी दिखलावों के अंदर सबके मन की आँखें मिसों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके चकित दर्शन, चंचल चलन को देखकर चरितार्थ होना चाहती थीं। जहाँ बड़े-बड़े आदमियों का यह हाल था, वहाँ थर्ड क्लास तिमंजले पर फटी-हालत नंगे-बदन, रूखी सूरत, बैठे हुए बीड़ी-सिगरेट के धुएँ से छत भर देने वाले मौके-बेमौके तालियाँ पीटते हुए, ‘इनकोर-इनकोर’ के अप्रतिहत शब्द से कानों के पर्दे पार कर देनेवाले, अशिष्ट, मुँहफट, कुली-क्लास के लोगों का बयान ही क्या ? वहीं इन धन-कुबेरों और संवाद-पत्रों के सर्वज्ञों, वकीलों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के साथ ये लोग भी कला के प्रेम में साम्यवाद के अधिकारी हो रहे थे।
देखते-देखते एक लारी आई। लोगों की निगाह तमाम बाधाओं को चीरती हुई, हवा की गोली की तरह, निशाने पर जा बैठी। पर, उस समय गाड़ी से उतरने पर, वे जितनी—मिस डली, मिस कुंदन, मिस हीरा, पन्ना, पुखराज, रमा, क्षमा, शांति, शोभा, किसमिस और अंगूर-बालाएँ—थीं, जिनमें किसी ने हिरन की चाल दिखाई, किसी ने मोर की, किसी ने नागिन-जैसी-सब-की-सब जैसे डामर से पुती, अफ्रीका से हाल ही आई, प्रोफेसर डीवर या मिस्टर चटर्जी की सिद्ध की हुई, हिंदुस्तान की आदिम जाति की ही कन्याएँ और बहने थीं, और ये सब इतने बड़े-बड़े लोग इन्हें ही कला की दृष्टि से देख रहे थे। कोई छः फिट ऊँची, तिस पर नाक नदारद। कोई डेढ़ ही हाथ की छटंकी, पर होठ आँखों की उपमा लिए हुए आकर्ण-विस्तृत। किसी की साढ़े तीन हाथ लम्बाई चौड़ाई में बदली हुई—एक-एक कदम पर पृथ्वी काँप उठती। किसी की आँखें मक्खियों-सी छोटी और गालों में तबले मढ़े हुए। किसी की उम्र का पता नहीं शायद सन् 57 के गदर में मिस्टर हडसन को गोद खिलाया हो। इस पर ऐसी दुलकी चाल सबने दिखाई, जैसे भुलभुल में पैर पड़े रहे हों। गेट के भीतर चले जाने के कुछ सेकेंड बाद तक जनता तृष्णा की विस्तृत अपार आँखों से कला के उस अप्राप्य अमृत का पान करती रही।
कुछ देर बाद एक प्राइवेट मोटर आई। बिना किसी इंगित के ही जनता की क्षुब्ध तरंग शांत हो गई। सब लोगों के अंग रूप की तड़ित् से प्रहत निश्चेष्ट रह गए। सर्वेश्वरी का हाथ पकड़े हुए कनक मोटर से उतर रही थी। सबकी आँखों के संध्याकाश में जैसे सुंदर इंद्र-धनुष अंकित हो गया हो। सबने देखा, मूर्तिमती प्रभात की किरण है।
उस दिन घर से अपने मन के अनुसार सर्वेश्वरी उसे सजा लाई थी। धानी रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथों में सोने की, रोशनी से चमकती हुई चूड़ियाँ; गले में हीरे का हार; कानों में चंपा; रेशमी फीते से बँधे तरंगित, खुले लंबे बाल; स्वस्थ, सुंदर देह; कान तक खिंची, किसी की खोज-सी करती हुई बड़ी-बड़ी आँखें; काले रंग से कुछ स्याह कर तिरछाई हुई भौंहें। लोग स्टेज की अभिनेत्री शकुंतला को मिस कनक के रूप में अपलक नेत्रों से देख रहे थे।
लोगों के मनोभावों को समझकर सर्वेश्वरी देर कर रही थी। मोटर से सामान उतरवाने, ड्राइवर को मोटर लाने का वक्त बतलाने, नौकर को कुछ भूला हुआ सामान मकान से ले आने की आज्ञा देने में लगी रही। फिर धीरे-धीरे कनक का हाथ पकड़े हुए, अपनी अर्दली के साथ, ग्रीन-रूम की तरफ चली गई।
लोग जैसे स्वप्न देखकर जागे। फिर चहल-पहल मच गई। लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। धन-कुबेर सेठ दूसरे परिचितों से आँखों के इशारे करने लगे। इन्हीं लोगों में विजयपुर के कुँवर साहब भी थे। और, न जाने कौन-कौन-से राजे-महाराजे सौंदर्य के समुद्र से अतंद्र अम्लान निकली हुई इस अप्सरा की कृपा-दृष्टि के भिक्षुक हो रहे थे।
जिस समय कनक खड़ी थी, कुँवर साहब अपनी आँखों से नहीं, खुर्दबीन की आँखों से उसके बृहत् रूप के अंश में अपने को सबसे बड़ा हक़दार साबित कर रहे थे, और इस कार्य में उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा था। कनक उस समय मुस्किरा रही थी।
भीड़ तितर-बितर होने लगी। खेल आरंभ होने में पौन घण्टा और रह गया। लोग पानी, पान, सोडा-लेमनेड आदि खाने-पीने में लग गए। कुछ लोग बीड़ियाँ फूँकते हुए खुली, असभ्य भाषा में कनक की आलोचना कर रहे थे।
ग्रीन-रूम में अभिनेत्रियाँ सज रही थीं। कनक नौकर नहीं थी, उसकी माँ भी नौकर नहीं थी। उसकी माँ उसे स्टेज पर पूर्णिमा के चाँद की तरह एक ही रात में लोगों की दृष्टि में खोलकर प्रसिद्ध कर देना चाहती थी। थिएटर के मालिक पर उसका काफी प्रभाव था। साल में कई बार उसी स्टेज पर, टिकट ज्यादा बिकने के लोभ से, थिएटर के मालिक उसे गाने तथा अभिनय करने के लिए बुलाते थे। वह जिस रोज स्टेज पर उतरती, रंगशाला दर्शक-मंडली से भर जाती। कनक रिहर्सल में कभी नहीं गई, यह भार उसकी माता ने ले लिया था।
कनक को शकुंतला का वेश पहनाया जाने लगा। उसके कपड़े उतार दिए गए। एक साधारण-सा वस्त्र, वल्कन की जगह, पहना दिया गया। गले में फूलों का हार। बाल अच्छी तरह खोल दिए गए। उसकी सखियाँ अनुंसूया और प्रियंवदा भी सज गईं। उधर राजकुमार को दुष्यंत का वेश पहनाया जाने लगा। और और पात्र भी सजाकर तैयार कर दिए गए।
राजकुमार भी कंपनी में नौकर नहीं था। वह शौकिया बड़ी-बड़ी कंपनियों में उतरकर प्रधान पार्ट किया करता था। इसका कारण खुद मित्रों से बयान किया करता। कहा करता था, हिंदी के स्टेज पर लोग ठीक-ठीक हिंदी-उच्चारण नहीं करते, उर्दू के उच्चारण की नकल करते हैं, इससे हिंदी का उच्चारण बिगड़ जाता है। हिंदी के उच्चारण में जीभ की स्वतंत्र गति होती है। यह हिंदी ही की शिक्षा के द्वारा दुरुस्त होगी। कभी-कभी हिंदी में वह स्वयं भी नाटक लिखा करता। यह शकुंतला-नाटक उसी की लिखा हुआ था। हिंदी की शुभकामनाओं से प्रेरित हो उसने विवाह भी नहीं किया। इससे घरवाले कुपित भी हुए थे, पर उसने परवां नहीं की। कलकत्ता-सिटी-कॉलेज में वह हिंदी का प्रोफेसर है। शरीर जैसा हृष्ट-पुष्ट, वैसा ही वह सुंदर और बलिष्ठ भी है। कलकत्ता की साहित्य-समितियाँ उसे अच्छी तरह पहचानती हैं।
शकुंतला ! शकुंतला !! शकुंतला !!!
शकुंतला मिस कनक
दुष्यंत राजकुमार वर्मा, एम्. ए.
प्रशंसा में और भी बड़े-बड़े आकर्षक शब्द लिए हुए थे। थिएटर-शौकीनों को हाथ बढ़ाकर स्वर्ग मिला। वे लोग थिएटर का तमाम इतिहास कंठाग्र रखते थे। जितने भी ऐक्टर (अभिनेता) और छोटी-छोटी जितनी भी मशहूर ऐक्ट्रेस (अभिनेत्रियाँ) थीं, उन्हें सबके नाम मालूम थे, सबकी सूरतें पहचानते थे, पर यह मिस कनक अपरिचित थी। विज्ञापन के नीचे कनक की तारीफ भी खूब की गई थी। लोग टिकट खरीदने के लिए उतावले हो गए। टिकट-घर के सामने अपार भीड़ लग गई, जै़से आदमियों का सागर तरंगित हो रहा हो। एक-एक झोंके से बाढ़ के पानी की तरह वह जनसमुद्र इधर-से-उधर डोल उठता था। बॉक्स, आर्केस्ट्रा, फर्स्ट क्लास में भी और और दिनों से ज्यादा भीड़ थी।
विजयपुर के कुँअर साहब भी उन दिनों कलकत्ते की सैर कर रहे थे। इन्हें स्टेट से छः हजार मासिक जेब-खर्च मिलता था। वह सब नई रोशनी, नए फैशन में फूँककर ताप लेते थे। आपने भी एक बॉक्स किराए पर लिया। थिएटर की मिसों की प्रायः आपकी कोठी में दावत होती थी, और तरह-तरह के तोहफे आप उनके मकान पहुँचा दिया करते थे। संगीत का आपको अजहद शौक था। खुद भी गाते थे, पर आवाज जैसे ब्रह्मभोज के पश्चात कड़ाह रगड़ने की। लोग इस पर भी कहते थे, क्या मँजी हुई आवाज है ! आपको भी मिस कनक का पता मालूम न था। इससे और उतावले हो रहे थे। जैसे ससुराल जा रहे हों, और स्टेशन के पास गाड़ी पहुँच गई हो।
देखते-देखते संध्या के छः का समय हुआ। थियेटर-गेट के सामने पान खाते, सिगरेट पीते, हँसी-मजाक करते हुए बड़ी-बड़ी तोंदवाले सेठ छड़ियाँ चमकाते, सुनहली डंडी का चश्मा लगाए हुए कॉलेज के छोकरे, अंग्रेजी अखबारों की एक-एक प्रति लिए हुए हिंदी के संपादक सहकारियों पर अपने अपार ज्ञान का बुखार उतारते हुए, पहले ही से कला की कसौटी पर अभिनय की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हुए टहल रहे थे। इन सब बाहरी दिखलावों के अंदर सबके मन की आँखें मिसों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके चकित दर्शन, चंचल चलन को देखकर चरितार्थ होना चाहती थीं। जहाँ बड़े-बड़े आदमियों का यह हाल था, वहाँ थर्ड क्लास तिमंजले पर फटी-हालत नंगे-बदन, रूखी सूरत, बैठे हुए बीड़ी-सिगरेट के धुएँ से छत भर देने वाले मौके-बेमौके तालियाँ पीटते हुए, ‘इनकोर-इनकोर’ के अप्रतिहत शब्द से कानों के पर्दे पार कर देनेवाले, अशिष्ट, मुँहफट, कुली-क्लास के लोगों का बयान ही क्या ? वहीं इन धन-कुबेरों और संवाद-पत्रों के सर्वज्ञों, वकीलों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के साथ ये लोग भी कला के प्रेम में साम्यवाद के अधिकारी हो रहे थे।
देखते-देखते एक लारी आई। लोगों की निगाह तमाम बाधाओं को चीरती हुई, हवा की गोली की तरह, निशाने पर जा बैठी। पर, उस समय गाड़ी से उतरने पर, वे जितनी—मिस डली, मिस कुंदन, मिस हीरा, पन्ना, पुखराज, रमा, क्षमा, शांति, शोभा, किसमिस और अंगूर-बालाएँ—थीं, जिनमें किसी ने हिरन की चाल दिखाई, किसी ने मोर की, किसी ने नागिन-जैसी-सब-की-सब जैसे डामर से पुती, अफ्रीका से हाल ही आई, प्रोफेसर डीवर या मिस्टर चटर्जी की सिद्ध की हुई, हिंदुस्तान की आदिम जाति की ही कन्याएँ और बहने थीं, और ये सब इतने बड़े-बड़े लोग इन्हें ही कला की दृष्टि से देख रहे थे। कोई छः फिट ऊँची, तिस पर नाक नदारद। कोई डेढ़ ही हाथ की छटंकी, पर होठ आँखों की उपमा लिए हुए आकर्ण-विस्तृत। किसी की साढ़े तीन हाथ लम्बाई चौड़ाई में बदली हुई—एक-एक कदम पर पृथ्वी काँप उठती। किसी की आँखें मक्खियों-सी छोटी और गालों में तबले मढ़े हुए। किसी की उम्र का पता नहीं शायद सन् 57 के गदर में मिस्टर हडसन को गोद खिलाया हो। इस पर ऐसी दुलकी चाल सबने दिखाई, जैसे भुलभुल में पैर पड़े रहे हों। गेट के भीतर चले जाने के कुछ सेकेंड बाद तक जनता तृष्णा की विस्तृत अपार आँखों से कला के उस अप्राप्य अमृत का पान करती रही।
कुछ देर बाद एक प्राइवेट मोटर आई। बिना किसी इंगित के ही जनता की क्षुब्ध तरंग शांत हो गई। सब लोगों के अंग रूप की तड़ित् से प्रहत निश्चेष्ट रह गए। सर्वेश्वरी का हाथ पकड़े हुए कनक मोटर से उतर रही थी। सबकी आँखों के संध्याकाश में जैसे सुंदर इंद्र-धनुष अंकित हो गया हो। सबने देखा, मूर्तिमती प्रभात की किरण है।
उस दिन घर से अपने मन के अनुसार सर्वेश्वरी उसे सजा लाई थी। धानी रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथों में सोने की, रोशनी से चमकती हुई चूड़ियाँ; गले में हीरे का हार; कानों में चंपा; रेशमी फीते से बँधे तरंगित, खुले लंबे बाल; स्वस्थ, सुंदर देह; कान तक खिंची, किसी की खोज-सी करती हुई बड़ी-बड़ी आँखें; काले रंग से कुछ स्याह कर तिरछाई हुई भौंहें। लोग स्टेज की अभिनेत्री शकुंतला को मिस कनक के रूप में अपलक नेत्रों से देख रहे थे।
लोगों के मनोभावों को समझकर सर्वेश्वरी देर कर रही थी। मोटर से सामान उतरवाने, ड्राइवर को मोटर लाने का वक्त बतलाने, नौकर को कुछ भूला हुआ सामान मकान से ले आने की आज्ञा देने में लगी रही। फिर धीरे-धीरे कनक का हाथ पकड़े हुए, अपनी अर्दली के साथ, ग्रीन-रूम की तरफ चली गई।
लोग जैसे स्वप्न देखकर जागे। फिर चहल-पहल मच गई। लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। धन-कुबेर सेठ दूसरे परिचितों से आँखों के इशारे करने लगे। इन्हीं लोगों में विजयपुर के कुँवर साहब भी थे। और, न जाने कौन-कौन-से राजे-महाराजे सौंदर्य के समुद्र से अतंद्र अम्लान निकली हुई इस अप्सरा की कृपा-दृष्टि के भिक्षुक हो रहे थे।
जिस समय कनक खड़ी थी, कुँवर साहब अपनी आँखों से नहीं, खुर्दबीन की आँखों से उसके बृहत् रूप के अंश में अपने को सबसे बड़ा हक़दार साबित कर रहे थे, और इस कार्य में उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा था। कनक उस समय मुस्किरा रही थी।
भीड़ तितर-बितर होने लगी। खेल आरंभ होने में पौन घण्टा और रह गया। लोग पानी, पान, सोडा-लेमनेड आदि खाने-पीने में लग गए। कुछ लोग बीड़ियाँ फूँकते हुए खुली, असभ्य भाषा में कनक की आलोचना कर रहे थे।
ग्रीन-रूम में अभिनेत्रियाँ सज रही थीं। कनक नौकर नहीं थी, उसकी माँ भी नौकर नहीं थी। उसकी माँ उसे स्टेज पर पूर्णिमा के चाँद की तरह एक ही रात में लोगों की दृष्टि में खोलकर प्रसिद्ध कर देना चाहती थी। थिएटर के मालिक पर उसका काफी प्रभाव था। साल में कई बार उसी स्टेज पर, टिकट ज्यादा बिकने के लोभ से, थिएटर के मालिक उसे गाने तथा अभिनय करने के लिए बुलाते थे। वह जिस रोज स्टेज पर उतरती, रंगशाला दर्शक-मंडली से भर जाती। कनक रिहर्सल में कभी नहीं गई, यह भार उसकी माता ने ले लिया था।
कनक को शकुंतला का वेश पहनाया जाने लगा। उसके कपड़े उतार दिए गए। एक साधारण-सा वस्त्र, वल्कन की जगह, पहना दिया गया। गले में फूलों का हार। बाल अच्छी तरह खोल दिए गए। उसकी सखियाँ अनुंसूया और प्रियंवदा भी सज गईं। उधर राजकुमार को दुष्यंत का वेश पहनाया जाने लगा। और और पात्र भी सजाकर तैयार कर दिए गए।
राजकुमार भी कंपनी में नौकर नहीं था। वह शौकिया बड़ी-बड़ी कंपनियों में उतरकर प्रधान पार्ट किया करता था। इसका कारण खुद मित्रों से बयान किया करता। कहा करता था, हिंदी के स्टेज पर लोग ठीक-ठीक हिंदी-उच्चारण नहीं करते, उर्दू के उच्चारण की नकल करते हैं, इससे हिंदी का उच्चारण बिगड़ जाता है। हिंदी के उच्चारण में जीभ की स्वतंत्र गति होती है। यह हिंदी ही की शिक्षा के द्वारा दुरुस्त होगी। कभी-कभी हिंदी में वह स्वयं भी नाटक लिखा करता। यह शकुंतला-नाटक उसी की लिखा हुआ था। हिंदी की शुभकामनाओं से प्रेरित हो उसने विवाह भी नहीं किया। इससे घरवाले कुपित भी हुए थे, पर उसने परवां नहीं की। कलकत्ता-सिटी-कॉलेज में वह हिंदी का प्रोफेसर है। शरीर जैसा हृष्ट-पुष्ट, वैसा ही वह सुंदर और बलिष्ठ भी है। कलकत्ता की साहित्य-समितियाँ उसे अच्छी तरह पहचानती हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book