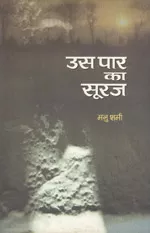|
लेख-निबंध >> उस पार का सूरज उस पार का सूरजमनु शर्मा
|
281 पाठक हैं |
||||||
मनु शर्मा जी के निबन्ध
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मनु शर्मा जी के इन निबन्धों में उनके व्यक्तित्व की सरसता
है, जीवन के अनेक क्षेत्रों के उनके अनुभव की गहराई है, उनके अगाध ज्ञान
की गरिमा है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी न ऊपर से ओढ़ दिखाई देते हैं और न
बलात ठूँसा ही लगता है। सब कुछ सहज और स्वाभाविक है। पाठकों को कहीं कथा
का रस आता है, कहीं सगुंफित विचारों की परत-दर-परत खुलने का आनन्द मिलता
है।
इसमें लेखन का चिन्तन, विचार आस्था इत्यादि उनकी संवेदनाओं में घुल-मिलकर आए हैं। जीवन की कोई घटना, कोई संदर्भ कोई कथा, कोई प्रतीक या सामान्य-असामान्य व्यक्ति लेखन के मन को उद्धेलित करता है और यही उद्धेलन लेखक के चिंतन का आधार बनता है। इस चिन्तन में उनके निजत्व के साथ देशी-विदेशी विचारक, पौराणिक संदर्भ पुराण-पुरूष, आर्ष ग्रंथ और कभी-कभी अति सामान्य पुरूष उभरता है। इसमें कहीं तत्त्व-चिंतन की गंभीर बातें हैं, कहीं कला का संबद्ध विचार हैं, कहीं पश्चात्य न्याय-दृष्टि से असहमति है, कहीं जीवन मूल्य की प्रतिष्ठा है, कहीं अन्धविश्वासों से असहमति है और कहीं आज के जीवन और समाज की गिरावट है। यानी कहीं गम्भीर और कहीं बड़ी बातें तो कहीं छोटी और सामान्य बातें है। उनके चिन्तन का ताना-बाना बहुत दूर तक फैला है।
इसमें लेखन का चिन्तन, विचार आस्था इत्यादि उनकी संवेदनाओं में घुल-मिलकर आए हैं। जीवन की कोई घटना, कोई संदर्भ कोई कथा, कोई प्रतीक या सामान्य-असामान्य व्यक्ति लेखन के मन को उद्धेलित करता है और यही उद्धेलन लेखक के चिंतन का आधार बनता है। इस चिन्तन में उनके निजत्व के साथ देशी-विदेशी विचारक, पौराणिक संदर्भ पुराण-पुरूष, आर्ष ग्रंथ और कभी-कभी अति सामान्य पुरूष उभरता है। इसमें कहीं तत्त्व-चिंतन की गंभीर बातें हैं, कहीं कला का संबद्ध विचार हैं, कहीं पश्चात्य न्याय-दृष्टि से असहमति है, कहीं जीवन मूल्य की प्रतिष्ठा है, कहीं अन्धविश्वासों से असहमति है और कहीं आज के जीवन और समाज की गिरावट है। यानी कहीं गम्भीर और कहीं बड़ी बातें तो कहीं छोटी और सामान्य बातें है। उनके चिन्तन का ताना-बाना बहुत दूर तक फैला है।
इन्हें पढ़ने के बाद
मनु शर्माजी जब निबंध-यात्रा पर निकलते हैं तब वह क्षेत्र भी उनका अपना
होता है। कथा लिखते समय जैसे अपने पात्रों के साथ वे जीते हैं, उनका
दुःख-सुख उनका होता है, वही स्थिति निबंधों के क्षेत्र में भी उनकी है। वे
निबंधों को जीते हैं, भोगते हैं और रस लेते हैं। भावना के क्षेत्र में
उनके ये निबंध उनके ‘अपने’ होते हुए भी
‘सबके’ लगते हैं।
इन निबंधों में शर्माजी के व्यक्तित्व की सरसता है, अनुभव की गहराई है, अगाध ज्ञान की गरिमा है, जीवन का संत्रास है और क्षणों की सुखानुभूति भी। अपनी निबंध यात्रा में उनका मन चेतना के न जाने कितने धरातल पर दस्तक देता है। सबकुछ सहज और स्वाभाविक है। पाठकों को कहीं कथा का रस आता है, तो कहीं संगुंफित विचारों के परत-दर परत खुलने का आनंद मिलता है।
पिछले-दस बारह वर्षों में लिखे गए ये निबंध अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं में छपे हैं। इनमें लेखक का चिंतन, विचार, आस्था इत्यादि उनकी संवेदनाओं में घुल-मिलकर आए हैं। जीवन की कोई घटना, कोई संदर्भ, कोई कथा, कोई प्रतीक या सामान्य-असामान्य व्यक्ति लेखक के मन को उद्वेलित करता है और यही उद्वेलन लेखक के चिंतन का आधार बनता है।
हिंदी में व्यक्ति-व्यंजक निबंधों और ललित निबंधों को लेकर भी गंभीर विवाद है। व्यक्ति-व्यंजक में निजत्व और ललित में लालित्य को लोग प्रधान मानते हैं। लेकिन ऐसा भेद करना पानी पर लकीर खींचना है। निजत्व ही ललित बनकर व्यक्त होता है। व्यक्ति-चेतना को केंद्र में रखकर निबंध लिखनेवालों में दो प्रकार के रचनाकार हैं-एक वे जो व्यक्ति-सापेक्षता को अपने जीवन के प्रसंगों, कथात्मकता और नाटकीयता से उभारते हैं; जैसे-पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त आदि। दूसरे प्रकार के वे निबंधकार हैं, जो निबंध में लालित्य को ही महत्त्व देते हैं। निजी जीवन के प्रसंग, सांस्कृतिक चेतना, लोक-तत्त्व प्रतीक, मिथक इत्यादि के द्वारा लालित्य प्रकट होता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंधों से लालित्य पर बल दिया जाने लगा। वे अपने चिंतन के फलक का विस्तार छायावादी कवियों के समान करते हैं। द्विवेदीजी का लालित्य अपने भावों या विचारों के उद्वेलन, संस्कृत छंदों के उद्धरण, प्रतीक अथवा मिथक की रचना करते हुए उत्पन्न होता है। उनके निबंधों में सर्वत्र भाव-प्रेरित लय है। ये निबंध कविता के समान स्वतःस्फूर्त हैं। द्विवेदीजी का कवि अकसर उनके गद्यकार पर बीस पड़ जाता है। पं. विद्यानिवास मिश्र अपनी वैयक्तिकता को लोक-चेतना और आधुनिक बोध से जोड़ते हैं। कुबेरनाथ राय इन निबंधकारों से अलग हैं। इनमें प्रतीकों और मिथकों को रचने की प्रवृत्ति है। कथा कहने की प्रवृत्ति, बहुज्ञता और जीवन के प्रति राग से वे पाठकों को अपनी ओर खींचते हैं।
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किसी घटना, किसी एक रोचक प्रसंग या किसी एक बात से निबंधों की शुरुआत करते हैं। नाटकीयता और कथात्मकता इनके निबंधों को रोचक बनाती है। सहजता इनकी एक अन्य विशेषता है। सियाराम शरण गुप्त ने भी अपने अपने निबंधों में छोटी-छोटी बातों को कहीं संस्मरण और कहीं व्यंग्य के माध्यम से कहा है। यह व्यक्ति-चेतना है। हिंदी में व्यक्ति-व्यंजक निबंध लिखनेवालों की ये दो परंपराएँ हैं। इन्हें व्यक्ति-व्यंजक और ललित कहकर अलग करना उचित नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। फिर भी अंग्रेजी के व्यक्ति-व्यंजक निबंधों से हिंदी के व्यक्ति-व्यंजक निबंधों की पहचान अलग है। अंग्रेजी के निबंधकारों की तरह अपने घर-परिवार, इष्ट-मित्र, पसंद-नापसंद का विवरण हिंदी के निबंधकार नहीं देते हैं। वे चुटकी लेते हैं, व्यंग्य करते हैं, किसी विश्वस्त और निकट व्यक्ति की तरह बात करते हैं।
मनु शर्मा के ये निबंध हजारीप्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र के निबंधों से हटकर हैं। उनकी निजता अपने निबंधों में अधिक खुलती है। वे अपनी बेबसी, अंतर्विरोध आदि को भी कहते हैं। घर-परिवार, पास-पड़ोस, परिचित-अल्पपरिचित के संदर्भ इन निबंधों में हैं। कथात्मक और नाटकीयता इन संदर्भों को आकर्षक बना देती हैं। शर्माजी मूलतः कथाकार हैं। उनका यह कौशल निबंधों में भी दिखाई पड़ता है। ‘क्रांति की प्रतीक्षा में’ में एक डाकिए के जरिए खत्म होते हुए मूल्यों की वेदना मुखरित है। ‘टूटना एक खूबसूरत प्याली का’ आकर्षण, सौंदर्य बोध और बुद्धि जन्य तर्कों का ताना-बाना है। ‘बुधिया की कोठरी में साँप’ में कथा और नाटक दोनों हैं। ‘काग-ग्रास’ में पत्नी के निधन की सघन वेदना उभरी है। लेखक कभी संवेदना को उभारता है, कभी आज की गिरावट को कहता है, कभी अपने मनोभावों को व्यक्त करता है और कभी अपने चिंतन को आधार देता है। ये कथाएँ या तो लेखक के परिचितों की हैं अथवा पढ़ी हुई हैं। जिन्होंने लेखक को प्रभावित किया है।
मनु शर्मा छोटी-छोटी बातों से निबंध शुरू करते हैं। उनके निबंधों के केंद्र में चिंतन है। उद्धरण, कथा, नाटकीयता, मिथक इत्यादि चिंतन को प्रभावशाली बनाने के उपक्रम हैं। ये तत्त्व उन्हें पाठक से जोड़ते भी हैं। चिंतन में कहीं तत्त्व-चिंतन की गंभीर बातें हैं, कहीं कला से संबद्ध विचार, कहीं पाश्चात्य न्याय दृष्टि से असहमति, कहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान और अवतारवाद जैसे गंभीर विषयों पर चिंतन, कहीं जीवन-मूल्य की प्रतिष्ठा, कहीं अंधविश्वासों से असहमति है और कहीं आज के जीवन और समाज की गिरावट है। यानी कहीं गंभीर और बड़ी बातें हैं तो कहीं छोटी और सामान्य बातें हैं। चिंतन का विषय इतिहास, संस्कृति, राजनीति, दर्शन कला और समकालीन जीवन भी है।
मनु शर्मा का मन एकदम भारतीय है। भारतीय संस्कृति और जीवन-शैली उनके व्यक्तित्व में समाई हुई है। कोई इसे सगुण चिंतन कहे, विशुद्ध भारतीय या और कुछ कह ले; मगर उनके मन में राम, कृष्ण, शिव और गांधी के लिए स्थान है तो लाओत्से, युवान च्वांग, नीत्से, कार्ल मार्क्स और गालिब के लिए भी है।
इन निबंधों में शर्माजी के व्यक्तित्व की सरसता है, अनुभव की गहराई है, अगाध ज्ञान की गरिमा है, जीवन का संत्रास है और क्षणों की सुखानुभूति भी। अपनी निबंध यात्रा में उनका मन चेतना के न जाने कितने धरातल पर दस्तक देता है। सबकुछ सहज और स्वाभाविक है। पाठकों को कहीं कथा का रस आता है, तो कहीं संगुंफित विचारों के परत-दर परत खुलने का आनंद मिलता है।
पिछले-दस बारह वर्षों में लिखे गए ये निबंध अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं में छपे हैं। इनमें लेखक का चिंतन, विचार, आस्था इत्यादि उनकी संवेदनाओं में घुल-मिलकर आए हैं। जीवन की कोई घटना, कोई संदर्भ, कोई कथा, कोई प्रतीक या सामान्य-असामान्य व्यक्ति लेखक के मन को उद्वेलित करता है और यही उद्वेलन लेखक के चिंतन का आधार बनता है।
हिंदी में व्यक्ति-व्यंजक निबंधों और ललित निबंधों को लेकर भी गंभीर विवाद है। व्यक्ति-व्यंजक में निजत्व और ललित में लालित्य को लोग प्रधान मानते हैं। लेकिन ऐसा भेद करना पानी पर लकीर खींचना है। निजत्व ही ललित बनकर व्यक्त होता है। व्यक्ति-चेतना को केंद्र में रखकर निबंध लिखनेवालों में दो प्रकार के रचनाकार हैं-एक वे जो व्यक्ति-सापेक्षता को अपने जीवन के प्रसंगों, कथात्मकता और नाटकीयता से उभारते हैं; जैसे-पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त आदि। दूसरे प्रकार के वे निबंधकार हैं, जो निबंध में लालित्य को ही महत्त्व देते हैं। निजी जीवन के प्रसंग, सांस्कृतिक चेतना, लोक-तत्त्व प्रतीक, मिथक इत्यादि के द्वारा लालित्य प्रकट होता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंधों से लालित्य पर बल दिया जाने लगा। वे अपने चिंतन के फलक का विस्तार छायावादी कवियों के समान करते हैं। द्विवेदीजी का लालित्य अपने भावों या विचारों के उद्वेलन, संस्कृत छंदों के उद्धरण, प्रतीक अथवा मिथक की रचना करते हुए उत्पन्न होता है। उनके निबंधों में सर्वत्र भाव-प्रेरित लय है। ये निबंध कविता के समान स्वतःस्फूर्त हैं। द्विवेदीजी का कवि अकसर उनके गद्यकार पर बीस पड़ जाता है। पं. विद्यानिवास मिश्र अपनी वैयक्तिकता को लोक-चेतना और आधुनिक बोध से जोड़ते हैं। कुबेरनाथ राय इन निबंधकारों से अलग हैं। इनमें प्रतीकों और मिथकों को रचने की प्रवृत्ति है। कथा कहने की प्रवृत्ति, बहुज्ञता और जीवन के प्रति राग से वे पाठकों को अपनी ओर खींचते हैं।
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किसी घटना, किसी एक रोचक प्रसंग या किसी एक बात से निबंधों की शुरुआत करते हैं। नाटकीयता और कथात्मकता इनके निबंधों को रोचक बनाती है। सहजता इनकी एक अन्य विशेषता है। सियाराम शरण गुप्त ने भी अपने अपने निबंधों में छोटी-छोटी बातों को कहीं संस्मरण और कहीं व्यंग्य के माध्यम से कहा है। यह व्यक्ति-चेतना है। हिंदी में व्यक्ति-व्यंजक निबंध लिखनेवालों की ये दो परंपराएँ हैं। इन्हें व्यक्ति-व्यंजक और ललित कहकर अलग करना उचित नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। फिर भी अंग्रेजी के व्यक्ति-व्यंजक निबंधों से हिंदी के व्यक्ति-व्यंजक निबंधों की पहचान अलग है। अंग्रेजी के निबंधकारों की तरह अपने घर-परिवार, इष्ट-मित्र, पसंद-नापसंद का विवरण हिंदी के निबंधकार नहीं देते हैं। वे चुटकी लेते हैं, व्यंग्य करते हैं, किसी विश्वस्त और निकट व्यक्ति की तरह बात करते हैं।
मनु शर्मा के ये निबंध हजारीप्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र के निबंधों से हटकर हैं। उनकी निजता अपने निबंधों में अधिक खुलती है। वे अपनी बेबसी, अंतर्विरोध आदि को भी कहते हैं। घर-परिवार, पास-पड़ोस, परिचित-अल्पपरिचित के संदर्भ इन निबंधों में हैं। कथात्मक और नाटकीयता इन संदर्भों को आकर्षक बना देती हैं। शर्माजी मूलतः कथाकार हैं। उनका यह कौशल निबंधों में भी दिखाई पड़ता है। ‘क्रांति की प्रतीक्षा में’ में एक डाकिए के जरिए खत्म होते हुए मूल्यों की वेदना मुखरित है। ‘टूटना एक खूबसूरत प्याली का’ आकर्षण, सौंदर्य बोध और बुद्धि जन्य तर्कों का ताना-बाना है। ‘बुधिया की कोठरी में साँप’ में कथा और नाटक दोनों हैं। ‘काग-ग्रास’ में पत्नी के निधन की सघन वेदना उभरी है। लेखक कभी संवेदना को उभारता है, कभी आज की गिरावट को कहता है, कभी अपने मनोभावों को व्यक्त करता है और कभी अपने चिंतन को आधार देता है। ये कथाएँ या तो लेखक के परिचितों की हैं अथवा पढ़ी हुई हैं। जिन्होंने लेखक को प्रभावित किया है।
मनु शर्मा छोटी-छोटी बातों से निबंध शुरू करते हैं। उनके निबंधों के केंद्र में चिंतन है। उद्धरण, कथा, नाटकीयता, मिथक इत्यादि चिंतन को प्रभावशाली बनाने के उपक्रम हैं। ये तत्त्व उन्हें पाठक से जोड़ते भी हैं। चिंतन में कहीं तत्त्व-चिंतन की गंभीर बातें हैं, कहीं कला से संबद्ध विचार, कहीं पाश्चात्य न्याय दृष्टि से असहमति, कहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान और अवतारवाद जैसे गंभीर विषयों पर चिंतन, कहीं जीवन-मूल्य की प्रतिष्ठा, कहीं अंधविश्वासों से असहमति है और कहीं आज के जीवन और समाज की गिरावट है। यानी कहीं गंभीर और बड़ी बातें हैं तो कहीं छोटी और सामान्य बातें हैं। चिंतन का विषय इतिहास, संस्कृति, राजनीति, दर्शन कला और समकालीन जीवन भी है।
मनु शर्मा का मन एकदम भारतीय है। भारतीय संस्कृति और जीवन-शैली उनके व्यक्तित्व में समाई हुई है। कोई इसे सगुण चिंतन कहे, विशुद्ध भारतीय या और कुछ कह ले; मगर उनके मन में राम, कृष्ण, शिव और गांधी के लिए स्थान है तो लाओत्से, युवान च्वांग, नीत्से, कार्ल मार्क्स और गालिब के लिए भी है।
-डॉ.
विश्वनाथ प्रसाद
जीवन क्या जीया
सुबह से ही बधाई के टेलीफोन आ रहे हैं। आज मैंने जन्म की पचहत्तरवीं मंजिल
छू ली। वक्त के कैलेंडर का एक पन्ना और झड़ गया। जब जीवन की पूँजी
धीरे-धीरे चुकती चली जा रही है तब बधाई किस बात की ? इस बात की कि जीवन के
पचहत्तर वर्ष मैंने पूरे कर लिये, बहुत से लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए
और काल-कवलित हो गए। सचमुच यह प्रसन्नता की बात है, कम-से-कम उस देश में
तो अवश्य ही जहाँ औसत उम्र सिर्फ उनसठ वर्ष है। अवश्य मैं दूसरों की उम्र
छीनकर जीया हूँ। दूसरों की पूँजी पर डाका डाला है।
और इस प्रदूषण के युग में, जहाँ हवा-पानी, नीति—राजनीति, नैतिकता-सामाजिकता सबकुछ प्रदूषित है; जहाँ खाने-पीने की हर वस्तु मिलावटी हो; जहाँ दूध भी सिंथेटिक मिलता हो।...मेरे एक मित्र ने एक दिन इस बात की शिकायत की कि आज रात मैं सो नहीं पाया। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि पूरी रात पड़ोस में कुहराम मचा रहा। किसी बात पर सुमेर के मझले बेटे ने जहर खा लिया। ऐसा रोना-पीटना शुरू हुआ जो भोर तक चलता रहा। डॉक्टर के आते ही एकदम स्थिति बदल गई। उसने जहर की शीशी देखकर कहा, ‘अरे, यह तो बड़ा तेज जहर है। इसके पेट में जाते ही इसे मर जाना चाहिए था; पर यह अभी भी जीवित है। दाल में कुछ काला जरूर है।’
बाद में पता चला कि जहर में मिलावट थी, इसीलिए वह सीली हुई आतिशबाजी की तरह ‘फुर्र’ से करके रह गया। उसके घर के लोग इस मिलावट पर प्रसन्न हैं। विषहीन सर्प और अमंत्रित ब्रह्मास्त्र उनके लिए अवश्य ही अभिनंदित होंगे जिन पर वे आक्रमण किए जाने वाले हों।
हो सकता है, मेरे मित्र द्वारा बताई इस घटना का यथार्थ भी मिलावटी हो; पर इससे तो इतना स्पष्ट हो ही जाता है कि इस देश में अब ऐसा कवि शायद ही पैदा हो, जो यह लिख सके कि ‘अमिय सराहहि अमरता गरल सराहहि मीचु।’
ऐसी स्थिति में भी मैंने जीवन के चौहत्तर वर्ष पूरे कर लिये। मेरे मित्रों का प्रसन्न होना लाजिमी है। पर इसी शहर में ऐसे लोग भी हैं, जो जिंदगी की सड़क पर मुझसे काफी आगे निकल गए हैं। कांग्रेस के भूतपूर्व मेयर कुंजू बाबू तो शतक बनाने के करीब हैं। या तो हममें जिजीविषा अधिक है या फिर बेहयाई, जो हममें मौत की मार खाते हुए भी जिदंगी का तमाशा घुसकर देखने की ललक बनाए रखती है। शायद इसी ललक का दूसरा नाम जिजीविषा हो।
याद आता है, ‘गीता’ में कृष्ण ने स्वयं को ‘पीपल’ कहा है-‘अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां नारदः।’ अर्थात्-मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद। आखिर उन्होंने अपने लिए वृक्षों में पीपल को ही क्यों चुना ? वे इससे और भी गौरववाली तथा उपयोगी वृक्षों को चुन सकते थे। वे कदंब को चुन सकते थे, बहुतों का चीर-हरण करके उसकी डाल का आश्रय लिया था। वे करील का नाम ले सकते थे, उसके कुंजों में उन्होंने कैसी-कैसी रास-लीलाएँ की थीं और स्वयं ‘कुंज-बिहारी’ की संज्ञा पाई थी। वे रसाल का नाम ले सकते थे, जिसका फल एक बार मुँह लग जाए तो मुँह से छूटता ही नहीं। वे देवदारु का नाम ले सकते थे, वह तो देवताओं का वृक्ष ही है। फिर उन्होंने मुँडेरों पर भी उग आनेवाले पीपल को ही अपना प्रतिनिधि क्यों चुना ? शायद इसीलिए कि पीपल में अद्भुत जिजीविषा है। जहाँ पड़ा वहीं जम गया। मिट्टी अनुकूल नहीं, परवाह नहीं। जो है उसी को अनुकूल बना लेगा, पत्थर को भी मिट्टी कर देगा। पानी नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं। जब मिलेगा तब ही लेगा। धूप नहीं मिली तो भी चिंता नहीं। भूली-भटकी दो-एक किरणें भी आ जाएँगी तो वही काफी होंगी। नहीं कुछ मिलेगा तो पर्यावरण से मिलेगा ही, उसी का स्तनपान कर वह जी लेगा।
आप एकदम उखाड़कर फेंक दीजिए तो दो-चार दिनों बाद ही उखाड़ी हुई दरार से शातिर चोर की तरह झाँकता दिखाई देगा, और जहाँ उखाड़कर फेंक दीजिए वहीं जम जाएगा। परिस्थितियों द्वारा कृष्ण मथुरा से उखाड़कर फेंके गए तो समुद्र के किनारे जम गए। एक द्वारका ही बसा ली।
आज का विज्ञान कहता है कि पीपल सभी वृक्षों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन देता है। एक तो स्वयं जीने की उसकी अद्भुत शक्ति तथा दूसरों को जीवन प्रदान करने की उसकी क्षमता। शायद इन्हीं गुणों के कारण उसमें कृष्ण को अपना रुप दिखाई दिया हो।
पर मैं कृष्ण नहीं हूँ, शायद उनका शतांश भी नहीं। फिर मुझमें ऐसी जिजीविषा कहाँ ! जरा सा रक्तचाप बढ़ा कि घबराने लगा। मेरी घबराहट भी अजीब, जिसमें मृत्यु का भय नहीं। उस कृष्ण का अनुचर मैं, जिसने मृत्यु की वास्तविकता बताई, जिसने लोगों को मरना सिखाया, मृत्यु से क्यों डरूँ। फिर भी मेरी घबराहट में भय है जीवन की अपंगुता का।
आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ और दृष्टि जीवन के आंरभिक छोर पर पड़ती है तब एक घटना याद आती है। उन दिनों मैं पंचगंगा घाट के पास ही छासी टोले में रहता था। माँ पूरे कार्तिक मास गंगा नहाती थी; इसलिए भी कि यह स्नानपर्व मेरे जन्म के दिन से आरंभ होता था। स्नान के लिए मुझे भी साथ ले जाती थी। मैं उसका प्यारा बेटा था, चौथा या पाँचवाँ। मुझसे पहले के उसके सभी बेटे मर गए थे। उम्र यही छह सात की रही होगी। लौटते समय पंचगंगा घाट की ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ मुझे अँगुली पकड़कर चढ़ाती थी। छह सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते मैं थक जाता था, फिर वह गोद में उठा लेती थी। एक दिन मैं बड़ा उत्साहित हुआ और छह के बाद सातवीं सीढ़ी भी चढ़ गया। उस दिन मेरी माँ बहुत प्रसन्न हुई थी। उसने सबसे कहा था, ‘आज मेरा बेटा एक सीढ़ी और चढ़ गया !’...आज जब लोग मुझे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तब मुझे लगता है, मणिकर्णिका घाट की एक सीढ़ी और उतर गया। अब कितनी सीढ़ियाँ बाकी हैं, पता नहीं। इस अज्ञान के ही कारण तो अभी जीवन में रस है।
अज्ञान का सुख भी अपने ढंग का सुख है। उसे ‘भव-भुजंग का भय’ नहीं। वह जानता ही नहीं कि ‘भव-भुजंग’ क्या होता है, वह कैसे डसता है; क्योंकि उसने ‘आदम के ज्ञान’ का फल नहीं चखा है। जग के प्रपंच में रहते हुए भी उससे दूर है। ‘सबसे भल वे मूढ़ जिन्हें न ब्यापै जगत गति।’ जीवन की एक अवस्था यह भी है। यही प्रकृत अवस्था है। इसकी वृत्ति पशु प्रवृत्ति है, जिसमें इच्छाएँ सीमित हैं। भूख लगी, जो मिला उसी पर मुँह मारा। भोग जगा मिल लिये। अपने बिहारी लाल इसी स्थिति पर प्रसन्न हैं-
खाने को कंकड़ी भली सदा परेवी संग।
सुखी परेवा जगत में तू ही एक विहंग।।
आप सोचते होंगे कि मैं किस पचड़े में पड़ा। बेवक्त की शहनाई छेड़ दी। मूसल के ब्याह में हँसुए का गीत गाने लगा। दरअसल मुझ पर एच.जी. गार्डनर के लेख-‘इनडिफेंस ऑफ इग्नोरेंस’ की छाया पड़ गई थी और मैं यह नहीं देख पाया कि यह सुख तो पशुओं का सुख है। आदमी पशु नहीं है। पशु से आदमी तक की विकास-यात्रा से ज्ञान की विकास-यात्रा है। अज्ञात से ज्ञात की यात्रा है, प्रकृति से संस्कृति की यात्रा है-और यह संस्कृति हमारे संस्कारों का परिणाम है। हमारे सारे संस्कार उस गंगा से जुड़े हैं जिसकी सीढ़ियों की अभी मैं बात कर रहा था।
मेरे जन्म के बाद भी माँ गंगा-पूजन करने आई होगी। कर्ण-छेदन और मुंडन के बाद भी मुझे गंगा आराधना के लिए लाया गया था। उपनयन और विवाह के बाद भी मेरी ‘गंगा पुजइया’ इसी गंगा तट पर आई थी और जब अंत्येष्टि के लिए मणिकर्णिका की अग्रिम सीढ़ी पर लाया जाऊँगा तब यही गंगा मुक्तिदायिनी होगी। यह गंगा-धारा हमारे सभी संस्कारों की चश्मदीद गवाह है। गंगा ही हमारी संस्कृति की जीवन रेखा है-आज से नहीं, भगीरथ के समय से ही। कहते हैं, राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या की थी, तब कहीं, किसी तरह गंगा धरती पर आई थीं।
भगीरथ का यह प्रयत्न निजी था, अपने परिवार को तारने के लिए था। यह निजी कार्य आज सामाजिक हो गया। तुलसी का ‘स्वांतःसुखाय परांतःसुखाय’ बन गया। इसकी मोक्षदायिनी प्रकृति के प्रति विश्वास बढ़ता गया। राजा हरिश्चंद्र भी बिके तो इसी के किनारे एक डोम के हाथ।... पर हमारा ज्ञान इस अवधारणा के विपरीत पड़ता है। शोध बताता है कि राजा हरिश्चंद्र की ग्यारहवीं पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए थे। जब भागीरथ ही नहीं रहे होंगे तो कहाँ रही होगी गंगा; फिर राजा हरिश्चंद्र के बिकने का तो सवाल ही नहीं।
बात अटपटी अवश्य लगती है, पर अब तो यह ‘मिथ’ है। ‘मिथ’ तर्कातीत होता है। वह यथार्थ नहीं पर ‘यथार्थ का भ्रम है। ‘मिथ’ मिथ्या के करीब होकर भी सत्य से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि विश्वास ही उसका आधार है, उसका जीवन है। ‘मिथ’ में इतिहास को खोजना अंधे कुएँ में पानी तलाश करना है। अरे, कुआँ तो कुआँ है, चाहे अंधा हो या पानीदार।
वैज्ञानिक की नजर दूसरी है। उसका निष्कर्ष है कि आज गंगा काफी प्रदूषित हो चुकी है। उसका जल पीने के योग्य क्या, स्नान करने लायक भी नहीं रहा। क्या यह प्रदूषित गंगा मोक्षदायिनी हो सकती है ? यदि मोक्षदायिनी होगी भी तो उसका मोक्ष भी प्रदूषित होगा। पर यथार्थ कुछ और है और सत्य कुछ और। मोक्षदायिनी गंगा वह नहीं जो हमें दिखाई देती है, वरन् वह है जो हमारे भीतर आस्था के धरातल पर बहती है, जिसका उद्गम गंगोत्तरी नहीं वरन किसी भगीरथ का अपराजेय तप है। उसकी धारा एक लंबी परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों से हम तक चली आई और हमारे बाद भी बहती रहेगी। रामेश्वरम् के समुद्र-तट पर डुबकी लगाते हुए लोगों को ‘जय माँ गंगे’ कहते मैंने सुना है। यह इस बात का प्रमाण है कि बाहर का पानी खारा हो या प्रदूषित, पर हमारे भीतर की गंगा कभी प्रदूषित नहीं होती। वह तभी प्रदूषित होगी जब हमारी आस्था प्रदूषित होगी या उसे सँजोकर रखनेवाला हमारा मन प्रदूषित होगा। इसी से तो रैदास कहते हैं-‘जब मन चंगा तो कठौती में गंगा।’
मैं गंगा-लाभ की बात क्यों सोचने लगा, जब टेलीफोन पर लोग जीवन की जय बोल रहे हों, ‘जीवेम शरदः शतम्’ की कामना कर रहे हों। कुछ लोगों ने सौ वसंतों तक जीने की भी बात कही है; जबकि पूरा वैदिक वाङ्मय शरत् की बात करता है। लगता है, वैदिक युग में ‘शरत्’ से ही वर्ष आरंभ होता था। बाद में इस कृषि-प्रधान देश में वर्षा से वर्ष का आरंभ होने लगा। वर्षा से आरंभ होने के कारण ही इस कालावधि को ‘वर्ष’ की संज्ञा मिली। विक्रम संवत् चैत्र मास से अवश्य आरंभ होता है, पर वसंत से उसका कोई संबंध नहीं।
यों वसंत और शरत् दोनों संधि ऋतुएँ हैं। वसंत शिशिर की हिमानी शीत से ठिठुरी प्रकृति के मुक्ति का उल्लास है, जो फूलों में विहँस पड़ता है तो शरद वर्षा से उद्वेलित और गदराई वारि-धाराओं को पागलपन तथा कीचड़ व गँदलेपन से धरती की मुक्ति की उज्ज्वलता है, जो आकाश से लेकर घर-आँगन तक दिखाई देती है। किसी युग में जब आवागमन के आज जैसे साधन नहीं थे तब चौमासे की समाप्ति पर यात्राएँ आरंभ हो जाती थीं, जीवन गतिशील हो जाता था। हम शक्ति की आराधना में लग जाते हैं। बँगला के ‘कीर्तिवासी रामायण’ के अनुसार राम ने भी शक्ति की आराधना की थी और उसी अपराजेय शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया था। यही कथा निराला की ‘राम की शक्ति की पूजा’ का आधार बनी।
वसंत में काम भस्म हुआ था और शरत् में रावण। काम भस्म होने के बाद अनंग होकर हममें जीवित है। लगता है, रावण भी अनंग होकर हममें जीवित है और आज भी सज्जनों को त्रासित करता है। मेरे एक मित्र कवि की यही मुख्य चिंता है-‘घर-घर रावण, घर-घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊँ ?’
वसंत में बहार है, मस्ती है, रंगबाजी है, रँगरेलियाँ हैं, उन्माद है; पर शरत् में गांभीर्य है, गति है, गंदगी को धो डालने की ललक है। वसंत के मूल में वासना है, शरत् के मूल में उपासना। वसंत संबद्ध है रति से, काम से; शरत् संबद्ध है शक्ति से, राम से। शायद शरत् के आगमन पर जन्म लेने के कारण ही मेरे पितामह ने मुझे राम-भक्त ‘हनुमान प्रसाद’ की संज्ञा दी। शायद इसके पीछे उनकी मंशा भी मेरे दीर्घजीवी होने की थी, जिसकी शुभकामना आज प्रातः से ही मेरे मित्र टेलीफोन पर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इन शुभकामनाओं के पीछे वैदिक ऋषियों की यह वाणी है-‘जीवेम शरदः शतम्। पश्चेम शरदः शतम् । श्रृणुयाम शरदः शतम्। प्रब्रवाम शरदः शतम्। अदीनामस्याम शरदः शतम्। भूयस्य शरदः शतात्। अर्थात्-हम सौ वर्षों तक देखते हुए जीएँ, सुनते हुए जीएँ, प्रवचन करते हुए जीएँ। अदीन होकर शान से जीएँ और सौ वर्षों से अधिक भी आनंदपूर्वक जीएँ। इन क्रियमाण शक्तियों के बिना अशक्य और असहाय होकर जीना भी कोई जीना है। धन्यवाद !
और इस प्रदूषण के युग में, जहाँ हवा-पानी, नीति—राजनीति, नैतिकता-सामाजिकता सबकुछ प्रदूषित है; जहाँ खाने-पीने की हर वस्तु मिलावटी हो; जहाँ दूध भी सिंथेटिक मिलता हो।...मेरे एक मित्र ने एक दिन इस बात की शिकायत की कि आज रात मैं सो नहीं पाया। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि पूरी रात पड़ोस में कुहराम मचा रहा। किसी बात पर सुमेर के मझले बेटे ने जहर खा लिया। ऐसा रोना-पीटना शुरू हुआ जो भोर तक चलता रहा। डॉक्टर के आते ही एकदम स्थिति बदल गई। उसने जहर की शीशी देखकर कहा, ‘अरे, यह तो बड़ा तेज जहर है। इसके पेट में जाते ही इसे मर जाना चाहिए था; पर यह अभी भी जीवित है। दाल में कुछ काला जरूर है।’
बाद में पता चला कि जहर में मिलावट थी, इसीलिए वह सीली हुई आतिशबाजी की तरह ‘फुर्र’ से करके रह गया। उसके घर के लोग इस मिलावट पर प्रसन्न हैं। विषहीन सर्प और अमंत्रित ब्रह्मास्त्र उनके लिए अवश्य ही अभिनंदित होंगे जिन पर वे आक्रमण किए जाने वाले हों।
हो सकता है, मेरे मित्र द्वारा बताई इस घटना का यथार्थ भी मिलावटी हो; पर इससे तो इतना स्पष्ट हो ही जाता है कि इस देश में अब ऐसा कवि शायद ही पैदा हो, जो यह लिख सके कि ‘अमिय सराहहि अमरता गरल सराहहि मीचु।’
ऐसी स्थिति में भी मैंने जीवन के चौहत्तर वर्ष पूरे कर लिये। मेरे मित्रों का प्रसन्न होना लाजिमी है। पर इसी शहर में ऐसे लोग भी हैं, जो जिंदगी की सड़क पर मुझसे काफी आगे निकल गए हैं। कांग्रेस के भूतपूर्व मेयर कुंजू बाबू तो शतक बनाने के करीब हैं। या तो हममें जिजीविषा अधिक है या फिर बेहयाई, जो हममें मौत की मार खाते हुए भी जिदंगी का तमाशा घुसकर देखने की ललक बनाए रखती है। शायद इसी ललक का दूसरा नाम जिजीविषा हो।
याद आता है, ‘गीता’ में कृष्ण ने स्वयं को ‘पीपल’ कहा है-‘अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां नारदः।’ अर्थात्-मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद। आखिर उन्होंने अपने लिए वृक्षों में पीपल को ही क्यों चुना ? वे इससे और भी गौरववाली तथा उपयोगी वृक्षों को चुन सकते थे। वे कदंब को चुन सकते थे, बहुतों का चीर-हरण करके उसकी डाल का आश्रय लिया था। वे करील का नाम ले सकते थे, उसके कुंजों में उन्होंने कैसी-कैसी रास-लीलाएँ की थीं और स्वयं ‘कुंज-बिहारी’ की संज्ञा पाई थी। वे रसाल का नाम ले सकते थे, जिसका फल एक बार मुँह लग जाए तो मुँह से छूटता ही नहीं। वे देवदारु का नाम ले सकते थे, वह तो देवताओं का वृक्ष ही है। फिर उन्होंने मुँडेरों पर भी उग आनेवाले पीपल को ही अपना प्रतिनिधि क्यों चुना ? शायद इसीलिए कि पीपल में अद्भुत जिजीविषा है। जहाँ पड़ा वहीं जम गया। मिट्टी अनुकूल नहीं, परवाह नहीं। जो है उसी को अनुकूल बना लेगा, पत्थर को भी मिट्टी कर देगा। पानी नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं। जब मिलेगा तब ही लेगा। धूप नहीं मिली तो भी चिंता नहीं। भूली-भटकी दो-एक किरणें भी आ जाएँगी तो वही काफी होंगी। नहीं कुछ मिलेगा तो पर्यावरण से मिलेगा ही, उसी का स्तनपान कर वह जी लेगा।
आप एकदम उखाड़कर फेंक दीजिए तो दो-चार दिनों बाद ही उखाड़ी हुई दरार से शातिर चोर की तरह झाँकता दिखाई देगा, और जहाँ उखाड़कर फेंक दीजिए वहीं जम जाएगा। परिस्थितियों द्वारा कृष्ण मथुरा से उखाड़कर फेंके गए तो समुद्र के किनारे जम गए। एक द्वारका ही बसा ली।
आज का विज्ञान कहता है कि पीपल सभी वृक्षों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन देता है। एक तो स्वयं जीने की उसकी अद्भुत शक्ति तथा दूसरों को जीवन प्रदान करने की उसकी क्षमता। शायद इन्हीं गुणों के कारण उसमें कृष्ण को अपना रुप दिखाई दिया हो।
पर मैं कृष्ण नहीं हूँ, शायद उनका शतांश भी नहीं। फिर मुझमें ऐसी जिजीविषा कहाँ ! जरा सा रक्तचाप बढ़ा कि घबराने लगा। मेरी घबराहट भी अजीब, जिसमें मृत्यु का भय नहीं। उस कृष्ण का अनुचर मैं, जिसने मृत्यु की वास्तविकता बताई, जिसने लोगों को मरना सिखाया, मृत्यु से क्यों डरूँ। फिर भी मेरी घबराहट में भय है जीवन की अपंगुता का।
आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ और दृष्टि जीवन के आंरभिक छोर पर पड़ती है तब एक घटना याद आती है। उन दिनों मैं पंचगंगा घाट के पास ही छासी टोले में रहता था। माँ पूरे कार्तिक मास गंगा नहाती थी; इसलिए भी कि यह स्नानपर्व मेरे जन्म के दिन से आरंभ होता था। स्नान के लिए मुझे भी साथ ले जाती थी। मैं उसका प्यारा बेटा था, चौथा या पाँचवाँ। मुझसे पहले के उसके सभी बेटे मर गए थे। उम्र यही छह सात की रही होगी। लौटते समय पंचगंगा घाट की ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ मुझे अँगुली पकड़कर चढ़ाती थी। छह सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते मैं थक जाता था, फिर वह गोद में उठा लेती थी। एक दिन मैं बड़ा उत्साहित हुआ और छह के बाद सातवीं सीढ़ी भी चढ़ गया। उस दिन मेरी माँ बहुत प्रसन्न हुई थी। उसने सबसे कहा था, ‘आज मेरा बेटा एक सीढ़ी और चढ़ गया !’...आज जब लोग मुझे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तब मुझे लगता है, मणिकर्णिका घाट की एक सीढ़ी और उतर गया। अब कितनी सीढ़ियाँ बाकी हैं, पता नहीं। इस अज्ञान के ही कारण तो अभी जीवन में रस है।
अज्ञान का सुख भी अपने ढंग का सुख है। उसे ‘भव-भुजंग का भय’ नहीं। वह जानता ही नहीं कि ‘भव-भुजंग’ क्या होता है, वह कैसे डसता है; क्योंकि उसने ‘आदम के ज्ञान’ का फल नहीं चखा है। जग के प्रपंच में रहते हुए भी उससे दूर है। ‘सबसे भल वे मूढ़ जिन्हें न ब्यापै जगत गति।’ जीवन की एक अवस्था यह भी है। यही प्रकृत अवस्था है। इसकी वृत्ति पशु प्रवृत्ति है, जिसमें इच्छाएँ सीमित हैं। भूख लगी, जो मिला उसी पर मुँह मारा। भोग जगा मिल लिये। अपने बिहारी लाल इसी स्थिति पर प्रसन्न हैं-
खाने को कंकड़ी भली सदा परेवी संग।
सुखी परेवा जगत में तू ही एक विहंग।।
आप सोचते होंगे कि मैं किस पचड़े में पड़ा। बेवक्त की शहनाई छेड़ दी। मूसल के ब्याह में हँसुए का गीत गाने लगा। दरअसल मुझ पर एच.जी. गार्डनर के लेख-‘इनडिफेंस ऑफ इग्नोरेंस’ की छाया पड़ गई थी और मैं यह नहीं देख पाया कि यह सुख तो पशुओं का सुख है। आदमी पशु नहीं है। पशु से आदमी तक की विकास-यात्रा से ज्ञान की विकास-यात्रा है। अज्ञात से ज्ञात की यात्रा है, प्रकृति से संस्कृति की यात्रा है-और यह संस्कृति हमारे संस्कारों का परिणाम है। हमारे सारे संस्कार उस गंगा से जुड़े हैं जिसकी सीढ़ियों की अभी मैं बात कर रहा था।
मेरे जन्म के बाद भी माँ गंगा-पूजन करने आई होगी। कर्ण-छेदन और मुंडन के बाद भी मुझे गंगा आराधना के लिए लाया गया था। उपनयन और विवाह के बाद भी मेरी ‘गंगा पुजइया’ इसी गंगा तट पर आई थी और जब अंत्येष्टि के लिए मणिकर्णिका की अग्रिम सीढ़ी पर लाया जाऊँगा तब यही गंगा मुक्तिदायिनी होगी। यह गंगा-धारा हमारे सभी संस्कारों की चश्मदीद गवाह है। गंगा ही हमारी संस्कृति की जीवन रेखा है-आज से नहीं, भगीरथ के समय से ही। कहते हैं, राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या की थी, तब कहीं, किसी तरह गंगा धरती पर आई थीं।
भगीरथ का यह प्रयत्न निजी था, अपने परिवार को तारने के लिए था। यह निजी कार्य आज सामाजिक हो गया। तुलसी का ‘स्वांतःसुखाय परांतःसुखाय’ बन गया। इसकी मोक्षदायिनी प्रकृति के प्रति विश्वास बढ़ता गया। राजा हरिश्चंद्र भी बिके तो इसी के किनारे एक डोम के हाथ।... पर हमारा ज्ञान इस अवधारणा के विपरीत पड़ता है। शोध बताता है कि राजा हरिश्चंद्र की ग्यारहवीं पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए थे। जब भागीरथ ही नहीं रहे होंगे तो कहाँ रही होगी गंगा; फिर राजा हरिश्चंद्र के बिकने का तो सवाल ही नहीं।
बात अटपटी अवश्य लगती है, पर अब तो यह ‘मिथ’ है। ‘मिथ’ तर्कातीत होता है। वह यथार्थ नहीं पर ‘यथार्थ का भ्रम है। ‘मिथ’ मिथ्या के करीब होकर भी सत्य से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि विश्वास ही उसका आधार है, उसका जीवन है। ‘मिथ’ में इतिहास को खोजना अंधे कुएँ में पानी तलाश करना है। अरे, कुआँ तो कुआँ है, चाहे अंधा हो या पानीदार।
वैज्ञानिक की नजर दूसरी है। उसका निष्कर्ष है कि आज गंगा काफी प्रदूषित हो चुकी है। उसका जल पीने के योग्य क्या, स्नान करने लायक भी नहीं रहा। क्या यह प्रदूषित गंगा मोक्षदायिनी हो सकती है ? यदि मोक्षदायिनी होगी भी तो उसका मोक्ष भी प्रदूषित होगा। पर यथार्थ कुछ और है और सत्य कुछ और। मोक्षदायिनी गंगा वह नहीं जो हमें दिखाई देती है, वरन् वह है जो हमारे भीतर आस्था के धरातल पर बहती है, जिसका उद्गम गंगोत्तरी नहीं वरन किसी भगीरथ का अपराजेय तप है। उसकी धारा एक लंबी परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों से हम तक चली आई और हमारे बाद भी बहती रहेगी। रामेश्वरम् के समुद्र-तट पर डुबकी लगाते हुए लोगों को ‘जय माँ गंगे’ कहते मैंने सुना है। यह इस बात का प्रमाण है कि बाहर का पानी खारा हो या प्रदूषित, पर हमारे भीतर की गंगा कभी प्रदूषित नहीं होती। वह तभी प्रदूषित होगी जब हमारी आस्था प्रदूषित होगी या उसे सँजोकर रखनेवाला हमारा मन प्रदूषित होगा। इसी से तो रैदास कहते हैं-‘जब मन चंगा तो कठौती में गंगा।’
मैं गंगा-लाभ की बात क्यों सोचने लगा, जब टेलीफोन पर लोग जीवन की जय बोल रहे हों, ‘जीवेम शरदः शतम्’ की कामना कर रहे हों। कुछ लोगों ने सौ वसंतों तक जीने की भी बात कही है; जबकि पूरा वैदिक वाङ्मय शरत् की बात करता है। लगता है, वैदिक युग में ‘शरत्’ से ही वर्ष आरंभ होता था। बाद में इस कृषि-प्रधान देश में वर्षा से वर्ष का आरंभ होने लगा। वर्षा से आरंभ होने के कारण ही इस कालावधि को ‘वर्ष’ की संज्ञा मिली। विक्रम संवत् चैत्र मास से अवश्य आरंभ होता है, पर वसंत से उसका कोई संबंध नहीं।
यों वसंत और शरत् दोनों संधि ऋतुएँ हैं। वसंत शिशिर की हिमानी शीत से ठिठुरी प्रकृति के मुक्ति का उल्लास है, जो फूलों में विहँस पड़ता है तो शरद वर्षा से उद्वेलित और गदराई वारि-धाराओं को पागलपन तथा कीचड़ व गँदलेपन से धरती की मुक्ति की उज्ज्वलता है, जो आकाश से लेकर घर-आँगन तक दिखाई देती है। किसी युग में जब आवागमन के आज जैसे साधन नहीं थे तब चौमासे की समाप्ति पर यात्राएँ आरंभ हो जाती थीं, जीवन गतिशील हो जाता था। हम शक्ति की आराधना में लग जाते हैं। बँगला के ‘कीर्तिवासी रामायण’ के अनुसार राम ने भी शक्ति की आराधना की थी और उसी अपराजेय शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया था। यही कथा निराला की ‘राम की शक्ति की पूजा’ का आधार बनी।
वसंत में काम भस्म हुआ था और शरत् में रावण। काम भस्म होने के बाद अनंग होकर हममें जीवित है। लगता है, रावण भी अनंग होकर हममें जीवित है और आज भी सज्जनों को त्रासित करता है। मेरे एक मित्र कवि की यही मुख्य चिंता है-‘घर-घर रावण, घर-घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊँ ?’
वसंत में बहार है, मस्ती है, रंगबाजी है, रँगरेलियाँ हैं, उन्माद है; पर शरत् में गांभीर्य है, गति है, गंदगी को धो डालने की ललक है। वसंत के मूल में वासना है, शरत् के मूल में उपासना। वसंत संबद्ध है रति से, काम से; शरत् संबद्ध है शक्ति से, राम से। शायद शरत् के आगमन पर जन्म लेने के कारण ही मेरे पितामह ने मुझे राम-भक्त ‘हनुमान प्रसाद’ की संज्ञा दी। शायद इसके पीछे उनकी मंशा भी मेरे दीर्घजीवी होने की थी, जिसकी शुभकामना आज प्रातः से ही मेरे मित्र टेलीफोन पर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इन शुभकामनाओं के पीछे वैदिक ऋषियों की यह वाणी है-‘जीवेम शरदः शतम्। पश्चेम शरदः शतम् । श्रृणुयाम शरदः शतम्। प्रब्रवाम शरदः शतम्। अदीनामस्याम शरदः शतम्। भूयस्य शरदः शतात्। अर्थात्-हम सौ वर्षों तक देखते हुए जीएँ, सुनते हुए जीएँ, प्रवचन करते हुए जीएँ। अदीन होकर शान से जीएँ और सौ वर्षों से अधिक भी आनंदपूर्वक जीएँ। इन क्रियमाण शक्तियों के बिना अशक्य और असहाय होकर जीना भी कोई जीना है। धन्यवाद !
काग-ग्रास
पत्नी के श्राद्ध के दिन गो-ग्रास, श्वान-ग्रास देने के बाद जब मैं ऊपर छत
पर ‘काग-ग्रास’ देने गया तो एक भी कौआ दिखाई नहीं
दिया। पितृपक्ष और कौआ नहीं। गुड़ पड़ा ही और चींटे नदारद ! आश्चर्य की
बात तो है ही। ‘आव-आव’ और
‘काँव-काँव’ की अनेक आवाजें भी लगाई थीं, पर सुने कौन
? आवाजें आकाश में खोती चली गईं। दूर-दूर तक दृष्टि दौड़ाई, न कौआ न कौए
का पूत। अंत में लाचार होकर मुँड़ेर पर ‘काग-ग्रास’
रखकर चला आया, क्योंकि प्रतीक्षा कर रहे ब्राह्मणों को भोजन कराना था।
कर्मकांडीय वर्जना यह थी कि जब तक ब्राह्मण भोजन न कर लें तब तक स्वयं न अन्न ग्रहण करना चाहिए और न जल। इसीलिए ब्राह्मणों को विदा करने के बाद एक बार फिर ऊपर देखने गया कि किसी कौए ने कृपा की या नहीं; पर निराशा ही हाथ लगी। अब भी मुँड़ेर पर ‘काग-ग्रास’ लावारिस पड़ा था।
बात सन् 1992 पितृपक्ष की है। इसी वर्ष मेरी पत्नी का निधन हुआ था। ताजा-ताजा घटना थी। घाव हरा था। सोच में पड़ा कि यदि किसी कौए ने यह ‘ग्रास’ ग्रहण नहीं किया तो पत्नी की आत्मा भूखी रह जाएगी। भूख-प्यास भूलकर मैं केवल आसमान देखता रहा। सूरज पश्चिम की ओर ढुलकने लगा था। मन भरा-भरा था। याद आया, बचपन में जब दादी किसी पर नाराज होती थीं, उसे शाप देते हुए कहती थीं, ‘जा, तोहारे छानी पर कौओ न बैठी !’ आज सचमुच वह दिन आ गया। यह किसी क्रुद्ध वृद्ध का शाप तो नहीं है, जो मेरे लिए पितृपक्ष में कौआ भी दुर्लभ हो गया। तब तक नीचे से पुत्रवधू की आवाज आई, ‘आज क्या भूखे ही रहेंगे ?’
‘अभी तक कोई कौआ दिखाई नहीं दिया।’ मैंने कहा।
‘तब मुँड़ेर पर ‘कौरा’ रखकर चले आइए।’ बहू ने कहा’ ‘सभी लोग भोजन कर चुके हैं। केवल परिवार के ही लोग बाकी हैं। आपकी ही प्रतीक्षा की जा रही है।’
मेरे पास भी इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था।
चलते समय फिर मैंने उस ‘काग-ग्रास’ की ओर देखा। अचानक जैसे मनु ने सावधान किया, ‘वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वप्रदेमुवि।’ कौओं तथा कीड़े-मकोड़े के लिए सावधानीपूर्वक भूमि पर वलि रखनी चाहिए। जिससे मिट्टी आदि लगने से वह गंदी न हो जाए।
मैंने मुँड़ेर की वह जमीन फिर धोई, पोंछी और वह ‘काग-अंश’ रखकर, मन-ही-मन आज के पूज्य काग बंधुओं को समर्पित कर इस विश्वास के साथ नीचे चला कि कोई-न-कोई कौआ तो चला ही आएगा।
इसी संदर्भ में बिहारी याद आए-
दिन दस आदर पाइकै, कर ले आप गुमान।
जौ लौ काग सराद पच्छ, तौ लौ तव सम्मान।।
इस पक्ष में कौआ सचमुच सम्मानित हो जाता है। यदि सम्मानित होनेवाला प्राणी गुमान करे, थोड़ा-बहुत नखरा दिखाए तो आश्चर्य क्या ! यद्यपि यह भी उसकी क्षुद्रता का ही लक्षण है। हो सकता है, यह कौए का गुमान ही हो या नखरा कि भोजन के लिए बुलाया जाए और वह न आए। तब तो वह मेरे हटने पर ही आ जाएगा। आखिर मियाँजी जाएँगे कहाँ ! ‘पछताएँगे और वही चना-गुड़ खाएँगे।’
यह सोचकर नीचे चला आया और परिवार के साथ भोजन करने लगा। जैसा ऐसे अवसरों पर होता है, लोग मेरी पत्नी के गुणों की चर्चा भी करते रहे और भोजन भी चलता रहा। पर मैं उसी सोच में डूबा रहा कि यदि किसी कौए ने कृपा नहीं की तो मेरे ‘काग-ग्रास’ का क्या होगा ?
शीघ्र ही बहू ने मेरे मौन की गंभीरता को अनुभव किया और वह सबको चुप कराते हुए बोली, ‘आप लोग अम्मा की चर्चा बंद करें, पापाजी गंभीर हो गए हैं।’
‘नहीं, यह बात नहीं है।’ मैंने तुरंत प्रतिवाद किया, ‘मैं केवल यह सोच रहा हूँ कि कौए के लिए निकाले गए ‘कौरे’ का क्या होगा ? क्योंकि शाम हो ही रही है और इसी तरह दिन डूब जाएगा, तब तो कोई कौआ आने से रहा।’
कर्मकांडीय वर्जना यह थी कि जब तक ब्राह्मण भोजन न कर लें तब तक स्वयं न अन्न ग्रहण करना चाहिए और न जल। इसीलिए ब्राह्मणों को विदा करने के बाद एक बार फिर ऊपर देखने गया कि किसी कौए ने कृपा की या नहीं; पर निराशा ही हाथ लगी। अब भी मुँड़ेर पर ‘काग-ग्रास’ लावारिस पड़ा था।
बात सन् 1992 पितृपक्ष की है। इसी वर्ष मेरी पत्नी का निधन हुआ था। ताजा-ताजा घटना थी। घाव हरा था। सोच में पड़ा कि यदि किसी कौए ने यह ‘ग्रास’ ग्रहण नहीं किया तो पत्नी की आत्मा भूखी रह जाएगी। भूख-प्यास भूलकर मैं केवल आसमान देखता रहा। सूरज पश्चिम की ओर ढुलकने लगा था। मन भरा-भरा था। याद आया, बचपन में जब दादी किसी पर नाराज होती थीं, उसे शाप देते हुए कहती थीं, ‘जा, तोहारे छानी पर कौओ न बैठी !’ आज सचमुच वह दिन आ गया। यह किसी क्रुद्ध वृद्ध का शाप तो नहीं है, जो मेरे लिए पितृपक्ष में कौआ भी दुर्लभ हो गया। तब तक नीचे से पुत्रवधू की आवाज आई, ‘आज क्या भूखे ही रहेंगे ?’
‘अभी तक कोई कौआ दिखाई नहीं दिया।’ मैंने कहा।
‘तब मुँड़ेर पर ‘कौरा’ रखकर चले आइए।’ बहू ने कहा’ ‘सभी लोग भोजन कर चुके हैं। केवल परिवार के ही लोग बाकी हैं। आपकी ही प्रतीक्षा की जा रही है।’
मेरे पास भी इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था।
चलते समय फिर मैंने उस ‘काग-ग्रास’ की ओर देखा। अचानक जैसे मनु ने सावधान किया, ‘वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वप्रदेमुवि।’ कौओं तथा कीड़े-मकोड़े के लिए सावधानीपूर्वक भूमि पर वलि रखनी चाहिए। जिससे मिट्टी आदि लगने से वह गंदी न हो जाए।
मैंने मुँड़ेर की वह जमीन फिर धोई, पोंछी और वह ‘काग-अंश’ रखकर, मन-ही-मन आज के पूज्य काग बंधुओं को समर्पित कर इस विश्वास के साथ नीचे चला कि कोई-न-कोई कौआ तो चला ही आएगा।
इसी संदर्भ में बिहारी याद आए-
दिन दस आदर पाइकै, कर ले आप गुमान।
जौ लौ काग सराद पच्छ, तौ लौ तव सम्मान।।
इस पक्ष में कौआ सचमुच सम्मानित हो जाता है। यदि सम्मानित होनेवाला प्राणी गुमान करे, थोड़ा-बहुत नखरा दिखाए तो आश्चर्य क्या ! यद्यपि यह भी उसकी क्षुद्रता का ही लक्षण है। हो सकता है, यह कौए का गुमान ही हो या नखरा कि भोजन के लिए बुलाया जाए और वह न आए। तब तो वह मेरे हटने पर ही आ जाएगा। आखिर मियाँजी जाएँगे कहाँ ! ‘पछताएँगे और वही चना-गुड़ खाएँगे।’
यह सोचकर नीचे चला आया और परिवार के साथ भोजन करने लगा। जैसा ऐसे अवसरों पर होता है, लोग मेरी पत्नी के गुणों की चर्चा भी करते रहे और भोजन भी चलता रहा। पर मैं उसी सोच में डूबा रहा कि यदि किसी कौए ने कृपा नहीं की तो मेरे ‘काग-ग्रास’ का क्या होगा ?
शीघ्र ही बहू ने मेरे मौन की गंभीरता को अनुभव किया और वह सबको चुप कराते हुए बोली, ‘आप लोग अम्मा की चर्चा बंद करें, पापाजी गंभीर हो गए हैं।’
‘नहीं, यह बात नहीं है।’ मैंने तुरंत प्रतिवाद किया, ‘मैं केवल यह सोच रहा हूँ कि कौए के लिए निकाले गए ‘कौरे’ का क्या होगा ? क्योंकि शाम हो ही रही है और इसी तरह दिन डूब जाएगा, तब तो कोई कौआ आने से रहा।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book