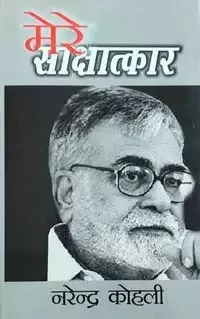|
उपन्यास >> संघर्ष की ओर संघर्ष की ओरनरेन्द्र कोहली
|
43 पाठक हैं |
||||||
राम की कथा पर आधारित श्रेष्ठ उपन्यास...
"अर्थात स्फुट घटनाओं का बंद होना, किसी बड़ी दुर्घटना की भूमिका है?" राम ने पूछा।
"कदाचित् ऐसा ही है आर्य! छोटी-छोटी टोलियां अपना पक्ष देखकर व्यापक संगठनों का अंग बनती जा रही हैं।"
"राक्षस सेनाओं के शिविर कहां हैं?" लक्ष्मण ने जिज्ञासा की।
"मुझे उसका ज्ञान नहीं भद्र!" ब्रह्मचारी बोला, "यह तो आपको कुलपति ही बता सकेंगे। वैसे भी हम आश्रम के पर्याप्त निकट पहुंच चुके हैं। आप लोग आश्रम में चलकर विश्राम करें।"
प्रवेश करते ही राम को लगा, जैसे सारा आश्रम ही परिवर्तित हो चुका था। आध्यात्मिक साधना का वातावरण तो अब भी वहां था; किंतु साथ ही शस्त्राभ्यास करती हुई विभिन्न टोलियां भी पहली ही दृष्टि में ध्यान आकर्षित करती थीं। आते-जाते प्रायः ब्रह्मचारी सशस्त्र थे तथा उनकी चाल-ढाल में सैनिक प्रशिक्षण का स्पष्ट आभास मिलता था। ऋषि ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया।
"स्वागत राम!" सुतीक्ष्ण का स्वर उल्लसित था, "मुझे भय था, मेरे पिछले व्यवहार की छाया, तुम लोगों के मार्ग की बाधा न बने।"
"सद्भावना के प्रकाश में छायाएं ठहर नहीं पातीं ऋषिवर!" राम मुस्कराए, "छायाएं कितनी ही घनी क्यों न हों।"
ऋषि ने सबको आसन देकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बोले, "वह समय भी क्या था राम! राक्षसों का आतंक जैसे हमारी हड्डी-हड्डी, मज्जा-मज्जा में धंसकर बैठ गया था। आज सोचता हूं तो आश्चर्य होता है। किस बात से भयभीत थे हम? मृत्यु से? राक्षस हमें मार तो वैसे भी डालते, हम उनका विरोध करते, न करते। हम लोग जो मनुष्य को सम्मानपूर्ण मानवीय जीवन जीने का संदेश देते हैं-स्वयं ही कितना अपमानजनक तथा कायरतापूर्ण जीवन जी रहे थे! स्वयं ही चकित हूं कि ऐसा कैसे हो गया था। मैं, गुरु अगस्त्य का शिष्य-स्वयं जाज्वल्यमान अग्नि से उसका तेज ग्रहण करने वाला मैं-कैसा भीरु हो गया था कि स्वयं तो कोई साहस कर ही नहीं पाता था; तुम जब साक्षात् वीरता सरीखे अपने शस्त्रागार के साथ आश्रम में पधारे तो मेरा मन चीत्कार करता रहा, 'राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था तुम मेरे निकट रहो, मुझ से दूर मत जाना।' और जिह्वा से मैं ऐसे वाक्य कहता रहा, जिनको सुनकर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति मेरा मुख न देखना चाहता।..."
"अब क्या हो गया है, आर्य कुलपति?" लक्ष्मण मुस्करा रहे थे।
"तुम्हें मुस्कराने का अधिकार है सौमित्र। प्रत्येक व्यक्ति को मुझ पर मुस्कराने का अधिकार है।" ऋषि गंभीर स्वर में बोले, "हम लोग सचमुच इतने बौने हो गए थे कि आज स्वयं भी अपने-आप पर मुस्कराने का मन होता है। अपनी ही दृष्टि में पतित तथा घृणित होने का इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है कि मन से सदा जिनके पक्षधर थे, आज उन्हें अपनी पक्षधरता का विश्वास दिलाने के लिए, अपने मुख से कह-कहकर स्वयं को हास्यास्पद बना रहे हैं..."
|
|||||