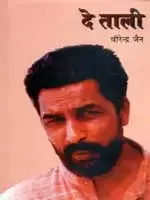|
पत्र एवं पत्रकारिता >> दे ताली दे तालीवीरेन्द्र जैन
|
197 पाठक हैं |
||||||
हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता का आज के समय क्या दायित्व है और इस का क्या प्रभाव पड़ रहा है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता इन दिनों खासी चर्चा में है। साहित्य
संबंधी पत्रिकाएँ भी इस दौर में जितनी निकल रही हैं, संभवतः किसी दौर में
नहीं निकलीं। फिर भी कोई सकारात्मक माहौल नहीं बन पा रहा। आखिर क्यों ?
इसके लिए हम किसे दोष दें ? क्या उनके मुद्दे ज्वलंत नहीं हैं ? क्या उनके सरोकार बहुजन हिताय नहीं हैं ? क्या उनका प्रचार-प्रसार संभव नहीं हो पा रहा है ? क्या उनके पाठक नहीं हैं ? क्या लेखकों के विचार पाठकों को उद्वेलेति नहीं करते ?
कमोवेश यही हाल साहित्यिक लेखन का भी नजर आ रहा है। एक साहत्यिक समालोचक की नजर में जो रचना कालजयी होती है, दूसरा उसे सालजयी भी नहीं मानता। बेहतर रचनाएँ चर्चा का एक कोना भी नहीं घेर पातीं और बदतर रचनाएँ सारा आकाश हथिया लेती हैं। यह सब संभव कैसे हो पाता ? कौन हैं वे लोग जो पाठकों को भ्रमित करते हैं, किसी रचना और रचनाकार को मुंहजोर या सिरमौर बनाने की मुहिम चलाते हैं ?
वीरेन्द्र जैन ने अपनी इन दो उपन्यासिकाओं में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। जिन दिनों ये उपन्यासिकाएँ एक लंबे अंतराल से इंडिया टुडे में धारावाहिक प्रकाशित हुई थीं, हिंदी के साहित्यिक माहौल को खासा गर्माया था। कहने की जरूरत नहीं, कभी राजकमल चौधरी की लेखनी मेरे ध्वंस (छदम उजागर करने) में काफी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल यह काम वीरेन्द्र जैन कर रहे हैं। (‘मुड़-मु़डके देखता हूँ’ आत्म कथा में)
इसके लिए हम किसे दोष दें ? क्या उनके मुद्दे ज्वलंत नहीं हैं ? क्या उनके सरोकार बहुजन हिताय नहीं हैं ? क्या उनका प्रचार-प्रसार संभव नहीं हो पा रहा है ? क्या उनके पाठक नहीं हैं ? क्या लेखकों के विचार पाठकों को उद्वेलेति नहीं करते ?
कमोवेश यही हाल साहित्यिक लेखन का भी नजर आ रहा है। एक साहत्यिक समालोचक की नजर में जो रचना कालजयी होती है, दूसरा उसे सालजयी भी नहीं मानता। बेहतर रचनाएँ चर्चा का एक कोना भी नहीं घेर पातीं और बदतर रचनाएँ सारा आकाश हथिया लेती हैं। यह सब संभव कैसे हो पाता ? कौन हैं वे लोग जो पाठकों को भ्रमित करते हैं, किसी रचना और रचनाकार को मुंहजोर या सिरमौर बनाने की मुहिम चलाते हैं ?
वीरेन्द्र जैन ने अपनी इन दो उपन्यासिकाओं में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। जिन दिनों ये उपन्यासिकाएँ एक लंबे अंतराल से इंडिया टुडे में धारावाहिक प्रकाशित हुई थीं, हिंदी के साहित्यिक माहौल को खासा गर्माया था। कहने की जरूरत नहीं, कभी राजकमल चौधरी की लेखनी मेरे ध्वंस (छदम उजागर करने) में काफी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल यह काम वीरेन्द्र जैन कर रहे हैं। (‘मुड़-मु़डके देखता हूँ’ आत्म कथा में)
राजेन्द्र यादव
सचमुच अश्लील लगता है, जब गुजरात के भूकंप में लाखों लोग तबाह
हो गए हों, शहर और पूरा प्रदेश खुले आसमान के नीचे रोटी और छत पाने के लिए
हाथ-पाँव मार रहा हो, तो हम साहित्य और संस्कृति के इन टुच्चे पक्षों को
लेकर सिर फोड़ रहे हैं।
राजेन्द्र यादव
प्रभा खेतान के सहयोग से आनेवाली पत्रिका ‘हंस’ के
स्त्री भूमंडलीकरण विशेषांक, मार्च 2001 में अपने स्तंभ ‘मेरी
तेरी उसकी बात’ के लिए वरिष्ठ कथाकार और हंस के संपादक
राजेन्द्र यादव ने जिस सुबह उक्त पंक्तियाँ लिखी होंगी, संभवताः उसी शाम
नई संसद भवन से दो फर्लांग के दायरे में आला अफसरों, धनाढ्य वर्ग और
राजनेताओं के मशहूर चेम्सफोर्ड क्लब में साहित्यकारों का जमावड़ा सुरापान
हेतु जुटा था। जुटना ही था, चूँकि जिस किसी सुबह-सवेरे कोई सात्विक उद्गार
प्रस्फुटित किया जाए, उस शाम गला तर करना लाजिमी हो जाता है। खासकर तब, जब
टीवी चैनल के साहित्य चर्चा कार्यक्रम में किसी रचनाकार की भूरि-भूरि और
उसकी प्रतिभा और अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़-चढ़ कर तारीफ कर देने का
‘कु’ या ‘सु’ कार्य कर दिया गया
हो।
उस सुबह भी यही हुआ था। एक नामवर आलोचक ने जुम्मा जुम्मा एक दशक पहले साहित्य क्षेत्र में पदार्पण करने वाली कथाकार की ऐसी कृति की जमकर तारीफ की थी जिसके बारे में बकौल एक कलाकार नयी कहानी के तीसरे सवार का कहना था कि वह हिंदी की अरुंधति, महाश्वेता और न जाने क्या-क्या है। और बतौर एक अन्य महिला कथाकार जिसमें कई मशहूर और धुरंधर उपन्यासों की गूँज सुनाई देती है। अलबत्ता उस सुरापान समारोह में राजेन्द्र जी थे या नहीं, खबर नहीं।
यों यह रचना कथाकार राजेन्द्र यादव से यहीं तक, वह भी संयोग से, वाबस्ता है। आगे यह रचना उतनी ही काल्पनिक है जितने यथार्थ राजेन्द्र जी के उक्त उद्गार हैं। जो पाठक उनके संपूर्ण उदगार पढ़ना चाहें वे हंस का उपरोक्त अंक पढें । मेरी यह रचना इस दिशा में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी।
चेम्पफोर्ड में जुटी साहित्यकर सांसदों की भीड़ सत्ता पक्ष के सांसदों की थी या प्रतिपक्ष के सांसदों की, इस बारे में ठीक-ठीक संज्ञा दे पाना कठिन है।
दरअसल भारतीय संसद और साहित्यकार संसद में यही बुनियादी अंतर होता है कि वह सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का। लेकिन हिंदी की साहित्यकार संसद में आज भी यह विभाजन स्पष्ट तो दूर अस्पष्ट रूप में भी चिह्नित नहीं किया जा सकता।
बहरहाल, चेम्सफोर्ड क्लब में उस शाम जो साहित्यकार मौजूद थे, वे अपने, तईं यह मानते थे कि साहित्य की सत्ता इन दिनों उन्हीं के हाथों में है, साहित्य में उन्हीं का सिक्का चलता है, उन्हीं का डंका बजता है, वही सनदें-मसनदें देते-लेते हैं, इसलिए वह सत्ता पक्ष कहे जा सकते थे।
लेकिन साहित्य में चूँकि सत्ता पक्ष होना आलोचना का शिकार होना भी है, संदेश की सुई के ऐन सामने होना भी है, इसलिए वे यदा-कदा अपने तेवरों से, दिखावटी गुस्से से, यथास्थितिवाद में परिवर्तन की आकांक्षा और भोथरे प्रयासों का ढिंढ़ोरा पीट-पीटकर यह भी मनवाना चाहते थे कि वे प्रतिपक्ष हैं। उन्हें यही माना जाए।
घोषित रूप से यह जमावडा़ हिंदी साहित्य को अपनी ओर हाँकने को उद्धत और सत्ता पक्ष की सिरचढी़ स्वयंसेवियों की भीड़ और उसकी लाठियों से साहित्य की स्वायत्तता को कैसे बचाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जुटा था, लेकिन हो कुछ और ही रहा था। हर किसी दूसरे के कान में तो कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था, लेकिन सामूहिक रूप से किसी को कोई संबोधित नहीं कर रहा था।
उन लाठियों से चिंतित होने के नाम पर जुटे इस जमावड़े में वे तीन लठियाँ भी मौजूद थीं, जो इन दिनों साहित्य को हाँकने में जुटी हुई थीं। इनमें सर्वप्रमुख थी राष्ट्रपिता की लंबी लाठी जो कही जाती है अहिंसक लेकिन जिसकी क्षमता घाव करे गंभीर का प्रमाण थी। यह लाठी कई बार तो बिना चले ही, बिना दिखे ही, दांडियों को अपने पीछे चलने को प्रलोभित कर लेती थी।
दूसरी पुलिसिया लाठी थी जो सीमा प्रहरी जवान की तरह जब भी हरकत में आती थी, कइयों को रौंद जाती थी, वह तो यहाँ नहीं थी, क्यों नहीं थी, यह आगे खुलासा किया जाएगा, अलबत्ता यहाँ उसकी अदना-सी साथिन लखनवी छड़ी जरूर मौजूद थी। तीसरी दलित या पिछड़ी वह लाठी थी जो देखने में तो किसी और काम आती दिखाई देती थी, लेकिन अदृश्य रूप से असहमतों के सिर फोड़ने, मार-मार कर अधमरा कर देने, पगला देने, कुत्ता बना देने के काम आती थी और सहमतों, सेवकों, समर्थिकाओं को आकाश में उनके कद से कहीं ज्यादा ऊँचा उठाने के काम भी अंजाम देती थी।
सीमा प्रहरीनुमा पुलिसिया लाठी के अलावा यहाँ लाठी दिलदाशी और लाठी जब्बारपुरी भी नहीं थी, वे तीनों यहाँ क्यों नहीं थीं, आईं नहीं थीं या बुलाई नहीं गई थीं, उन्हें साहित्यजगत की इस ज्वलंत समस्या से कुछ लेना-देना नहीं था या यहाँ जिन लोगों ने साहित्य संसद को जमा किया था, वे नहीं चाहते थे कि इस मसले पर उनकी भी राय ली जाए या उन्हें भी साथ लेकर चला जाए, यह अंदाजना कठिन नहीं था।
घोषित उद्धेश्य के लिए यह जमावड़ा नहीं जुटा था, इसका संकेत यहाँ कि उपस्थिति से भी हो रहा था। यहाँ राष्ट्रपिता विश्वभारती के राष्ट्रपुत्र देवानांप्रिय भी थे। सत्ता पक्ष की संस्तुति पर हिंदी के हित में लंदन तक मोर्चा फतह कर आए और आपातकाल के बाद से ‘मौखिक ही मौखिक है’ का सिद्धांत प्रतिपादित कर चुके, उस पर लगातार अमल कर रहे बेसहारों के सहाराश्री आलोचक जी भी थे। कभी एक्टविस्ट रहे पूर्व पत्रकार, पूर्व गुड़सहाराश्री और अब पत्रकारों के वरिष्ठ नये शूरमा भोपीली भी थे। ये तीनों ही अंतरंग वार्ताओं में उभयपक्षी घोषित किए जाते थे, अलबत्ता सार्वजनिक मंचों से उन्हें ऐसा कहने की हिम्मत अभी कोई-कोई खरे-खोटे ही कर पाते थे।
इस साहित्यकार संसद में चल रही कनबतियों से बहुत जल्द यह उजागर हो ही गया कि यह जमावड़ा यकीनन घोषित एजेंडे के लिए नहीं, अघोषित एजेंडे के लिए जुटाया गया है।
दरअलस पिछले दिनों ही इस साल के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी महिला कथाकर को दे दिया जा सकता है, और बहुत संभव है वह महिला कथाकार बंगवासिनी हो।
इस खबर ने कई साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकों को बेचैन कर दिया था। वजह यह थी कि हिंदी में हर साहित्यिक संपादक चाहे पत्रिका कैसी भी और कितने भी अल्प समय तक क्यों न संपादित करता रहा हो, एक न एक लेखिका को सामने लाने का गुमान जरूर पाले रखता था। इन दिनों जितनी साहित्यिक पत्रिकाएँ बाजार में थीं, उतनी ही लेखिकाएँ भी चर्चा में थीं, जिनके बारे में अलग-अलग संपादकों का यह दावा था कि वे उनकी, नितांत उनकी खोज हैं, लिहाजा साहित्यालोक का सारा आकाश उनके आँचल में ला समेटना उनका नैतिक-अनैतिक दायित्व है। इसके लिए चाहे पंखहीन हंस ही क्यों न उड़ाना पड़े, कैसी भी पहल क्यों न करनी पड़े, कितने ही कथादेश क्यों न खोजने पडे़ या फिर वतर्मान साहित्य के आकलन और परिवेश का कैसा भी तिया-पाँचा क्यों न करना पड़े।
हाल-फिलहाल हिंदी के साहित्याकाश पर तीन देवियों का परचम लहरा रहा था। एक थीं पणिपुत्री जिनका उपन्यास ‘धाक’ कइयों की धड़कन बढ़ाए हुए था, दूसरी थीं पणिवर्धन जिनका ‘लावा’ पूरे उफान पर था और तीसरी थीं बंगवासिनी मेनका मुरारका जिनका ‘केलिकथा’ अपने खाते में खासे बोल-कुबोल बटोर रहा था।
साहित्य अकादमी अगले साल का पुरस्कार किसी महिला कथाकार को देने का मन बना चुकी है, इस खबर ने साहित्यिक पत्रिका ‘पारा’ के संपादक यारा जी को खासा बेचैन कर दिया था। पिछले कई वर्षों से पणिपुत्री को साहित्य एकादमी में पुरस्कृत होते देखना चाहते थे। इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे थे। इन प्रयासों का ही नतीजा था कि जब एक वयोवृद्ध साहित्यकार साहित्य अकादमी की निर्णायक धुरी थे, तब पणिपुत्री के निवास पर चीफ की दावत आयोजित की गई थी। वह पणिपुत्री को पुरस्कार तो नहीं दिलवा सके, अलबत्ता बकौल मणिपुत्री उस दावत के लिए जब भी कहीं उनसे पणिपुत्री की भेट होती थी, वे उनके करीब आकर धीमे से पूछते थे, इन दिनों कौन सा उपन्यास लिख रही हो ?
एक अन्य ऐसे ही साहित्यकार जब राजधानी पधारे तब एक दोपहर राजधानी से बहिर्गमन कर वह भी प्रश्न प्रदेश गए थे और दोपहर के भोजनोपरांत पणिपुत्री के करकमलों से एक शॉल और अपनी पत्रिका के 11 आजीवन सदस्यों के चंदे के रूप में 11000 रुपये का चेक लेकर लौटे थे। वे आजीवन सदस्य कौन थे, कहाँ रहते थे, अभी पैदा भी हुए थे कि नहीं, जीवित भी थे कि नहीं, यह सब न उन्हें बताया गया था न ही उन्होंने जानने के लिए अपनी ओर से कोई पहल की थी। एक अन्य आलोचक और संपादक भी राजधानी की सारी वसुधा को धता बताते डिनर के लिए पणिपुत्री के घर पधारे थे और उन्हें भी वह सब अर्पित किया गया था जो पहले वालों को किया जा चुका था। इसके साथ अकादमी विजेता एक कवि भी अपने इलाके को छो़ड़ नये इलाके तक कार में सवार हो पहुँचे थे। ये तमाम संत-महंत या लेखक-आलोचक संपादक समागम हुए थे यारा जी के सुझाव और आदेश पर।
यह जमावड़ा भी पणिपुत्री के सौजन्य से, यारा जी की सदारत में ही आयोजित किया गया है, इसकी गवाही यहाँ जुटी साहित्यकारों की मूरतें भी दे रही थीं। पणिपुत्री स्वयं तो सपति और सपर्स मौजूद थीं ही, जिन तीनों पर इस सुरा समागम का भार था, निर्जन-सत्ता के प्रखर पत्रकार, इक न्यारे बंगले के मालिक, बीएमडब्लू सुरंग, भाभा सिन्हा, काशी-दामाद, मनोहर जी, प्रबंधक जी, मणिकांचन, विश्वकर्मा, मित्रो, सातों आसमान, दरीदा, चौथी हथेली, श्याम किशोर, साहित्य अकादमी पुरस्कार की सलाहकार समिति, चयन समिति और निर्णायक मंडल के वर्तमान ही नहीं संभावित सदस्य तक मौजूद थे। पहाड़ पर लालटेन जल रही थी, रात का रिपोर्टर भी हाजिर था, रात में हारमोनियम बजानेवाले भी गिलास थामे खड़े थे, कगार पर आग भी सुलग रही थी लेकिन दरवाजा कहीं नहीं था, न ही शहर में कर्फ्यू था।
अपनी प्रतिद्वंद्वी लाठियों, जिन्हें कभी-कभी सौजन्यतावश सहयोगी, समानधर्मी लाठियाँ भी कहना पड़ जाता था, के हरकत में आते ही, यारा जी का सक्रिय और चिंतित होना स्वाभाविक ही था। पणिपुत्री को वे अपनी निर्मिति मानते थे। यों भी कागज पर वे कुछ भी चिंताएँ उकेरते रहें, व्यवहार में ऐसी चिंताएँ ही उनका ओढ़ना-बिछौना थीं। किसे उठाना है, किसे गिराना है, कहाँ दिखना है, कहाँ छिप जाना है, इसी किस्म की चिंताएँ उनका दिन-रात का सुख चैन हरे रहती हैं, इनका निदान उन्हें प्रफुल्ल-प्रसन्न रखता है और इनमें मिली असफलता-सफलता पर उनका भक्त समुदाय, वाहवाही समाज विस्तार पाता या सिकुड़ता है।
गिलास हाथ में थामे यारा जी चहुंओर यह देखकर तसल्ली करने में व्यस्त थे कि सब आ तो गए न ! गले-गले तक तर हो तो गए न ! किसी को कोई मलाल तो नहीं, किसी की कोई इच्छा अधूरी-अतृप्त तो नहीं ! और हाँ, कोई अयाचित तो घुसपैठ करने में सफल नहीं हो गया ? जो यहाँ गला तर भी कर जाए और कल को गला फाड़-फाड़ कर यहाँ का ब्यौरा चौराहे पर सुनाने से भी बाज नहीं आए।
तभी राष्ट्रपिता विश्वभारती के राष्ट्रपुत्र अपना तमतमाता चेहरा, हालाँकि यह एक हर हाल मे खुशदिल चेहरा था, भोपाल गैस त्रासदी के दौर तक में भी यह चेहरा खुशदिल देखा जा चुका था, विश्व कविता समागम में मशगूल देखा गया था, लेकिन देखने वालों को, जैसा कि कहा जा चुका है, वैसा होने का आभास देता था, यारा जी उनकी ऐन नजर के सामने आ गया।
राष्ट्रपुत्र यारा जी के करीब आए और औरों से थोड़ा हटकर बैठे यारा जी के साथवाली कुर्सी पर बैठकर उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगे। फिर तो जब तक यह सुरा समारोह चला, इन दोनों की फुसफुस वार्ता जारी रही। इस कनबतियाँ का स्वरूप पूरे समय एक ही रहा। यानी शुरू से अन्त तक देवानांप्रिय फुसफुसाते रहे और यारा जी उनकी फुसफुसाहट पर एकचित्त हो अपना एक कान लगाये रहे।
सुरा समारोह समाप्त होने पर यों तो सभी प्रसन्न नजर आ रहे थे। जैसे गुजरात में आए भूकंप के लिए अपना सर्वस्व दान कर, बदले में आत्म-सुख पाकर बाहर आएं हों, लेकिन इनमें भी दो लोग विशेषतः प्रसन्न थे। एक तो इस समारोह की मेजबान पणिपुत्री, जिन्हें एक साथ इतने सारे कलम के सिपाहियों को सुरा पान कराकर किसी रचना पाठ से मिलने वाले सुख से कहीं अधिक सुख की प्राप्ति हुई थी और भविष्य में फल प्राप्ति का आभास मिला था और दूसरे थे प्रगतिशील विचारों की जनवादी पत्रिका पारा के संपादक यारा जी।
हालाँकि यारा जी को देखकर लग नहीं रहा था कि वे परम-प्रसन्न हैं। यों यारा जी अपनी खुशी या खंदक छिपाने में बहुत पारंगत नहीं है, फिर भी यहाँ जो इनके चेहरे पर होनी थी, वह नहीं आ पा रही थी, इसकी वजह थी खुशी के संग-साथ सहेली की तरह चेंटी एक दुविधा।
वह रात यारा जी ने बहुत बेचैनी में काटी। पहले अनिर्णय की स्थिति के चलते, और फिर निर्णय को तुरंत अमल में न ला पाने की विविशता में।
यारा जी कोई बात शुरू करने से पहले और बात पूरी करके दोनों कोहनियों को मेज पर टिकाते हैं, फिर अपनी चौड़ी, सख्त हथेलियों को मिलाते हुए जो आवाज पैदा करते हैं, उससे देखने और सुननेवालों को आभास होता है जैसे कहा जा रहा हो-‘तो फिर....दे ताली।’
अगली सुबह पत्रिका के दफ्तर में पहुँचते ही उन्होने ‘पारा’ के कनिष्ठ संपादन सहयोगी अनलकांत को अपने केबिन में बुलाया। उनके आते ही कुछ निर्देश देने को उद्दत होने से पहले ताली बजाई, फिर बोले, ‘‘ऐसा है, हमारी पत्रिका का अगला अंक सौ नहीं, डेढ़ सौ पन्नों का रहेगा। और हाँ, उसकी सौ प्रतियाँ मोटे, भारी, अच्छे कागज पर छपेगी। ध्यान रहे, यह कागज मोटा, भारी, अच्छा तो हो, लेकिन देखने में बिल्कुल वैसा हो जैसा सामान्यतः अपनी पत्रिका में इस्तेमाल होता है।’’
अनलकांत ने पूछा, ‘‘जी, अतिरिक्त पन्नों पर जो सामाग्री जाएगी, हमारा कहने का मतलब यह है कि जो जा सकती है, वह कब तक मिलेगी ? ऐसा है न सर जी, आप तो जानते हैं हम तो नितांत अकेला हूँ, फिर उसे टाइमली तैयार भी करना होगा न जी।’’
‘‘वह सब तुम्हें आज ही दे दी जाएगी। पूरी नहीं, ज्यादातर। बाकी एक-दो दिन में मिलेगी।’’
यारा जी जानते हैं कि उनके पास एक ही सहयोगी है। उन्हें स्वयं कल ही शहर से बाहर जाना है। ऐसा न हो कि कहीं इतनी अतिरिक्त सामग्री को तैयार करने में यह इतना समय लगा दे कि अंक आने में देर हो जाए। ऐसा हुआ तो उससे बिक्री पर बुरा असर पडे़गा ।
‘‘एक काम करो, वह जो तुम्हारी लंबी कहानी कई महीनों से नहीं जा पा रही है, एक तो उसी को तैयार कर लो, बीस पृष्ठ तो वही ले लेगी। पणिपुत्री की आगामी किताब ‘कदमबाई का कायाकल्प’ की जो पाँच समीक्षाएँ कंपोज्ड पडी़ हैं, पाँचों को एक साथ दे दो। बीस पन्ने उनमें खप जाएँगे। अब बचे दस या आठ पन्ने, सो उनके लिए ऐसा करते हैं, भाभा सिन्हा को कहे देते हैं कि इस बार वह अपना स्तंभ विस्तार से लिख दें। ठीक रहेगा न ? उसके बाद भी जगह बच जाए तो मेरी किताबों के प्रकाशकों के विज्ञापन छाप देना। उनसे भुगतान मैं वसूल कर लूँगा।’’
अड़तालिस-पचास पन्नों की प्रकाशन सामग्री का गणित समझाने के बाद यारा जी ने फिर वही किया, यानी--‘दे ताली।’
‘‘जी अच्छा, ऐसा ही करूँगा।’’ सहायक ने असहाय भाव से कहा। चूँकि यारा जी ताली बजा चुके थे सो अनलकांत का अब वहाँ रुके रहना संभव नहीं रह गया था। फिर भी चूँकि वे अभी भी असमंजस में थे, सो वहीं बने हुए थे।
‘‘तो ठीक है,’’ फिर ताली बजाने के बाद यारा जी नये सिरे से शुरू हुए, ‘‘तैयारियाँ करो। पत्रिका समय से आनी चाहिए। याद रखना, सौ प्रतियाँ मोटे कागज पर छपनी हैं। और हाँ, उन प्रतियों का बंडल मँगवाकर नफीस के हवाले कर देना। उसमें से एक भी प्रति इधर-उधर न हो।’’
इस बार अनलकांत ने यारा जी की ताली बजने का इंतजार नहीं किया। हालाँकि उनका असमंजस कायम था, लेकिन इस बीच उन्हें यह बोधिसत्व हो चुका था कि उनके असमंजस का निदान संपादक जी के पास तो नहीं है।
अनलकांत उसी ध्यानावस्था में केबिन से निकले और अपनी कुर्सी पर आ विराजे। उनकी बहुप्रतीक्षित कहानी ‘उपहार अंतर्वस्त्रों का’ का प्रकाशन पारा के आगामी अंक में होना तय हो गया था, लेकिन इस सूचना से लदे-फदे होने के बावजूद वे खुश नहीं हो पा रहे थे। उन्हें केवल आभास नहीं, पूरा यकीन था कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। संपादक जी ने उन्हें वह पटखनी दी थी कि न सहते बन रहा था, न सहलाते। वह लालीपॉप थमाता था जो न निगलते बन रहा था, न उगलते।
उनकी कहानी पारा में छपेगी तो जरूर, लेकिन आगामी अंक की घोषणा मेंउसकी सूचना के बिना। अब वे स्वयं जितने लोगों को कहानी छपने की सूचना दे लें और पढ़ने का आग्रह कर लें, उतनी ही गनीमत। जिनसे संपर्क नहीं साध पाएँगे उन्हें तो खबर ही न होगी कि वे अगला अंक आने पर खरीदें भी और उनकी कहानी पढें भी। अनलकांत मन ही मन यह भी जान और मान रहे थे कि उनकी कहानी छपने का निर्णय लिया ही इसलिए गया है क्योंकि समय का अभाव है। किसी और ऐसे लेखक की कहानी छापते हैं जिसका नाम अगले अंक की घोषणा में नहीं गया है। तो न तो वह खुद अगले अंक की दस-बीस प्रतियाँ खरीद पाएगा, न मित्रों-परिचितों को खरीदने के लिए प्रेरित कर पाएगा। ऐसे में उसे छापकर भी पत्रिका तीस-पचास प्रतियों की अतिरिक्त बिक्री से वंचित रह जायेगी।
पिछले चार साल से पारा में कनिष्ठ सहयोगी संपादक के रूप में काम करते-करते अनलकांत यह जान चुके थे कि इस पत्रिका की प्रसार संख्या न बढ़ रही है, न घट रही है। जिस बार जिन क्षेत्रों और शहरों के लेखकों की रचनाएँ अगले अंक में छपने की सूचना होती है, वहाँ के पत्रिका बिक्रेता बढी़ हुई संख्या में अंक मँगाते हैं, और जहाँ का कोई नहीं होता, वहाँ के बिक्रेता प्रतियाँ घटा देते हैं। यानी अनुपात वही का वही रहता है। अलबत्ता हर अंक के साथ कुछ नाराज पाठक जरूर जमा होते रहते हैं, क्योंकि प्रायः ही जिस अंक में जितने लेखकों की रचनाएँ छापने की सूचना अगले अंक के विज्ञापन में दी जाती है, किसी भी अंक में उतनी रचनाएँ समा नहीं पातीं। सो जिन रचनाओं को पढ़ने के लिए खुद उन रचनाओं के लेखकों ने ज्यादा मात्रा में और उसके प्रशंसकों ने एकाध प्रति खरीदी होती है, उनका मायूस और नाराज होने का हक बनाना लाजिमी ही कहा और माना जाना चाहिए।
अनलकांत को एक नयी दुविधा भी अपने घेरे में लिए हुए थी। आखिर ऐसी कौन-सी मुसीबत आन पड़ी है जो महीने के अंतिम दिनों में संपादक महोदय को पत्रिका के पन्ने बढा़ने पड़ रहे हैं ?
अनलकांत को खबर है कि संपादक जी तो अपना फैसला सुनाकर कल ही ‘साहित्य में लघु पत्रिकाओं का बड़ा योगदान’ विषयक गोष्ठी की अध्यक्षता करने रायपुर चले जाएँगे, यहाँ रहते तब भी खटना तो अनलकांत को ही था, अब अगर न कहता हूँ तो ऐसा न हो वे अपना इरादा ही बदल लें, और हाँ करने के बाद भी कहां चैन है ? जब तक मैं पूरे अंक की तैयारी करूँगा, तब तक ऐसा न हो, उधर रायपुर से संपादक जी का फोन आ जाए कि नहीं, बढ़े हुए पन्ने नहीं जाएँगे। तब ? तब तो सारा श्रम ही निरर्थक नहीं हो जाएगा ?
अनलकांत मनन करने लगे। इस संभावना को संपादक जी सत्य संभाषण में न बदल सकें इसका एक उपाए उनके दिमाग में भी गया। उस पर अमल करने से पहले उन्होंने इतना अलंघनीय उपाय त्वरित गति से खोज लेने के लिए अपनी पीठ थपथपाई।
ऐसा करता हूं यह खुशखबरी पणिपुत्री को दे देता हूँ। बहाना है ही, किताब का आवरण चाहिए होगा कि नहीं ? तब जरूर संपादक जी इस फैसले को फिर से बदलने के बारे में कतई नहीं सोचेंगे और सोचा भी तो अमल में नहीं ला सकेंगे।
जिस उपाय को त्वरित गति से सोच जाने के एवज में अनलकांत ने क्षण भर पहले अपनी पीठ थपथपाई थी वह उपाय अभी उनके मन में पुख्ता घर बना भी न पाया था कि उन्हें एक नयी आशंका ने घेरा। आशंका भी ऐसी कि उनके पिछले इरादे को उनके मन से सिरे ही धो-पोंछ दिया।
मान लो, पत्रिका अतिरिक्त पन्नों के साथ ही छपी, और उसमें मेरी कहानी भी रही,
उस सुबह भी यही हुआ था। एक नामवर आलोचक ने जुम्मा जुम्मा एक दशक पहले साहित्य क्षेत्र में पदार्पण करने वाली कथाकार की ऐसी कृति की जमकर तारीफ की थी जिसके बारे में बकौल एक कलाकार नयी कहानी के तीसरे सवार का कहना था कि वह हिंदी की अरुंधति, महाश्वेता और न जाने क्या-क्या है। और बतौर एक अन्य महिला कथाकार जिसमें कई मशहूर और धुरंधर उपन्यासों की गूँज सुनाई देती है। अलबत्ता उस सुरापान समारोह में राजेन्द्र जी थे या नहीं, खबर नहीं।
यों यह रचना कथाकार राजेन्द्र यादव से यहीं तक, वह भी संयोग से, वाबस्ता है। आगे यह रचना उतनी ही काल्पनिक है जितने यथार्थ राजेन्द्र जी के उक्त उद्गार हैं। जो पाठक उनके संपूर्ण उदगार पढ़ना चाहें वे हंस का उपरोक्त अंक पढें । मेरी यह रचना इस दिशा में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी।
चेम्पफोर्ड में जुटी साहित्यकर सांसदों की भीड़ सत्ता पक्ष के सांसदों की थी या प्रतिपक्ष के सांसदों की, इस बारे में ठीक-ठीक संज्ञा दे पाना कठिन है।
दरअसल भारतीय संसद और साहित्यकार संसद में यही बुनियादी अंतर होता है कि वह सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का। लेकिन हिंदी की साहित्यकार संसद में आज भी यह विभाजन स्पष्ट तो दूर अस्पष्ट रूप में भी चिह्नित नहीं किया जा सकता।
बहरहाल, चेम्सफोर्ड क्लब में उस शाम जो साहित्यकार मौजूद थे, वे अपने, तईं यह मानते थे कि साहित्य की सत्ता इन दिनों उन्हीं के हाथों में है, साहित्य में उन्हीं का सिक्का चलता है, उन्हीं का डंका बजता है, वही सनदें-मसनदें देते-लेते हैं, इसलिए वह सत्ता पक्ष कहे जा सकते थे।
लेकिन साहित्य में चूँकि सत्ता पक्ष होना आलोचना का शिकार होना भी है, संदेश की सुई के ऐन सामने होना भी है, इसलिए वे यदा-कदा अपने तेवरों से, दिखावटी गुस्से से, यथास्थितिवाद में परिवर्तन की आकांक्षा और भोथरे प्रयासों का ढिंढ़ोरा पीट-पीटकर यह भी मनवाना चाहते थे कि वे प्रतिपक्ष हैं। उन्हें यही माना जाए।
घोषित रूप से यह जमावडा़ हिंदी साहित्य को अपनी ओर हाँकने को उद्धत और सत्ता पक्ष की सिरचढी़ स्वयंसेवियों की भीड़ और उसकी लाठियों से साहित्य की स्वायत्तता को कैसे बचाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जुटा था, लेकिन हो कुछ और ही रहा था। हर किसी दूसरे के कान में तो कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था, लेकिन सामूहिक रूप से किसी को कोई संबोधित नहीं कर रहा था।
उन लाठियों से चिंतित होने के नाम पर जुटे इस जमावड़े में वे तीन लठियाँ भी मौजूद थीं, जो इन दिनों साहित्य को हाँकने में जुटी हुई थीं। इनमें सर्वप्रमुख थी राष्ट्रपिता की लंबी लाठी जो कही जाती है अहिंसक लेकिन जिसकी क्षमता घाव करे गंभीर का प्रमाण थी। यह लाठी कई बार तो बिना चले ही, बिना दिखे ही, दांडियों को अपने पीछे चलने को प्रलोभित कर लेती थी।
दूसरी पुलिसिया लाठी थी जो सीमा प्रहरी जवान की तरह जब भी हरकत में आती थी, कइयों को रौंद जाती थी, वह तो यहाँ नहीं थी, क्यों नहीं थी, यह आगे खुलासा किया जाएगा, अलबत्ता यहाँ उसकी अदना-सी साथिन लखनवी छड़ी जरूर मौजूद थी। तीसरी दलित या पिछड़ी वह लाठी थी जो देखने में तो किसी और काम आती दिखाई देती थी, लेकिन अदृश्य रूप से असहमतों के सिर फोड़ने, मार-मार कर अधमरा कर देने, पगला देने, कुत्ता बना देने के काम आती थी और सहमतों, सेवकों, समर्थिकाओं को आकाश में उनके कद से कहीं ज्यादा ऊँचा उठाने के काम भी अंजाम देती थी।
सीमा प्रहरीनुमा पुलिसिया लाठी के अलावा यहाँ लाठी दिलदाशी और लाठी जब्बारपुरी भी नहीं थी, वे तीनों यहाँ क्यों नहीं थीं, आईं नहीं थीं या बुलाई नहीं गई थीं, उन्हें साहित्यजगत की इस ज्वलंत समस्या से कुछ लेना-देना नहीं था या यहाँ जिन लोगों ने साहित्य संसद को जमा किया था, वे नहीं चाहते थे कि इस मसले पर उनकी भी राय ली जाए या उन्हें भी साथ लेकर चला जाए, यह अंदाजना कठिन नहीं था।
घोषित उद्धेश्य के लिए यह जमावड़ा नहीं जुटा था, इसका संकेत यहाँ कि उपस्थिति से भी हो रहा था। यहाँ राष्ट्रपिता विश्वभारती के राष्ट्रपुत्र देवानांप्रिय भी थे। सत्ता पक्ष की संस्तुति पर हिंदी के हित में लंदन तक मोर्चा फतह कर आए और आपातकाल के बाद से ‘मौखिक ही मौखिक है’ का सिद्धांत प्रतिपादित कर चुके, उस पर लगातार अमल कर रहे बेसहारों के सहाराश्री आलोचक जी भी थे। कभी एक्टविस्ट रहे पूर्व पत्रकार, पूर्व गुड़सहाराश्री और अब पत्रकारों के वरिष्ठ नये शूरमा भोपीली भी थे। ये तीनों ही अंतरंग वार्ताओं में उभयपक्षी घोषित किए जाते थे, अलबत्ता सार्वजनिक मंचों से उन्हें ऐसा कहने की हिम्मत अभी कोई-कोई खरे-खोटे ही कर पाते थे।
इस साहित्यकार संसद में चल रही कनबतियों से बहुत जल्द यह उजागर हो ही गया कि यह जमावड़ा यकीनन घोषित एजेंडे के लिए नहीं, अघोषित एजेंडे के लिए जुटाया गया है।
दरअलस पिछले दिनों ही इस साल के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी महिला कथाकर को दे दिया जा सकता है, और बहुत संभव है वह महिला कथाकार बंगवासिनी हो।
इस खबर ने कई साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकों को बेचैन कर दिया था। वजह यह थी कि हिंदी में हर साहित्यिक संपादक चाहे पत्रिका कैसी भी और कितने भी अल्प समय तक क्यों न संपादित करता रहा हो, एक न एक लेखिका को सामने लाने का गुमान जरूर पाले रखता था। इन दिनों जितनी साहित्यिक पत्रिकाएँ बाजार में थीं, उतनी ही लेखिकाएँ भी चर्चा में थीं, जिनके बारे में अलग-अलग संपादकों का यह दावा था कि वे उनकी, नितांत उनकी खोज हैं, लिहाजा साहित्यालोक का सारा आकाश उनके आँचल में ला समेटना उनका नैतिक-अनैतिक दायित्व है। इसके लिए चाहे पंखहीन हंस ही क्यों न उड़ाना पड़े, कैसी भी पहल क्यों न करनी पड़े, कितने ही कथादेश क्यों न खोजने पडे़ या फिर वतर्मान साहित्य के आकलन और परिवेश का कैसा भी तिया-पाँचा क्यों न करना पड़े।
हाल-फिलहाल हिंदी के साहित्याकाश पर तीन देवियों का परचम लहरा रहा था। एक थीं पणिपुत्री जिनका उपन्यास ‘धाक’ कइयों की धड़कन बढ़ाए हुए था, दूसरी थीं पणिवर्धन जिनका ‘लावा’ पूरे उफान पर था और तीसरी थीं बंगवासिनी मेनका मुरारका जिनका ‘केलिकथा’ अपने खाते में खासे बोल-कुबोल बटोर रहा था।
साहित्य अकादमी अगले साल का पुरस्कार किसी महिला कथाकार को देने का मन बना चुकी है, इस खबर ने साहित्यिक पत्रिका ‘पारा’ के संपादक यारा जी को खासा बेचैन कर दिया था। पिछले कई वर्षों से पणिपुत्री को साहित्य एकादमी में पुरस्कृत होते देखना चाहते थे। इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे थे। इन प्रयासों का ही नतीजा था कि जब एक वयोवृद्ध साहित्यकार साहित्य अकादमी की निर्णायक धुरी थे, तब पणिपुत्री के निवास पर चीफ की दावत आयोजित की गई थी। वह पणिपुत्री को पुरस्कार तो नहीं दिलवा सके, अलबत्ता बकौल मणिपुत्री उस दावत के लिए जब भी कहीं उनसे पणिपुत्री की भेट होती थी, वे उनके करीब आकर धीमे से पूछते थे, इन दिनों कौन सा उपन्यास लिख रही हो ?
एक अन्य ऐसे ही साहित्यकार जब राजधानी पधारे तब एक दोपहर राजधानी से बहिर्गमन कर वह भी प्रश्न प्रदेश गए थे और दोपहर के भोजनोपरांत पणिपुत्री के करकमलों से एक शॉल और अपनी पत्रिका के 11 आजीवन सदस्यों के चंदे के रूप में 11000 रुपये का चेक लेकर लौटे थे। वे आजीवन सदस्य कौन थे, कहाँ रहते थे, अभी पैदा भी हुए थे कि नहीं, जीवित भी थे कि नहीं, यह सब न उन्हें बताया गया था न ही उन्होंने जानने के लिए अपनी ओर से कोई पहल की थी। एक अन्य आलोचक और संपादक भी राजधानी की सारी वसुधा को धता बताते डिनर के लिए पणिपुत्री के घर पधारे थे और उन्हें भी वह सब अर्पित किया गया था जो पहले वालों को किया जा चुका था। इसके साथ अकादमी विजेता एक कवि भी अपने इलाके को छो़ड़ नये इलाके तक कार में सवार हो पहुँचे थे। ये तमाम संत-महंत या लेखक-आलोचक संपादक समागम हुए थे यारा जी के सुझाव और आदेश पर।
यह जमावड़ा भी पणिपुत्री के सौजन्य से, यारा जी की सदारत में ही आयोजित किया गया है, इसकी गवाही यहाँ जुटी साहित्यकारों की मूरतें भी दे रही थीं। पणिपुत्री स्वयं तो सपति और सपर्स मौजूद थीं ही, जिन तीनों पर इस सुरा समागम का भार था, निर्जन-सत्ता के प्रखर पत्रकार, इक न्यारे बंगले के मालिक, बीएमडब्लू सुरंग, भाभा सिन्हा, काशी-दामाद, मनोहर जी, प्रबंधक जी, मणिकांचन, विश्वकर्मा, मित्रो, सातों आसमान, दरीदा, चौथी हथेली, श्याम किशोर, साहित्य अकादमी पुरस्कार की सलाहकार समिति, चयन समिति और निर्णायक मंडल के वर्तमान ही नहीं संभावित सदस्य तक मौजूद थे। पहाड़ पर लालटेन जल रही थी, रात का रिपोर्टर भी हाजिर था, रात में हारमोनियम बजानेवाले भी गिलास थामे खड़े थे, कगार पर आग भी सुलग रही थी लेकिन दरवाजा कहीं नहीं था, न ही शहर में कर्फ्यू था।
अपनी प्रतिद्वंद्वी लाठियों, जिन्हें कभी-कभी सौजन्यतावश सहयोगी, समानधर्मी लाठियाँ भी कहना पड़ जाता था, के हरकत में आते ही, यारा जी का सक्रिय और चिंतित होना स्वाभाविक ही था। पणिपुत्री को वे अपनी निर्मिति मानते थे। यों भी कागज पर वे कुछ भी चिंताएँ उकेरते रहें, व्यवहार में ऐसी चिंताएँ ही उनका ओढ़ना-बिछौना थीं। किसे उठाना है, किसे गिराना है, कहाँ दिखना है, कहाँ छिप जाना है, इसी किस्म की चिंताएँ उनका दिन-रात का सुख चैन हरे रहती हैं, इनका निदान उन्हें प्रफुल्ल-प्रसन्न रखता है और इनमें मिली असफलता-सफलता पर उनका भक्त समुदाय, वाहवाही समाज विस्तार पाता या सिकुड़ता है।
गिलास हाथ में थामे यारा जी चहुंओर यह देखकर तसल्ली करने में व्यस्त थे कि सब आ तो गए न ! गले-गले तक तर हो तो गए न ! किसी को कोई मलाल तो नहीं, किसी की कोई इच्छा अधूरी-अतृप्त तो नहीं ! और हाँ, कोई अयाचित तो घुसपैठ करने में सफल नहीं हो गया ? जो यहाँ गला तर भी कर जाए और कल को गला फाड़-फाड़ कर यहाँ का ब्यौरा चौराहे पर सुनाने से भी बाज नहीं आए।
तभी राष्ट्रपिता विश्वभारती के राष्ट्रपुत्र अपना तमतमाता चेहरा, हालाँकि यह एक हर हाल मे खुशदिल चेहरा था, भोपाल गैस त्रासदी के दौर तक में भी यह चेहरा खुशदिल देखा जा चुका था, विश्व कविता समागम में मशगूल देखा गया था, लेकिन देखने वालों को, जैसा कि कहा जा चुका है, वैसा होने का आभास देता था, यारा जी उनकी ऐन नजर के सामने आ गया।
राष्ट्रपुत्र यारा जी के करीब आए और औरों से थोड़ा हटकर बैठे यारा जी के साथवाली कुर्सी पर बैठकर उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगे। फिर तो जब तक यह सुरा समारोह चला, इन दोनों की फुसफुस वार्ता जारी रही। इस कनबतियाँ का स्वरूप पूरे समय एक ही रहा। यानी शुरू से अन्त तक देवानांप्रिय फुसफुसाते रहे और यारा जी उनकी फुसफुसाहट पर एकचित्त हो अपना एक कान लगाये रहे।
सुरा समारोह समाप्त होने पर यों तो सभी प्रसन्न नजर आ रहे थे। जैसे गुजरात में आए भूकंप के लिए अपना सर्वस्व दान कर, बदले में आत्म-सुख पाकर बाहर आएं हों, लेकिन इनमें भी दो लोग विशेषतः प्रसन्न थे। एक तो इस समारोह की मेजबान पणिपुत्री, जिन्हें एक साथ इतने सारे कलम के सिपाहियों को सुरा पान कराकर किसी रचना पाठ से मिलने वाले सुख से कहीं अधिक सुख की प्राप्ति हुई थी और भविष्य में फल प्राप्ति का आभास मिला था और दूसरे थे प्रगतिशील विचारों की जनवादी पत्रिका पारा के संपादक यारा जी।
हालाँकि यारा जी को देखकर लग नहीं रहा था कि वे परम-प्रसन्न हैं। यों यारा जी अपनी खुशी या खंदक छिपाने में बहुत पारंगत नहीं है, फिर भी यहाँ जो इनके चेहरे पर होनी थी, वह नहीं आ पा रही थी, इसकी वजह थी खुशी के संग-साथ सहेली की तरह चेंटी एक दुविधा।
वह रात यारा जी ने बहुत बेचैनी में काटी। पहले अनिर्णय की स्थिति के चलते, और फिर निर्णय को तुरंत अमल में न ला पाने की विविशता में।
यारा जी कोई बात शुरू करने से पहले और बात पूरी करके दोनों कोहनियों को मेज पर टिकाते हैं, फिर अपनी चौड़ी, सख्त हथेलियों को मिलाते हुए जो आवाज पैदा करते हैं, उससे देखने और सुननेवालों को आभास होता है जैसे कहा जा रहा हो-‘तो फिर....दे ताली।’
अगली सुबह पत्रिका के दफ्तर में पहुँचते ही उन्होने ‘पारा’ के कनिष्ठ संपादन सहयोगी अनलकांत को अपने केबिन में बुलाया। उनके आते ही कुछ निर्देश देने को उद्दत होने से पहले ताली बजाई, फिर बोले, ‘‘ऐसा है, हमारी पत्रिका का अगला अंक सौ नहीं, डेढ़ सौ पन्नों का रहेगा। और हाँ, उसकी सौ प्रतियाँ मोटे, भारी, अच्छे कागज पर छपेगी। ध्यान रहे, यह कागज मोटा, भारी, अच्छा तो हो, लेकिन देखने में बिल्कुल वैसा हो जैसा सामान्यतः अपनी पत्रिका में इस्तेमाल होता है।’’
अनलकांत ने पूछा, ‘‘जी, अतिरिक्त पन्नों पर जो सामाग्री जाएगी, हमारा कहने का मतलब यह है कि जो जा सकती है, वह कब तक मिलेगी ? ऐसा है न सर जी, आप तो जानते हैं हम तो नितांत अकेला हूँ, फिर उसे टाइमली तैयार भी करना होगा न जी।’’
‘‘वह सब तुम्हें आज ही दे दी जाएगी। पूरी नहीं, ज्यादातर। बाकी एक-दो दिन में मिलेगी।’’
यारा जी जानते हैं कि उनके पास एक ही सहयोगी है। उन्हें स्वयं कल ही शहर से बाहर जाना है। ऐसा न हो कि कहीं इतनी अतिरिक्त सामग्री को तैयार करने में यह इतना समय लगा दे कि अंक आने में देर हो जाए। ऐसा हुआ तो उससे बिक्री पर बुरा असर पडे़गा ।
‘‘एक काम करो, वह जो तुम्हारी लंबी कहानी कई महीनों से नहीं जा पा रही है, एक तो उसी को तैयार कर लो, बीस पृष्ठ तो वही ले लेगी। पणिपुत्री की आगामी किताब ‘कदमबाई का कायाकल्प’ की जो पाँच समीक्षाएँ कंपोज्ड पडी़ हैं, पाँचों को एक साथ दे दो। बीस पन्ने उनमें खप जाएँगे। अब बचे दस या आठ पन्ने, सो उनके लिए ऐसा करते हैं, भाभा सिन्हा को कहे देते हैं कि इस बार वह अपना स्तंभ विस्तार से लिख दें। ठीक रहेगा न ? उसके बाद भी जगह बच जाए तो मेरी किताबों के प्रकाशकों के विज्ञापन छाप देना। उनसे भुगतान मैं वसूल कर लूँगा।’’
अड़तालिस-पचास पन्नों की प्रकाशन सामग्री का गणित समझाने के बाद यारा जी ने फिर वही किया, यानी--‘दे ताली।’
‘‘जी अच्छा, ऐसा ही करूँगा।’’ सहायक ने असहाय भाव से कहा। चूँकि यारा जी ताली बजा चुके थे सो अनलकांत का अब वहाँ रुके रहना संभव नहीं रह गया था। फिर भी चूँकि वे अभी भी असमंजस में थे, सो वहीं बने हुए थे।
‘‘तो ठीक है,’’ फिर ताली बजाने के बाद यारा जी नये सिरे से शुरू हुए, ‘‘तैयारियाँ करो। पत्रिका समय से आनी चाहिए। याद रखना, सौ प्रतियाँ मोटे कागज पर छपनी हैं। और हाँ, उन प्रतियों का बंडल मँगवाकर नफीस के हवाले कर देना। उसमें से एक भी प्रति इधर-उधर न हो।’’
इस बार अनलकांत ने यारा जी की ताली बजने का इंतजार नहीं किया। हालाँकि उनका असमंजस कायम था, लेकिन इस बीच उन्हें यह बोधिसत्व हो चुका था कि उनके असमंजस का निदान संपादक जी के पास तो नहीं है।
अनलकांत उसी ध्यानावस्था में केबिन से निकले और अपनी कुर्सी पर आ विराजे। उनकी बहुप्रतीक्षित कहानी ‘उपहार अंतर्वस्त्रों का’ का प्रकाशन पारा के आगामी अंक में होना तय हो गया था, लेकिन इस सूचना से लदे-फदे होने के बावजूद वे खुश नहीं हो पा रहे थे। उन्हें केवल आभास नहीं, पूरा यकीन था कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। संपादक जी ने उन्हें वह पटखनी दी थी कि न सहते बन रहा था, न सहलाते। वह लालीपॉप थमाता था जो न निगलते बन रहा था, न उगलते।
उनकी कहानी पारा में छपेगी तो जरूर, लेकिन आगामी अंक की घोषणा मेंउसकी सूचना के बिना। अब वे स्वयं जितने लोगों को कहानी छपने की सूचना दे लें और पढ़ने का आग्रह कर लें, उतनी ही गनीमत। जिनसे संपर्क नहीं साध पाएँगे उन्हें तो खबर ही न होगी कि वे अगला अंक आने पर खरीदें भी और उनकी कहानी पढें भी। अनलकांत मन ही मन यह भी जान और मान रहे थे कि उनकी कहानी छपने का निर्णय लिया ही इसलिए गया है क्योंकि समय का अभाव है। किसी और ऐसे लेखक की कहानी छापते हैं जिसका नाम अगले अंक की घोषणा में नहीं गया है। तो न तो वह खुद अगले अंक की दस-बीस प्रतियाँ खरीद पाएगा, न मित्रों-परिचितों को खरीदने के लिए प्रेरित कर पाएगा। ऐसे में उसे छापकर भी पत्रिका तीस-पचास प्रतियों की अतिरिक्त बिक्री से वंचित रह जायेगी।
पिछले चार साल से पारा में कनिष्ठ सहयोगी संपादक के रूप में काम करते-करते अनलकांत यह जान चुके थे कि इस पत्रिका की प्रसार संख्या न बढ़ रही है, न घट रही है। जिस बार जिन क्षेत्रों और शहरों के लेखकों की रचनाएँ अगले अंक में छपने की सूचना होती है, वहाँ के पत्रिका बिक्रेता बढी़ हुई संख्या में अंक मँगाते हैं, और जहाँ का कोई नहीं होता, वहाँ के बिक्रेता प्रतियाँ घटा देते हैं। यानी अनुपात वही का वही रहता है। अलबत्ता हर अंक के साथ कुछ नाराज पाठक जरूर जमा होते रहते हैं, क्योंकि प्रायः ही जिस अंक में जितने लेखकों की रचनाएँ छापने की सूचना अगले अंक के विज्ञापन में दी जाती है, किसी भी अंक में उतनी रचनाएँ समा नहीं पातीं। सो जिन रचनाओं को पढ़ने के लिए खुद उन रचनाओं के लेखकों ने ज्यादा मात्रा में और उसके प्रशंसकों ने एकाध प्रति खरीदी होती है, उनका मायूस और नाराज होने का हक बनाना लाजिमी ही कहा और माना जाना चाहिए।
अनलकांत को एक नयी दुविधा भी अपने घेरे में लिए हुए थी। आखिर ऐसी कौन-सी मुसीबत आन पड़ी है जो महीने के अंतिम दिनों में संपादक महोदय को पत्रिका के पन्ने बढा़ने पड़ रहे हैं ?
अनलकांत को खबर है कि संपादक जी तो अपना फैसला सुनाकर कल ही ‘साहित्य में लघु पत्रिकाओं का बड़ा योगदान’ विषयक गोष्ठी की अध्यक्षता करने रायपुर चले जाएँगे, यहाँ रहते तब भी खटना तो अनलकांत को ही था, अब अगर न कहता हूँ तो ऐसा न हो वे अपना इरादा ही बदल लें, और हाँ करने के बाद भी कहां चैन है ? जब तक मैं पूरे अंक की तैयारी करूँगा, तब तक ऐसा न हो, उधर रायपुर से संपादक जी का फोन आ जाए कि नहीं, बढ़े हुए पन्ने नहीं जाएँगे। तब ? तब तो सारा श्रम ही निरर्थक नहीं हो जाएगा ?
अनलकांत मनन करने लगे। इस संभावना को संपादक जी सत्य संभाषण में न बदल सकें इसका एक उपाए उनके दिमाग में भी गया। उस पर अमल करने से पहले उन्होंने इतना अलंघनीय उपाय त्वरित गति से खोज लेने के लिए अपनी पीठ थपथपाई।
ऐसा करता हूं यह खुशखबरी पणिपुत्री को दे देता हूँ। बहाना है ही, किताब का आवरण चाहिए होगा कि नहीं ? तब जरूर संपादक जी इस फैसले को फिर से बदलने के बारे में कतई नहीं सोचेंगे और सोचा भी तो अमल में नहीं ला सकेंगे।
जिस उपाय को त्वरित गति से सोच जाने के एवज में अनलकांत ने क्षण भर पहले अपनी पीठ थपथपाई थी वह उपाय अभी उनके मन में पुख्ता घर बना भी न पाया था कि उन्हें एक नयी आशंका ने घेरा। आशंका भी ऐसी कि उनके पिछले इरादे को उनके मन से सिरे ही धो-पोंछ दिया।
मान लो, पत्रिका अतिरिक्त पन्नों के साथ ही छपी, और उसमें मेरी कहानी भी रही,
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book