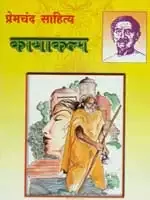|
सदाबहार >> कायाकल्प कायाकल्पप्रेमचंद
|
237 पाठक हैं |
|||||||
कायाकल्प पुस्तक का कागजी संस्करण...
Kayakalp
कागजी संस्करण
कायाकल्प
1
दोपहर का समय था; चारों तरफ अँधेरा था। आकाश में तारे छिटके हुए थे। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो संसार से जीवन का लोप हो गया हो। हवा भी बन्द हो गई थी। सूर्य-ग्रहण लगा हुआ था। त्रिवेणी के घाट पर यात्रियों की ऐसी भीड़ थी, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वे सभी हिन्दू, जिनके दिल में श्रद्धा और धर्म का अनुराग था, भारत के हर एक प्रान्त से इस महान अवसर पर त्रिवेणी की पावन धारा में अपने पापों का विसर्जन करने के लिए आ पहुँचे थे, मानो उस अँधेरे में भक्ति और विश्वास ने अधर्म पर छापा मारने के लिए अपनी असंख्य सेना सजाई हो। लोग इतने उत्साह से त्रिवेणी के सँकरे घाट की ओर गिरते-पड़ते लपके चले जाते थे कि यदि जल की शीतल धारा की जगह अग्नि का जलता हुआ कुण्ड होता, तो भी लोग उसमें कूदते हुए ज़रा भी न झिझकते !
कितने आदमी कुचले गए, कितने डूब गए, कितने खो गए, कितने अपंग हो गए, इसका अनुमान करना कठिन है। धर्म का विकट संग्राम था। एक तो सूर्य-ग्रहण, उस पर यह असाधारण अद्भुत प्राकृतिक छटा ! सारा दृश्य धार्मिक वृत्तियों को जगानेवाला था। दोपहर को तारों का प्रकाश माया के परदे को फाड़कर आत्मा को आलोकित करता हुआ मालूम होता था। वैज्ञानिकों की बात जाने दीजिए, पर जनता में न जाने कितने दिनों से वह विश्वास फैला हुआ था कि तारागण दिन को कहीं किसी सागर में डूब जाते हैं। आज वही तारागण आँखों के सामने चमक रहे थे, फिर भक्ति क्यों न जाग उठे ! सद्वृत्तियाँ क्यों न आँखें खोल दें !
घण्टे भर के बाद फिर प्रकाश होने लगा, तारागण फिर अदृश्य हो गए, सूर्य भगवान की समाधि टूटने लगी।
यात्रीगण अपने-अपने पापों की गठरियाँ त्रिवेणी में डालकर जाने लगे। संध्या होते-होते घाट पर सन्नाटा छा गया। हाँ, कुछ घायल, कुछ अधमरे प्राणी जहाँ-तहाँ पड़े कराह रहे थे और ऊँचे कगार से कुछ दूर पर एक नाली में पड़ी तीन-चार साल की एक लड़की चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थी।
सेवा समितियों के युवक, जो अब तक भीड़ सँभालने का विफल प्रयत्न कर रहे थे, अब डोलियाँ कंधों पर ले-लेकर घायलों और भूले भटकों की खबर लेने आ पहुँचे। सेवा और दया का कितना अनुपम दृश्य था।
सहसा एक युवक के कानों में उस बालिका के रोने की आवाज पड़ी। अपने साथी से बोला—यशोदा, उधर कोई लड़का रो रहा है।
यशोदा-हाँ, मालूम तो होता है। इन मूर्खों को कोई कैसे समझाए कि यहाँ बच्चों को लाने का काम नहीं। चलो, देखें।
दोनों ने उधर जाकर देखा, तो एक बालिका नाली में पड़ी रो रही है। गोरा रंग था, भरा हुआ शरीर, बड़ी-बड़ी आँखें, गोरा मुखड़ा, सिर से पाँव तक गहनों से लदी हुई। किसी अच्छे घर की लड़की थी। रोते-रोते उसकी आँखें लाल हो गयी थीं। इन दोनों युवकों को देखकर डरी और चिल्लाकर रो पड़ी। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोला—बेटी, रो मत, हम तुझे तेरी अम्मा के घर पहुँचा देंगे। तुझी को खोज रहे थे। तेरे बाप का क्या नाम है ?
लड़की चुप तो हो गई, पर संशय की दृष्टि से देख-देख सिसक रही थी। इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सकी।
यशोदा ने फिर चुमकारकर पूछा—बेटी, तेरा घर कहाँ है ?
लड़की ने कोई जवाब न दिया।
यशोदा : अब बताओ महमूद, क्या करें ?
महमूद एक अमीर मुसलमान का लड़का था। यशोदानन्दन से उसकी बड़ी दोस्ती थी। उसके साथ वह भी सेवासमिति में दाखिल हो गया था। बोला—क्या बताऊँ ? कैंप में ले चलो, शायद कुछ पता चले।
यशोदा : अभागे ज़रा-ज़रा से बच्चों को लाते हैं और इतना भी नहीं करते कि उन्हें अपना नाम और पता तो याद करा दें।
महमूद : क्यों बिटिया, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है ?
लड़की ने धीरेसे कहा—बाबूजी !
महमूद—तुम्हारा घर इसी शहर में है या कहीं और ?
लड़की—मैं तो बाबूजी के साथ लेल पर आयी थी !
महमूद—तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं ?
लड़की—कुछ नहीं कलते।
यशोदा : इस वक़्त अगर इसका बाप मिल जाए तो सच कहता हूँ, बिना मारे न छोड़ूँ। बच्चू गहने पहनाकर लाये थे, जाने कोई तमाशा देखने आये हों !
महमूद—और मेरा जी चाहता है कि तुम्हें पीटूँ। मियाँ-बीवी यहाँ आये तो बच्चे को किस पर छोड़ आते। घर में और कोई न हो तो ?
यशोदा : तो फिर उन्हीं को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी ?
महमूद : तुम ‘एथीइस्ट’ (नास्तिक) हो; तुम क्या जानो की सच्चा मज़हबी जोश किसे कहते हैं ?
यशोदा : ऐसे मज़हबी जोश को दूर से ही सलाम करता हूँ। इस वक़्त दोनों मियाँ-बीवी हाय-हाय कर रहे होंगे।
महमूद—कौन जाने, वे भी यहीं कुचल-कुचला गए हों।
लड़की ने साहस कर कहा—तुम हमें घल पहुँचा दोगे ? बाबूजी तुमको पैछा देंगे !
यशोदा : अच्छा बेटी, चलो, तुम्हारे बाबूजी को खोजें।
दोनों मित्र बालिका को लिए हुए कैंप में आये, यहाँ पर कुछ पता न चला। तब दोनों उस तरफ गये, जहाँ मैदान में बहुत से यात्री पड़े हुए थे। महमूद ने बालिका को कन्धे पर बैठा लिया और यशोदानन्दन चारों तरफ़ चिल्लाते फिरे—यह किसकी लड़की है ? किसी की लड़की तो नहीं खो गई ? यह आवाज़ें सुनकर कितने ही यात्री, हाँ-हाँ, कहाँ-कहाँ, करके दौड़े; पर लड़की को देखकर निराश लौट गए।
चिराग़ जले तक दोनों मित्र घूमते रहे। नीचे-ऊपर, क़िले के आस-पास, रेल के स्टेशन पर, अलोपी देवी के मन्दिर की तरफ यात्री-ही-यात्री पड़े हुए थे; पर बालिका के माता-पिता का कहीं पता न चला। आखिर निराश होकर दोनों आदमी कैंप लौट आये।
दूसरे दिन समिति के और कई सेवकों ने फिर पता लगाना शुरू किया। दिन-भर दौड़े, सारा प्रयाग छान मारा, सभी धर्मशालाओं की ख़ाक छानी; पर कहीं पता न चला।
तीसरे दिन समाचार-पत्रों में नोटिस दिया गया और दो दिन वहाँ और रहकर समिति आगरे लौट गयी। लड़की को भी अपने साथ लेती गयी। उसे आशा थी कि समाचार-पत्रों से शायद सफलता मिल जाए। जब समाचार-पत्रों से कुछ पता न चला, तब विवश होकर कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं के अनाथालय में रख दिया। महाशय यशोदानन्दन ही उस अनाथालय के मैनेजर थे।
कितने आदमी कुचले गए, कितने डूब गए, कितने खो गए, कितने अपंग हो गए, इसका अनुमान करना कठिन है। धर्म का विकट संग्राम था। एक तो सूर्य-ग्रहण, उस पर यह असाधारण अद्भुत प्राकृतिक छटा ! सारा दृश्य धार्मिक वृत्तियों को जगानेवाला था। दोपहर को तारों का प्रकाश माया के परदे को फाड़कर आत्मा को आलोकित करता हुआ मालूम होता था। वैज्ञानिकों की बात जाने दीजिए, पर जनता में न जाने कितने दिनों से वह विश्वास फैला हुआ था कि तारागण दिन को कहीं किसी सागर में डूब जाते हैं। आज वही तारागण आँखों के सामने चमक रहे थे, फिर भक्ति क्यों न जाग उठे ! सद्वृत्तियाँ क्यों न आँखें खोल दें !
घण्टे भर के बाद फिर प्रकाश होने लगा, तारागण फिर अदृश्य हो गए, सूर्य भगवान की समाधि टूटने लगी।
यात्रीगण अपने-अपने पापों की गठरियाँ त्रिवेणी में डालकर जाने लगे। संध्या होते-होते घाट पर सन्नाटा छा गया। हाँ, कुछ घायल, कुछ अधमरे प्राणी जहाँ-तहाँ पड़े कराह रहे थे और ऊँचे कगार से कुछ दूर पर एक नाली में पड़ी तीन-चार साल की एक लड़की चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थी।
सेवा समितियों के युवक, जो अब तक भीड़ सँभालने का विफल प्रयत्न कर रहे थे, अब डोलियाँ कंधों पर ले-लेकर घायलों और भूले भटकों की खबर लेने आ पहुँचे। सेवा और दया का कितना अनुपम दृश्य था।
सहसा एक युवक के कानों में उस बालिका के रोने की आवाज पड़ी। अपने साथी से बोला—यशोदा, उधर कोई लड़का रो रहा है।
यशोदा-हाँ, मालूम तो होता है। इन मूर्खों को कोई कैसे समझाए कि यहाँ बच्चों को लाने का काम नहीं। चलो, देखें।
दोनों ने उधर जाकर देखा, तो एक बालिका नाली में पड़ी रो रही है। गोरा रंग था, भरा हुआ शरीर, बड़ी-बड़ी आँखें, गोरा मुखड़ा, सिर से पाँव तक गहनों से लदी हुई। किसी अच्छे घर की लड़की थी। रोते-रोते उसकी आँखें लाल हो गयी थीं। इन दोनों युवकों को देखकर डरी और चिल्लाकर रो पड़ी। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोला—बेटी, रो मत, हम तुझे तेरी अम्मा के घर पहुँचा देंगे। तुझी को खोज रहे थे। तेरे बाप का क्या नाम है ?
लड़की चुप तो हो गई, पर संशय की दृष्टि से देख-देख सिसक रही थी। इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सकी।
यशोदा ने फिर चुमकारकर पूछा—बेटी, तेरा घर कहाँ है ?
लड़की ने कोई जवाब न दिया।
यशोदा : अब बताओ महमूद, क्या करें ?
महमूद एक अमीर मुसलमान का लड़का था। यशोदानन्दन से उसकी बड़ी दोस्ती थी। उसके साथ वह भी सेवासमिति में दाखिल हो गया था। बोला—क्या बताऊँ ? कैंप में ले चलो, शायद कुछ पता चले।
यशोदा : अभागे ज़रा-ज़रा से बच्चों को लाते हैं और इतना भी नहीं करते कि उन्हें अपना नाम और पता तो याद करा दें।
महमूद : क्यों बिटिया, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है ?
लड़की ने धीरेसे कहा—बाबूजी !
महमूद—तुम्हारा घर इसी शहर में है या कहीं और ?
लड़की—मैं तो बाबूजी के साथ लेल पर आयी थी !
महमूद—तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं ?
लड़की—कुछ नहीं कलते।
यशोदा : इस वक़्त अगर इसका बाप मिल जाए तो सच कहता हूँ, बिना मारे न छोड़ूँ। बच्चू गहने पहनाकर लाये थे, जाने कोई तमाशा देखने आये हों !
महमूद—और मेरा जी चाहता है कि तुम्हें पीटूँ। मियाँ-बीवी यहाँ आये तो बच्चे को किस पर छोड़ आते। घर में और कोई न हो तो ?
यशोदा : तो फिर उन्हीं को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी ?
महमूद : तुम ‘एथीइस्ट’ (नास्तिक) हो; तुम क्या जानो की सच्चा मज़हबी जोश किसे कहते हैं ?
यशोदा : ऐसे मज़हबी जोश को दूर से ही सलाम करता हूँ। इस वक़्त दोनों मियाँ-बीवी हाय-हाय कर रहे होंगे।
महमूद—कौन जाने, वे भी यहीं कुचल-कुचला गए हों।
लड़की ने साहस कर कहा—तुम हमें घल पहुँचा दोगे ? बाबूजी तुमको पैछा देंगे !
यशोदा : अच्छा बेटी, चलो, तुम्हारे बाबूजी को खोजें।
दोनों मित्र बालिका को लिए हुए कैंप में आये, यहाँ पर कुछ पता न चला। तब दोनों उस तरफ गये, जहाँ मैदान में बहुत से यात्री पड़े हुए थे। महमूद ने बालिका को कन्धे पर बैठा लिया और यशोदानन्दन चारों तरफ़ चिल्लाते फिरे—यह किसकी लड़की है ? किसी की लड़की तो नहीं खो गई ? यह आवाज़ें सुनकर कितने ही यात्री, हाँ-हाँ, कहाँ-कहाँ, करके दौड़े; पर लड़की को देखकर निराश लौट गए।
चिराग़ जले तक दोनों मित्र घूमते रहे। नीचे-ऊपर, क़िले के आस-पास, रेल के स्टेशन पर, अलोपी देवी के मन्दिर की तरफ यात्री-ही-यात्री पड़े हुए थे; पर बालिका के माता-पिता का कहीं पता न चला। आखिर निराश होकर दोनों आदमी कैंप लौट आये।
दूसरे दिन समिति के और कई सेवकों ने फिर पता लगाना शुरू किया। दिन-भर दौड़े, सारा प्रयाग छान मारा, सभी धर्मशालाओं की ख़ाक छानी; पर कहीं पता न चला।
तीसरे दिन समाचार-पत्रों में नोटिस दिया गया और दो दिन वहाँ और रहकर समिति आगरे लौट गयी। लड़की को भी अपने साथ लेती गयी। उसे आशा थी कि समाचार-पत्रों से शायद सफलता मिल जाए। जब समाचार-पत्रों से कुछ पता न चला, तब विवश होकर कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं के अनाथालय में रख दिया। महाशय यशोदानन्दन ही उस अनाथालय के मैनेजर थे।
2
बनारस में महात्मा कबीर के चौरे के निकट मुंशी वज्रधरसिंह का मकान है। आप हैं तो राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते हैं और कहते हैं। ‘मुंशी’ की उपाधि से आपको बहुत प्रेम है। ‘ठाकुर’ के साथ आपको गँवारपन का बोध होता है, इसलिए हम भी आपको मुंशीजी कहेंगे। आप कई साल से सरकारी पेंशन पाते हैं। बहुत छोटे पद से तरक्की करते-करते आपने अन्त में तहसीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान् पद पर तीन मास से अधिक न रहे और उतने दिन भी केवल एवज़ पर रहे; पर आप अपने को ‘साबिक तहसीलदार’ लिखते थे और मुहल्लेवाले भी उन्हें खुश करने को ‘तहसीलदार साहब’ ही कहते थे। यह नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रु। मिलती थी, इसलिए तहसीलदार साहब को बाज़ार-हाट खुद ही करनी पड़ती थीं। घर में चार प्राणियों का खर्च था। एक लड़की थी, एक लड़का और स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतनी ज़हीन था कि अपने पिता के पेंशन के जमाने में जब घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी, केवल अपने बुद्धि-बल से उसने एम.ए. की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशीजी ने पहले से ही सिफ़ारिश पहुँचानी शुरू की थी। दरबारी की कला में वह निपुण थे। हुक्काम को सलाम करने का उन्हें मरज़ था। हाकिमों के दिये हुए सैकडों प्रशंसा-पत्र उनकी अतुलनीय सम्पत्ति थे। उन्हें वह बड़े गर्व से दूसरों को दिखाया करते थे। कोई नया हाकिम आये, उससे ज़रूर, रब्त-ज़ब्त कर लेते थे। हुक्काम ने चक्रधर का खयाल करने के वादे भी किये थे; लेकिन जब परीक्षा का नतीज़ा निकला और मुंशीजी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा, तो उन्होंने जाने से साफ़ इनकार किया !
मुंशीजी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा—क्यों ? क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ?
चक्रधर—मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है।
वज्रधर—वह ख़ब्त तुम्हें कब से सवार हुआ ? नौकरी के सिवा और करोगे ही क्या ?
चक्रधर—मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ।
वज्रधर—आज़ाद रहना था तो एम.ए. क्यों किया ?
चक्रधर—इसलिए कि आज़ादी का महत्व समझूँ।
उस दिन से पिता और पुत्र में आये दिन बमचख
मचती रहती थी। मुंशीजी बुढ़ापे में भी शौक़ीन आदमी थे। अच्छा खाने और अच्छा पहनने की इच्छा अभी तक बनी हुई थी। अब तक इसी ख़याल से दिल को समझाते थे कि लड़का नौकर हो जाएगा तो मौज़ करेंगे। अब लड़के का रंग देखकर बार-बार झुँझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते थे—अभी तुम्हें कुछ नहीं सूझती, जब मैं मर जाऊँगा तब सूझेगी। तब सिर पर हाथ रख कर रोओगे। लाख बार कह दिया—बेटा, यह ज़माना खुशामद औऱ सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई सेंत भी न पूछेगा। तुम बैठे आज़ादी का मज़ा उठा रहे हो और तुम्हारे पीछे वाले बाज़ी मारे जाते हैं। वह ज़माना लद गया, जब विद्वानों की क़द्र थी। अब तो विद्वान टके सेर मिलते हैं, कोई बात नहीं पूछता। जैसे और चीजें बनाने के कारखाने खुल गए हैं, उसी तरह विद्वानों के कारखाने भी हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है।
चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब तो न देते; पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जो मार्ग तय कर लिया था, उससे वह न हटते थे। उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। अगर पेट पालना ही जीवन का आदर्श हो, तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। मज़दूर एक अक्षर भी नहीं जानता, फिर भी वह अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट बड़े मजे से पाल लेता है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊँचा न हुआ, तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या को साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखों मर जाते; लेकिन नौकरी के लिए आवेदन-पत्र लेकर कहीं न जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वह सेवाकार्य में अग्रसर रहा करते थे और अब तो इसके सिवा उन्हें और कुछ सूझता ही न था। दोनों की सेवा और सहायता में जो आनन्द और आत्मगौरव था, वह दफ़्तर में बैठकर कलम घिसने में कहाँ ?
इस प्रकार दो साल गुज़र गए। मुंशी वज्रधर ने समझा था, जब यह भूत इसके सिर से उतर जाएगा, शादी-ब्याह की फिक्र होगी, तो आप-ही-आप नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। जवानी का नशा बहुत दिनों तक नहीं ठहरता। लेकिन जब दो साल गुज़र जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण न दिखाई दिया, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा—दुनिया का दस्तूर है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। तुम अपने घर को अँधेरा रखकर मस्जिद को रोशन करना चाहते हो। जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों की किस मुँह से मदद करेगा ! मैं बुढ़ापे में खाने-कपड़े को तरसूँ और तुम दूसरों का कल्याण करते फिरो। मैंने तुम्हें पैदा किया, दूसरों ने नहीं; मैंने तुम्हें पाला-पोसा दूसरों ने नहीं; मैं गोद में लेकर हकीम-वैद्यों के द्वार-द्वार दौडता-फिरा, दूसरे नहीं। तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ मेरा है, दूसरों का नहीं।
चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुँह न मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज ही में कोई जगह मिल सकती थी। वहाँ सभी उनका आदर करते थे; लेकिन यह उन्हें मंजूर न था। वह कोई ऐसा धन्धा चाहते थे, जिससे थोड़ी देर रोज़ काम करके अपने पिता की मदद कर सकें। एक घण्टे से अधिक समय नहीं देना चाहते थे। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरिसेवकसिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए सुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापक की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। 30 रु. मासिक तक वेतन रक्खा। कॉलेज का कोई भी अध्यापक इतने वेतन पर राज़ी न हुआ। आखिर उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी ज़िम्मेदारी का था; किन्तु चक्रधर इतने सुशील, इतने गम्भीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको विश्वास था।
दूसरे दिन से चक्रधर ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया।
मुंशीजी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा—क्यों ? क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ?
चक्रधर—मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है।
वज्रधर—वह ख़ब्त तुम्हें कब से सवार हुआ ? नौकरी के सिवा और करोगे ही क्या ?
चक्रधर—मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ।
वज्रधर—आज़ाद रहना था तो एम.ए. क्यों किया ?
चक्रधर—इसलिए कि आज़ादी का महत्व समझूँ।
उस दिन से पिता और पुत्र में आये दिन बमचख
मचती रहती थी। मुंशीजी बुढ़ापे में भी शौक़ीन आदमी थे। अच्छा खाने और अच्छा पहनने की इच्छा अभी तक बनी हुई थी। अब तक इसी ख़याल से दिल को समझाते थे कि लड़का नौकर हो जाएगा तो मौज़ करेंगे। अब लड़के का रंग देखकर बार-बार झुँझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते थे—अभी तुम्हें कुछ नहीं सूझती, जब मैं मर जाऊँगा तब सूझेगी। तब सिर पर हाथ रख कर रोओगे। लाख बार कह दिया—बेटा, यह ज़माना खुशामद औऱ सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई सेंत भी न पूछेगा। तुम बैठे आज़ादी का मज़ा उठा रहे हो और तुम्हारे पीछे वाले बाज़ी मारे जाते हैं। वह ज़माना लद गया, जब विद्वानों की क़द्र थी। अब तो विद्वान टके सेर मिलते हैं, कोई बात नहीं पूछता। जैसे और चीजें बनाने के कारखाने खुल गए हैं, उसी तरह विद्वानों के कारखाने भी हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है।
चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब तो न देते; पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जो मार्ग तय कर लिया था, उससे वह न हटते थे। उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। अगर पेट पालना ही जीवन का आदर्श हो, तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। मज़दूर एक अक्षर भी नहीं जानता, फिर भी वह अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट बड़े मजे से पाल लेता है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊँचा न हुआ, तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या को साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखों मर जाते; लेकिन नौकरी के लिए आवेदन-पत्र लेकर कहीं न जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वह सेवाकार्य में अग्रसर रहा करते थे और अब तो इसके सिवा उन्हें और कुछ सूझता ही न था। दोनों की सेवा और सहायता में जो आनन्द और आत्मगौरव था, वह दफ़्तर में बैठकर कलम घिसने में कहाँ ?
इस प्रकार दो साल गुज़र गए। मुंशी वज्रधर ने समझा था, जब यह भूत इसके सिर से उतर जाएगा, शादी-ब्याह की फिक्र होगी, तो आप-ही-आप नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। जवानी का नशा बहुत दिनों तक नहीं ठहरता। लेकिन जब दो साल गुज़र जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण न दिखाई दिया, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा—दुनिया का दस्तूर है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। तुम अपने घर को अँधेरा रखकर मस्जिद को रोशन करना चाहते हो। जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों की किस मुँह से मदद करेगा ! मैं बुढ़ापे में खाने-कपड़े को तरसूँ और तुम दूसरों का कल्याण करते फिरो। मैंने तुम्हें पैदा किया, दूसरों ने नहीं; मैंने तुम्हें पाला-पोसा दूसरों ने नहीं; मैं गोद में लेकर हकीम-वैद्यों के द्वार-द्वार दौडता-फिरा, दूसरे नहीं। तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ मेरा है, दूसरों का नहीं।
चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुँह न मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज ही में कोई जगह मिल सकती थी। वहाँ सभी उनका आदर करते थे; लेकिन यह उन्हें मंजूर न था। वह कोई ऐसा धन्धा चाहते थे, जिससे थोड़ी देर रोज़ काम करके अपने पिता की मदद कर सकें। एक घण्टे से अधिक समय नहीं देना चाहते थे। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरिसेवकसिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए सुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापक की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। 30 रु. मासिक तक वेतन रक्खा। कॉलेज का कोई भी अध्यापक इतने वेतन पर राज़ी न हुआ। आखिर उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी ज़िम्मेदारी का था; किन्तु चक्रधर इतने सुशील, इतने गम्भीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको विश्वास था।
दूसरे दिन से चक्रधर ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया।
3
कई महीने बीत गए। चक्रधर महीने के अन्त में रुपये लाते और माता के हाथ पर रख देते। अपने लिए उन्हें रुपये की कोई ज़रूरत न थी। दो मोटे कुरतों पर साल काट देते थे। हाँ, पुस्तकों से उन्हें रुचि न थी; पर इसके लिए कॉलेज का पुस्तकालय खुला हुआ था, सेवा-कार्य के लिए चन्दों से रुपये आ जाते थे। मुंशी वज्रधर का मुँह भी कुछ सीधा हो गया। डरे की इससे ज़्यादा दबाऊँ तो शायद यह भी हाथ से जाय। समझ गए कि जब तक विवाह की बेड़ी पाँव में न पड़ेगी, यह महाशय काबू में न आएँगे। वह बेड़ी बनवाने का विचार करने लगे।
मनोरमा की उम्र अभी तेरह वर्ष से अधिक न थी; लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए झेंप होती थी। वह यही प्रयत्न करते थे कि ठाकुर साहब की उपस्थिति में ही उसे पढ़ाएँ। यदि कभी ठाकुर साहब कहीं चले जाते, तो चक्रधर को महान संकट का सामना करना पड़ता था।
एक दिन चक्रधर इसी संकट में जा फँसे। ठाकुर साहब कहीं गए हुए थे। चक्रधर कुर्सी पर बैठे; पर मनोरमा की ओर न ताककर द्वार की ओर ताक रहे थे, मानो वहाँ बैठते डरते हों। मनोरमा वाल्मीकीय रामायण पढ़ रही थी। उसने दो-तीन बार चक्रधर की ओर ताका, पर उन्हें द्वार की ओर ताकते देखकर फिर किताब देखने लगी। उसके मन में सीता वनवास पर एक शंका हुई थी और वह इसका समाधान करना चाहती थी। चक्रधर ने द्वार की ओर ताकते हुए पूछा—चुप क्यों बैठी हो, आज का पाठ क्यों नहीं पढ़तीं ?
मनोरमा—मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, आज्ञा हो तो पूछूँ ?
चक्रधर ने कातर भाव से कहा—क्या बात है ?
मनोरमा—रामचन्द्र ने सीताजी को घर से निकाला, तो वह चली क्यों गयीं ?
चक्रधर—और क्या करतीं ?
मनोरमा—वह जाने से इनकार कर सकती थीं। एक तो राज्य पर उनका अधिकार भी रामचन्द्र ही के समान था, दूसरे वह निर्दोष थीं। अगर वह यह अन्याय न स्वीकार करतीं, तो क्या उन पर कोई आपत्ति हो सकती थी ?
चक्रधर—हमारे यहाँ पुरुषों की आज्ञा मानना स्त्रियों का परम धर्म माना गया है। यदि सीताजी पति की आज्ञा न मानतीं, तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जातीं।
मनोरमा—यह तो मैं जानती हूँ कि स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन क्या सभी दशाओं में ? जब राजा से साधारण प्रजा न्याय का दावा कर सकती है, तो क्या उसकी स्त्री नहीं कर सकती ? जब रामचन्द्र ने सीता की परीक्षा ले ली थी और अन्तःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निन्दा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना कहाँ का न्याय था ?
चक्रधर—राजधर्म का आदर्श पालन करना था।
मनोरमा—तो क्या दोनों प्राणी जानते थे कि इस संसार के लिए आदर्श खड़ा कर रहे हैं ? इससे तो यह सिद्ध होता है कि वे कोई अभिनय कर रहे थे। अगर आदर्श भी मान लें, तो यह ऐसा आदर्श है, जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। यह आदर्श नहीं है, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचन्द्र की जगह होते, तो क्या आप भी सीता को घर से निकाल देते ?
चक्रधर बड़े असमंजस में पड़ गए। उनके मन में स्वयं ही यही शंका और लगभग इसी उम्र में हुई थी; पर वह इसका समाधान न कर सके थे। अब साफ़-साफ़ जवाब देने की ज़रूरत पड़ी, तो बगलें झाँकने लगे।
मनोरमा ने उन्हें चुप देखकर फिर पूछा—क्या आप भी उन्हें घर से निकाल देते ?
चक्रधर—नहीं, मैं तो शायद न निकालता।
मनोरमा—आप निन्दा की ज़रा भी परवाह न करते ?
चक्रधर—नहीं, मैं झूठी निन्दा की परवाह न करता।
मनोरमा की आँखें खुशी से चमक उठीं, प्रफुल्लित होकर बोली—यही बात मेरे भी मन में थी। मैं दादाजी से, भाईजी से, पण्डितजी से, लौंगी अम्मा से, भाभी से, यही शंका की, पर सब लोग यही कहते थे कि रामचन्द्र तो भगवान् हैं, उनके विषय में कोई शंका हो ही नहीं सकती। आपने आज मेरे मन की बात कही। मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। अब मैं उन लोगों को खूब आडे़ हाथों लूँगी।
उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया। पढ़ने-लिखने से उसे विशेष रुचि हो गई। चक्रधर उसे जो काम करने को दे जाते, वह उसे अवश्य पूरा करती। पहले की भाँति अब हीले-हवाले न करती। जब उनके आने का समय होता, तो पहले से ही आकर बैठ जाती और उनका इन्तज़ार करती। अब उसे उनसे अपने मन के भाव प्रकट करते हुए संकोच न होता। वह जानती थी कि कम-से-कम यहाँ उनका निरादर न होगा, उसकी हँसी न उड़ाई जाएगी।
ठाकुर हरिसेवक सिंह की आदत थी कि पहले दो-चार महीने तक तो नौकरों को वेतन ठीक समय पर दे देते; पर ज्यों-ज्यों नौकर पुराना होता जाता था, उन्हें उसके वेतन की याद भूलती जाती थी। उनके यहाँ कई नौकर ऐसे भी पड़े थे, जिन्होंने वर्षों से अपने वेतन नहीं पाए थे, न चक्रधर संकोचवश माँगते थे। उधर घर में रोज़ तकरार होती थी। मुंशी वज्रधर बार-बार तकाजे करते, झुंझलाते-माँगते क्यों नहीं ? क्या मुँह में दही जमा हुआ है, या काम नहीं करते ? लिहाज़ भले आदमी का किया जाता है। ऐसे लुच्चों का लिहाज़ नहीं किया जाता जो मुफ़्त में काम कराना चाहते हैं।
आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब को एक पुरचा लिखकर अपना वेतन माँगा। ठाकुर साहब ने पुरचा लौटा दिया—व्यर्थ की लिखा-पढ़ी की उन्हें फुरसत न थी और कहा—उनको जो कुछ कहना हो, खुद आकर कहें। चक्रधर शरमाते हुए गये और कुछ शिष्टाचार के बाद रुपये माँगे। चार महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी न माँगा। अब तो आपके पूरे 120 रु. हो गए। मेरा हाथ इस वक़्त तंग है। ज़रा दस-पाँच दिन ठहरिए। आपको महीने-महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए, मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी ! खैर, जाइए, दस-पाँच दिन में रुपये मिल जाएँगे।
चक्रधर कुछ कह न सके। लौटे, तो मुँह पर घोर निराशा छाई हुई थी। आज दादाजी शायद जीता न छोड़ेंगे—इस ख़याल से उनका दिल काँपने लगा। मनोरमा ने उनका पुरजा अपने पिता के पास ले जाते हुए पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा—दादाजी ने आपसे क्या कहा ?
चक्रधर उसके सामने रुपये-पैसे का ज़िक्र न करना चाहते थे। झेंपते हुए बोले—कुछ तो नहीं।
मनोरमा—आपको रुपये नहीं दिये ?
चक्रधर का मुँह लाल हो गया—मिल जाएँगे।
मनोरमा—आपको 120 रु. चाहिए ना ?
चक्रधर—इस वक़्त कोई ज़रूरत नहीं है।
मनोरमा—ज़रूरत न होती तो आप माँगते ही नहीं। दादाजी में बड़ा ऐब है कि किसी के रुपये देते हुए मोह लगता है। देखिए, मैं जाकर..
चक्रधर ने रोककर कहा—नहीं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं।
मनोरमा नहीं मानी। तुरन्त घर में गयी और एक क्षण में पूरे रुपये लाकर मेज़ पर रख दिये, मानो कहीं गिना-गिनाये रखे हुए थे।
चक्रधर—तुमने ठाकुर साहब को व्यर्थ कष्ट दिया।
मनोरमा—मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया ! उनसे तो कहा भी नहीं। दादाजी किसी की ज़रूरत नहीं समझते। अगर अपने लिए कभी मोटर मँगवानी हो, तो तुरन्त मँगवा लेंगे; पहाडों पर जाना हो, तो तुरन्त चले जाएँगे, पर जिसके रुपये होते हैं, उसको न देंगे।
वह तो पढ़ने लग गई; लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या आ पड़ी कि रुपये लूँ या न लूँ। उन्होंने निश्चय किया कि न लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वह उठ खड़े हुए और बिना रुपये लिए बाहर निकल आये। मनोरमा रुपये लिए पीछे-पीछे बरमादे तक आयी। बार-बार कहती रहीं—इन्हें आप लेते जाइए।
जब दादाजी दें तो मुझे लौटा दीजिएगा। पर चक्रधर ने एक न सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए।
मनोरमा की उम्र अभी तेरह वर्ष से अधिक न थी; लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए झेंप होती थी। वह यही प्रयत्न करते थे कि ठाकुर साहब की उपस्थिति में ही उसे पढ़ाएँ। यदि कभी ठाकुर साहब कहीं चले जाते, तो चक्रधर को महान संकट का सामना करना पड़ता था।
एक दिन चक्रधर इसी संकट में जा फँसे। ठाकुर साहब कहीं गए हुए थे। चक्रधर कुर्सी पर बैठे; पर मनोरमा की ओर न ताककर द्वार की ओर ताक रहे थे, मानो वहाँ बैठते डरते हों। मनोरमा वाल्मीकीय रामायण पढ़ रही थी। उसने दो-तीन बार चक्रधर की ओर ताका, पर उन्हें द्वार की ओर ताकते देखकर फिर किताब देखने लगी। उसके मन में सीता वनवास पर एक शंका हुई थी और वह इसका समाधान करना चाहती थी। चक्रधर ने द्वार की ओर ताकते हुए पूछा—चुप क्यों बैठी हो, आज का पाठ क्यों नहीं पढ़तीं ?
मनोरमा—मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, आज्ञा हो तो पूछूँ ?
चक्रधर ने कातर भाव से कहा—क्या बात है ?
मनोरमा—रामचन्द्र ने सीताजी को घर से निकाला, तो वह चली क्यों गयीं ?
चक्रधर—और क्या करतीं ?
मनोरमा—वह जाने से इनकार कर सकती थीं। एक तो राज्य पर उनका अधिकार भी रामचन्द्र ही के समान था, दूसरे वह निर्दोष थीं। अगर वह यह अन्याय न स्वीकार करतीं, तो क्या उन पर कोई आपत्ति हो सकती थी ?
चक्रधर—हमारे यहाँ पुरुषों की आज्ञा मानना स्त्रियों का परम धर्म माना गया है। यदि सीताजी पति की आज्ञा न मानतीं, तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जातीं।
मनोरमा—यह तो मैं जानती हूँ कि स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन क्या सभी दशाओं में ? जब राजा से साधारण प्रजा न्याय का दावा कर सकती है, तो क्या उसकी स्त्री नहीं कर सकती ? जब रामचन्द्र ने सीता की परीक्षा ले ली थी और अन्तःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निन्दा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना कहाँ का न्याय था ?
चक्रधर—राजधर्म का आदर्श पालन करना था।
मनोरमा—तो क्या दोनों प्राणी जानते थे कि इस संसार के लिए आदर्श खड़ा कर रहे हैं ? इससे तो यह सिद्ध होता है कि वे कोई अभिनय कर रहे थे। अगर आदर्श भी मान लें, तो यह ऐसा आदर्श है, जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। यह आदर्श नहीं है, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचन्द्र की जगह होते, तो क्या आप भी सीता को घर से निकाल देते ?
चक्रधर बड़े असमंजस में पड़ गए। उनके मन में स्वयं ही यही शंका और लगभग इसी उम्र में हुई थी; पर वह इसका समाधान न कर सके थे। अब साफ़-साफ़ जवाब देने की ज़रूरत पड़ी, तो बगलें झाँकने लगे।
मनोरमा ने उन्हें चुप देखकर फिर पूछा—क्या आप भी उन्हें घर से निकाल देते ?
चक्रधर—नहीं, मैं तो शायद न निकालता।
मनोरमा—आप निन्दा की ज़रा भी परवाह न करते ?
चक्रधर—नहीं, मैं झूठी निन्दा की परवाह न करता।
मनोरमा की आँखें खुशी से चमक उठीं, प्रफुल्लित होकर बोली—यही बात मेरे भी मन में थी। मैं दादाजी से, भाईजी से, पण्डितजी से, लौंगी अम्मा से, भाभी से, यही शंका की, पर सब लोग यही कहते थे कि रामचन्द्र तो भगवान् हैं, उनके विषय में कोई शंका हो ही नहीं सकती। आपने आज मेरे मन की बात कही। मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। अब मैं उन लोगों को खूब आडे़ हाथों लूँगी।
उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया। पढ़ने-लिखने से उसे विशेष रुचि हो गई। चक्रधर उसे जो काम करने को दे जाते, वह उसे अवश्य पूरा करती। पहले की भाँति अब हीले-हवाले न करती। जब उनके आने का समय होता, तो पहले से ही आकर बैठ जाती और उनका इन्तज़ार करती। अब उसे उनसे अपने मन के भाव प्रकट करते हुए संकोच न होता। वह जानती थी कि कम-से-कम यहाँ उनका निरादर न होगा, उसकी हँसी न उड़ाई जाएगी।
ठाकुर हरिसेवक सिंह की आदत थी कि पहले दो-चार महीने तक तो नौकरों को वेतन ठीक समय पर दे देते; पर ज्यों-ज्यों नौकर पुराना होता जाता था, उन्हें उसके वेतन की याद भूलती जाती थी। उनके यहाँ कई नौकर ऐसे भी पड़े थे, जिन्होंने वर्षों से अपने वेतन नहीं पाए थे, न चक्रधर संकोचवश माँगते थे। उधर घर में रोज़ तकरार होती थी। मुंशी वज्रधर बार-बार तकाजे करते, झुंझलाते-माँगते क्यों नहीं ? क्या मुँह में दही जमा हुआ है, या काम नहीं करते ? लिहाज़ भले आदमी का किया जाता है। ऐसे लुच्चों का लिहाज़ नहीं किया जाता जो मुफ़्त में काम कराना चाहते हैं।
आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब को एक पुरचा लिखकर अपना वेतन माँगा। ठाकुर साहब ने पुरचा लौटा दिया—व्यर्थ की लिखा-पढ़ी की उन्हें फुरसत न थी और कहा—उनको जो कुछ कहना हो, खुद आकर कहें। चक्रधर शरमाते हुए गये और कुछ शिष्टाचार के बाद रुपये माँगे। चार महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी न माँगा। अब तो आपके पूरे 120 रु. हो गए। मेरा हाथ इस वक़्त तंग है। ज़रा दस-पाँच दिन ठहरिए। आपको महीने-महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए, मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी ! खैर, जाइए, दस-पाँच दिन में रुपये मिल जाएँगे।
चक्रधर कुछ कह न सके। लौटे, तो मुँह पर घोर निराशा छाई हुई थी। आज दादाजी शायद जीता न छोड़ेंगे—इस ख़याल से उनका दिल काँपने लगा। मनोरमा ने उनका पुरजा अपने पिता के पास ले जाते हुए पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा—दादाजी ने आपसे क्या कहा ?
चक्रधर उसके सामने रुपये-पैसे का ज़िक्र न करना चाहते थे। झेंपते हुए बोले—कुछ तो नहीं।
मनोरमा—आपको रुपये नहीं दिये ?
चक्रधर का मुँह लाल हो गया—मिल जाएँगे।
मनोरमा—आपको 120 रु. चाहिए ना ?
चक्रधर—इस वक़्त कोई ज़रूरत नहीं है।
मनोरमा—ज़रूरत न होती तो आप माँगते ही नहीं। दादाजी में बड़ा ऐब है कि किसी के रुपये देते हुए मोह लगता है। देखिए, मैं जाकर..
चक्रधर ने रोककर कहा—नहीं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं।
मनोरमा नहीं मानी। तुरन्त घर में गयी और एक क्षण में पूरे रुपये लाकर मेज़ पर रख दिये, मानो कहीं गिना-गिनाये रखे हुए थे।
चक्रधर—तुमने ठाकुर साहब को व्यर्थ कष्ट दिया।
मनोरमा—मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया ! उनसे तो कहा भी नहीं। दादाजी किसी की ज़रूरत नहीं समझते। अगर अपने लिए कभी मोटर मँगवानी हो, तो तुरन्त मँगवा लेंगे; पहाडों पर जाना हो, तो तुरन्त चले जाएँगे, पर जिसके रुपये होते हैं, उसको न देंगे।
वह तो पढ़ने लग गई; लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या आ पड़ी कि रुपये लूँ या न लूँ। उन्होंने निश्चय किया कि न लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वह उठ खड़े हुए और बिना रुपये लिए बाहर निकल आये। मनोरमा रुपये लिए पीछे-पीछे बरमादे तक आयी। बार-बार कहती रहीं—इन्हें आप लेते जाइए।
जब दादाजी दें तो मुझे लौटा दीजिएगा। पर चक्रधर ने एक न सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book