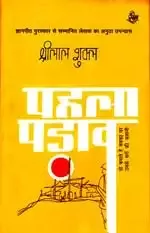|
विविध उपन्यास >> पहला पड़ाव पहला पड़ावश्रीलाल शुक्ल
|
122 पाठक हैं |
||||||
इस उपन्यास में बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में ईट-पत्थर होते जा रहे आदमी की त्रासदी की कथा वर्णन किया है...
Pahala Padav
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
राग दरबारी-जैसे कालजयी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल हिन्दी के वरिष्ठ और विशिष्टि कथाकार हैं। उनकी कलम जिस निस्संग व्यंग्यात्मकता से समकालीन सामाजिक यथार्थ को परत-दर-परत उघाड़ती रही है, पहला-पड़ाव उसे और आर्थिक ऊँचाई सौंपता है।
श्रीलाल शुक्ल ने अपने इस नए उपन्यास को राज-मजदूरों, मिस्त्रियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और शिक्षित बेरोज़गारों के जीवन पर केन्द्रित किया है और उन्हें एक सूत्र में पिरोये रखने के लिए एक दिलचस्प कथाफलक की रचना की है। संतोषकुमार उर्फ सत्ते परामात्मा जी की बनती हुई चौथी बिल्डिंग की मुंशीगीरी करते हुए न सिर्फ-अपनी डेली-पैसिंजरी, एक औसत गाँव-देहात और ‘चल-चल रे नौजवान’ टाइप ऊँचे संबोधनों की शिकार बेरोज़गार जिन्दगी की बखिया उधेड़ता है, बल्कि वही हमें जसोदा उर्फ ‘मेमसाहब’-जैसे जीवंत नारी चरित्र से भी परिचित कराता है। इसके अलावा उपन्यास के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों को लेखक ने अपनी गहरी सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक सहजता प्रदान की है और उनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक अंतर्विरोधों, उन्हें प्रभावित-परिचालित करती हुई शक्तियों और मनुष्य-स्वभाव की दुर्बलताओं को अत्यंत कलात्मकता से उजागर किया है।
वस्तुतः श्रीलाल शुक्ल की यह कथाकृति बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में ईंट-पत्थर होते जा रहे आदमी की त्रासदी को अत्यन्त मानवीय और यथार्थवादी फलक पर उकेरती है।
श्रीलाल शुक्ल ने अपने इस नए उपन्यास को राज-मजदूरों, मिस्त्रियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और शिक्षित बेरोज़गारों के जीवन पर केन्द्रित किया है और उन्हें एक सूत्र में पिरोये रखने के लिए एक दिलचस्प कथाफलक की रचना की है। संतोषकुमार उर्फ सत्ते परामात्मा जी की बनती हुई चौथी बिल्डिंग की मुंशीगीरी करते हुए न सिर्फ-अपनी डेली-पैसिंजरी, एक औसत गाँव-देहात और ‘चल-चल रे नौजवान’ टाइप ऊँचे संबोधनों की शिकार बेरोज़गार जिन्दगी की बखिया उधेड़ता है, बल्कि वही हमें जसोदा उर्फ ‘मेमसाहब’-जैसे जीवंत नारी चरित्र से भी परिचित कराता है। इसके अलावा उपन्यास के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों को लेखक ने अपनी गहरी सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक सहजता प्रदान की है और उनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक अंतर्विरोधों, उन्हें प्रभावित-परिचालित करती हुई शक्तियों और मनुष्य-स्वभाव की दुर्बलताओं को अत्यंत कलात्मकता से उजागर किया है।
वस्तुतः श्रीलाल शुक्ल की यह कथाकृति बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में ईंट-पत्थर होते जा रहे आदमी की त्रासदी को अत्यन्त मानवीय और यथार्थवादी फलक पर उकेरती है।
1
चैत की अमावस के पहले से ही मेडूराम उर्फ़ नेता का मन कसमसाने लगा था। उनकी मेमसाहब भी अभी-अभी दीवार से अपनी घनुष-जैसी तनी पीठ टिकाकर एक गीत गुनगुनातीं। उनके बोल हमारी समझ में न आते लेकिन उतना हम समझ लेते कि उन्हें भी अपने गाँव की याद सता रही है। ऐसा कई दिन से हो रहा था। काम के वक्त भी मेमसाहब इधर-उधर कुछ उखड़ी-उखड़ी रहतीं थीं। खोपड़ी पर सीमेंट की फटी बोरी की एक एँडर रक्खे, उस पर छह मंजिलों में सजी ग्यारह ईंटें लिए जब वे मिस्त्री के पास पहुँचती तो उन्हें अब पहलेवाली फुर्ती से न फेंकतीं; वे पहले नेता को धिक्कारतीं। धिक्कार के बोल थेः जोत-जवारे के दिनों में भी गाँव न चलेगा ? यहाँ रहेगा तो बचा खुचा है उसे भी जुए में फूँक देगा। मिस्त्री, जो रोज शाम नेता के साथ जुआ खेलने थे, बड़ी समझदारी से कहतेः जुए का काम बड़ा कच्चा है। इधर, चिकने लहरिया बालोंवाले साँवले चेहरे में ऊबड़-खाबड़ दाँतों की मटमैली छटा दिखाते हुए नेता मुझे सुनाकर जवाब देतेः मुंसी जाने दे तब न।
मुंसी मैं ही था। सुनकर हाकिमाना अंदाज से मैं दूसरी ओर किसी मजदूर को सुस्ती छोड़कर चुस्ती दिखाने के लिए आवाज़ देता। पर मैं जानता था कि बिलासपुरी मज़दूर का जी उखड़ जाए तो उसे बिलासपुर से लेकर दिल्ली तक की कोई भी ताकत तब तक नहीं रोक सकती जब तक उसके हाथ में पुराने कर्ज़ का चाबुक न हो, जो मेरे हाथ में नहीं था। यह अच्छा ही था, उसके बिना मेरे गंदे हाथ कुछ और गंदे होने से बच गए थे। रोज-रोज की झिकझिक से ऊबकर आठ- दस दिन बाद मैंने उन दोनों को घर जाने को कह दिया।
बड़े तामझाम से, यानी अल्लम-गल्लम से भरी बाल्टी, टीन की ट्रंक और सीमेंट की बोरी में भूसे-जैसी ठुँसी घरेलू फटीचरी के साथ वे स्टेशन जाने को निकले। मैंने उन्हें समझाया कि यहाँ से जाने के लिए लखनऊ से इलाहाबादवाली दिन की गाड़ी पकड़ो और दिन-ही-दिन निकल जाओ। रात में न चलना। जैसी की उम्मीद थी, नेता की दिन की गाड़ी छूट गई। वे रातवाली से ही गए। तीन स्टेशन पार करके निगोंहा स्टेशन आते-आते गाड़ी में ही लुट गए। फिर रास्ते से किसी तरह वापस लौटे। अगले दिन वे फिर हमारे अधबने मकान के आगे मजदूरी करने के लिए खड़े हो गए। मेमसाहब ने लूटमार का पूरा-पूरा हाल बताया; विलाप नहीं किया, थोड़ा प्रलाप-भर किया। उसने लूटमार की भयंकरता भले ही न प्रकट की हो, नेता को बुजगदिली की पक्की सनद मिल गई। खुद नेता राजा जनक बने हुए निर्विकार मुद्रा में –अगर बेहरकत निगाह और फैले ओठों और निकले दाँतों को ऐसी मुद्रा माना जाए-सचमुच बैठे रहे। फिर, जिस तरह हवाई जहाज की दुर्घटना के बाद मरे हुए विमानचालकों और खुद अपनी दरकी हुई पसलियों को नजर अंदाज करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई राजकाज की किसी फ़ाइल को बेलौक ढंग से देखने लगे होंगे, लगभग वैसे ही अंदाज़ में नेता ने कहा, ‘‘मिस्त्री अब आज कि चिलम तुम्हारे भरोसे।’’ चिलम यानी गाँजा। मिस्त्री ने उन्हें घूरकर देखा, मासूम आवाज़ में मुझसे कहा, ‘‘पता नहीं क्या बकता रहता है।’’
मेमसाहब बोलीं:
‘‘डिब्बे की बत्तियाँ झपझप करती थीं। गाड़ी धीमी पड़ जातीं, रुकती तो बुझने लगतीं, बत्ती की सींक-भर दिखती, डिब्बे में घुप्प अँधेरा हो जाता। गाड़ी खिचिड़-खिचिड़ करके चल रही थी। तभी जो लड़का मेरे पास बैठा था, सीधा खड़ा हो गया। उसके हाथ में कट्टा था मेरी तो छाती धक्क-से रह गई....।’’
मेरा मन रहजनों के देसी तमंचे के दबदबें और मेमसाहब की छाती के बीच भटकने ही वाला था कि उसकी उँगली मेरी ओर उठ गई। बोलीं, ‘‘इन्हीं मुंसी- जैसा था, मरियल इतना ही लम्बा ऐसा ही दुबला-पतला। इन्हीं के जैसे बड़े-बड़े बाल। पुलिस जहाँ भी कहे, उसे सौ के बीच में पहचान लूँगी। ...
‘‘उसने अपना कट्टा तुम्हारे इन नेता की कनप़टी में ठोक दिया। दो-तीन लड़के और भी थे। डिब्बे के दरवाजों के पास खड़े होकर उन्होंने भी कट्टे निकाल लिए। एक के हाथ में छुरा था, वह सबको सुना कर बोला, चुपचाप बैठे रहो। अपने माल के पीछे जान मत दो।.....
‘‘नेता भोलानाथ बने बैठे रहे। भाँय-भाँय यही करते बनती है, वहाँ चोर कुत्ते की तरह कूँ तक नहीं की। संदूक मुझे ही खोलनी पड़ी। डिब्बे में हमारे उधर के और भी कई लोग थे। सभी के करम फूटे थे.....।
मेमसाहब की आवाज़ बड़ी प्यारी थी। कभी भूले-से सहज सुर में बोलतीं तो लगता, किसी अँधेरे कोने में तुम्हें बैठाकर फुसला रही हैं। पर उन्हें जोर से बोलने की आदत पड़ गयी थी, दिन-भर मर्दों के बीच काम करने का असर रहा होगा। इस वक्त उनकी आवाज़ में कुछ और भी तीखी झनक थी। क़ायदे से मुझे उनकी बात मिस्त्री की तरह कुछ ज़्यादा गौर से सुननी चाहिए थी। पर मेरा ध्यान उनके तमतमाए चेहरे और धक्क से रह जानेवावली सुडौल छाती के कारण भटका हुआ था। इसलिए भी कि रहज़नी की त्रास-भरी घटना मुझे ज़्यादा हिला नहीं पा रही थी। उसमें मेरे लिए कुछ नया नहीं था।
थाने का सिपाही पोस्टमार्डम कराने के लिए इंसान की लाश को मार्चुअरी के लिए से चलता है। उसे कपड़े से सिलवाकर रिक्शे पर रखवा लेता है। लाश का सिर रिक्शे के बाहर हिलगा रहता है। पाँव दूसरी ओर तने रहते हैं। रिक्शा किर्र-किर्र चलता रहता है। सिपाही बीड़ी फूँकता हुआ बाजार का नाजारा देखता रिक्शे पर बैठा रहता है। उस वक़्त सिपाही के मन में जितनी भावुकता होती है, उतनी ही भावुकता के साथ चाय सुड़कते हुए मैं रेलगाड़ी की रहज़नी का क़िस्सा सुन सकता हूँ।
एक मज़दूर को आवाज़ देकर मैंने उसे़ दो रुपय का नोट दिया, कहा, ‘‘नुक्कड़ से चार गिलास चाय ले आयो।’’
लूटमार का क़िस्सा सुनने की मुझे जरूरत न थी। उसका मैं सोते हुए भी आँखों देखा हाल बयान कर सकता हूँ। परसों रात नेता-दंपत्ति और दूसरे मुसाफिरों को लूटनेवाली जो युवाशक्ति थी, वह मेरे पुराने साथियों की होगी। इस पर मैं दस का नोट लगाने को तैयार हूँ।
कुछ समाजशास्त्री पंडितो ने भारतीय रेलगाड़ी को पहियों पर चलना-फिरता भारतीय गाँव बताया है। पर दरअसल रेलगाड़ी के मुक़ाबले गाँव बड़ी अदना चीज है। रेलगाड़ी गाँव कस्बा शहर-सभी की सभ्यता और संस्कृति का संगम है, इन सबके साथ अपनी गुंडागर्दी का भी; वैसे गुण्डागर्दी का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं वह भी सभ्यता में शामिल है, या शायद दोनों मिलकर गुंडागर्दी में। बहरहाल, जब आपके डिब्बे पर ककड़ी-खीरा, जामुन, आम, तला चना, अमरूद, मूँगफली और गन्ना बेचनेवाले कड़कदार आवाज़ के साथ धावा बोलते हैं तो वह गाँव हो जाता है। जवान बिटियाँ को बछिया की तरह आगे करके सोहर गाती हुई बेवा कटोरा खनकाकर उसकी शादी के लिए भीख माँगती है तो वही डिब्बा टाउन ऐरिया बन जाता है। जब पाकेट मार और ज़हर खिलाने वाले डिब्बे में घुसते हैं और उनके साथी घुटनों पर अटैची की मेज़ बनाकर ताश खेलते और ठर्रा पीते है तो वहाँ एकदम चौबीस कैरेटवाला शहर उतर आता है। अंधे, लूले, लँगड़े, कोढ़ी और मिठाई-पान-बीड़ी-सिगरेट बेचनेवाले डिब्बे में किसी शहरी हनुमान जी के मंदिर का माहौल पैदा करते हैं। अगर आप इन सब के बीच बधुआ बनकर जी रहे हैं तो आप मुसाफिर है और आपको टिकट की जरूरत है। अगर आप चोर-उचक्के या डकैत हैं खोंचेवाले या दूधिया हैं, भिखभंगे है या नौजवान डेली पैसेंजर हैं, तो फिर आप रेलवे के आदमी हैं; रेलवे स्टाफ से दुआ-सलाम करते हुए आप पहियों पर चलते-फिरते इस भारतवर्ष को बिना रोक-टोक अपनी पतलून की जेब में डालकर घूम सकते हैं। मुसाफिरों का उस पर कोई हक नहीं हैं, भारतीय रेल इसी समुदाय की बपौती है।
इस समुदाय में-मैं अपने इलाक़े की बात कर रहा हूँ –सबसे ज़्यादा ताकतवर गुट दैनिक यात्रियों का, यानी ‘डेलीवालों’ का है। दूधिया का भी। वास्तव में रेलवे के इस रसातल में प्रभुसत्ता के दावेदार यही दोनों गुट हैं। मौका़ पाते ही दूधिए पिंडारियों की तरह डिब्बे में घुस जाते है। ‘वे अपने दूध के कनस्तर खिड़की में बाधकर बाहर टाँग देते हैं और अपनी साईकिलें डिब्बें में खींचकर पुवाल की तरह जमा कर देतें है।
नौसिखिए मुसाफिर डिब्बें के किनारे-किनारे लटके हुए कनस्तरों के इन नारियल फलों को देखकर दुहकर या उसे धोखे में आ जाएँ कि यहाँ गाँव के कई मेहनतकश ग्वाले बैठे हुए जो दूध दुहकर या उसे घर-घर से इकट्ठा करके, मुँह अँधेरे बीवी-बच्चो को पीछे छोड़ पापी पेट के लिए शहर की ओर भागे हैं, पर समझदार मुसाफिर उस डिब्बे को ताऊनवाली बस्ती मानकर उधर मुँह नहीं करते। उधर डेलीवाले भी, जो खासतौर से रिज़र्व डिब्बों पर हमला करने के विशेषज्ञ हैं, बिना अपनी ताकत और सामूहिक ताक़त की पड़ताल किए दूधियों के मुँह नहीं लगते। ये दोनों गुट शहर से तीस-चालीस मील के देहाती स्टेशनों से आ-आकर रेल पर दैनिक यात्रा करते है और बराबर अशांतिपूर्ण सहअस्तित्व की हालत में रहते हैं।
तो, यह काम, निश्चित ही डेलीवालों का था। पिछले साल तक मैं खुद डेली पैसेंजर रहा हूँ। उस लाइन के लगभग सभी डेलीवालों को पहचानता हूँ। बरसों हम सब रेल पर साथ-साथ चले हैं। दूर-दूर से हम सब लोग बाँधकर लखनऊ आते थे। सब पढ़ते ही नहीं थे, कुछ नौकरी भी करते थे। पढ़नेवाले यूनिवर्सिटी में ही नहीं, शिया कालेज, कन्यकुब्ज कालेज, दयानंद ऐंग्लों वैदिक कालेज, विद्यांत हिंदू कालेज, क्रिश्चियन कालेज आदि में लेकर चुटकी भंडार पाठशाला तक फैले थे। सबकों बी.ए., एम.ए. करना था फिर आई.ए.एस. के इम्तिहान से शुरुआत करके और बाद में घूस देकर ग्रामीण विकास बैक की चपरासगिरी या बहुत हुआ तो निर्बल वर्ग विकास निगम में लेखा लिपिक की कुर्सी पर बैठना था। डेली पैसेंजरों से लगभग चालीस फ़ीसदी ऐसे ही भूतपूर्व छात्र थे जो अब सरकारी या लगभग-सरकारी नौकरी करते है और चूँकी उनमें से बहुतों ने नगद पैसे देकर नौकरी खरीदी थी, इसलिए वे उसे अपनी मौरूसी जायदाद मानते थे। डेली पैसेंजर का अपना संगठन था और रेलवेवालों की दुम में खटखटा बाँधने के लिए उसकी बाक़ायदा कार्यकारिणी थी जिसका दो साल तक मैं, यानी खुद मैं उपाध्याय रह चुका था।
डेलीवालों में बैंक और बीमा के कुछ कर्मचारियों को छोड़कर, जिनके मुकाबले ज़िले के कलेक्टर की तनख्वाह कुछ थोड़ी ही कम होती है, ज़्यादातर तीसरी और चौथी श्रेणी के कम तनख़्वाह कर्मी थे। पर उनकी ऐंठ से ही पता चल जाता था कि ये डेलीवाले है, वह अपने गिरोह का साहारा पाते ही खूँख्वार तेंदुआ बन जाते जाएगा। इसलिए डेलीवालों को सौ खून मुआफ़ थे। उनके कालेज या दफ़्तर पहुँचने का और वहाँ से घर के लिए चल देने का वक़्त प्रिंसिपल या दफ़्तर के हकीम नहीं तय करते थे, इसका फैसला रेलवे का टाइम टेबुल करता था। दो साल पहले मैंने ही डेली पैसेंजर असोसिएशन के वाइसचेयरमैन की हैसियत से एक ज्ञापन देकर बेमतलब विनम्रता दिखाए बिना ऐलान किया था कि कालेज और दफ्तर के घंटों और हमारी आमद-रक्त के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी रेलवे मिनिस्टर की है।
अब अगर कुछ डेलीवाले इस नेता-जैसे फक्कड़ आदमी की कनपटी पर कट्टा ठोंक देते हैं या किसी मोहतरमा के गले से चेन खींच लेते हैं तो क़ानून कुछ भी कहे, यह कोई ख़ास बात नहीं है। यह एक खिलवाड़ है या, ज्यादा-से-ज्यादा,उनका व्यवहारिक जीवन-दर्शन है।
वैसे उनका व्यवहारिक जीवन-दर्शन कुछ ज्यादा ही व्यावहारिक है। मसलन, अगर गाँव स्टेशन से दो मील की दूरी पर है तो स्टेशन आने के पहले गाँव के पास चेन खींच लेना या होज़पाइप निकाल कर गाड़ी को रोक लेना बिलकुल स्वाभाविक होगा। एक दिन की बात हो तो स्टेशन से घर तक पैदल चल लें, पर हर रोज दो-दो बार दो मील पगडंडी नापने का काम कौन चिड़ीमार करेगा ? वैसे ही, गाड़ी चाहे जैसी भीड़ हो, वे बैठकर चलेंगे उन्हें रोज ही रेल से चलना है, खड़े-ख़ड़े कहाँ तक टाँगे तोड़ें ? तभी किसी शरीफ दिखनेवाले मुसाफिर के दाएँ-बाँए, जगह हो या न हो, धँस जाएँगे और उसे अपने नितंब के एक बटा चौंसठ अंश पर टिकने को मजबूर कर देंगे। मुसाफिर हयादार हुआ तो खुद उठकर खड़ा हो जाएगा और खिड़की के बाहर की छटा निहारने लगेगा। तब हमारे डेलीवाले साथी उसकी सौम्यता को पहचानते हुए, गाली-गलौज का सहज संबोधन छोड़कर मौसम के विषय में योरोपीय शिष्टाचार निभाते हुए उससे कहेंगे कि आज बडी गर्मी है और आपके उधर बारिश हुई या नहीं। यही व्यवहार- बुद्धि टिकट पर भी लागू होती है। रोज-रोज चलना है, कहाँ तक टिकट खरीदें ? कल तो लिया ही था। और अगर माहवारी टिकट की बात हो तो इस महीने में दशहरे की छुट्टियाँ भी तो हैं, दस दिन के लिए माहवारी टिकट लेनेवाले भकुए इस इलाक़े में नहीं रहते।
इन तर्कों का तोड़ दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर-जैसे ज़िलों यानी कला और संस्कृति के चुनौती-भरे कार्यों में पच्चानबे प्रतिशत और आर्थिक विकास के मामले में पाँच प्रतिशत अंक पानेवाले मध्यप्रदेश नामक राज्य के भीतरी क्षेत्रों से आनेवाले मजदूरों की लूटपाट पर होता है। ये लोग हमारे राज्य की संपत्ति लेकर आपने गाँव जा रहे है, इतने रुपयों का क्या करेंगे ? रुपया खर्च करने की तमीज भी है उन्हें ? उसे फूँक-तापकर आखिर यहीं वापस आएँगे न ? अच्छा है कि इन्हें अभी से हल्का कर दिया जाए। रुपया सत्कर्म में लग जाएगा। वह कालिज की फीस भरने या बड़े भाई की नौकरी के लिए हाकिम को घूस देने के काम आएगा। कुछ न हुआ तो शहर के किसी मेहनतकश ढाबेवाले के हाथ पर उसके मुर्गें और रम के बदले बख़्शीश के तौर पर रख दिया जाएगा।
‘‘एक काला-काला लड़का है, ’’मैंने कहा,’’ मुँह पर चेचक के दाग हैं। बालों में चाहे जितना तेल-पानी चुपड़े, वे खड़े ही रहते हैं। जिसने नेता की कनपटी पर कट्टा ठोंका था वह यही लड़का तो नहीं है ?’’
मेमसाहब ने मुझे घूरा, बोलीं,’’ बोल तो दिया मुंसी जी, वह तुम्हारा ही जैसा था। तुम काले हो ? तुम्हारे मुँह पर दाग हैं ?’’
‘‘चुप रह।’’ नेता बोले, पर उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ।
तब यह काम बरचरन एंड कंपनी का है-मैंने सोचा पर कहा नहीं। वह मेरे साथ बी.ए. तक पढ़ा है, अब कानून पढ़ रहा है। मेरा ही जैसा गोरा-चिट्टा और दुबला-पतला है। एक बार टिकट मुसाफिरों की मजिस्ट्रेटी जाँच होने लगी। पुलसवालों ने हरचरन को रपटा लिया, वह उन्हें बुत्ता देकर स्टेशन मास्टर के कमरे में मेज के नीचे दुबक गया। स्टेशन मास्टर को वहीं नौकरी करनी थी। बाहर गलियारे की ओर उँगली उठाकर चीखने लगे, ‘वह गया, वह गया !’ पीठ की तरफ से हम दोनों इतना एक-से दीखते थे कि एक पुलिसवाले ने मुझे ही दबोच लिया। उस दिन अपने फूफा के पैसे से उनका टिकट खरीदते वक़्त उसी से मैंने अपना भी टिकट ले लिया था। सिपाही को झटककर मैंने कहा, ‘खबरदार मुझे चमड़े के हाथ न लगाना।’ दुनिया के आठवे अजूबे जैसा टिकट अपनी जेब से निकालकर मैं उनकी नाक के सामने हिलने लगा; रेलवे प्रशासन के खिलाफ एक संक्षिप्त पर मार्मिक भाषण भी दिया।
यह एक मामूली-सी घटना है। पिछले साल राजनीतिशास्त्र में एम.ए. करके निठल्ले बैठने से यल.यल.बी. होना भला, यह मानकर कानून की डिग्री के लिए एक स्थानीय कालेज मे नाम लिखवा चुकने के बाद इस अधबने मकान के मालिक का मुंशी बनने तक मेरा गड्ढ, जिसका कि नाम ज़िन्दगी है, इस तरह की सैकड़ों मामूली घटनाओं से भरा पड़ा है।
मैंने कहा, ‘‘मेमसाहब, घबराओं नहीं। लुटेरों का पता मैं लगाऊँगा।’’
‘‘रुपिया भी लौट आवेगा ?’’
‘‘वह अब क्या लौटेगा, पर कम-से-कम उत्तर प्रदेश में दुबारा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं होगा।’’ कहते ही मैंने शरीर को डाइरेक्टर जनरल आफ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश की चुस्ती-दुरुस्ती वर्दी में सजा हुआ पाया। बिना आँख मूँदे ही मैं अपने ख़याली सिनेमा की वह रील देखने लगा जिसमें मेरे इशारे पर निगोहाँ थाने की मुस्तैद पुलिस हरकत और उसके साथियों को पेड़ की डाल से चमगादड़-जैसा लटकाकर उनसे रेल डकैती का पूरा ब्यौरा उगलवा रही है।
मुंसी मैं ही था। सुनकर हाकिमाना अंदाज से मैं दूसरी ओर किसी मजदूर को सुस्ती छोड़कर चुस्ती दिखाने के लिए आवाज़ देता। पर मैं जानता था कि बिलासपुरी मज़दूर का जी उखड़ जाए तो उसे बिलासपुर से लेकर दिल्ली तक की कोई भी ताकत तब तक नहीं रोक सकती जब तक उसके हाथ में पुराने कर्ज़ का चाबुक न हो, जो मेरे हाथ में नहीं था। यह अच्छा ही था, उसके बिना मेरे गंदे हाथ कुछ और गंदे होने से बच गए थे। रोज-रोज की झिकझिक से ऊबकर आठ- दस दिन बाद मैंने उन दोनों को घर जाने को कह दिया।
बड़े तामझाम से, यानी अल्लम-गल्लम से भरी बाल्टी, टीन की ट्रंक और सीमेंट की बोरी में भूसे-जैसी ठुँसी घरेलू फटीचरी के साथ वे स्टेशन जाने को निकले। मैंने उन्हें समझाया कि यहाँ से जाने के लिए लखनऊ से इलाहाबादवाली दिन की गाड़ी पकड़ो और दिन-ही-दिन निकल जाओ। रात में न चलना। जैसी की उम्मीद थी, नेता की दिन की गाड़ी छूट गई। वे रातवाली से ही गए। तीन स्टेशन पार करके निगोंहा स्टेशन आते-आते गाड़ी में ही लुट गए। फिर रास्ते से किसी तरह वापस लौटे। अगले दिन वे फिर हमारे अधबने मकान के आगे मजदूरी करने के लिए खड़े हो गए। मेमसाहब ने लूटमार का पूरा-पूरा हाल बताया; विलाप नहीं किया, थोड़ा प्रलाप-भर किया। उसने लूटमार की भयंकरता भले ही न प्रकट की हो, नेता को बुजगदिली की पक्की सनद मिल गई। खुद नेता राजा जनक बने हुए निर्विकार मुद्रा में –अगर बेहरकत निगाह और फैले ओठों और निकले दाँतों को ऐसी मुद्रा माना जाए-सचमुच बैठे रहे। फिर, जिस तरह हवाई जहाज की दुर्घटना के बाद मरे हुए विमानचालकों और खुद अपनी दरकी हुई पसलियों को नजर अंदाज करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई राजकाज की किसी फ़ाइल को बेलौक ढंग से देखने लगे होंगे, लगभग वैसे ही अंदाज़ में नेता ने कहा, ‘‘मिस्त्री अब आज कि चिलम तुम्हारे भरोसे।’’ चिलम यानी गाँजा। मिस्त्री ने उन्हें घूरकर देखा, मासूम आवाज़ में मुझसे कहा, ‘‘पता नहीं क्या बकता रहता है।’’
मेमसाहब बोलीं:
‘‘डिब्बे की बत्तियाँ झपझप करती थीं। गाड़ी धीमी पड़ जातीं, रुकती तो बुझने लगतीं, बत्ती की सींक-भर दिखती, डिब्बे में घुप्प अँधेरा हो जाता। गाड़ी खिचिड़-खिचिड़ करके चल रही थी। तभी जो लड़का मेरे पास बैठा था, सीधा खड़ा हो गया। उसके हाथ में कट्टा था मेरी तो छाती धक्क-से रह गई....।’’
मेरा मन रहजनों के देसी तमंचे के दबदबें और मेमसाहब की छाती के बीच भटकने ही वाला था कि उसकी उँगली मेरी ओर उठ गई। बोलीं, ‘‘इन्हीं मुंसी- जैसा था, मरियल इतना ही लम्बा ऐसा ही दुबला-पतला। इन्हीं के जैसे बड़े-बड़े बाल। पुलिस जहाँ भी कहे, उसे सौ के बीच में पहचान लूँगी। ...
‘‘उसने अपना कट्टा तुम्हारे इन नेता की कनप़टी में ठोक दिया। दो-तीन लड़के और भी थे। डिब्बे के दरवाजों के पास खड़े होकर उन्होंने भी कट्टे निकाल लिए। एक के हाथ में छुरा था, वह सबको सुना कर बोला, चुपचाप बैठे रहो। अपने माल के पीछे जान मत दो।.....
‘‘नेता भोलानाथ बने बैठे रहे। भाँय-भाँय यही करते बनती है, वहाँ चोर कुत्ते की तरह कूँ तक नहीं की। संदूक मुझे ही खोलनी पड़ी। डिब्बे में हमारे उधर के और भी कई लोग थे। सभी के करम फूटे थे.....।
मेमसाहब की आवाज़ बड़ी प्यारी थी। कभी भूले-से सहज सुर में बोलतीं तो लगता, किसी अँधेरे कोने में तुम्हें बैठाकर फुसला रही हैं। पर उन्हें जोर से बोलने की आदत पड़ गयी थी, दिन-भर मर्दों के बीच काम करने का असर रहा होगा। इस वक्त उनकी आवाज़ में कुछ और भी तीखी झनक थी। क़ायदे से मुझे उनकी बात मिस्त्री की तरह कुछ ज़्यादा गौर से सुननी चाहिए थी। पर मेरा ध्यान उनके तमतमाए चेहरे और धक्क से रह जानेवावली सुडौल छाती के कारण भटका हुआ था। इसलिए भी कि रहज़नी की त्रास-भरी घटना मुझे ज़्यादा हिला नहीं पा रही थी। उसमें मेरे लिए कुछ नया नहीं था।
थाने का सिपाही पोस्टमार्डम कराने के लिए इंसान की लाश को मार्चुअरी के लिए से चलता है। उसे कपड़े से सिलवाकर रिक्शे पर रखवा लेता है। लाश का सिर रिक्शे के बाहर हिलगा रहता है। पाँव दूसरी ओर तने रहते हैं। रिक्शा किर्र-किर्र चलता रहता है। सिपाही बीड़ी फूँकता हुआ बाजार का नाजारा देखता रिक्शे पर बैठा रहता है। उस वक़्त सिपाही के मन में जितनी भावुकता होती है, उतनी ही भावुकता के साथ चाय सुड़कते हुए मैं रेलगाड़ी की रहज़नी का क़िस्सा सुन सकता हूँ।
एक मज़दूर को आवाज़ देकर मैंने उसे़ दो रुपय का नोट दिया, कहा, ‘‘नुक्कड़ से चार गिलास चाय ले आयो।’’
लूटमार का क़िस्सा सुनने की मुझे जरूरत न थी। उसका मैं सोते हुए भी आँखों देखा हाल बयान कर सकता हूँ। परसों रात नेता-दंपत्ति और दूसरे मुसाफिरों को लूटनेवाली जो युवाशक्ति थी, वह मेरे पुराने साथियों की होगी। इस पर मैं दस का नोट लगाने को तैयार हूँ।
कुछ समाजशास्त्री पंडितो ने भारतीय रेलगाड़ी को पहियों पर चलना-फिरता भारतीय गाँव बताया है। पर दरअसल रेलगाड़ी के मुक़ाबले गाँव बड़ी अदना चीज है। रेलगाड़ी गाँव कस्बा शहर-सभी की सभ्यता और संस्कृति का संगम है, इन सबके साथ अपनी गुंडागर्दी का भी; वैसे गुण्डागर्दी का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं वह भी सभ्यता में शामिल है, या शायद दोनों मिलकर गुंडागर्दी में। बहरहाल, जब आपके डिब्बे पर ककड़ी-खीरा, जामुन, आम, तला चना, अमरूद, मूँगफली और गन्ना बेचनेवाले कड़कदार आवाज़ के साथ धावा बोलते हैं तो वह गाँव हो जाता है। जवान बिटियाँ को बछिया की तरह आगे करके सोहर गाती हुई बेवा कटोरा खनकाकर उसकी शादी के लिए भीख माँगती है तो वही डिब्बा टाउन ऐरिया बन जाता है। जब पाकेट मार और ज़हर खिलाने वाले डिब्बे में घुसते हैं और उनके साथी घुटनों पर अटैची की मेज़ बनाकर ताश खेलते और ठर्रा पीते है तो वहाँ एकदम चौबीस कैरेटवाला शहर उतर आता है। अंधे, लूले, लँगड़े, कोढ़ी और मिठाई-पान-बीड़ी-सिगरेट बेचनेवाले डिब्बे में किसी शहरी हनुमान जी के मंदिर का माहौल पैदा करते हैं। अगर आप इन सब के बीच बधुआ बनकर जी रहे हैं तो आप मुसाफिर है और आपको टिकट की जरूरत है। अगर आप चोर-उचक्के या डकैत हैं खोंचेवाले या दूधिया हैं, भिखभंगे है या नौजवान डेली पैसेंजर हैं, तो फिर आप रेलवे के आदमी हैं; रेलवे स्टाफ से दुआ-सलाम करते हुए आप पहियों पर चलते-फिरते इस भारतवर्ष को बिना रोक-टोक अपनी पतलून की जेब में डालकर घूम सकते हैं। मुसाफिरों का उस पर कोई हक नहीं हैं, भारतीय रेल इसी समुदाय की बपौती है।
इस समुदाय में-मैं अपने इलाक़े की बात कर रहा हूँ –सबसे ज़्यादा ताकतवर गुट दैनिक यात्रियों का, यानी ‘डेलीवालों’ का है। दूधिया का भी। वास्तव में रेलवे के इस रसातल में प्रभुसत्ता के दावेदार यही दोनों गुट हैं। मौका़ पाते ही दूधिए पिंडारियों की तरह डिब्बे में घुस जाते है। ‘वे अपने दूध के कनस्तर खिड़की में बाधकर बाहर टाँग देते हैं और अपनी साईकिलें डिब्बें में खींचकर पुवाल की तरह जमा कर देतें है।
नौसिखिए मुसाफिर डिब्बें के किनारे-किनारे लटके हुए कनस्तरों के इन नारियल फलों को देखकर दुहकर या उसे धोखे में आ जाएँ कि यहाँ गाँव के कई मेहनतकश ग्वाले बैठे हुए जो दूध दुहकर या उसे घर-घर से इकट्ठा करके, मुँह अँधेरे बीवी-बच्चो को पीछे छोड़ पापी पेट के लिए शहर की ओर भागे हैं, पर समझदार मुसाफिर उस डिब्बे को ताऊनवाली बस्ती मानकर उधर मुँह नहीं करते। उधर डेलीवाले भी, जो खासतौर से रिज़र्व डिब्बों पर हमला करने के विशेषज्ञ हैं, बिना अपनी ताकत और सामूहिक ताक़त की पड़ताल किए दूधियों के मुँह नहीं लगते। ये दोनों गुट शहर से तीस-चालीस मील के देहाती स्टेशनों से आ-आकर रेल पर दैनिक यात्रा करते है और बराबर अशांतिपूर्ण सहअस्तित्व की हालत में रहते हैं।
तो, यह काम, निश्चित ही डेलीवालों का था। पिछले साल तक मैं खुद डेली पैसेंजर रहा हूँ। उस लाइन के लगभग सभी डेलीवालों को पहचानता हूँ। बरसों हम सब रेल पर साथ-साथ चले हैं। दूर-दूर से हम सब लोग बाँधकर लखनऊ आते थे। सब पढ़ते ही नहीं थे, कुछ नौकरी भी करते थे। पढ़नेवाले यूनिवर्सिटी में ही नहीं, शिया कालेज, कन्यकुब्ज कालेज, दयानंद ऐंग्लों वैदिक कालेज, विद्यांत हिंदू कालेज, क्रिश्चियन कालेज आदि में लेकर चुटकी भंडार पाठशाला तक फैले थे। सबकों बी.ए., एम.ए. करना था फिर आई.ए.एस. के इम्तिहान से शुरुआत करके और बाद में घूस देकर ग्रामीण विकास बैक की चपरासगिरी या बहुत हुआ तो निर्बल वर्ग विकास निगम में लेखा लिपिक की कुर्सी पर बैठना था। डेली पैसेंजरों से लगभग चालीस फ़ीसदी ऐसे ही भूतपूर्व छात्र थे जो अब सरकारी या लगभग-सरकारी नौकरी करते है और चूँकी उनमें से बहुतों ने नगद पैसे देकर नौकरी खरीदी थी, इसलिए वे उसे अपनी मौरूसी जायदाद मानते थे। डेली पैसेंजर का अपना संगठन था और रेलवेवालों की दुम में खटखटा बाँधने के लिए उसकी बाक़ायदा कार्यकारिणी थी जिसका दो साल तक मैं, यानी खुद मैं उपाध्याय रह चुका था।
डेलीवालों में बैंक और बीमा के कुछ कर्मचारियों को छोड़कर, जिनके मुकाबले ज़िले के कलेक्टर की तनख्वाह कुछ थोड़ी ही कम होती है, ज़्यादातर तीसरी और चौथी श्रेणी के कम तनख़्वाह कर्मी थे। पर उनकी ऐंठ से ही पता चल जाता था कि ये डेलीवाले है, वह अपने गिरोह का साहारा पाते ही खूँख्वार तेंदुआ बन जाते जाएगा। इसलिए डेलीवालों को सौ खून मुआफ़ थे। उनके कालेज या दफ़्तर पहुँचने का और वहाँ से घर के लिए चल देने का वक़्त प्रिंसिपल या दफ़्तर के हकीम नहीं तय करते थे, इसका फैसला रेलवे का टाइम टेबुल करता था। दो साल पहले मैंने ही डेली पैसेंजर असोसिएशन के वाइसचेयरमैन की हैसियत से एक ज्ञापन देकर बेमतलब विनम्रता दिखाए बिना ऐलान किया था कि कालेज और दफ्तर के घंटों और हमारी आमद-रक्त के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी रेलवे मिनिस्टर की है।
अब अगर कुछ डेलीवाले इस नेता-जैसे फक्कड़ आदमी की कनपटी पर कट्टा ठोंक देते हैं या किसी मोहतरमा के गले से चेन खींच लेते हैं तो क़ानून कुछ भी कहे, यह कोई ख़ास बात नहीं है। यह एक खिलवाड़ है या, ज्यादा-से-ज्यादा,उनका व्यवहारिक जीवन-दर्शन है।
वैसे उनका व्यवहारिक जीवन-दर्शन कुछ ज्यादा ही व्यावहारिक है। मसलन, अगर गाँव स्टेशन से दो मील की दूरी पर है तो स्टेशन आने के पहले गाँव के पास चेन खींच लेना या होज़पाइप निकाल कर गाड़ी को रोक लेना बिलकुल स्वाभाविक होगा। एक दिन की बात हो तो स्टेशन से घर तक पैदल चल लें, पर हर रोज दो-दो बार दो मील पगडंडी नापने का काम कौन चिड़ीमार करेगा ? वैसे ही, गाड़ी चाहे जैसी भीड़ हो, वे बैठकर चलेंगे उन्हें रोज ही रेल से चलना है, खड़े-ख़ड़े कहाँ तक टाँगे तोड़ें ? तभी किसी शरीफ दिखनेवाले मुसाफिर के दाएँ-बाँए, जगह हो या न हो, धँस जाएँगे और उसे अपने नितंब के एक बटा चौंसठ अंश पर टिकने को मजबूर कर देंगे। मुसाफिर हयादार हुआ तो खुद उठकर खड़ा हो जाएगा और खिड़की के बाहर की छटा निहारने लगेगा। तब हमारे डेलीवाले साथी उसकी सौम्यता को पहचानते हुए, गाली-गलौज का सहज संबोधन छोड़कर मौसम के विषय में योरोपीय शिष्टाचार निभाते हुए उससे कहेंगे कि आज बडी गर्मी है और आपके उधर बारिश हुई या नहीं। यही व्यवहार- बुद्धि टिकट पर भी लागू होती है। रोज-रोज चलना है, कहाँ तक टिकट खरीदें ? कल तो लिया ही था। और अगर माहवारी टिकट की बात हो तो इस महीने में दशहरे की छुट्टियाँ भी तो हैं, दस दिन के लिए माहवारी टिकट लेनेवाले भकुए इस इलाक़े में नहीं रहते।
इन तर्कों का तोड़ दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर-जैसे ज़िलों यानी कला और संस्कृति के चुनौती-भरे कार्यों में पच्चानबे प्रतिशत और आर्थिक विकास के मामले में पाँच प्रतिशत अंक पानेवाले मध्यप्रदेश नामक राज्य के भीतरी क्षेत्रों से आनेवाले मजदूरों की लूटपाट पर होता है। ये लोग हमारे राज्य की संपत्ति लेकर आपने गाँव जा रहे है, इतने रुपयों का क्या करेंगे ? रुपया खर्च करने की तमीज भी है उन्हें ? उसे फूँक-तापकर आखिर यहीं वापस आएँगे न ? अच्छा है कि इन्हें अभी से हल्का कर दिया जाए। रुपया सत्कर्म में लग जाएगा। वह कालिज की फीस भरने या बड़े भाई की नौकरी के लिए हाकिम को घूस देने के काम आएगा। कुछ न हुआ तो शहर के किसी मेहनतकश ढाबेवाले के हाथ पर उसके मुर्गें और रम के बदले बख़्शीश के तौर पर रख दिया जाएगा।
‘‘एक काला-काला लड़का है, ’’मैंने कहा,’’ मुँह पर चेचक के दाग हैं। बालों में चाहे जितना तेल-पानी चुपड़े, वे खड़े ही रहते हैं। जिसने नेता की कनपटी पर कट्टा ठोंका था वह यही लड़का तो नहीं है ?’’
मेमसाहब ने मुझे घूरा, बोलीं,’’ बोल तो दिया मुंसी जी, वह तुम्हारा ही जैसा था। तुम काले हो ? तुम्हारे मुँह पर दाग हैं ?’’
‘‘चुप रह।’’ नेता बोले, पर उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ।
तब यह काम बरचरन एंड कंपनी का है-मैंने सोचा पर कहा नहीं। वह मेरे साथ बी.ए. तक पढ़ा है, अब कानून पढ़ रहा है। मेरा ही जैसा गोरा-चिट्टा और दुबला-पतला है। एक बार टिकट मुसाफिरों की मजिस्ट्रेटी जाँच होने लगी। पुलसवालों ने हरचरन को रपटा लिया, वह उन्हें बुत्ता देकर स्टेशन मास्टर के कमरे में मेज के नीचे दुबक गया। स्टेशन मास्टर को वहीं नौकरी करनी थी। बाहर गलियारे की ओर उँगली उठाकर चीखने लगे, ‘वह गया, वह गया !’ पीठ की तरफ से हम दोनों इतना एक-से दीखते थे कि एक पुलिसवाले ने मुझे ही दबोच लिया। उस दिन अपने फूफा के पैसे से उनका टिकट खरीदते वक़्त उसी से मैंने अपना भी टिकट ले लिया था। सिपाही को झटककर मैंने कहा, ‘खबरदार मुझे चमड़े के हाथ न लगाना।’ दुनिया के आठवे अजूबे जैसा टिकट अपनी जेब से निकालकर मैं उनकी नाक के सामने हिलने लगा; रेलवे प्रशासन के खिलाफ एक संक्षिप्त पर मार्मिक भाषण भी दिया।
यह एक मामूली-सी घटना है। पिछले साल राजनीतिशास्त्र में एम.ए. करके निठल्ले बैठने से यल.यल.बी. होना भला, यह मानकर कानून की डिग्री के लिए एक स्थानीय कालेज मे नाम लिखवा चुकने के बाद इस अधबने मकान के मालिक का मुंशी बनने तक मेरा गड्ढ, जिसका कि नाम ज़िन्दगी है, इस तरह की सैकड़ों मामूली घटनाओं से भरा पड़ा है।
मैंने कहा, ‘‘मेमसाहब, घबराओं नहीं। लुटेरों का पता मैं लगाऊँगा।’’
‘‘रुपिया भी लौट आवेगा ?’’
‘‘वह अब क्या लौटेगा, पर कम-से-कम उत्तर प्रदेश में दुबारा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं होगा।’’ कहते ही मैंने शरीर को डाइरेक्टर जनरल आफ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश की चुस्ती-दुरुस्ती वर्दी में सजा हुआ पाया। बिना आँख मूँदे ही मैं अपने ख़याली सिनेमा की वह रील देखने लगा जिसमें मेरे इशारे पर निगोहाँ थाने की मुस्तैद पुलिस हरकत और उसके साथियों को पेड़ की डाल से चमगादड़-जैसा लटकाकर उनसे रेल डकैती का पूरा ब्यौरा उगलवा रही है।
2
मोटर रुकने पर परमात्मा जी तुरंत नीचे नहीं उतरे; खिड़की के शीशे चढ़ाए, नाक सिकोड़ थोड़ी देर अंदर ही बैठे रहे। श्यामवर्ण ठिंगनी काया, उस पर उम्दा सफ़ारी सूट, मत्थे पर रोली कि बिंदी। गाड़ी के शीशे हल्के रंगीन थे, अंदर कार के गद्दे गहरे नीले रंग के। गाड़ी के रुकते-रुकते बालू, चूना, सुर्खी, धूल आदि सनीमा-जैसा झलका। जो धूल दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे, उड़ी थी धीरे-धीरे पुरानी जगह और हम लोगों के कपड़ो और चेहरों पर आकर बैठ गई। तब ड्राइवर ने दरवाज़ा खेला। परमत्मा जी ने उतरते ही पूछा, ‘‘बढ़ई का क्या हुआ ?’’
‘‘आज भी नहीं आया।’’
‘‘उसके घर पर पता लगवाया ?’’
‘‘मैं खुद कल दो बार गया था, आज सवेरे भी किसी शादी में गया है। कब लौटेगा किसी को पता नहीं ।’’
‘‘पेशगी कितना दिया था ?’’
‘‘तीन सौ सत्तर रुपए।’’
‘‘तुम रहे पोंगा ही। अब भूल जाओ, किसी दूसरे का इंतजार करो वह तीन सौ सत्तर भी भूल जाओ। पर तुम्हें क्या तुम तो पहले ही भूले हो।’’
मैंने ओंठ बंद करके उन्हें दाएँ-बाएँ फैलाया और आँख सिकोड़ीं। हम डेलीवाले ऐसे ही मुस्कराते थे कहा, ‘‘जीजा जी, ऐसा नहीं है। तीन सौ सत्तर की जगह पाँच सौ न वसूलू तो कहिएगा....।’’
वे मेरे जीजा यानी मेरी बहन के पति परमेश्वर नहीं हैं, फिर भी मैं उन्हें जीजाजी कहता हूँ। उनको मेरे गाँववाले पड़ोसी की लड़की ब्याही है। थोड़ा फ़्लैशबैक मारा जाए तो कहा जा सकता है कि उनका ब्याह उस लड़की से हुआ है जो बचपन में मेरी दोस्त थी; कविता की रसभरी ज़बान में सहचरी। हम खेत की मेड़ों पर और बागों में साथ-साथ दौड़े थे; खलियान मे पुवाल के ढेरों में कब्र बनाकर अंग-से-अंग मिलाकर एक साथ दफन हुए थे, एक साथ बालों के तिनके झाड़ते हुए फ़रिश्तों की तरफ उठे थे। बाद में मेरी वह सचमुच की सहचरी बन गई थी पर कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण इसके खिलाफ़ पड़ गए।
‘‘आज भी नहीं आया।’’
‘‘उसके घर पर पता लगवाया ?’’
‘‘मैं खुद कल दो बार गया था, आज सवेरे भी किसी शादी में गया है। कब लौटेगा किसी को पता नहीं ।’’
‘‘पेशगी कितना दिया था ?’’
‘‘तीन सौ सत्तर रुपए।’’
‘‘तुम रहे पोंगा ही। अब भूल जाओ, किसी दूसरे का इंतजार करो वह तीन सौ सत्तर भी भूल जाओ। पर तुम्हें क्या तुम तो पहले ही भूले हो।’’
मैंने ओंठ बंद करके उन्हें दाएँ-बाएँ फैलाया और आँख सिकोड़ीं। हम डेलीवाले ऐसे ही मुस्कराते थे कहा, ‘‘जीजा जी, ऐसा नहीं है। तीन सौ सत्तर की जगह पाँच सौ न वसूलू तो कहिएगा....।’’
वे मेरे जीजा यानी मेरी बहन के पति परमेश्वर नहीं हैं, फिर भी मैं उन्हें जीजाजी कहता हूँ। उनको मेरे गाँववाले पड़ोसी की लड़की ब्याही है। थोड़ा फ़्लैशबैक मारा जाए तो कहा जा सकता है कि उनका ब्याह उस लड़की से हुआ है जो बचपन में मेरी दोस्त थी; कविता की रसभरी ज़बान में सहचरी। हम खेत की मेड़ों पर और बागों में साथ-साथ दौड़े थे; खलियान मे पुवाल के ढेरों में कब्र बनाकर अंग-से-अंग मिलाकर एक साथ दफन हुए थे, एक साथ बालों के तिनके झाड़ते हुए फ़रिश्तों की तरफ उठे थे। बाद में मेरी वह सचमुच की सहचरी बन गई थी पर कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण इसके खिलाफ़ पड़ गए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book