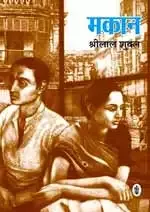|
उपन्यास >> मकान मकानश्रीलाल शुक्ल
|
261 पाठक हैं |
||||||
संघर्ष, शोषण और अव्यवस्था के दौर से गुजरते हुए तीक्ष्ण प्रतिक्रियाएँ.....
Makan
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
नारायण एक सितारवादक है। जीविका के लिए वह परिवार को दूसरी जगह छोड़कर अपने पुराने शहर में आता है और यहीं से मकान की तलाश शुरू होती है। एक दौरान उसका सितार से साथ छूटने लगता है; और अब वह जिनके साथ जुड़ता है उसमें मकान बाँटनेवाला अफसर है कर्मचारी-यूनियन का नेता बारीन हालदार है, पुरानी शिष्या श्यामा है, वेश्या-पुत्री सिम्मी है और वे तमाम तत्त्व हैं जो जिंदगी के बिखराव को तीखा बनाते है।
इस संघर्ष शोषण और अव्यवस्था के दौर से गुजरते हुए तीक्ष्ण प्रतिक्रियाएँ व्यक्त होती हैः ‘मजाक देखा तुमने ? हम आसमान में उपग्रह उड़ा सकते हैं पर इस निगम के सीवेज के लिए मशीनों का जुगाड़ नहीं कर सकते। यहाँ सीवेज की सफाई के लिए तो बलि के बकरे चाहिए, पर बिस्कुट बनाने के लिए यहाँ से नयी मशीनें मौजूद हैं.....’
‘जैसे कुछ तांत्रिक लोग शराब पीने से पहले माँ काली के नाम पर दो-चार बूँटें जमीन पर छिड़क देते हैं; वैसे ही हाउसिगं की पूरी-की-पूरी स्कीम गटकने से पहले चतुर लोग हरिजनों के नाम दस-बीस प्लाट निकाल देते हैं...’ उपन्यास का अंत सर्वथा अप्रत्याशित मोड़ पर होता है।
‘मकान’ यशस्वी कथाकार श्रीलाल शुक्ला की बहुप्रशंसित कृति है। वस्तुतः की पृष्ठभूमि में कलाकार के जीवन की आकांक्षाओं, जिम्मेदारियों, विसंगतियों और तनावों को केन्द्र बनाकर लिखा गया हिंदी में अपनी तरह का यह पहला उपन्यास है।
1971 में, इस उपन्यास की शुरुआत के दिनों में जो ‘जेम’ और ‘स्काउट’ भर थे
और
1976 में इसके पूरे होने तक जो इसे समझने और इसकी आलोचना करने की वयस्कता
पा चुके हैं
उन्हीं
आशुतोष और विनीता
को
इस संघर्ष शोषण और अव्यवस्था के दौर से गुजरते हुए तीक्ष्ण प्रतिक्रियाएँ व्यक्त होती हैः ‘मजाक देखा तुमने ? हम आसमान में उपग्रह उड़ा सकते हैं पर इस निगम के सीवेज के लिए मशीनों का जुगाड़ नहीं कर सकते। यहाँ सीवेज की सफाई के लिए तो बलि के बकरे चाहिए, पर बिस्कुट बनाने के लिए यहाँ से नयी मशीनें मौजूद हैं.....’
‘जैसे कुछ तांत्रिक लोग शराब पीने से पहले माँ काली के नाम पर दो-चार बूँटें जमीन पर छिड़क देते हैं; वैसे ही हाउसिगं की पूरी-की-पूरी स्कीम गटकने से पहले चतुर लोग हरिजनों के नाम दस-बीस प्लाट निकाल देते हैं...’ उपन्यास का अंत सर्वथा अप्रत्याशित मोड़ पर होता है।
‘मकान’ यशस्वी कथाकार श्रीलाल शुक्ला की बहुप्रशंसित कृति है। वस्तुतः की पृष्ठभूमि में कलाकार के जीवन की आकांक्षाओं, जिम्मेदारियों, विसंगतियों और तनावों को केन्द्र बनाकर लिखा गया हिंदी में अपनी तरह का यह पहला उपन्यास है।
1971 में, इस उपन्यास की शुरुआत के दिनों में जो ‘जेम’ और ‘स्काउट’ भर थे
और
1976 में इसके पूरे होने तक जो इसे समझने और इसकी आलोचना करने की वयस्कता
पा चुके हैं
उन्हीं
आशुतोष और विनीता
को
3अक्तूबर, 1974-गुरुवार
नारायण
इस नगर की सड़कें जितनी गंदी हैं, नगर-निगम का दफ्तर उतना ही शानदार है।
यह नहीं कि ऐसा आज पहली बार लगा हो। यह लगभग रोज़ ही होता है। दफ्तर तिमंज़िला का एक गुलाबी-बिस्कुटी मायालोक है जिसकी सृष्टि दो सौ बीघे के बीचोबीच हुई है। लता–कुजं, उनके पास या बीच से निकलने वाली टेढ़ी-मेढ़ी वीथियाँ, फूलों की विस्तीर्ण क्यारियाँ, नक़ली झीलें आलंकारि वृक्षों की क़तारें, उनके बीच से निकली हुई सीधी-साफ़ सड़कें, मख़मली दूब के मैदान आदि मिलकर आपस में इस ज़मीन का बँटवारा कर चुके हैं। यहाँ आते ही मुझे लगता है कि इस धुआँते-गन्धाते नगर के लिए ऐसा दफ़्तर ग़लत है।
सवेरे जिस सड़क से मैं उस दफ्तर की ओर आता हूँ, उसका बड़ा पौराणिक महत्त्व है। मुझे विश्वास है कि द्वापर में युधिष्ठिर को नरक-दर्शन कराने के लिए इसी सड़क पर लाया गया था। दस बजे तक यह सड़क ट्रक-मोटर-बस-ताँगा-रिक्शा-साइकिल-ठेला-पैदल आदि से खचाखच भर जाती है और इतनी लम्बी-चौड़ी होते हुए भी गलियों से बदतर हो जाती है। सड़क पर पड़े हुए कूड़े के ढेर और पशुओं के सचल दल प्रत्येक यात्री की गति को दुर्गति में बदल देते है। गाय-भैंसों के खुर के नीचे दूधों नहाती-पूतों फलती, गोबर से सनी, मूत से गीली, कूड़े-भरी और कबाड़ से घिरी इस सड़क को छोड़कर जैसे ही मैं नगर-निगम के दफ्तर की चाहरदीवारी के अन्दर आता हूँ, मुझे स्वास्ति का अनुभव होता है-आज भी हुआ। एक क्षण को मेरी साइकिल की किर्र-किर्र सितार पर बजते हुए वृन्दावनी सारंग की मध्य लय हो जाती है। पर हरियाली और स्वच्छता और सम्भ्रान्ति के पहले दर्शन के बाद ही एक झटका लगता है कि य़ह इमारत ग़लत है-वह झटका आज भी लगा। जैसे वृन्दावनी सारंग की गत में किसी घटिया वादक ने गान्धार डाल दिया हो और बड़े आत्मविश्वास से आँखें मटकाकर श्रोताओं के मुँह से वाह-वाह निकवाला चाहता हो, यहाँ आकर कुछ ऐसी ही खीझ मन में पैदा होती है। मेरे लिए यह दफ्तर की इमारत नहीं है, एक वर्जित स्वर है
यदि जीवन-संगीत का रूपक सही है तो इसे वर्जित स्वर मानकर भी मैं अपने संगीत में लगभग रोज़ देखता हूँ और रोज़ प्रयोग करता हूँ। इस इमारत को न देखना चाहकर भी इसे रोज़ देखता हूँ और उकसाता हूँ। जीवन की यह एक ट्रेजेडी है कि हम जिनको नहीं देखना चाहते, उन्हीं को बार-बार देखना पड़ता है और जिन्हें हम बहुत चाहते है, उन्हें देखने को तरसते रह जाते हैं।
फटीचर और ठाठदार दीखने के बीच चालीस पैसे का फर्क़ है। तीस पैसे का ख़र्च करके आज सबेरे मैंने पतलून और बुश्शर्ट पर इस्त्री करायी थी और दस पैसे की जूतों पर पालिश हुई थी। मुझे फटीचर दीखने का डर नहीं था पर यह डर ज़रूर था कि नगर-निगम के बड़े अफ़सर से अगर मैं आज नहीं मिल पाया और कल या परसों मिलना हुआ, तो तब तक इन कपड़ों पर शिकन और जूतों में धूल की झुर्रियां पड़ जायेंगी और तब मैं सुसम्भ्रान्त श्रीनारायण वन्धोपाध्याय न होकर नगर-निगम का असिस्टेंट-भर रह जाऊँगा। चालीस पैसे में पायी गयी स्मार्टनेस खत्म होने के पहले ही मुझे अफ़सर की स्मार्टनेस का मुक़ाबला करने पहुँच जाना चाहिए।
दफ़्तर के पिछवाड़े एक शेड के नीचे असंख्य साइकिलों का मलबा जमा हो चुका है। मैं घड़ी देखता हूँ; साढ़े दस बज रहा है। दफ्तर के लिए आधे घंटे की देर हो गयी है, पर मैं एक घंटे बाद भी पहुँचूँ, तो प्रलय नहीं होगा। मेरा सेक्शन ऑफिसर खुद आजकल साढ़े ग्यारह के बाद आता है क्योंकि सवेरे अस्पताल जाकर कुछ देर उसे अपने बीमार लड़के के पास बैठना पड़ता है; उसके बाद वह एक नर्स के साथ आधा-पौन घंटा अस्पताल की कैंटीन में बिताता है। दफ्तर आते-आते वह जीवन की जटिलता का बड़े वेग से अनुभव करने लगता है और फिर उस अनुभव के सहारे जीवन को ‘कुछ-रोकर, कुछ-गाकर’ झेलने की फिलॉसफी पर मुझे व्याख्यान देता है। कैंटीन में यानी नर्स के साथ बिताये गये क्षणों के बारे में वह व्यथित काव्यमय शब्दों से मुझे कई बार बता चुका है कि वे क्षण उसके जीवन के मरुस्थल में निर्झरिणी की भाँति हैं। मैं उसे बताते-बताते रह जाता है कि हो सकता है कि वे इस मरुस्थल की मृगतृष्णा-भर हों।
पर मैं उसकी प्रौढ़ भावुकता को झटका नहीं देना चाहता। मेरी भावुकता पर, और उसकी भावुकता को समझने की मेरा क्षमता पर उसे अगाध विश्वास है क्योंकि मैं उसका मातहत हूँ, दूसरे जाति से बंगाली हूँ और तीसरे, सितार बजाने वाले एक ललित-कलित कलाकार के रूप में विख्यात हूँ।
साइकिल में ताला डालकर मैं इमारत के उस हिस्से की ओर चला जहाँ हमारा सबसे बड़ा अफ़सर ‘रक्तकरबी’ की यक्षपुरी के राजा की भाँति नेपथ्य में छिपकर बैठता है। पर दस कदम चलते ही हर कदम पर उठने वाली एक शंका दुर्निवार हो गयी। शंका बहुत मामूली, पर बहुत खिजाने वाली थी—यही कि साइकिल में मैंने ताला बन्द किया है या नहीं, मैं जानता था कि मैंने ताला बन्द किया है, पर इस जानकारी पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दफ्तर में मैं लाखों की जोड़-बाकी बिना किसी कैलकुलेटिंग मशीन के निकालता हूँ और अपने अंकों की शुद्धता पर शंका नहीं करता; सितार के तारों पर मैं घंटों कठिन-से-कठिन रागों को उतारता रहता हूँ और एक क्षण के लिए भी उनके स्वरों की शास्त्रीयता पर सन्देह नहीं करता, वही मैं इस डेढ़ रुपल्ली के ताले से हारा हुआ हूँ और कभी निश्चिंत होकर सोच नहीं पाता कि ताला ठीक से लगा हुआ है। तभी होटल के अपने कमरे में ताला लगाकर मुझे लौट-लौटकर आना पड़ता ही और ताले को झटकना पड़ा। वह ठीक से बन्द था।
सिमेंट-कांक्रीट की टेढ़ी-मेढ़ी गली थी जिसके किनारे-किनारे फूलों की क्यारियाँ और घने-घने लता-वितान थे। उस पर चलते हुए मुझे फिर ताले के बारे में उकताहट हुई। पर इस शंका-रूपी नागिन की हिलती पूँछ को मैं हिम्मत से देखता रहा। शंका ही करनी है तो नचिकेता की तरह, श्वेतकेतु की तरह शंका करो, भातखण्डे के संगीत शास्त्र वाले शिष्य की तरह शंका करो, जो कुरेद-कुरेदकर रागों का तत्त्व निकालता है उसे आत्मसात करता है; मैंने अपने-आप से कहा। पर मेरी शंका फटीचर असिस्टेंट एकाउंटेंट की थी, जो सात साल पुरानी साइकिल के लिए विकल हो रहा था। यह जीवन की दूसरी ट्रेजडी है कि हम जैसों के जीवन को, जिनकी ललकार दशों दिशाओं में गूँज रही है, शेर-चीते नहीं, छोटे-छोटे चूहे खाते हैं।
गलियारे के दोनों ओर एकड़ों में नापी जाने वाली लॉन है, जिसके किनारे-किनारे जीनिया के बरसात-झेले और गुलमेहँदी के नय़े फूलों की क्यारियाँ हैं.। दूसरी क्यारियों में जाड़े के फूलों की फसल तैयार होने जा रही है जिसके लिए पिछले साल की भाँति इस साल अफसर की पत्नी को पुष्प-प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिलेगा और तृतीय पुरस्कार उन्हें के एक माली को गुलदस्ता बनाने के विए मिलेगा।
शुरू अक्तूबर की हवा धूप की क्रूरता को घटा रही है फिर भी मेरा कॉलर पसीने से चिपचिपा उठा है। मेरे मन से फिर से फिछले दिन की स्मृतियाँ उभप आयी हैं जिनमें मैं सिनेमाघर के पास खड़ी हुई एक लड़की को देखता हूँ जो निश्चय ही बाजारू है, पर जिसे साहस और पूर्व-अभ्यास की कमी के कारण मैं बुला नहीं पाता; मैं दफ्तर के रजिस्टरों पर झुका हुआ फोन से स्वामी शान्तानन्द की विनम्र वाणी सुनता हूँ, और उनके निमन्त्रण को तुरन्त स्वीकार न करके जवाब में कहता हूँ, ‘‘स्वामी जी अभी क्षमा करें, सोचकर मैं बताऊँगा’, मैं दिल्ली से आये बच्चों के पत्र के बारे में सोचता हूँ जिसका सात दिन से केवल इस कार उत्तर नहीं दिया जा सका कि मैं डाकघर जाकर लिफाफा नहीं खरीद सका, रात को एक युवा कलाकार का वायलिन-वादन सुनकर मैं उसके मुँह पर कहता हूँ, ‘इसमें दम नहीं है।’ पिछले दिन की यादों के साथ मेरी मन लालसा, सन्ताप, पश्चाताप प्रेम आदि से लबालब उठता है और यद्यपि मैंने किसी वेश्या के पर्स में झाँककर कभी नहीं देखा, मैं कहता हूँ कि जिसमें किसी फिल्म-सो के आधे टिकट, लिपिस्टिक के टुकड़े, कमीज के टूटे बटन, चिटों पर लिखे हुए टेलीफोन नम्बर और जन्म-निरोध की गोलियों से लेकर किसी फकीर से पायी भभूत की पुड़िया तक पड़ी हो।
बीते हुए कल के बारे में यह सब सोचता हुआ मैं गली से उतरकर लॉन में आ जाता हूँ और कुछ छायादार पेड़ों का, और ज्यॉमेट्री की इस गधा-साध्य का सहारा लेता हुआ कि-त्रिभुज की दो भूजाएँ मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती हैं, लॉन के दूसरे किनारे तक पहुँच जाता हूँ। इस साध्य के सहारे रास्ते की दूरी सचमुच कम हो गयी, तभी एक पेड़ की नीचे बैठी हुई औरत की गोद में कोई बीमार-सा बच्चा बड़े जोर से चीखा। चारों ओर पत्थर-सा जमी हुई नीरवता के साथ यह विश्वासघात जैसा था। मैं चौंककर ठिठक गया।
चौंकते ही मैं परेशानी में फँस गया-तावे वाले नहीं, एक दूसरी परेशानी कि ऐसे ही अनुभव से, इसी प्रकार के दृश्य से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ, कि यह सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, कि पिछली बार जब मेरे साथ यह सब हुआ था तब कोई उलझाव-सी घटना भी घटी थी ! अन्धविश्वास वाली दुश्चिन्ता के साथ मैंने आँखें मिचमिचायीं और हवा, धूप, हरियाली, औरत, बच्चे, आदि के परिचित संसार में अपने को वापस खींचना चाहा, खींच लिया; ऐसी खुशी हुई, जैसे कोई दुःस्वप्न देखने के पहले ही नींद खुल गयी हो। अफसर के कमरे की वाला जीना मेरे सामने थी। मेहतरों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली थी और उनके प्रतिनिधि बरामदे में खड़े-खड़े बकझक कर रहे थे। हरे पर्दे और बन्द दरवाजों के पीछे बैठा हुआ कोई हाकिम शायद उनके चले जाने की राह देख रहा होगा और वे इस भरोसे से वहाँ खड़े हुए अर्ध-अश्लीलता से अशलीलता की ओर बढ़ रहे थे कि उनका कोई-न-कोई शब्द-बाण हाकिम के कान में जरूर चुभेगा, तब वह नाक-भौं सिकोड़ता हुआ बाहर आएगा और वार्तालाप की गुंजयश निकलेगी। इस भीड़ को तोड़ता और किसी अलक्षित लक्ष्य पर नाक-भौं सिकोड़ता हुआ मैं बरामदे में चलता रहा। मेरे पीछे एक बाबू शू-शू करके, जैसे भेड़ों के झुण्ड को सड़क पार कराना हो, मेहतरों को उस वक्त चले जाने और शाम को पाँच बजे वापस आने की हिदायत देता रहा। मैं बरामदे के उस भाग में पहुँचा जहाँ चूहे नहीं, ऊदबिलाव बैठते हैं
और जिनके ओहदे सहायक, अनु, उद्य, संय्कित, अतिरिक्त आदि विशेषणों से शुरु और एधिकारी की संज्ञा से खत्म होते हैं अपने नाम से ही जो बड़े-बड़े संज्ञावानों को निस्संज्ञ कर देता है। वहाँ कुछ बुर्केदार औरतें, हाथ में कागज लिए, बरामदे के खम्भों से टिकी खड़ी थीं। उन्हें देखकर मुझे बचपन में पढ़ी हुई अलिफ-लैला की एक कथा याद आयी जिसमें बीराने में खड़े हुए पत्थर के बुतों का जिक्र था, जो आसमान से किसी फरिश्ते के उतरने का इंतजार कर रहे थे।
एक मेहतर गीले कपड़ों को हाथ के अभ्यस्त झटके से दायें-बायें घुमाता फ़र्श पोंछने की दैनिक रश्म पूरी कर रहा था। मैंने घड़ी देखी, दस बजकर चालीस हो रहा था। आगे निकलने के लिए मैंने उसे रुकने को कहा, पर उसके रुकते-रुकते उसका गीला कपड़े मेरे जूते को छू गया और जहाँ छुआ, वहाँ पालीस पर एक धब्बा उभर आया।
यह नहीं कि ऐसा आज पहली बार लगा हो। यह लगभग रोज़ ही होता है। दफ्तर तिमंज़िला का एक गुलाबी-बिस्कुटी मायालोक है जिसकी सृष्टि दो सौ बीघे के बीचोबीच हुई है। लता–कुजं, उनके पास या बीच से निकलने वाली टेढ़ी-मेढ़ी वीथियाँ, फूलों की विस्तीर्ण क्यारियाँ, नक़ली झीलें आलंकारि वृक्षों की क़तारें, उनके बीच से निकली हुई सीधी-साफ़ सड़कें, मख़मली दूब के मैदान आदि मिलकर आपस में इस ज़मीन का बँटवारा कर चुके हैं। यहाँ आते ही मुझे लगता है कि इस धुआँते-गन्धाते नगर के लिए ऐसा दफ़्तर ग़लत है।
सवेरे जिस सड़क से मैं उस दफ्तर की ओर आता हूँ, उसका बड़ा पौराणिक महत्त्व है। मुझे विश्वास है कि द्वापर में युधिष्ठिर को नरक-दर्शन कराने के लिए इसी सड़क पर लाया गया था। दस बजे तक यह सड़क ट्रक-मोटर-बस-ताँगा-रिक्शा-साइकिल-ठेला-पैदल आदि से खचाखच भर जाती है और इतनी लम्बी-चौड़ी होते हुए भी गलियों से बदतर हो जाती है। सड़क पर पड़े हुए कूड़े के ढेर और पशुओं के सचल दल प्रत्येक यात्री की गति को दुर्गति में बदल देते है। गाय-भैंसों के खुर के नीचे दूधों नहाती-पूतों फलती, गोबर से सनी, मूत से गीली, कूड़े-भरी और कबाड़ से घिरी इस सड़क को छोड़कर जैसे ही मैं नगर-निगम के दफ्तर की चाहरदीवारी के अन्दर आता हूँ, मुझे स्वास्ति का अनुभव होता है-आज भी हुआ। एक क्षण को मेरी साइकिल की किर्र-किर्र सितार पर बजते हुए वृन्दावनी सारंग की मध्य लय हो जाती है। पर हरियाली और स्वच्छता और सम्भ्रान्ति के पहले दर्शन के बाद ही एक झटका लगता है कि य़ह इमारत ग़लत है-वह झटका आज भी लगा। जैसे वृन्दावनी सारंग की गत में किसी घटिया वादक ने गान्धार डाल दिया हो और बड़े आत्मविश्वास से आँखें मटकाकर श्रोताओं के मुँह से वाह-वाह निकवाला चाहता हो, यहाँ आकर कुछ ऐसी ही खीझ मन में पैदा होती है। मेरे लिए यह दफ्तर की इमारत नहीं है, एक वर्जित स्वर है
यदि जीवन-संगीत का रूपक सही है तो इसे वर्जित स्वर मानकर भी मैं अपने संगीत में लगभग रोज़ देखता हूँ और रोज़ प्रयोग करता हूँ। इस इमारत को न देखना चाहकर भी इसे रोज़ देखता हूँ और उकसाता हूँ। जीवन की यह एक ट्रेजेडी है कि हम जिनको नहीं देखना चाहते, उन्हीं को बार-बार देखना पड़ता है और जिन्हें हम बहुत चाहते है, उन्हें देखने को तरसते रह जाते हैं।
फटीचर और ठाठदार दीखने के बीच चालीस पैसे का फर्क़ है। तीस पैसे का ख़र्च करके आज सबेरे मैंने पतलून और बुश्शर्ट पर इस्त्री करायी थी और दस पैसे की जूतों पर पालिश हुई थी। मुझे फटीचर दीखने का डर नहीं था पर यह डर ज़रूर था कि नगर-निगम के बड़े अफ़सर से अगर मैं आज नहीं मिल पाया और कल या परसों मिलना हुआ, तो तब तक इन कपड़ों पर शिकन और जूतों में धूल की झुर्रियां पड़ जायेंगी और तब मैं सुसम्भ्रान्त श्रीनारायण वन्धोपाध्याय न होकर नगर-निगम का असिस्टेंट-भर रह जाऊँगा। चालीस पैसे में पायी गयी स्मार्टनेस खत्म होने के पहले ही मुझे अफ़सर की स्मार्टनेस का मुक़ाबला करने पहुँच जाना चाहिए।
दफ़्तर के पिछवाड़े एक शेड के नीचे असंख्य साइकिलों का मलबा जमा हो चुका है। मैं घड़ी देखता हूँ; साढ़े दस बज रहा है। दफ्तर के लिए आधे घंटे की देर हो गयी है, पर मैं एक घंटे बाद भी पहुँचूँ, तो प्रलय नहीं होगा। मेरा सेक्शन ऑफिसर खुद आजकल साढ़े ग्यारह के बाद आता है क्योंकि सवेरे अस्पताल जाकर कुछ देर उसे अपने बीमार लड़के के पास बैठना पड़ता है; उसके बाद वह एक नर्स के साथ आधा-पौन घंटा अस्पताल की कैंटीन में बिताता है। दफ्तर आते-आते वह जीवन की जटिलता का बड़े वेग से अनुभव करने लगता है और फिर उस अनुभव के सहारे जीवन को ‘कुछ-रोकर, कुछ-गाकर’ झेलने की फिलॉसफी पर मुझे व्याख्यान देता है। कैंटीन में यानी नर्स के साथ बिताये गये क्षणों के बारे में वह व्यथित काव्यमय शब्दों से मुझे कई बार बता चुका है कि वे क्षण उसके जीवन के मरुस्थल में निर्झरिणी की भाँति हैं। मैं उसे बताते-बताते रह जाता है कि हो सकता है कि वे इस मरुस्थल की मृगतृष्णा-भर हों।
पर मैं उसकी प्रौढ़ भावुकता को झटका नहीं देना चाहता। मेरी भावुकता पर, और उसकी भावुकता को समझने की मेरा क्षमता पर उसे अगाध विश्वास है क्योंकि मैं उसका मातहत हूँ, दूसरे जाति से बंगाली हूँ और तीसरे, सितार बजाने वाले एक ललित-कलित कलाकार के रूप में विख्यात हूँ।
साइकिल में ताला डालकर मैं इमारत के उस हिस्से की ओर चला जहाँ हमारा सबसे बड़ा अफ़सर ‘रक्तकरबी’ की यक्षपुरी के राजा की भाँति नेपथ्य में छिपकर बैठता है। पर दस कदम चलते ही हर कदम पर उठने वाली एक शंका दुर्निवार हो गयी। शंका बहुत मामूली, पर बहुत खिजाने वाली थी—यही कि साइकिल में मैंने ताला बन्द किया है या नहीं, मैं जानता था कि मैंने ताला बन्द किया है, पर इस जानकारी पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दफ्तर में मैं लाखों की जोड़-बाकी बिना किसी कैलकुलेटिंग मशीन के निकालता हूँ और अपने अंकों की शुद्धता पर शंका नहीं करता; सितार के तारों पर मैं घंटों कठिन-से-कठिन रागों को उतारता रहता हूँ और एक क्षण के लिए भी उनके स्वरों की शास्त्रीयता पर सन्देह नहीं करता, वही मैं इस डेढ़ रुपल्ली के ताले से हारा हुआ हूँ और कभी निश्चिंत होकर सोच नहीं पाता कि ताला ठीक से लगा हुआ है। तभी होटल के अपने कमरे में ताला लगाकर मुझे लौट-लौटकर आना पड़ता ही और ताले को झटकना पड़ा। वह ठीक से बन्द था।
सिमेंट-कांक्रीट की टेढ़ी-मेढ़ी गली थी जिसके किनारे-किनारे फूलों की क्यारियाँ और घने-घने लता-वितान थे। उस पर चलते हुए मुझे फिर ताले के बारे में उकताहट हुई। पर इस शंका-रूपी नागिन की हिलती पूँछ को मैं हिम्मत से देखता रहा। शंका ही करनी है तो नचिकेता की तरह, श्वेतकेतु की तरह शंका करो, भातखण्डे के संगीत शास्त्र वाले शिष्य की तरह शंका करो, जो कुरेद-कुरेदकर रागों का तत्त्व निकालता है उसे आत्मसात करता है; मैंने अपने-आप से कहा। पर मेरी शंका फटीचर असिस्टेंट एकाउंटेंट की थी, जो सात साल पुरानी साइकिल के लिए विकल हो रहा था। यह जीवन की दूसरी ट्रेजडी है कि हम जैसों के जीवन को, जिनकी ललकार दशों दिशाओं में गूँज रही है, शेर-चीते नहीं, छोटे-छोटे चूहे खाते हैं।
गलियारे के दोनों ओर एकड़ों में नापी जाने वाली लॉन है, जिसके किनारे-किनारे जीनिया के बरसात-झेले और गुलमेहँदी के नय़े फूलों की क्यारियाँ हैं.। दूसरी क्यारियों में जाड़े के फूलों की फसल तैयार होने जा रही है जिसके लिए पिछले साल की भाँति इस साल अफसर की पत्नी को पुष्प-प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिलेगा और तृतीय पुरस्कार उन्हें के एक माली को गुलदस्ता बनाने के विए मिलेगा।
शुरू अक्तूबर की हवा धूप की क्रूरता को घटा रही है फिर भी मेरा कॉलर पसीने से चिपचिपा उठा है। मेरे मन से फिर से फिछले दिन की स्मृतियाँ उभप आयी हैं जिनमें मैं सिनेमाघर के पास खड़ी हुई एक लड़की को देखता हूँ जो निश्चय ही बाजारू है, पर जिसे साहस और पूर्व-अभ्यास की कमी के कारण मैं बुला नहीं पाता; मैं दफ्तर के रजिस्टरों पर झुका हुआ फोन से स्वामी शान्तानन्द की विनम्र वाणी सुनता हूँ, और उनके निमन्त्रण को तुरन्त स्वीकार न करके जवाब में कहता हूँ, ‘‘स्वामी जी अभी क्षमा करें, सोचकर मैं बताऊँगा’, मैं दिल्ली से आये बच्चों के पत्र के बारे में सोचता हूँ जिसका सात दिन से केवल इस कार उत्तर नहीं दिया जा सका कि मैं डाकघर जाकर लिफाफा नहीं खरीद सका, रात को एक युवा कलाकार का वायलिन-वादन सुनकर मैं उसके मुँह पर कहता हूँ, ‘इसमें दम नहीं है।’ पिछले दिन की यादों के साथ मेरी मन लालसा, सन्ताप, पश्चाताप प्रेम आदि से लबालब उठता है और यद्यपि मैंने किसी वेश्या के पर्स में झाँककर कभी नहीं देखा, मैं कहता हूँ कि जिसमें किसी फिल्म-सो के आधे टिकट, लिपिस्टिक के टुकड़े, कमीज के टूटे बटन, चिटों पर लिखे हुए टेलीफोन नम्बर और जन्म-निरोध की गोलियों से लेकर किसी फकीर से पायी भभूत की पुड़िया तक पड़ी हो।
बीते हुए कल के बारे में यह सब सोचता हुआ मैं गली से उतरकर लॉन में आ जाता हूँ और कुछ छायादार पेड़ों का, और ज्यॉमेट्री की इस गधा-साध्य का सहारा लेता हुआ कि-त्रिभुज की दो भूजाएँ मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती हैं, लॉन के दूसरे किनारे तक पहुँच जाता हूँ। इस साध्य के सहारे रास्ते की दूरी सचमुच कम हो गयी, तभी एक पेड़ की नीचे बैठी हुई औरत की गोद में कोई बीमार-सा बच्चा बड़े जोर से चीखा। चारों ओर पत्थर-सा जमी हुई नीरवता के साथ यह विश्वासघात जैसा था। मैं चौंककर ठिठक गया।
चौंकते ही मैं परेशानी में फँस गया-तावे वाले नहीं, एक दूसरी परेशानी कि ऐसे ही अनुभव से, इसी प्रकार के दृश्य से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ, कि यह सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, कि पिछली बार जब मेरे साथ यह सब हुआ था तब कोई उलझाव-सी घटना भी घटी थी ! अन्धविश्वास वाली दुश्चिन्ता के साथ मैंने आँखें मिचमिचायीं और हवा, धूप, हरियाली, औरत, बच्चे, आदि के परिचित संसार में अपने को वापस खींचना चाहा, खींच लिया; ऐसी खुशी हुई, जैसे कोई दुःस्वप्न देखने के पहले ही नींद खुल गयी हो। अफसर के कमरे की वाला जीना मेरे सामने थी। मेहतरों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली थी और उनके प्रतिनिधि बरामदे में खड़े-खड़े बकझक कर रहे थे। हरे पर्दे और बन्द दरवाजों के पीछे बैठा हुआ कोई हाकिम शायद उनके चले जाने की राह देख रहा होगा और वे इस भरोसे से वहाँ खड़े हुए अर्ध-अश्लीलता से अशलीलता की ओर बढ़ रहे थे कि उनका कोई-न-कोई शब्द-बाण हाकिम के कान में जरूर चुभेगा, तब वह नाक-भौं सिकोड़ता हुआ बाहर आएगा और वार्तालाप की गुंजयश निकलेगी। इस भीड़ को तोड़ता और किसी अलक्षित लक्ष्य पर नाक-भौं सिकोड़ता हुआ मैं बरामदे में चलता रहा। मेरे पीछे एक बाबू शू-शू करके, जैसे भेड़ों के झुण्ड को सड़क पार कराना हो, मेहतरों को उस वक्त चले जाने और शाम को पाँच बजे वापस आने की हिदायत देता रहा। मैं बरामदे के उस भाग में पहुँचा जहाँ चूहे नहीं, ऊदबिलाव बैठते हैं
और जिनके ओहदे सहायक, अनु, उद्य, संय्कित, अतिरिक्त आदि विशेषणों से शुरु और एधिकारी की संज्ञा से खत्म होते हैं अपने नाम से ही जो बड़े-बड़े संज्ञावानों को निस्संज्ञ कर देता है। वहाँ कुछ बुर्केदार औरतें, हाथ में कागज लिए, बरामदे के खम्भों से टिकी खड़ी थीं। उन्हें देखकर मुझे बचपन में पढ़ी हुई अलिफ-लैला की एक कथा याद आयी जिसमें बीराने में खड़े हुए पत्थर के बुतों का जिक्र था, जो आसमान से किसी फरिश्ते के उतरने का इंतजार कर रहे थे।
एक मेहतर गीले कपड़ों को हाथ के अभ्यस्त झटके से दायें-बायें घुमाता फ़र्श पोंछने की दैनिक रश्म पूरी कर रहा था। मैंने घड़ी देखी, दस बजकर चालीस हो रहा था। आगे निकलने के लिए मैंने उसे रुकने को कहा, पर उसके रुकते-रुकते उसका गीला कपड़े मेरे जूते को छू गया और जहाँ छुआ, वहाँ पालीस पर एक धब्बा उभर आया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book