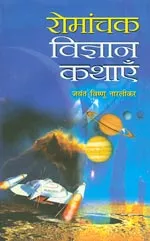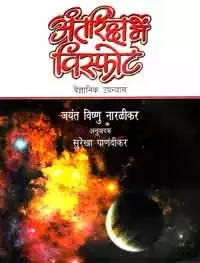|
कहानी संग्रह >> रोमांचक विज्ञान कथाएँ रोमांचक विज्ञान कथाएँजयंत विष्णु नारलीकर
|
48 पाठक हैं |
||||||
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक श्री जयंत विष्णु नारलीकर द्वारा लिखित ये विज्ञान कथाएँ रहस्य, रोमांच एवं अदभुत कल्पनाशीलता से भरी हुई है...
"तुम ठीक तो हो?" उसने पूछा।
'तुम कौन शैतान हो?" मैंने आपे से बाहर होते हुए पूछा। पहले अपनी कमजोरी
प्रकट करने की चिढ़ मेरे मन में थी और मैं उससे उबरना चाहता था।
"मैं अजीत ही हूँ और कोई नहीं। सिर्फ मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ।" फिर अजीत ने
मेरा दायाँ हाथ उठाया और अपनी छाती पर रख दिया। उसका दिल भी दाईं ओर धड़क रहा
था।
एक अजीबो-गरीब, पर आपस में जुड़ी हुई तसवीर मेरे मन में बनने लगी। मैंने अजीत
को आईने के सामने खड़ा कर दिया और फिर मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया, जिसने
मुझे अजीत के आने के बाद शाम से ही परेशान कर रखा था। बहुत मामूली रूप से ही
सही, पर वह कुछ अलग लग रहा था। अब आईने के भीतर से झाँकती उसकी छाया मुझे उस
जीते-जागते शक से कहीं ज्यादा जानी-पहचानी लग रही थी, जिसे मैंने कंधे से
पकड़ रखा था। तो क्या अजीत ने किसी तरह अपने आपको शीशे में दिखनेवाली छाया
में बदल डाला था? ठीक उसी वक्त मुझे खब्बू प्रमोद की कहर बरपानेवाली गेंदबाजी
याद आ गई। क्या वह असली प्रमोद था या उसकी छाया थी? शर्तिया वह कोई भ्रम या
छलावा नहीं था, क्योंकि उसके खेल को केवल मैंने ही अकेले नहीं देखा था बल्कि
हजारों लोगों के साथ-साथ टी.वी. कैमरों ने भी उसके खेल को कैद किया था। तो
क्या गणेशजी की मूर्ति भी असली मूर्ति की छाया थी? मैंने मेज पर रखी मूर्ति
को दोबारा और अच्छी तरह से देखा। यह भी उतनी ही ठोस और असली थी जितना कि मेरे
सामने खड़ा दाँत निकालकर हँसता हुआ अजीत।
"तुम्हें इस तरह परेशान करने पर मुझे अफसोस है। लेकिन मैंने जो शानदार खोज की
है, उसका यकीन दिलाने का कोई और तरीका नहीं था। किताबों में दिए गए
सिद्धांतों के साथ ही मैं अपनी कथा शुरू करूँगा। शुरू-शुरू में..'
'अपनी कथा चलाने से पहले भगवान् के लिए मुझे एक बात बताओ। क्या मेरा यह खयाल
ठीक है कि प्रमोद की रहस्यमय गेंदबाजी के पीछे तुम्हारा ही हाथ था?"
'सचमुच!" अजीत ने कहा।
उसके बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई, वह मैं यथासंभव उसी के शब्दों में बयान
करता हूँ-
"तुम्हें याद होगा कि करीब पाँच साल पहले कैंब्रिज में पढ़ाई पूरी करने के
बाद मैं एक सरकारी प्रयोगशाला में आधिकारिक रूप से अनुसंधान कार्य करने लगा
था। मुझे मौलिक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल होने के साथ-साथ
काम करने का ताजा जोश भी था। पर जल्द ही मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि
मुझे पता लगा कि प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्य न होकर कागजी काम, चापलूसी और
तिकड़मबाजी पर ज्यादा जोर रहता था।
मोहभंग होने के साथ-साथ मैं अपने सहकर्मियों से कटने लगा था, जो कि केवल
गप्पबाजी में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। मुझे जो काम दिया जाता, मैं उसे तुरंत
ही निपटा दिया करता, क्योंकि इस तरह का काम काफी कम होता था, इसलिए मुझे अपनी
सोच और अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा अतिरिक्त समय मिलने लगा
था। मेरे अंतर्मुखी स्वभाव को जानकर सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी
मुझे अकेला छोड़ दिया।
'लंबे समय से एक अजीबो-गरीब विचार ने मेरे मन में उथल-पुथल मचा रखी थी।
कैंब्रिज में आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत का अध्ययन करने के
पश्चात् यह विचार मेरे मन में बैठ गया था।
'चूँकि तुम इस सिद्धांत से अपरिचित हो, इसलिए तुम्हें पहले इसके कुछ खास
पहलुओं के बारे में बता दूँ, जो मेरे काम के थे।
"आइंस्टीन ने इस विचार का प्रतिपादन किया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण
अंतरिक्ष और समय की ज्यामिति या आयामों में परिवर्तन आ जाता है। हम सभी
यूक्लिड की ज्यामिति से परिचित हैं, जो हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों को बखूबी
पूरा करती है। लेकिन करीब डेढ़ सदी पहले गणितज्ञों ने सोचना शुरू कर दिया था
कि तार्किक तौर पर केवल यूक्लिड की ज्यामिति ही स्थिर नहीं है। यूक्लिड के
सिद्धांतों से अलग नियमों पर आधारित गैर-यूक्लिड ज्यामितियों की कल्पना भी की
जा सकती थी। लेकिन आइंस्टीन ही वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन् 1915 में
उन अमूर्त, निराकार विचारों को भौतिक सिद्धांत में ढाला। उनका तर्क था कि
भारी गुरुत्वाकर्षणवाले पिंडों के इर्द-गिर्द गैर-यूक्लिड ज्यामितियाँ होती
हैं और उन्होंने इनका वर्णन करने के लिए समीकरण भी दिए। उनके द्वारा की गई
कुछ भविष्यवाणियों को पिछली सदी के उत्तरार्द्ध में जाँचा-परखा भी गया था,
जिसमें वे सही साबित हुई थीं।
उदाहरण के लिए, प्रकाश की किरणों को ही लें, जिनके बारे में माना जाता है कि
ये सीधी रेखा में ही चलेंगी। अब अलग-अलग ज्यामितियों में सीधी रेखा की
परिभाषा और कसौटी अलग होगी। सूर्य के निकट इसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के
कारण ज्यामिति इस हद तक परिवर्तित हो जाएगी कि सौर-भुजा के पास से गुजरनेवाली
प्रकाश-किरण का पथ उस स्थिति से भिन्न होगा जब वह सूर्य की अनुपस्थिति में
गुजरती है। ये परिवर्तन हालाँकि बहुत सूक्ष्म थे, लेकिन उनका मापन किया गया
और इस तरह सापेक्षतावाद के समान सिद्धांत की भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई।
"सापेक्षतावाद के शब्दों में हम कहते हैं कि अंतरिक्ष काल की ज्यामिति वक्रीय
होती है, जबकि गुरुत्व बल की उपस्थिति में यह सरल होती है। किसी गोले की सतह
पर चलनेवाला द्विआयामी जीव सतह की वक्रता के प्रति सचेत होता है। ऐसी ही किसी
वक्रता की बेहद ऊँचे आयामों में कल्पना करें ऐसी कल्पना मानसिक स्तर पर कठिन
है, लेकिन गणित के लिए आसान है। "अब मैं तसवीर में एक और धारणा को ले आऊँगा।
यह है मोड़ या ट्विस्ट की अवधारणा। क्या आपने मॉनियस स्ट्रिप के बारे में
सुना है ? अगर आप कमर में पेटी बाँधते हैं तो इसे एक मोड़ देकर आप मॉनियस
स्ट्रिप बना सकते हैं। इसकी कई खूबियाँ होती हैं, जैसे-मूल पेटी, जिसकी दो
सतहें थीं, के विपरीत इसकी केवल एक सतह ही होती है। अगर आप किसी साधारण पेटी
या पट्टी को लंबाई के साथ-साथ बीच से काटें तो दो अलग-अलग पट्टियाँ मिलेंगी।
अब मॉनियस पट्टी को इसी तरह काटने की कोशिश करें। आपको केवल आश्चर्य ही
मिलेगा। अब कल्पना करें कि हमारा चपटा जीव इस मॉनियस स्ट्रिप की एक ही सतह पर
रेंग रहा है। कल्पना करें कि उसका केवल एक ही हाथ–बायाँ हाथ है। लेकिन अगर वह
पट्टी का पूरा चक्कर लगा ले तो वह पाएगा कि उसका एक हाथ, जो बायाँ है वह अब
दायाँ हाथ हो गया है! अगर आपको यकीन न हो तो इसे कागज की पट्टी पर आजमाकर
देखें, हमारे जैसे त्रिआयामी अंतरिक्ष की लाभकारी स्थिति से देख रहे प्रेक्षक
के लिए जीव एक अक्ष के चारों ओर आधे घूर्णन से गुजर चुका होता, जो उसके शरीर
में सिर से पैर तक होता। हालाँकि जीव को इसका पता नहीं चलता। उसके लिए तो
उसके सीमित द्विआयामी परिप्रेक्ष्य में यह घटना परावर्तन की तरह ही लगेगी।
|
|||||