|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
जो मिले सुर
विभिन्न संगीतानुष्ठानों में, जिन्हें न जाने कितनी बार सुना है, जिनकी
स्वतःस्फूर्त, आवेदनसमृद्ध गायकी ने, अपने स्वर के वैचित्र्य से रसोत्तीर्ण कर,
न जाने कितनी बार संगीत के आनन्दार्णव में, आकंठ डुबोकर रख दिया है, जिनकी
तारसप्तक में कंठ-प्रक्षेपण की अद्भुत दिव्य दक्षता, सुन-सुनकर भी कभी मन नहीं
भरा, उनका एक सर्वथा नवीन सरल रूप, सम्प्रति एक घरेलू परिवेश में देखने को मिला
तो समझ में आ गया कि इस महान् संगीतकार ने, यह दक्षता कैसे प्राप्त की। उनकी
श्रेष्ठ गायकी के अभिनव्य का मूलधन है-उनकी सहज, सरल निष्ठा। जो व्यक्ति अपनी
प्रतिभा से अनभिज्ञ रहता है, उसी की प्रतिभा, अविकृत हो प्रतिपल निखरकर
बुद्धिदीप्त पुनर्विन्यास से स्वयं अलंकृत होती रहती है। उनकी स्वर-संगीत के
सुचिंतित वैशिष्ट्य का वर्णन करने की न मुझमें योग्यता है, न सामर्थ्य, किन्तु,
इस बार जितना ही उन्हें देखा, लगा, इस अद्भुत कंठ-शिल्प की वयस, भले ही चेहरे
पर छाप छोड़ रही हो, कंठ की वयस यौवन की देहरी पर ही थमककर खड़ी हो गई है और
सदा वहीं चौखटा थामे खड़ी रहेगी।
जीवन में अनेक सुख्यात गायक-गायिकाओं को सुनने-देखने का अवसर विधाता ने प्रदान किया। तब की गायकी और आज की गायकी में निरन्तर घट रहे परिवर्तन को भी लक्ष्य किया है। इसमें दो मत हो ही नहीं सकते कि तब जो धैर्य और स्थैर्य, श्रोताओं और संगीतकारों में था, वह समय की तीव्र गति के साथ पद रखता-रखता, कहीं खो गया है। मुझे वे सुदीर्घ गोष्ठियाँ याद हो आती हैं, जब सारी-सारी रात संगीत की उद्वेलित तरंगों में डूबते-उतराते बीत जाती थी। रामपुर और ओरछा में कैशोर्य बीता। दोनों ही थीं संगीत-प्रेमी रियासतें। प्रायः बेगम अख्तर, कज्जन, राधा रानी, दुलारी, सिद्धेश्वरी, मुनीर जान वहाँ आतीं। मेरे पिता रामपुर नवाब के गृहमन्त्री थे। मेजबानी का प्रबन्ध उन्हें ही सम्हालना पड़ता। अतः जाने-अनजाने संगीत की घुट्टी, स्वयमेव कंठ में उतरती गई। वे भारी-भारी पेशवाज, शुतुरमुर्ग के अंडों-सी मोतियों की मालाएँ, शमातुलम्बर, हिना की मदमस्त खुशबू में डूबे से दुर्लभ राग और रागिनियाँ, फूलों के गजरे, चिक की चिलमन के पीछे मन्त्रमुग्ध होकर सुनता पूरा अन्तःपुर ! मुझे याद है जब ओरछा युवराज राजाबहादुर की सगाई के जल्से में गाने के लिए पधारी सिद्धेश्वरी, मेघ राग गा रही थीं और समा बँध ही रहा था कि कुछ पेशेदार आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने चट गाना रोक दिया। चेहरा तमतमा उठा और उठने को तत्पर होकर गरजीं, “अन्नदाता, पहले सुननेवाले तैयार कर लीजिए, तब सुनानेवालों को बुलाइए!"।
स्वयं महाराज वीरसिंहजू देव ने बड़े मान-मनुहार से उन्हें मनाकर रोका और एक ही गरज में सचमुच सुननेवाले सुनना सीख गए।
आज सौभाग्य से, कलापारखी श्रोताओं का अभाव नहीं है, भले ही बहुत कम श्रोताओं को संगीत का वास्तविक ज्ञान हो, किन्तु भला हो संस्कृति के प्रति हमारी नवीन निष्ठा का, आप किसी भी पाश्चात्य सभ्यता-प्रेमी गृह में जाइए, आपको पंडित भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन मंसूर, गंगूबाई, किशोरी, मालिनी, पंडित जसराज के कैसेट सुनने को मिल ही जाएँगे।
एक बात मैंने और भी देखी है, जैसे पहले राज्याश्रयी हो, संगीत और संगीतकार दोनों लाभान्वित होकर दिन-प्रतिदिन निखरते थे, वैसे ही आज भारत के अनेक समर्थ, समृद्ध व्यक्ति, या अपने गृह में या किसी मंच पर संगीत एवं संगीतकारों को सींचने लगे हैं। यह वास्तव में एक शुभ लक्षण है। यहीं पर स्पिक मैके का योगदान भी उल्लेखनीय है। युवा पीढ़ी इस ओर बड़े उत्साह से जुटी है, किन्तु इसका एक दुर्बल पक्ष भी है। ऐसे आयोजनों के आयोजक, स्वयं अपने अहं को प्रश्रय देने, बड़े-बड़े कलाकारों के कन्धे पर अंतरंगता में हाथ रखने की क्षमता हासिल करने, यदि राजनीति के क्षुद्र मोहरे चलाने का प्रयास करने लगे, तो यह प्रयास निष्फल ही सिद्ध होगा।
स्वयं पण्डित भीमसेनजी ने स्वीकार किया कि स्पिक मैके द्वारा बहुत प्रशंसनीय कार्य हो रहा है, हम संगीत की बारीकियाँ समझें, न समझें, समझने की चेष्टा तो कर रहे हैं। जब एक बार मनुष्य अच्छे भोजन का स्वाद ले लेता है तो कुपथ्य को स्वयं ही अनिच्छा से खिसका देता है। वर्षों पूर्व जो बड़ी पते की बात सिद्धेश्वरीजी ने कही थी, ‘पहले सुननेवाले तैयार कर लीजिए, फिर सुनानेवाले को बुलाइए', स्पिक मैके को यही करना चाहिए-आज कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा, जहाँ गुणी श्रोता, संगीत के वास्तविक जानकार न हों। उनको यथोचित सम्मान देना, ऐसी संस्थाओं का पहला कर्त्तव्य है। पर होता यह है कि ऐसे अवसरों पर उन्हें कभी-कभी आमन्त्रित ही नहीं किया जाता। यदि वे ही वंचित रहें तो समीक्षक ही कहाँ जुटेंगे?
कभी हजारीप्रसादजी ने कहा था कि आज के आलोचक तो पुस्तक बिना पढ़े ही उसकी आलोचना कर बैठते हैं, वह भी ऐसी कि त्रैलोक्य विकम्पित! यही उस दिन पंडितजी भी कहने लगे, “म्यूजिक क्रिटिक तो आज सब बन जाते हैं।"
अतीत के किसी संगीतकार के लिए लिखी गई किसी संगीत-समीक्षा से वे क्षुब्ध थे, “अजी, जब आपने उन्हें कभी सुना ही नहीं तो लिख कैसे सकते हैं?"
“आप तो विदेश जाते रहते हैं। वहाँ के श्रोता क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत को सराह पाते हैं?"
“वहाँ के श्रोता, वास्तविक अर्थों में श्रोता हैं।” पंडितजी बोले, “मैं अभी जापान गया था, जिस धैर्य से श्रोताओं ने दुरूह भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुना और सराहा, वह मेरे लिए एक सुखद अनुभव था...अफगानिस्तान तो खैर भारतीय शास्त्रीय संगीत से अपरिचित नहीं है, किन्तु अमेरिका, जापान एक सर्वथा भिन्न परिवेश, भाषा, संस्कृति के बावजूद भारतीय शास्त्रीय संगीत को सराहना सीख गए हैं, वह वास्तव में एक मधुर अनुभूति रही।"
उस दिन पंडितजी के साथ पूरे दो घंटे बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉ. सुशीला मिश्रा टेप पर उनका साक्षात्कार ले रही थीं, उन्होंने मुझे भी सुअवसर दिया कि चाहूँ तो पंडितजी से कुछ प्रश्न पूछू, पर मैं क्या पूछती? मुझे लगा, ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व पर लेखनी का फोकस व्यर्थ है। ऐसा व्यक्तित्व तो स्वयं ही उठने, बैठने, बोलने, बतियाने में पद-पद पर अपना साक्षात्कार लिपिबद्ध करता जाता है। उस सन्ध्या को उत्तर-दक्षिण गोष्ठी में उनका गायन था। पंडितजी को कुछ राग-रागिनियों की लिस्ट दे दी गई थी। “आजकल क्या गायेंगे आप?” किसी ने पूछा।
“आजकल दिमाग में बिहाग ही घूम रहा है-वही गाऊँ या फिर तिलक कामोद।"
किन्तु, गाया उन्होंने यमन था। फिर जोगिया, भीम पलासी और समापन किया था अपने उस विख्यात मनमोहक भजन से, जो ब्रह्मानन्द का नहीं रहा, पंडित भीमसेन का ही होकर रह गया है- 'जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा।'
मुझे उस दिन उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति जोगिया ही लगी थी-'पिया के मिलन की आस...' उनकी रससिद्ध मुद्राएँ, कभी आकाश को उठी उनकी प्रलम्ब भुजा, कभी कंठ में साकार हो गई विरहिणी की व्यथा...बार-बार ये पंक्तियाँ भी जैसे उस एक पंक्ति में एकाकार हो गई थीं :
जीवन में अनेक सुख्यात गायक-गायिकाओं को सुनने-देखने का अवसर विधाता ने प्रदान किया। तब की गायकी और आज की गायकी में निरन्तर घट रहे परिवर्तन को भी लक्ष्य किया है। इसमें दो मत हो ही नहीं सकते कि तब जो धैर्य और स्थैर्य, श्रोताओं और संगीतकारों में था, वह समय की तीव्र गति के साथ पद रखता-रखता, कहीं खो गया है। मुझे वे सुदीर्घ गोष्ठियाँ याद हो आती हैं, जब सारी-सारी रात संगीत की उद्वेलित तरंगों में डूबते-उतराते बीत जाती थी। रामपुर और ओरछा में कैशोर्य बीता। दोनों ही थीं संगीत-प्रेमी रियासतें। प्रायः बेगम अख्तर, कज्जन, राधा रानी, दुलारी, सिद्धेश्वरी, मुनीर जान वहाँ आतीं। मेरे पिता रामपुर नवाब के गृहमन्त्री थे। मेजबानी का प्रबन्ध उन्हें ही सम्हालना पड़ता। अतः जाने-अनजाने संगीत की घुट्टी, स्वयमेव कंठ में उतरती गई। वे भारी-भारी पेशवाज, शुतुरमुर्ग के अंडों-सी मोतियों की मालाएँ, शमातुलम्बर, हिना की मदमस्त खुशबू में डूबे से दुर्लभ राग और रागिनियाँ, फूलों के गजरे, चिक की चिलमन के पीछे मन्त्रमुग्ध होकर सुनता पूरा अन्तःपुर ! मुझे याद है जब ओरछा युवराज राजाबहादुर की सगाई के जल्से में गाने के लिए पधारी सिद्धेश्वरी, मेघ राग गा रही थीं और समा बँध ही रहा था कि कुछ पेशेदार आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने चट गाना रोक दिया। चेहरा तमतमा उठा और उठने को तत्पर होकर गरजीं, “अन्नदाता, पहले सुननेवाले तैयार कर लीजिए, तब सुनानेवालों को बुलाइए!"।
स्वयं महाराज वीरसिंहजू देव ने बड़े मान-मनुहार से उन्हें मनाकर रोका और एक ही गरज में सचमुच सुननेवाले सुनना सीख गए।
आज सौभाग्य से, कलापारखी श्रोताओं का अभाव नहीं है, भले ही बहुत कम श्रोताओं को संगीत का वास्तविक ज्ञान हो, किन्तु भला हो संस्कृति के प्रति हमारी नवीन निष्ठा का, आप किसी भी पाश्चात्य सभ्यता-प्रेमी गृह में जाइए, आपको पंडित भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन मंसूर, गंगूबाई, किशोरी, मालिनी, पंडित जसराज के कैसेट सुनने को मिल ही जाएँगे।
एक बात मैंने और भी देखी है, जैसे पहले राज्याश्रयी हो, संगीत और संगीतकार दोनों लाभान्वित होकर दिन-प्रतिदिन निखरते थे, वैसे ही आज भारत के अनेक समर्थ, समृद्ध व्यक्ति, या अपने गृह में या किसी मंच पर संगीत एवं संगीतकारों को सींचने लगे हैं। यह वास्तव में एक शुभ लक्षण है। यहीं पर स्पिक मैके का योगदान भी उल्लेखनीय है। युवा पीढ़ी इस ओर बड़े उत्साह से जुटी है, किन्तु इसका एक दुर्बल पक्ष भी है। ऐसे आयोजनों के आयोजक, स्वयं अपने अहं को प्रश्रय देने, बड़े-बड़े कलाकारों के कन्धे पर अंतरंगता में हाथ रखने की क्षमता हासिल करने, यदि राजनीति के क्षुद्र मोहरे चलाने का प्रयास करने लगे, तो यह प्रयास निष्फल ही सिद्ध होगा।
स्वयं पण्डित भीमसेनजी ने स्वीकार किया कि स्पिक मैके द्वारा बहुत प्रशंसनीय कार्य हो रहा है, हम संगीत की बारीकियाँ समझें, न समझें, समझने की चेष्टा तो कर रहे हैं। जब एक बार मनुष्य अच्छे भोजन का स्वाद ले लेता है तो कुपथ्य को स्वयं ही अनिच्छा से खिसका देता है। वर्षों पूर्व जो बड़ी पते की बात सिद्धेश्वरीजी ने कही थी, ‘पहले सुननेवाले तैयार कर लीजिए, फिर सुनानेवाले को बुलाइए', स्पिक मैके को यही करना चाहिए-आज कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा, जहाँ गुणी श्रोता, संगीत के वास्तविक जानकार न हों। उनको यथोचित सम्मान देना, ऐसी संस्थाओं का पहला कर्त्तव्य है। पर होता यह है कि ऐसे अवसरों पर उन्हें कभी-कभी आमन्त्रित ही नहीं किया जाता। यदि वे ही वंचित रहें तो समीक्षक ही कहाँ जुटेंगे?
कभी हजारीप्रसादजी ने कहा था कि आज के आलोचक तो पुस्तक बिना पढ़े ही उसकी आलोचना कर बैठते हैं, वह भी ऐसी कि त्रैलोक्य विकम्पित! यही उस दिन पंडितजी भी कहने लगे, “म्यूजिक क्रिटिक तो आज सब बन जाते हैं।"
अतीत के किसी संगीतकार के लिए लिखी गई किसी संगीत-समीक्षा से वे क्षुब्ध थे, “अजी, जब आपने उन्हें कभी सुना ही नहीं तो लिख कैसे सकते हैं?"
“आप तो विदेश जाते रहते हैं। वहाँ के श्रोता क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत को सराह पाते हैं?"
“वहाँ के श्रोता, वास्तविक अर्थों में श्रोता हैं।” पंडितजी बोले, “मैं अभी जापान गया था, जिस धैर्य से श्रोताओं ने दुरूह भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुना और सराहा, वह मेरे लिए एक सुखद अनुभव था...अफगानिस्तान तो खैर भारतीय शास्त्रीय संगीत से अपरिचित नहीं है, किन्तु अमेरिका, जापान एक सर्वथा भिन्न परिवेश, भाषा, संस्कृति के बावजूद भारतीय शास्त्रीय संगीत को सराहना सीख गए हैं, वह वास्तव में एक मधुर अनुभूति रही।"
उस दिन पंडितजी के साथ पूरे दो घंटे बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉ. सुशीला मिश्रा टेप पर उनका साक्षात्कार ले रही थीं, उन्होंने मुझे भी सुअवसर दिया कि चाहूँ तो पंडितजी से कुछ प्रश्न पूछू, पर मैं क्या पूछती? मुझे लगा, ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व पर लेखनी का फोकस व्यर्थ है। ऐसा व्यक्तित्व तो स्वयं ही उठने, बैठने, बोलने, बतियाने में पद-पद पर अपना साक्षात्कार लिपिबद्ध करता जाता है। उस सन्ध्या को उत्तर-दक्षिण गोष्ठी में उनका गायन था। पंडितजी को कुछ राग-रागिनियों की लिस्ट दे दी गई थी। “आजकल क्या गायेंगे आप?” किसी ने पूछा।
“आजकल दिमाग में बिहाग ही घूम रहा है-वही गाऊँ या फिर तिलक कामोद।"
किन्तु, गाया उन्होंने यमन था। फिर जोगिया, भीम पलासी और समापन किया था अपने उस विख्यात मनमोहक भजन से, जो ब्रह्मानन्द का नहीं रहा, पंडित भीमसेन का ही होकर रह गया है- 'जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा।'
मुझे उस दिन उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति जोगिया ही लगी थी-'पिया के मिलन की आस...' उनकी रससिद्ध मुद्राएँ, कभी आकाश को उठी उनकी प्रलम्ब भुजा, कभी कंठ में साकार हो गई विरहिणी की व्यथा...बार-बार ये पंक्तियाँ भी जैसे उस एक पंक्ति में एकाकार हो गई थीं :
'गाढ़ोत्कंठा गुरुषु दिवसेष्वेषु
गच्छत्सु बालां
जातामन्ये शिशिर मथितां
पद्मिनी वान्यरूपाम्
गच्छत्सु बालां
जातामन्ये शिशिर मथितां
पद्मिनी वान्यरूपाम्
शिशिरमथिता पद्मिनी की महती वेदना, वही उत्कंठा गाढ़ से गाढ़तर होती, उसी
पंक्ति में बार-बार प्रखर हो रही थी-'पिया के मिलन की आस' कभी विधुर, कभी मधुर,
कुछ घंटों पूर्व पंडितजी की ही एक बात याद हो आई-खाँ साहब के गायन की चर्चा हो
रही थी, जब सुशीलाजी ने उनके आवाज बदलने की बात कही तो पंडितजी ने कहा था, “कोई
भी ऐसा गायक नहीं, जो आवाज नहीं बदलता, कभी धीर, कभी स्निग्ध, कभी बुलन्द, कभी
कोमल-यह भी एक कला है।"
कंठ का यही बहुरूपिया कलेवर खाँ साहब में भी था, फैयाज खान में भी। यही चमत्कार पंडितजी के सिद्धकंठ में भी है। तारसप्तक में जहाँ सहस्रों मेघों का गुरुगर्जन है, वहीं भद्रसप्तक में शीतल स्निग्धता :
कंठ का यही बहुरूपिया कलेवर खाँ साहब में भी था, फैयाज खान में भी। यही चमत्कार पंडितजी के सिद्धकंठ में भी है। तारसप्तक में जहाँ सहस्रों मेघों का गुरुगर्जन है, वहीं भद्रसप्तक में शीतल स्निग्धता :
तीरथ तो सब करे
वासना ना मरे
वासना ना मरे
दूसरा जो वैशिष्ट्य मुझे उनके गायन में दृष्टिगत होता है, वह है उनके मंचीय
शिष्टाचार की चरम उपलब्धि। लखनऊ के इसी मंच पर मैंने इस शिष्टाचार का नितान्त
अभाव भी देखा है। परम गुणी, ख्यातिप्राप्त एक संगीतज्ञा के द्वारा, शहर की ही
एक युवा प्रतिभाशाली गायिका को भरी सभा में डपटते देखा तो चित्त खिन्न हुआ था।
यह भी क्या कि खचाखच भरे हाल में श्रोता कान लगाए प्रतीक्षा में बैठे हैं,
किन्तु सुगायिका या सुगायक या सुवादक को मूड बनाने में आवश्यक अबेर हो रही है।
उधर न गंभीर चेहरे पर सामान्य स्मित की रेखा है, न निर्विकार मुद्रा का मेघखण्ड
ही हट रहा है। पुरानी पीढ़ी का यह मंचीय आभिजात्य कोई पंडितजी से सीखे! मंच पर
आते हैं तो स्वयं ही यमन की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। नवीन पीढ़ी में यह
मंचीय शिष्टाचार मैंने तबलावादक जाकिर हुसैन में देखा। तबले पर उनकी अँगुलियाँ
थिरकी और ओठों पर हँसी से पूरा मंच गुलजार हो उठता है।
पंडितजी का गायन चल रहा था, पूरे हाल में सुईपटक सन्नाटा था। उनकी पत्नी वत्सलाजी मेरे पार्श्व में बैठी थीं। मैं बार-बार कनखियों से देख रही थी। उस शान्त, सौम्य चेहरे पर एक सन्तुष्ट स्निग्धता थी। नित्य ही तो वे अपने मर्मज्ञ गायक सहचर की दिगंतव्यापी कीर्ति के ऐसे अनेकानेक पर्व देखती रहती होंगी, कैसा लगता होगा उन्हें? अभिज्ञान शाकुन्तल में एक जगह कहा गया है कि रमणीय वस्तुओं को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर, सुखी जनों में भी एक पर्युत्सुकी भाव अर्थात् व्याकुलता आ जाती है। क्या वही व्याकुलता उस चेहरे को ऐसा स्निग्ध बना रही थी?
वत्सलाजी स्वयं सुगायिका हैं। वास्तविक अर्थ में उनकी सच्ची सहचरी मंच पर पंडितजी के पार्श्व में बैठी रहें या हम दर्शक-श्रोताओं के साथ, कहीं न कहीं उनकी अंतर्निहित अद्वैत भावधारा, निश्चित रूप से पंडितजी के कंठ को सींचती रहती है। इसकी पुष्टि स्वयं पंडितजी उस दिन अपने साक्षात्कार में कर चुके थे।
“वत्सलाजी का आपके जीवन में क्या योगदान रहा?"
पंडितजी का उत्तर, तत्काल तरकस के तीर-सा छूटा था, “देखिए, जीवन में बड़े से बड़ा कलाकार भी कभी-कभी बेसुरा हो उठता है। जब कभी कोई ऐसा क्षण आया है, इन्हीं ने मेरा स्वर सम्हाला है।"
कैसा गूढ सत्य था उनके इस कथन में। सप्तपदी के सात फेरों के श्लोकों में 'सदा सुखदुःखानुगामिनी' ही में एक सफल सहचरी की परिभाषा निहित है, वही परिभाषा वत्सलाजी में साकार हुई। गम्भीर, सौम्य, मृदुभाषिणी, निरन्तर छाया-सी पति के पीछे-पीछे चलती उनका स्वर साधती, वत्सला स्वयं उनका स्वर बन गई हैं। लगता है पंडितजी का निवेदन 'मिले सुर में सुर' उन्हीं के लिए है।
जो मंच पर स्थित होते ही एक ऐसे गंभीर सिद्ध लगने लगते हैं कि छूने में भी भय हो, वही अनौपचारिक गोष्ठी में हैं एक अत्यन्त सरल व्यक्ति। खाने के बाद, मैंने अपने जर्दे की चुटकी ली तो बोले, “लीजिए, यह चखकर देखिए", सरौता तो उनके साथ ही चलता है...तम्बाकू की चुटकी भी चलती रहती है, लेकिन उनका तम्बाकू भी उनके गुरुगम्भीर गायन की भाँति सामान्य हाजमे वाला नहीं पचा सकता! मैंने बढ़कर उनकी दी चुटकी मुँह में भरी, तम्बाकू क्या था पूरे देसी तमंचे का बारूद था। थूकूँ तो कहाँ, कंठ में ही नीलकंठ बन घुटक लिया। घुटका क्या कि ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली-इस ऐटमिक चुटकी के बाद पंडितजी गा कैसे पाते हैं?
“क्यों, कैसा लगा ?" उन्होंने पूछा।
शायद मेरे माथे पर पसीना देख लिया था। मैं किस मुँह से कहती कि, “जो खाएगा, सोई परम पद पाएगा..."
इतना ही जानती हूँ, जिस दिन उस दुर्लभ चुटकी को कंठ में घुटक, सहन करने की क्षमता हासिल कर लूँगी, उसी दिन समढूंगी कि उस दिव्य कंठ को सराहने की कुछ योग्यता तो हासिल कर ही ली है।
पंडितजी का गायन चल रहा था, पूरे हाल में सुईपटक सन्नाटा था। उनकी पत्नी वत्सलाजी मेरे पार्श्व में बैठी थीं। मैं बार-बार कनखियों से देख रही थी। उस शान्त, सौम्य चेहरे पर एक सन्तुष्ट स्निग्धता थी। नित्य ही तो वे अपने मर्मज्ञ गायक सहचर की दिगंतव्यापी कीर्ति के ऐसे अनेकानेक पर्व देखती रहती होंगी, कैसा लगता होगा उन्हें? अभिज्ञान शाकुन्तल में एक जगह कहा गया है कि रमणीय वस्तुओं को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर, सुखी जनों में भी एक पर्युत्सुकी भाव अर्थात् व्याकुलता आ जाती है। क्या वही व्याकुलता उस चेहरे को ऐसा स्निग्ध बना रही थी?
वत्सलाजी स्वयं सुगायिका हैं। वास्तविक अर्थ में उनकी सच्ची सहचरी मंच पर पंडितजी के पार्श्व में बैठी रहें या हम दर्शक-श्रोताओं के साथ, कहीं न कहीं उनकी अंतर्निहित अद्वैत भावधारा, निश्चित रूप से पंडितजी के कंठ को सींचती रहती है। इसकी पुष्टि स्वयं पंडितजी उस दिन अपने साक्षात्कार में कर चुके थे।
“वत्सलाजी का आपके जीवन में क्या योगदान रहा?"
पंडितजी का उत्तर, तत्काल तरकस के तीर-सा छूटा था, “देखिए, जीवन में बड़े से बड़ा कलाकार भी कभी-कभी बेसुरा हो उठता है। जब कभी कोई ऐसा क्षण आया है, इन्हीं ने मेरा स्वर सम्हाला है।"
कैसा गूढ सत्य था उनके इस कथन में। सप्तपदी के सात फेरों के श्लोकों में 'सदा सुखदुःखानुगामिनी' ही में एक सफल सहचरी की परिभाषा निहित है, वही परिभाषा वत्सलाजी में साकार हुई। गम्भीर, सौम्य, मृदुभाषिणी, निरन्तर छाया-सी पति के पीछे-पीछे चलती उनका स्वर साधती, वत्सला स्वयं उनका स्वर बन गई हैं। लगता है पंडितजी का निवेदन 'मिले सुर में सुर' उन्हीं के लिए है।
जो मंच पर स्थित होते ही एक ऐसे गंभीर सिद्ध लगने लगते हैं कि छूने में भी भय हो, वही अनौपचारिक गोष्ठी में हैं एक अत्यन्त सरल व्यक्ति। खाने के बाद, मैंने अपने जर्दे की चुटकी ली तो बोले, “लीजिए, यह चखकर देखिए", सरौता तो उनके साथ ही चलता है...तम्बाकू की चुटकी भी चलती रहती है, लेकिन उनका तम्बाकू भी उनके गुरुगम्भीर गायन की भाँति सामान्य हाजमे वाला नहीं पचा सकता! मैंने बढ़कर उनकी दी चुटकी मुँह में भरी, तम्बाकू क्या था पूरे देसी तमंचे का बारूद था। थूकूँ तो कहाँ, कंठ में ही नीलकंठ बन घुटक लिया। घुटका क्या कि ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली-इस ऐटमिक चुटकी के बाद पंडितजी गा कैसे पाते हैं?
“क्यों, कैसा लगा ?" उन्होंने पूछा।
शायद मेरे माथे पर पसीना देख लिया था। मैं किस मुँह से कहती कि, “जो खाएगा, सोई परम पद पाएगा..."
इतना ही जानती हूँ, जिस दिन उस दुर्लभ चुटकी को कंठ में घुटक, सहन करने की क्षमता हासिल कर लूँगी, उसी दिन समढूंगी कि उस दिव्य कंठ को सराहने की कुछ योग्यता तो हासिल कर ही ली है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book









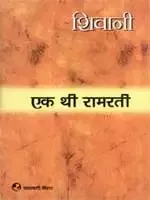


_s.webp)
