|
जीवन कथाएँ >> सुनहु तात यह अकथ कहानी सुनहु तात यह अकथ कहानीशिवानी
|
156 पाठक हैं |
||||||
शिवानी की जिन्दगी पर आधारित संस्मरण...
माँ ने गिने तो पूरे दो हजार थे। एक अजनबी प्रवासी परिवार की ऐसी उदार
सहायता! फिर हमसे उनका परिचय तो केवल दो वर्ष ही का था। एक ओर नितान्त
अपरिचित प्रतिवेशियों की यह अकारण उदारता थी, तो उधर मेरे लखपति चचेरे भाइयों
ने भेजे थे कुल 500 रुपए। वे जिन्हें मेरे पितामह ने पुत्रवत् पाला, जनेऊ
किया, पढ़ाया, मकान बनाकर दिया, आज वे ही माँ को लिख रहे थे, 'तुम तो जानती
हो, हम पर अभी पूरे परिवार का बोझ है, कितनी बेटियाँ ब्याहनी हैं, उस पर
वकालत न चलने से हम सब भाई घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उसी दिन जीवन का
सबसे कठिन सत्य हमको स्वयं कंठस्थ हो गया था कि इस संसार में अक्सर अपने सगे
भी पराए बन जाते हैं और पराए सगे। यह चिट्ठी आने के दूसरे दिन, हमारा बनिया
वेंकटाचलम आया। नोटों की मोटी गड्डी अपनी लुंगी की अंटी से खोल अम्माँ को
थमाकर कहने लगा, "अम्माँ, इस परेदश में तुम कैसे सब करेगा? रखो, जब बेटा
नौकरी करने लगे, तब लौटा देना।"
माँ की आँखों में आँसू आ गए थे। हमारे महीने का सामान, उसी की दुकान से आता था। उस महीने तो पिता की बीमारी के कारण हम उसका हिसाब भी चुकता नहीं कर पाए थे। यह भी सम्भव था कि हम दो-चार दिन में सुदूर पहाड़ स्वदेश लौट जाएँ और फिर कभी लौटकर ही न आएँ? फिर उन दिनों के चार हजार, आज के चालीस हजार होते थे, पर न कोई लिखत, न पढ़त! उस अपढ़ व्यक्ति की कैसी सच्ची संवेदना रही होगी। देखने में यह कदर्य कुत्सित था। रंग काला भुजंग, चौड़ी फैली नाक, पृथुल अधर, लाल-लाल खून टपकाती आँखें, सारे शरीर में काले बीभत्स बाल। दक्षिणी ठसके से बँधी लुंगी की आधी यवनिका उठा, हमें देखते ही वह अपने अन्य ग्राहकों को देखकर अनदेखा कर कहता, “अम्मा वा-वा (आओ-आओ)...!"
पीठ पीछे हम उसे जामवंत कहकर पुकारते, तो माँ हमें डपट देतीं, "इतना भला आदमी है, कभी रुपयों के लिए तकाजा नहीं करता, तुम लोगों के लिए, अपनी पत्नी के हाथ का बना मायसोर पाक भेजता है और तुम उसे जामवंत पुकार, उसकी हँसी उड़ाते हो?"
"तो जामवंत क्या बुरा था, माँ?" मेरे बड़े भाई त्रिभुवन छौंक लगाते तो पड़ोसन गिरिजा बहन मुँह में साड़ी दबाकर हँसने लगती।
मेरे सुदर्शन अग्रज त्रिभुवन पर उनका विशेष स्नेह था। तब उनके घर ही के भीतर उनका मन्दिर स्थित था। चाँदी की झकझकाती देवमूर्ति के सम्मुख निरन्तर जलती दक्षिणी पीतल के पानस में शतमुखी घृतज्योति। बेंगलूरी अगरबत्ती के साथ रिसी-बसी बेले मोतिया के गजरे की सुगन्ध हमारा स्वागत करने देहरी तक चली आती।
एक बार मसखरे त्रिभुवन, जिन्हें हम त्रिभी कहकर पुकारते थे, साड़ी पहन बेला का गजरा लगा किसी पुरानी फिल्मी नायिका का अभिनय कर रहे थे और हम हँसते-हँसते दुहरे हुए जा रहे थे। नक्की स्वर में वे लटके-झटके के साथ हमारे रसोइया देवीदत्तजी के पैरों में लिपट गए, “प्राणनाथ, मैं तो आपकी जन्म-जन्मांतर की दासी हूँ, पद-प्रहार भी करेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगी।"
देवीदत्तजी भी थियेटरी जोश में आ गए, "तब ले खा मेरी लात।" कह उन्होंने कसकर लात क्या मारी कि जलजला आ गया। दोनों हाथों से साड़ी का लंगोट बना क्षण-भर पूर्व की अपनी स्त्रियोचित क्रीड़ा भुला, त्रिभुवन उन्हें मारने भागे। आगे-आगे देवीदत्तजी, पीछे-पीछे त्रिभुवन।
"त्रिभी-त्रिभी, क्या कर रहा है? पड़ोसी क्या कहेंगे?" माँ चीखती रहीं, पर त्रिभी वहाँ थे ही कहाँ ? वे तो शेषाद्रिपुरम् की परिधि लाँघ पूरी लंका नाप चुके थे। वह विचित्र दौड़ देखने, सड़क के दोनों ओर भीड़ जुट गई। थोड़ी देर में हँसती-हँसती गिरिजा बहन आ गईं, "मावशी (वे हमारी माँ को इसी विचित्र सम्बोधन से पुकारती थीं), धन्य भाग हमारे, आज अर्जुन का वृहन्नला रूप भी देख लिया।"
रविवार का हमारे लिए तब विशेष महत्त्व रहता। उस दिन हमारे पिता बड़े-बड़े हंडों में दूध मँगवा औंटाकर केशर, पिश्ता डाल हमारी आइसक्रीम मशीन में भरते, फिर इर्द-गिर्द भरा जाता शोरा, नमक और बर्फ। बारी-बारी से हम सातों भाई-बहन, उस हैंडल को घुमाते। पहले-पहले हैंडल बड़ी आसानी से घूमता, फिर जैसे-जैसे आइसक्रीम जमने लगती, हैंडल घुमाना एक पीड़ादायक प्रक्रिया बन उठती। जैसे ही ढकना खोलकर घोषणा होती 'कि बच्चो, अपनी-अपनी प्लेट ले आओ, आइसक्रीम तैयार है, हम घेरा बाँधकर बैठ जाते। नियमानुसार पहली परिवेशना बड़ी बहन के बच्चों से ही प्रारम्भ होती। वैसा स्वाद और वह मिठास क्या अब कभी नसीब होगी? अतीत के उन सुखद क्षणों की स्मृति, बढ़ती वयस के साथ-साथ और प्रगाढ़ होती चली जाती है, इसी से शायद कहते हैं कि मनुष्य को मौत नहीं, स्मृतियाँ मारती हैं।
कभी-कभी पिता के मित्र मि. हेनरी अपने साथ साउथ परेड के उस आइसक्रीम पॉर्लर में ले जाते, जहाँ सुनहले बालों को झटके से पीछे फेंकती सुन्दरी परिवेशिका गोल-गुलाबी आइसक्रीम के थक्के पर उसी रंग का पारदर्शी बिस्किट खोंस हमें थमा जातीं। साउथ परेड उन दिनों एकदम साहबी इलाका था। आस्ट्रेलियन नारीलोलुप फौजियों की हम नाना कहानियाँ सुनते रहते, फिर भी कभी-कभी पिता के साथ जाते, तो उनका साया हमें निर्भीक बना देता। कभी दिन डूबे लौटते तो चिन्तातुरा माँ, पिता को डपट देतीं, “हद हो गई, मति मारी गई है क्या तुम्हारी? सयानी लड़कियों को लेकर कोई साउथ परेड जाता है? दिन-रात तो पढ़ते रहते हो, फौजी कैसे बौरा गए हैं।"
पिता उन्हें हँसकर टाल देते, “बेंगलूर का कौन फौजी मुझे नहीं जानता?"
आज वही बेंगलूर अचानक आपादमस्तक बदल गया है। न वे फौजी हैं, न उनका उत्पात! इतना बदल गया है कि दूसरी बार बेंगलूर गई, तो लाख भटकने पर भी अपना घर नहीं ढूँढ़ पाई। जहाँ कदम-कदम पर कभी मन्दिर थे, वहाँ अब हैं 'पब'। आधुनिक पब-तीर्थ बन गया है बेंगलूर, आए दिन फैशन शो। बेले के गजरे भी किसी शून्य में विलीन हो गए हैं। लड़कों के-से कटे बालों में भला गजरे लगें भी कैसे। चिकपेट का वह जनसंकुल सँकरा बाजार, जहाँ के विजयलक्ष्मी स्टोर से पचास रुपये में जैसी बाठे की कांजीवरम् साड़ी खरीदी जा सकती थी, वैसी अब शायद पाँच हजार में भी नहीं मिलेगी। दो-दो रुपये में असली जरीदार बॉर्डर के खंड ब्लाउज पीस। आज लगता है, हमने सचमुच ही अन्धेर नगरी का वह अविश्वसनीय परिवेश देखा है, जहाँ गदहा भी पँजीरी खाता था।
हम गरमी की छुट्टियों के बाद, आश्रम लौटते, तो सहपाठिनों की लम्बी लिस्ट अभूतपूर्व तोहफा थीं। महीन ढाकाई मलमली-सी जमीन पर असली जरी की गोल-गोल बूटियाँ, जैसे नक्षत्र-खचित आकाश ही साड़ी पर उतर आया हो। दाम कुल चालीस। हमें सबसे लम्बी लिस्ट थमाती हमारी आत्मीया प्रीति पांडे, जो बाद में किशोर साहू से प्रेम-विवाह कर प्रीति साहू बनी। उन दिनों उसकी किशोर से कोर्टशिप चल रही थी और मुझे लगता है, उस कोर्टशिप पर विवाह की स्थायी मोहर लगाने में हमारी लाई पीतापुरी साड़ियों का विशेष योगदान रहा होगा। प्रीति कट्टर ब्राह्मण परिवार की पुत्री थी, यद्यपि नैनीताल की जर्मन नन्स की शिक्षा ने उसे बचपन से ही निर्भीक, साहसी बना दिया था, फिर भी उन दिनों प्रेम-विवाह की चर्चा भी संस्कारी पर्वत कन्याओं के लिए वर्जित थी, उस पर ब्राह्मण की पुत्री का वैश्य से विवाह ! विवाह हुआ और कुछ वर्षों तक प्रीति मायके से दूर ही रही, किन्तु समाज भी कैसा विचित्र है। पहले तो हो-हल्ला मचाता है, फिर बड़ी सहजता से सामाजिक प्राणी की अबाध्यता को स्वीकार कर लेता है।
|
|||||









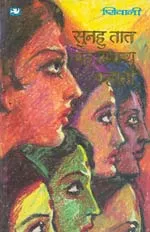


_s.webp)
