|
जीवन कथाएँ >> सुनहु तात यह अकथ कहानी सुनहु तात यह अकथ कहानीशिवानी
|
156 पाठक हैं |
||||||
शिवानी की जिन्दगी पर आधारित संस्मरण...
छह
बेंगलूर में ही एक दक्षिणी बालक हमारा शिष्य बना। वह अपनी बुआ गिरिजा मौसी के यहाँ रहने आया और उन्हीं ने आग्रह किया कि हम कभी-कभी पढ़ा दिया करें। न वह हिन्दी बोल पाता, न अंग्रेज़ी, कभी-कभी हम उसकी नित्य की मनहूस बैठकों से ऊब जाते।
"तू यहाँ रोज-रोज क्यों आता है रे?" मैंने एक दिन पूछ दिया, तो उसके काले चेहरे पर सफेद दाँतों की विद्युतवहिन-सी चमकी।
"बताऊँ?"
"बता ना?" मैंने कुछ खीझकर ही कहा।
"तुम सब लोग इतना सफेद हो ना इसलिए!" बड़े भोलेपन से वह मुस्कराया।
अपने काले रंग की कुंठा ही शायद उसे हमारे यहाँ खींच लाती थी।
राखी बंधवाने तो वह पौ फटते ही ऋषि-मुनियों के-से अडिग धैर्य से हमारे दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाता।
फिर चालीस वर्षों के सुदीर्घ व्यवधान के बीच हम उसे एकदम ही। भूल-बिसर गए थे और जब एक दिन मिला, तो मैं उसे पहचान नहीं पाई।
अपनी लम्बी यात्रा से ऊबी-थकी मैं अपने कूपे में अकेली थी। हाथ में एक ब्रीफकेस लिए वह सामने की बर्थ पर बैठ गया।
उसका चेहरा एक क्षण को पहचाना-सा लगा, पर मैं इतनी थकी थी कि करवट बदलकर सो गई। ऐसी गहरी नींद मुझे कम ही आती है, पर गाड़ी एक झटके के साथ किसी बड़े स्टेशन पर रुकी, तो देखा कूपा खाली है और मेरा सहयात्री उतर चुका है।
सहसा मेरी दृष्टि अपने सूटकेस पर पड़ी, पूरा सूटकेस उथला-पुथला पड़ा था। धड़कते हृदय से मैंने सब सामान टटोला, सब ठीक-ठाक था। मेरे कुलदेवताओं की पोटली, मेरा पासपोर्ट, दो हजार रुपये, जो मैंने बड़े कौशल से साडियों की तह के बीच रखे थे, सब यथास्थान यथावत रखे थे, कैसा विचित्र दस्यु था वह । सहसा डालर, दीनार और देश-विदेश की मुद्राओं से भरे एक वालेट पर नजर गई, साथ में था वह चिरकुट, "बरसों पहले तुमने राखी बाँधी थी, तब पास में कुछ नहीं था, आज दे रहा हूँ।"-तुम्हारा भाई।
अचानक जैसे एक दिन हमारी देहरी पर बिना किसी परिचय के वह धम्म से आकर बैठ गया था, वैसे ही मेरा वह भाई ट्रेन की देहरी फाँद न जाने किस अनाम स्टेशन पर उतर गया। जब बेंगलूर गई थी, तो मन्दिर के पुजारी ने ही बताया था कि गिरिजा मौसी का वह भतीजा अब कुख्यात दस्युराज बन चुका है। उसके सिर पर लाखों का इनाम है, पर अब तक उसे कोई पकड़ नहीं सका। उसका क्षेत्र वायु वेग से भागती विशिष्ट गाड़ियाँ ही रहती हैं। न जाने कितनी हत्याएँ कर चुका है वह आदिम। जैसा भी हृदयहीन, जालिम, जल्लाद हो अपनी काली कलाई पर बँधी राखी की डोर भूला नहीं था।
विधाता कठोर से कठोर हृदय में भी मानवता का सामान्य स्पर्श छोड़ ही देता है। मनुष्य कितना ही पतित क्यों न हो, उसका अन्तःकरण उसे कभी-नकभी झकझोरता अवश्य है। मैंने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है। टीकमगढ़ की जेल में मैं कुख्यात डाकू देशपत से मिली हूँ। कैसा सौजन्य, कैसी विनम्रता! उस सरल व्यक्ति को देखकर कौन कह सकता था कि वह जन्म-कैद भुगत रहा है फिर उसी जेल में बन्दिनी एक पतिहंता मालिन मिली, जिसने मेरे लाख कहने पर भी चेहरे का घूँघट नहीं हटाया। कहने लगी, “यह चेहरा क्या अब आप जैसे भले घर की बहू-बेटियों को दिखा सकती हूँ, बिन्नू?" वे उस युग की अपराधिनें थीं, जिनकी बर्बरता की कहानियाँ नहीं लिखी गईं, जिन पर हुई बर्बरता के बारे में फ़िल्में नहीं बनीं। बनती भी कैसे? अपना अपराध स्वयं स्वीकार करने का अदम्य साहस तो था ही उनमें और था अपने किए दुष्कृत्य पर पश्चात्ताप भी। लखनऊ मॉडल जेल में अनेक घाघ खड़पेंच अपराधियों से मिली, तो भी मेरी यही धारणा पुष्ट हुई कि जघन्य-से-जघन्य अपराधी के हृदय में भी प्रेम, करुणा, दया, अवश्य किसी-न-किसी रूप में छिपी रहती है। वह मनुष्य ही है, जो अन्य मनुष्य को अपराधी बनाता है।
गोमती से संलग्न लखनऊ से एक बीहड़ रास्ता पिपराघाट को जाता है। एक दिन मार्ग भटक मैं उसी रास्ते पर घूमने निकल गई। उस दिन वहीं मुझे कुख्यात डाकू सुखदेव मिला था। एक हाथ की अँगुलियाँ गायब, जो पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने में वह पुलिस की मुठभेड़ में गँवा बैठा था। जीर्ण धोती, पीला पड़ गया कुरता। मैं तो यही सोचती रही कि वह अर्जुनगंज से आ रहा कोई दूधवाला है, पर जब वह स्वयं संरक्षक बन सड़क तक मुझे पहुँचा अपनी सीख देने लगा, तो मैं चौंकी, पर फिर भी नहीं समझी कि वह मुझे अपनी ही कुख्यात बिरादरी के प्रति सतर्क कर रहा है, "बहू जी, ई सड़क बहुत खतरनाक है, अकेली मत निकला करो, फिर सोना पहने हो।"
उसी ने कहा था, "बहुत नीक लिखत हो बहूजी, कभी हमारी जिनगी पर भी कुछ लिख डालो।" मेरा माथा ठनका। उसका अनुरोध पूरा तो किया, किन्तु जब तक मेरी कहानी 'पथ-प्रदर्शक' छपी, वह पुलिस की मुठभेड़ में फँस, अनन्त पथ का पथ-प्रदर्शक बन चुका था। तब ही मुझे पता लगा कि वह और कोई नहीं स्वयं सुखदेव डाकू ही था। डाकू और चोरों के अलावा जीवन में कई बार मैंने तथाकथित पतिताओं में भी, सती-साध्वी का वह सात्विक रूप देखा है, जो दुर्भाग्य से आज प्रतिष्ठित गृहों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। इस युग में आज विवाह, कल विच्छेद होते हैं, या फिर विवाहित जोड़े साथ रहकर भी ऐसे विलंग-बेगाने बन जाते हैं कि पति की मैत्री किसी और के साथ, पत्नी भी परपुरुष के साथ बेरोक-टोक इधर-उधर घूम रही है। पत्नी भटकी तो फिर घर पर निठल्ला छोड़ दिया गया पति क्यों चूके? वह भी अपना प्रबन्ध कर लेता है। दुर्दशा होती है, तो बस बच्चों की। उसी पैबन्द लगी ज़िन्दगी पर भला लेखन कब तक पैबन्द लगाता रहेगा? ऐसे लोगों की व्यथा-कथा की तुलना में इसी से मुझे अपनी उस संगीत गुरु राजुला सावित्री की कथा कालजयी लगी थी, जिसने अपने माथे पर कलंक और हृदय पर पत्थर रख अपने प्रेमी को जीतेजी बदनामी से बचा लिया।
राजुला मुझे पहाड़ी सिखाने आती थी। घर-भर का विरोध स्वीकार करने पर ही मैं उस विलक्षण नारी को गुरु रूप में पा सकी थी। वह एक पेशावर गायिका 'हुड़क्याणी' थी। पहाड़ में प्रायः 'हुड़क' वाद्य लिए एक सहचर भी इन गायिकाओं के साथ चलता है, किन्तु राजुला 'अकेली ही, एक डफली बजा कर गाया करती और कभी किसी से कुछ माँगती नहीं थी। दे दिया, तो ले लिया। उसकी आवाज में पेशावर गायिका की एक विचित्र गूंज थी। भले ही उसकी नाक किसी कुख्यात रोग का शिकार बन बैठ-सी गई हो, किन्तु जवानी में वह इमारत बुलन्द रही होगी, यह कोई देखकर ही कह सकता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book









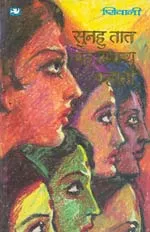


_s.webp)
