|
जीवन कथाएँ >> सुनहु तात यह अकथ कहानी सुनहु तात यह अकथ कहानीशिवानी
|
156 पाठक हैं |
||||||
शिवानी की जिन्दगी पर आधारित संस्मरण...
पहाड़ की होली का तब अपना ही जादू था। आमल की एकादशी से होली की बैठकें
लगतीं। मोट के दन (कालीन), उन पर बिछती दुग्ध-धवल चादरें, सफेद गिलाफ चढ़ा
गावतकिया, उनका सहारा लिए लखनऊ की अम्बरी तम्बाकू की सुगन्धित धूम्र-रेखा से
हुक्के का कश खींचते प्रतिष्ठित व्यक्ति। थोड़ी ही देर में थाल के थाल जम्बू
हुँके आलू और गोझे परिवेशित होते, पीतल के चमचमाते गिलासों में मसाले डली
अदरक की चाय। फिर आरम्भ होती बैठक होली-
अपनों बीरन मोहे दे री ननदिया
मैं होली खेलन जाऊँ वृन्दावन।
या
जाय पइँ पी के अंक
चाहे कलंक लगैरी...
तबले पर संगत करते कुमाऊँ के अल्लारक्खा, दाम दा, हारमोनियम पर पहाड के जलगाँवकर, कांति दा; और रसीले कंठ का माधुर्य बिखेरते वे संगीत रसिक गायक, जिन्होंने न कभी विधिवत संगीत की शिक्षा पाई, न किसी गुरु का गंडा ही बाँधा। स्वयं विधाता ने जिनके कंठ में प्रतिभा को खुंटे की गाय-सा बाँधकर रख दिया था। न कहीं अश्लील प्रलाप, न छींटाकशी; वह मधुर स्वरलहरी, सम पार आती, तो वाह-वाह की साधुध्वनि छज्जे को गुंजायमान करती सड़क तक चली जाती।
राह चलते लोग-ठिठककर खड़े हो जाते, “कौन गा रहा है यह? भवानी शाह या बद्रिया?"
स्त्रियों का प्रवेश उस होली बैठक में निषिद्ध था। उनकी बैठकें अलग ही जमतीं। ठीक होली के दिन हमें घर के दो पुराने नौकरों के साथ, हमारे पितामह अल्मोड़ा के सीमान्त पर बने बड़ी बहन के खाली बँगले में भेज देते। कभी कठोर पितामह के प्रति हमारा अबोध हृदय विद्रोह कर उठता-'भला यह भी कोई बात हुई? घर के लड़कों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं और घर की पुत्रियों को जहाँ चाहा, गाय-सा हाँक दिया। फिर बड़ा होने पर एक बार होली का हुड़दंग देखा तो समझ में आ गया कि पितामह हमें क्यों उस अरण्य में निष्कासित करते थे। बहुत तड़के ही अबीर-गुलाल बिखेरती उन रंगीले होल्यारों की टोली के उस दिन सौ खून माफ रहते। उनके गाने की प्रथम पंक्ति में मौहल्ले की प्रत्येक किशोरी का नाम गुँथा रहता। प्रथम पंक्ति सदा एक ही रहती-
चलो चलो ए दुनिया वालो
दिल्ली में दरबार है।
फिर उस दरबार में गिन-गिनकर उन सबकी काल्पनिक हाजिरी ली जाती, जिन्हें दूर से ही देखकर, उनके मन को कभी विकार की उद्दाम तरंगों ने उद्धेलित किया होगा। यद्यपि अन्य प्रदेशों की तुलना में पहाड़ की होली, तब भी मर्यादामंडित रहती थी, किन्तु एक यही दिन तो है जिस दिन भारतीय मनुष्य का रुग्ण मन, मनचाही कुलाटें ले अपने विकारग्रस्त चित्त को स्वयं तरोताजा कर लेता है। होली का वह भय, अभी भी हमारे मन से नहीं गया। न जाने कब, कौन गाने की विवेकहीन अंतश में हमारा नाम न गूँथ दे!
पहाड़ में उन दिनों सूखी होली का ही चलन था, केवल अबीर-गुलाल से सने चेहरे लेकर ढोलक बजाती टोली हमारे आँगन में अशीष देने आती, तो हम पर लगाया गया कर्फ्यू हटा लिया जाता-
हो हो होलक रे
वो नर जीवै जो खेले फाग,
हो हो होलक रे।
स्वयं हमारी होली की बैठकें भी, कुछ कम रंगीन नहीं होतीं। हमारे पुराने रसोइया पुरुषोत्तम लोहनी हमारे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ही अधिक थे। रसोई में तो अब कभी-कभार ही झाँकते। अपना राज-दंड उन्होंने अपने छोटे भाई देवीदत्तजी को थमा दिया था। बड़े लोहनीजी की पत्नी कभी होली देखने हमारे यहाँ आती, तो हमारी महफिल गुलजार हो जाती। दोनों हाथ जोड़े किसी उद्धत कामी कुटिल गोरे साहब की काल्पनिक मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाती साठ वर्ष की उस वृद्धा की अभिनयकुशलता हमें हँसा-हँसाकर लहालोट कर देती
हाथ जोड़ें गोरा जी
मैं तो बूढ़ी बामणी।
क्या लटके और कैसे-कैसे झटके! घूघट से ढका उस अवगुंठनवती का झुरी पड़ा चेहरा न देखा होता, तो सब यही समझते कि कोई सोलह वर्ष की किशोरी ही थिरक रही है।
आज अंतरतर में छिपी स्मृतियों का बाँध सहसा सहस्र धाराओं में फूट निकला है। उसे रोक पाने में, मैं उसी प्रवाह में तिनके-सा बही जा रही हूँ।
सम्मिलित परिवार में रहकर हमने जो कुछ सीखा, वह आनेवाली पीढ़ी शायद कभी नहीं सीख पाएगी। आज के सीमित परिवार, अपने ही इर्द-गिर्द एक अमिट लक्ष्मण-रेखा खींच उसी में सिमटकर रह गए हैं। उन्हें चिन्ता है तो अपनी और अपने परिवार की। इस भावना ने आज हमें अत्यधिक स्वार्थपरक बना दिया है। शायद यह छूत भी हमें विदेश से ही लगा है। वसुधा अब कुटुम्ब के दायरे में नहीं रह गई है, किन्तु पहले ऐसा नहीं था। मेरी छोटी बहन की सास का ही उदाहरण लूँ, तो वे बड़े दिल की एक उदार महिला थीं। न जाने कितने उनके आश्रय में पले, पढ़-लिखकर योग्य बने, यहाँ तक कि अपने घरेलू नौकर को भी उन्होंने अपने पुत्र के साथ पढ़ाकर बैरिस्टर बना दिया।
"कैसे कर सकीं आप यह?" मैंने एक दिन पूछा तो बोली, "देख, अपने और पराये बच्चों में कभी भेदभाव न करो, तो स्वयं भगवान आकर चूल्हा-चक्की सम्हाल लेता है। मेरे पाँच बेटे, चार बेटियाँ, भानजे-भतीजे, नौकर सबको एक लाइन में बिठाती और एक-एक कटोरा रख देती। बड़ी कड़ाही में दूध उबाल सबकी कटोरी में बराबर-बराबर डालती चली जाती। घर में खाना पका, तो सबके लिए एक-सा, यह नहीं कि अपने बच्चों की दाल में घी डाल दिया औरों के में नहीं। अपने और पराये बच्चों में कभी भेदभाव मत करना, फिर खुद समझ जाएगी कि मैं कैसे यह सब कर सकी।"
तब कहाँ थी डबलरोटी, चीज़, अंडे या मक्खन? या फिर वे लुभावने सीरियल्स। किसी के मनमोहक डिब्बे में सजीला मुर्गा बाँग दे रहा है, किसी में गेहूँ की सनहरी बालें फरफरा रही हैं। बासी रोटी में घी चुपड़, चीनी बुरक रोल बना थमा दिया बच्चों को, उसे पहाड़ में बाल कहा जाता था। उसी क्रीम-रोल को खाकर हम भी बड़े हुए हैं, डबलरोटी का स्वाद तो पहाड़ से बाहर जाने के बाद चखा।
ठीक नौ बजे स्कूल जानेवाले बच्चों की टोली जीमने बैठ जाती। कभीकभी स्कूल का लम्बा फासला तय करते ही फिर भूख लग जाती। घर का खाना प्रायः घर की औरतें ही पकाया करतीं, केवल एक धुली साड़ी पहन, आचमन कर चौके में घुसती और पकाने के बाद ही बाहर निकल सकती थीं। परिवार तो बड़े ही होते थे, इसी से उसी अनुपात में खाना भी बड़े-बड़े भड्डू (भगौने) और कड़ाहों में बनता। उन भारीभरकम बर्तनों को नीचे उतारना स्त्रियों के लिए सम्भव नहीं होता, इसी से परिवेशन करते घर के पुरुष या फिर समृद्ध घरों में रसोइया। दाल, चावल, सब्जी से ही काम नहीं चल सकता था, इसी से बड़े परिवारों को ध्यान में रख एक टपकिया अवश्य बनता, या लाई पालक का, पिसे चावल का लगाव देकर बनाया गया, "काफा', या फिर घुइया के पत्रों में पिसी कुल्थे की दाल मिला ‘पंपटौल।' दाडिम की चटनी भी रहती ही, क्योंकि पहाड़ की जलवायु में अचार डाले भी जाते, तो फफूंद लग जाती।
|
|||||









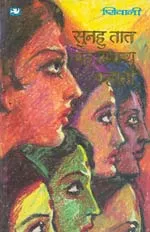


_s.webp)
