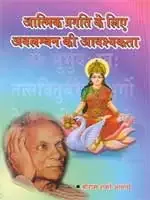|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकता आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकताश्रीराम शर्मा आचार्य
|
13 पाठक हैं |
||||||
आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की क्या आवश्यकता है
इष्ट निर्धारण-प्रगति क्रम का सुनिश्चित आधार-पथ निश्चित करना है। ईश्वरीय सत्ता का मनुष्य में अवतरण 'उत्कृष्टता' के रूप में होता है। चिन्तन और चरित्र में उच्च-स्तरीय उमंगें उठने लगती हैं तथा उसी स्तर की गतिविधियाँ चल पड़ती हैं। उत्कृष्टता की उपासना ही ईश्वर उपासना है। यही उपास्य है। लक्ष्य भी इसी को बनाना पड़ता है। इष्टदेव का निर्धारण किस रूप में किया जाय, आज इस संदर्भ में अनेकों विकल्पों के जंजाल बने खड़े हैं। प्राचीनकाल में ऐसा न था। तत्वज्ञानी एक निश्चय पर पहुँचे थे और उन्होंने समस्त साधकों को वही निष्कर्ष अपनाने का परामर्श दिया था। भारतीय संस्कृति जिसे वस्तुः: विश्व संस्कृति कहा जाना चाहिए-साधना के संदर्भ में एक ही निश्चय पर पहुँची है कि आत्मिक प्रगति की साधना के लिए इष्ट रूप में गायत्री का ही वरण, होना चाहिए।
गायत्री को इष्ट मानने की अनादि परम्परा है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने कमल पुष्प पर बैठकर आकाशवाणी द्वारा निर्देशित गायत्री उपासना की थी और सूजन की सामथ्र्य प्राप्त की थी। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। त्रिदेवों की उपास्य गायत्री रही है। देव गुरु बृहस्पति ने-दक्षिण मार्गी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने-वाम मार्गी साधनायें गायत्री के ही आत्मिक और भौतिक पक्षों को लेकर प्रचलित की-थी। सप्तऋषि, गायत्री की सप्त व्याहतियों के प्रतीक माने जाते हैं। राम-कृष्ण आदि अवतारों की इष्ट गायत्री रही है। इसी महामंत्र की व्याख्या में चारों वेद तथा अन्यान्य धर्मशास्त्र रचे गये हैं। दत्तात्रेय के चौबीस गुरु गायत्री के चौबीस अक्षर ही हैं। चौबीस योग, चौबीस तप प्रसिद्ध हैं। यह सभी गायत्री के तत्वज्ञान और साधना-विधान का विस्तार है। गायत्री गुरुमंत्र है। दीक्षा में उसी को माध्यम बनाया जाता है। हिन्दू धर्म के दो प्रतीक हैं-शिखा और सूत्र। दोनों ही गायत्री के प्रतीक हैं। गायत्री का ज्ञान पक्ष मस्तिष्क पर शिखा के रूप में और कर्म पक्ष कन्धे पर यज्ञोपवीत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। परम्परागत उपासना-विधि संध्या है। संध्या में गायत्री का समावेश अनिवार्य है। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि गायत्री अनादि धर्म परम्परा एवं अध्यात्म परम्परा का आधार भूत तथ्य है। उपासना में उसी का प्रयोग सर्वोत्तम है।
तत्त्वदर्शन की दृष्टि से गायत्री 'ऋतम्भरा प्रज्ञा' है। ऋतम्भरा अर्थात् विवेक संगत श्रद्धा। प्रज्ञा अर्थात् श्रेय साधक दूरदर्शिता। इस समग्र विवेकशीलता को गायत्री कह सकते हैं। इस बीज मंत्र का विशाल वृक्ष ब्रह्मविद्या है ! अध्यात्म का यह दार्शनिक पक्ष है। साधना प्रयोजन में इसी के विभिन्न उपचार योगाभ्यासों, तप साधनों एवं धर्मानुष्ठानों के रूप में प्रचलित हैं। इष्ट का-लक्ष्य का-उपास्य का निर्धारण, दिव्यदर्शियों ने गायत्री के रूप में गहन अध्यवसाय और अनवरत अनुभव-अध्यास, के आधार पर किया है। वह प्राचीनकाल की ही तरह अपनी उपयोगिता यथावत् अक्षुण्ण रखे हुए है।
|
|||||
- श्रद्धा का आरोपण - गुरू तत्त्व का वरण
- समर्थ बनना हो, तो समर्थों का आश्रय लें
- इष्टदेव का निर्धारण
- दीक्षा की प्रक्रिया और व्यवस्था
- देने की क्षमता और लेने की पात्रता
- तथ्य समझने के उपरान्त ही गुरुदीक्षा की बात सोचें
- गायत्री उपासना का संक्षिप्त विधान