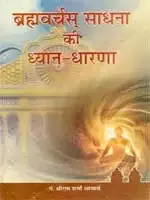|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> ब्रह्मवर्चस् साधना की ध्यान-धारणा ब्रह्मवर्चस् साधना की ध्यान-धारणाश्रीराम शर्मा आचार्य
|
127 पाठक हैं |
||||||
ब्रह्मवर्चस् की ध्यान धारणा....
पंचमुखी गायत्री की उच्चस्तरीय साधना का स्वरूप
गायत्री-शक्ति और गायत्री-विद्या को भारतीय धर्म में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उसे वेदमाता-भारतीय धर्म और संस्कृति की जननी-उद्गम गंगोत्री कहा गया है। इस चौबीस अक्षर के छोटे से मंत्र के तीन चरण है। ॐ एवं तीन व्याहृतियों वाला चौथा चरण है। इन चारों चरणों का व्याख्यान चार वेदों में हुआ है। वेद भारतीय तत्त्वज्ञान और धर्म-अध्यात्म के मूल है। गायत्री उपासना की भी इतनी ही व्यापक एवं विस्तृत परिधि है।
गायत्री माता के आलंकारिक चित्रों, प्रतिमाओं में एक मुख-दो भुजाओं का चित्रण है। कमंडलु और पुस्तक हाथ में है। इसका तात्पर्य इस महाशक्ति को मानवता की-उत्कृष्ट आध्यात्मिकता की प्रतिमा बनाकर उसे मानवी आराध्य के रूप में प्रस्तुत करना है। इसकी उपासना के दो आधार है- ज्ञान और कर्म। पुस्तक से ज्ञान का और कंमडलु जल से कर्म का उद्बोधन कराया गया है। यही वेदमाता है। उसी को विश्व-माता की संज्ञा दी गई है। सर्वजनीन और सर्वप्रथम इसी उपास्य को मान्यता दी गई है।
उच्चस्तरीय साधना में इस प्रतीक-प्रतिमा का रूप यत्किचित बदल जाता है। यह पंचमुखी है। योगाराधन में यही उपास्य है। पाँच मुख और दस भुजा वाली प्रतिमा में कई संकेत हैं। दस भुजाएँ, दस इंद्रियों की सूक्ष्म-शक्ति का संकेत करती है और बताती है कि उनकी संग्रहीत एवं दिव्य सामर्थ्य गायत्री माता की समर्थ भुजाओं के समतुल्य है। दस दिशाओं में उसकी व्यापकता भरी हुई है। दस दिग्पाल-दस दिग्राज पृथ्वी का संरक्षण करते माने गए हैं। गायत्री की दस भुजाएँ ही दस दिगपाल हैं। उनमें धारण किए हुए विविध आयुधों ये यह पता चलता है कि वह सामर्थ्य कितने प्रकार की धाराएँ प्रवाहित करती एवं कितने क्षेत्रों को प्रभावित करती है।
उच्चस्तरीय साधना में पंचमुखी गायत्री प्रतिमा में पंचकोशी गायत्री उपासना की आवश्यकता का संकेत है। ये पाँचकोश अंतर्जगत् के पाँच देव, पाँच प्राण, पाँच महान सद्गुण, पंचाग्नि, पंचतत्त्व, आत्मसत्ता के पाँच कलेवर आदि कहे जाते हैं। पंचदेवों की साधना से उन्हें जागृत-सिद्ध कर लेने से जीवन में अनेकानेक संपत्तियों और विभूतियों के अवतरण का रहस्योद्घाटन किया गया है। पाँच प्राणों को चेतना की पाँच धाराएँ, चिंतन की प्रखरताएँ कहा गया है। चेतना की उत्कृष्टता इन्हीं के आधार पर बढती और प्रचंड होती है। प्राण विद्या भी गायत्री विद्या का ही एक अंग है। गायत्री शब्द का अर्थ भी गय=प्राण+त्रीत्राता। अर्थात् प्राण शक्ति का परित्राण करने वाली दिव्य-क्षमता के रूप में किया गया है। कठोपनिषद में पंचाग्नि विद्या के रूप में इस प्राण तत्त्व को इन्हीं पाँच धाराओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
गायत्री के पाँच मुखों, पंचकोशों के रूप में उन पाँच तत्त्वों की प्रखरता का वर्णन है, जिनसे यह समस्त विश्व और मानव शरीर बना है। स्थूल रूप में यह पाँच तत्त्व पैरों तले रौंदी जाने वाली मिट्टी, कपड़े धोने के लिए काम आने वाली पानी, चूल्हे में जलने वाली आग, पोला आकाश और उसमें मारी-मारी फिरने वाली हवा के रूप में देखे जाते हैं, पर यदि उनकी सूक्ष्म क्षमता पर गहराई से दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि इन तत्त्वों के नगण्य से परमाणु तक कितनी अद्भुत शक्ति अपने में धारण किए बैठे हैं। उनकी रासायनिक एवं ऊर्जागत क्षमता कितनी महान है। पंच तत्त्वों से बना यह स्थूल जगत् और उनकी तन्मात्राओं से बना सूक्ष्म जगत् कितना
अद्भुत, कितना रहस्यमय है, यह समझाने का प्रयत्न किया जाता है तो बुद्धि थक कर उसे विराट् ब्रह्म की साकार प्रतिमा मानकर ही संतोष करती है। इन पाँच तत्त्वों के अद्भुत रहस्यों का संकेत गायत्री के पाँच मुखों में बताया गया है और समझाया गया है कि यदि इनका ठीक प्रकार उपयोग, परिष्कार किया जा सके तो उनका प्रतिफल प्रत्यक्ष पाँच देवों की उपासना जैसा हो सकता है। पृथ्वी, अग्नि, वरुण, मरुत, अनंत इन पाँच देवताओं को पौराणिक कथा-प्रसंग में उच्चस्तरीय क्षमता संपन्न बताया गया है। कुंती ने इन्हीं पाँच देवताओं की आराधना करके पाँच देवोपम पुत्ररत्न पाए थे। पंचमुखी, पंचकोशी उच्चस्तरीय उपासना में तत्त्व-दर्शन की-तत्त्व साधना की गरिमा का संकेत है।
मानव सत्ता के तीन शरीर है-कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण शरीर में पाँच संवेदनाएँ, सूक्ष्म शरीर में पाँच प्राण चेतनाएँ और स्थूल शरीर में पाँच शक्ति धाराएँ विद्यमान है और उच्चस्तरीय साधना विज्ञान का सहारा लेकर उन्हें उभारे जाने का संकेत एवं निर्देश है।
पाँच देवों में (१) भवानी (२) गणेश (३) ब्रह्मा (४)विष्णु (५)महेश की गणना होती है। इन्हें क्रमश: बलिष्ठता, बुद्धिमत्ता, उपार्जन शक्ति, अभिवर्धन, पराक्रम एवं परिवर्तन की प्रखरता कह सकते हैं। ये पाँच देवता ब्रह्मांडव्यापी ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के रूप में संव्याप्त हैं और सृष्टि संतुलन एवं संचालन में योगदान करते हैं। यही पाँच शक्तियाँ आत्मसत्ता में भी विद्यमान हैं और इस छोटे ब्रह्मांड को सुखी-समुन्नत बनाने का उत्तरदायित्व सँभालते हैं। इन्हें पाँच कोशों में सन्निहित अंतर्जगत् के पाँच देव कहा जा सकता है। पंचकोश साधना की सफलता को उपर्युक्त पाँच देवताओं के द्वास प्राप्त हो सकने वाले अनदान-वरदान के रूप में अनुभव किया जाता है।
कोश खजानों को भी कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है और गर्भ में असीम रत्न-राशि भरी होने की बात सर्वविदित है। जमीन में भी जल, तेल, धातुएँ, रत्न तथा अन्यान्य बहूमूल्य पदार्थ मिलते हैं। यह खजाने खदाई करने पर ही मिलते हैं। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा हुआ धन प्रायः जमीन में गड़ा होता था। उत्तराधिकारी उसे खोदते, निकालते और लाभान्वित होते थे। ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य विभूतियाँ आत्मसत्ता के मर्मस्थलों में छिपी रहती हैं। पंचकोश जागरण की साधना से उस वैभव को-सिद्धि-संपदा को साधक उपलब्ध करते हैं।
आत्मसत्ता के पाँच कलेवरों के रूप में पंचकोशों को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है। शास्त्रकारों ने मानवीसत्ता को पाँच वर्गों में विभक्त किया है। उनके नाम हैं-(१) अन्नमय कोश (२) प्राणमय कोश (३) मनोमय कोश (४) विज्ञानमय कोश (५) आनंदमय कोश।
अन्नमय कोश का अर्थ है-इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश अर्थात् जीवनी शक्ति, मनोमय कोश अर्थात् विचार बुद्धि, विज्ञानमय कोश अर्थात् भाव प्रवाह, आनंदमय कोश अर्थात् आत्मबोध, आत्मस्वरूप में स्थिति। ये पाँच चेतना के स्तर है।
निम्न स्तर के प्राणी इनमें भूमिका में पड़े रहते हैं। कृमिकीटकों की चेतना इंद्रियों की प्रेरणा के इर्द-गिर्द अपना चिंतन सीमित रखती है। वे शरीर की जीवनी-शक्ति मात्र से जीवित रहते हैं। संकल्प-बल उनके जीवन-मरण में सहायक नहीं होता। मनुष्य की जिजीविषा इस शरीर को अशक्त-असमर्थ होने पर भी जीवित रख सकती है, पर निम्न वर्ग के प्राणी मात्र सर्दी-गर्मी बढ़ने जैसे ऋतुओं से प्रभावित होकर अपना प्राण त्याग देते हैं। उन्हें जीवनसंघर्ष के अवरोध में पड़ने की इच्छा नहीं होती।
प्राणमय कोश की क्षमता जीवनी-शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जीवित रहने की सुदृढ़ और स्थिर इच्छा शक्ति के रूप में उसे देखा जा सकता है। स्वस्थ, सुदृढ़ और दीर्घ जीवन का लाभ शरीर को इसी आधार पर मिलता है। मनस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएँ प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दीन-हीन, भयभीत, शंकाशील, निराश, खिन्न, हतप्रभ व्यक्ति अपने इसी दोष के कारण उपेक्षित, तिरस्कृत एवं उपाहासास्पद बने रहते हैं। उत्साह के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहने वाली कर्मनिष्ठा का जहाँ अभाव होगा, वहाँ अवनति और अवगति के अतिरिक्त और कुछ रहेगा ही नहीं। साहस बाजी मारता है। बहादुरों के गले में अनादि काल से विजय बैजयन्ती पहनाई जाती रही है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा।
मनोमय कोश का अर्थ है-विचारशीलता, विवेक बुद्धि। यह तत्त्व जिसमें जितना सजग होगा, उसे उसी स्तर का मनस्वी या मनोबल संपन्न कहा जाएगा। यों मन हर जीवित प्राणी का होता है। कीट-पतंग भी उससे रहित नहीं हैं, पर मनोमय कोश के व्याख्याकारों ने उसे दूरदर्शिता, तर्क-प्रखरता एवं विवेकशीलता के रूप में विस्तारपूर्वक समझाया है। मन की स्थिति हवा की तरह है, वह दिशा विशेष तक सीमित न रहकर स्वेच्छाचारी वन्य पशु की तरह किधर भी उछलता-कूदता है। पक्षियों की तरह किसी भी दिशा में चल पड़ता है। इसे दिशा देना, चिंतन के अनुपयोगी प्रवाह में बहने से बचा कर उपयुक्त मार्ग पर सुनियोजित करना, मनस्वी होने का प्रधान चिह्न है। मनोनिग्रह-मनोजय इसी का नाम है।
एकाग्रता एवं चित्तवत्ति-निरोध का बहुत माहात्म्य योगशास्त्रों में बताया गया है। इसका अर्थ चिंतन प्रक्रि या को ठप्प कर देना, एक ही ध्यान में निमग्न रहना नहीं, वरन यह है कि विचारों का प्रवाह नियत-निर्धारित प्रयोजन में ही रुचिपूर्वक लगा रहे । यह कुशलता जिनको करतलगत हो जाती है, वे जो भी लक्ष्य निश्चित करते हैं, उसमें प्रायः अभीष्ट सफलता ही प्राप्त करके रहते हैं। बिखराव की दशा में चिंतन की गहराई में उतरने का अवसर नहीं मिलता। अस्तु किसी विषय में प्रवीणता और पारंगतता भी हाथ नहीं लगती। संसार में विशेषज्ञों का स्वागत होता है, यहाँ हर क्षेत्र में "ए-वन" की माँग है और यह उपलब्धि कुशाग्र बुद्धि पर ही नहीं वरन् सघन मनोमय के साथ संबद्ध है। इस मनोयोग का वरदान प्राप्त करने के लिए जो प्रयास-व्यायाम करने पड़ते हैं, उन्हें ही मनोमय कोश की साधना कहते हैं।
विज्ञानमय कोश को सामान्य भाषा में भावना प्रवाह कह सकते हैं। यह चेतना की गहराई में अवस्थित अंत:करण से संबंधित है। विचार-शक्ति से भाव-शक्ति कहीं गहरी है, साथ ही उसकी क्षमता एवं प्रेरणा भी अत्यधिक सशक्त है। मनुष्य विचारशील ही नहीं, संवेदनशील भी है। ये संवेदनाएँ ही उत्कृष्ट स्तर की आकांक्षाएँ उत्पन्न करती हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर मनुष्य बेचैन-विचलित हो उठता है, जब कि विचार-प्रवाह मात्र मस्तिष्कीय हलचल भर पैदा कर पाता है। देव और दैत्य का वर्गीकरण इस भाव चेतना के स्तर को देखकर ही किया जाता है।
विज्ञानमय कोश की संतुलित साधना मनुष्य को दयालु, उदार, सज्जन, सहृदय, संयमी एवं शालीन बनाती है। उसे दूसरों को दु:खी देखकर उसकी स्थिति में अपने को रखकर व्यथित होने की 'सहानुभूति' का अभ्यास होता है। तदनुसार औरों का दुःख बँटाने की, सेवा-परायणता की आकांक्षा सदा उठती रहती है। विभिन्न प्रकार के परमार्थ इसी स्थिति में बन पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मभावना सुविस्तृत होते-होते अतीव व्यापक बन जाती है। तब दूसरों के सुख में भी अपने निज के सुख जैसा आभास मिलता है।
आनंदमय कोश का विकास यह देखकर परखा जा सकता है कि मनुष्य क्षुब्ध, उद्विग्न, चिंतित, खिन्न, रुष्ट असंतुष्ट रहता है अथवा हँसती, मुस्कराती, हलकी-फुलकी, सखी, संतुष्ट जिंदगी जीता है। मोटी मान्यता यह है कि वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों के कारण मनुष्य सुखी-दुःखी रहते हैं, पर गहराई से विचार करने पर यह मान्यता सर्वथा निरर्थक सिद्ध होती है। एक ही बात पर सोचने के अनेक दृष्टिकोण होते हैं। सोचने का तरीका किस स्तर का अपनाया गया-यही है मनुष्य के खिन्न अथवा प्रसन्न रहने का कारण।
अपने स्वरूप का, संसार की वास्तविकता का बोध होने पर सर्वत्र आनंद-ही-आनंद है। दुःख तो अपने आपे को भूल जाने का, संसार को सब कुछ समझ बैठने के अज्ञान का है। यह अज्ञान ही भव-बंधन है, इसे ही माया कहते हैं। प्राणी विविध ताप इसी नरक की आग में जलने से सहता है। सच्चिदानंद परमात्मा के इस सुरम्य नंदन वन जैसे उद्यान में दुःख का एक कण भी नहीं, दु:खी तो हम केवल अपने दृष्टि-दोष के कारण होते हैं। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का विकृत रूप देखकर ही डरते और भयभीत होते हैं। यदि यह दृष्टि-दोष सुधर जाय, तो मिथ्या आभास के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति का निवारण होने में देर न लगे और आत्मा की निरंतर आनंद से परिपूर्ण-परितृप्त रहने की स्थिति बनी रहे।
पाँच कोशों की भावनात्मक पृष्ठभूमि यही है। इन्हीं कसौटियों पर कसकर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में जाना जा सकता है कि वह आत्मिक दृष्टि से कितना गिरा-पिछड़ा है अथवा उठने-विकसित होने में सफल हुआ है।
|
|||||
- ब्रह्मवर्चस् साधना का उपक्रम
- पंचमुखी गायत्री की उच्चस्तरीय साधना का स्वरूप
- गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना
- साधना की क्रम व्यवस्था
- पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा
- कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा
- ध्यान-धारणा का आधार और प्रतिफल
- दिव्य-दर्शन का उपाय-अभ्यास
- ध्यान भूमिका में प्रवेश
- पंचकोशों का स्वरूप
- (क) अन्नमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ख) प्राणमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ग) मनोमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (घ) विज्ञानमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ङ) आनन्दमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- कुंडलिनी के पाँच नाम पाँच स्तर
- कुंडलिनी ध्यान-धारणा के पाँच चरण
- जागृत जीवन-ज्योति का ऊर्ध्वगमन
- चक्र श्रृंखला का वेधन जागरण
- आत्मीयता का विस्तार आत्मिक प्रगति का आधार
- अंतिम चरण-परिवर्तन
- समापन शांति पाठ