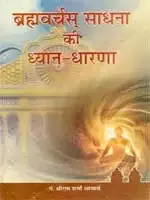|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> ब्रह्मवर्चस् साधना की ध्यान-धारणा ब्रह्मवर्चस् साधना की ध्यान-धारणाश्रीराम शर्मा आचार्य
|
127 पाठक हैं |
||||||
ब्रह्मवर्चस् की ध्यान धारणा....
गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना
पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार ब्रह्मा जी की दो पत्नियाँ हैंएक गायत्री, दूसरी सावित्री। इस अलंकार से तत्त्व दर्शन के रूप में यह समझना चाहिए कि परब्रह्म-परमात्मा की दो प्रमुख शक्तियाँ हैं-एक भाव चेतना-परा प्रकृति, दूसरी पदार्थ चेतना-अपरा प्रकृति। परा प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति संपर्क से उसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं आत्मा का परिकर कहा जा सकता है। अपरा प्रकृति के रूप में वही महातत्त्व बनकर इस विराट् ब्रह्मांड में क्रियाशील दृष्टिगोचर होता है। इसी अपरा प्रकृति को पदार्थ सत्ता एवं जड प्रकृति कहते हैं। पदार्थों की समस्त हलचलें इसी पर निर्भर हैं। परमाणुओं का अपनी धुरी पर घूमना, उनके द्वारा विविध-विधि क्रियाकलापों का संचालन होना, उसी अपरा प्रकृति की सूक्ष्म प्रेरणा से संभव होता है। विद्युत, ताप, प्रकाश, चुंबकत्व, रसायन, ईथर आदि उसी के विभाग हैं। पदार्थ विज्ञान इन्हीं शक्तियों को काम में लाकर अगणित आविष्कार करने और यांत्रिक सुविधा-साधन उत्पन्न करने में लगा हुआ है। इस - अपरा प्रकृति को अध्यात्म की भाषा में सावित्री कहा गया है। २. कुंडलिनी इसी दूसरी शक्ति का नाम है।
गायत्री और सावित्री का अंतर और भी स्पष्ट समझना हो तो गायत्री को ज्ञान-शक्ति और सावित्री को क्रिया-शक्ति कह सकते हैं। गायत्री चेतना की सामर्थ्य है और सावित्री पदार्थ के अंतराल में काम करने वाली क्षमता। इन्हीं दोनों के प्रभाव से यह समस्त संसार और मानवी काय-कलेवर अपनी हलचलों को जीवित रखे हुए है। गायत्री चेतना का शास्त्र, ब्रह्म विद्या है और सावित्री शक्ति की व्याख्या कुंडलिनी विज्ञान के रूप में की जाती है। गायत्री को पंचकोशी साधना के अंतर्गत और सावित्री को कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत प्रखर-परिष्कृत बनाया जाता है। गायत्री साधना चेतनात्मक रहस्यों का, दिव्य विभूतियों का अनुदान प्रस्तुत करती है और कुंडलिनी भौतिक सिद्धियों के लिए आवश्यक पथ-प्रशस्त करती है। एकांगी प्रगति अपर्याप्त है। उत्कर्ष उभय-पक्षीय होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म-विज्ञान के माध्यम से पंचकोशी गायत्री उपासना के साथ-साथ ब्रह्मतेजस् की-कुंडलिनी जागरण साधना को चलाते रहने का भी निर्देश है। इसे विरोधाभास की दृष्टि से नहीं वरन् पूरक प्रक्रिया का शुभारंभ ही समझना चाहिए।
समन्वयात्मक साधना का जितना महत्त्व है, उतना एकांगी का, .' असंबद्ध का नहीं। प्रायः साधना क्षेत्र में इन दोनों में यही भूल होती रही है। ज्ञान मार्गी-राजयोगी, भक्तिपरक साधना तक सीमित रह जाते हैं और हठयोगी, कर्मकांडी तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं। उपयोगिता दोनों की है। महत्ता किसी की भी कम नहीं, पर उनका एकांगीपन उचित नहीं, दोनों का जोड़ा और मिलाया जाना चाहिए। यह शिव-पार्वती विवाह ही गणेश जैसा भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसे पदार्थात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है।
गायत्री साधना का उददेश्य मानसिक चेतनाओं का जागरण और कुंडलिनी साधना का प्रयोजन पदार्थगत सक्रियताओं का अभिवर्धन है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। समर्थ शरीर और समर्थ मस्तिष्क परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें गाड़ी के दो पहिए कहना चाहिए। एक के बिना दूसरा निरर्थक रहता है। रुग्ण रहने वाला तत्त्व ज्ञानी और मूढ़मति नरपशु दोनों ही अधूरे हैं। आवश्यकता दोनों के समन्वय की है। यों वरिष्ठ और कनिष्ठ का चुनाव करना है तो प्राथमिकता मानसिक चेतना को ही मिलेगी।
मस्तिष्क मार्ग से प्रकट होने वाली चेतनात्मक शक्तियों की सिद्धियों का वारापार नहीं। योगी, तत्त्वज्ञानी, परादर्शी, मनीषी, विज्ञानी, कलाकार, आत्मवेत्ता, महामानव इसी शक्ति का उपयोग करके अपने वर्चस्व को प्रखर बनाते हैं। ज्ञान शक्ति के चमत्कारों से कौन अपरिचित है? मस्तिष्क का महत्त्व किसे मालूम नहीं? उसके विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना से समाधि तक के अगणित प्रयोग किए जाते रहते हैं। इस व्यावहारिक क्षेत्र को गायत्री उपासना-परा प्रकृति की साधना ही कहना चाहिए।
दूसरी क्षमता है, क्रिया शक्ति अर्थात् अपरा प्रकृति। शरीरगत अवयवों का सारा क्रिया-कलाप इसी से चलता है। श्वास-प्रश्वास, संचार, निद्रा, जागृति, मलों का विर्सजन, ऊष्मा, ज्ञान तत्त्व, विद्युत प्रवाह आदि अगणित प्रकार के क्रिया-कलाप शरीर में चलते रहते हैं। उन्हें अपरा प्रकृति का कर्तृत्व कहना चाहिए, इसे जड़ पदार्थों को गतिशील रखने वाली क्रिया शक्ति कहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्त्व भी कम नहीं। आरोग्य, दीर्घ जीवन, बलिष्ठता, स्फूर्ति, साहसिकता, सौंदर्य आदि कितनी ही शरीरगत विशेषताएँ इसी पर निर्भर हैं। इसे व्यावहारिक रूप से कुंडलिनी शक्ति कहना चाहिए। आहार, व्यायाम, विश्राम आदि द्वारा साधारणतया इसी शक्ति की साधना-उपासना की जाती है।
यों प्रधान तो मस्तिष्क स्थित दिव्य चेतना ही है। वह बिखर जाय तो तत्काल मृत्यु आ खड़ी होगी, पर कम उपयोगिताशरीरगत पदार्थ चेतना की भी नहीं है। उसकी कमी होने से मनुष्य दुर्बल, रुग्ण, अकर्मण्य, निस्तेज, कुरूप और कायर बनकर रह जायगा। निरर्थक, निरुपयोगी,भार-भूत जिंदगी की लाश ही ढोता रहेगा।
गायत्री का केंद्र सहस्रार-मस्तिष्क का मस्तिष्क-ब्रह्मरंध्र है। कुंडलिनी का केंद्र काम बीज-मूलाधार चक्र। गायत्री ब्रह्मचेतना की और सावित्री ब्रह्म-तेज की प्रतीक है। दोनों की परस्पर सघन एकता और अविच्छिन्न घनिष्ठता है। एक को उत्तर ध्रुवऔर दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव कह सकते हैं। पृथ्वी की धुरी के यह दोनों ही छोर हैं। मानवी सत्ता के भी यही दो ध्रुव मिलजुलकर जीवन का समग्र संचार करते हैं। गायत्री से दिव्य आध्यात्मिक विभूतियाँ उपलब्ध होती हैं और सावित्री से भौतिक ऋद्धिसिद्धियाँ। गायत्री उपासना की उच्चस्तरीय साधना पंचकोशों की, पंचयोगों की साधना बन जाती है। सावित्री कुंडलिनी है और उसे पाँच तप साधनों द्वारा जगाया जाता है। योग और तप के समन्वय से ही संपूर्ण आत्मसाधना का स्वरूप बनता और समग्र प्रतिफल मिलता है। इसलिए पंचकोशों की गायत्री और कुंडलिनी जागरण की सावित्री विद्या का समन्वित अवलंबन अपनाना ही हितकर है। बिजली की दो धाराएँ मिलने पर ही शक्ति प्रवाह में परिणत होती है। आत्मिक प्रगति का रथ भी इन्हीं दो पहियों के सहारे महान लक्ष्य की दिशा में गतिशील होता है।
उल्लेख किया जा चुका है कि कुंडलिनी को अपरा प्रकृति कहा जाता है और शरीर में उसका स्थान मूलाधार में है। इसे 'जीवन अग्नि' (लाइफ फायर) के नाम से भी जाना जाता है। मूलाधार क्षेत्र में त्रिकोण शक्ति बीज है, जिसकी संगति सुमेरु से बिठाई जाती है।
एक सर्पाकार विद्युत प्रवाह इस सुमेरु के आस-पास लिपटा बैठा है। इसी को महासर्पिणी कुंडलिनी कहते हैं। इसे विद्युत भ्रमर भी कह सकते हैं। तेज बहने वाली नदियों में कहीं-कहीं भँवर पड़ते हैं। जहाँ भँवर पड़ते हैं, वहाँ पानी की चाल सीधी अग्रगामी न होकर गोल गह्वर की गति में बदल जाती है। मनुष्य शरीर में सर्वत्र तो नाड़ी संस्थान के माध्यम से सामान्य गति से विद्युत प्रवाह बहता है, पर उस मूलाधार स्थित सुमेरु के समीप जाकर वह भँवर गह्वर की तरह चक्राकार घूमती रहती है। इसे सर्पिणी कहते हैं। कुंडलिनी की आकृति, सर्प की-सी आकृति मानी गई है।
नदी प्रवाह में भंवरों की शक्ति अद्भुत होती है। उनमें फँसकर बड़े-बड़े जहाज भी सँभल नहीं पाते और देखते-देखते डूब जाते हैं। साधारण नदी प्रवाह में जितनी शक्ति और गति रहती है उससे ६० गुनी अधिक शक्ति भँवर में पाई जाती है। शरीरगत विद्युत प्रवाह में अन्यत्र पाई जाने वाली क्षमता की तुलना में कुंडलिनी की शक्ति हजारों गुनी बड़ी है। उसका स्वरूप एवं विज्ञान यदि ठीक तरह समझा जा सके और उस विद्युत प्रवाह का प्रयोग--उपयोग जाना जा सके, तो निःसंदेह व्यक्ति सर्व सामर्थ्य संपन्न सिद्ध पुरुष बन सकता है।
कुंडलिनी का मध्यवर्ती जागरण मनुष्य शरीर में एक अद्भुत प्रकार की तड़ित उत्पन्न कर देता है।
वस्तुतः स्थूल कुंडलिनी का महासर्पिणी स्वरूप मूलाधार से लेकर मेरुदंड समेत ब्रह्मरंध्र तक फैले हुए सर्पाकृति कलेवर में ही पूरी तरह देखा जा सकता है। ऊपर-नीचे मुडे हए दो महान शक्तिशाली चक्र ही उसके आगे-पीछे वाले दो मुख हैं।
मेरुदंड पोला है, उसके भीतर जो कुछ है, उसकी चर्चा शरीर शास्त्र के स्थूल-प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर दूसरे ढंग से की जा सकती है। शल्य-क्रिया द्वारा जो देखा जा सकता है, वह रचना क्रम दूसरा है। इसमें सूक्ष्म प्रक्रिया के अंतर्गत योगशास्त्र की दृष्टि से परिधि में सन्निहित दिव्य-शक्तियों की चर्चा करनी है। योगशास्त्र के अनुसार मेरुदण्ड में एक ब्रह्म-नाड़ी है। उसके अंतर्गत इड़ा और पिंगला दो शिरायें गतिशील है। यह नाड़ियाँ रक्तवाहिनी शिरायें नहीं समझी जानी चाहिए। वस्तुत: ये विद्युतधाराएँ हैं। जैसे बिजली के तार में ऊपर एक-एक रबड़ का खोल चढ़ा होता है और उसके भीतर जस्ते तथा ताँबे का ठंडागरम तार रहता है, उसी प्रकार इन नाड़ियों को समझा जाना चाहिए। ब्रह्म नाड़ी रबड़ का खोल हुआ, उसके भीतर इड़ा और पिंगला ठंडे-गरम तारों की तरह हैं। इनका स्थल कलेवर या अस्तित्व नहीं है। शल्य-क्रिया द्वारा यह नाड़ियाँ नहीं देखी जा सकतीं। इस रचना क्रम को, सूक्ष्म विद्युत-धाराओं को दिव्य रचना ही कहना चाहिए।
मस्तिष्क के भीतरी भाग में यों कतिपय 'कोष्ठकों' के अंतर्गत भरा हआ मज्जा भाग ही देखने को मिलेगा। खर्दबीन से और कुछ नहीं देखा जा सकता, पर सभी जानते हैं कि उस दिव्य संस्थान के नगण्य से दीखने वाले घटकों के अंतर्गत विलक्षण शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्त्व, सारा चिंतन, सारा क्रियाकलाप और सारा शारीरिक, मानसिक अस्तित्त्व इन घटकों के ऊपर ही अवलंबित रहता है। देखने में सभी का मस्तिष्क लगभग एक जैसा दीखेगा, पर उसकी सूक्ष्म स्थिति में पृथ्वी, आकाश जैसा अंतर दीखता है, उसके आधार पर व्यक्तियों का घटिया-बढ़िया होना सहज आँका जा सकता है। यही सूक्ष्मता कुंडलिनी के संबंध में व्यक्त की जा सकती है। मूलाधार, सहस्रार, ब्रह्म नाड़ी, इड़ापिंगला इन्हें शल्य-क्रिया द्वारा नहीं देखा जा सकता। यह सारी दिव्य-रचना ऐसी सूक्ष्म है, जो देखी तो नहीं जा सकती, पर उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है।
मलद्वार और जननेंद्रिय के बीच जो लगभग चार अंगुल जगह खाली पड़ी है, उसी के गह्वर में एक त्रिकोण परमाणु पाया जाता है। सारे शरीर में गोल कण हैं, यह एक ही तिकोना है। यहाँ एक प्रकार का शक्ति-भ्रमर है। शरीर में प्रवाहित होने वाली तथा मशीनों में संचारित बिजली की गति का क्रम यह है कि वह आगे बहती है, फिर तनिक पीछे हटती है और फिर उसी क्रम से आगे बढ़ती, पीछे हटती हुई अपनी अभीष्ट दिशा में दौड़ती चली जाती है किंतु मूलाधार । स्थित त्रिकोण कण के शक्ति भँवर में सन्निहित बिजली गोल घेरे में पेड़ से लिपटी हुई बेल की तरह घूमती हुई संचारित होती है। यह संचार क्रम प्राय: साढ़े तीन लपेटों का है। आगे चलकर यह विद्युत धारा इस विलक्षण गति को छोड़कर सामान्य रीति से प्रवाहित होने लगती है।
यह प्रवाह निरंतर मेरुदंड में होकर मस्तिष्क के उस मध्य बिंदु तक दौड़ता रहता है, जिसे ब्रह्मदंड या सहस्रार कमल कहते हैं। इस शक्ति केंद्र का मध्य अणु भी शरीर के अन्य अणुओं से भिन्न रचना का है। वह गोल न होकर चपटा है। उसके किनारे चिकने न होकर खरदरे हैं। आरी के दाँतों से उस खरदरेपन की तुलना की जा सकती है। योगियों का कहना है कि उन दाँतों की संख्या एक हजार है। अलंकारिक दृष्टि से इसे एक ऐसे कमल पुष्प की तरह चित्रित किया जाता है, जिसमें पंखड़ियाँ खिली हुई हों। इस अलंकार के आधार पर ही इस अणु का नामकरण 'सहस्रारकमल' किया गया है।
जिस प्रकार पृथ्वी में चेतना एवं क्रिया उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानव पिंड देह के भी दो ही अति सूक्ष्म शक्ति संस्थान हैं। उत्तरी ध्रुव है-ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क सहस्रार कमल। ध्यान से लेकर समाधि तक और आत्मचिंतन से लेकर भक्तियोग तक की सारी आध्यात्मिक साधनाएँ तथा मनोबल, आत्मबल एवं संकल्प-जन्य सिद्धियों का केंद्र बिंदु इसी स्थान पर है।
दूसरा दक्षिणी ध्रुव मूलाधार चक्र, सुमेरु संस्थान, सुषुम्ना केंद्र है, जो मल-मूत्र के संस्थानों के बीचोंबीच अवस्थित है। कुंडलिनी, महासर्पिणी, प्रचंड क्रिया-शक्ति इसी स्थान पर सोई पड़ी है। उत्तरी ध्रुव की महासर्पिणी अपने सहचर महासर्प के बिना निरानंद मूर्च्छित जीवन व्यतीत करती है। मनुष्य शरीर विश्व की समस्त विशेषताओं का प्रतीक-प्रतिबिंब होते हुए भी तुच्छसा जीवन व्यतीत करते हुए कीट-पतंग की मौत मर जाता है। कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता, इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे पिंड के, देह के दोनों ध्रुव मूर्च्छित पड़े
हैं, यदि वे सजग हो गए होते तो ब्रह्मांड जैसी महान चेतना अपने पिंड में भी परिलक्षित होती।
मूत्र स्थान यों एक प्रकार से घृणित एवं उपेक्षित स्थान है, पर तत्त्वतः उसकी सामर्थ्य मस्तिष्क में अवस्थित ब्रह्मरंध्र जितनी ही है। वह हमारी सक्रियता का केंद्र है। यों नाक, कान आदि छिद्र भी मल विर्सजन के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर उन्हें कोई ढकता नहीं। मूत्र यंत्र को ढकने की अनादि एवं आदिम परिपाटी के पीछे वह सर्तकता है, जिसमें यह निर्देश है कि इस संस्थान से जो अजस्र शक्ति-प्रवाह बहता है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। शरीर के अन्य अंगों के तरह यों प्रजनन अवयव भी मांस-मज्जा मात्र से ही बने हैं, पर उनके दर्शन मात्र से मन विचलित हो उठता है। अश्लील चित्र अथवा अश्लील चिंतन जब मस्तिष्क में उथलपुथल पैदा कर देता है, तो उन अवयवों का दर्शन यदि भावनात्मक हलचल को उच्छृखल बना दे तो आश्चर्य ही क्या है? यहाँ यह रहस्य जान लेना ही चाहिए कि मूत्र स्थान में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित नहीं रहने दी जा सकती। उन्हें आवरण में रखने से उनका अपव्यय बचता है और अन्यों के मानसिक संतुलन को क्षति नहीं पहुँचती। छोटे बच्चों को भी कटिबंध इसीलिए पहनाते हैं। ब्रह्मचारियों को धोती के अतिरिक्त लँगोट भी बाँधे रहना पडता है। पहलवान भी ऐसा ही करते हैं। संन्यास और वानप्रस्थ में भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
उत्तरी ध्रुव सहस्रार-कमल में विक्षोभ उत्पन्न करने और उसकी शक्ति को अस्त-व्यस्त करने का दोष लोभ, मोह, क्रोध, जैसी दुष्प्रवृत्तियों का है। मस्तिष्क उन चिंताओं में दौड़ जाता है, तो उसे आत्मचिंतन के लिए ब्रह्म-शक्ति के संचय के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव मूलाधार में भरी प्रचंड क्षमता को कार्य-शक्ति में लगा दिया जाय तो मनुष्य पर्वत उठाने एवं समुद्र मथने जैसे कार्यों को कर सकता है। क्रिया-शक्ति मानव प्राणी में असीम है, किंतु उसका क्षय कामुक विषय-विकारों में होता रहता है। यदि इस प्रवाह को गलत दिशा से रोक कर सही दिशा में लगाया जा सके, तो मनुष्य की कार्य क्षमता साधारण न रहकर दैत्यों अथवा देवताओं जैसी हो सकती है।
पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। यह सारा चित्रण सूक्ष्म रूप से मानव शरीर में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति के प्रयोगप्रयोजन का है। हमारा मूत्र संस्थान खारी जल से भरा समुद्र है। उसे अगणित रत्नों का भाण्डागार कह सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की सुविस्तृत रत्न राशि इसमें छिपी हुई है। प्रजापति के संकेत पर एक बार समुद्र मथा गया है। देव और दानव इसका मंथन करने जुट गए। असुर उसे अपनी ओर खींचते थे अर्थात कामुकता की ओर घसीटते थे और देवता उसे रचनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने के लिए तत्पर थे। यह खींच-तान दूध में से मक्खन निकालने वाली बिलौने की, मंथन की क्रिया चित्रित की गई है।
समुद्र मंथन उपाख्यान में यह भी वर्णन है कि भगवान ने कछुआ का रूप बनाकर आधार स्थापित किया, उनकी पीठ पर सुमेरु पर्वत 'रई' के स्थान पर अवस्थित हुआ। वासुकि नाग के साड़े तीन फेरे उस पर्वत पर लगाये गए और उसके द्वारा मंथन कार्य संपन्न हुआ। कच्छप और सुमेरु मूलाधार चक्र में अवस्थित वह शक्ति बीज है, जो दूसरे कणों की तरह गोल न होकर चपटा है और जिसकी पीठ, नाभि ऊपर की ओर उभरी हई है। इसके चारों ओर महासर्पिणी, कुंडलिनी साढ़े तीन फेरे लपेटकर पड़ी हुई है। इसे जगाने का कार्य, मंथन का प्रकरण उद्दाम वासना के उभार और दमन के रूप में होता है। देवता और असुर दोनों ही मनोभाव अपना-अपना जोर अजमाते हैं और मंथन आरंभ हो जाता है। कृष्ण की रासलीला का आध्यात्मिक रहस्य कुछ इसी प्रकार का है। उस प्रकरण की गहराई में जाने और विवेचन करने का यह अवसर नहीं है। अभी तो इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि कामुकता की उद्दीप्त स्थिति को प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित करने का पुरुषार्थ समुद्र मंथन से रत्न राशि निकालने का प्रयोजन पूरा करता है।
पंचकोशी साधना के अंतर्गत मानवी सत्ता के अंतर्गत विशिष्ट शक्ति स्रोतों-अद्भुत व्यक्तित्वों का विकास किया जाता है। कुंडलिनी साधना के अंतर्गत अपने अंदर बीज रूप में सन्निहित महाशक्ति को जागृत करके, उसके अधोगामी प्रवाह को रोककर बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। ये साधनाएँ आत्मसत्ता को परमात्मसत्ता से जोड़ने, उस स्तर तक पहुँचाने में समर्थ हैं। इनके लिए सामान्य साधना-क्रम से ऊपर उठ कर कुछ विशिष्ट साधना प्रकियाएँ भी अपनानी पडती हैं। उन्हें बहत कठिन एवं दुर्लभ माना जाता है। ब्रह्मवर्चस् साधना-क्रम के अंतर्गत उन्हें यथासाध्य सुलभ एवं सुगम बनाकर प्रस्तुत किया गया है। ताकि हर स्थिति का व्यक्ति, थोड़ी तत्परता बरत कर उनका लाभ निर्भय होकर उठा सके।
|
|||||
- ब्रह्मवर्चस् साधना का उपक्रम
- पंचमुखी गायत्री की उच्चस्तरीय साधना का स्वरूप
- गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना
- साधना की क्रम व्यवस्था
- पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा
- कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा
- ध्यान-धारणा का आधार और प्रतिफल
- दिव्य-दर्शन का उपाय-अभ्यास
- ध्यान भूमिका में प्रवेश
- पंचकोशों का स्वरूप
- (क) अन्नमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ख) प्राणमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ग) मनोमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (घ) विज्ञानमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ङ) आनन्दमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- कुंडलिनी के पाँच नाम पाँच स्तर
- कुंडलिनी ध्यान-धारणा के पाँच चरण
- जागृत जीवन-ज्योति का ऊर्ध्वगमन
- चक्र श्रृंखला का वेधन जागरण
- आत्मीयता का विस्तार आत्मिक प्रगति का आधार
- अंतिम चरण-परिवर्तन
- समापन शांति पाठ