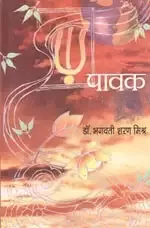|
उपन्यास >> पावक पावकभगवतीशरण मिश्र
|
177 पाठक हैं |
||||||
आचार्यों की श्रृंखला के अन्तिम आचार्य श्रीमद्वल्लभाचार्य के जीवन को आधार बनाकर प्रस्तुत यह उपन्यास उनकी अद्भुत जीवन गाथा का एक प्रामाणिक दस्तावेज
Pavak
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
यह पुस्तक लेखक के 20 वर्षों के श्रम का प्रतिफल है। आचार्यों की श्रृंखला के अन्तिम आचार्य श्रीमद्वल्लभाचार्य के जीवन को आधार बनाकर प्रस्तुत यह उपन्यास उनकी अद्भुत जीवन गाथा का एक प्रामाणिक दस्तावेज तो है ही, इसके अतिरिक्त भी यह बहुत-कुछ है।
इसे दो खण्डों में प्रस्तुत किया जा रहा है-‘पावक’ और ‘अग्निपुरुष’। दोनों खण्ड स्वतंत्र हैं। द्वितीय खंड को इस तरह लिखा गया है कि इसे पढ़ते समय प्रथम खंड को नहीं पढ़ने से किसी असुविधा का भान नहीं हो।
अपसंस्कृति के इस युग में जहाँ आयातीत विदेशी मूल्यों ने समृद्ध भारतीय संस्कृति और परम्परा को आखेट बनाकर देश को विखंडन के कगार पर खड़ा कर दिया है, वहीं यह कृति उच्चतर मानवीय मूल्यों की स्थापना को समर्पित है। दिग्भ्रमित वर्तमान पीढ़ी को यह मानवता, एकता और अपनी समृद्ध परम्परा का सशक्त सन्देश देने में अद्वितीय है।
मुख्य बात यह है कि इसमें सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय-वेद, वेदान्त, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि-प्रायः अपनी समग्रता में उपलब्ध हैं। इस उपन्यास का अध्ययन कर कोई भी भारतीय अपनी उदात्त संस्कृति और परम्परा से परिचित हो सकता है।
इस तरह यह कृति आज के देशकाल के लिए अत्यन्त प्रासंगिक है। यह एक ही साथ प्राचीन और अति अर्वाचीन भी है।
अपनी सुमधुर भाषा और प्रभावकारी शिल्प के माध्यम से, प्रख्यात उपन्यासकार ने आधुनिक पाठकों को एक ऐसी अनुपम भेंट दी है जो उसी के वश की बात है।
एक वाक्य में, यह ग्रन्थ इस आर्य-भूमि के साहित्य संस्कृति तथा अध्यात्म का एक वृहत् कोष है जो जीवन को सही अर्थों में जीने के सन्देश से प्राणवन्त है।
इसे नहीं पढ़ने वाला बहुत-कुछ से वंचित रहने को बाध्य होगा। इस कृति को लेकर यही कहने को बाध्य होना पड़ता है-‘न भूतो न भविष्यति।’
इसे दो खण्डों में प्रस्तुत किया जा रहा है-‘पावक’ और ‘अग्निपुरुष’। दोनों खण्ड स्वतंत्र हैं। द्वितीय खंड को इस तरह लिखा गया है कि इसे पढ़ते समय प्रथम खंड को नहीं पढ़ने से किसी असुविधा का भान नहीं हो।
अपसंस्कृति के इस युग में जहाँ आयातीत विदेशी मूल्यों ने समृद्ध भारतीय संस्कृति और परम्परा को आखेट बनाकर देश को विखंडन के कगार पर खड़ा कर दिया है, वहीं यह कृति उच्चतर मानवीय मूल्यों की स्थापना को समर्पित है। दिग्भ्रमित वर्तमान पीढ़ी को यह मानवता, एकता और अपनी समृद्ध परम्परा का सशक्त सन्देश देने में अद्वितीय है।
मुख्य बात यह है कि इसमें सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय-वेद, वेदान्त, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि-प्रायः अपनी समग्रता में उपलब्ध हैं। इस उपन्यास का अध्ययन कर कोई भी भारतीय अपनी उदात्त संस्कृति और परम्परा से परिचित हो सकता है।
इस तरह यह कृति आज के देशकाल के लिए अत्यन्त प्रासंगिक है। यह एक ही साथ प्राचीन और अति अर्वाचीन भी है।
अपनी सुमधुर भाषा और प्रभावकारी शिल्प के माध्यम से, प्रख्यात उपन्यासकार ने आधुनिक पाठकों को एक ऐसी अनुपम भेंट दी है जो उसी के वश की बात है।
एक वाक्य में, यह ग्रन्थ इस आर्य-भूमि के साहित्य संस्कृति तथा अध्यात्म का एक वृहत् कोष है जो जीवन को सही अर्थों में जीने के सन्देश से प्राणवन्त है।
इसे नहीं पढ़ने वाला बहुत-कुछ से वंचित रहने को बाध्य होगा। इस कृति को लेकर यही कहने को बाध्य होना पड़ता है-‘न भूतो न भविष्यति।’
यह पुस्तक
इस पुस्तक को क्या नाम देंगे ? यह पूर्णतया ऐतिहासिक तो है ही, आध्यात्मिक भी है। इतिहास और अध्याय दोनों शुष्क विषय हैं सामान्य पाठक के लिए इस बाधा को दूर करने के लिए इसे औपन्यासिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। भाषा, शैली और विशेष औपन्यासिक शिल्पों का सहारा लेकर इसमें पठनीयता भरने का मैंने प्रचुर प्रयास किया है। अतः, सामान्य पाठक भी इसे नीरस और दुरुह नहीं पाएँगे।
गलत है कि अध्यात्म धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है। वैश्वीकरण और उन्मुखता बाजार के प्रभाव ने नई पीढी़ के कुछ लोगों को दिग्भ्रमित अवश्य किया है। किन्तु देखकर आश्चर्य होता है कि मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में नवयुवकों, नवयुवतियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उन्हें भी अध्यात्म में आस्था की नई किरण दिखाई पड़ने लगी है। बुजुर्ग तो स्वभावतः आस्थावान हो ही जाते है अतः यह पुस्तक पुरानी और नई पीढ़ी को समान रूप से समर्पित है। दोनों की आस्थाएँ और प्रगाढ़ होंगी इसी दृष्टिकोण से यह वृहतकाय पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है।
सही नहीं है कि मोटी पुस्तकों का युग बीत गया। प्रायः सभी उपन्यास विशालकाय हैं पर उनकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा रही है। 15-20 वर्ष पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के भी अभी तक नए संस्करण निकालने पड़ रहे हैं। टी.वी. और इंटर्नेट1 लिखित शब्दों की हत्या करने में सफल नहीं हुए अपितु पुस्तकों के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान सराहनीय सिद्ध हो रहा है।
वल्लभाचार्य एक अवतारी पुरुष थे। हिन्दी वाले उन्हें कम ही जानते हैं पर इतना वे अवश्य जानते हैं कि वे हिन्दी के सर्वधिक कवि सूरदास के गुरू थे। इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होगा कि श्रीमदवल्लभाचार्य नहीं तो सूरदास भी नहीं होते और न होता उनका ‘सूर सागर’। वल्लभाचार्य,, आचार्य की परम्परा के अन्तिम आचार्य थे। आदि शंकराचार्य आदि उनका ‘सूर सागर’ वल्लभाचार्य, आचार्यों की परम्परा के अन्तिम आचार्य थे। आदि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और रामानुजाचार्य के सदृश्य आचार्यों के मध्य वह एक देदीप्यामान नक्षत्र की तरह शोभित हैं आदि शंकराचार्य को छोड़ दें, यद्यपि उनके अद्धैत मत के विरुद्ध ही उन्होंने अपने शुद्धाद्धैत मत का प्रचार कर और उनके अनुयायियों
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. अभी-अभी लेखक की पुस्तक ‘शान्तिदूत’ (राजपाल एंड सन्ज़ गेट, दिल्ली-6) चेन्नई के ‘पेंटामीडिया’ द्वारा पूरी ‘इंटरनेट’ पर धारावाहिक प्रसारित हुए है।
को परास्त करके अपना विजय-ध्वज फहराया, तो शेष आचार्यों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण-भक्ति के तो वे एकमात्र आचार्य हैं। कृष्ण-भक्ति का ऐसा आचार्य न उनके जन्मधारणा को पर इन सैकड़ों वर्षों में उनको पराभूत करे ऐसा तो कोई नहीं पैदा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र आदि उनके अनुयायियों की संख्या अनन्त है। वाणाणसी के गोपाल-मन्दिर में उनका एक प्रसिद्ध पीठ है। जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी उनके मतावलम्बी विद्यमान हैं। तमिलनाडु, केरल और बिहार के सदृश्य कुछ दुर्भाग्य-ग्रस्त राज्य हैं जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को विभिन्न आयामों से पूर्णतया परिचित नहीं हो सके, यद्यपि इन स्थानों में उनको जानने वालों की कमी नहीं है।
यह पुस्तक आचार्य-श्री के अद्भुद व्यक्तित्व और चमरत्कारिक कृतित्व से सम्पूर्ण राष्ट्र को परिचित कराने के लिए ही यथासम्भव ललित एवं प्रवाहमान भाषा में पस्तुत की गई है।
समझना गलत होगा कि आचार्य मात्र कृष्णोपासक और कृष्ण-भक्ति के प्रचारक थे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी इनकी मुख्य चिन्ता के विषय थे। मनुष्य-मात्र को उसके आत्मबल और विश्वास से परिचित कराना इनका प्रमुख उद्देश्य था। यवनों से पददलित और देशी राजाओं के पारस्परिक विद्वेष के कारण राष्ट्र तो टूटन और बिखराव के कगार पर पहुँच ही चुका था, सामान्य जन बलात् धर्म-परिवर्तन और विदेशियों के निरन्तर वृद्धिशील आतंक से अवसाद-ग्रस्त हो, जीवन के प्रति ही उदासीन हो चले थे। ऐसी स्थिति में भक्ति ही एक मात्र सहारा थी। श्रीमदवल्लभाचार्य ने इस सूत्र को पकड़ा और उसके सहारे न केवल देश को, और विखंडन से बचाया अपितु जनता को अवसाद और भय से मुक्ति दे उनके अन्दर जिजीविषा भरने का भी प्रयास किया।
श्रीमदवल्लभाचार्य पहले आचार्य थे जिन्होंने सम्पूर्ण देश का तीन बार परिभ्रमण किया। उनके इन राष्ट्र-परिभ्रमणों से भी देशवासियों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता का परिचय मिलता है।
परिभ्रमण और प्रवचन से बचा उनका समय ग्रन्थ-लेखन और उनके इष्टदेव श्रीनाथजी के स्वरूप की सेवा-सुश्रूषा में व्यतीत होता था। श्रीनाथजी (भगवान कृष्ण का गोवर्द्धनधारी-रूप) को उन्होंने गिरिराज (गोवर्द्धन) पर प्रतिष्ठित किया था। उनके जीवनकाल तक श्रीनाथ जी इसी मंदिर में रहे। श्रीमद्वल्लभाचार्य भी घूम-फिरकर वहाँ आते रहे। सूरदास को भी उन्होंने श्रीनाथ जी के कारण अपने साथ जोड़ा। यह सब इस पुस्तक के पृष्ठों में विस्तार से मिलेगा।
आज भी गोवर्धन के समीप पारसौली नामक ग्राम के समीप चन्द-सरोवर के पास महाप्रभु श्रीमदवल्लभाचार्य की बैठक सुरक्षित है। उसी के पार्श्व में सूरदास की समाधि भी है। सूर-पंचशती के अवसर पर वहाँ से थोड़ा हटकर सूरदास को सूर की स्मृति में निर्मित हुआ सूर के गुरू आचार्य-श्री की सुधि लेने के लिए हिन्दी वालों को कोई स्थान चिन्ता नहीं रही।
राजस्थान में नाथद्वारा एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ है। तिरुपति के पश्चात् उसी का स्थान है। सैकड़ों-हजारों दर्शक वहाँ प्रतिदिन जाते हैं पर यह कितनों को पता है कि इस मन्दिर का विग्रह वही है जो श्रीमद्वल्लभाचार्य को गोवर्द्धन पर प्राप्त हुआ था और जिसकी पूजा-अर्चना उन्होंने गोवर्धन-स्थिति मन्दिर में आजीवन की थी ?
उनके मृत्युपरान्त, औरंगजेब के मूर्ति-भंजन-अभियान से घबराकर उनके यशस्वी पुत्र विठ्ठलनाथ इस विग्रह को गोवर्द्धन से हटाकर राजस्थान ले गए। वहाँ श्रीनाथजी के पहुँचने से ही ‘श्रीनाथद्वारा’ नगर बस आया। श्रीनाथ जी और महाप्रुभ में अभेद था। दोनों महाप्रभु की भक्ति के कारण दो स्वरूप पर एक प्राण हो गए थे। जो नाथद्वारा में श्रीकृष्ण विग्रह के दर्शन करते हैं, वे स्वतः महाप्रभु के भी दर्शन प्राप्त कर लेते हैं पर इस तथ्य में कितने भिज्ञ हैं ?
नहीं समझा जाए कि पुस्तक मात्र एक –दो वर्षों के श्रम की देन है। प्रायः हर वर्ष मेरी एक पुस्तक आ जाती है।, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक मात्र एक वर्ष में लिखी गई। मैं कई पुस्तकों पर एक साथ काम करता हूँ। इस पुस्तक ने तो कम-से-कम बीस वर्षों का समय लिया। ऐतिहासिक-पौराणिक पुस्तकों की मेरी रचना-प्रक्रिया यह है कि मैं विषय से सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रिक कर लेता हूं और उसका अध्ययन कर उसको आत्मसात करने के पश्चात् ही पुस्तक में हाथ लगाता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करता हूँ। इसमें सामग्री मिले या नहीं; कहीं-कहीं मिल जाती है पर विषय की प्रामाणिकता अवश्य सिद्ध हो जाती है। अतः मेरी हर कृति, अध्ययन, अन्वेषण और पूर्ण गवेषणा पर आधारित है।
इस कृति को पूर्ण होने में बीस वर्ष लगे यह अतिशयोक्ति नहीं। इसके आधार हैं।
नाथद्वार पहले-पहल मैं 1979 में गया था। बीस नहीं अपितु इक्कीस वर्ष पूर्व। वहाँ जाने पर पता लगा कि वहाँ का विग्रह श्रीमदवल्लाचार्य द्वारा पूजित है। नाथद्वारा मैं पुनः कम-से-कम चार बार गया। लोगों से वार्तालाप हुआ, सामग्री भी मिली।
जब मैं रेल-मन्त्रालय में संयुक्त निदेशक (राज्यभाषा) था तो मुझे चम्पारण्य के आसपास एक रेल-कार्यालय का निरीक्षण करने जाना पड़ा। मेरे हिन्दी –अधिकारी ने कहा कि कुछ दूर चम्पारण्य में श्रीमदवल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, आप देखना चाहेंगे ? मैं सहर्ष प्रस्तुत हो गया। झाड़-झंखाड़ों से निपटता हुआ मैं उस स्थान पर पहुँच ही गया जहाँ घोर जंगल में महाप्रभु का जन्म हुआ था। वहाँ एक स्मारक निर्माणाधीन था। वह तो अब भव्य रूप ले चुका होगा। इससे बाहर आया तो कुछ मकान-‘स्टॉल’ नए-नए बने मिले। वहाँ भी श्रीमदल्लभाचार्य से सम्बन्धित सामग्री और उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ उपलब्ध थे। यह 1982 की बात है। अब तो वहाँ बहुत-कुछ बन गया होगा।
मैंने वाराणसी में हनुमान-घाट के भी दर्शन किए जहाँ महाप्रभु का लालन-पालन हुआ था। वाराणसी के उन स्थानों को देख जो महाप्रभु से सम्बन्धित हैं।
गोवर्द्धन-(गिरिराज) जिस पर अब भी श्रीनाथ जी का प्राचीन भव्य मन्दिर अवस्थित है- के दर्शन मैंने कई बार किए। गोवर्द्धन की कई परिक्रमाएँ भी कीं जिनका वर्णन उचित नहीं। तिरुपति तो जाना हुआ ही, विंध्याचल, अयोध्या, हरिद्वार आदि भी गया।
महाप्रभु ने जहाँ-जहाँ रुककर भगवत-पाठ किया वहाँ-वहाँ उनकी बैठक बन गई। बैठक-स्थान एक स्मारक ही बन गया।
देश में ऐसी चौंसठ बैठकें वर्तमान हैं। सबको देखना सम्भव नहीं और आवश्यक भी नहीं। कई स्थानों पर एक या दो कमरे के जर्जर या मरम्मत किए छोटे भवन के सिवा कुछ नहीं मिलता। सामग्री आदि की तो बात ही नहीं। कुछ स्थानों को अवश्य अभी तक पूर्णतया सुरक्षित रखा गया है।
कांकरौली-स्थान, नाथद्वारा के बाद सर्वाधिक जाग्रत स्थल है।
गोकुल की बैठक भी आकर्षण रूप में सुरक्षित है। ब्रज अकादमी वृन्दावन (अब प्रायः बन्द) में रहते हुए एक गोकुलवासी मित्र के साथ मैं गोकुल भी गया। वहाँ समय-समय से उत्सव होते रहते हैं, और वल्लभाचार्य के भक्त वहाँ भरे पड़े हैं। लोगों के वार्तालाप करने से ज्ञात हुआ है कि उन्हें आज भी इस बात पर गर्व है कि महाप्रभु के चरण वहाँ पड़े थे और उन्होंने पर्याप्त समय वहाँ व्यतीत किया था। वृन्दावन और मथुरा में भी मैंने महाप्रभु से सम्बन्धित स्थलों के दर्शन किए।
वाराणसी का गोपाल मन्दिर वल्लभ-प्रेमियों का प्रसिद्ध पीठ है। मैं 1997 में वहाँ अपने मित्र श्री एस.सी.शर्मा के साथ गया। मेरा सौभाग्य कि वहाँ वल्लभ-वंश की अन्तिम वृद्ध महिला मठ की दूसरी ओर के मन्दिर में रहती थीं। प्रबन्धक से सूचना मिली तो मैंने उनके पास, दर्शन-हेतु निवेदन भिजवाया। अब तक मैं पुस्तक पर पर्याप्त कार्य कर चुका था ।
उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, ‘‘मैं अब किसी को ‘‘इंटरव्यू’’ आदि नहीं देती।
मैं विवश हुआ पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर सूचना भिजवाई कि मैं उनका इंटरव्यू नहीं लूँगा। एक प्रश्न भी नहीं पूछूँगा, अपितु मुख भी नहीं खोलूँगा। मैं महाप्रभु पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। उनके वंश की इस अन्तिम देवी के केवल दर्शन-मात्र से मेरी पुस्तक सार्थक हो जाएगी।
इस बार उनका हृदय पिघला। उन्होंने मुझे कहलवाया कि मैं अगले दिन दस बजे आऊँ और जब वे मन्दिर लौटने लगें तो मार्ग के किनारे खड़े होकर उनके दर्शन कर लूँ।
मैं दूसरे दिन पुनः वहाँ गया। यथास्थान खड़ा हो गया। एक स्वयंसेवक भी मेरे साथ था। वह मन्दिर से लौटने लगीं तो स्वयंसेवक ने पहचनवाया। श्वेतवस्त्रा वह वृद्धा, सरस्वती स्वरूप ही लग रही थीं। पास आईं तो मैंने धरती का स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया निवेदन किया। वे क्षण-भर को रुकीं। मेरा साहस बढ़ा। मेरा बन्द मुँह खुल पड़ा और मैंने संक्षेप में निवेदन किया, ‘‘ आप केवल अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी पुस्तक धन्य हो जाएगी। ’’
उनकी मुझ पर कुछ विशेष ही कृपा हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘तीन बजे आइए तो मैं आपको कुछ सामग्री दूँगी।’’
मैं पुनः तीन बजे आ गया, वे स्वयं तो नहीं आईं पर तीन दासियों के माध्यम से ढेर सारी सामग्री भिजवा दी-कई स्मारिकाएँ, कई मूल ग्रन्थ, कई संकलन। उतनी सामग्री मुझ अकेले के उठाए क्या उठे ? अन्ततः मैंने सेविकाओं से ही अनुरोध किया कि बाहर प्रबन्धक के कमरे तक वे उन्हें पहुँचा दें।
इस तरह इस पुस्तक पर महाप्रभु की वंशजा का आशीर्वाद भी अंकित है। यह मेरा अतिरिक्त सौभाग्य है।
गोपाल-मन्दिर के ही तत्कालीन पीठाधीश ने कोई दो घंटे तक महाप्रभु और शुद्धाद्धैत तथा पुष्टिमार्ग पर संक्षेप पर सार्थक रूप में प्रकाश डाला। मैं उनका ऋणी हूँ।
कठिन थी श्रीमदवल्लाभाचार्य-रचित ग्रंन्थों की उपलब्धि। यद्यपि उपन्यास में उनके संस्कृत गंन्थों का उद्धरण देना उचित नहीं था फिर भी उनके साहित्य, उनकी भाषा, उनके शिल्प, उनकी तर्क-शक्ति से भिज्ञता आवश्यक थी।
ब्रज-अकादमी वृन्दावन के संस्थापक-अध्यक्ष श्री 1008 श्री पाद बाबा (अब स्वर्गीय) ने न केवल मुझे अपने पुस्तकालय में महाप्रभु की बहुत-सी पुस्तकें उपल्ब्ध करा दीं अपितु मेरे प्रायः दो सप्ताह के वहाँ निवास के समय मेरी पूर्ण सुविधा का भी ध्यान रखा प्रभु उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।
पुस्तक-लेखन का आरम्भ इतने अध्ययन-अन्वेषण के पश्चात् 1994 में ही विधिवत आरम्भ हो गया था। यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं थी। इस मध्य मेरी कई पुस्तकें भी आ गईं पर वल्लभाचार्य बहुत कठिन सिद्ध हो रहे थे।
1999 अगस्त प्रायः तीन सौ टंकित पृष्ठ तैयार हो गये थे। सोचा था इतने ही प्रायः और लिखने होंगे; 2000 में तो पुस्तक आ ही जाएगी, पर दुर्भाग्य ऐसा कि अगस्त 1999 से जुलाई 2000 तक मैं दिल्ली में इस कार्य के लिए प्रायः एकाकी रहा। पर लिखने के नाम पर मैं प्रायः एक वर्ष में 50 पृष्ठ भी नहीं लिख पाया। कारण कुछ नहीं पर जिस लेखकीय ‘मूड’ की मैंने बात रखी थी, वह आड़े आ गईं। मेरा ‘मूड’ ही नहीं बना। आश्चर्य, ऐसा पहले कभी नहीं था, मैंने रचनाओं पर रचनाएँ देता गया हूँ। ‘मूड’ क्या है इसमें मेरा परिचय ही नहीं। पर इस बार हो गया।, शायद ऐतिहासिक से अधिक आध्यात्मिक प्रकृति की होने के कारण इस पुस्तक को किसी आध्यात्मिक स्थल पर ही समाप्त होना था।
मैं 19 जुलाई, 2000 को केवल एक सप्ताह के लिए दिल्ली से पटना आया। दिल्ली लौटने के लिए 26 जुलाई के आरक्षण को सहसा रद्द कराना पड़ा। कुछ आवश्यक कार्य आ गया। कार्य कुछ लम्बा ही खिंचता गया। प्रवास-अवधि अनिश्चित हो गई। मैं विविश पटना-सिटी के बालकिशनगंज के प्रसिद्ध आश्रम शाक्य साधना केन्द्र के संस्थापक एवं सुप्रसिद्ध तान्त्रिक एवं ज्योतिर्विद् प्रेम बाबा के यहाँ ठहर गया।
आश्रम का वातावरण आध्यात्मिक होने के अतिरिक्त रमणीय भी है। पेड़-पौधों, लता-बल्लियों से युक्त यह एक तपोवन-सा ही लगता है। प्रेम बाबा अपने यन्त्र-तन्त्र तथा प्रायः अहर्निश हवन पूजन के द्वारा लोगों का मनस्पात हरते रहते हैं। उनकी मनोकांक्षाएँ पूर्ण करते हैं। उनकी साध्वी पत्नी पूनम माता आश्रम की व्यवस्था भी चलाती हैं और अपने नियमित पूजा-पाठ का ध्यान भी रखती हैं।
एक दिन पेड़-पौधों से घिरे आश्रम के बरामदे में बैठा मैं सोच रहा था कि बाबा के यहाँ सैकड़ों लोग नित्य आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे वल्लभाचार्य का क्या होगा ? वह अधूरे ही पड़े रहने को आरम्भ हुए है क्या ?
स्थान, सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। बाबा द्वारा निरन्तर जारी जप और हवन ने इसे मनोकामना-पूर्ति का स्थल ही बना दिया है।
मेरी रुकी कलम भी दूसरी ही सुबह (6 अगस्त) को चल पड़ी और ऐसी चली कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। आध्यात्मिक ऊर्जा ने जैसे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी प्रदान की। सरकारी कार्य तो अपनी गति से हो रहा था पर मैं जो नित्यक्रिया के पश्चात् छह बजे सुबह लिखने बैठता तो छह बजे शाम को ही उठता। बीच में केवल नाश्ता और भोजन के लिए समय निकालता। यह क्रम महीनों अबाध गति से चला, फलस्वरूप पुस्तक यहीं रहते-रहते समाप्त हो गईं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आश्रम की आध्यात्मिकता ने ही इस असम्भव-से प्रतीक होते कार्य को सरल बनाया। मैं प्रेम बाबा और उनकी देवी-स्वरूपा पत्नी पूनम मैंया का बहुत कृतज्ञ हूँ।
इस पुस्तक के सम्बन्ध में एक-दो बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है।
प्रथम तो यह है कि मैंने इसमें औपन्यासिक शिल्प को एक नया आयाम दिया है। ऐसे उपन्यास में पाठक के आमने-सामने नहीं आना चाहिए। मैंने पूरी तरह इसे अमान्य कर दिया है। ऐसे भी उपन्यास में मूलतः उपन्यासकार ही आदि से अन्त तक बोलता है भले ही वह विभिन्न पात्रों के माध्यम से बोले। उपन्यासकार की इस अप्रत्यक्ष उपस्थिति को मैंने कई बार स्थानों का प्रत्यक्ष कर दिया है। उपन्यासकार और पाठक आमने-सामने हुए हैं। इसे अगर समीक्षक-उपन्यास-विधा का हनन मानें तो उन्हें इसका अधिकार प्राप्त है। किंतु किसी भी विधा में एक ही शिल्प, एक ही शैली अथवा ‘टेकनिक’ को शव की तरह अपने स्कन्धों पर ढोए जाने का मैं कायल नहीं हूँ। समीक्षा के मापदण्ड बदलते रहते हैं तो लेखक इतना निरीह क्यों, कि वह औपन्यासिक शिल्प के गढे-गढ़ाए ढाँचे में बँधा रहे ? उसे तोड़ना उसका अधिकार है। उसकी मौलिकता। कई अध्यायों के प्रारम्भ में मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी आई जो मेरे चिन्तन को मुखर करती है और आगे जाने वाले घटनाक्रम को भी इंगित करने में सक्षम है। यह पहले भी कई उपन्यासों में हुआ है। पाठकों ने इसे सराहा है तो आलोचकों को बना-बनाया बहाना मिल गया है।
इस उपन्यास में लेखक-पाठक-संवाद कुछ अधिक ही दृष्टिगोचर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पाठक पहले की तरह ही मेरी शैली से प्रसन्न होंगे और समीक्षक भी अपनी आदत के अनुसार अप्रसन्न। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।, मैंने पुस्तक को अधिक आकर्षण और पठनीय बनाने हेतु ही इस शिल्प को अपनाया है। खैर, कई विदेशी लेखक तो इस ‘तकनीक’ का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं।
एक बात और पुस्तक में मूल कथा के साथ कई अन्तर्कथाएँ मिलेंगी। जैसा आरम्भ में कहा, एक ऐतिहासिक सह-आध्यात्मिक उपन्यास बहुत हद तक सामान्य पाठक के लिए दुहरू हो सकता है। अन्तर्कथाएँ औपन्यासिक कृति को प्राणवन्त और प्रासंगिक बनाती हैं और पाठकों को मनोरंजक में सहायक होती हैं। अतः, उपन्यास के कलेवर के विस्तार के कतरे को झेलते हुए भी मैंने अन्तर्कथाओं से मुँह मोड़ना उचित नहीं समझा। इनमें से कुछ पाठकों की परिचित भी होंगी पर उन्हें परोसने का अंदाज निश्चित ही भिन्न होगा। समीक्षक इनको लेकर कुछ भी कहने को स्वतन्त्र हैं।
गलत है कि अध्यात्म धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है। वैश्वीकरण और उन्मुखता बाजार के प्रभाव ने नई पीढी़ के कुछ लोगों को दिग्भ्रमित अवश्य किया है। किन्तु देखकर आश्चर्य होता है कि मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में नवयुवकों, नवयुवतियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उन्हें भी अध्यात्म में आस्था की नई किरण दिखाई पड़ने लगी है। बुजुर्ग तो स्वभावतः आस्थावान हो ही जाते है अतः यह पुस्तक पुरानी और नई पीढ़ी को समान रूप से समर्पित है। दोनों की आस्थाएँ और प्रगाढ़ होंगी इसी दृष्टिकोण से यह वृहतकाय पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है।
सही नहीं है कि मोटी पुस्तकों का युग बीत गया। प्रायः सभी उपन्यास विशालकाय हैं पर उनकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा रही है। 15-20 वर्ष पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के भी अभी तक नए संस्करण निकालने पड़ रहे हैं। टी.वी. और इंटर्नेट1 लिखित शब्दों की हत्या करने में सफल नहीं हुए अपितु पुस्तकों के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान सराहनीय सिद्ध हो रहा है।
वल्लभाचार्य एक अवतारी पुरुष थे। हिन्दी वाले उन्हें कम ही जानते हैं पर इतना वे अवश्य जानते हैं कि वे हिन्दी के सर्वधिक कवि सूरदास के गुरू थे। इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होगा कि श्रीमदवल्लभाचार्य नहीं तो सूरदास भी नहीं होते और न होता उनका ‘सूर सागर’। वल्लभाचार्य,, आचार्य की परम्परा के अन्तिम आचार्य थे। आदि शंकराचार्य आदि उनका ‘सूर सागर’ वल्लभाचार्य, आचार्यों की परम्परा के अन्तिम आचार्य थे। आदि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और रामानुजाचार्य के सदृश्य आचार्यों के मध्य वह एक देदीप्यामान नक्षत्र की तरह शोभित हैं आदि शंकराचार्य को छोड़ दें, यद्यपि उनके अद्धैत मत के विरुद्ध ही उन्होंने अपने शुद्धाद्धैत मत का प्रचार कर और उनके अनुयायियों
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. अभी-अभी लेखक की पुस्तक ‘शान्तिदूत’ (राजपाल एंड सन्ज़ गेट, दिल्ली-6) चेन्नई के ‘पेंटामीडिया’ द्वारा पूरी ‘इंटरनेट’ पर धारावाहिक प्रसारित हुए है।
को परास्त करके अपना विजय-ध्वज फहराया, तो शेष आचार्यों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण-भक्ति के तो वे एकमात्र आचार्य हैं। कृष्ण-भक्ति का ऐसा आचार्य न उनके जन्मधारणा को पर इन सैकड़ों वर्षों में उनको पराभूत करे ऐसा तो कोई नहीं पैदा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र आदि उनके अनुयायियों की संख्या अनन्त है। वाणाणसी के गोपाल-मन्दिर में उनका एक प्रसिद्ध पीठ है। जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी उनके मतावलम्बी विद्यमान हैं। तमिलनाडु, केरल और बिहार के सदृश्य कुछ दुर्भाग्य-ग्रस्त राज्य हैं जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को विभिन्न आयामों से पूर्णतया परिचित नहीं हो सके, यद्यपि इन स्थानों में उनको जानने वालों की कमी नहीं है।
यह पुस्तक आचार्य-श्री के अद्भुद व्यक्तित्व और चमरत्कारिक कृतित्व से सम्पूर्ण राष्ट्र को परिचित कराने के लिए ही यथासम्भव ललित एवं प्रवाहमान भाषा में पस्तुत की गई है।
समझना गलत होगा कि आचार्य मात्र कृष्णोपासक और कृष्ण-भक्ति के प्रचारक थे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी इनकी मुख्य चिन्ता के विषय थे। मनुष्य-मात्र को उसके आत्मबल और विश्वास से परिचित कराना इनका प्रमुख उद्देश्य था। यवनों से पददलित और देशी राजाओं के पारस्परिक विद्वेष के कारण राष्ट्र तो टूटन और बिखराव के कगार पर पहुँच ही चुका था, सामान्य जन बलात् धर्म-परिवर्तन और विदेशियों के निरन्तर वृद्धिशील आतंक से अवसाद-ग्रस्त हो, जीवन के प्रति ही उदासीन हो चले थे। ऐसी स्थिति में भक्ति ही एक मात्र सहारा थी। श्रीमदवल्लभाचार्य ने इस सूत्र को पकड़ा और उसके सहारे न केवल देश को, और विखंडन से बचाया अपितु जनता को अवसाद और भय से मुक्ति दे उनके अन्दर जिजीविषा भरने का भी प्रयास किया।
श्रीमदवल्लभाचार्य पहले आचार्य थे जिन्होंने सम्पूर्ण देश का तीन बार परिभ्रमण किया। उनके इन राष्ट्र-परिभ्रमणों से भी देशवासियों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता का परिचय मिलता है।
परिभ्रमण और प्रवचन से बचा उनका समय ग्रन्थ-लेखन और उनके इष्टदेव श्रीनाथजी के स्वरूप की सेवा-सुश्रूषा में व्यतीत होता था। श्रीनाथजी (भगवान कृष्ण का गोवर्द्धनधारी-रूप) को उन्होंने गिरिराज (गोवर्द्धन) पर प्रतिष्ठित किया था। उनके जीवनकाल तक श्रीनाथ जी इसी मंदिर में रहे। श्रीमद्वल्लभाचार्य भी घूम-फिरकर वहाँ आते रहे। सूरदास को भी उन्होंने श्रीनाथ जी के कारण अपने साथ जोड़ा। यह सब इस पुस्तक के पृष्ठों में विस्तार से मिलेगा।
आज भी गोवर्धन के समीप पारसौली नामक ग्राम के समीप चन्द-सरोवर के पास महाप्रभु श्रीमदवल्लभाचार्य की बैठक सुरक्षित है। उसी के पार्श्व में सूरदास की समाधि भी है। सूर-पंचशती के अवसर पर वहाँ से थोड़ा हटकर सूरदास को सूर की स्मृति में निर्मित हुआ सूर के गुरू आचार्य-श्री की सुधि लेने के लिए हिन्दी वालों को कोई स्थान चिन्ता नहीं रही।
राजस्थान में नाथद्वारा एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ है। तिरुपति के पश्चात् उसी का स्थान है। सैकड़ों-हजारों दर्शक वहाँ प्रतिदिन जाते हैं पर यह कितनों को पता है कि इस मन्दिर का विग्रह वही है जो श्रीमद्वल्लभाचार्य को गोवर्द्धन पर प्राप्त हुआ था और जिसकी पूजा-अर्चना उन्होंने गोवर्धन-स्थिति मन्दिर में आजीवन की थी ?
उनके मृत्युपरान्त, औरंगजेब के मूर्ति-भंजन-अभियान से घबराकर उनके यशस्वी पुत्र विठ्ठलनाथ इस विग्रह को गोवर्द्धन से हटाकर राजस्थान ले गए। वहाँ श्रीनाथजी के पहुँचने से ही ‘श्रीनाथद्वारा’ नगर बस आया। श्रीनाथ जी और महाप्रुभ में अभेद था। दोनों महाप्रभु की भक्ति के कारण दो स्वरूप पर एक प्राण हो गए थे। जो नाथद्वारा में श्रीकृष्ण विग्रह के दर्शन करते हैं, वे स्वतः महाप्रभु के भी दर्शन प्राप्त कर लेते हैं पर इस तथ्य में कितने भिज्ञ हैं ?
नहीं समझा जाए कि पुस्तक मात्र एक –दो वर्षों के श्रम की देन है। प्रायः हर वर्ष मेरी एक पुस्तक आ जाती है।, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक मात्र एक वर्ष में लिखी गई। मैं कई पुस्तकों पर एक साथ काम करता हूँ। इस पुस्तक ने तो कम-से-कम बीस वर्षों का समय लिया। ऐतिहासिक-पौराणिक पुस्तकों की मेरी रचना-प्रक्रिया यह है कि मैं विषय से सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रिक कर लेता हूं और उसका अध्ययन कर उसको आत्मसात करने के पश्चात् ही पुस्तक में हाथ लगाता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करता हूँ। इसमें सामग्री मिले या नहीं; कहीं-कहीं मिल जाती है पर विषय की प्रामाणिकता अवश्य सिद्ध हो जाती है। अतः मेरी हर कृति, अध्ययन, अन्वेषण और पूर्ण गवेषणा पर आधारित है।
इस कृति को पूर्ण होने में बीस वर्ष लगे यह अतिशयोक्ति नहीं। इसके आधार हैं।
नाथद्वार पहले-पहल मैं 1979 में गया था। बीस नहीं अपितु इक्कीस वर्ष पूर्व। वहाँ जाने पर पता लगा कि वहाँ का विग्रह श्रीमदवल्लाचार्य द्वारा पूजित है। नाथद्वारा मैं पुनः कम-से-कम चार बार गया। लोगों से वार्तालाप हुआ, सामग्री भी मिली।
जब मैं रेल-मन्त्रालय में संयुक्त निदेशक (राज्यभाषा) था तो मुझे चम्पारण्य के आसपास एक रेल-कार्यालय का निरीक्षण करने जाना पड़ा। मेरे हिन्दी –अधिकारी ने कहा कि कुछ दूर चम्पारण्य में श्रीमदवल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, आप देखना चाहेंगे ? मैं सहर्ष प्रस्तुत हो गया। झाड़-झंखाड़ों से निपटता हुआ मैं उस स्थान पर पहुँच ही गया जहाँ घोर जंगल में महाप्रभु का जन्म हुआ था। वहाँ एक स्मारक निर्माणाधीन था। वह तो अब भव्य रूप ले चुका होगा। इससे बाहर आया तो कुछ मकान-‘स्टॉल’ नए-नए बने मिले। वहाँ भी श्रीमदल्लभाचार्य से सम्बन्धित सामग्री और उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ उपलब्ध थे। यह 1982 की बात है। अब तो वहाँ बहुत-कुछ बन गया होगा।
मैंने वाराणसी में हनुमान-घाट के भी दर्शन किए जहाँ महाप्रभु का लालन-पालन हुआ था। वाराणसी के उन स्थानों को देख जो महाप्रभु से सम्बन्धित हैं।
गोवर्द्धन-(गिरिराज) जिस पर अब भी श्रीनाथ जी का प्राचीन भव्य मन्दिर अवस्थित है- के दर्शन मैंने कई बार किए। गोवर्द्धन की कई परिक्रमाएँ भी कीं जिनका वर्णन उचित नहीं। तिरुपति तो जाना हुआ ही, विंध्याचल, अयोध्या, हरिद्वार आदि भी गया।
महाप्रभु ने जहाँ-जहाँ रुककर भगवत-पाठ किया वहाँ-वहाँ उनकी बैठक बन गई। बैठक-स्थान एक स्मारक ही बन गया।
देश में ऐसी चौंसठ बैठकें वर्तमान हैं। सबको देखना सम्भव नहीं और आवश्यक भी नहीं। कई स्थानों पर एक या दो कमरे के जर्जर या मरम्मत किए छोटे भवन के सिवा कुछ नहीं मिलता। सामग्री आदि की तो बात ही नहीं। कुछ स्थानों को अवश्य अभी तक पूर्णतया सुरक्षित रखा गया है।
कांकरौली-स्थान, नाथद्वारा के बाद सर्वाधिक जाग्रत स्थल है।
गोकुल की बैठक भी आकर्षण रूप में सुरक्षित है। ब्रज अकादमी वृन्दावन (अब प्रायः बन्द) में रहते हुए एक गोकुलवासी मित्र के साथ मैं गोकुल भी गया। वहाँ समय-समय से उत्सव होते रहते हैं, और वल्लभाचार्य के भक्त वहाँ भरे पड़े हैं। लोगों के वार्तालाप करने से ज्ञात हुआ है कि उन्हें आज भी इस बात पर गर्व है कि महाप्रभु के चरण वहाँ पड़े थे और उन्होंने पर्याप्त समय वहाँ व्यतीत किया था। वृन्दावन और मथुरा में भी मैंने महाप्रभु से सम्बन्धित स्थलों के दर्शन किए।
वाराणसी का गोपाल मन्दिर वल्लभ-प्रेमियों का प्रसिद्ध पीठ है। मैं 1997 में वहाँ अपने मित्र श्री एस.सी.शर्मा के साथ गया। मेरा सौभाग्य कि वहाँ वल्लभ-वंश की अन्तिम वृद्ध महिला मठ की दूसरी ओर के मन्दिर में रहती थीं। प्रबन्धक से सूचना मिली तो मैंने उनके पास, दर्शन-हेतु निवेदन भिजवाया। अब तक मैं पुस्तक पर पर्याप्त कार्य कर चुका था ।
उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, ‘‘मैं अब किसी को ‘‘इंटरव्यू’’ आदि नहीं देती।
मैं विवश हुआ पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर सूचना भिजवाई कि मैं उनका इंटरव्यू नहीं लूँगा। एक प्रश्न भी नहीं पूछूँगा, अपितु मुख भी नहीं खोलूँगा। मैं महाप्रभु पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। उनके वंश की इस अन्तिम देवी के केवल दर्शन-मात्र से मेरी पुस्तक सार्थक हो जाएगी।
इस बार उनका हृदय पिघला। उन्होंने मुझे कहलवाया कि मैं अगले दिन दस बजे आऊँ और जब वे मन्दिर लौटने लगें तो मार्ग के किनारे खड़े होकर उनके दर्शन कर लूँ।
मैं दूसरे दिन पुनः वहाँ गया। यथास्थान खड़ा हो गया। एक स्वयंसेवक भी मेरे साथ था। वह मन्दिर से लौटने लगीं तो स्वयंसेवक ने पहचनवाया। श्वेतवस्त्रा वह वृद्धा, सरस्वती स्वरूप ही लग रही थीं। पास आईं तो मैंने धरती का स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया निवेदन किया। वे क्षण-भर को रुकीं। मेरा साहस बढ़ा। मेरा बन्द मुँह खुल पड़ा और मैंने संक्षेप में निवेदन किया, ‘‘ आप केवल अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी पुस्तक धन्य हो जाएगी। ’’
उनकी मुझ पर कुछ विशेष ही कृपा हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘तीन बजे आइए तो मैं आपको कुछ सामग्री दूँगी।’’
मैं पुनः तीन बजे आ गया, वे स्वयं तो नहीं आईं पर तीन दासियों के माध्यम से ढेर सारी सामग्री भिजवा दी-कई स्मारिकाएँ, कई मूल ग्रन्थ, कई संकलन। उतनी सामग्री मुझ अकेले के उठाए क्या उठे ? अन्ततः मैंने सेविकाओं से ही अनुरोध किया कि बाहर प्रबन्धक के कमरे तक वे उन्हें पहुँचा दें।
इस तरह इस पुस्तक पर महाप्रभु की वंशजा का आशीर्वाद भी अंकित है। यह मेरा अतिरिक्त सौभाग्य है।
गोपाल-मन्दिर के ही तत्कालीन पीठाधीश ने कोई दो घंटे तक महाप्रभु और शुद्धाद्धैत तथा पुष्टिमार्ग पर संक्षेप पर सार्थक रूप में प्रकाश डाला। मैं उनका ऋणी हूँ।
कठिन थी श्रीमदवल्लाभाचार्य-रचित ग्रंन्थों की उपलब्धि। यद्यपि उपन्यास में उनके संस्कृत गंन्थों का उद्धरण देना उचित नहीं था फिर भी उनके साहित्य, उनकी भाषा, उनके शिल्प, उनकी तर्क-शक्ति से भिज्ञता आवश्यक थी।
ब्रज-अकादमी वृन्दावन के संस्थापक-अध्यक्ष श्री 1008 श्री पाद बाबा (अब स्वर्गीय) ने न केवल मुझे अपने पुस्तकालय में महाप्रभु की बहुत-सी पुस्तकें उपल्ब्ध करा दीं अपितु मेरे प्रायः दो सप्ताह के वहाँ निवास के समय मेरी पूर्ण सुविधा का भी ध्यान रखा प्रभु उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।
पुस्तक-लेखन का आरम्भ इतने अध्ययन-अन्वेषण के पश्चात् 1994 में ही विधिवत आरम्भ हो गया था। यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं थी। इस मध्य मेरी कई पुस्तकें भी आ गईं पर वल्लभाचार्य बहुत कठिन सिद्ध हो रहे थे।
1999 अगस्त प्रायः तीन सौ टंकित पृष्ठ तैयार हो गये थे। सोचा था इतने ही प्रायः और लिखने होंगे; 2000 में तो पुस्तक आ ही जाएगी, पर दुर्भाग्य ऐसा कि अगस्त 1999 से जुलाई 2000 तक मैं दिल्ली में इस कार्य के लिए प्रायः एकाकी रहा। पर लिखने के नाम पर मैं प्रायः एक वर्ष में 50 पृष्ठ भी नहीं लिख पाया। कारण कुछ नहीं पर जिस लेखकीय ‘मूड’ की मैंने बात रखी थी, वह आड़े आ गईं। मेरा ‘मूड’ ही नहीं बना। आश्चर्य, ऐसा पहले कभी नहीं था, मैंने रचनाओं पर रचनाएँ देता गया हूँ। ‘मूड’ क्या है इसमें मेरा परिचय ही नहीं। पर इस बार हो गया।, शायद ऐतिहासिक से अधिक आध्यात्मिक प्रकृति की होने के कारण इस पुस्तक को किसी आध्यात्मिक स्थल पर ही समाप्त होना था।
मैं 19 जुलाई, 2000 को केवल एक सप्ताह के लिए दिल्ली से पटना आया। दिल्ली लौटने के लिए 26 जुलाई के आरक्षण को सहसा रद्द कराना पड़ा। कुछ आवश्यक कार्य आ गया। कार्य कुछ लम्बा ही खिंचता गया। प्रवास-अवधि अनिश्चित हो गई। मैं विविश पटना-सिटी के बालकिशनगंज के प्रसिद्ध आश्रम शाक्य साधना केन्द्र के संस्थापक एवं सुप्रसिद्ध तान्त्रिक एवं ज्योतिर्विद् प्रेम बाबा के यहाँ ठहर गया।
आश्रम का वातावरण आध्यात्मिक होने के अतिरिक्त रमणीय भी है। पेड़-पौधों, लता-बल्लियों से युक्त यह एक तपोवन-सा ही लगता है। प्रेम बाबा अपने यन्त्र-तन्त्र तथा प्रायः अहर्निश हवन पूजन के द्वारा लोगों का मनस्पात हरते रहते हैं। उनकी मनोकांक्षाएँ पूर्ण करते हैं। उनकी साध्वी पत्नी पूनम माता आश्रम की व्यवस्था भी चलाती हैं और अपने नियमित पूजा-पाठ का ध्यान भी रखती हैं।
एक दिन पेड़-पौधों से घिरे आश्रम के बरामदे में बैठा मैं सोच रहा था कि बाबा के यहाँ सैकड़ों लोग नित्य आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे वल्लभाचार्य का क्या होगा ? वह अधूरे ही पड़े रहने को आरम्भ हुए है क्या ?
स्थान, सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। बाबा द्वारा निरन्तर जारी जप और हवन ने इसे मनोकामना-पूर्ति का स्थल ही बना दिया है।
मेरी रुकी कलम भी दूसरी ही सुबह (6 अगस्त) को चल पड़ी और ऐसी चली कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। आध्यात्मिक ऊर्जा ने जैसे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी प्रदान की। सरकारी कार्य तो अपनी गति से हो रहा था पर मैं जो नित्यक्रिया के पश्चात् छह बजे सुबह लिखने बैठता तो छह बजे शाम को ही उठता। बीच में केवल नाश्ता और भोजन के लिए समय निकालता। यह क्रम महीनों अबाध गति से चला, फलस्वरूप पुस्तक यहीं रहते-रहते समाप्त हो गईं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आश्रम की आध्यात्मिकता ने ही इस असम्भव-से प्रतीक होते कार्य को सरल बनाया। मैं प्रेम बाबा और उनकी देवी-स्वरूपा पत्नी पूनम मैंया का बहुत कृतज्ञ हूँ।
इस पुस्तक के सम्बन्ध में एक-दो बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है।
प्रथम तो यह है कि मैंने इसमें औपन्यासिक शिल्प को एक नया आयाम दिया है। ऐसे उपन्यास में पाठक के आमने-सामने नहीं आना चाहिए। मैंने पूरी तरह इसे अमान्य कर दिया है। ऐसे भी उपन्यास में मूलतः उपन्यासकार ही आदि से अन्त तक बोलता है भले ही वह विभिन्न पात्रों के माध्यम से बोले। उपन्यासकार की इस अप्रत्यक्ष उपस्थिति को मैंने कई बार स्थानों का प्रत्यक्ष कर दिया है। उपन्यासकार और पाठक आमने-सामने हुए हैं। इसे अगर समीक्षक-उपन्यास-विधा का हनन मानें तो उन्हें इसका अधिकार प्राप्त है। किंतु किसी भी विधा में एक ही शिल्प, एक ही शैली अथवा ‘टेकनिक’ को शव की तरह अपने स्कन्धों पर ढोए जाने का मैं कायल नहीं हूँ। समीक्षा के मापदण्ड बदलते रहते हैं तो लेखक इतना निरीह क्यों, कि वह औपन्यासिक शिल्प के गढे-गढ़ाए ढाँचे में बँधा रहे ? उसे तोड़ना उसका अधिकार है। उसकी मौलिकता। कई अध्यायों के प्रारम्भ में मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी आई जो मेरे चिन्तन को मुखर करती है और आगे जाने वाले घटनाक्रम को भी इंगित करने में सक्षम है। यह पहले भी कई उपन्यासों में हुआ है। पाठकों ने इसे सराहा है तो आलोचकों को बना-बनाया बहाना मिल गया है।
इस उपन्यास में लेखक-पाठक-संवाद कुछ अधिक ही दृष्टिगोचर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पाठक पहले की तरह ही मेरी शैली से प्रसन्न होंगे और समीक्षक भी अपनी आदत के अनुसार अप्रसन्न। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।, मैंने पुस्तक को अधिक आकर्षण और पठनीय बनाने हेतु ही इस शिल्प को अपनाया है। खैर, कई विदेशी लेखक तो इस ‘तकनीक’ का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं।
एक बात और पुस्तक में मूल कथा के साथ कई अन्तर्कथाएँ मिलेंगी। जैसा आरम्भ में कहा, एक ऐतिहासिक सह-आध्यात्मिक उपन्यास बहुत हद तक सामान्य पाठक के लिए दुहरू हो सकता है। अन्तर्कथाएँ औपन्यासिक कृति को प्राणवन्त और प्रासंगिक बनाती हैं और पाठकों को मनोरंजक में सहायक होती हैं। अतः, उपन्यास के कलेवर के विस्तार के कतरे को झेलते हुए भी मैंने अन्तर्कथाओं से मुँह मोड़ना उचित नहीं समझा। इनमें से कुछ पाठकों की परिचित भी होंगी पर उन्हें परोसने का अंदाज निश्चित ही भिन्न होगा। समीक्षक इनको लेकर कुछ भी कहने को स्वतन्त्र हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book