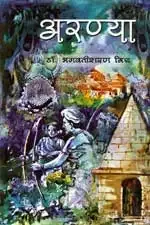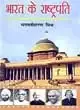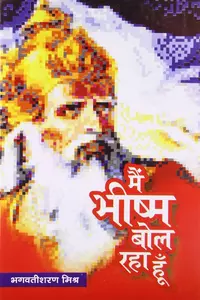|
उपन्यास >> अरण्या अरण्याभगवतीशरण मिश्र
|
210 पाठक हैं |
||||||
बस्तर की आदिवासी संस्कृति एवं समृद्ध परम्परा तथा वहाँ की अधिष्ठात्री देवी दन्तेश्वरी की पृष्ठभूमि पर एक पौराणिक, सह ऐतिहासिक, सह आँचलिक, आध्यात्मिक औपन्यासिक कृति
Aranya a hindi book by Bhagwati Sharan Mishra - अरण्या - भगवतीशरण मिश्र
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रख्यात उन्यासकार डॉ. भगवतीशरण मिश्र की गणना अग्रणी पौराणिक और ऐतिहासिक कृतिकार के रूप में होती है।
इनका उपन्यास ‘शान्तिदूत’ सम्पूर्णतः ‘इन्टरनेट’ पर आकर इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान कर चुका है। बस्तर की आदिवासी संस्कृति एवं समृद्ध परम्परा तथा वहाँ की अधिष्ठात्री देवी दन्तेश्वरी की पृष्ठभूमि पर एक पौराणिक सह ऐतिहासिक सह आँचलिक आध्यात्मिक औपन्यासिक कृति जिसमें प्राचीनतम सभ्यता और आधुनिक युग-बोध का आकर्षण सम्मिश्रण उपलब्ध है।
इनका उपन्यास ‘शान्तिदूत’ सम्पूर्णतः ‘इन्टरनेट’ पर आकर इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान कर चुका है। बस्तर की आदिवासी संस्कृति एवं समृद्ध परम्परा तथा वहाँ की अधिष्ठात्री देवी दन्तेश्वरी की पृष्ठभूमि पर एक पौराणिक सह ऐतिहासिक सह आँचलिक आध्यात्मिक औपन्यासिक कृति जिसमें प्राचीनतम सभ्यता और आधुनिक युग-बोध का आकर्षण सम्मिश्रण उपलब्ध है।
अपनी बात
मैंने सामाजिक एवं ऐतिहासिक-पौराणिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। किंतु गत एक दशक से अधिक मेरी परिगणना विशेषकर ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यासकार के रूप में होती है। इधर इसमें एक और आयाम जुड़ गया है। वह है आध्यात्मिक।
जब से मैंने ‘पवनपुत्र’ तथा श्रीमद्वल्लाभाचार्य पर आधारित दो खण्डीय उपन्यास ‘पावक’ और ‘अग्निपुरुष’ (आत्माराम एण्ड सन्स) की रचना की है। तब से यह आध्यात्मिकता मेरे साथ विशेष रूप से चस्पा हो गई है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं अपितु मैं तो यह मानता हूँ कि यह युग आध्यात्मिक पुनरुत्थान का युग है।
स्पष्ट कहना पड़ेगा कि विभिन्न अनास्थावादी आन्दोलनों की हवा कब की निकल गई। तथाकथित प्रगतिवाद और अनीश्ववाद जिस भूमि पर उत्पन्न हुए वहाँ का साम्राज्य सौ वर्ष पूर्ण किए बिना ही खण्ड-खण्ड हो गया। ईश्वर को नकारनेवाले ईश्वर को आलिंगनबद्ध करने दौड़े। गिरजों और मस्जिदों के बन्द कपाट खुल गए। विडम्बना तो यह है कि इन वादों से प्रतिबद्ध लोग इस देश में अभी तक इनके शवों के स्तम्भों पर ढोए चल रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि यही चन्द लोग अपने को मुख्य धारा के प्रतिनिधि ही नहीं मानते हैं अपितु शिष्यों की एक अटूट परम्परा बनाकर नई पीढ़ी के युवा लेखक-लेखिकाओं को दिग्भ्रमित करने से भी नहीं चूकते। इनसे सम्बद्ध पूर्वाग्रहग्रस्त समीक्षकों, आलोचकों के अनावाश्यक दम्भ के गुबार को फोड़ने के लिए यह कहना ही पर्याप्त होगा कि इस कथन में पर्याप्त सच्चाई है कि एक असफल लेखक ही समीक्षक बनता है।
दुर्भाग्य तो यह है कि इन स्वयंभू समीक्षकों ने अब तक कुछ विशेष प्रदान नहीं किया। इनमें न कोई रामचन्द्र शुक्ल बन सका न महावीर प्रसाद द्विवेदी। पर अवसादग्रस्त लोग इनके चरण-चुम्बन को विवश हैं और अपनी मौलिकता को ताक पर रखकर इनके कभी के चूके सिद्धांतों और वादों के पक्षधर बन अपठनीय और अनास्थापूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत करने को विवश हैं। यह इस पीढ़ी का दुर्भाग्य ही है।
मैंने इस युग को आध्यात्मिक पुनरुत्थान का युग कहा था। अपनी इस उक्ति पर मैं पूर्णतया कायम हूँ। और यह मेरी ही नहीं अनेक प्रकार की अनुभूतियों पर आधृत है। मैंने अपनी औपन्यासिक कृति ‘पावक’ की भूमिका में एक बात लिखी थी उसे यहाँ उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत होता है, ‘‘गलत है कि अध्यात्म धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है। वैश्वीकरण और उन्मुक्त बाजार के प्रभाव ने नई पीढ़ी के कुछ लोगों को दिग्भ्रमित अवश्य किया है किन्तु देखकर आश्चर्य होता है कि मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में नवयुवकों-नवयुवतियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उन्हें भी अध्यात्म में आस्था की एक नई किरण दिखाई पड़ने लगी है।’’
मेरा यह कथन हाल ही में 28 मई के ‘इण्डिया टुडे’ में प्रकाशित शेफाली वासदेव के एक निबन्ध से सम्पुष्ट होता है। इस लेख का शीर्षक भी सचमुच यथार्थाधारित एवं प्रतीकात्मक बन पड़ा है, ‘है प्रभु से मिलने की प्यास’। पर्याप्त अन्वेषण और परिवेक्षण के बाद इस लेख में कई चौकाने वाली बातें सामने आई हैं। एक उद्धरण प्रस्तुत है : ‘‘आध्यात्मिकता का यह नया रूप फैशन-विशेषज्ञों से शेयर दलालों और पेशेवरों से लेकर गृहणियों को समान भाव से आकर्षित कर रहा है। पहले सत्संग अपने को दूसरों से अधिक साबित करने का उपक्रम माना जाता था। इन दोनों धर्मस्थलों, ध्यान-केन्द्रों और विभिन्न सम्प्रदायों के आश्रम में बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। इनमें से बहुत से पेशेवर भी होते हैं जो सत्संग में जाने के लिए अन्य पार्टियों का कार्यक्रम भी त्याग देते हैं।’’
लेख में कई आध्यात्मोन्मुख लोगों से साक्षात्कार भी किया गया है। इनमें हर तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति ने जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र सूक्ष्म जीव-विज्ञान के और जो एशिया में इस विषय के विशेषज्ञों में से माने जाते थे का कथन है—‘‘नेत्र विज्ञानी तो बहुत से हैं पर दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो दुनिया के लोगों के नेत्र खोल सकें।’’ अब एक एशिया-प्रसिद्ध नेत्र वैज्ञानिक स्वयं अन्तर्चक्षुओं को खोलने की बात करें तो मेरा यह कहना कि यह युग आध्यात्मिक पुनरुत्थान का है सच है या नहीं ?
इसी लेख के अनुसार एक अड़तीस वर्षीय युवती कृपाल माथुर कहती हैं—‘‘मेरी जिन्दगी में एक दुःखद हादसे के बाद सत्संग के प्रति मेरा रुझान तेजी से बढ़ा। इन दो घण्टों में मैं अतिरिक्त जीवनशक्ति का अनुभव करती हूँ।’’
इस निबन्ध को पढ़ने से आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक सत्संगों में भाग लेनेवाले केवल बूढ़े और चुके हुए लोग नहीं हैं। यह बात पहले भी रेखांकित की गई है। इस निबन्ध से उद्धरण लें तो ‘‘सत्संग-हालों में हर हफ्ते सम्मिलित होने वाले हजारों लोगों में रंग-बिरंगे बालों, चमकती नेलपालिश और छोटे गोटेदार बैगवाली युवतियाँ आसानी से देखी जा सकती हैं। कुछ तो नई डिजाइन की कुर्तियां और कुछ जीन पहनकर आती हैं। इसी तरह बहुत से युवा व्यवस्थित ढंग से कुर्ता पाजामा पहने, मोबाइल बन्द करके हाथ में बैठे मिलते हैं, जिसे ईश्वर के साथ उनके उस साप्ताहिक मिलन में किसी तरह का व्यवधान न आए। ये युवा अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ अत्यन्त विनम्रता जताते हैं। नई पीढ़ी की पहचान माने जानेवाली अकड़ और छिछोरापन उनमें यहाँ कतई नहीं दिखता।’’
मैंने अपने उपन्यास ‘पावक’ से जो उद्धरण ऊपर दिया है वह 2001 का और यह निबन्ध मई 2003 का है। क्या अब भी कोई यह कहने का दुस्साहस कर सकता है कि नई पीढ़ी भी निरन्तर अध्यात्म की ओर आकृष्ट होती जा रही है। अपवादों की बात भी नकारी नहीं जा सकती। ऐसे युवाओं की भी कमी नहीं जो ‘खाओ-पीओ, मौज मनाओ’, की उक्ति के कायल हैं। पर देर-सबेर वे भी अध्यात्म की शरण में आयेंगे ही क्योंकि भोग एक सीमा के बाद सुख और आनन्द का कारक नहीं रहता। इसका अनुभव उन धनाढ्य विदेशियों से पूछें जो सब कुछ छोड़ शान्ति के लिए भारत की ओर मुख करते हैं।
आप अपना अनास्थावादी और अनीश्वरवादी राग अलापते रहिए। लेकिन जिन्हें अध्यात्म ने सुकून दिया है वे उसे आपके कहने से ठुकरा नहीं देंगे।
गलत है कि वैज्ञानिक दैवी शक्तियों में विश्वास नहीं करते। आइन्स्टिन ने भी खुले शब्दों में आपने कई अन्वेषणों के मूल में किसी आन्तरिक स्फुरणा की बात स्वीकारी थी। यह दैवी इंगित नहीं तो और क्या था ? विख्यात नेत्र वैज्ञानिक का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। ‘इण्डिया टुडे’ के समान प्रतिष्ठित पत्रिका के इसी लेख में एक इलैक्ट्रिक इंजीनियर योगेश का कहना है कि ‘‘ये भजन तुरन्त चमत्कारिक असर डालते हैं।’’
अब जब वैज्ञानिक भी चमत्कारों से परहेज नहीं करते तो मैंने माता दन्तेश्वरी के चमत्कारों का उल्लेख कर कौन-सा गलत काम किया है ? दन्तेश्वरी का उल्लेख आ ही गया तो मैं यह स्पष्ट करूँ कि यह उपन्यास बस्तर की अद्भुत आदिवासी संस्कृति और उसकी समृद्ध परम्परा के साथ-साथ शक्तिपीठ माता दन्तेश्वरी को केन्द्र में रखकर ही लिखा गया है। इसमें आदिवासियों के लोकगीत हैं जो मातृ-मन्दिर की घण्टियों की संगीत ध्वनि भी है और आदिवासियों किशोर-किशोरियों की निश्छल प्रेमगाथा भी।
ऐसा बहुत कम स्थानों पर है लेकिन बस्तर क्षेत्र के लिए जो कभी दण्डकारण्य कहा जाता था और जहाँ राम, सीता की खोज में भटकते रहे थे यह एक कठोर सत्य है कि दन्तेश्वरी मन्दिर के इर्द-गिर्द ही यहाँ की सामाजिक-पारिवारिक एवं राजनीतिक गतिविधियाँ पूर्णतया केन्द्रित हैं। आदिवासियों की देवी तो यह नाममात्र को हैं, यहाँ की सभी तरह की आबादी उनकी छत्रछाया में पलती है। साथ ही दूर-दिगन्त के लोग भी दन्तेश्वरी देवी के प्रभाव, उनकी शक्ति तथा मनोकामना-पूर्ति करने की उनकी अनुकम्पा से आकृष्ट होकर यहाँ आते रहते हैं।
हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि यह औपन्यासिक कृति मुख्यतः दन्तेश्वरी पर ही आधृत है। आदिवासी जीवन और आदिवासियों की संस्कृति एवं परम्परा इस कृति में अवश्य है और जहाँ तक सम्भव है वह अपनी सम्पूर्णता में उभरकर आई है किन्तु यह सबकुछ गौण है, प्रमुख हैं माता दन्तेश्वरी ही।
दन्तेश्वरी में चमत्कारी शक्ति है तो है, उसकी उपेक्षा कर अपने को अत्याधुनिक कहाने का मुझे शौक नहीं। फिर जब बात सार्वजविक रूप से जिम्मेवार लोगों से स्वीकारी जाएँ तो उसे नकारने का मुझे क्या अधिकार है ? एक उदाहरण प्रस्तुत है। अभी-अभी 14 जुलाई के टाइम्स आफ इण्डिया में एक समाचार आया जिसे श्री लवकुमार मिश्रा ने रायपुर से दिया है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है।
इस समाचार के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने उद्घोषित किया है कि माता दन्तेश्वरी उनके स्वप्न में आई और उन्होंने आदेश दिया कि क्षेत्र के सभी देव-गुड़ियों (ग्रामीण मन्दिरों) का पुनरुद्धार किया जाए। इस स्वप्न पर विश्वास कर श्री जोगी ने इस समाचार के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया।
‘टाइम्स आफ इण्डिया’ एक प्रतिष्ठित और अतिपठित समाचार पत्र माना जाता है। इससे किसी अन्धविश्वास को प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं हो सकती। अतः मैंने अगर दन्तेश्वरी की चमत्कारिक शक्ति एवं महत्ता को रेखांकित किया है तो मैं न अन्धविश्वास को प्रश्रय दे रहा हूँ न देवी के असंख्य अनुयायी ही अन्धविश्वासी हैं। अन्धविश्वासी वस्तुतः वे हैं जो आँखें होते हुए भी सत्य पर संशय का पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। जिनका मिथ्या अहं कटु यथार्थ को पचा नहीं पाता। जो आँखें रहते भी अन्धे की तरह व्यवहार करते हैं। अन्धविश्वासी तो वही हैं न कि वो जो अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति का साहस करते हैं। मानकर चलना पड़ेगा कि यह विश्व दैवी शक्तियों से संचालित है और इन शक्तियों में जिन्हें चमत्कार कहते हैं वह करने की भी क्षमता है। अपने अनुभव के आधार पर कहना पड़ेगा कि माता दन्तेश्वरी में भी अपार चमत्कारी शक्तियाँ हैं। कोई इनका लाभ न उठा सके तो यह उसका दुर्भाग्य है।
हाँ यह पुस्तक मुख्यतः मन्दिर पर आधृत है। प्रश्न उठ सकता है कि क्या मात्र मन्दिर पर कोई उपन्यास गढ़ा जा सकता है। उत्तर उपस्थित है। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पर दो विशिष्ट उपन्यास आ चुके हैं। असम की कामाख्या देवी पर भी आधृत उपन्यास पिछले वर्षों ही आया।
यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह औपन्यासिक कृति काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थाधारित है। इसकी रचना के लिए पर्याप्त परिभ्रमण, संवाद, गवेषण एवं सामग्री-चयन तथा स्वाध्याय का सहरा लिया गया है।
ऐतिहासिक-पौराणिक लेखन की मेरी यही विधि अथवा रचना-प्रक्रिया रही है। मैं सर्वप्रथम उनसे सम्बद्ध स्थानों का भ्रमण करता हूँ फिर उनसे सम्बन्धित जितनी सामग्री प्राप्त हो सकती है उतनी एकत्रित करता हूँ और उसे आत्मसात करने के पश्चात् ही लिखने बैठता हूँ। परिभ्रमण के क्रम में व्यक्तियों से संवाद भी होता है। उसका भी यथासाध्य उपयोग रचना के सृजन के समय किया जाता है। अरण्या लिखने के पूर्व मैंने दो बार बस्तर क्षेत्र एवं दन्तेश्वरी मन्दिर का भ्रमण किया। जगदलपुर तथा अन्य स्थानों से आदिवासी-जीवन एवं देवी मन्दिर से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित की। आदिवासी एवं गैर आदिवासी लोगों से उनकी संस्कृति, परम्परा एवं सर्वोपरि देवी दन्तेश्वरी में उनकी आस्था के कारणों के सम्बन्ध में वार्तालाप किया। इन वार्तालापों और प्राप्त सामग्री के अध्ययन के पश्चात् ही अरण्या रची गई।
यह मैं नहीं मानता कि यथार्थपरक होने के पश्चात् भी इसमें कल्पना का स्थान शून्य है। कल्पना किसी जीवन्त कृति विशेषकर रचनात्मक कृति का प्राण है। स्वीकार करना पड़ेगा कि जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ मैंने कल्पना को खुलकर खेलने दिया। जब भी अवसर मिला है प्राकृतिक वर्णन को पर्याप्त स्थान दिया है। इससे पुस्तक की पठनीयता में निश्चित ही अभिवृद्धि हुई है।
एक बात और कहनी पड़ेगी माता दन्तेश्वरी पर मुख्यतः आधृत होने के पश्चात् भी यह कृति किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय से सम्बद्ध नहीं है। पाठक पाएँगे कि जहाँ पुस्तक में गीता का उद्धरण हैं वही ‘बाइबिल’ के भी कुछ कम नहीं हैं। इस्लाम का भी उल्लेख है। हाँ यह ‘स्यूडो स्कुलरिज्म’ के युग की एक पूर्णतया ‘सेक्युलर’ कृति है।
पुस्तक की भाषा और शिल्प के सम्बन्ध में कुछ कहना पड़ेगा।
भाषिक सौंन्दर्य पर मेरा सदा जोर रहा है। मैं तत्सम शब्दों का आग्रही हूँ। कभी-कभी कुछ कठिन शब्द भी अवश्य आ जाते हैं पर भाषा की प्रवहमानता में वे ऐसे घुलमिल जाते हैं कि पठनीयता में कभी बाधा नहीं आती। गति को रोक नहीं पाते।
कहीं-कहीं पत्रानुसार भी भाषा का प्रयोग करना पड़ा है पर ऐसा कम ही हुआ क्योंकि पुस्तक को तो अन्ततः हिन्दी में ही होना या, अतः आदिवासी भाषाओं का यत्र-तत्र दिखाने भर का प्रयोग पठनीयता में बाधक ही बनता।
पुस्तक की आध्यात्मिकता को तो आरम्भ में रेखांकित किया गया पर इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पक्ष अछूते ही रह गए क्योंकि सच कहा जाए तो यह पुस्तक पौराणिक एक ऐतिहासिक सह अध्यात्मिक है।
जहाँ तक पौराणिक की बात है सती के मोह और उसके पिता दक्ष प्रजापति की कथा पुराणाधारित है। पुराणों में किसी विषय को लेकर थोड़ा-बहुत मत-वैभिन्य रहता ही है. अतः अगर यह विवरण किसी को अपने अभिज्ञान से किंचित भिन्न लगे तो उसमें लेखक का कोई दोष नहीं।
मूल ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ मैं नहीं करता। इस पुस्तक में भी नहीं हुआ है। हाँ औपन्यासिक तकादों के कारण कुछ काल्पनिक पात्र एवं घटनाएँ अवश्य डालनी पड़ी हैं जिनकी पहचान कठिन नहीं होगी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक काल-खंड पर ही आधृत है। जो उपन्यास बनाया जा सकता था, बस्तर के किसी काल-खण्ड को मैंने चुना है। यह आज से प्रायः छह सौ वर्ष पुराना है।
उपन्यास को उसी काल में छोड़ देना मैंने उचित नहीं समझा है और एक संक्षिप्त उपसंहार के द्वारा बस्तर तथा उसकी अधिष्ठात्री देवी माता दन्तेश्वरी की अद्यतन स्थिति से भी पाठकों को परिचित कराना उचित समझा है। आश्चर्य है कि प्रायः छह सौ वर्ष की सततता आज भी बनी हुई है। आदिवासियों की संस्कृति और परम्परा में शायद ही कोई परिवर्तन आया है। हाँ, उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति में विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात् स्वाभाविक परिवर्तन आया है जो उनके पक्ष में है। उपन्यास की आधार-भूमि माता दन्तेश्वरी की लोकप्रियता में इन वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई एवं सभ्यता तथा आधुनिकता की किरणों के इस क्षेत्र की सारी गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। आश्चर्य हो सकता है पर यह सत्य है कि बस्तर के जन-जीवन का संचालन-सूत्र अभी भी माता दन्तेश्वरी के ही सर्व-समर्थ करों में है। दूर-दराज के भक्तों-दर्शकों का तो यह स्थान स्वेच्छा-पूर्ति के तीर्थ के रूप में निरन्तर अधिकाधिक प्रसिद्ध होता ही जा रहा है। मार्ग पहले की अपेक्षा अधिक सुगम हो गया है। अब जंगलों के दुर्गम पथों से नहीं जाना पड़ता। रायपुर (जो मध्यप्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बनने पर उसकी राजधानी बना) से सीधी सड़क आती है। दक्षिण से आये तो विशाखापत्तनम् से जगदलपुर और वहाँ से दन्तवेड़ा तक दन्तेश्वरी मन्दिर तक विश्वसनीय सड़क मार्ग है। जगदलपुर स्वयं एक रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ तक रेलगाड़ी से पहुँचने के पश्चात् सड़क मार्ग से एक छोटी यात्रा ही मन्दिर तक करनी पड़ती है जिसके लिए टैक्सी, टैम्पो से लेकर हर सवारी उपलब्ध है।
मंदिर के पास कई दुकानों में माता के पूजा-पाठ की सभी सामग्री मिलती है। इधर की देवियों को लहंगा चुनरी या प्रॉक तक अधिक प्रिय हैं। माता दन्तेश्वरी के परिधान में भी इन्हीं का उपयोग होता है। ये परिधान, भक्त खरीदकर अपने साथ भी ला सकते हैं।
उपन्यास के शिल्प की बात होते-होते रह गई। जैसे यह उपन्यास एक तरह से पूरी तरह देवी दन्तेश्वरी द्वारा ही लिखित है, इसी तरह, प्रतीत होता है, इस भूमिका पर भी वे हावी हैं। जो चीज जहाँ चाहोगी, वहीं आयेगी।
तो शिल्प पर भी बात कर ही लें। मेरे उपन्यास की एक विशेषता है कि वे उद्देश्यपरक तो होते ही हैं, कहीं-कहीं वे चिन्तनपरक भी होते हैं। प्रायः अध्यायों का आरम्भ कुछ ऐसी चिन्तनशील बातों से होता है जिससे लेखक के दार्शनिक मनोभाव तो स्पष्ट होते ही हैं, अध्याय में आने वाले विषय का भी पूर्वाभास हो जाता है। इससे मेरे उपन्यासों की लोकप्रियता बाधित नहीं हुई है अपितु उसके फलस्वरूप मेरा एक विशेष पाठक-वर्ग प्रस्तुत हुआ है। यही कारण है 1983-84 में प्रकाशित उपन्यासों ‘पहला सूरज’ और ‘पवनपुत्र’ के संस्करण अभी तक होते जा रहे हैं।
औपन्यासिक विधा को एक गढ़े-गढ़ाएँ साँचे में बंधे देखने वालों को यह प्रयोग रास नहीं भी आया और लोग उंगली लगाने में भी पीछे नहीं रहे। इसका उत्तर मैंने गतवर्ष प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘पावक’ में अच्छी तरह दिया है, उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ना केवल इतना है कि ऐसे शिल्प को अपनाने के लिए सामर्थ्य भी आवश्यक है। केवल कथोपकथन की बैशाखी के सहारे उपन्यास गढ़ देने वाले इस चिन्तनपरक शिल्प पर किधर से हाथ आजमाएँगे ? बात कड़वी लग सकती है पर वह कड़वी हमें भी लगती है, जब कहा जाता है कि ऐतिहासिक-पौराणिक उपन्यासों की क्या आवश्यकता है, उनके बदले पुराण, इतिहास ही नहीं पढ़ लें ? उत्तर है कि आप पौराणिक उपन्यास ही नहीं पढ़ सकते तो पुराण क्या खाकर पढ़िएगा ? रह गई बात इतिहास की तो सबको विदित है कि इतिहास एक नीरस विषय है। उसे सरसता प्रदान करने के लिए ही ऐतिहासिक उपन्यासों की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों का चले तो हिन्दी साहित्य को आचार्य चतुरसेन शास्त्री के ‘वयं रक्षाम्:: ‘वैशाली की नगर वधू’, वृन्दालाल वर्मा के ‘गढ़ कुंडाल’ हजारी प्रसाद द्वेवेदी के ‘चारु-चन्द्र लेख’ तथा बाणभट्ट’ की आत्म कथा’ और अमृतलाल नागर के ‘मानस के हंस’ तथा ‘खंजन नयन’ और इस लेखक के ‘पावक’ तथा पीताम्बरा’ से वचंति ही रहना पड़े।
और पुराण-इतिहास को क्या केवल उपन्यासकारों ने ही अपनी उपजीव्य बनाया है ? काव्यकारों ने नहीं ? यदि यही बात रहती है तो प्रसाद की ‘कामायनी’, मैथलीशरण गुप्त का ‘साकेत’, हरिऔध का ‘प्रिय प्रवास’ तथा दिनकर की ‘रश्मिरथी’ और ‘कुरुक्षेत्र’ किधर से आते ?
पौराणिक-ऐतिहासिक उपन्यास-लेखन की धारा बहुत पूर्व से चल पड़ी है और वह इधर कुछ नए लेखकों के सहयोग से पुस्टतर ही हुई है। अब तो मैंने इसमें अध्यात्म के उफनते प्रवाह को भी समेट लिया है। किसी पाठक-समीक्षक, में शक्ति हो तो इस प्रवाह को अवरुद्ध करके दिखा दे। मैं पुनः नई पीढ़ी में जगी अध्यात्म-सम्मान का स्वागत करता हुआ हूँ। तथा जिस आध्यात्मिक पुनरुत्थान की मैंने चर्चा की है उसमें रचनात्मक अवदान के लिए सहकर्मी उपन्यासकार बन्धुओं का आह्वान करता हूँ।
मैं इस भूमिका को और अधिक नहीं खींचना चाहता। शेष बातें पुस्तक स्वयं बोलेगी।
इस अवसर मैं कुछ लोगों का साधुवाद अवश्य करना चाहूँगा जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेरणा इस पुस्तक लेखन में मिली है। इनमें प्रमुख है सांसद एवं साहित्यकार तथा लन्दन में भारत के भूतपूर्व राजदूत लक्ष्मी सिंघवी, साहित्यकार बन्धुगण सर्वश्री राजेन्द्र अवस्थी, जयप्रकाश भारती, डॉ. श्याम सिंह शशि, डॉ. सतीश राजपुस्करणा, श्री कृष्णानन्द, कवि समीक्षक डॉ. शिवनारायण, भागनेघ बैजनाथ पाठक सशक्त सम्पादक एवं उपन्यास श्री उदयराज सिंह, सुदामा मिश्र तथा बिहार के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री के.के. श्रीवास्तव और उनकी विदुषी धर्मपत्नी।
आत्माराम एण्ड सन्स के श्री सुशील पुरी एवं उनके पुत्र श्री सुधीर पुरी एवं उनके भतीजे श्री योगेश्वर पुरी का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने पुस्तक को यथाशीघ्र इतने आकर्षक कलेवर प्रस्तुत किया।
श्री सुभाष तनेजा का मैं विशेष आभार मानता हूँ जिन्होंने इस पाण्डुलिपि को प्रस्तुत करने में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की।
अन्ततः यह पुस्तक माता दन्तेश्वरी की कृ़पा का ही सुफल है जिनकी अन्तर्प्रेरणा के बिना यह कार्य पूर्ण नहीं होता। मैं उन्हें अन्तर्मन से अपना नमन निवेदित करना चाहता हूँ और उनसे अभ्यर्थना करता हूँ कि वे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा का वर्षण करती रहें।
जब से मैंने ‘पवनपुत्र’ तथा श्रीमद्वल्लाभाचार्य पर आधारित दो खण्डीय उपन्यास ‘पावक’ और ‘अग्निपुरुष’ (आत्माराम एण्ड सन्स) की रचना की है। तब से यह आध्यात्मिकता मेरे साथ विशेष रूप से चस्पा हो गई है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं अपितु मैं तो यह मानता हूँ कि यह युग आध्यात्मिक पुनरुत्थान का युग है।
स्पष्ट कहना पड़ेगा कि विभिन्न अनास्थावादी आन्दोलनों की हवा कब की निकल गई। तथाकथित प्रगतिवाद और अनीश्ववाद जिस भूमि पर उत्पन्न हुए वहाँ का साम्राज्य सौ वर्ष पूर्ण किए बिना ही खण्ड-खण्ड हो गया। ईश्वर को नकारनेवाले ईश्वर को आलिंगनबद्ध करने दौड़े। गिरजों और मस्जिदों के बन्द कपाट खुल गए। विडम्बना तो यह है कि इन वादों से प्रतिबद्ध लोग इस देश में अभी तक इनके शवों के स्तम्भों पर ढोए चल रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि यही चन्द लोग अपने को मुख्य धारा के प्रतिनिधि ही नहीं मानते हैं अपितु शिष्यों की एक अटूट परम्परा बनाकर नई पीढ़ी के युवा लेखक-लेखिकाओं को दिग्भ्रमित करने से भी नहीं चूकते। इनसे सम्बद्ध पूर्वाग्रहग्रस्त समीक्षकों, आलोचकों के अनावाश्यक दम्भ के गुबार को फोड़ने के लिए यह कहना ही पर्याप्त होगा कि इस कथन में पर्याप्त सच्चाई है कि एक असफल लेखक ही समीक्षक बनता है।
दुर्भाग्य तो यह है कि इन स्वयंभू समीक्षकों ने अब तक कुछ विशेष प्रदान नहीं किया। इनमें न कोई रामचन्द्र शुक्ल बन सका न महावीर प्रसाद द्विवेदी। पर अवसादग्रस्त लोग इनके चरण-चुम्बन को विवश हैं और अपनी मौलिकता को ताक पर रखकर इनके कभी के चूके सिद्धांतों और वादों के पक्षधर बन अपठनीय और अनास्थापूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत करने को विवश हैं। यह इस पीढ़ी का दुर्भाग्य ही है।
मैंने इस युग को आध्यात्मिक पुनरुत्थान का युग कहा था। अपनी इस उक्ति पर मैं पूर्णतया कायम हूँ। और यह मेरी ही नहीं अनेक प्रकार की अनुभूतियों पर आधृत है। मैंने अपनी औपन्यासिक कृति ‘पावक’ की भूमिका में एक बात लिखी थी उसे यहाँ उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत होता है, ‘‘गलत है कि अध्यात्म धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है। वैश्वीकरण और उन्मुक्त बाजार के प्रभाव ने नई पीढ़ी के कुछ लोगों को दिग्भ्रमित अवश्य किया है किन्तु देखकर आश्चर्य होता है कि मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में नवयुवकों-नवयुवतियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उन्हें भी अध्यात्म में आस्था की एक नई किरण दिखाई पड़ने लगी है।’’
मेरा यह कथन हाल ही में 28 मई के ‘इण्डिया टुडे’ में प्रकाशित शेफाली वासदेव के एक निबन्ध से सम्पुष्ट होता है। इस लेख का शीर्षक भी सचमुच यथार्थाधारित एवं प्रतीकात्मक बन पड़ा है, ‘है प्रभु से मिलने की प्यास’। पर्याप्त अन्वेषण और परिवेक्षण के बाद इस लेख में कई चौकाने वाली बातें सामने आई हैं। एक उद्धरण प्रस्तुत है : ‘‘आध्यात्मिकता का यह नया रूप फैशन-विशेषज्ञों से शेयर दलालों और पेशेवरों से लेकर गृहणियों को समान भाव से आकर्षित कर रहा है। पहले सत्संग अपने को दूसरों से अधिक साबित करने का उपक्रम माना जाता था। इन दोनों धर्मस्थलों, ध्यान-केन्द्रों और विभिन्न सम्प्रदायों के आश्रम में बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। इनमें से बहुत से पेशेवर भी होते हैं जो सत्संग में जाने के लिए अन्य पार्टियों का कार्यक्रम भी त्याग देते हैं।’’
लेख में कई आध्यात्मोन्मुख लोगों से साक्षात्कार भी किया गया है। इनमें हर तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति ने जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र सूक्ष्म जीव-विज्ञान के और जो एशिया में इस विषय के विशेषज्ञों में से माने जाते थे का कथन है—‘‘नेत्र विज्ञानी तो बहुत से हैं पर दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो दुनिया के लोगों के नेत्र खोल सकें।’’ अब एक एशिया-प्रसिद्ध नेत्र वैज्ञानिक स्वयं अन्तर्चक्षुओं को खोलने की बात करें तो मेरा यह कहना कि यह युग आध्यात्मिक पुनरुत्थान का है सच है या नहीं ?
इसी लेख के अनुसार एक अड़तीस वर्षीय युवती कृपाल माथुर कहती हैं—‘‘मेरी जिन्दगी में एक दुःखद हादसे के बाद सत्संग के प्रति मेरा रुझान तेजी से बढ़ा। इन दो घण्टों में मैं अतिरिक्त जीवनशक्ति का अनुभव करती हूँ।’’
इस निबन्ध को पढ़ने से आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक सत्संगों में भाग लेनेवाले केवल बूढ़े और चुके हुए लोग नहीं हैं। यह बात पहले भी रेखांकित की गई है। इस निबन्ध से उद्धरण लें तो ‘‘सत्संग-हालों में हर हफ्ते सम्मिलित होने वाले हजारों लोगों में रंग-बिरंगे बालों, चमकती नेलपालिश और छोटे गोटेदार बैगवाली युवतियाँ आसानी से देखी जा सकती हैं। कुछ तो नई डिजाइन की कुर्तियां और कुछ जीन पहनकर आती हैं। इसी तरह बहुत से युवा व्यवस्थित ढंग से कुर्ता पाजामा पहने, मोबाइल बन्द करके हाथ में बैठे मिलते हैं, जिसे ईश्वर के साथ उनके उस साप्ताहिक मिलन में किसी तरह का व्यवधान न आए। ये युवा अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ अत्यन्त विनम्रता जताते हैं। नई पीढ़ी की पहचान माने जानेवाली अकड़ और छिछोरापन उनमें यहाँ कतई नहीं दिखता।’’
मैंने अपने उपन्यास ‘पावक’ से जो उद्धरण ऊपर दिया है वह 2001 का और यह निबन्ध मई 2003 का है। क्या अब भी कोई यह कहने का दुस्साहस कर सकता है कि नई पीढ़ी भी निरन्तर अध्यात्म की ओर आकृष्ट होती जा रही है। अपवादों की बात भी नकारी नहीं जा सकती। ऐसे युवाओं की भी कमी नहीं जो ‘खाओ-पीओ, मौज मनाओ’, की उक्ति के कायल हैं। पर देर-सबेर वे भी अध्यात्म की शरण में आयेंगे ही क्योंकि भोग एक सीमा के बाद सुख और आनन्द का कारक नहीं रहता। इसका अनुभव उन धनाढ्य विदेशियों से पूछें जो सब कुछ छोड़ शान्ति के लिए भारत की ओर मुख करते हैं।
आप अपना अनास्थावादी और अनीश्वरवादी राग अलापते रहिए। लेकिन जिन्हें अध्यात्म ने सुकून दिया है वे उसे आपके कहने से ठुकरा नहीं देंगे।
गलत है कि वैज्ञानिक दैवी शक्तियों में विश्वास नहीं करते। आइन्स्टिन ने भी खुले शब्दों में आपने कई अन्वेषणों के मूल में किसी आन्तरिक स्फुरणा की बात स्वीकारी थी। यह दैवी इंगित नहीं तो और क्या था ? विख्यात नेत्र वैज्ञानिक का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। ‘इण्डिया टुडे’ के समान प्रतिष्ठित पत्रिका के इसी लेख में एक इलैक्ट्रिक इंजीनियर योगेश का कहना है कि ‘‘ये भजन तुरन्त चमत्कारिक असर डालते हैं।’’
अब जब वैज्ञानिक भी चमत्कारों से परहेज नहीं करते तो मैंने माता दन्तेश्वरी के चमत्कारों का उल्लेख कर कौन-सा गलत काम किया है ? दन्तेश्वरी का उल्लेख आ ही गया तो मैं यह स्पष्ट करूँ कि यह उपन्यास बस्तर की अद्भुत आदिवासी संस्कृति और उसकी समृद्ध परम्परा के साथ-साथ शक्तिपीठ माता दन्तेश्वरी को केन्द्र में रखकर ही लिखा गया है। इसमें आदिवासियों के लोकगीत हैं जो मातृ-मन्दिर की घण्टियों की संगीत ध्वनि भी है और आदिवासियों किशोर-किशोरियों की निश्छल प्रेमगाथा भी।
ऐसा बहुत कम स्थानों पर है लेकिन बस्तर क्षेत्र के लिए जो कभी दण्डकारण्य कहा जाता था और जहाँ राम, सीता की खोज में भटकते रहे थे यह एक कठोर सत्य है कि दन्तेश्वरी मन्दिर के इर्द-गिर्द ही यहाँ की सामाजिक-पारिवारिक एवं राजनीतिक गतिविधियाँ पूर्णतया केन्द्रित हैं। आदिवासियों की देवी तो यह नाममात्र को हैं, यहाँ की सभी तरह की आबादी उनकी छत्रछाया में पलती है। साथ ही दूर-दिगन्त के लोग भी दन्तेश्वरी देवी के प्रभाव, उनकी शक्ति तथा मनोकामना-पूर्ति करने की उनकी अनुकम्पा से आकृष्ट होकर यहाँ आते रहते हैं।
हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि यह औपन्यासिक कृति मुख्यतः दन्तेश्वरी पर ही आधृत है। आदिवासी जीवन और आदिवासियों की संस्कृति एवं परम्परा इस कृति में अवश्य है और जहाँ तक सम्भव है वह अपनी सम्पूर्णता में उभरकर आई है किन्तु यह सबकुछ गौण है, प्रमुख हैं माता दन्तेश्वरी ही।
दन्तेश्वरी में चमत्कारी शक्ति है तो है, उसकी उपेक्षा कर अपने को अत्याधुनिक कहाने का मुझे शौक नहीं। फिर जब बात सार्वजविक रूप से जिम्मेवार लोगों से स्वीकारी जाएँ तो उसे नकारने का मुझे क्या अधिकार है ? एक उदाहरण प्रस्तुत है। अभी-अभी 14 जुलाई के टाइम्स आफ इण्डिया में एक समाचार आया जिसे श्री लवकुमार मिश्रा ने रायपुर से दिया है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है।
इस समाचार के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने उद्घोषित किया है कि माता दन्तेश्वरी उनके स्वप्न में आई और उन्होंने आदेश दिया कि क्षेत्र के सभी देव-गुड़ियों (ग्रामीण मन्दिरों) का पुनरुद्धार किया जाए। इस स्वप्न पर विश्वास कर श्री जोगी ने इस समाचार के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया।
‘टाइम्स आफ इण्डिया’ एक प्रतिष्ठित और अतिपठित समाचार पत्र माना जाता है। इससे किसी अन्धविश्वास को प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं हो सकती। अतः मैंने अगर दन्तेश्वरी की चमत्कारिक शक्ति एवं महत्ता को रेखांकित किया है तो मैं न अन्धविश्वास को प्रश्रय दे रहा हूँ न देवी के असंख्य अनुयायी ही अन्धविश्वासी हैं। अन्धविश्वासी वस्तुतः वे हैं जो आँखें होते हुए भी सत्य पर संशय का पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। जिनका मिथ्या अहं कटु यथार्थ को पचा नहीं पाता। जो आँखें रहते भी अन्धे की तरह व्यवहार करते हैं। अन्धविश्वासी तो वही हैं न कि वो जो अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति का साहस करते हैं। मानकर चलना पड़ेगा कि यह विश्व दैवी शक्तियों से संचालित है और इन शक्तियों में जिन्हें चमत्कार कहते हैं वह करने की भी क्षमता है। अपने अनुभव के आधार पर कहना पड़ेगा कि माता दन्तेश्वरी में भी अपार चमत्कारी शक्तियाँ हैं। कोई इनका लाभ न उठा सके तो यह उसका दुर्भाग्य है।
हाँ यह पुस्तक मुख्यतः मन्दिर पर आधृत है। प्रश्न उठ सकता है कि क्या मात्र मन्दिर पर कोई उपन्यास गढ़ा जा सकता है। उत्तर उपस्थित है। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पर दो विशिष्ट उपन्यास आ चुके हैं। असम की कामाख्या देवी पर भी आधृत उपन्यास पिछले वर्षों ही आया।
यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह औपन्यासिक कृति काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थाधारित है। इसकी रचना के लिए पर्याप्त परिभ्रमण, संवाद, गवेषण एवं सामग्री-चयन तथा स्वाध्याय का सहरा लिया गया है।
ऐतिहासिक-पौराणिक लेखन की मेरी यही विधि अथवा रचना-प्रक्रिया रही है। मैं सर्वप्रथम उनसे सम्बद्ध स्थानों का भ्रमण करता हूँ फिर उनसे सम्बन्धित जितनी सामग्री प्राप्त हो सकती है उतनी एकत्रित करता हूँ और उसे आत्मसात करने के पश्चात् ही लिखने बैठता हूँ। परिभ्रमण के क्रम में व्यक्तियों से संवाद भी होता है। उसका भी यथासाध्य उपयोग रचना के सृजन के समय किया जाता है। अरण्या लिखने के पूर्व मैंने दो बार बस्तर क्षेत्र एवं दन्तेश्वरी मन्दिर का भ्रमण किया। जगदलपुर तथा अन्य स्थानों से आदिवासी-जीवन एवं देवी मन्दिर से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित की। आदिवासी एवं गैर आदिवासी लोगों से उनकी संस्कृति, परम्परा एवं सर्वोपरि देवी दन्तेश्वरी में उनकी आस्था के कारणों के सम्बन्ध में वार्तालाप किया। इन वार्तालापों और प्राप्त सामग्री के अध्ययन के पश्चात् ही अरण्या रची गई।
यह मैं नहीं मानता कि यथार्थपरक होने के पश्चात् भी इसमें कल्पना का स्थान शून्य है। कल्पना किसी जीवन्त कृति विशेषकर रचनात्मक कृति का प्राण है। स्वीकार करना पड़ेगा कि जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ मैंने कल्पना को खुलकर खेलने दिया। जब भी अवसर मिला है प्राकृतिक वर्णन को पर्याप्त स्थान दिया है। इससे पुस्तक की पठनीयता में निश्चित ही अभिवृद्धि हुई है।
एक बात और कहनी पड़ेगी माता दन्तेश्वरी पर मुख्यतः आधृत होने के पश्चात् भी यह कृति किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय से सम्बद्ध नहीं है। पाठक पाएँगे कि जहाँ पुस्तक में गीता का उद्धरण हैं वही ‘बाइबिल’ के भी कुछ कम नहीं हैं। इस्लाम का भी उल्लेख है। हाँ यह ‘स्यूडो स्कुलरिज्म’ के युग की एक पूर्णतया ‘सेक्युलर’ कृति है।
पुस्तक की भाषा और शिल्प के सम्बन्ध में कुछ कहना पड़ेगा।
भाषिक सौंन्दर्य पर मेरा सदा जोर रहा है। मैं तत्सम शब्दों का आग्रही हूँ। कभी-कभी कुछ कठिन शब्द भी अवश्य आ जाते हैं पर भाषा की प्रवहमानता में वे ऐसे घुलमिल जाते हैं कि पठनीयता में कभी बाधा नहीं आती। गति को रोक नहीं पाते।
कहीं-कहीं पत्रानुसार भी भाषा का प्रयोग करना पड़ा है पर ऐसा कम ही हुआ क्योंकि पुस्तक को तो अन्ततः हिन्दी में ही होना या, अतः आदिवासी भाषाओं का यत्र-तत्र दिखाने भर का प्रयोग पठनीयता में बाधक ही बनता।
पुस्तक की आध्यात्मिकता को तो आरम्भ में रेखांकित किया गया पर इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पक्ष अछूते ही रह गए क्योंकि सच कहा जाए तो यह पुस्तक पौराणिक एक ऐतिहासिक सह अध्यात्मिक है।
जहाँ तक पौराणिक की बात है सती के मोह और उसके पिता दक्ष प्रजापति की कथा पुराणाधारित है। पुराणों में किसी विषय को लेकर थोड़ा-बहुत मत-वैभिन्य रहता ही है. अतः अगर यह विवरण किसी को अपने अभिज्ञान से किंचित भिन्न लगे तो उसमें लेखक का कोई दोष नहीं।
मूल ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ मैं नहीं करता। इस पुस्तक में भी नहीं हुआ है। हाँ औपन्यासिक तकादों के कारण कुछ काल्पनिक पात्र एवं घटनाएँ अवश्य डालनी पड़ी हैं जिनकी पहचान कठिन नहीं होगी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक काल-खंड पर ही आधृत है। जो उपन्यास बनाया जा सकता था, बस्तर के किसी काल-खण्ड को मैंने चुना है। यह आज से प्रायः छह सौ वर्ष पुराना है।
उपन्यास को उसी काल में छोड़ देना मैंने उचित नहीं समझा है और एक संक्षिप्त उपसंहार के द्वारा बस्तर तथा उसकी अधिष्ठात्री देवी माता दन्तेश्वरी की अद्यतन स्थिति से भी पाठकों को परिचित कराना उचित समझा है। आश्चर्य है कि प्रायः छह सौ वर्ष की सततता आज भी बनी हुई है। आदिवासियों की संस्कृति और परम्परा में शायद ही कोई परिवर्तन आया है। हाँ, उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति में विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात् स्वाभाविक परिवर्तन आया है जो उनके पक्ष में है। उपन्यास की आधार-भूमि माता दन्तेश्वरी की लोकप्रियता में इन वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई एवं सभ्यता तथा आधुनिकता की किरणों के इस क्षेत्र की सारी गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। आश्चर्य हो सकता है पर यह सत्य है कि बस्तर के जन-जीवन का संचालन-सूत्र अभी भी माता दन्तेश्वरी के ही सर्व-समर्थ करों में है। दूर-दराज के भक्तों-दर्शकों का तो यह स्थान स्वेच्छा-पूर्ति के तीर्थ के रूप में निरन्तर अधिकाधिक प्रसिद्ध होता ही जा रहा है। मार्ग पहले की अपेक्षा अधिक सुगम हो गया है। अब जंगलों के दुर्गम पथों से नहीं जाना पड़ता। रायपुर (जो मध्यप्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बनने पर उसकी राजधानी बना) से सीधी सड़क आती है। दक्षिण से आये तो विशाखापत्तनम् से जगदलपुर और वहाँ से दन्तवेड़ा तक दन्तेश्वरी मन्दिर तक विश्वसनीय सड़क मार्ग है। जगदलपुर स्वयं एक रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ तक रेलगाड़ी से पहुँचने के पश्चात् सड़क मार्ग से एक छोटी यात्रा ही मन्दिर तक करनी पड़ती है जिसके लिए टैक्सी, टैम्पो से लेकर हर सवारी उपलब्ध है।
मंदिर के पास कई दुकानों में माता के पूजा-पाठ की सभी सामग्री मिलती है। इधर की देवियों को लहंगा चुनरी या प्रॉक तक अधिक प्रिय हैं। माता दन्तेश्वरी के परिधान में भी इन्हीं का उपयोग होता है। ये परिधान, भक्त खरीदकर अपने साथ भी ला सकते हैं।
उपन्यास के शिल्प की बात होते-होते रह गई। जैसे यह उपन्यास एक तरह से पूरी तरह देवी दन्तेश्वरी द्वारा ही लिखित है, इसी तरह, प्रतीत होता है, इस भूमिका पर भी वे हावी हैं। जो चीज जहाँ चाहोगी, वहीं आयेगी।
तो शिल्प पर भी बात कर ही लें। मेरे उपन्यास की एक विशेषता है कि वे उद्देश्यपरक तो होते ही हैं, कहीं-कहीं वे चिन्तनपरक भी होते हैं। प्रायः अध्यायों का आरम्भ कुछ ऐसी चिन्तनशील बातों से होता है जिससे लेखक के दार्शनिक मनोभाव तो स्पष्ट होते ही हैं, अध्याय में आने वाले विषय का भी पूर्वाभास हो जाता है। इससे मेरे उपन्यासों की लोकप्रियता बाधित नहीं हुई है अपितु उसके फलस्वरूप मेरा एक विशेष पाठक-वर्ग प्रस्तुत हुआ है। यही कारण है 1983-84 में प्रकाशित उपन्यासों ‘पहला सूरज’ और ‘पवनपुत्र’ के संस्करण अभी तक होते जा रहे हैं।
औपन्यासिक विधा को एक गढ़े-गढ़ाएँ साँचे में बंधे देखने वालों को यह प्रयोग रास नहीं भी आया और लोग उंगली लगाने में भी पीछे नहीं रहे। इसका उत्तर मैंने गतवर्ष प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘पावक’ में अच्छी तरह दिया है, उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ना केवल इतना है कि ऐसे शिल्प को अपनाने के लिए सामर्थ्य भी आवश्यक है। केवल कथोपकथन की बैशाखी के सहारे उपन्यास गढ़ देने वाले इस चिन्तनपरक शिल्प पर किधर से हाथ आजमाएँगे ? बात कड़वी लग सकती है पर वह कड़वी हमें भी लगती है, जब कहा जाता है कि ऐतिहासिक-पौराणिक उपन्यासों की क्या आवश्यकता है, उनके बदले पुराण, इतिहास ही नहीं पढ़ लें ? उत्तर है कि आप पौराणिक उपन्यास ही नहीं पढ़ सकते तो पुराण क्या खाकर पढ़िएगा ? रह गई बात इतिहास की तो सबको विदित है कि इतिहास एक नीरस विषय है। उसे सरसता प्रदान करने के लिए ही ऐतिहासिक उपन्यासों की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों का चले तो हिन्दी साहित्य को आचार्य चतुरसेन शास्त्री के ‘वयं रक्षाम्:: ‘वैशाली की नगर वधू’, वृन्दालाल वर्मा के ‘गढ़ कुंडाल’ हजारी प्रसाद द्वेवेदी के ‘चारु-चन्द्र लेख’ तथा बाणभट्ट’ की आत्म कथा’ और अमृतलाल नागर के ‘मानस के हंस’ तथा ‘खंजन नयन’ और इस लेखक के ‘पावक’ तथा पीताम्बरा’ से वचंति ही रहना पड़े।
और पुराण-इतिहास को क्या केवल उपन्यासकारों ने ही अपनी उपजीव्य बनाया है ? काव्यकारों ने नहीं ? यदि यही बात रहती है तो प्रसाद की ‘कामायनी’, मैथलीशरण गुप्त का ‘साकेत’, हरिऔध का ‘प्रिय प्रवास’ तथा दिनकर की ‘रश्मिरथी’ और ‘कुरुक्षेत्र’ किधर से आते ?
पौराणिक-ऐतिहासिक उपन्यास-लेखन की धारा बहुत पूर्व से चल पड़ी है और वह इधर कुछ नए लेखकों के सहयोग से पुस्टतर ही हुई है। अब तो मैंने इसमें अध्यात्म के उफनते प्रवाह को भी समेट लिया है। किसी पाठक-समीक्षक, में शक्ति हो तो इस प्रवाह को अवरुद्ध करके दिखा दे। मैं पुनः नई पीढ़ी में जगी अध्यात्म-सम्मान का स्वागत करता हुआ हूँ। तथा जिस आध्यात्मिक पुनरुत्थान की मैंने चर्चा की है उसमें रचनात्मक अवदान के लिए सहकर्मी उपन्यासकार बन्धुओं का आह्वान करता हूँ।
मैं इस भूमिका को और अधिक नहीं खींचना चाहता। शेष बातें पुस्तक स्वयं बोलेगी।
इस अवसर मैं कुछ लोगों का साधुवाद अवश्य करना चाहूँगा जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेरणा इस पुस्तक लेखन में मिली है। इनमें प्रमुख है सांसद एवं साहित्यकार तथा लन्दन में भारत के भूतपूर्व राजदूत लक्ष्मी सिंघवी, साहित्यकार बन्धुगण सर्वश्री राजेन्द्र अवस्थी, जयप्रकाश भारती, डॉ. श्याम सिंह शशि, डॉ. सतीश राजपुस्करणा, श्री कृष्णानन्द, कवि समीक्षक डॉ. शिवनारायण, भागनेघ बैजनाथ पाठक सशक्त सम्पादक एवं उपन्यास श्री उदयराज सिंह, सुदामा मिश्र तथा बिहार के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री के.के. श्रीवास्तव और उनकी विदुषी धर्मपत्नी।
आत्माराम एण्ड सन्स के श्री सुशील पुरी एवं उनके पुत्र श्री सुधीर पुरी एवं उनके भतीजे श्री योगेश्वर पुरी का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने पुस्तक को यथाशीघ्र इतने आकर्षक कलेवर प्रस्तुत किया।
श्री सुभाष तनेजा का मैं विशेष आभार मानता हूँ जिन्होंने इस पाण्डुलिपि को प्रस्तुत करने में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की।
अन्ततः यह पुस्तक माता दन्तेश्वरी की कृ़पा का ही सुफल है जिनकी अन्तर्प्रेरणा के बिना यह कार्य पूर्ण नहीं होता। मैं उन्हें अन्तर्मन से अपना नमन निवेदित करना चाहता हूँ और उनसे अभ्यर्थना करता हूँ कि वे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा का वर्षण करती रहें।
डॉ. भगवतीशरण मिश्र
सम्पर्क—जी.एच.-13/805
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-7
श्रावणी पूर्णिमा (2003)
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book