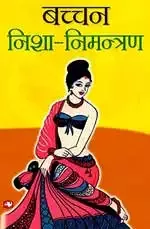|
कविता संग्रह >> निशा निमंत्रण निशा निमंत्रणहरिवंशराय बच्चन
|
81 पाठक हैं |
||||||
बच्चन की श्रेष्ठ कविताओं का संग्रह....
Nisha Nimantran
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
बच्चन की ख्याति ‘मधुशाला’ की रचना के साथ हुई, जो सन् 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसके तीन वर्ष पूर्व उनकी कविताओं का प्रथम संग्रह ‘तेरा हार’ प्रकाशित हुआ था। उस समय भी काव्य-प्रेमियों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ था। ‘मधुशाला’ ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया।
हरिवंशराय बच्चन का जन्म 27 नवम्बर, 1907 को प्रयाग में हुआ था। उनकी शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल, कायस्थ-पाठशाला, गवर्नमेंट कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई। 1941 से’ 52 तक वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरर रहे। 1952 से’ 54 तक इंग्लैंड में रहकर उन्होंने केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। विदेश से लौटकर उन्होंने एक वर्ष अपने पूर्व पद पर तथा कुछ मास आकाशवाणी, इलाहाबाद में काम किया। दिसम्बर, 1955 में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय के हिन्दी-विशेषज्ञ के रूप में बुला लिया, जहां दस वर्ष रहकर उन्होंने हिन्दी को राजनयिक काम-काज का सक्षम माध्यम बनाया। अप्रैल, 1966 में राष्ट्रपति डॉ. राधाकष्णन ने उन्हें राज-सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया।
बच्चन का कहना है : ‘‘मैं जीवन की समस्त अनुभूतियों को कविता का विषय मानता हूं लेकिन मेरी अनुभूति में कल्पना और जीवन में मरण भी सम्मिलित है।’’
हरिवंशराय बच्चन का जन्म 27 नवम्बर, 1907 को प्रयाग में हुआ था। उनकी शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल, कायस्थ-पाठशाला, गवर्नमेंट कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई। 1941 से’ 52 तक वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरर रहे। 1952 से’ 54 तक इंग्लैंड में रहकर उन्होंने केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। विदेश से लौटकर उन्होंने एक वर्ष अपने पूर्व पद पर तथा कुछ मास आकाशवाणी, इलाहाबाद में काम किया। दिसम्बर, 1955 में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय के हिन्दी-विशेषज्ञ के रूप में बुला लिया, जहां दस वर्ष रहकर उन्होंने हिन्दी को राजनयिक काम-काज का सक्षम माध्यम बनाया। अप्रैल, 1966 में राष्ट्रपति डॉ. राधाकष्णन ने उन्हें राज-सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया।
बच्चन का कहना है : ‘‘मैं जीवन की समस्त अनुभूतियों को कविता का विषय मानता हूं लेकिन मेरी अनुभूति में कल्पना और जीवन में मरण भी सम्मिलित है।’’
अपने पाठकों से
(सातवें संस्करण से)
‘निशा-निमंत्रण’ का सातवाँ संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। नया संस्करण इस बात का सबूत है कि लोग मेरी रचना को आज भी खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और उसका आनन्द लेना चाहते हैं। किसी भी रचना के प्रचार में प्रायः उसके पाठकों का ही विशेष हाथ होता है। इस कारण मैं इस अवसर पर ‘निशा निमंत्रण’ के पिछले छः संस्करणों के पाठकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने स्वयं इस रचना का रस लेकर अपने परिचितों और मित्रों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। ‘निशा-निमंत्रण के नये पाठकों को इन लगभग बीस हजार प्रतियों के बड़े संयत अनुमान से भी, चालीस-पचास हजार पाठकों की रुचि का विश्वास हो तो यह स्वाभाविक बात होगी।
कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने पाठकों के ऊपर भारी बोझ डाला है। उनके सामने अपनी कविताएँ रख दी हैं और उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। उन्हें जो कुछ भी जानने की जिज्ञासा हुई है उसे उन्होंने मेरी पंक्तियों के अन्दर ही देखने-खोजने का प्रयत्न किया है। कभी उनका अनुमान गलत हुआ है-कभी सही। बात को ठीक-ठीक जानने की कामना से कुछ लोगों ने मुझे पत्र भी लिखे हैं और मैंने उनका समाधान करने के लिए यथोचित उत्तर दिए हैं-इन मामलों में ठीक बताने की भी सीमाएँ हैं। लेकिन ज्यादातर पाठकों ने अपनी ग्राह्यता-और इसके अनेक स्तर होते हैं-और मेरी पंक्तियों की क्षमता के बीच किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर अपने को सन्तुष्ट कर लिया है। कविता जब कवि की लेखनी से निकल गई तो उसका अपना अस्तित्व हो जाता है, और पाठक से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उसे किसी समालोचक, व्याख्याता, यहाँ तक कि स्वयं कवि का भी मुहताज नहीं होना चाहिए। कुछ इसी प्रकार के विचारों ने मुझे चुप रक्खा है।
जहाँ तक कविता से रस अथवा आनन्द पाने का सम्बन्ध है, मैं अब भी समझता हूँ, उसका प्रतिपादन कविता के बाहर से नहीं किया जा सकता। उसे तो कविता के अन्दर से ही लेना होगा। यदि इस रस अथवा आनन्द के स्रोत की खोज खुद की जाए तो उसमें कुछ विशेषता, कुछ विचित्रता और जु़ड़ती है। मेरी रचना उस रस का आभास अथवा संकेत कैसे देती है कि आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, इसे मैं स्वयं नहीं जानता।
यहाँ मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनके विषय में प्रायः मेरे पाठकों की जिज्ञासा रही है, गो विशुद्ध काव्यानन्द से इन बातों का केवल दूरी का सम्बन्ध रह सकता है।
महात्मा गांधी का सत्याग्रह आन्दोलन 1930 में आरम्भ हुआ। उस समय मैं एम.ए. में पढ़ रहा था। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। कुछ दिन तो चर्खा कातने, नमक बनाने, खद्दर बेचने, स्कूल-कॉलेजों में पिकेटिंग करने, गाँवों में जाकर व्याख्यान देने, शहर में सभाओं में बैठकर नेताओं की तकरीरें सुनने और लम्बे-लम्बे जुलूस बनाकर नारे लगाने में बीत गए। बाला-बाला क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क रहा। आन्दोलन ठण्डा पड़ा तो मैंने अपने आपको जग और जीवन के समक्ष पाया-संघर्ष में धँसा, समस्याओं से उलझा, अनुभवों में डूबता-उतराता। भावनाएँ मुखरित होने लगीं। एक दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा-क्या मैं कवि हूँ ?
‘रुबाइयात उमर खैयाम’ से मेरा परिचय तो पुराना था पर अब वह मेरी परम प्रिय पुस्तक हो गई थी। रात को मेरे तकिए के नीचे रहती, दिन को मेरी जेब में। अपने ऊपर खैयाम के प्रभाव को मैंने इन पंक्तियों में स्वीकार किया है :
कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने पाठकों के ऊपर भारी बोझ डाला है। उनके सामने अपनी कविताएँ रख दी हैं और उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। उन्हें जो कुछ भी जानने की जिज्ञासा हुई है उसे उन्होंने मेरी पंक्तियों के अन्दर ही देखने-खोजने का प्रयत्न किया है। कभी उनका अनुमान गलत हुआ है-कभी सही। बात को ठीक-ठीक जानने की कामना से कुछ लोगों ने मुझे पत्र भी लिखे हैं और मैंने उनका समाधान करने के लिए यथोचित उत्तर दिए हैं-इन मामलों में ठीक बताने की भी सीमाएँ हैं। लेकिन ज्यादातर पाठकों ने अपनी ग्राह्यता-और इसके अनेक स्तर होते हैं-और मेरी पंक्तियों की क्षमता के बीच किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर अपने को सन्तुष्ट कर लिया है। कविता जब कवि की लेखनी से निकल गई तो उसका अपना अस्तित्व हो जाता है, और पाठक से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उसे किसी समालोचक, व्याख्याता, यहाँ तक कि स्वयं कवि का भी मुहताज नहीं होना चाहिए। कुछ इसी प्रकार के विचारों ने मुझे चुप रक्खा है।
जहाँ तक कविता से रस अथवा आनन्द पाने का सम्बन्ध है, मैं अब भी समझता हूँ, उसका प्रतिपादन कविता के बाहर से नहीं किया जा सकता। उसे तो कविता के अन्दर से ही लेना होगा। यदि इस रस अथवा आनन्द के स्रोत की खोज खुद की जाए तो उसमें कुछ विशेषता, कुछ विचित्रता और जु़ड़ती है। मेरी रचना उस रस का आभास अथवा संकेत कैसे देती है कि आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, इसे मैं स्वयं नहीं जानता।
यहाँ मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनके विषय में प्रायः मेरे पाठकों की जिज्ञासा रही है, गो विशुद्ध काव्यानन्द से इन बातों का केवल दूरी का सम्बन्ध रह सकता है।
महात्मा गांधी का सत्याग्रह आन्दोलन 1930 में आरम्भ हुआ। उस समय मैं एम.ए. में पढ़ रहा था। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। कुछ दिन तो चर्खा कातने, नमक बनाने, खद्दर बेचने, स्कूल-कॉलेजों में पिकेटिंग करने, गाँवों में जाकर व्याख्यान देने, शहर में सभाओं में बैठकर नेताओं की तकरीरें सुनने और लम्बे-लम्बे जुलूस बनाकर नारे लगाने में बीत गए। बाला-बाला क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क रहा। आन्दोलन ठण्डा पड़ा तो मैंने अपने आपको जग और जीवन के समक्ष पाया-संघर्ष में धँसा, समस्याओं से उलझा, अनुभवों में डूबता-उतराता। भावनाएँ मुखरित होने लगीं। एक दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा-क्या मैं कवि हूँ ?
‘रुबाइयात उमर खैयाम’ से मेरा परिचय तो पुराना था पर अब वह मेरी परम प्रिय पुस्तक हो गई थी। रात को मेरे तकिए के नीचे रहती, दिन को मेरी जेब में। अपने ऊपर खैयाम के प्रभाव को मैंने इन पंक्तियों में स्वीकार किया है :
तुम्हारी मदिरा से अभिषिक्त
हुए थे जिस दिन मेरे प्राण
उसी दिन मेरे मुख की बात
हुई थी अंतरतम की तान
हुए थे जिस दिन मेरे प्राण
उसी दिन मेरे मुख की बात
हुई थी अंतरतम की तान
(आरती और अंगारे)
मैंने ‘रुबाइयात उमर खैयाम’ का अनुवाद कर डाला। खैयाम की दुनिया की रंगीनी ने मुझे इतना मोह लिया कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी मुझे सबसे उपयुक्त प्रतीक वे ही जान पड़े जिनकी ओर खैयाम ने संकेत किया था-हाला, प्याला, मधुशाला और मधुबाला।
1933-’34 में मैंने ‘मधुशाला’ लिखी।
1934’35 में मैंने ‘मधुबाला’ लिखी।
हर तूफान मन्द पड़ता है, हर नशा उतरता है। मेरी भावनाओं ने तीव्रतम स्थिति छू ली थी। वहाँ पर ज्यादा देर टिका रहना असम्भव था। जीवन का पहिया घूम गया-
1933-’34 में मैंने ‘मधुशाला’ लिखी।
1934’35 में मैंने ‘मधुबाला’ लिखी।
हर तूफान मन्द पड़ता है, हर नशा उतरता है। मेरी भावनाओं ने तीव्रतम स्थिति छू ली थी। वहाँ पर ज्यादा देर टिका रहना असम्भव था। जीवन का पहिया घूम गया-
गिर-गिर टूटे घट-प्याले,
बुझ दीप गए सब क्षण में,
सब चले किए सिर नीचे
ले अरमानों की झोली।
गूँजी मदिरालय भर में
लो चलो-चलो की बोली।
बुझ दीप गए सब क्षण में,
सब चले किए सिर नीचे
ले अरमानों की झोली।
गूँजी मदिरालय भर में
लो चलो-चलो की बोली।
(मधुशाला)
अब वे मेरे गान कहाँ हैं !
टूट गई मरकत की प्याली,
लुप्त हुई मदिरा की लाली,
टूट गई मरकत की प्याली,
लुप्त हुई मदिरा की लाली,
मेरा व्याकुल मन बहलानेवाले अब सामान कहाँ हैं ?
(निशा-निमंत्रण)
और उल्लास की चोटी से अवसाद के गहर में गिरकर मैंने हलाहल मरघट’ और ‘अतीत का गीत’ की प्रतिध्वनि से अपने को व्यक्त करना चाहा। (‘हलाहल’ पुस्तक-रूप में प्रकाशित हो चुका है। ‘मरघट’ और ‘अतीत का गीत’ दीमकों की जूठन के रूप में मेरे कागज-पत्रों में कहीं पड़े हैं।)
नियति का व्यंग्य कि जब मधुशाला टूट चुकी है और मधु का प्याला फूट चुका तब मुझसे मधु के गीत लिखने की कैफियत माँगी जाने लगी और क्षय के रोग में पड़े हुए मैंने इस प्रकार उत्तर दिया :
नियति का व्यंग्य कि जब मधुशाला टूट चुकी है और मधु का प्याला फूट चुका तब मुझसे मधु के गीत लिखने की कैफियत माँगी जाने लगी और क्षय के रोग में पड़े हुए मैंने इस प्रकार उत्तर दिया :
एक दिन मैंने लिया था काल से कुछ श्वास का ऋण,
आज भी उसको चुकाता, ले रहा वह क्रूर गिन-गिन;
ब्याज में मुझसे उगाहा है हृदय का गान उसने,
किंतु होने में उऋण अब शेष केवल और दो दिन;
गिर पड़ूंगा तान चादर सर्वथा निश्चिंत होकर,
भूलकर जग ने किया किस-किस तरह अपमान मेरा।
क्या किया मैंने, नहीं जो कर चुका संसार अब तक ?
वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी ?
हैं लिखे मधुगीत मैंने ही खड़े जीवन-समर में।
आज भी उसको चुकाता, ले रहा वह क्रूर गिन-गिन;
ब्याज में मुझसे उगाहा है हृदय का गान उसने,
किंतु होने में उऋण अब शेष केवल और दो दिन;
गिर पड़ूंगा तान चादर सर्वथा निश्चिंत होकर,
भूलकर जग ने किया किस-किस तरह अपमान मेरा।
क्या किया मैंने, नहीं जो कर चुका संसार अब तक ?
वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी ?
हैं लिखे मधुगीत मैंने ही खड़े जीवन-समर में।
(मधुकलश)
लेकिन नियति का व्यंग्य अभी पूरा नहीं हुआ था। मरण की प्रतीक्षा में मैं था। जीवन के पार क्या होगा, इसकी चिन्ता मुझे थी-इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा ?-पर नियति को तो मरण से भी अधिक भयंकर एकाकीपन मेरे जीवन में लाना था।
न झिझका औ’ न हुआ भयभीत
न भागा ही लेकर के प्राण,
दिखा जब मुझको आता काल
कफन का ले हाथों में थान;
बढ़ाया पट जब मेरी ओर,
उठा, तैयार हुआ तत्काल,
निकट जो मेरे थे वरदान
दिया, पर, उसने उन पर डाल।
न भागा ही लेकर के प्राण,
दिखा जब मुझको आता काल
कफन का ले हाथों में थान;
बढ़ाया पट जब मेरी ओर,
उठा, तैयार हुआ तत्काल,
निकट जो मेरे थे वरदान
दिया, पर, उसने उन पर डाल।
(हलाहल)
मेरी पत्नी श्यामा बीमार हो गई और दो सौ सोलह दिन चारपाई पर पड़ी रहकर, हमारे बचाने के सारे उपायों को विफल कर, उस पार चली गई।
‘गुलहजारा’ कविता की इन पंक्तियों में,
मृत्यु शैया पर पड़े अति
रुग्ण की अंतिम हँसी-सी,
यत्न करके लिख रही है,
एक लघु कलिका निराली।
मृत्यु शैया पर पड़े अति
रुग्ण की अंतिम हँसी-सी,
यत्न करके लिख रही है,
एक लघु कलिका निराली।
(मधुकलश)
उसी का एक चित्र है :
उठा करता था मन में प्रश्न
कि जाने क्या होगा उस पार
निवारण करने में संदेह
मजहबी पोथे थे बेकार
चले तुम, पूछा हैं ! किस ओर !
कहा बस तुमने एक जबान
तुम्हें थी जिसकी खोज-तलाश,
उसी का करने अनुसन्धान।
उठा करता था मन में प्रश्न
कि जाने क्या होगा उस पार
निवारण करने में संदेह
मजहबी पोथे थे बेकार
चले तुम, पूछा हैं ! किस ओर !
कहा बस तुमने एक जबान
तुम्हें थी जिसकी खोज-तलाश,
उसी का करने अनुसन्धान।
(हलाहल)
मेरा ‘इस पार-उस पार’ गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। शायद आज भी है, पर उसके पीछे जो दर्शन है, उसका अनुभव उन लोगों को नहीं होता जो मुझसे बार-बार इस गीत को सुनाने का अनुरोध करते हैं। कई लोगों ने इस कविता की पैरोडियाँ भी लिखी हैं। नियति ने मेरे साथ इतना बड़ा व्यंग्य किया था कि इन नटखट पैरोडियों पर दुखी होने के बजाय मैं मुस्करा दिया हूँ।
अन्त का इतना था विश्वास
विदा का लिख डाला था गीत,
कलेजे को हाथों से थाम
सुना करते थे मन के गीत;
गए थे वे तज मेरा साथ
मगर वह गीत लगा है संग,
ध्वनित हो बहु कण्ठों से आज,
किया करता है मुझ पर व्यंग्य।
विदा का लिख डाला था गीत,
कलेजे को हाथों से थाम
सुना करते थे मन के गीत;
गए थे वे तज मेरा साथ
मगर वह गीत लगा है संग,
ध्वनित हो बहु कण्ठों से आज,
किया करता है मुझ पर व्यंग्य।
(हलाहल)
1930 के अन्त से जो संघर्ष मेरे जीवन में आरम्भ हुआ था उस की चरम स्थिति 1936 के अन्त में श्यामा के देहावसान में पहुँची।
सत्य मिटा, सपना भी टूटा।
सत्य मिटा, सपना भी टूटा।
(निशा-निमंत्रण)
लेकिन में अभी टूटा नहीं था। मैंने अपने जीवन से खेल किया था। मैंने जीवन के क्रम में विश्रृंखल किया था। जो कड़ी मैंने एक दिन झटके से तोड़ दी थी, उसे फिर से पकड़ने का मैंने निश्चय किया। एम.ए. की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैंने फिर से युनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया। यह भी सोचा था कि इस प्रकार मैं अपनी दुःखद स्मृतियों को भुलावा दे सकूँगा। एक वर्ष तक कविता की पंक्ति तक भी न लिखी। शायद मेरे महाशोक से मुझे काठ-सा मार गया था या मेरे आँसू अभी पिघले न थे कि निकलें। दुःखद स्मृतियों को इतनी सरलता से झुठलाना सम्भव नहीं। 1937 के अन्त में इधर तो मेरी परीक्षा निकट आने लगी और उधर मेरे भीतर कुछ विवश करने लगा कि मैं अपने को अभिव्यक्ति दूँ। यह ‘निशा-निमंत्रण’ के गीतों की पृष्ठभूमि है।
जो मेरी ‘मधुबाला’ और ‘मधुशाला’ से परिचित होकर ‘निशा-निमंत्रण’ के गीतों को पढ़ेंगे, वे सहज ही देखेंगे कि मेरी शब्द-योजना, मेरे छन्द मेरे रुपक-एक शब्द में-मेरी शैली में, कितना परिवर्तन आ गया है। कहाँ-
पग-पायल की झनकार हुई,
पीने को एक पुकार हुई।
और कहाँ-
हमें छोड़कर चली गईं, लो, दिन की मौन संगिनी छाया।
अंग्रेजी में एक कहावत है-स्टाइल इज द मैन-जैसा जो आदमी, वैसी उसकी शैली। मेरा जीवन बदल गया था। मेरी शैली बदल गई। शुरू-शुरू में कुछ भोले लोगों ने पूछा था, अब आप पहले जैसे गीत क्यों नहीं लिखते ? मेरा उत्तर था, अब मैं पहले जैसा आदमी नहीं रहा।
एक प्रश्न मुझसे बहुत बात पूछा गया है-इन गीतों में यह ‘साथी’ कौन है ?
‘साथी, अंत दिवस का आया।’
‘साथी, नया वर्ष आया है।’
‘साथी, सो न, कर कुछ बात।’ आदि-आदि
मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि इसे यदि रुढ़ अर्थ में लेंगे या इसके पीछे किसी व्यक्ति-विशेष की खोज करेंगे तो आप गलती करेंगे। यदि आप मेरी राय माने तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ‘साथी’ आप अपने को ही समझ लें साथी वही तो जिसे मैंने अपनी कथा-व्यथा कहने के लिए सम्बोधित किया है।
कविता की प्रजा दो प्रकार की होती है। एक वह, जो कविता को बौद्धिक संवेदन देती है, उससे तटस्थ रहती है, उसे कौतूहल की दृष्टि से देखती है। दूसरी वह, जो उसे हार्दिक सहानुभूति देती है, उसकी भावधारा में बहती है, उसे अपने प्राणों में रसा-बसा लेती है।
आपको अपनी अभिव्यक्ति का अंग बनाकार मैं केवल अपनी रुचि बतलाना चाहता हूँ कि मुझे कविता की किस प्रकार की प्रजा पसन्द है।
कविता किससे कैसी प्रतिक्रिया कराती है, यह बहुत-कुछ कविता के आन्तरिक गुणों पर निर्भर है और इस विषय में मुझे मुँह नहीं खोलना चाहिए।
इन गीतों को आप कितना अपनाते हैं, इनमें कितना अपने को पाते हैं, यह तो इन्हें गाकर ही आप जान सकेंगे।
जो मेरी ‘मधुबाला’ और ‘मधुशाला’ से परिचित होकर ‘निशा-निमंत्रण’ के गीतों को पढ़ेंगे, वे सहज ही देखेंगे कि मेरी शब्द-योजना, मेरे छन्द मेरे रुपक-एक शब्द में-मेरी शैली में, कितना परिवर्तन आ गया है। कहाँ-
पग-पायल की झनकार हुई,
पीने को एक पुकार हुई।
और कहाँ-
हमें छोड़कर चली गईं, लो, दिन की मौन संगिनी छाया।
अंग्रेजी में एक कहावत है-स्टाइल इज द मैन-जैसा जो आदमी, वैसी उसकी शैली। मेरा जीवन बदल गया था। मेरी शैली बदल गई। शुरू-शुरू में कुछ भोले लोगों ने पूछा था, अब आप पहले जैसे गीत क्यों नहीं लिखते ? मेरा उत्तर था, अब मैं पहले जैसा आदमी नहीं रहा।
एक प्रश्न मुझसे बहुत बात पूछा गया है-इन गीतों में यह ‘साथी’ कौन है ?
‘साथी, अंत दिवस का आया।’
‘साथी, नया वर्ष आया है।’
‘साथी, सो न, कर कुछ बात।’ आदि-आदि
मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि इसे यदि रुढ़ अर्थ में लेंगे या इसके पीछे किसी व्यक्ति-विशेष की खोज करेंगे तो आप गलती करेंगे। यदि आप मेरी राय माने तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ‘साथी’ आप अपने को ही समझ लें साथी वही तो जिसे मैंने अपनी कथा-व्यथा कहने के लिए सम्बोधित किया है।
कविता की प्रजा दो प्रकार की होती है। एक वह, जो कविता को बौद्धिक संवेदन देती है, उससे तटस्थ रहती है, उसे कौतूहल की दृष्टि से देखती है। दूसरी वह, जो उसे हार्दिक सहानुभूति देती है, उसकी भावधारा में बहती है, उसे अपने प्राणों में रसा-बसा लेती है।
आपको अपनी अभिव्यक्ति का अंग बनाकार मैं केवल अपनी रुचि बतलाना चाहता हूँ कि मुझे कविता की किस प्रकार की प्रजा पसन्द है।
कविता किससे कैसी प्रतिक्रिया कराती है, यह बहुत-कुछ कविता के आन्तरिक गुणों पर निर्भर है और इस विषय में मुझे मुँह नहीं खोलना चाहिए।
इन गीतों को आप कितना अपनाते हैं, इनमें कितना अपने को पाते हैं, यह तो इन्हें गाकर ही आप जान सकेंगे।
-बच्चन
एक कहानी
कहानी है सृष्टि के प्रारम्भ की। पृथ्वी पर मनुष्य था, मनुष्य में हृदय था, हृदय में पूजा की भावना थी, पर देवता न थे। वह सूर्य को अर्घ्यदान देता था, अग्नि को हविष् समर्पित करता था, पर इतने से ही सन्तुष्ट न था। वह कुछ और चाहता था।
उसने ऊपर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, ‘हे स्वर्ग, तूने हमारे लिए पृथ्वी पर सब सुविधाएँ दीं, पर तूने हमारे लिए कोई देवता नहीं दिया। तू देवताओं से भरा हुआ है, हमारे लिए एक देवता भेज दे जिसे हम अपनी भेंट चढ़ा सकें, जो हमारी भेंट पाकर मुस्करा सके, जो हमारे हृदय की भावनाओं को समझ सके। हमें एक साक्षात् देवता भेज दे।’
पृथ्वी के बाल-काल के मनुष्य की उस प्रार्थना में इतनी सरलता थी, इतनी सत्यता कि स्वर्ग पसीज उठा। आकाशवाणी हुई, ‘जा, मंदिर बना, शरद् ऋतु की पूर्णिमा को जिस समय चंद्रबिंब क्षितिज के ऊपर उठेगा उसी समय मंदिर में देवता प्रकट होंगे। जा, मंदिर बना।’ मनुष्य का हृदय आनन्द से गद्गद हो उठा। उसने स्वर्ग को बारंबार प्रणाम किया।
पृथ्वी पर देवता आएँगे ! इस प्रत्याशा ने मनुष्य के जीवन में अपरिमित स्फूर्ति भर दी। अल्पकाल में ही मंदिर का निर्माण हो गया। चंदन का द्वार लग गया। पुजारी की नियुक्ति हो गई। शरत् पूर्णिमा भी आ गई। भक्तगण सवेरे से ही जलपात्र और फूल अक्षत के थाल ले-लेकर मंदिर के चारों ओर एकत्रित होने लगे। संध्या तक अपार जन-समूह इकट्ठा हो गया। भक्तों की एक आंख पूर्व क्षितिज पर थी और दूसरी मंदिर के द्वार पर। पुजारी को आदेश था कि देवता प्रकट होते ही वह शंख-ध्वनि करे और मंदिर-द्वार खोल दे।
पुजारी देवता की प्रतीक्षा में बैठा था-अपलक नेत्र, उत्सुक मन। सहसा देवता प्रकट हो गए। वे कितने सुन्दर थे, कितने सरल थे, कितने सुकुमार थे, कितने कोमल ! देवता देवता ही थे। बाहर भक्तों ने चंद्रबिंब देख लिया था। अगणित कंठों ने एक-साथ नारे लगाए। देवता की जय, देवता की जय ! इस महारव से दसों दिशाएं गूंज उठीं, पर मंदिर से शंखध्वनि न सुन पड़ी !
पुजारी ने झरोखे से एक बार अपार जन-समूह को देखा और एक बार सुन्दर, सरल सुकुमार, कोमल देवता को। पुजारी काँप उठा। समस्त जन-समूह क्रुद्ध कंठस्वर से एक साथ चिल्लाने लगा, ‘मन्दिर का द्वार खोलो, खोलो !’ पुजारी का हाथ कितनी बार सांकल तक जा-जाकर लौट आया।
हजारों हाथ एक साथ मन्दिर के कपाट को पीटने लगे धक्के देन लगे। देखते ही देखते चन्दन का द्वार टूटकर गिर पड़ा; भक्तगण मंदिर में घुस पड़े। पुजारी अपनी आँखें मूंदकर एक कोने में खड़ा हो गया।
देवता की पूजा होने लगी। बात की बात में देवता फूलों से लद गए, फूलों में छिप गए, फूलों से दब गए। रात भर भक्तगण इस पुष्प राशि को बढ़ाते रहे।
और सबेरे जब पुजारी ने फूलों को हटाया तो उसके नीचे थी देवता की लाश।
उसने ऊपर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, ‘हे स्वर्ग, तूने हमारे लिए पृथ्वी पर सब सुविधाएँ दीं, पर तूने हमारे लिए कोई देवता नहीं दिया। तू देवताओं से भरा हुआ है, हमारे लिए एक देवता भेज दे जिसे हम अपनी भेंट चढ़ा सकें, जो हमारी भेंट पाकर मुस्करा सके, जो हमारे हृदय की भावनाओं को समझ सके। हमें एक साक्षात् देवता भेज दे।’
पृथ्वी के बाल-काल के मनुष्य की उस प्रार्थना में इतनी सरलता थी, इतनी सत्यता कि स्वर्ग पसीज उठा। आकाशवाणी हुई, ‘जा, मंदिर बना, शरद् ऋतु की पूर्णिमा को जिस समय चंद्रबिंब क्षितिज के ऊपर उठेगा उसी समय मंदिर में देवता प्रकट होंगे। जा, मंदिर बना।’ मनुष्य का हृदय आनन्द से गद्गद हो उठा। उसने स्वर्ग को बारंबार प्रणाम किया।
पृथ्वी पर देवता आएँगे ! इस प्रत्याशा ने मनुष्य के जीवन में अपरिमित स्फूर्ति भर दी। अल्पकाल में ही मंदिर का निर्माण हो गया। चंदन का द्वार लग गया। पुजारी की नियुक्ति हो गई। शरत् पूर्णिमा भी आ गई। भक्तगण सवेरे से ही जलपात्र और फूल अक्षत के थाल ले-लेकर मंदिर के चारों ओर एकत्रित होने लगे। संध्या तक अपार जन-समूह इकट्ठा हो गया। भक्तों की एक आंख पूर्व क्षितिज पर थी और दूसरी मंदिर के द्वार पर। पुजारी को आदेश था कि देवता प्रकट होते ही वह शंख-ध्वनि करे और मंदिर-द्वार खोल दे।
पुजारी देवता की प्रतीक्षा में बैठा था-अपलक नेत्र, उत्सुक मन। सहसा देवता प्रकट हो गए। वे कितने सुन्दर थे, कितने सरल थे, कितने सुकुमार थे, कितने कोमल ! देवता देवता ही थे। बाहर भक्तों ने चंद्रबिंब देख लिया था। अगणित कंठों ने एक-साथ नारे लगाए। देवता की जय, देवता की जय ! इस महारव से दसों दिशाएं गूंज उठीं, पर मंदिर से शंखध्वनि न सुन पड़ी !
पुजारी ने झरोखे से एक बार अपार जन-समूह को देखा और एक बार सुन्दर, सरल सुकुमार, कोमल देवता को। पुजारी काँप उठा। समस्त जन-समूह क्रुद्ध कंठस्वर से एक साथ चिल्लाने लगा, ‘मन्दिर का द्वार खोलो, खोलो !’ पुजारी का हाथ कितनी बार सांकल तक जा-जाकर लौट आया।
हजारों हाथ एक साथ मन्दिर के कपाट को पीटने लगे धक्के देन लगे। देखते ही देखते चन्दन का द्वार टूटकर गिर पड़ा; भक्तगण मंदिर में घुस पड़े। पुजारी अपनी आँखें मूंदकर एक कोने में खड़ा हो गया।
देवता की पूजा होने लगी। बात की बात में देवता फूलों से लद गए, फूलों में छिप गए, फूलों से दब गए। रात भर भक्तगण इस पुष्प राशि को बढ़ाते रहे।
और सबेरे जब पुजारी ने फूलों को हटाया तो उसके नीचे थी देवता की लाश।
2
अब भी पृथ्वी पर मनुष्य था, मनुष्य में हृदय था, हृदय में पूजा की भावना थी, पर देवता न थे। वह सूर्य को अर्घ्यदान देता था, अग्नि को हविष् समर्पित करता था, पर अब उसका असंतोष पहले से कहीं अधिक था। एक बार देवता की प्राप्ति ने उसकी प्यास जगा दी थी, उसकी चाह बढ़ा दी थी। वह कुछ और चाहता था।
मनुष्य ने अपराध किया था और इस कारण वह लज्जित था। देवता की प्राप्ति स्वर्ग से ही हो सकती थी, पर वह स्वर्ग के सामने जाए किस मुँह से। उसने सोचा, स्वर्ग का हृदय महान् है, मनुष्य के एक अपराध को भी क्या वह क्षमा न करेगा ?
उसने सिर नीचा करके कहा, ‘हे स्वर्ग, हमारा अपराध क्षमा कर अब हमसे ऐसी भूल न होगी, हमारी फिर वही प्रार्थना है पहले वाली।’मनुष्य उत्तर की प्रत्याशा में खड़ा रहा। उसे कुछ भी उत्तर न मिला।
बहुत दिन बीत गए। मनुष्य ने सोचा समय सब कुछ भुला देता है, स्वर्ग से फिर प्रार्थना करनी चाहिए।
उसने हाथ जोड़कर विनय की, ‘हे स्वर्ग, तू अगणित देवताओं का आवास है, हमें केवल एक देवता का प्रसाद और दे, हम उन्हें बहुत सँभाल-कर रक्खेंगे।’
मनुष्य का ही स्वर दिशाओं से प्रतिध्वनित हुआ। स्वर्ग मौन रहा।
बहुत दिन फिर बीत गए। मनुष्य हार नहीं मानेगा। उसका यत्न नहीं रुकेगा। उसकी आवाज स्वर्ग को पहुँचती होगी।
उसने दृढ़ता के साथ खड़े होकर कहा, हे स्वर्ग, जब हमारे हृदय में पूजा की भावना है तो देवता पर हमारा अधिकार है। तू हमारे अधिकार हमें क्यों नहीं देता ?’
आकाश से गड़गड़ाहट का शब्द हुआ और कई शिलाखंड पृथ्वी पर आ गिरे।
मनष्य ने बड़े आश्चर्य से उन्हें देखा और मत्था ठोंककर बोला, ‘‘वाह रे स्वर्ग, हमने तुझसे माँगा था देवता और तूने हमें भेजा है पत्थर ! पत्थर !!’
स्वर्ग बोला, ‘हे महान् मनुष्य, जब से मैंने तेरी प्रार्थना सुनी तब से मैं एक गाँव से देवताओं के द्वार-द्वार घूमता रहा हूँ। मनुष्य की पूजा स्वीकार करने का प्रस्ताव सुनकर देवता थर-थर काँपते हैं। तेरी पूजा देवताओं को अस्वीकृत नहीं, असह्य है। तेरा एक पुष्प जब तेरे आत्म-समर्पण की भावना को लेकर देवता पर चढ़ता है तब उसका भार समस्त ब्रह्माण्ड के भार को हल्का कर देता है। तेरा एक बूँद अर्घ्यजल जब तेरे विगलित हृदय के अश्रुओं का प्रतीक बनकर देवताओं को अर्पित होता है तब सागर अपनी लघुता पर हाहाकार कर उठता है। छोटे देवों ने मुझसे क्या कहा, उसे क्या बताऊँ ! देवताओं में सबसे अधिक तेजःपुंज सूर्य ने कहा था-मनुष्य पृथ्वी से मुझे जल चढ़ाता है, मुझे भय है किसी न किसी दिन मैं अवश्य ठण्डा पड़ जाऊँगा और मनुष्य किसी अन्य सूर्य की खोज करेगा !-हे विशाल मानव, तेरी पूजा को सह सकने की शक्ति केवल इन पाषाणों में है !’
उसी दिन से मनु्ष्य ने पत्थरों को पूजना आरम्भ किया था और यह जानकर हिमालय सिहर उठा !
मनुष्य ने अपराध किया था और इस कारण वह लज्जित था। देवता की प्राप्ति स्वर्ग से ही हो सकती थी, पर वह स्वर्ग के सामने जाए किस मुँह से। उसने सोचा, स्वर्ग का हृदय महान् है, मनुष्य के एक अपराध को भी क्या वह क्षमा न करेगा ?
उसने सिर नीचा करके कहा, ‘हे स्वर्ग, हमारा अपराध क्षमा कर अब हमसे ऐसी भूल न होगी, हमारी फिर वही प्रार्थना है पहले वाली।’मनुष्य उत्तर की प्रत्याशा में खड़ा रहा। उसे कुछ भी उत्तर न मिला।
बहुत दिन बीत गए। मनुष्य ने सोचा समय सब कुछ भुला देता है, स्वर्ग से फिर प्रार्थना करनी चाहिए।
उसने हाथ जोड़कर विनय की, ‘हे स्वर्ग, तू अगणित देवताओं का आवास है, हमें केवल एक देवता का प्रसाद और दे, हम उन्हें बहुत सँभाल-कर रक्खेंगे।’
मनुष्य का ही स्वर दिशाओं से प्रतिध्वनित हुआ। स्वर्ग मौन रहा।
बहुत दिन फिर बीत गए। मनुष्य हार नहीं मानेगा। उसका यत्न नहीं रुकेगा। उसकी आवाज स्वर्ग को पहुँचती होगी।
उसने दृढ़ता के साथ खड़े होकर कहा, हे स्वर्ग, जब हमारे हृदय में पूजा की भावना है तो देवता पर हमारा अधिकार है। तू हमारे अधिकार हमें क्यों नहीं देता ?’
आकाश से गड़गड़ाहट का शब्द हुआ और कई शिलाखंड पृथ्वी पर आ गिरे।
मनष्य ने बड़े आश्चर्य से उन्हें देखा और मत्था ठोंककर बोला, ‘‘वाह रे स्वर्ग, हमने तुझसे माँगा था देवता और तूने हमें भेजा है पत्थर ! पत्थर !!’
स्वर्ग बोला, ‘हे महान् मनुष्य, जब से मैंने तेरी प्रार्थना सुनी तब से मैं एक गाँव से देवताओं के द्वार-द्वार घूमता रहा हूँ। मनुष्य की पूजा स्वीकार करने का प्रस्ताव सुनकर देवता थर-थर काँपते हैं। तेरी पूजा देवताओं को अस्वीकृत नहीं, असह्य है। तेरा एक पुष्प जब तेरे आत्म-समर्पण की भावना को लेकर देवता पर चढ़ता है तब उसका भार समस्त ब्रह्माण्ड के भार को हल्का कर देता है। तेरा एक बूँद अर्घ्यजल जब तेरे विगलित हृदय के अश्रुओं का प्रतीक बनकर देवताओं को अर्पित होता है तब सागर अपनी लघुता पर हाहाकार कर उठता है। छोटे देवों ने मुझसे क्या कहा, उसे क्या बताऊँ ! देवताओं में सबसे अधिक तेजःपुंज सूर्य ने कहा था-मनुष्य पृथ्वी से मुझे जल चढ़ाता है, मुझे भय है किसी न किसी दिन मैं अवश्य ठण्डा पड़ जाऊँगा और मनुष्य किसी अन्य सूर्य की खोज करेगा !-हे विशाल मानव, तेरी पूजा को सह सकने की शक्ति केवल इन पाषाणों में है !’
उसी दिन से मनु्ष्य ने पत्थरों को पूजना आरम्भ किया था और यह जानकर हिमालय सिहर उठा !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book