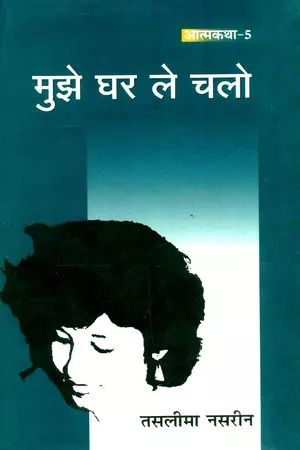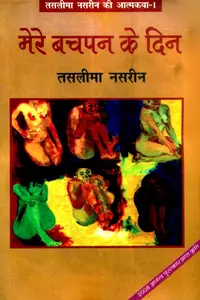|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
उस मकान की दूसरी मंजिल पर यान हेनरिक के बच्चों का एक कमरा था, जहाँ खिलौनों के ढेर में बिस्तर बिछा हुआ था। गैबी ने ङ को वह कमरा दिखा दिया। ङ इससे पहले भी विदेश आए थे, यहाँ रह चुके थे। उनके लिए इन लोगों का घर-द्वार, आचार-व्यवहार, ज़रूर अपरिचित नहीं लग रहा होगा। मैंने गौर किया गैबी की धारणा को मिटाए बिना ही ङ उसके साथ दूसरे माले पर चले गए। यह धारणा मिटाने का जिम्मा क्या सिर्फ मेरा था? गैबी के होंठों की मुस्कान पल-पल बदलती जा रही थी। वह ऐसी भंगिमा में बात करता था, मेरे कंधे पर हाथ रखता था, मुझ तक लपककर आता था, मुझे लिपटाकर चूम लेता था, मानो वर्षों से मुझे पहचानता हो, सिर्फ पहचानता ही नहीं, मेरा बेहद पुराना दोस्त या रिश्तेदार हो। इस मामले में मेरे संकोच का कोई अंत नहीं था। किसी भी शर्त पर चूमना तो दूर की वात, लिपटा-लिपटी भी मेरे लिए संभव नहीं था। बहरहाल, गैबी बेहद व्यस्त था! रेडियो-टेलीविजन पर वह लगातार इंटरव्यू दिए जा रहा था। इंटरव्यू के बीच खाली वक्त में वह इस घर में भी झाँक जाता था। टुकड़ों-टुकड़ों में वातें करता था! कभी पुलिस के साथ, कभी-कभी मुझसे और ङ के साथ।
“तुम क्या कुछ लिख रही हो? लेखक जीव हो, लिखना छोड़कर रहने में ज़रूर बेहद परेशानी हो रही होगी।' गैबी वोलता रहा, “अगर तुम चाहो, तो यहाँ भी लिखना-पढ़ना कर सकती हो।"
"कैसे?"
गैबी उठकर वगल के कमरे में चला गया।
अगले ही पल वंडल-भर कागज़ और कलम लाकर मेरे सामने रखते हुए उसने कहा, “उम्मीद है, फ़िलहाल इनसे ही काम चल जाएगा। कल ही मैं ढेरों कागज और कलम ले आऊँगा।"
गैबी ख़ासा अंतरंग जीव था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लिखने को कहने भर से तो लिखना संभव नहीं होता। इसके अलावा अर्सा हुआ हाथ से मैं नहीं लिख पाती, कम्प्यूटर पर लिखने की आदत पड़ चुकी है। अपनी इस अक्षमता पर मुझे ग्लानि भी कम नहीं है। इंसान अगर सच ही लेखक है, तो उसमें किसी भी परिवेश में लिखने की क्षमता होनी चाहिए।
"हाँ, तो शुरू कर दो।"
गैबी के "शुरू कर दो" जुमले में, तन-मन में चमक भर देने जैसा कुछ था। मुझे किसी खुशी की खुशबू महसूस हुई।
"ठीक ही तो! घर में बैठे-बैठे भी तो कुछ लिखा जा सकता है!"
गैबी और ङ, दोनों ने ही मेरे लिखने के बारे में ऐसे गंभीर लहजे में बोलना शरू किया कि मझे लगा. मेरे हर अक्षर, हर शब्द. हर वाक्य की तरफ समची दनिया टकटकी बाँधे देख रही है। दुनिया पर तरस खाकर ही मैं कुछ दान करूँ। आह! मैं कितनी क्षमतावती सरस्वती थी!
"अब, मुझसे हाथ से नहीं लिखा जाता।" मैंने मिनमिनाकर कहा।
"क्यों?" गैबी की आँखों में ढेर-ढेर विस्मय झलक उठा।
"कंप्यूटर पर लिखने की आदत पड़ चुकी है-"
उसने मेरी बात सुनी, मगर अनसनी कर देने जैसी मुद्रा में मेरी तरफ देखा। एक बार फिर वही जुमला सुनने के लिए, उसने अपने कान आगे बढ़ा दिए। मगर सुना कुछ भी नहीं।
अचानक उसे कोई और बात याद आ गयी और उसने वही बात छेड़ दी, "सुनो, एक बात के बारे में तुम्हें पहले से ही आगाह कर दूँ। अपने को कभी कम्युनिस्ट मत कहना और कभी भी अपने को नारीवादी मत कहना।"
“क्यों? यह कैसी बात? समाजतंत्र में आस्था रखने में ऐसा क्या नुकसान है?"
"पश्चिम में कम्युनिज्म बकवास शब्द है।"
"लेकिन अपने को नारीवादी क्यों न कहूँ? मैं तो नारीवादी ही हूँ।"
होंठों पर उँगली रखकर गैवी ने उसी तरह धीमी आवाज़ में जवाव दिया, "होशियार! अब यह शब्द अपनी जुवान पर मत लाना। यहाँ नारीवादियों को कोई पसंद नहीं करता।"
"वजह?"
"वे लोग मर्द-दुश्मन होती हैं! समलैंगिक होती हैं।"
“धत् ! वकवास बात है।''
"बकवास नहीं है। सुनो, मेरी वात मानो। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ।" गैबी चला गया। मेरा मन क्षोभ से कड़वा आया।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ