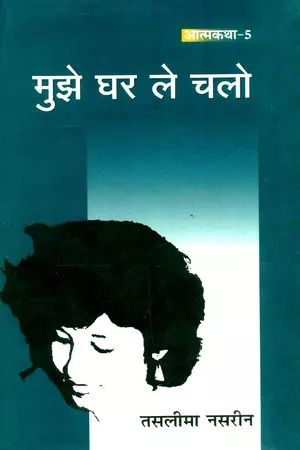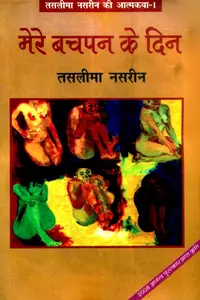|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
बहरहाल काफी देर तक छोटू' दा की छिः-छिः कथा सुनते रहने के बाद आखिरकार मुझे फोन रख देना पड़ा। उसके लहजे में एक किस्म की व्यंग्य-भरी उच्छृखलता थी। क्यों? मेरी किसी प्राप्ति की तरफ निगाह डालने के बजाय वह सड़े-गले झूठ में मज़ा क्यों ले रहा था? वह उन लोगों के पक्ष में मज़ा ले रहा था, जो लोग मेरी हत्या के लिए साल-भर तक उछल-कूद मचाते रहे। मैं इस छोटू' दा को पहचान नहीं पाती। वैसे मैं अपने को भी पहचान नहीं पाती, जो 'मैं' फोन रख देने के बाद भी, फोन के सामने आधी रात तक बैठी रही! भोर हो गई, मैं बैठी रही। सामने की खिड़की के उस पार मौत जैसा अँधेरा! अँधेरे में स्थिर, निश्चल काला पानी! काले पानी में चंद व्यापारिक नावें ! आसमान में कहीं बूंद-भर भी रोशनी नहीं है! यहाँ-वहाँ, दो-एक कृत्रिम रोशनी! कुछ ही देर में यह कृत्रिमता, महासमारोह के साथ अपना राज-पाठ शुरू कर देगी, जहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है! मैं अपनी नन्ही-सी देह लिए सबसे दूर यहाँ पड़ी रहूँगी! इस शहर में! बस खा-पी रही हूँ, चल-फिर रही हूँ, उठ-बैठ रही हूँ। इस समाज और इस समाज के लोगों से मेरा शैशव, कैशोर्य, यौवन का, कुछ भी कोई तुच्छ तिनका-भर जुड़ाव नहीं है। मेरा जीवनवोध, मेरा लिखना-पढ़ना, मेरी जंग, मेरे सपनों के साथ, यहाँ की किसी भी बात का कोई वास्ता नहीं है। इसके बावजूद मुझे ही यहाँ पुलिस-सुरक्षा दी जा रही है! किसे दिखाने के लिए? ताकि किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत न पड़े। वैसे अब तक तो सभी जान ही चुके हैं कि इस्लामी कट्टरवादी जिस लड़की को मार डालना चाहते थे, स्वीडन जैसे उदार मानवतावादी राष्ट्र ने उसकी जान बचा ली और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा में, राष्ट्रीय मान-सम्मान देकर उसे सिर पर विरा रखा है। सिर पर या काठ के मंच पर? मैं उस मंच से, मंच के ढाँचे से मुक्ति चाहती हूँ! इस शर्मनाक सुरक्षा से मैं रिहाई पाना चाहती हूँ। क्या इस बात की किसी को ख़बर है?
सुनो, सुरक्षा-व्यवस्था, अब, मुझे मुक्ति दो,
ब्रह्मपुत्र नद के उस पार शंभुगंज,
उसके दक्खिन में सवा माइल पैदल चलकर,
एक जामुन का पेड़! पिछवाड़े एक कच्ची झोंपड़ी!
मुझे वहीं जाना है! वहीं है, पार्वती लोगों का घर!
पार्वती को जानते हो?
जहाँ चूल्हे पर भात तक नहीं खदबदाता. दोनों जून,
जहाँ कोटरी की छादन के छेदों से
टपकता है वा का जल!
मुझे रिहा कर दो न्यू कैसल, नॉटिंघम्, बेलफास्ट,
रिहा कर दो ब्रसेल्फ, वॉन, ड्रेसडन, म्यूनिख!
अब मैं नहीं चाहती भाषण देना, ऊँचे-ऊँचे मंच पर!
नहीं चाहती लोगों की तालियाँ!
फूलों के गुलदस्तों का मुझे कोई शौक नहीं!
मुझे माफ करो, चार्ल्स ब्रिज,
माफ करो कुक्सहेवेन के पव,
माफ करो, यूरोपियन पार्लियामेंट...
अब सपनों के पौधे नहीं सींचती पार्वती,
मुझे जाना है, पार्वती के घर!
मेरे पास पानी मौजूद है, आँखों में!
इतना लिखकर मैं सो गई, लिखने की उसी मेज़ पर सिर रखकर! भीगा हुआ कागज मेरे गाल से चिपका रहा! अकेली मैं! कहीं कोई नहीं! कहीं, कोई आहट, कोई अवाज़ तक नहीं! ऐसी निर्जन निस्तब्धता में, मैं कभी नहीं रही। मेरी एक अदद माँ थी, अब्बू थे, भाई लोग थे! मेरी बहन थी! घर-भर लोग थे! दोस्त, संगी-साथी थे। उन लोगों के शोरगुल, धौल-धप्पे में मैं जिंदगी गुज़ार रही थी! वह क्या मेरा पिछला जीवन था? उस जीवन के साथ अब दुबारा मेरी भेंट क्यों नहीं होती?
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ