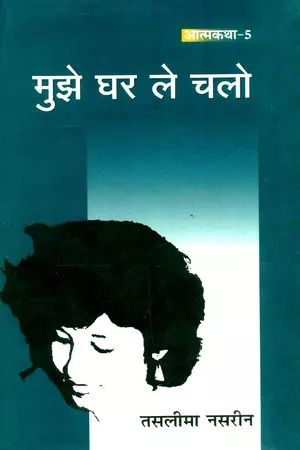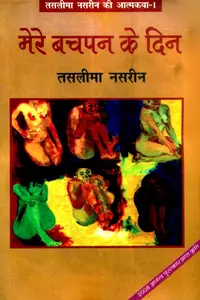|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
देश आज़ाद होने के बाद, हमारे नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र वगैरह अच्छे-अच्छे लफ्जों से ठांसकर, गणतंत्र तैयार किया था, लेकिन गणतंत्र का नियम ही यही है कि जैसे राजनीति में भिन्न-भिन्न मतवाद होते हैं, उसी तरह किसी भी विषय में भिन्न-भिन्न मत हो ही सकते हैं। किसी भी विषय पर सभी लोग एकमत नहीं होते और हर किसी को अपनी राय जाहिर करने की आज़ादी है। चलो, मान लिया कि मेरी राय, बाकी सभी लोगों की राय से विल्कुल अलग थी, लेकिन इस वजह से मेरे घर पर हमला क्यों? मुझ पर पत्थर क्यों बरसाए जाएंगे? खुले आम, डंके की चोट पर, मेरे सिर की कीमत क्यों लगाई जाएगी? मुझे अपना देश क्यों छोड़ना पड़ेगा? पच्चीस साल की आज़ादी ने, हममें से किसी को भी, सच्चे अर्थों में आज़ाद नहीं किया।
असल में, गरीब देश है, सबके लिए आहार नहीं जुटा पाता। सबके सिर पर छत नहीं है; तन-बदन पर कपड़े नहीं हैं; सबको शिक्षा का अवसर नहीं मिलता।
चलो, गर्व करने लायक धन-दौलत, रुपए-पैसे भले ही न हो, हमारा कुछ इतिहास तो है। भाषा आंदोलन, मुक्ति-युद्ध का इतिहास । जो कौम अपनी भाषा और संस्कृति वचाने के लिए जुलूस निकालती है, सभाएँ करती है और उन लोगों के खून से राजपथ नहा उठता है, जो जाति धर्म का बंधन तुच्छ करके जंग पर उतर आती है, ऐसी शद्ध-पवित्र कौम दिनोदिन वाद-हाल क्यों हुई जा रही है? धर्म ने राजनीति पर अपने दाँत गड़ा दिए हैं; संसद और समाज को निगल रही है। स्कूलों की संख्या वढ़ने के बजाय मस्जिद-मदरसों की वाढ़ आ गई है। कितावें जलाने-फूंकने का यज्ञ जारी है। मुट्ठी भर असभ्य लोगों ने लेखक-हत्या की कसम उठा रखी है और सभी लोगों ने आराम से इस तरफ से अपना मुँह फेर रखा है। इन सबके लिए तो 16 दिसंबर नहीं आता! ऐसा तो पाकिस्तानी तानाशाहों के ज़माने में होता था। रवीन्द्र संगीत गाना नहीं चलेगा, राधा-कृष्ण, भगवान वगैरह शब्दां वाले भजन-गीतां का प्रचार वंद! अगर ऐसा कुछ लिखा या किया जाए, जिसकी राय औरों से मेल न खाती हो, वह चाहे कवि हो या राजनीतिज्ञ, चाहे गायक हो या परचून की दुकान का मोची-उसके पेट पर रस्सी वाँधकर उसे खींच लाओ और जेल में ठूस लो। बचपन में मैंने अपने भाइयों को गाते हुए सुना है, लेकिन अब वे लोग मेरी जुबान से भापा छीन लेना चाहते हैं। वे लोग वात-बात में, मेरे हाथ-पाँव जंजीर से जकड़ देना चाहते हैं। फिर पिछले और आज के शासकों में फर्क कहाँ रहा? इन्हीं सबके लिए ही क्या सुदीर्घ नौ महीनों तक जंग जारी रही? माँ ने कहा था कि अव से हम सब जी भरकर अपनी वात जाहिर कर सकेंगे। रास्ते-घाट पर चल सकेंगे; निश्चिन्त होकर जी सकेंगे। अव हमें भागते नहीं फिरना होगा, लेकिन तुझे तो भागते रहना पड़ रहा है। तो माँ ने क्या गलत कहा था? ज़रूर उन्होंने ग़लत कहा था। सच तो यह है कि सन् इकहत्तर की सोलह दिसंवर को, हमें अपने लिए एक देश मिला था, लेकिन इसे ठीक तरह से मन लायक गढ़ा नहीं गया। मैं तो एक ऐसे बांग्लादेश का सपना देखती हूँ, जहाँ पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी वंग भापी आ मिलेंगे। धर्म में विश्वासी और अविश्वासी, औरत-मर्द, एक जैसा अधिकार लेकर जीएँगे। अपनी मन-मर्जी के मुताविक बातें करने पर, सुनने पर जेल या जुर्माना नहीं होगा। अपने देश या देश के बाहर फ़रार-हाल में भागते नहीं फिरना होगा। हाँ, मैं एक ऐसे बांग्लादेश के ख्वाब देखती हूँ, जहाँ इंसान को अपनी तकलीफ या सुख की बात कहने में कोई दुविधा नहीं होगी, वहाँ इंसान खाते-पहनते, सुख-चैन से जीएगा, जीवन बसर करेगा। जहाँ मैं भी अपनी मर्जी के मुताबिक चल-फिर सकूँगी, पुस्तक-मेलों के अड्डा में भाग ले सकूँगी, इंसानों की भीड़ में घुल-मिल सकूँगी। इक्कीस फरवरी की भोर, शहीद मीनार पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे सकूँगी। पच्चीस मार्च और सोलह दिसंबर को मैं भी कविता-पाठ कर सकूँगी! मंचों पर, जुसूसों में, मठ-मैदानों में! अपने घर की छत पर झंडा लहरा सकूँगी।
एक-एक करके साल-दर-साल गुज़रते जा रहे हैं। आज भी मेरी देश-वापसी नहीं हुई मेरे अपने देश, मेरे अपने घर की तरफ मैं नहीं लौट पाई। मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ, अपनी दुःखियारी माँ की गोद में वापस पहुँचना चाहती हूँ। अर्सा हुए मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। बस, आखिरी बार उसे तव देखा था, जिस रात समूची देह पर काली चादर लपेटकर, मुझे हवाईअड्डे जाना पड़ा था। मेरी माँ फर्श पर लोट-लोटकर रो रही थी! निस्तब्ध रात का सन्नाटा और छाती-फाड़ रुलाई, कहीं दुश्मन के कानों तक न पहुँचे, किसी को मेरे जाने की आहट न मिले, इसलिए किसी ने उनका मुँह दबोच लिया था। माँ की गोद सूनी करकं, इंसान, बस चला गया! किसी लापता ठिकाने की तरफ चल दिया। अब माँ अकेली है! हाथ बढ़ाने पर शून्यता और खालीपन की विशाल देह-भर उसके हाथ आती होगी, और कुछ नहीं! अब जब माँ चीख-चीखकर रोती होगी और दीवालों से सर टकराती होगी, अड़ोसी-पड़ोसी सुनते होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा, जो उनकी पीठ पर तसल्ली का हाथ रखे।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ