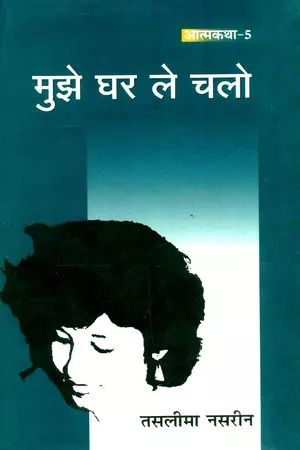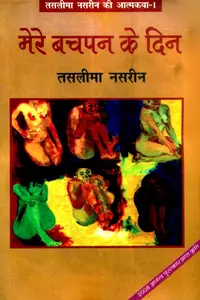|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
बांग्लादेश में मैंने जिंदगी के बत्तीस साल गुज़ारे हैं। उन बत्तीस सालों में मुझे ढेरों दुःख मिला है! अनगिनत दुःख! काफी कुछ के लिए, अनगिनत वार उदास हुई हूँ, मैं चीख-चीखकर रोई हूँ! लेकिन यह अहसास कभी नहीं हुआ कि वक्त थम गया है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है। कभी भी मेरी समूची जिंदगी, फिसलकर, अतीत के खड्डे में नहीं जा गिरी! अब यह हालत है कि मेरे आगे-पीछे, अतीत के अलावा और कोई जिंदगी नहीं है। मैं अतीत में जी रही हूँ, अतीत में ही जीती रहूँगी। मुझे वर्तमान का कभी अहसास नहीं होता। अब जिस जिंदगी में हूँ, वह है भी और नहीं भी! मुझे लेकर, देश-देश में उत्सव मनाया जा रहा है। उन उत्सवों में, मैं भी शामिल होती हूँ! आँखें भर-भरकर विभिन्न देश देखती हूँ, लेकिन जो भी देखती हूँ, अगले दिन याद नहीं रहता। अगर याद भी करूँ तो क्या देखा, क्यों देखा, इसकी कोई वजह मैं नहीं ढूंढ़ पाती। मुझे बहुत-से लोग सलाह देते हैं,-इतना-इतना जो घूमती हो, इतने तजुर्वे बटोर रही हो, सब लिख डालो, लेकिन मेरे मन में कभी बूंद-भर भी इच्छा नहीं जागती। इच्छा न होने पर भी कभी-कभी लिखने के नाम पर लिखने बैठी हैं, लेकिन एक शब्द भी लिखना, मेरे लिए संभव नहीं हुआ। कभी-कभी अचानक इच्छा जागी भी और कागज-कलम लेकर या कम्प्यूटर के सामने बैठी भी, तो भी दिन-भर में एक भी वाक्य नहीं लिख पाई। मेरा कम्प्यूटर मेज पर पड़ा रहता है. मैं खिडकी के सामने बैठी रहती या बिस्तर पर लेटी रहती हूँ। चारों तरफ की निःशब्दता में मेरी अपनी निःशब्दता घुल-मिलकर एकाकार हो जाती है और एक खौफ़नाक मृत्यु जैसी परिस्थिति साकार हो उठती है। कभी तो मेरी यह समझ में ही नहीं आता कि असल में मैं इंसान हूँ या मशीन! ज़िंदा हूँ या मुर्दा?
कहाँ तो मुझे अपना निर्वासित जीवन धीरे-धीरे कबूल कर लेना चाहिए था, इस जीवन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए था, इस जीवन का सारा सौंदर्य ग्रहण करके, अपने को समृद्ध करना चाहिए था। जो मिल रहा है, उसके लिए मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन हैरत है, दिनों दिन सब कुछ के प्रति अजीव निस्पृहता का अहसास होने लगा है। मैंने अपने सिर पर पहनाया गया मुकुट तोड़-फोड़ डाला है; ऐसे तमाम आमंत्रण-निमंत्रण अपनी दोनों हथेलियों से हटाकर, परे कर दिए हैं, जो मुझे जिंदगी में दुवारा नहीं मिलने वाले। मुझे श्रद्धा-सम्मान की भी परवाह नहीं रही। लोग मेरी किताबें छापना चाहते हैं, लेकिन तमाम आवेदन इधर-उधर उड़ते-फड़फड़ाते, खिड़की की राह बाहर चले जाते हैं। पुरस्कार देना चाहते हैं, नहीं लूंगी। आओ, अपना वक्तव्य दो, नहीं दूंगी। आओ, अपनी जिंदगी के तजुर्बे बताओ, नाऊ! विरोध करना है, बगावत करना है। जुलूस में चलना है आओ! ना! नारीवाद पर कुछ कहोगी, नास्तिकता की । बात? ना! मानवतावाद के बारे में? मानवता के बारे में? ना! लोग इंतज़ार कर रहे हैं, करें! रो रहे हैं, रोने दो! मेरा कुछ भी मन नहीं होता! कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। ऐश ट्रे में भरी हुई राख इधर-उधर छितराने लगी है! चाय की प्यालियों में राख! पानी के गिलास में राख! छोटी तश्तरी में राख! चम्मचों पर राख! मेज़ पर राख! कुर्सियों पर राख! बिस्तर पर राख! किचन में राख! टायलेट में राख! फर्श पर राख! कालीन पर राख! इतनी सारी राख में मैं उड़ती हुई! ये राख मुझे कहाँ उड़ाएँ लिए जा रही है, यह राख ही जाने! यह जानना, मेरे वश में नहीं है। वक्त भी नहीं है! समूचा कमरा विराट ऐश ट्रे बन गया है। मैं खुद भी एक राखदान बन गई हूँ। मेरे अंदर जो कुछ भी है, सब धीरे-धीरे राख होता जा रहा है। दिमाग, गले की नसें, फुसफुस, हृतपिंड, किडनी, यकृत, अग्नाशय, पाकस्थली, छोटी आँत, बड़ी आँत, मूत्राशय, योनि-सब राख होते जा रहे हैं।
जब इस कदर निस्पृहता छाई रहती है, तब गंदगी, कूड़ा-करकट, आलतू-फालतू, फफूंद, बैक्टीरिया, दुर्गन्ध में पड़ी रहती हूँ। इसी में बहती रहती हूँ, डूबी रहती हूँ। फोन बजता रहता है, मैं फोन नहीं उठाती। चिट्रियों के ढेर लगे हैं। मैं एक भी चिट्ठी नहीं खोलती। कमरे से बाहर नहीं निकलती। घर से बाहर तब निकलती हूँ, जब सिगरेट या खाना ख़त्म हो जाता है। टेलीविजन के सामने बैठी रहती हूँ। सारे कार्यक्रम जर्मन भाषा में, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ता। सिर्फ टकटकी बाँधे देखती रहती हूँ। जितना कुछ खाना होता है, सोफे पर लेटी-लेटी खाती रहती हूँ। संगीत नहीं सुनती। कविताएँ नहीं पढ़ती। किसी किताब तक को हाथ नहीं लगाती। जब एक भी थाली साफ-सुथरी नहीं बचती, एक भी चम्मच साफ़ नहीं बचता, तब दोस्तों से कहकर, काम कराने के लिए, कोई बंदा रख लेती हूँ! इस बार पूर्व जर्मनी की कोई लड़की आई है! पचास मार्क फ़ी घंटे के हिसाब से उसने काम शुरू किया है। अपने दफ्तर का काम-काज निबटाकर, शाम को वह मेरे यहाँ चली आती है। उसे लड़की का नाम है-उरसुला। वह एक अक्षर भी अंग्रेजी नहीं जानती। जुबान पर ताला जड़े, वह हर दिन तीन घंटे काम करती रहती है।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ