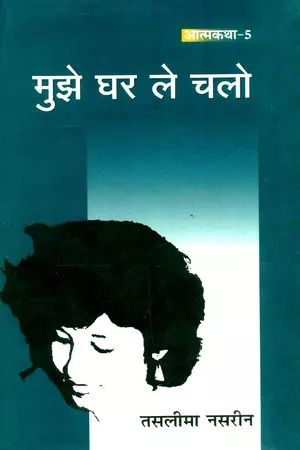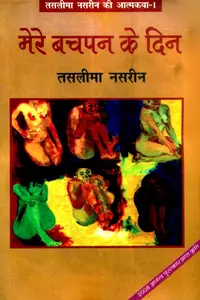|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
जब तन-मन में ऐसी निस्पृहता छाई है, मैं बैंक से आया कोई पत्र भी खोलकर नहीं देखती। बैंक के ज़रूरी कागजात महीनों-महीनों बिना खोले पड़े रहते हैं। कभी-कभी तो तमाम चिट्ठियाँ बिना खोले ही कूड़े की टोकरी में फेंक देती हूँ या वे अन-खुली चिट्ठियाँ कागज़ों के ढेर में समा जाती हैं। जब नितांत अकेलेपन का अहसासा होता है तो मैं बस में या ट्राम या मेट्रो में सवार नहीं होती, इन दिनों मैं टैक्सी में चढ़ती हूँ। जहाँ-तहाँ मुट्ठी भर रुपए दे आती हूँ। कितने रुपए बचे हैं, कितने रुपए खर्च हो गए, मैं हिसाब नहीं रखती। दुनिया में कहाँ, क्या हो रहा है, यह जानने का भी मन नहीं होता।
जब निस्पृहता छाई होती है, तब घंटों-घंटों, खामखाह ही ढाका, मयमनसिंह, कलकत्ता, फोन पर बातें करती रहती हूँ। जब ऐसी निस्पृहता के मूड में होती हूँ, छोटू' दा को ब्रसेल्स से बर्लिन चले आने को कहती हूँ। छोटू' दा के साथ बहुत खुशी खुशी समूचा शहर घूमती-फिरती हूँ। उसके लिए शर्ट-जूते ख़रीद देती हूँ। वह जो चाहता है, वह तो देती ही हूँ, जो नहीं चाहता, वह भी ख़रीद देती हूँ। रुपए मैं कागज़ की तरह उड़ाती रहती हूँ। रुपए अब मेरे लिए काफी कुछ महज कागज जैसे हैं। डेआआडे ने मुझे सबसे खूबसूरत इलाके के, बेहद खूबसूरत मकान में एक एपार्टमेंट दिया है और महीने के खर्च के लिए ढाई हज़ार ङ्येचेमार्क देता है। वे ढाई हज़ार डॅयेचेमार्क अपनी आँखों से मैंने कभी नहीं देखे। उल्टे मुझे ही डेआआडे को देना पड़ता है! वजह है, फोन बिल! हर महीने, फोन का विल आता है, साढ़े तीन हज़ार-चार हज़ार मार्क! यानी दो से तीन लाख रुपए! डेआआडे जो बिल चुकाता है, उसमें ढाई हज़ार काटकर बाकी बिल मुझे भेज देता है। बाकी बिल मैं चुका देती हूँ। मेरी जेब में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मौजूद रहता है। कार्ड के जरिए, मैं कितने रुपए खर्च करती हूँ, इसका मैंने कभी हिसाब नहीं रखा, आज भी नहीं रखती। मेरे आस-पास के लोगों की मेरे अंदर के एकाकीपन की बूंद-भर भी ख़बर नहीं होती। छोटू' दा भी बेख़बर रहता है। मेरा जितना भी संबल या अर्जन-उपार्जन होता है, सब छोटू' दा को दे डालती हूँ। उसे किताबें, कपड़े लत्ते, फोटो एलबम, उपहार की चीजें, उस पर लुटा देती हूँ। वेनिस की चाबी, बार्सेलोना की चाबी, वाल्टेयर की पाँचों खंड किताबें, जिने सारे सोने के मेडल मिले हैं, सब उसे दे देती हूँ, अपने पास कुछ भी नहीं रखती।
छोटू' दा अचरज से मुँह बाए मुझे देखता रहता है।
“यह सब तो तेरे काम की चीजें है, मुझे क्यों दे रही है?"
“यह सब ले जाकर, मेरे घर में रख देना।" मैं शांत आवाज़ में कहती हूँ। "तेरा कैसे चलेगा?"
"काफी अच्छी तरह चल चुका मेरा। तुम जाकर कमाल हुसैन से बात करो। कहना, चाहे जैसे भी हो, मैं अपने वतन वापस लौटना चाहती हूँ।"
यह बात छोटू' दा भी समझता है कि मैं अपना सारा कुछ जो दिए दे रही हूँ, उसकी वजह यही है कि मैं अपने देश जाऊँगी। चाहे जैसे भी हो, जरूर जाऊँगी। छोट्र' दा वतन वापस लौट जाता है, लेकिन उम्मीद की ख़बर, वह कभी नहीं सुनाता। छोटू दा मुझे कोई उम्मीद नहीं बँधाता। खैर, उम्मीद की ख़बर, कोई भी नहीं देता।
अच्छा, चलो, बांग्लादेश नहीं जा सकती, कलकत्ता तो जा सकती हूँ? वहाँ निखिल सरकार हैं. परे पश्चिम बंगाल में मेरे कितने ही शभाकांक्षी मौजूद हैं। मैं अपने नाते-रिश्तेदारों को खबर कर देंगी कि वे सभी लोग कलकत्ता चले आएँ। वहीं भेंट हो जाएगी। मैं दमफूली सांसें सम्हाले हुए स्वीडन के दूतावास में पहुँचती हूँ। वीसा के लिए दरखास्त लिखती हूँ। वे लोग मुझे काफी देर-देर तक खड़ा रखते हैं, बिठाए रखते हैं और बाद में सूचित कर देते हैं कि मैं अगले दिन आऊँ। अगले दिन मैं फिर जाती हूँ। खड़ी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। दो-तीन घंटे गुज़र जाने के बाद, अंदर से खवर आती है, आज काम नहीं होगा, मैं किसी और दिन आऊँ।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ