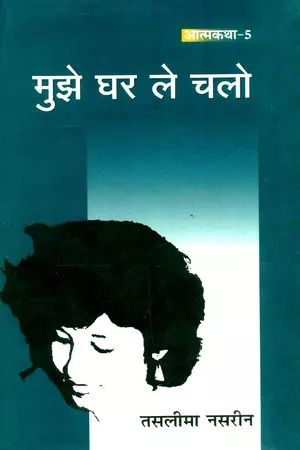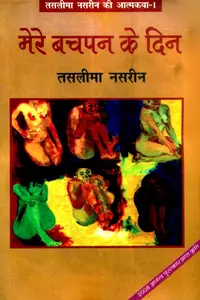|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
और दिन जाती हूँ, कहा जाता है, किसी और दिन! जब मैं बेहद उतावली हो उठती हूँ, तो राजदूत मुझे इत्तला देते हैं कि मेरी दरखास्त दिल्ली भेज दी गई है, दिल्ली से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब दिल्ली ने वीसा देने की अनुमति के वारे में तार भेजा जाएगा, तभी मुझे वीसा मिलेगा, अन्यथा नहीं! दिल्ली से खवर कव आएगी, यह जानने के लिए में फोन करती हूँ, फैक्स भेजती हूँ, अभी सशरीर जा धमकती हूँ और उनकी परेशानी की वजह बनती हूँ। इसी तरह महीन-दो महीन-तीन महीने गुज़र जाते हैं। वे लोग जानकारी देते हैं, वीसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरे इस सहज-सरल सवाल का जवाव उतना सहज नहीं होता। कोई मुश्किल जवाव भी नहीं मिलता। मझे वीसा क्यों नहीं मिलेगा, मझे यह जानने का भी हक नहीं है। नहीं, इसके बाद भी मैं उम्मीद नहीं हारती। कुछ ही महीनों बाद मैं फिर दरख्वास्त जमा करती हूँ। मेरे साथ फिर वही बर्ताव किया गया है। मुझे वीसा नहीं मिलेगा। मुझे भारत में नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों, मैंने क्या कोई गुनाह किया है? मैं तो सिर्फ अपने नाते-रिश्तेदारों से मिलने जाऊँगी। मझे जाने दें। इस विदेश में मेरा दम घुट रहा है। मैं अव, जी नहीं पा रही हूँ। मुझे अपनी मिट्टी, अपने लोगों के पास जाने दें, मुझे सांस लेने दें। ना, मेरा कोई आवेदन, कोई आवेग, किसी को हल्का-सा भी स्पर्श नहीं करता। सब अपनी-अपनी रौ में, अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। हाँ, किसी-किसी को मेरे लिए दुःख भी होता है, वे लोग इसके लिए मेरे दुर्भाग्य को जिम्मेदार ठहराकर मुँह फेर लेते हैं या फिर भारत-बांग्लादेश की कूटनीति के बारे में उलझनों के जाल पर गंभीर आरोप मढ़ते हुए, अपने-अपने सुख-चैन की तलाश में दत्तचित्त हो जाते हैं। सन् चौरानवे, पन्चानवे, छियानवे...कई साल पार हो गए, मैं भिन्न देश में नितांत अकेली पडी रहती हैं। किसी हरे-भरे पेड को जड से उखाड़कर, बर्फ की पर्तों तले उछाल फेंका गया। मुझे अहसास हो रहा है, मेरे डाल-पत्ते नष्ट होते जा रहे हैं, मेरे फल-फूल मुरझाते जा रहे हैं, मेरी जड़ों में सड़न पकड़ चुकी है और मैं घटते-घटते इत्ती-सी हो गई हूँ, विल्कुल अदृश्य होती जा रही हूँ।
बांग्लादेश के लेखकों, बुद्धिजीवी लोगों से मेरा संपर्क धीरे-धीरे धूमिल पड़ता जा रहा है। दिनोदिन वे मेरी पहुँच से बाहर जाते-जाते, वे लोग आकाश में सुदूर नक्षत्र वन गए हैं। अकेली मैं ही क्या फोन करती रहूँ? और कोई तो कभी एक छोटा सा पत्र तक लिखने या फोन करने का दायित्व महसूस नहीं करता। वैसे यह वात मैं भी समझती हैं कि उनकी नये-नये समाचारों में, मैं शामिल नहीं हैं। काश, मुझे वतन लौटा लाने के लिए, कोई तो कुछ कहे। मेरे कितने ही घनिष्ठ लेखकों से, माँ ने कितनी-कितनी आरजू-मिन्नत की, लेकिन किसी ने माँ की तरह पलटकर भी नहीं देखा। मन का अभिमान मुझे और भी गहरे बर्फ तले दवा देता है। अभिमान की धारदार ठंडी छुरी मेरे जीवन की सारी गर्माहट थक्के-थक्के की शक्ल में काटती रहती है।
वैसे अनगिनत लेखक अपना वतन छोड़ने के लिए लाचार किए गए हैं। वहुतेरे लोगों ने निर्वासन में जिंदगी गुज़ारी है। मैं कोई अकेली नहीं हूँ। वे लोग तो ख़ासे मजे में जीते रहे। उस तरह मैं क्यों नहीं जी पाती? मुझं क्यों तकलीफ होती है? इस सर्द देश में काठ के मकानों में, फूल के गमले में वोए हुए चारे की तरह मैं ! मुझे यहीं पलने-बढ़ने और बड़े होने की हिदायत दी जाती है, लेकिन वहाँ की रोशनी-हवा तो मेरे लिए नहीं है। यहाँ जीना, मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे अपना देश चाहिए, अपनी माटी चाहिए। वही जीवन पाने के लिए में मासूम-सी, आकुल-व्याकुल रहती हूँ। मेरी जिंदगी, मेरे पास से कहीं खोती जा रही है। यहाँ मुझे एक अजनवी, जिंदगी थमा दी गई है और कहा जाता है, यही जिंदगी जीओ, लेकिन वह जिंदगी तो मेरी नहीं हैं इस जिंदगी को तो मैं पहचानती भी नहीं। यह जिंदगी कैसे जी जाती है, मैं नही जानती। जान कहाँ की सर्वग्रासी भूख मुझे नोंच-नोंचकर खाए जा रही है। वह भूख जितनी हहरकर मुझ पर हमलावर हाती है, मेरी सांसों की तकलीफ, उछल-उछलकर आकाश के वादल छू लेना चाहती है। बादलों को छूने से पहले ही व इधर-उधर फिसल जाते हैं। सिर्फ अकारथ-सा वर्फीला हाथ फैला रह जाता है। एक अकथनीय यंत्रणा हथेली से निकलकर समूचे तन-बदन में फैल जाती है और उस यंत्रणा से सिर्फ मेरा तन या मन ही नहीं, समूचा अस्तित्व तड़प उठता है।
हर देश में मुझे लेकर तहलका मचा हुआ हैं, मैं हूँ राजनैतिक नज़रिए से बिल्कुल 'करेक्ट' यानी उपयुक्त चीज़ हूँ। मुझे मंच पर विठा दो और खुद अपने लिए नाम कमाओ। जब मैं मंच से उतर आऊँ, मुझे धन्यावाद दे देना, बस! मैं फिर वही अकेली की अकेली! उसके बाद मैं समूची दुनिया में अकेली हो आती हूँ। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किए बैठी रहती हूँ। उसके बाद मैं मर गई या ज़िंदा हूँ, कोई खवर भी नहीं लेगा। ख़बर लेना चाहेगा भी नहीं। तीखे अकेलेपन में मैं एक के वाद एक सिगरेट फूंकती रहती हूँ और खांसती रहती हूँ। मैं ढलती जाती हूँ। ऐसा एक भी वंदा नहीं है, जो मेरे कंधे पर हौले-से हाथ रखे। बहुत बार तो मेरा मन होता है, आत्महत्या कर लूँ।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ