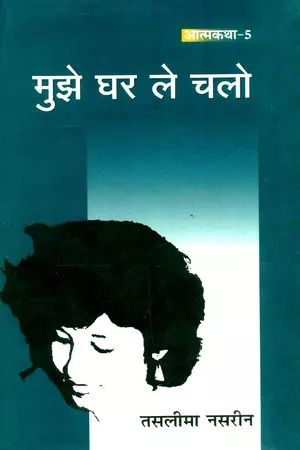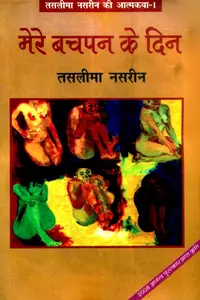|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
यह बात मैं बखूबी समझती हूँ कि मैं सकुशल नहीं हूँ। देश की जो थोड़ी बहुत खबरें मिलती रहती हैं, उससे मेरे वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं बंधती। मुझे पता चला, छोटू' दा ने अपने बीवी-बच्चों को अमेरिका भेज दिया है। मैंने छोटू' दा से इतना-इतना कहा कि मैं वापस लौट आऊँगी। हम सब एक साथ रहेंगे। कोई देश से बाहर न जाए। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने बारी-बारी से अपने बीवी-बच्चों को विदेश भेज दिया। उसने मिलन को भी भेज़ दिया है। अमेरिका में मिलन के पाँव जरा जम जाएँ. वह यास्मीन को भी बला लेगा। जब मुझे इस किस्म की खबरें मिलती हैं, एक-एक करके मेरे सपनों का महल ढहता जा रहा है। सपनों के बिना इंसान जिंदा कैसे रहे? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं ज़िंदा भी हूँ या नहीं। छाती के अंदर हर वक्त अकेलेपन की आँधी चलती रहती है। जैसे छाती के अंदर कुछ भी नहीं है! सब खोखला है। सांस लेते हुए भी डर लगता है! जैसे सांसें अंदर जाते ही शून्य में विलीन हो जाएँगी। अगर सभी लोग एक-एक करके चले जाएँगे तो मैं किसके पास लौटूंगी? उनमें से क्या कोई भी, एक-दूसरे से अलग होकर सुखी हो सकेगा? बेहद अकेलापन लगता है। यह जो जीवन में जी रही हूँ, बेहद अर्थहीन लगता है। इस जीवन के दिन-रात, सुबह-दोपहर-शाम में नहीं गिनती। ये शामें, रात, आधी रात, तीसरे पहर की रात, गंभीर रात, भोर-रात-ये सब तो मेरी गिनती में ही नहीं आतीं! ये सब मुझे अपने भी नहीं लगती। लगता है, जैसे मैं इन सबसे मीलों दूर हूँ। लगता है, ये सब समय मेरे नहीं, किसी और के हैं। मैं किसी दूसरे के वरामदे में, किसी और के समय में, अनाहूत-सी आकर खड़ी हो गई हूँ। इन दिनों मैं जो जीवन जी रही हूँ, उसे असल में जीवन नहीं कहते! जीवन-पार के बाद का अतिरिक्त जीवन है! अतिरिक्त चीज़ है! गैर-ज़रूरी!
मुझे एक अदद मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। उस मौत में मुझे अपने खरखराने की आवाज़ भी सुनाई देती है। नहीं, मैं विस्मित नहीं होती। मरी हुई लाश को जैसे किसी बात पर अचरज नहीं होता, मेरी भी मरी हुई देह को कोई अचरज नहीं छूता। मेरी समूची देह, चट्टान की तरह कैसी सख्त हो आई है। मन, शरीर से विलग होता जा रहा है, कहाँ गुम होता हा रहा है, वह मन ही जाने। मैं भी गुम होते हुए मन की राह नहीं रोकती। सभी के प्रति मुझे अभिमान हो आया है। एक देश ने मुझे निर्वासन की सज़ा दे डाली। उस देश के तमाम कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, नारीवादियों ने कितने आराम से मेरी इस सज़ा को कबूल कर लिया। जो लोकतंत्र के अधिकार के पक्ष में संघर्ष कर रहे हैं, वे लोग भी, कभी एक बार मेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाते। कोई भी नहीं कहता-"देश की बेटी, अब अपने देश लौट आए।" किसी ने भी सरकार से एक बार भी मामूली-सी भी माँग नहीं की। वैसे माँग क्या वे लोग नहीं कर रहे हैं? तरह-तरह की माँगे, लगातार पेश कर रहे हैं। इंसान क्या हर अन्याय, हर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रकट नहीं कर रहा है? सिर्फ एक अत्याचार का कोई प्रतिवाद नहीं होता। पता नहीं, कैसे तो इंसान इस ढंग से किसी इंसान को भूल जाता है, जिसके बारे में लोग अब तक यही दम भरते रहे हैं कि वह उनके बेहद करीब की प्राणी थी। अपने देश मैं कब वापस लौटूंगी, मुझे नहीं पता। उस देश के चप्पे-चप्पे से तसलीमा नाम मिटा दिया गया है। इस नाम की कोई प्राणी, उस देश में कभी नहीं थी, आज भी नहीं है। इस नाम को लेकर, किसी को कोई सिरदर्द नहीं है। खैर, नहीं है तो न सही! लेकिन मैं अपने शैशव, अपने कैशोर्य, अपनी तरुणाई, अपने यौवन तक लौटना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के पास लौटना चाहती हूँ। अपनी माँ की गोद में! मुझे नाम नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस, चाहे जैसे भी मैं अपनी जिंदगी तक लौटना चाहती हूँ।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ