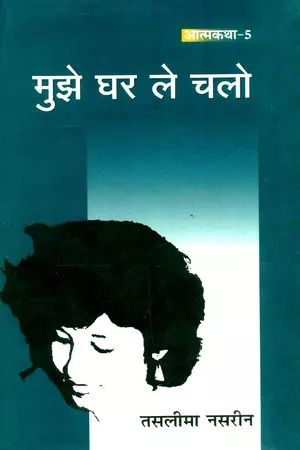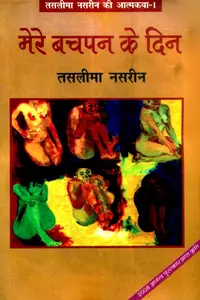|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
कोई संस्कृति अच्छी है, कोई बुरी-मूों की तरह अब, मैं ऐसा कोई जुमला जुबान पर नहीं लाती। मैंने बखूबी महसूस किया है कि पश्चिम और पूरव, दोनों ही संस्कृतियों में बहुत-सी अच्छी-अच्छी बातें हैं। दोनों ही संस्कृतियों की बुरी बातें अगर निकाल दी जाएँ और अच्छी-अच्छी बातें बटोरकर एक जगह इकट्ठी कर ली जाएँ तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह अतुलनीय हो उठेगा। जब मैं उस देश में थी, समाज के सड़े-गले नियमों के खिलाफ़ लड़ती रही। समष्टि से निकलकर व्यक्ति में परिणत होने जा रही थी, लेकिन जिस वजह से मेरी जंग जारी थी, उस स्वातंत्र्य का पूर्ण रूप यहाँ विद्यमान है, खासकर उत्तरी यूरोपीय देशों में! और सच पूछे तो उस रूप ने मुझे दुश्चिन्ता में डाल दिया है। स्वतंत्रवाद या इंडिवीजुअलिज़्म का यही चेहरा मैंने मन-ही-मन चाहा था? सच कहूँ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था, ऐसी तमन्ना भी नहीं की थी। स्वतंत्रता आखिरकार इंसान को इतने भयावह एकाकीपन की तरफ खींच ले जाती है कि उस चहारदीवारी में अकेले अपने अलावा और कोई नहीं होता। मैं खूब समझती हूँ कि मेरे लिए उस किस्म के अकेलेपन में जीना असंभव है। किसी और के लिए भी मैं ऐसे दुःसह जीवन की कामना नहीं कर सकती। मैं पूरब की तरफ नजरें गड़ाये अलग से कुछ नहीं देखती, बल्कि पश्चिमी नज़रों से भी देखू, तो भी मारे दहशत के सिकुड़ जाती हूँ।
पश्चिम का स्वतंत्रवाद इंसान को कितने भीषण रूप से अकंला करता जा रहा है, यहाँ के जीवन में धंसकर देखे विना समझ में नहीं आ सकता। यह असंभव है। यहाँ हर किसी की जिंदगी, उसकी अपनी है। कोई और उसमें नाक या टाँग या कुछ भी नहीं अड़ा सकता। अगर कोई दुःख झेलता है तो वह दुःख उसकं अकेले का है। कोई किसी के दुःख में हिस्सा नहीं बँटाएगा। खुशी-स्फूर्ति का भी वही आलम ! तुम्हारी खुशी, तुम्हारी तकलीफ, सब तुम्हारा अकेले का है। अगर कुछ बाँटना ही है, तो खुशी वाँटी। अपनी-अपनी जिंदगी के दुःख-तकलीफ ही सहने-झेलने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। इंसान का इंसान से रिश्ता घटते-घटते ऐसी स्थिति में आ पहँचा है कि अंत समय में कत्ता या फाँसी का फंदा ही आखिरी भरोसा बच रहता है। मानसिक रोग विशेषज्ञ के दरवाजे पर सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं लोगों की लगी होती है। पूरब के लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मन उदास है? तो क्या हआ? दोस्त-यार हैं, नाते-रिश्तेदार हैं, फिर भी मन उदास क्यों है, यह बताओ? मन में जितने ख़याल हैं, जितनी सोचें हैं, सब निःसंकोच जाहिर करो। चलो, कम-से-कम वातचीत तो की जा सकती है। वातचीत करके तकलीफ का वोझ तो कम किया जा सकता है। कम-से-कम कोई एक कंधा तो होता है, अपना सिर टेकने के लिए। एक हाथ तो होता है, हथेली थामने के लिए, एक दिल तो होता अपना दिल हल्का करने के लिए। पश्चिमी परिवेश में बेहद तीखे अकेलेपन के अँधेरे में जब मैं डूबती जा रही थी, पूरब की संस्कृति की अनिवार्यता, मैं अपनी रग-रग में महसूस कर रही थी। इस देश में अगर किसी से कहूँ कि मैं अपने को अकेली महसूस कर रही हूँ, वे लोग इसका सटीक अनुवाद हरगिज नहीं कर पाएँगे। महीने में बीस दिन मैं विभिन्न देशों का भ्रमण करती हूँ। चरम व्यस्तता की जिंदगी! ऊपर से तारका होने की ख्याति! फिर यह अकेलापन कहाँ से आता है? लेकिन आता है! उस खड़खड़िया की राह आता है! सर्दी की नुकीली सूई की तरह आता है और कहीं और नहीं, सीधे दिमाग मैं चुभ जाता है, मन को विल्कुल जड़-पत्थर और तन-बदन को आदतों का गुलाम बना डालता है। उस पल मेरे पास मैं के नाम पर कछ भी नहीं होता।
मुझे हरदम यही लगता रहता है, जैसे मैं किसी जेलखाने में कैद हूँ। यहाँ न दो कदम आगे बढ़ा जा सकता है, न पीछे हटा जा सकता है। जिस आज़ादी के लिए, मैं जिंदगी-भर लड़ती रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरी आँखों के सामने ही वह आजादी लुटी जा रही है। मैं जुबान खोलकर कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पाती। इस विदेश-भुंई में क्या से क्या हो जाए, कौन जाने? अगर कुछ हो गया तो कौन बचाने आएगा? निःसंगता मुझे मौसी-बुआ की तरह लोरियाँ गा-गाकर, दिन-भर, रात-भर सुलाये रखती है। जागते ही मैं देखती हूँ, मैं नितांत अकेली हूँ। कैसा है यह अकेलापन, मैं किसी को समझा भी नहीं सकती। बहुतेरे लोगों को अपना दोस्त कहकर मैं तसल्ली महसूस करती हूँ। हालाँकि सच्चे मायने में मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन अर्से पुरानी जान-पहचान को भी हमें 'दोस्त' कहने की आदत होती है या मेरा भी कोई दोस्त है, मैं नितांत अकेली नहीं हूँ, यह सोच-सोचकर, झूठ-मूठ ही सही, हम राहत पाना चाहते हैं। किसी भी वक्त, मैं अपने देश लौट जाऊँगी। वस, दिन गिन रही हूँ, लेकिन मेरे देश लौटने की ख़बर, आखिर मुझे कौन देगा? मैं नहीं जानती। कुछ नहीं जानती। मेरे भाई डॉक्टर कमाल हुसैन से बातचीत जारी रखे हुए हैं। मुकदमे की क्या खवर है, कट्टरवादी क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कहती है? ये तमाम सवाल मैं फोन पर बार-बार करती रहती हूँ। फोन के दूसरे छोर से जो जवाव मिलता है, वह सुनकर मेरा मन नहीं भरता। देश, विल्कुल देश की तरह ही है, लेकिन यह दूरद्वीपवासिनी अपने देश को आवाजें देती हुई, आकुल-व्याकुल होकर रोती है-
बाल्टिक सागर के पार, काठ का लाल-सुर्ख घर है,
घर के सामने खाली मैदान, मैदान में दूर-दूर तक चेरी,
स्ट्रॉबेरी और सेब के पेड!
ये सब पक-पककर पड़े रहते हैं घास पर,
कभी-कभी आ पहुँचते हैं हिरण, घास खाने
और पेड़ों से लगकर अपना बदन खुजलाने!
घूमते-फिरते आती हैं मैगयाइ पाखी, थोड़ी-सी निर्जन हवा भी!
उस घर में थोड़ा-थोड़ा करके, गढ़ उठी है मेरी दुनिया,
दाल-चावल, नून-तेल की गृहस्थी!
शाम की चाय में दो चम्मच निःसंगता घोलकर पीने का जगत!
रात-रात भर अरण्य के अंधेरे को बिठाकर अपने सिरहाने,
अलाव तापते-तापते, गपशप करने का जहान!
या अलस्सुबह आँखों में उतरते ही नींद,
अंगड़ाई लेते हुए तरोताज़ा होता संसार!
अब भी, लौटा लो मुझे,
अब भी, मुझे धूल-रेत, नदी, हवा, सरसों खेत और ब्रह्मपुत्र दे दो मुझे!
अब भी, दे दो मुझे नलथान, लिपा-पुता आँगन,
हाथ-पंखे की हवा, टिन की छादन की रिमझिम,
झींगुर की शोरभरी वर्षा,
धुआँ उठते भात में मागुर मछली, धनिया पत्ती का शोरबा!
अभी भी, स्कैंडिनेविया की देह से हटा लो, छूने को उन्मुख मेरी जड़ें!
मुझे बचा लो!
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ