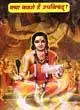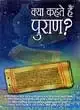|
जीवनी/आत्मकथा >> कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधीमहेश शर्मा
|
73 पाठक हैं |
||||||
11 अप्रैल, 1869 को पोरबंदर में जन्मीं कस्तूरबाई या कस्तूरबा उम्र में गांधीजी से छह महीने बड़ी थीं। तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उनका व्यक्तित्व गांधीजी को चुनौती देता प्रतीत होता है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
दो शब्द
11 अप्रैल, 1869 को पोरबंदर में जन्मीं कस्तूरबाई या कस्तूरबा उम्र में
गांधीजी से छह महीने बड़ी थीं। तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उनका
व्यक्तित्व गांधीजी को चुनौती देता प्रतीत होता है। स्वयं गांधीजी इस बात
को स्वीकार करते हुए कहते हैं: ‘‘जो लोग मेरे और बा
के निकट संपर्क में आए हैं, उनमें अधिक संख्या तो ऐसे लोगों की है, जो
मेरी अपेक्षा बा पर अनेक गुनी अधिक श्रद्धा रखते
हैं।’’
वैसे भी वटवृक्ष को आकार देनेवाला बीज प्राय: मिट्टी तले ही छिप जाता है।
तेरह वर्ष की उम्र में बा बापू के साथ विवाह-सूत्र में बँध गई थीं। शुरुआती दिनों में नवदंपती में बहुत खटपट रहती थी। गांधीजी को बा की निरक्षरता बहुत चुभती थी। धीरे-धीरे उन्होंने बा को कामचलाऊ पढ़ने-लिखने योग्य बनाया और बा भी बापू के रंग में रँगती चली गईं। बापू सिद्धांत बनाते और बा उनपर अमल करतीं।
दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान रंगभेद की नीति के विरुद्ध बा कई बार जेल गईं। भारत में भी, आजादी की लड़ाई में उन्होंने बापू के कदम-से-कदम मिलाया। 22 फरवरी, 1944 को जेल में ही उनका निधन हुआ।
यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि राष्ट्रमाता बा की उज्जवल जीवन-गाथा आनेवाली पीढ़ियों का युगों-युगों तक पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। इसी आस्था और विश्वास के साथ।
वैसे भी वटवृक्ष को आकार देनेवाला बीज प्राय: मिट्टी तले ही छिप जाता है।
तेरह वर्ष की उम्र में बा बापू के साथ विवाह-सूत्र में बँध गई थीं। शुरुआती दिनों में नवदंपती में बहुत खटपट रहती थी। गांधीजी को बा की निरक्षरता बहुत चुभती थी। धीरे-धीरे उन्होंने बा को कामचलाऊ पढ़ने-लिखने योग्य बनाया और बा भी बापू के रंग में रँगती चली गईं। बापू सिद्धांत बनाते और बा उनपर अमल करतीं।
दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान रंगभेद की नीति के विरुद्ध बा कई बार जेल गईं। भारत में भी, आजादी की लड़ाई में उन्होंने बापू के कदम-से-कदम मिलाया। 22 फरवरी, 1944 को जेल में ही उनका निधन हुआ।
यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि राष्ट्रमाता बा की उज्जवल जीवन-गाथा आनेवाली पीढ़ियों का युगों-युगों तक पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। इसी आस्था और विश्वास के साथ।
-लेखक
जीवनगाथा
‘‘बा का जबर्दस्त गुण था-सहज ही मुझमें समा जाना। मैं
नहीं जानता था कि यह गुण उनमें छिपा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे मेरा
सार्वजनिक जीवन उज्जवल बनता गया, वैसे-वैसे बा खिलती गईं और पुख्ता
विचारों के साथ मुझमें यानी मेरे काम में समाती गईं।’’
-महात्मा
गांधी
कहा गया कि ‘हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता
है’, यह बात कस्तूरबा पर अक्षरश: सत्य सिद्ध होती है। गांधीजी
को महात्मा बनाने में बा का बहुत बड़ा हाथ था। गांधी जैसे कठोर, निरंकुश,
अनुशासनप्रिय, हठी और असामान्य व्यक्ति के साथ बा ने कदम-कदम पर समझौता
किया और उनकी प्रत्येक अच्छी-बुरी बात को शिरोधार्य किया। स्वयं बापू ने
कहा था-‘‘बा ही है, जो इतना सहन करती है। मेरे जैसे
आदमी के साथ जीवन बिताना बड़ा कठिन काम है। इनके अलावा कोई और होता तो
मेरा निर्वाह होना कठिन था।
जन्म
दया, करुणा और ममता की मूर्ति कस्तूरबा का जन्म गुजरात के पोरबंदर नगर में
11 अप्रैल, 1869 को हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुलदास मकनजी था जो एक
साधारण व्यापारी थे। माता ब्रजकुँवर एक आदर्श गृहस्थ महिला थीं।
बा के परिवार में माता-पिता के अलावा तीन भाई और एक बहन और भी थे; इनमें दो सगे भाई और एक बहन जल्दी ही काल-कवलित हो गए। बाकी बचे कस्तूरबा और छोटे भाई माधवदास।
बा के परिवार में माता-पिता के अलावा तीन भाई और एक बहन और भी थे; इनमें दो सगे भाई और एक बहन जल्दी ही काल-कवलित हो गए। बाकी बचे कस्तूरबा और छोटे भाई माधवदास।
शिक्षा
बा के माता-पिता वैष्णव धर्मावलंबी थे। अत: अच्छे संस्कार उन्हें विरासत
में मिले थे। एक कमी थी, निरक्षर रहने की, जो उन्हें जीवन भर सालती रही।
गांधीजी भी इसके लिए उन्हें जीवन भर उपालंभ देते रहे।
तत्कालीन समाज में गुजरात के कठियावाड़ इलाके में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था, यही कारण था कि बा को भी नहीं पढ़ाया गया और वे निरक्षर रह गईं। बाद में गांधीजी ने स्वयं उन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
तत्कालीन समाज में गुजरात के कठियावाड़ इलाके में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था, यही कारण था कि बा को भी नहीं पढ़ाया गया और वे निरक्षर रह गईं। बाद में गांधीजी ने स्वयं उन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
विवाह
बा के पिता गोकुलदास मकनजी गांधीजी के पिता करमचंद यानी
‘काबा’ गांधी के मित्र थे। इस मित्रता को रिश्तेदारी
में बदलने के लिए दोनों परिवारों ने बा और मोहनदास का विवाह करने का
निश्चय किया।
उन दिनों सौराष्ट्र के साथ-साथ भारत के अनेक भागों में कम उम्र में विवाह कर देने की परंपरा थी। अत: मात्र सात वर्ष की आयु में बा और मोहनदास की सगाई कर देने पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। बा अपने भावी पति मोहनदास से लगभग छह महीने बड़ी थीं।
बाद में सन् 1883 में, तेरह वर्ष का आयु में दोनों का विवाह कर दिया गया। सगाई और विवाह तब दोनों को पर्व-त्योहार की तरह ही लगे थे। गांधीजी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा करते हुए लिखा है-‘‘मुझे याद नहीं पड़ता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। इसी तरह विवाह के समय भी कुछ नहीं पूछा गया। सिर्फ तैयारियों से पता चला कि विवाह होने वाला है। उस समय तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, बाजे बजेंगे, बारात निकलेगी, अच्छा-अच्छा खाने को मिलेगा, एक नई लड़की के साथ हँसी-खेल करेंगे, वगैरह इच्छाओं के सिवा और कोई विशेष भाव मेरे मन में रहा हो, ऐसा याद नहीं आता। उस समय तो सबकुछ ठीक और मनभावन लग रहा था। मैं खुद शादी करने को उत्सुक था।’’
विवाह के बाद गांधी भरसक प्रयत्न करते थे कि बा अधिकतर समय उन्हीं के साथ गुजारें, लेकिन उनके भरे-पूरे परिवार और तत्कालीन रूढ़िवादी परंपराओं में यह संभव नहीं हो पाता था। उन्हें रात्रि के समय ही साथ रहने का अवसर मिल पाता था। इस व्यथा का वर्णन करते हुए गांधीजी ने लिखा है-‘‘मुझे अपनी पत्नी को आदर्श स्त्री बनाना था। वह साफ बने, साफ रहे, मैं जो सीखूँ, सीखे; मैं जो पढ़ूँ, पढ़े और हम दोनों एक-दूसरे में ओत-प्रोत रहें; यह मेरी भावना थी, वे निरक्षर थीं, स्वभाव की सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ कम बोलनेवालीं। उन्हें अपने अज्ञान पर असंतोष नहीं था। मैंने अपने बचपन में उनको कभी यह इच्छा करते हुए नहीं पाया कि जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, उस तरह वह खुद भी पढ़ें तो अच्छा हो। उन्हें पढ़ाने कि मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसमें दो कठिनाइयाँ थी-एक तो बा की पढ़ने की भूख खुली नहीं थी; दूसरे बा अनुकूल हो जातीं तो भी उस जमाने के भरे-पूरे परिवार में इस इच्छा को पूरा करना आसान नहीं था।’’
इस प्रकार बा को पढ़ाने की गांधीजी की इच्छा कभी मूर्त रूप नहीं ले सकी। इस मानसिक द्वंद्व का वर्णन करते हुए गांधीजी ने लिखा है-‘‘एक तो मुझे जबर्दस्ती पढ़ाना था और वह भी रात्रि के एकांत में हो सकता था। घर के बड़े-बूढ़ों के सामने पत्नी की तरफ देख तक नहीं सकते थे। बातें तो हो ही कैसे सकती थीं। उस समय काठियावाड़ में घूँघट निकालने का निरर्थक और अंधविश्वासी रिवाज था। आज भी बहुत-कुछ मौजूद है। इसलिए पढ़ाने के अवसर भी मेरे लिए प्रतिकूल थे। अतएव मुझे कबूल करना चाहिए कि जवानी में मैंने बा को पढ़ाने की जितनी भी कोशिशें कीं, वे सब करीब-करीब बेकार गईं। जब मैं ‘विषय’ की नींद से जागा, तब सार्वजनिक जीवन में पड़ चुका था, इसलिए मेरी स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि मैं ज्यादा समय दे सकूँ। शिक्षक के जरिए पढ़ाने की मेरी कोशिशें भी बेकार हुईं। नतीजा यह हुआ कि आज कस्तूरबा मुश्किल से पत्र लिख सकती हैं और मामूली गुजराती समझ लेती हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता, तो आज वे विदुषी स्त्री होतीं। उनके पढ़ने के आलस्य को मैं जीत सकता।
उन दिनों सौराष्ट्र के साथ-साथ भारत के अनेक भागों में कम उम्र में विवाह कर देने की परंपरा थी। अत: मात्र सात वर्ष की आयु में बा और मोहनदास की सगाई कर देने पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। बा अपने भावी पति मोहनदास से लगभग छह महीने बड़ी थीं।
बाद में सन् 1883 में, तेरह वर्ष का आयु में दोनों का विवाह कर दिया गया। सगाई और विवाह तब दोनों को पर्व-त्योहार की तरह ही लगे थे। गांधीजी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा करते हुए लिखा है-‘‘मुझे याद नहीं पड़ता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। इसी तरह विवाह के समय भी कुछ नहीं पूछा गया। सिर्फ तैयारियों से पता चला कि विवाह होने वाला है। उस समय तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, बाजे बजेंगे, बारात निकलेगी, अच्छा-अच्छा खाने को मिलेगा, एक नई लड़की के साथ हँसी-खेल करेंगे, वगैरह इच्छाओं के सिवा और कोई विशेष भाव मेरे मन में रहा हो, ऐसा याद नहीं आता। उस समय तो सबकुछ ठीक और मनभावन लग रहा था। मैं खुद शादी करने को उत्सुक था।’’
विवाह के बाद गांधी भरसक प्रयत्न करते थे कि बा अधिकतर समय उन्हीं के साथ गुजारें, लेकिन उनके भरे-पूरे परिवार और तत्कालीन रूढ़िवादी परंपराओं में यह संभव नहीं हो पाता था। उन्हें रात्रि के समय ही साथ रहने का अवसर मिल पाता था। इस व्यथा का वर्णन करते हुए गांधीजी ने लिखा है-‘‘मुझे अपनी पत्नी को आदर्श स्त्री बनाना था। वह साफ बने, साफ रहे, मैं जो सीखूँ, सीखे; मैं जो पढ़ूँ, पढ़े और हम दोनों एक-दूसरे में ओत-प्रोत रहें; यह मेरी भावना थी, वे निरक्षर थीं, स्वभाव की सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ कम बोलनेवालीं। उन्हें अपने अज्ञान पर असंतोष नहीं था। मैंने अपने बचपन में उनको कभी यह इच्छा करते हुए नहीं पाया कि जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, उस तरह वह खुद भी पढ़ें तो अच्छा हो। उन्हें पढ़ाने कि मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसमें दो कठिनाइयाँ थी-एक तो बा की पढ़ने की भूख खुली नहीं थी; दूसरे बा अनुकूल हो जातीं तो भी उस जमाने के भरे-पूरे परिवार में इस इच्छा को पूरा करना आसान नहीं था।’’
इस प्रकार बा को पढ़ाने की गांधीजी की इच्छा कभी मूर्त रूप नहीं ले सकी। इस मानसिक द्वंद्व का वर्णन करते हुए गांधीजी ने लिखा है-‘‘एक तो मुझे जबर्दस्ती पढ़ाना था और वह भी रात्रि के एकांत में हो सकता था। घर के बड़े-बूढ़ों के सामने पत्नी की तरफ देख तक नहीं सकते थे। बातें तो हो ही कैसे सकती थीं। उस समय काठियावाड़ में घूँघट निकालने का निरर्थक और अंधविश्वासी रिवाज था। आज भी बहुत-कुछ मौजूद है। इसलिए पढ़ाने के अवसर भी मेरे लिए प्रतिकूल थे। अतएव मुझे कबूल करना चाहिए कि जवानी में मैंने बा को पढ़ाने की जितनी भी कोशिशें कीं, वे सब करीब-करीब बेकार गईं। जब मैं ‘विषय’ की नींद से जागा, तब सार्वजनिक जीवन में पड़ चुका था, इसलिए मेरी स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि मैं ज्यादा समय दे सकूँ। शिक्षक के जरिए पढ़ाने की मेरी कोशिशें भी बेकार हुईं। नतीजा यह हुआ कि आज कस्तूरबा मुश्किल से पत्र लिख सकती हैं और मामूली गुजराती समझ लेती हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता, तो आज वे विदुषी स्त्री होतीं। उनके पढ़ने के आलस्य को मैं जीत सकता।
२
बा का गृहस्थ जीवन
‘‘जो लोग मेरे और बा के निकट संपर्क में आए हैं उनमें
अधिक संख्या तो ऐसे लोगों की है, जो मेरी अपेक्षा बा पर अनेक गुनी अधिक
श्रद्धा रखते हैं।
-महात्मा गांधी
बा का गृहस्थ जीवन कांटों के ताज जैसा था। गांधीजी उनकी निरक्षरता से
कुढ़ते रहते थे और उन्हें ताने देते रहते थे। उनका सजना, सँवरना और घर से
बाहर निकलना भी उन्हें नापसंद था। वे शक्की और ईर्ष्यालु पति थे। इस बात
को उन्होंने भी स्वीकार किया था।
बा की सास पुतलीबाई का उनपर विशेष स्नेह था। बा की कर्मठता के कारण जल्दी ही परिवार के पूरे कामकाज का बोझ उनपर आ गया। अब पति के लिए और भी कम समय मिल पाता था। ससुरजी बीमार रहने लगे थे, अत: सासूजी का अधिकतर समय उनकी सेवा में बीत जाता था।
लंबी बीमारी के बाद ससुरजी के चल बसने के कारण बा पर काम का और अधिक बोझ आ गया। उन्हें अपनी माता के शब्द याद आ जाते थे कि ‘ससुराल में काम करते-करते कमर टेढ़ी हो जाएगी।’
इसी बीच शारीरिक कमजोरी के कारण उनका पहला शिशु जन्म लेते ही स्वर्ग सिधार गया। बा की जान भी मुश्किल से बच पाई। उनकी इस व्यथा को बाँटने वाला कोई नहीं था। वे रात्रि में चुपचाप आंसू बहातीं और दिन में घर-गृहस्थी के काम-काज में व्यस्त रहकर समय गुजारतीं।
बा की सास पुतलीबाई का उनपर विशेष स्नेह था। बा की कर्मठता के कारण जल्दी ही परिवार के पूरे कामकाज का बोझ उनपर आ गया। अब पति के लिए और भी कम समय मिल पाता था। ससुरजी बीमार रहने लगे थे, अत: सासूजी का अधिकतर समय उनकी सेवा में बीत जाता था।
लंबी बीमारी के बाद ससुरजी के चल बसने के कारण बा पर काम का और अधिक बोझ आ गया। उन्हें अपनी माता के शब्द याद आ जाते थे कि ‘ससुराल में काम करते-करते कमर टेढ़ी हो जाएगी।’
इसी बीच शारीरिक कमजोरी के कारण उनका पहला शिशु जन्म लेते ही स्वर्ग सिधार गया। बा की जान भी मुश्किल से बच पाई। उनकी इस व्यथा को बाँटने वाला कोई नहीं था। वे रात्रि में चुपचाप आंसू बहातीं और दिन में घर-गृहस्थी के काम-काज में व्यस्त रहकर समय गुजारतीं।
एकपत्नी-व्रत
विवाह के आरंभिक काल में बा और बापू में नादानी भरे झगड़े होते रहते थे।
दोनों में ‘कुट्टी’ हो जाती थी। कई-कई दिनों तक दोनों
बात नहीं करते थे।
एक दिन बापू ने एक निबंध में पढ़ा कि एकपत्नी-व्रत का पालन करना पति का धर्म है। यह बात उनके मन में गहरे उतर गई। लेकिन इसके साथ ही यह विचार भी मन में पैदा हुआ कि यदि पति एकपत्नी-व्रत का पालन करता है तो उसकी पत्नी को भी एकपति-व्रत का पालन करना चाहिए। इस विचार ने गांधीजी को एक ईर्ष्यालु पति बना दिया। ‘पालना चाहिए’ पर से वे ‘पलवाना चाहिए’ के विचार पर पहुँच गए।
गांधीजी ने इस विषय में लिखा है-‘‘जब मैं ‘पलवाना है’ के निष्कर्ष पर पहुँचा तो पत्नी के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए-इस विचार पर पहुँचा। पत्नी की पतिव्रता पर शक करने का मेरे पास कोई कारण न था, लेकिन ईर्ष्या कब कारण देखने बैठती है ? मुझे यह जानना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है। इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। यह चीज हमारे बीच दु:खद झगड़े का कारण बन गई। अनुमति के बिना कहीं न जा सकना तो एक तरह की कैद हुई। लेकिन कस्तूरबा इस तरह की कैद सहन करनेवाली थीं ही नहीं। जहाँ जाना चाहतीं, वहाँ मुझसे बिना पूछे जरूर जातीं। जितना ही मैं दबाता, उतना ही अधिक वे आजादी पा लेतीं और मैं ज्यादा चिढ़ता।’’
विवाह के आरंभिक काल में पुरुषों को प्राय: अपनी महत्ता और स्वामित्व सिद्ध करने का जोश चढ़ा रहता है, लेकिन स्त्रियाँ स्वभाव से ही सहनशील और धैर्य की प्रतिमूर्ति होती हैं। उनके इन्हीं गुणों के कारण गृहस्थी का जहाज टकराने से बचा रहता है। बापू स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखते हैं-‘‘कस्तूरबा ने जो आजादी ली थी, उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। एक बालिका, जिसके मन में पाप नहीं, वह मंदिर जाने के लिए या किसी से मिनले जाने के बारे में ऐसा दबाव क्यों सहन करे ? अगर मैं उस पर दबाव रखता हूँ तो वह मुझ पर क्यों न रखे ? किंतु यह तो अब समझ में आता है।
एक दिन बापू ने एक निबंध में पढ़ा कि एकपत्नी-व्रत का पालन करना पति का धर्म है। यह बात उनके मन में गहरे उतर गई। लेकिन इसके साथ ही यह विचार भी मन में पैदा हुआ कि यदि पति एकपत्नी-व्रत का पालन करता है तो उसकी पत्नी को भी एकपति-व्रत का पालन करना चाहिए। इस विचार ने गांधीजी को एक ईर्ष्यालु पति बना दिया। ‘पालना चाहिए’ पर से वे ‘पलवाना चाहिए’ के विचार पर पहुँच गए।
गांधीजी ने इस विषय में लिखा है-‘‘जब मैं ‘पलवाना है’ के निष्कर्ष पर पहुँचा तो पत्नी के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए-इस विचार पर पहुँचा। पत्नी की पतिव्रता पर शक करने का मेरे पास कोई कारण न था, लेकिन ईर्ष्या कब कारण देखने बैठती है ? मुझे यह जानना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है। इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। यह चीज हमारे बीच दु:खद झगड़े का कारण बन गई। अनुमति के बिना कहीं न जा सकना तो एक तरह की कैद हुई। लेकिन कस्तूरबा इस तरह की कैद सहन करनेवाली थीं ही नहीं। जहाँ जाना चाहतीं, वहाँ मुझसे बिना पूछे जरूर जातीं। जितना ही मैं दबाता, उतना ही अधिक वे आजादी पा लेतीं और मैं ज्यादा चिढ़ता।’’
विवाह के आरंभिक काल में पुरुषों को प्राय: अपनी महत्ता और स्वामित्व सिद्ध करने का जोश चढ़ा रहता है, लेकिन स्त्रियाँ स्वभाव से ही सहनशील और धैर्य की प्रतिमूर्ति होती हैं। उनके इन्हीं गुणों के कारण गृहस्थी का जहाज टकराने से बचा रहता है। बापू स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखते हैं-‘‘कस्तूरबा ने जो आजादी ली थी, उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। एक बालिका, जिसके मन में पाप नहीं, वह मंदिर जाने के लिए या किसी से मिनले जाने के बारे में ऐसा दबाव क्यों सहन करे ? अगर मैं उस पर दबाव रखता हूँ तो वह मुझ पर क्यों न रखे ? किंतु यह तो अब समझ में आता है।
अच्छे बुरे की पहचान
निरक्षर होने के बावजूद बा में अच्छे-बुरे को पहचानने की विवेक-शक्ति थी।
बुराई का वे डटकर सामना करती थीं और गांधीजी को चेतावनी देने से भी नहीं
चूकती थीं। एक बार जब गलत मित्रों की संगत में गांधीजी मांस आदि का सेवन
करने लगे तो बा चुप न रह सकीं, बल्कि उन्होंने बापू के अंत:करण को जगाने
के लिए जमाने की भलाई-बुराई पर विस्तार से चर्चा की और चेतावनी देते हुए
कहा कि यह सब करना उनके और उनके खानदान के लिए उचित नहीं है।
बाद में बापू ने उनकी समझदारी को स्वीकार करते हुए लिखा-‘‘पत्नी की चेतावनी को मैं गर्विष्ठ (घमंडी) पति भला क्यों मानने लगा।
३
बाद में बापू ने उनकी समझदारी को स्वीकार करते हुए लिखा-‘‘पत्नी की चेतावनी को मैं गर्विष्ठ (घमंडी) पति भला क्यों मानने लगा।
३
सेवा की प्रतिमूर्ति
‘‘बा में एक गुण बहुत मात्रा में है, जो दूसरी
बहुत-सी हिंदू स्त्रियों में न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। इच्छा से
हो या अनिच्छा से, ज्ञान से हो या अज्ञान से, मेरे पीछे चलने में उन्होंने
अपने जीवन की सार्थकता मानी है। और शुद्ध जीवन बिताने के लिए मेरे प्रयत्न
में मुझे कभी रोका नहीं। इसके कारण हमारी बुद्धि, शक्ति में बहुत अंतर
होते हुए भी मुझे यह लगा कि हमारा जीवन संतोषी, सुखी और ऊर्ध्वगामी
है।
-महात्मा
गांधी
>
बा के ससुर कमरचंद गांधी के निधन के बाद उनकी सास पुतलीबाई का मन दुनिया
से विरक्त हो गया था। पति-वियोग ने उन्हें धीर-गंभीर बना दिया था। पत्नी
पुतलीबाई अपने पति के निधन से चिंताग्रस्त थीं तो कस्तूरबा अपने पति के
कार्य-कलाप से।
गांधीजी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनके भविष्य को लेकर बड़े-बूढ़े विचार करने लगे कि उन्हें क्या बनाया जाए। अंत में, उनके मामा और बड़े भाई आदि ने निर्णय लिया कि उन्हें बैरिस्टर बनाया जाए।
बैरिस्टर की पढाई के लिए उन दिनों इंग्लैंड जाना पड़ता था। यह निर्णय सुनकर मोहनदास बहुत खुश हुए। उनकी यह अभिलाषा भी थी कि बड़े आदमी बनकर नाम कमाएँ।
दुखी और चिंतित थीं तो केवल कस्तूरबाई। उन्हें चिंता थी कि देश में ही इतने अंकुश के बावजूद वे (गांधी) गलत सोहबत में पड़ गए, मांस आदि खाने लगे और कर्ज चुकाने के लिए सोने के कड़े का टुकड़ा काटकर बेचने की बात उन्होंने स्वयं सबके सामने स्वीकार की। उधर, विदेश में न कोई देखनेवाला होगा, न सुननेवाला, कोई अंकुश भी नहीं होगा। वहाँ पता नहीं, वे संयमित रह पाएँगे कि नहीं ? इसी चिंता ने कस्तूरबाई (कस्तूरबा) को आधा कर दिया था। परंतु उनके मन की बात सुननेवाला कोई नहीं था।
सास पुतलीबाई हालाँकि संसार से विरक्त महिला थीं, अधिकतर धर्म-कर्म में डूबी रहती थीं, तथापि बहू के चेहरे पर खिंची चिंता की लकीरें उनसे छिप न सकी।
एक दिन प्रात: पुतलीबाई पूजागृह में थीं। तभी मोहनदास भगवान् को प्रणाम करने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन्हें रोक लिया।
‘‘मोहन बेटा ! जरा इधर तो आ।’
‘‘हाँ, माँ !’’ यह कहकर मोहनदास माँ के सामने बैठ गए।
‘‘सुना है, वकालत पढ़ने तू इंग्लैड जा रहा है ?’’
‘‘आप बड़े यह निर्णय लें और अनुमति दें तो ऐसा करने में मुझे प्रसन्नता होगी।’’
‘‘वहाँ जाकर क्या भला आदमी बना जा सकता है ?’’
‘‘जी माँ, वहाँ की परीक्षा में पास होकर खूब मान-प्रतिष्ठा अर्जित की जा सकती है। अच्छा काम मिल सकता है। हमारे परिवार के दिन फिर सकते हैं।’’
‘‘अगर, तू ऐसा समझता है तो जा।’’ पुतलीबाई विरक्ति के स्वर में कह रही थीं, ‘‘लेकिन विदेश में भी अपने खानदानी वैष्णवी संस्कार मत छोड़ना। परायी स्त्री का साथ मत करना, मांस-मदिरा को मत छूना। तुझे मेरी कसम है।’’
पास के कमरे में बैठी कस्तूरबाई सब सुन रही थीं। उन्हें खुशी थी कि उनकी सास ने उनके मन की बातों को उनते पति के सामने रख दिया था। उन्होंने अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया और पति के सुखद भविष्य की कामना की।
4 सितंबर, 1888 को मोहनदास इंग्लैड रवाना हो गए। उस समय बा 19 वर्ष की थीं। जाते समय उन्होंने सबसे विदाई ली, लेकिन बा से मिले अथवा नहीं, इसका विवरण कहीं नहीं मिलता। इतना तो तय है कि बिना मिले जाना बा को अच्छा नहीं लगा होगा या अधिक-से-अधिक बा ने पूछा होगा, ‘वापस कब आओगे’ और बापू ने कुछ आश्वासन दिया होगा।
मोहनदास जब इंग्लैड में वकालत पढ़ रहे थे तभी उनकी माता पुतलीबाई का निधन हो गया। बा का जीवन भारी दायित्व और व्यस्तता में गुम हो गया। उनकी जेठानी घंटों पूजा-पाठ में व्यस्त रहती थीं। अत: उनके बच्चों को नहलाना-धुलाना, उन्हें तैयार करके स्कूल भेजना, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि कार्यों में दिन कब गुजर जाता था, बा को पता ही नहीं चलता था।
बा का अपना एक शिशु तो जन्म के दो-चार दिन बाद ही चल बसा था। उसके बाद गाँधीजी के इंग्लैड जाने से पूर्व हरिलाल का जन्म हुआ था। इस बालक के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी बा पर थी।
गांधीजी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनके भविष्य को लेकर बड़े-बूढ़े विचार करने लगे कि उन्हें क्या बनाया जाए। अंत में, उनके मामा और बड़े भाई आदि ने निर्णय लिया कि उन्हें बैरिस्टर बनाया जाए।
बैरिस्टर की पढाई के लिए उन दिनों इंग्लैंड जाना पड़ता था। यह निर्णय सुनकर मोहनदास बहुत खुश हुए। उनकी यह अभिलाषा भी थी कि बड़े आदमी बनकर नाम कमाएँ।
दुखी और चिंतित थीं तो केवल कस्तूरबाई। उन्हें चिंता थी कि देश में ही इतने अंकुश के बावजूद वे (गांधी) गलत सोहबत में पड़ गए, मांस आदि खाने लगे और कर्ज चुकाने के लिए सोने के कड़े का टुकड़ा काटकर बेचने की बात उन्होंने स्वयं सबके सामने स्वीकार की। उधर, विदेश में न कोई देखनेवाला होगा, न सुननेवाला, कोई अंकुश भी नहीं होगा। वहाँ पता नहीं, वे संयमित रह पाएँगे कि नहीं ? इसी चिंता ने कस्तूरबाई (कस्तूरबा) को आधा कर दिया था। परंतु उनके मन की बात सुननेवाला कोई नहीं था।
सास पुतलीबाई हालाँकि संसार से विरक्त महिला थीं, अधिकतर धर्म-कर्म में डूबी रहती थीं, तथापि बहू के चेहरे पर खिंची चिंता की लकीरें उनसे छिप न सकी।
एक दिन प्रात: पुतलीबाई पूजागृह में थीं। तभी मोहनदास भगवान् को प्रणाम करने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन्हें रोक लिया।
‘‘मोहन बेटा ! जरा इधर तो आ।’
‘‘हाँ, माँ !’’ यह कहकर मोहनदास माँ के सामने बैठ गए।
‘‘सुना है, वकालत पढ़ने तू इंग्लैड जा रहा है ?’’
‘‘आप बड़े यह निर्णय लें और अनुमति दें तो ऐसा करने में मुझे प्रसन्नता होगी।’’
‘‘वहाँ जाकर क्या भला आदमी बना जा सकता है ?’’
‘‘जी माँ, वहाँ की परीक्षा में पास होकर खूब मान-प्रतिष्ठा अर्जित की जा सकती है। अच्छा काम मिल सकता है। हमारे परिवार के दिन फिर सकते हैं।’’
‘‘अगर, तू ऐसा समझता है तो जा।’’ पुतलीबाई विरक्ति के स्वर में कह रही थीं, ‘‘लेकिन विदेश में भी अपने खानदानी वैष्णवी संस्कार मत छोड़ना। परायी स्त्री का साथ मत करना, मांस-मदिरा को मत छूना। तुझे मेरी कसम है।’’
पास के कमरे में बैठी कस्तूरबाई सब सुन रही थीं। उन्हें खुशी थी कि उनकी सास ने उनके मन की बातों को उनते पति के सामने रख दिया था। उन्होंने अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया और पति के सुखद भविष्य की कामना की।
4 सितंबर, 1888 को मोहनदास इंग्लैड रवाना हो गए। उस समय बा 19 वर्ष की थीं। जाते समय उन्होंने सबसे विदाई ली, लेकिन बा से मिले अथवा नहीं, इसका विवरण कहीं नहीं मिलता। इतना तो तय है कि बिना मिले जाना बा को अच्छा नहीं लगा होगा या अधिक-से-अधिक बा ने पूछा होगा, ‘वापस कब आओगे’ और बापू ने कुछ आश्वासन दिया होगा।
मोहनदास जब इंग्लैड में वकालत पढ़ रहे थे तभी उनकी माता पुतलीबाई का निधन हो गया। बा का जीवन भारी दायित्व और व्यस्तता में गुम हो गया। उनकी जेठानी घंटों पूजा-पाठ में व्यस्त रहती थीं। अत: उनके बच्चों को नहलाना-धुलाना, उन्हें तैयार करके स्कूल भेजना, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि कार्यों में दिन कब गुजर जाता था, बा को पता ही नहीं चलता था।
बा का अपना एक शिशु तो जन्म के दो-चार दिन बाद ही चल बसा था। उसके बाद गाँधीजी के इंग्लैड जाने से पूर्व हरिलाल का जन्म हुआ था। इस बालक के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी बा पर थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book