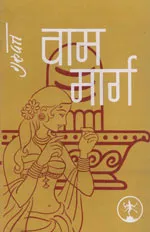|
ऐतिहासिक >> वाम मार्ग वाम मार्गगुरुदत्त
|
326 पाठक हैं |
||||||
एक रोचक उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कथानक का आधार-विषय
राजनीति में लैफ्टिस्ट (वामपक्षीय) भले ही ‘पार्लियामेन्टरी
सिस्टम’ की उपज हों, वास्तव में वामपक्षीय विचार-धारा के लोग तो
मानव-इतिहास के आदि काल से चले आ रहे हैं। जब से मनुष्य ने अपनी निज की,
समाज की तथा संसार की समस्याओं पर विचार करना आरम्भ किया है, तब से ही दो
प्रमुख विचार मनुष्य के मन को आन्दोलित करते रहे हैं। वर्तमान और भविष्य
ये उन दो विचारधाराओं की धुरी रहे है।
लैफ्टिस्ट (वामपक्षीय) केवल वर्तमान की ओर ध्यान रखने वाले रहे हैं। उनका दृष्टि-क्षेत्र सदा जन्म से मरण तक सीमित रहा है। राजनीति में सभी लैफ्टिस्ट सामयिक सफलता को ही मुख्य मानते हैं। प्रायः राजनीतिक लैफ्टिस्ट, जब सीमित काल में सफलता नहीं पा सकते, तो क्रान्ति की माँग करने लगते हैं। उन्हें सफलता में देरी असह्य हो जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए समय अल्प होने के कारण, वे उचित और अनुचित उपायों का विचार भी छोड़ बैठते हैं।
इसके विपरीत राईटिस्ट (दक्षिण-पंथीय विचार के लोग) वर्तमान जीवन को विराट् जीवन का एक बहुत छोटा भाग मानते हैं। इनका दृष्टि-क्षेत्र अति दूर तक फैला हुआ और गम्भीर होता है। उनको सफलता प्राप्त करने के लिये घबराहट, उतावली, निराशा नहीं होती। वे क्रान्ति को आवश्यक और लाभदायक नहीं मानते और न ही वे सफलता करने में अनुचित उपाय प्रयोग करना उचित समझते हैं। निज, समाज की अथवा संसार की उन्नति उपादेय मानते हुए भी, उसको झूठ, दगा अथवा पाप के मार्ग से प्राप्त करने में हानि मानते हैं।
यह है सिद्धान्तात्मक भेद वामपक्ष और दक्षिण पक्ष में। वाममार्ग मत, मज़हब के क्षेत्र में लैफ्टिज़्म (वामपक्ष) है। मज़हब मनुष्य के आचरण तथा मनुष्य और समाज के सम्बन्ध के विषय की बात बताता है। मनुष्य क्या है ? इसका आदि-अन्त कहाँ है ? संसार के साथ इसका क्या सम्बन्ध है ? मानव-समाज और व्यक्ति के अधिकारों में सीमा कहाँ है ? इन सब और इसी प्रकार की अनेक अन्य बातों में विवेचना करने कि समय, जो मनुष्य जीवन को जन्म से मरण तक ही मानते हैं, न इसके पहले कुछ था, न इसके पश्चात कुछ रहने को है, अर्थात् संसार के बहते पानी पर एक बुदजबुदा-मात्र ही यह है, वे वाम-मार्ग के अनुयायी माने जाते हैं। इनके दृष्टिकोण में एक विशेषता यह आ जाती है कि वे जो कुछ भी शरीर के भोग हैं, उनको ही प्रमुख मानते हैं और उनके भोगने के लिए एक अल्प समय ही अपने पास समझते हैं।
इनके विपरीत शुद्ध विचारधारा मानने वाले शरीर को गौण मान आत्मा को अपना एक मुख्य अंग मानते हैं। आत्मा को अमर मानते हैं और एक जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म तक चलने वाला मानते हैं। उनके लिये किसी दुस्तर–से-दुस्तर कार्य-साधन में भी, न तो उतावली की आवश्यकता होती है, न ही अनुचित उपायों के प्रयोग की। वे जन्म के पश्चात जन्म तक, किसी भले कार्य के फलीभूत होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनके लिये मरण, जीवन के अधिष्ठाता आत्मा के अन्त का सूचक नहीं। यह तो केवल जीर्ण वस्त्र बदलना-मात्र है।
इस विवेचना को आधार बनाकर इस पुस्तक की रचना की गई है।
इस सब का क्या लाभ होगा, इसका मूल्यांकन लेखक ने पुस्तक में किया है। शेष पाठकों के समझने की बात है।
जहाँ तक उपन्यास का सम्बन्ध है, सब पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। उपन्यास होने से रोचकता का ध्यान रखा गया है और इस अर्थ किसी बात में कहीं अतिशयोक्ति हो गई हो तो क्षम्य है।
लैफ्टिस्ट (वामपक्षीय) केवल वर्तमान की ओर ध्यान रखने वाले रहे हैं। उनका दृष्टि-क्षेत्र सदा जन्म से मरण तक सीमित रहा है। राजनीति में सभी लैफ्टिस्ट सामयिक सफलता को ही मुख्य मानते हैं। प्रायः राजनीतिक लैफ्टिस्ट, जब सीमित काल में सफलता नहीं पा सकते, तो क्रान्ति की माँग करने लगते हैं। उन्हें सफलता में देरी असह्य हो जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए समय अल्प होने के कारण, वे उचित और अनुचित उपायों का विचार भी छोड़ बैठते हैं।
इसके विपरीत राईटिस्ट (दक्षिण-पंथीय विचार के लोग) वर्तमान जीवन को विराट् जीवन का एक बहुत छोटा भाग मानते हैं। इनका दृष्टि-क्षेत्र अति दूर तक फैला हुआ और गम्भीर होता है। उनको सफलता प्राप्त करने के लिये घबराहट, उतावली, निराशा नहीं होती। वे क्रान्ति को आवश्यक और लाभदायक नहीं मानते और न ही वे सफलता करने में अनुचित उपाय प्रयोग करना उचित समझते हैं। निज, समाज की अथवा संसार की उन्नति उपादेय मानते हुए भी, उसको झूठ, दगा अथवा पाप के मार्ग से प्राप्त करने में हानि मानते हैं।
यह है सिद्धान्तात्मक भेद वामपक्ष और दक्षिण पक्ष में। वाममार्ग मत, मज़हब के क्षेत्र में लैफ्टिज़्म (वामपक्ष) है। मज़हब मनुष्य के आचरण तथा मनुष्य और समाज के सम्बन्ध के विषय की बात बताता है। मनुष्य क्या है ? इसका आदि-अन्त कहाँ है ? संसार के साथ इसका क्या सम्बन्ध है ? मानव-समाज और व्यक्ति के अधिकारों में सीमा कहाँ है ? इन सब और इसी प्रकार की अनेक अन्य बातों में विवेचना करने कि समय, जो मनुष्य जीवन को जन्म से मरण तक ही मानते हैं, न इसके पहले कुछ था, न इसके पश्चात कुछ रहने को है, अर्थात् संसार के बहते पानी पर एक बुदजबुदा-मात्र ही यह है, वे वाम-मार्ग के अनुयायी माने जाते हैं। इनके दृष्टिकोण में एक विशेषता यह आ जाती है कि वे जो कुछ भी शरीर के भोग हैं, उनको ही प्रमुख मानते हैं और उनके भोगने के लिए एक अल्प समय ही अपने पास समझते हैं।
इनके विपरीत शुद्ध विचारधारा मानने वाले शरीर को गौण मान आत्मा को अपना एक मुख्य अंग मानते हैं। आत्मा को अमर मानते हैं और एक जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म तक चलने वाला मानते हैं। उनके लिये किसी दुस्तर–से-दुस्तर कार्य-साधन में भी, न तो उतावली की आवश्यकता होती है, न ही अनुचित उपायों के प्रयोग की। वे जन्म के पश्चात जन्म तक, किसी भले कार्य के फलीभूत होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनके लिये मरण, जीवन के अधिष्ठाता आत्मा के अन्त का सूचक नहीं। यह तो केवल जीर्ण वस्त्र बदलना-मात्र है।
इस विवेचना को आधार बनाकर इस पुस्तक की रचना की गई है।
इस सब का क्या लाभ होगा, इसका मूल्यांकन लेखक ने पुस्तक में किया है। शेष पाठकों के समझने की बात है।
जहाँ तक उपन्यास का सम्बन्ध है, सब पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। उपन्यास होने से रोचकता का ध्यान रखा गया है और इस अर्थ किसी बात में कहीं अतिशयोक्ति हो गई हो तो क्षम्य है।
गुरुदत्त
प्रथम परिच्छेद
नास्तिक्य
पतित-पावनी गंगा के तट पर बसी हुई मोक्षदायिनी काशी, जहाँ जन्म-भर के
पापों से पीड़ित नर-नारी मरने से पूर्व अपनी आत्मा की शान्ति के लिए आते
हैं और जहाँ वेदों के प्रकाण्ड विद्वानों तथा कर्मकाण्डियों की परम्परा-सी
चल पड़ी है, वहीं चार्वाक जैसे वामपक्षीय एवं नास्तिक का पन्थ भी चल पड़ा
था। चार्वाक के प्रशिष्य नाकेश, विपरीत विचारधारा के पोषक होते हुए भी
राज्य परिषद के सदस्य बन, दीपक और छाया की कहावत चरितार्थ करते थे।
महाराज शूरसेन की राज्य-सभा में प्रत्येक विद्वान् का मान होता था और भिन्न-भिन्न विचारों के विचारक वहाँ स्थान पाते थे। जहाँ आस्तिक, कर्मवादी और पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाले महाराज के दक्षिण पार्श्व में बैठते थे वहाँ नाकेश इत्यादि विद्वान महाराज के वाम पार्श्व में आसन पाते थे। इसी कारण इनका नाम वामपक्षीय पड़ गया था।
नाकेश इत्यादि पण्डितों ने वाममार्गीय नाम स्वीकार भी कर लिया था। वह इस कारण नहीं कि उनको राज्य सभा में महाराज के बायें हाथ की ओर स्थान मिलता था, प्रत्युत इस कारण कि वे अपने मार्ग अर्थात् अपनी विचारधारा को सुन्दर, सुखप्रद और सुगम मानते थे।
महाराज शूरसेन की राज्य-परिषद् की एक विशेष बैठक हो रही थी। इसका विशेष प्रयोजन था। नगरपाल ने एक अपराधी को मृत्युदण्ड दिया था और उसके सम्बन्धियों ने महाराज के समक्ष क्षमा-याचिका प्रस्तुत की थी। उस याचिका को सुनने के लिए परिषद् बुलाई गई थी।
सभा में महाराज शूरसेन उच्च सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दक्षिण हाथ की ओर कुछ नीचे आसनों पर महामात्य वीरभद्र, न्यायाधीश पण्डित चतुरंग, नगरपंच श्री केशव और सेनापति राजन विद्यमान थे। महाराज के वाम हाथ की ओर महापण्डित नाकेश, प्रजाप्रतिनिधि शूद्रक, करनायक शूलांग और महिलाशिरोमणि प्रेक्षादेवी विराजमान थे। इनके अतिरिक्त साधारण कोटि के अन्य अनेकों विद्वान भी उपासीन थे।
अपराधी एक ब्राह्मण बालक था-उन्नीस-बीस वर्ष की आयु का; ब्रह्मचारी के पीत-वर्ण वस्त्र पहने, नग्न शिर, शिखा को बड़ी-सी गाँठ दिये, ओजस्वी मुख और लम्बे कद वाला। वह सभा भवन के मध्य में खड़ा था। उसके पीछे रक्षार्थ चार सैनिक खड़े थे। अपराधी के सम्बन्धी भी भवन में एक ओर खड़े थे। नगरपाल अपने स्थान के पीछे कुछ अन्तर पर कई नागरिक सम्मानयुक्त मुद्रा में खड़े थे।
महाराज की आज्ञा पाकर नगरपाल ने झुक कर नमस्कार किया, फिर उच्च स्वर में कहा, ‘‘काशिराज की जय हो।’’
इस घोषणा के बाद अपराधी के सम्बन्धियों में से एक वृद्ध ने, ‘‘महाराज की जय हो’’ कह कर आशीर्वाद दिया। इस पर महाराज ने नगरपाल को सम्बोधित कर पूछा, ‘‘इस बालक का क्या अपराध है?’’
‘‘महाराज ! इसने गुरु-पत्नी से सम्भोग किया है और हमारे शास्त्र के विधानानुसार इस अपराध का दण्ड अपराधी को चिता में जीवित जला देना है।’’ महाराज ने बालक के सुकुमार मुख को देखा तो उसके अपराधी होने में सन्देह करते हुए पूछा, ‘‘बालक ! क्या यह सत्य है?’’
‘सत्य है महाराज ! मैं इस नीच कर्म करने का अपराधी हूँ।’’
‘‘‘‘तुमको मृत्यु-दण्ड मिला है, जानते हो ?’’
‘‘हाँ महाराज ! जानता हूँ।’’
‘‘तुम क्या चाहते हो ?’’
‘‘मैं इस दण्ड के शीघ्र दिये जाने की प्रार्थना कर रहा हूँ।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘इस पतित शरीर से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। इसको भस्म कर देना चाहता हूँ जिससे इस पवित्र नगरी का वायुमण्डल दूषित न हो।’’
‘‘तो यह क्षमा याचिका किसने की है ?’’
सभा-मण्डप में एक ओर खड़े बालक के सम्बन्धियों से एक वृद्ध ब्राह्मण ने आगे बढ़, हाथ जोड़कर कहा, ‘‘महाराज ! भगवान् आपको चिरंजीवी रखे। इस याचना को करने वाला, करबद्ध यह वृद्ध ब्राह्मण सम्मुख उपस्थित है।’’
‘‘क्षमा किये जाने के लिए क्या युक्ति है ?’’
‘प्रथम, बालक का अपराध इतना नहीं है जितना इससे सहवास करने वाली स्त्री का है। वह भोग और विलास से परिचित थी। उसको इस विषय में बालक का पथ-प्रदर्शन कर उसे इस मार्ग पर चलने का प्रलोभन देना उचित नहीं था। वह स्त्री तीस वर्ष की आयु की होकर इस विषय में पर्याप्त अनुभव रखती होगी। अतः बालक इस कार्य में एक गौण अपराधी होने से क्षमा का भागी है।
‘‘द्वितीय यह, इस बालक वृद्ध और इस समीप खड़ी वृद्धा की एक-मात्र सन्तान है। यह हमारी वृद्धावस्था का एक-मात्र आश्रय है। इसको दण्ड देने से हम निर्दोष दण्डित हो जावेंगे। यह वृद्ध ब्राह्मण अपनी विद्या और ज्ञान से काशी के नागरिकों की सेवा करता रहा है। अपनी सेवाओं के उपलक्ष्य में इस बालक के जीवन-दान की याचना करने आया है।
‘‘तृतीय, बालक अल्प-वयस्क है, सुन्दर है, युवा है मेधावी है, शास्त्र और समाज की सेवा के योग्य है। इस कारण दया का भागी है।’’
महाराज ने ब्राह्मण की युक्तियाँ सुन कहा, ‘‘किसी अन्य को कुछ कहना है ?’’
ब्राह्मण के समीप खड़ी वृद्धा ब्राह्मणी ने घुटने टेक, माथा भूमि पर रख रूदन करते हुए कहा, ‘‘मेरे पुण्य कर्मों का फल, जिनसे मुझको ब्राह्मण-जन्म मिला है, महाराज को लगे। इस जन्म में किये मेरे सब श्रेष्ठ कर्मों के फल के महाराज भागी हों। मेरा बेटा मुझको मिल जाये।’’
महाराज आसन से उठ खड़े हुए और बोले, ‘‘देवी उठो ! तुम्हारे साथ न्याय होगा। दया के लिए भगवान से प्रार्थना करो। वह दयालु है, दयानिधि है, कृपासागर है।’’
ब्राह्मण ने अपनी अर्धांगिनी को उठाया। उसके सिर पर हाथ फेरा और ढाढस बँधाते हुए कहा, ‘‘प्रिये ! अधीर मत बनो। इस पवित्र काशी में अन्याय नहीं हो सकता; साथ ही न्याय दयायुक्त भी होगा।’’
ब्राह्मणी सिसकियाँ भरती हुई उठी और अपनी अवस्था को छिपाने के लिए ब्राह्मण के पीछे खड़ी हो गई।
महाराज शूरसेन ने नगरपाल से पूछा, ‘‘इस बालक से सहवास करने वाली स्त्री को क्या दण्ड मिला है ?’’
‘‘महाराज ! हमारे राज्य में स्त्रियों को दण्ड देने का विधान नहीं है। उनको अपने पतियों के हाथ में ही छोड़ दिया जाता है और वे ही उनके दण्ड का विधान करते हैं।’’
‘‘ऐसा क्यों है ? क्या वे राज्य की नागरिक नहीं हैं ?’’
‘‘हैं महाराज ! परन्तु यह प्रश्न तो महामात्य जी से अथवा न्यायाधीश से किया जाना चाहिए। यह सेवक व्यवस्था नहीं दे सकता न ही किसी व्यवस्था पर समालोचना कर सकता है।’
‘वीरभद्र !’’ महाराज ने महामात्य से पूछा, ‘‘स्त्रियों के लिए यह पृथक् विधान क्यों है ?’’
महाराज शूरसेन की राज्य-सभा में प्रत्येक विद्वान् का मान होता था और भिन्न-भिन्न विचारों के विचारक वहाँ स्थान पाते थे। जहाँ आस्तिक, कर्मवादी और पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाले महाराज के दक्षिण पार्श्व में बैठते थे वहाँ नाकेश इत्यादि विद्वान महाराज के वाम पार्श्व में आसन पाते थे। इसी कारण इनका नाम वामपक्षीय पड़ गया था।
नाकेश इत्यादि पण्डितों ने वाममार्गीय नाम स्वीकार भी कर लिया था। वह इस कारण नहीं कि उनको राज्य सभा में महाराज के बायें हाथ की ओर स्थान मिलता था, प्रत्युत इस कारण कि वे अपने मार्ग अर्थात् अपनी विचारधारा को सुन्दर, सुखप्रद और सुगम मानते थे।
महाराज शूरसेन की राज्य-परिषद् की एक विशेष बैठक हो रही थी। इसका विशेष प्रयोजन था। नगरपाल ने एक अपराधी को मृत्युदण्ड दिया था और उसके सम्बन्धियों ने महाराज के समक्ष क्षमा-याचिका प्रस्तुत की थी। उस याचिका को सुनने के लिए परिषद् बुलाई गई थी।
सभा में महाराज शूरसेन उच्च सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दक्षिण हाथ की ओर कुछ नीचे आसनों पर महामात्य वीरभद्र, न्यायाधीश पण्डित चतुरंग, नगरपंच श्री केशव और सेनापति राजन विद्यमान थे। महाराज के वाम हाथ की ओर महापण्डित नाकेश, प्रजाप्रतिनिधि शूद्रक, करनायक शूलांग और महिलाशिरोमणि प्रेक्षादेवी विराजमान थे। इनके अतिरिक्त साधारण कोटि के अन्य अनेकों विद्वान भी उपासीन थे।
अपराधी एक ब्राह्मण बालक था-उन्नीस-बीस वर्ष की आयु का; ब्रह्मचारी के पीत-वर्ण वस्त्र पहने, नग्न शिर, शिखा को बड़ी-सी गाँठ दिये, ओजस्वी मुख और लम्बे कद वाला। वह सभा भवन के मध्य में खड़ा था। उसके पीछे रक्षार्थ चार सैनिक खड़े थे। अपराधी के सम्बन्धी भी भवन में एक ओर खड़े थे। नगरपाल अपने स्थान के पीछे कुछ अन्तर पर कई नागरिक सम्मानयुक्त मुद्रा में खड़े थे।
महाराज की आज्ञा पाकर नगरपाल ने झुक कर नमस्कार किया, फिर उच्च स्वर में कहा, ‘‘काशिराज की जय हो।’’
इस घोषणा के बाद अपराधी के सम्बन्धियों में से एक वृद्ध ने, ‘‘महाराज की जय हो’’ कह कर आशीर्वाद दिया। इस पर महाराज ने नगरपाल को सम्बोधित कर पूछा, ‘‘इस बालक का क्या अपराध है?’’
‘‘महाराज ! इसने गुरु-पत्नी से सम्भोग किया है और हमारे शास्त्र के विधानानुसार इस अपराध का दण्ड अपराधी को चिता में जीवित जला देना है।’’ महाराज ने बालक के सुकुमार मुख को देखा तो उसके अपराधी होने में सन्देह करते हुए पूछा, ‘‘बालक ! क्या यह सत्य है?’’
‘सत्य है महाराज ! मैं इस नीच कर्म करने का अपराधी हूँ।’’
‘‘‘‘तुमको मृत्यु-दण्ड मिला है, जानते हो ?’’
‘‘हाँ महाराज ! जानता हूँ।’’
‘‘तुम क्या चाहते हो ?’’
‘‘मैं इस दण्ड के शीघ्र दिये जाने की प्रार्थना कर रहा हूँ।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘इस पतित शरीर से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। इसको भस्म कर देना चाहता हूँ जिससे इस पवित्र नगरी का वायुमण्डल दूषित न हो।’’
‘‘तो यह क्षमा याचिका किसने की है ?’’
सभा-मण्डप में एक ओर खड़े बालक के सम्बन्धियों से एक वृद्ध ब्राह्मण ने आगे बढ़, हाथ जोड़कर कहा, ‘‘महाराज ! भगवान् आपको चिरंजीवी रखे। इस याचना को करने वाला, करबद्ध यह वृद्ध ब्राह्मण सम्मुख उपस्थित है।’’
‘‘क्षमा किये जाने के लिए क्या युक्ति है ?’’
‘प्रथम, बालक का अपराध इतना नहीं है जितना इससे सहवास करने वाली स्त्री का है। वह भोग और विलास से परिचित थी। उसको इस विषय में बालक का पथ-प्रदर्शन कर उसे इस मार्ग पर चलने का प्रलोभन देना उचित नहीं था। वह स्त्री तीस वर्ष की आयु की होकर इस विषय में पर्याप्त अनुभव रखती होगी। अतः बालक इस कार्य में एक गौण अपराधी होने से क्षमा का भागी है।
‘‘द्वितीय यह, इस बालक वृद्ध और इस समीप खड़ी वृद्धा की एक-मात्र सन्तान है। यह हमारी वृद्धावस्था का एक-मात्र आश्रय है। इसको दण्ड देने से हम निर्दोष दण्डित हो जावेंगे। यह वृद्ध ब्राह्मण अपनी विद्या और ज्ञान से काशी के नागरिकों की सेवा करता रहा है। अपनी सेवाओं के उपलक्ष्य में इस बालक के जीवन-दान की याचना करने आया है।
‘‘तृतीय, बालक अल्प-वयस्क है, सुन्दर है, युवा है मेधावी है, शास्त्र और समाज की सेवा के योग्य है। इस कारण दया का भागी है।’’
महाराज ने ब्राह्मण की युक्तियाँ सुन कहा, ‘‘किसी अन्य को कुछ कहना है ?’’
ब्राह्मण के समीप खड़ी वृद्धा ब्राह्मणी ने घुटने टेक, माथा भूमि पर रख रूदन करते हुए कहा, ‘‘मेरे पुण्य कर्मों का फल, जिनसे मुझको ब्राह्मण-जन्म मिला है, महाराज को लगे। इस जन्म में किये मेरे सब श्रेष्ठ कर्मों के फल के महाराज भागी हों। मेरा बेटा मुझको मिल जाये।’’
महाराज आसन से उठ खड़े हुए और बोले, ‘‘देवी उठो ! तुम्हारे साथ न्याय होगा। दया के लिए भगवान से प्रार्थना करो। वह दयालु है, दयानिधि है, कृपासागर है।’’
ब्राह्मण ने अपनी अर्धांगिनी को उठाया। उसके सिर पर हाथ फेरा और ढाढस बँधाते हुए कहा, ‘‘प्रिये ! अधीर मत बनो। इस पवित्र काशी में अन्याय नहीं हो सकता; साथ ही न्याय दयायुक्त भी होगा।’’
ब्राह्मणी सिसकियाँ भरती हुई उठी और अपनी अवस्था को छिपाने के लिए ब्राह्मण के पीछे खड़ी हो गई।
महाराज शूरसेन ने नगरपाल से पूछा, ‘‘इस बालक से सहवास करने वाली स्त्री को क्या दण्ड मिला है ?’’
‘‘महाराज ! हमारे राज्य में स्त्रियों को दण्ड देने का विधान नहीं है। उनको अपने पतियों के हाथ में ही छोड़ दिया जाता है और वे ही उनके दण्ड का विधान करते हैं।’’
‘‘ऐसा क्यों है ? क्या वे राज्य की नागरिक नहीं हैं ?’’
‘‘हैं महाराज ! परन्तु यह प्रश्न तो महामात्य जी से अथवा न्यायाधीश से किया जाना चाहिए। यह सेवक व्यवस्था नहीं दे सकता न ही किसी व्यवस्था पर समालोचना कर सकता है।’
‘वीरभद्र !’’ महाराज ने महामात्य से पूछा, ‘‘स्त्रियों के लिए यह पृथक् विधान क्यों है ?’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book