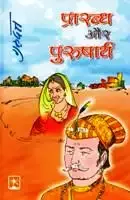|
सामाजिक >> प्रारब्ध और पुरुषार्थ प्रारब्ध और पुरुषार्थगुरुदत्त
|
443 पाठक हैं |
||||||
प्रारब्ध है पूर्व जन्म के कर्मों का फल। फल तो भोगना ही पड़ता है, परन्तु पुरुषार्थ से उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है
प्रथम उपन्यास ‘‘स्वाधीनता के पथ पर’’ से ही ख्याति की सीढ़ियों पर जो चढ़ने लगे कि फिर रुके नहीं।
विज्ञान की पृष्ठभूमि पर वेद, उपनिषद् दर्शन इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन आरम्भ किया तो उनको ज्ञान का अथाह सागर देख उसी में रम गये।
वेद, उपनिषद् तथा दर्शन शास्त्रों की विवेचना एवं अध्ययन अत्यन्त सरल भाषा में प्रस्तुत करना गुरुदत्त की ही विशेषता रही है।
उपन्यासों में भी शास्त्रों का निचोड़ तो मिलता ही है, रोचकता के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि उनका कोई भी उपन्यास पढ़ना आरम्भ करने पर समाप्त किये बिना छोड़ा नहीं जा सकता।
विज्ञान की पृष्ठभूमि पर वेद, उपनिषद् दर्शन इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन आरम्भ किया तो उनको ज्ञान का अथाह सागर देख उसी में रम गये।
वेद, उपनिषद् तथा दर्शन शास्त्रों की विवेचना एवं अध्ययन अत्यन्त सरल भाषा में प्रस्तुत करना गुरुदत्त की ही विशेषता रही है।
उपन्यासों में भी शास्त्रों का निचोड़ तो मिलता ही है, रोचकता के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि उनका कोई भी उपन्यास पढ़ना आरम्भ करने पर समाप्त किये बिना छोड़ा नहीं जा सकता।
प्रारब्ध और पुरुषार्थ
प्रारब्ध है पूर्व जन्म के कर्मों का फल। फल तो भोगना ही पड़ता है, परन्तु
पुरुषार्थ से उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है अथवा यह भी कहा जा सकते
हैं कि उसको सहन करने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ‘‘प्रारब्ध
और पुरुषार्थ’’ का यही कथानक है। अकबर के जीवन के एक
पृष्ठ को आधार बनाकर रचा गया अत्यन्त रोचक उपन्यास।
मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है। इस कारण भाग्य (प्रारब्ध) के विरुद्ध जब वह पुरुषार्थ करता है तो उसके परिणाम (शुभ अथवा अशुभ) का उत्तरदायित्व उसका अपना होता है। तब वह भाग्य पर दोषारोपण नहीं कर सकता।
मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है। इस कारण भाग्य (प्रारब्ध) के विरुद्ध जब वह पुरुषार्थ करता है तो उसके परिणाम (शुभ अथवा अशुभ) का उत्तरदायित्व उसका अपना होता है। तब वह भाग्य पर दोषारोपण नहीं कर सकता।
प्रथम परिच्छेद
आगरा से दस मील उत्तर की ओर मथुरा की सड़क के किनारे भटियारिन की सराय नाम
का एक स्थान था जिसके आज भग्नांश ही शेष रह गए हैं। अकबर के काल में वहाँ
एक सराय थी और अकबर के पोते शहंशाह शाहजहाँ के काल में वहाँ एक भरा-पूरा
गाँव था। इस पर भी इस निर्धनों के गाँव में महल और अटारियाँ थीं, सड़कें
और उद्यान थे। आज उस स्थान पर एक टीला है जो प्रकट करता है कि वह किसी
गाँव के मलबे का ढेर है।
अकबर अभी बीस-इक्कीस वर्ष की वयस् का ही था और अपने गुरु और सरपरस्त बहरामखाँ के शिकंजे से छूट कर खुदमुखत्यार शहंशाह के रूप में आए उसे दस-बारह वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अकबर दिल्ली और आगरा प्रायः आता-जाता रहता था। उसका स्वभाव था कि घोड़े पर सवार हो दिल्ली से एक दिन में मथुरा और मथुरा से आधे दिन में आगरा आ जाया करता था। मार्ग में भटियारिन की सराय एक नगण्य स्थान था। सरपट दौड़ते घोड़े पर सवार हो जाते हुए उसका इस सराय की ओर कभी ध्यान भी नहीं गया था। साथ ही उसने आगरा से तीन कोस उत्तर की ओर एक विशेष आरामगाह बना रखी थी। कभी आगरा पहुँचने में देर हो जाती तो रात इस आरामगाह में आराम कर वह प्रातः तरोताजा हो आगरा पहुँचने में लाभ समझता था।
इस आरामगाह का नाम ‘नगर चैन’ विख्यात था। वहाँ शाही सुख-आराम की सुविधा रहती थी। इस कारण ‘नगर चैन’ के समीप होने से भटियारिन की सराय की ओर शहंशाह का कभी ध्यान भी नहीं गया था।
इस दिन सराय के सामने से गुजरते हुए अकबर के घोड़े की नाल उखड़ गई। घोड़े ने लँगड़ाकर चलना आरंभ कर दिया। अकबर एक अनुभवी घुड़सवार होने के कारण घोड़े के लँगड़ाने को देख उसे खड़ा कर उतर गया। उसके साथ आ रहे आधा दर्जन सिहपाही भी खड़े हो गए। अकबर ने सिपाहियों के सालार से कहा, ‘‘करीमखाँ ! देखो, यह कौन-सी जगह है।’’
करीमखाँ इस वीराने में एक पक्का मकान बना देख उसकी ओर चल पड़ा। मकान एक अहाते की सूरत-शक्ल का था और अहाते में यात्रियों के रहने के कमरे थे। अहाते के भीतर जाने के लिए एक फाटक बना था और फाटक के बाहर एक दुकान और प्याऊ थी। दुकान भुने चने की थी और चना खानेवालों के लिए मिट्टी के मटके में ठंडा पानी रहता था। चने खाने पर वहाँ जल बिना दाम के मिलता था। दुकान में चना भूनने की भट्टी भी थी।
करीमखाँ शहंशाह को सड़क पर ही छोड़ इस दुकान की ओर आया और दुकान में बैठी एक कमसिन लड़की को कड़ाही में गरम-गरम रेत में चनों को भूनते और हिलाते देख पूछने लगा, ‘‘ए लड़की। यह कौन-सी जगह है ?’’
लड़की ने अपना सिर चनों की कड़ाही से ऊपर उठा इस प्रश्न करने वाले की ओर देख कह दिया, ‘‘ए तिलंगे ! यह भटियारिन की सराय है।’’
करीमखाँ लड़की की हाजिर जबावी पर विस्मय से उसके मुख को देखने लगा। लड़की ने उसे अपने मुख को देखते हुए कह दिया, ‘‘जेब में दाम है तो सराय में ठहर सकते हो।’’
करीमखाँ को लड़की की शोखी पसंद आई। वह भटियारिन के मैले और धुएँ से काले हुए कपड़ो में एक अति सुंदर मुख दिखाई दिया। बड़ी-बड़ी आँखें और मोटे-मोटे लाल होंठ, उभरती जवानी के लक्षण देख वह मुग्ध होकर उसका मुख देखता रह गया।
लड़की अब चने और रेत को कड़ाही में से छननी में ले हिला रही थी। उसने रेत कड़ाही में छन जाने पर भुने चने समीप रखी टोकरी में डाल दिए और दुकान के बाहर खड़े सिपाही से बोली, ‘‘मेरे मुख को क्या देख रहे हो ? क्या चाहते हो ?’’
करीमखाँ ने मुस्कराते हुए कहा, ‘‘पर मैं तिलंगा नहीं हूँ।’’
तिलंगे दक्षिण के सिपाहियों को कहते थे जो रोजगार की तलाश में उत्तरी भारत में राजा-रईसों की नौकरी करते थे। वे प्रायः हिंदू होते थे। करीमखाँ तो पठानी सलवार और कुर्ता तथा कुर्ते पर कुर्ती पहने हुए था।
लड़की ने तुरत उत्तर दिया, ‘‘तिलंगे नहीं तो लफंगे जरूर हो। किसलिए खड़े हो ?’’
करीमखाँ को शहंशाह के सड़क पर खड़े प्रतीक्षा करने की बात याद आ गई। इस कारण उसने मतलब की बात कर दी, ‘‘यहाँ घोड़े की नाल लगानेवाला कोई लोहार है ?’’
‘‘सराय के फाटक के भीतर साथ ही लोहार की दुकान है। वह नाल लगा देगा। किसकी नाल उखड़ गई है ?’’
करीमखाँ मुस्कराया और शहंशाह की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँच कर उसने कहा, ‘‘जहाँपनाह ! एक लोहार का पता चला है। लाइए घोड़ा, अभी ठीक करवा लाता हूँ।’’
‘‘और यह किस शै की दुकान है ?’’
‘‘एक भटियारिन की दुकान है और यह सराय है। नाम है भटियारिन की सराय।’’
‘‘हुज़ूर !...’’ करीमखाँ लड़की के विषय में कुछ कहना चाहता था, परंतु अन्य सिपाहियों की उपस्थिति में कह नहीं सका और घोड़े की लगाम पकड़ लँगड़ाते घोड़े को लेकर सराय के फाटक की ओर चल पड़ा।
दुकान के बाहर एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के साए में बैठ यात्री चने खाया करते थे और ठंडा पानी पी चनों का दाम दे चल देते थे। जो दिन के चौथे प्रहर पहुंचते थे और सूर्यास्त से पूर्व मंजिल पर पहुँचने की आशा नहीं रखते थे, वहीं सराय में रह जाते थे। सराय में दो पैसे नित्य के भाड़े पर मिलने वाली खाट से लेकर एक रुपया नित्य पर मिलने वाले कमरे तक का प्रबंध था। सराय के फाटक पर एक व्यक्ति खाट डाले बैठा था। उसने करीमखाँ को लँगड़ाते घोड़े के साथ आते देखा तो समझ गया कि घोड़े की नाल उखड़ गई है। उसने खाट पर बैठे-बैठे ही हाथ से लोहार की दुकान की ओर संकेत कर दिया।
करीमखाँ उस ओर चला गया। अकबर सड़क पर खड़ा रहने के स्थान, भटियारिन की दुकान के बाहर पीपल की छाया में आ खड़ा हुआ। लड़की फिर चने के दाने कड़ाही की रेत में डाल हिलाने लगी थी। वह दूसरे हाथ से कड़ाही के नीचे सूखे पत्ते इत्यादि डाल-डालकर आग को तीव्र कर रही थी।
अकबर की दृष्टि भी भटियारिन की ओर गई तो वह उसकी रूप-रेखा पर मुग्ध हो गया। उसने दुकान के सामने जाकर कहा, ‘‘सुंदरी ! एक टके के चने दो।’’
‘सुंदरी’ शब्द से लड़की का ध्यान भट्टी की ओर से हटकर शहंशाह पर गया। उसकी पोसाक और रूप-राशि देख लड़की समझ गई कि कोई रईस है। इसी समय उसने सड़क पर आधे दर्जन सिपाहियों को भी खड़े देखा। इस कारण वह बोली, ‘‘हुज़ूर ! ज़रा ठहरिए। इस पुर को निकाल लूँ तो देती हूँ।’’
‘‘किसकी बेटी हो ?’’
‘‘इस सराय के मालिक की।’’
‘‘वह कहाँ है ?’’
‘‘भीतर किसी काम से गया है।’’
‘‘बहुत सख्त काम वह तुमसे ले रहा है।’’ अकबर ने लड़की से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा। लड़की रेत और चने छननी में लेकर भुने रेत से पृथक कर रही थी। काम में व्यस्त और यात्री की ओर न देखते हुए उसने कह दिया, ‘‘हुज़ूर ! पेट की खातिर सब मेहनत करते हैं। आप भी तो इस धूप में यात्रा कर रहे हैं।’’
‘‘तो मैं भी पेट के लिए कर रहा हूँ ?’’ अकबर ने लड़की से बातों में दिल बहलाने के लिए कह दिया।
लड़की का सतर्क उत्तर था, ‘‘शरीर, मन और बुद्धि की तसल्ली के लिए ही तो सब संसार भाग-दौड़ रहा है।’’
‘‘ओह !’’ अकबर को लड़की के उत्तर में एक श्रेष्ठ मंतक (मीमांसा) युक्त कथन ही लगा। वह आवाक् लड़की के मुख को देखता रह गया।
लड़की ने तराजू उठाया और एक पत्थर का बाट डाल चने तोल तराजू का पलड़ा शहंशाह की ओर कर दिया और कहा, ‘‘हुज़ूर ! किसी रुमाल में डलवा लें।’’
अकबर तो लड़की के हाथ-पाँव और शरीर की बनावट को देख रहा था। लड़की ने तराजू के पलड़े को आगे किया और शहंशाह ने जब चनों के लिए रुमाल नहीं निकाला तो लड़की ने कहा, ‘‘यह हैं दो पैसे के चने बताइए, किसमें लेंगे ?’’
‘‘ओह !’’ अकबर ने जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला तो लड़की ने समझा कि रुमाल तो बहुत कीमती है। चनों से खराब भी हो सकता है। इस कारण उसने कहा, ‘‘तो इस पर डाल दूँ ? परंतु आप तो मेरे मुख को देख रहे हैं।’’
‘‘हाँ ! क्या उम्र है तुम्हारी ?’’
‘‘तो दो पैसे में यह भी बताना पड़ेगा ?’’
‘‘इसके बताने का दाम अलहदा भी दिया जा सकता है।’’
‘‘नहीं। मेरी माँ कहती है कि मैं आगामी कार्तिक से पंद्रह साल की हो जाऊँगी।’’
‘‘और तुम्हारी शादी नहीं हुई ?’’
इसका उत्तर लड़की ने नहीं दिया और चने बिछे रेशमी रुमाल पर डाल दो पैसे लेने के लिए हाथ पसार दिया।
अकबर ने जेब से एक स्वर्ण मुहर निकालकर लड़की की ओर बढ़ाई। लड़की मुहर को देखकर बोली, ‘‘इसका बाकी मेरे पास नहीं है।’’
‘‘और मेरे पास इससे कम नहीं हैं।’’
‘‘तो रहने दो।’’
‘‘और चनों के दाम ?’’
‘‘फिर कभी इधर आइएगा तो दे दीजिएगा।’’
‘‘और अगर मैं न दूँ तो ?’’
‘‘तो आप बेईमान भी हैं ? आप तो रईस मालूम होते हैं।’’
‘‘तो रईस बेईमान नहीं होते ?’’
‘‘उनको बेईमानी करने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा ने उन्हें इतना कुछ दिया होता है कि उन्हें दो पैसे के लिए मुकर जाने की जरूरत नहीं होती।’’
अकबर विचार कर रहा था कि वह तो नित्य अपने राज्य की वृद्धि के लिए झूठ, फरेब और बल का प्रयोग कर रहा है। तो क्या वह कंगला है जो यह करता है ?
उसे लड़की की दलील गलत समझ आई। उसकी तीन बेगमें तो राजमहल में ही थीं और उनके अतिरिक्त भी कई स्त्रियों से संबंध था। उस पर भी वह इस लड़की के सौंदर्य को, जो मैले, भट्टी के धुएँ से काले हुए कपड़ों में छुपा हुआ था, देख मन में इसको प्राप्त करने की लालसा करने लगा था।
वह यह समझा कि यह जीवन-मीमांसा निर्धनों को शांत और अपनी निर्धनता से संतुष्ट रखने के लिए किसी ने बनाई है। वस्तुस्थिति यह है कि धनवान अधिक लोभी होते हैं। निर्धन धनवानों से अधिक संतोषी और ईमानदार होते हैं।
‘‘मैं तो रईस हूँ, मगर दो पैसे के लिए बेईमान भी हो सकता हूँ।’’
‘‘तो परमात्मा तुमसे अगले जन्म में नाक में नकेल डालकर दिलवा देगा।’’
‘‘नहीं। मैं तो इसी जन्म में दाम अदा करना चाहता हूँ।’’
‘‘तो अपने किसी साथी से दो पैसे मांग लो।’’ इतना कहकर लड़की ने सड़क पर खड़े सिपाहियों की ओर देखा।
अकबर को यह बात समझ आई तो उसने कह दिया, ‘‘तो मैं देखता हूँ कि किसी के पास एक टका है अथवा नहीं।’’
इतना कह वह रुमाल में चने बाँध सड़क की ओर चल पड़ा। भटियारिन अपने काम में लीन हो गई और दो पैसे की बात भूल गई।
एक घड़ी लगी घोड़े की नाल लगाने में। करीमखाँ घोड़े की नाल लगवा उसे लगाम से पकड़ सड़क पर ले आया। सड़क पर करीमखाँ से शहंशाह ने कुछ बात कही और वह दो सिपाहियों के साथ दुकान पर आया और लपककर दुकान पर चढ़ लड़की को पकड़ कंधे पर डाल सड़क की ओर भागा।
लड़की ने शोर मचा दिया, ‘‘बचाओ ! बचाओ ! बाबा ! बचाओ !’’
सराय में से तीन-चार व्यक्ति हाथों में तलवारें लिए निकल आए और सड़क पर लड़की को छटपटाते हुए और चीख-पुकार करते हुए देख उधर लपके।
अकबर लड़की को अपने घोड़े पर लाद स्वयं घोड़े पर सवार हो सरपट भागता हुआ चल दिया। उसके सिपाही घोड़ों पर सवार हो शहंशाह के पीछे चल पड़े।
सराय में से निकले लोग हाथों में तलवार लिए लड़की का अपहरण करनेवालों को घोड़े दौड़ाते हुए और अपने पीछे उड़ती धूल छोड़ते हुए देखते रह गए।
अकबर अभी बीस-इक्कीस वर्ष की वयस् का ही था और अपने गुरु और सरपरस्त बहरामखाँ के शिकंजे से छूट कर खुदमुखत्यार शहंशाह के रूप में आए उसे दस-बारह वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अकबर दिल्ली और आगरा प्रायः आता-जाता रहता था। उसका स्वभाव था कि घोड़े पर सवार हो दिल्ली से एक दिन में मथुरा और मथुरा से आधे दिन में आगरा आ जाया करता था। मार्ग में भटियारिन की सराय एक नगण्य स्थान था। सरपट दौड़ते घोड़े पर सवार हो जाते हुए उसका इस सराय की ओर कभी ध्यान भी नहीं गया था। साथ ही उसने आगरा से तीन कोस उत्तर की ओर एक विशेष आरामगाह बना रखी थी। कभी आगरा पहुँचने में देर हो जाती तो रात इस आरामगाह में आराम कर वह प्रातः तरोताजा हो आगरा पहुँचने में लाभ समझता था।
इस आरामगाह का नाम ‘नगर चैन’ विख्यात था। वहाँ शाही सुख-आराम की सुविधा रहती थी। इस कारण ‘नगर चैन’ के समीप होने से भटियारिन की सराय की ओर शहंशाह का कभी ध्यान भी नहीं गया था।
इस दिन सराय के सामने से गुजरते हुए अकबर के घोड़े की नाल उखड़ गई। घोड़े ने लँगड़ाकर चलना आरंभ कर दिया। अकबर एक अनुभवी घुड़सवार होने के कारण घोड़े के लँगड़ाने को देख उसे खड़ा कर उतर गया। उसके साथ आ रहे आधा दर्जन सिहपाही भी खड़े हो गए। अकबर ने सिपाहियों के सालार से कहा, ‘‘करीमखाँ ! देखो, यह कौन-सी जगह है।’’
करीमखाँ इस वीराने में एक पक्का मकान बना देख उसकी ओर चल पड़ा। मकान एक अहाते की सूरत-शक्ल का था और अहाते में यात्रियों के रहने के कमरे थे। अहाते के भीतर जाने के लिए एक फाटक बना था और फाटक के बाहर एक दुकान और प्याऊ थी। दुकान भुने चने की थी और चना खानेवालों के लिए मिट्टी के मटके में ठंडा पानी रहता था। चने खाने पर वहाँ जल बिना दाम के मिलता था। दुकान में चना भूनने की भट्टी भी थी।
करीमखाँ शहंशाह को सड़क पर ही छोड़ इस दुकान की ओर आया और दुकान में बैठी एक कमसिन लड़की को कड़ाही में गरम-गरम रेत में चनों को भूनते और हिलाते देख पूछने लगा, ‘‘ए लड़की। यह कौन-सी जगह है ?’’
लड़की ने अपना सिर चनों की कड़ाही से ऊपर उठा इस प्रश्न करने वाले की ओर देख कह दिया, ‘‘ए तिलंगे ! यह भटियारिन की सराय है।’’
करीमखाँ लड़की की हाजिर जबावी पर विस्मय से उसके मुख को देखने लगा। लड़की ने उसे अपने मुख को देखते हुए कह दिया, ‘‘जेब में दाम है तो सराय में ठहर सकते हो।’’
करीमखाँ को लड़की की शोखी पसंद आई। वह भटियारिन के मैले और धुएँ से काले हुए कपड़ो में एक अति सुंदर मुख दिखाई दिया। बड़ी-बड़ी आँखें और मोटे-मोटे लाल होंठ, उभरती जवानी के लक्षण देख वह मुग्ध होकर उसका मुख देखता रह गया।
लड़की अब चने और रेत को कड़ाही में से छननी में ले हिला रही थी। उसने रेत कड़ाही में छन जाने पर भुने चने समीप रखी टोकरी में डाल दिए और दुकान के बाहर खड़े सिपाही से बोली, ‘‘मेरे मुख को क्या देख रहे हो ? क्या चाहते हो ?’’
करीमखाँ ने मुस्कराते हुए कहा, ‘‘पर मैं तिलंगा नहीं हूँ।’’
तिलंगे दक्षिण के सिपाहियों को कहते थे जो रोजगार की तलाश में उत्तरी भारत में राजा-रईसों की नौकरी करते थे। वे प्रायः हिंदू होते थे। करीमखाँ तो पठानी सलवार और कुर्ता तथा कुर्ते पर कुर्ती पहने हुए था।
लड़की ने तुरत उत्तर दिया, ‘‘तिलंगे नहीं तो लफंगे जरूर हो। किसलिए खड़े हो ?’’
करीमखाँ को शहंशाह के सड़क पर खड़े प्रतीक्षा करने की बात याद आ गई। इस कारण उसने मतलब की बात कर दी, ‘‘यहाँ घोड़े की नाल लगानेवाला कोई लोहार है ?’’
‘‘सराय के फाटक के भीतर साथ ही लोहार की दुकान है। वह नाल लगा देगा। किसकी नाल उखड़ गई है ?’’
करीमखाँ मुस्कराया और शहंशाह की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँच कर उसने कहा, ‘‘जहाँपनाह ! एक लोहार का पता चला है। लाइए घोड़ा, अभी ठीक करवा लाता हूँ।’’
‘‘और यह किस शै की दुकान है ?’’
‘‘एक भटियारिन की दुकान है और यह सराय है। नाम है भटियारिन की सराय।’’
‘‘हुज़ूर !...’’ करीमखाँ लड़की के विषय में कुछ कहना चाहता था, परंतु अन्य सिपाहियों की उपस्थिति में कह नहीं सका और घोड़े की लगाम पकड़ लँगड़ाते घोड़े को लेकर सराय के फाटक की ओर चल पड़ा।
दुकान के बाहर एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के साए में बैठ यात्री चने खाया करते थे और ठंडा पानी पी चनों का दाम दे चल देते थे। जो दिन के चौथे प्रहर पहुंचते थे और सूर्यास्त से पूर्व मंजिल पर पहुँचने की आशा नहीं रखते थे, वहीं सराय में रह जाते थे। सराय में दो पैसे नित्य के भाड़े पर मिलने वाली खाट से लेकर एक रुपया नित्य पर मिलने वाले कमरे तक का प्रबंध था। सराय के फाटक पर एक व्यक्ति खाट डाले बैठा था। उसने करीमखाँ को लँगड़ाते घोड़े के साथ आते देखा तो समझ गया कि घोड़े की नाल उखड़ गई है। उसने खाट पर बैठे-बैठे ही हाथ से लोहार की दुकान की ओर संकेत कर दिया।
करीमखाँ उस ओर चला गया। अकबर सड़क पर खड़ा रहने के स्थान, भटियारिन की दुकान के बाहर पीपल की छाया में आ खड़ा हुआ। लड़की फिर चने के दाने कड़ाही की रेत में डाल हिलाने लगी थी। वह दूसरे हाथ से कड़ाही के नीचे सूखे पत्ते इत्यादि डाल-डालकर आग को तीव्र कर रही थी।
अकबर की दृष्टि भी भटियारिन की ओर गई तो वह उसकी रूप-रेखा पर मुग्ध हो गया। उसने दुकान के सामने जाकर कहा, ‘‘सुंदरी ! एक टके के चने दो।’’
‘सुंदरी’ शब्द से लड़की का ध्यान भट्टी की ओर से हटकर शहंशाह पर गया। उसकी पोसाक और रूप-राशि देख लड़की समझ गई कि कोई रईस है। इसी समय उसने सड़क पर आधे दर्जन सिपाहियों को भी खड़े देखा। इस कारण वह बोली, ‘‘हुज़ूर ! ज़रा ठहरिए। इस पुर को निकाल लूँ तो देती हूँ।’’
‘‘किसकी बेटी हो ?’’
‘‘इस सराय के मालिक की।’’
‘‘वह कहाँ है ?’’
‘‘भीतर किसी काम से गया है।’’
‘‘बहुत सख्त काम वह तुमसे ले रहा है।’’ अकबर ने लड़की से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा। लड़की रेत और चने छननी में लेकर भुने रेत से पृथक कर रही थी। काम में व्यस्त और यात्री की ओर न देखते हुए उसने कह दिया, ‘‘हुज़ूर ! पेट की खातिर सब मेहनत करते हैं। आप भी तो इस धूप में यात्रा कर रहे हैं।’’
‘‘तो मैं भी पेट के लिए कर रहा हूँ ?’’ अकबर ने लड़की से बातों में दिल बहलाने के लिए कह दिया।
लड़की का सतर्क उत्तर था, ‘‘शरीर, मन और बुद्धि की तसल्ली के लिए ही तो सब संसार भाग-दौड़ रहा है।’’
‘‘ओह !’’ अकबर को लड़की के उत्तर में एक श्रेष्ठ मंतक (मीमांसा) युक्त कथन ही लगा। वह आवाक् लड़की के मुख को देखता रह गया।
लड़की ने तराजू उठाया और एक पत्थर का बाट डाल चने तोल तराजू का पलड़ा शहंशाह की ओर कर दिया और कहा, ‘‘हुज़ूर ! किसी रुमाल में डलवा लें।’’
अकबर तो लड़की के हाथ-पाँव और शरीर की बनावट को देख रहा था। लड़की ने तराजू के पलड़े को आगे किया और शहंशाह ने जब चनों के लिए रुमाल नहीं निकाला तो लड़की ने कहा, ‘‘यह हैं दो पैसे के चने बताइए, किसमें लेंगे ?’’
‘‘ओह !’’ अकबर ने जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला तो लड़की ने समझा कि रुमाल तो बहुत कीमती है। चनों से खराब भी हो सकता है। इस कारण उसने कहा, ‘‘तो इस पर डाल दूँ ? परंतु आप तो मेरे मुख को देख रहे हैं।’’
‘‘हाँ ! क्या उम्र है तुम्हारी ?’’
‘‘तो दो पैसे में यह भी बताना पड़ेगा ?’’
‘‘इसके बताने का दाम अलहदा भी दिया जा सकता है।’’
‘‘नहीं। मेरी माँ कहती है कि मैं आगामी कार्तिक से पंद्रह साल की हो जाऊँगी।’’
‘‘और तुम्हारी शादी नहीं हुई ?’’
इसका उत्तर लड़की ने नहीं दिया और चने बिछे रेशमी रुमाल पर डाल दो पैसे लेने के लिए हाथ पसार दिया।
अकबर ने जेब से एक स्वर्ण मुहर निकालकर लड़की की ओर बढ़ाई। लड़की मुहर को देखकर बोली, ‘‘इसका बाकी मेरे पास नहीं है।’’
‘‘और मेरे पास इससे कम नहीं हैं।’’
‘‘तो रहने दो।’’
‘‘और चनों के दाम ?’’
‘‘फिर कभी इधर आइएगा तो दे दीजिएगा।’’
‘‘और अगर मैं न दूँ तो ?’’
‘‘तो आप बेईमान भी हैं ? आप तो रईस मालूम होते हैं।’’
‘‘तो रईस बेईमान नहीं होते ?’’
‘‘उनको बेईमानी करने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा ने उन्हें इतना कुछ दिया होता है कि उन्हें दो पैसे के लिए मुकर जाने की जरूरत नहीं होती।’’
अकबर विचार कर रहा था कि वह तो नित्य अपने राज्य की वृद्धि के लिए झूठ, फरेब और बल का प्रयोग कर रहा है। तो क्या वह कंगला है जो यह करता है ?
उसे लड़की की दलील गलत समझ आई। उसकी तीन बेगमें तो राजमहल में ही थीं और उनके अतिरिक्त भी कई स्त्रियों से संबंध था। उस पर भी वह इस लड़की के सौंदर्य को, जो मैले, भट्टी के धुएँ से काले हुए कपड़ों में छुपा हुआ था, देख मन में इसको प्राप्त करने की लालसा करने लगा था।
वह यह समझा कि यह जीवन-मीमांसा निर्धनों को शांत और अपनी निर्धनता से संतुष्ट रखने के लिए किसी ने बनाई है। वस्तुस्थिति यह है कि धनवान अधिक लोभी होते हैं। निर्धन धनवानों से अधिक संतोषी और ईमानदार होते हैं।
‘‘मैं तो रईस हूँ, मगर दो पैसे के लिए बेईमान भी हो सकता हूँ।’’
‘‘तो परमात्मा तुमसे अगले जन्म में नाक में नकेल डालकर दिलवा देगा।’’
‘‘नहीं। मैं तो इसी जन्म में दाम अदा करना चाहता हूँ।’’
‘‘तो अपने किसी साथी से दो पैसे मांग लो।’’ इतना कहकर लड़की ने सड़क पर खड़े सिपाहियों की ओर देखा।
अकबर को यह बात समझ आई तो उसने कह दिया, ‘‘तो मैं देखता हूँ कि किसी के पास एक टका है अथवा नहीं।’’
इतना कह वह रुमाल में चने बाँध सड़क की ओर चल पड़ा। भटियारिन अपने काम में लीन हो गई और दो पैसे की बात भूल गई।
एक घड़ी लगी घोड़े की नाल लगाने में। करीमखाँ घोड़े की नाल लगवा उसे लगाम से पकड़ सड़क पर ले आया। सड़क पर करीमखाँ से शहंशाह ने कुछ बात कही और वह दो सिपाहियों के साथ दुकान पर आया और लपककर दुकान पर चढ़ लड़की को पकड़ कंधे पर डाल सड़क की ओर भागा।
लड़की ने शोर मचा दिया, ‘‘बचाओ ! बचाओ ! बाबा ! बचाओ !’’
सराय में से तीन-चार व्यक्ति हाथों में तलवारें लिए निकल आए और सड़क पर लड़की को छटपटाते हुए और चीख-पुकार करते हुए देख उधर लपके।
अकबर लड़की को अपने घोड़े पर लाद स्वयं घोड़े पर सवार हो सरपट भागता हुआ चल दिया। उसके सिपाही घोड़ों पर सवार हो शहंशाह के पीछे चल पड़े।
सराय में से निकले लोग हाथों में तलवार लिए लड़की का अपहरण करनेवालों को घोड़े दौड़ाते हुए और अपने पीछे उड़ती धूल छोड़ते हुए देखते रह गए।
2
सराय का मालिक रामकृष्ण भटियारा था। तीस वर्ष पूर्व वह मथुरा के समीप एक
गाँव से आगरा जाता हुआ थकावट दूर करने के लिए सड़क के किनारे बने एक कुएँ
की जगत पर बैठ गया। उसने अपने थैले से डोर-लोटा निकाल कुएँ से जल निकाल कर
पिया कुएँ का जल ठंडा और मीठा था। कुएँ के समीप घनी छाया का एक पीपल का
पेड़ देखकर वह विचार करने लगा कि आगरा में क्या रखा है। यहीं क्यों न
दुकान कर ले। दिल्ली-आगरा की सड़क तब भी बहुत चालू थी। रामकृष्ण के
बैठे-बैठे पंद्रह-बीस यात्री आए जो कुएँ से जल निकाल पी चलते गए।
रामकृष्ण गाँव में सबसे निर्धन व्यक्ति था। वहाँ खाने को तो मिल जाता था, परंतु जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए नकद कुछ नहीं मिलता था। अपने गाँव में भी वह चने, मक्की, बाजरा भून-भूनकर गाँववालों को दिया करता था, और उसके बदले में गाँव वाले उसे गेहूँ, गुड़, शाक-भाजी इत्यादि दे जाते थे। कोई धनी भूमिपति कभी फटा-पुराना कपड़ा भी दे जाता था, परंतु नकद एक भी पैसा उसके हाथ में नहीं आता था।
माता-पिता विहीन रामकृष्ण गाँव के जीवन से ऊब नगर में अपने भाग्य की परीक्षा लेने चल पड़ा था। मार्ग में कुएँ पर स्वयं थकावट दूर करने और जल पीने बैठा तो उसके देखते-देखते कई यात्री आए और उसके डोरी-लोटे से जल निकाल पी चल दिए। कोई आगरा को कोई मथुरा को।
रामकृष्ण मन में कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगा। परिणामस्वरूप वह कुएँ की जगत पर बैठा ही रह गया। लोग आए और चलते गए। सायंकाल हो गया और वह कुएँ की जगत पर ही एक ईंट का तकिया बनाकर लेट गया।
प्रातः उठा तो प्रातः की शीतल समीर में वह दृढ़ संकल्प हो वहाँ रहने का विचार करने लगा। दूर खेत में गोड़ाई करते किसानों के पास जा उनसे फावड़ा माँग लाया और पीपल के पेड़ की बगल में मनमानी भूमि पर निशान लगाकर उस पर अधिकार जमाने का प्रबंध करने लगा। वहाँ से एक कोस के अंतर पर एक गाँव से भुने चने उधार माँग लाया और कुएँ की जगत पर चादर बिछा उन पर भुने चने रख तथा लोटे से पानी निकाल प्याऊ लगा बैठ गया।
मध्याह्न के समय यात्री आकर ठहरने लगे। भुने चने रखे देख कुछ एक-एक पैसा दाम दे मोल ले खाने लगे तो रामकृष्ण लोटा-डोरी से जल निकाल उनको पिला देता। पहले दिन दस पैसे मिले। सायँ काल वह गाँव में गया। वह भटियारे को पाँच पैसे दे पुनः अगले दिन के लिए चने ले कुएँ की जगत पर आ बैठा। दिन चढ़ने से मध्याह्न तक वह अपने मकान के लिए मिट्टी खोद उसमें कुएँ से निकाले जल से गारा बना एक कोठरी की दीवारें बनाने लगा। मध्याह्न के समय वह कुएँ पर जल पिलाने तथा चने बेचने का काम करता था। वहाँ से कोई भी बड़ी बस्ती पाँच कोस से कम अंतर पर नहीं थी। इस कारण यात्री मध्याह्न के उपरांत ही आने लगते थे और प्यास तथा थकावट से व्याकुल कुएँ पर आते तो एक पैसे के चने और फोकट में जल पीकर तृप्त हो रामकृष्ण को आशीष देते हुए चल देते थे। रामकृष्ण सायं होते पड़ोस के गाँव में जाता और भटियारे को अपनी कमाई का आधा भाग देकर अगले दिन के लिए चने ले आता।
छः मास में वह अपने हाथ से ही एक कमरा बनाने में सफल हो गया। उसके पास बीस रुपये के लगभग जमा हो गए और उसने कमरे में भट्टी बना चने भूनने का प्रबन्ध स्वयं कर लिया।
छः महीने और लगे जब उसकी दुकान यात्रियों में विख्यात होने लगी। उसने अपने कमरे के साथ एक दूसरा कमरा भी बना लिया। कहावत है कि स्थान अनुकूल हो तो प्राणी उसमें रहने के लिए स्वतः ही आ जाते हैं।
पड़ोस के गाँव के भटियारे की लड़की युवा हो रही थी। रामकृष्ण को परिश्रम से उन्नति करते देख भटियारे ने ही अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। अब दो के स्थान पर चार हाथ कार्य करने लगे तो रामकृष्ण की दुकान और निवास आरामगाह का रूप धारण करने लगे। रामकृष्ण के पास रुपये भी एकत्रित होने लगे।
पाँच वर्ष में रामकृष्ण ने सराय बना ली। इस समय तक उसके तीन संताने भी हो चुकी थीं। गाँव में भटियारे के कार्य से सड़क पर यात्रियों की सेवा अधिक लाभ वाला काम सिद्ध हुआ।
दस वर्ष में रामकृष्ण का बड़ा लड़का मोहन आठ वर्ष का हो गया। उससे दो छोटे लड़के भी थे। नाम था भगवती और कल्याण। तब तक सराय पक्की ईंटों की बनने लगी थी। जो यात्री वहाँ रात को रहते उन्हें एक रात रहने का आधा रुपया देना पड़ता और उसी आधे रुपये में उसे एक समय की रोटी मिल जाती थी। अन्न-अनाज बहुत सस्ता था। एक रुपये का दो मन गेहूँ, बीस सेर गुड़ था। शाक-भाजी यात्रियों के मतलब की और दाल, नमक, मिर्च सब मिलाकर एक व्यकित के समय के खाने पर तीन-चार पैसे से अधिक नहीं बैठता था। सेवा रामकृष्ण की पत्नी और बच्चे कर देते थे और पाँच से दस तक यात्री वहाँ आकर रात को विश्राम पाते थे। इस प्रकार पाँच-छः रुपये नित्य की आय सराय की कोठरियों से हो जाती थी और निर्वाह तथा उन्नति मजे से होने लगी थी।
पाँच वर्ष और व्यतीत हुए तो सराय के अहाते के चारों और पक्की दीवार और उसमें तीन खुले बरामदे तथा सात कोठरियाँ बन गईं थीं। जो खुले बरामदों में सोते थे उनको खाट तथा खाना चार आने में मिल जाता था और जो कमरा लेते थे उनको बारह आने प्रति प्राणी देने पड़ते थे। कोठरियों में प्रायः बाल-बच्चों के साथ यात्रा करने वाले ठहरते थे।
रामकृष्ण की कल्पना का महल पंद्रह वर्ष के अनथक प्रयत्न से साकार होने लगा था। उन दिनों उसकी पत्नी राधा, बच्चे मोहन, भगवती और कल्याण तो घर के प्राणी थे। एक सेवक भी रखा हुआ था। जो यात्रियों को भोजन खिलाने-पिलाने में सहायक होता था। दो-तीन सहस्र रुपये वार्षिक की बचत होती थी और उसका अधिकांश रामकृष्ण सराय को अधिक और अधिक सुखप्रद तथा सुंदर बनाने में व्यय करता था। सराय के प्रांगण में छोटी-सी फुलवाड़ी भी लग गई थी। एक कमरा तो दरी, पलँग और बैठने की चौकियोंवाला बन गया था। इस कमरे के साथ पृथक् शौचालय भी बना दिया गया था।
रामकृष्ण गाँव में सबसे निर्धन व्यक्ति था। वहाँ खाने को तो मिल जाता था, परंतु जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए नकद कुछ नहीं मिलता था। अपने गाँव में भी वह चने, मक्की, बाजरा भून-भूनकर गाँववालों को दिया करता था, और उसके बदले में गाँव वाले उसे गेहूँ, गुड़, शाक-भाजी इत्यादि दे जाते थे। कोई धनी भूमिपति कभी फटा-पुराना कपड़ा भी दे जाता था, परंतु नकद एक भी पैसा उसके हाथ में नहीं आता था।
माता-पिता विहीन रामकृष्ण गाँव के जीवन से ऊब नगर में अपने भाग्य की परीक्षा लेने चल पड़ा था। मार्ग में कुएँ पर स्वयं थकावट दूर करने और जल पीने बैठा तो उसके देखते-देखते कई यात्री आए और उसके डोरी-लोटे से जल निकाल पी चल दिए। कोई आगरा को कोई मथुरा को।
रामकृष्ण मन में कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगा। परिणामस्वरूप वह कुएँ की जगत पर बैठा ही रह गया। लोग आए और चलते गए। सायंकाल हो गया और वह कुएँ की जगत पर ही एक ईंट का तकिया बनाकर लेट गया।
प्रातः उठा तो प्रातः की शीतल समीर में वह दृढ़ संकल्प हो वहाँ रहने का विचार करने लगा। दूर खेत में गोड़ाई करते किसानों के पास जा उनसे फावड़ा माँग लाया और पीपल के पेड़ की बगल में मनमानी भूमि पर निशान लगाकर उस पर अधिकार जमाने का प्रबंध करने लगा। वहाँ से एक कोस के अंतर पर एक गाँव से भुने चने उधार माँग लाया और कुएँ की जगत पर चादर बिछा उन पर भुने चने रख तथा लोटे से पानी निकाल प्याऊ लगा बैठ गया।
मध्याह्न के समय यात्री आकर ठहरने लगे। भुने चने रखे देख कुछ एक-एक पैसा दाम दे मोल ले खाने लगे तो रामकृष्ण लोटा-डोरी से जल निकाल उनको पिला देता। पहले दिन दस पैसे मिले। सायँ काल वह गाँव में गया। वह भटियारे को पाँच पैसे दे पुनः अगले दिन के लिए चने ले कुएँ की जगत पर आ बैठा। दिन चढ़ने से मध्याह्न तक वह अपने मकान के लिए मिट्टी खोद उसमें कुएँ से निकाले जल से गारा बना एक कोठरी की दीवारें बनाने लगा। मध्याह्न के समय वह कुएँ पर जल पिलाने तथा चने बेचने का काम करता था। वहाँ से कोई भी बड़ी बस्ती पाँच कोस से कम अंतर पर नहीं थी। इस कारण यात्री मध्याह्न के उपरांत ही आने लगते थे और प्यास तथा थकावट से व्याकुल कुएँ पर आते तो एक पैसे के चने और फोकट में जल पीकर तृप्त हो रामकृष्ण को आशीष देते हुए चल देते थे। रामकृष्ण सायं होते पड़ोस के गाँव में जाता और भटियारे को अपनी कमाई का आधा भाग देकर अगले दिन के लिए चने ले आता।
छः मास में वह अपने हाथ से ही एक कमरा बनाने में सफल हो गया। उसके पास बीस रुपये के लगभग जमा हो गए और उसने कमरे में भट्टी बना चने भूनने का प्रबन्ध स्वयं कर लिया।
छः महीने और लगे जब उसकी दुकान यात्रियों में विख्यात होने लगी। उसने अपने कमरे के साथ एक दूसरा कमरा भी बना लिया। कहावत है कि स्थान अनुकूल हो तो प्राणी उसमें रहने के लिए स्वतः ही आ जाते हैं।
पड़ोस के गाँव के भटियारे की लड़की युवा हो रही थी। रामकृष्ण को परिश्रम से उन्नति करते देख भटियारे ने ही अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। अब दो के स्थान पर चार हाथ कार्य करने लगे तो रामकृष्ण की दुकान और निवास आरामगाह का रूप धारण करने लगे। रामकृष्ण के पास रुपये भी एकत्रित होने लगे।
पाँच वर्ष में रामकृष्ण ने सराय बना ली। इस समय तक उसके तीन संताने भी हो चुकी थीं। गाँव में भटियारे के कार्य से सड़क पर यात्रियों की सेवा अधिक लाभ वाला काम सिद्ध हुआ।
दस वर्ष में रामकृष्ण का बड़ा लड़का मोहन आठ वर्ष का हो गया। उससे दो छोटे लड़के भी थे। नाम था भगवती और कल्याण। तब तक सराय पक्की ईंटों की बनने लगी थी। जो यात्री वहाँ रात को रहते उन्हें एक रात रहने का आधा रुपया देना पड़ता और उसी आधे रुपये में उसे एक समय की रोटी मिल जाती थी। अन्न-अनाज बहुत सस्ता था। एक रुपये का दो मन गेहूँ, बीस सेर गुड़ था। शाक-भाजी यात्रियों के मतलब की और दाल, नमक, मिर्च सब मिलाकर एक व्यकित के समय के खाने पर तीन-चार पैसे से अधिक नहीं बैठता था। सेवा रामकृष्ण की पत्नी और बच्चे कर देते थे और पाँच से दस तक यात्री वहाँ आकर रात को विश्राम पाते थे। इस प्रकार पाँच-छः रुपये नित्य की आय सराय की कोठरियों से हो जाती थी और निर्वाह तथा उन्नति मजे से होने लगी थी।
पाँच वर्ष और व्यतीत हुए तो सराय के अहाते के चारों और पक्की दीवार और उसमें तीन खुले बरामदे तथा सात कोठरियाँ बन गईं थीं। जो खुले बरामदों में सोते थे उनको खाट तथा खाना चार आने में मिल जाता था और जो कमरा लेते थे उनको बारह आने प्रति प्राणी देने पड़ते थे। कोठरियों में प्रायः बाल-बच्चों के साथ यात्रा करने वाले ठहरते थे।
रामकृष्ण की कल्पना का महल पंद्रह वर्ष के अनथक प्रयत्न से साकार होने लगा था। उन दिनों उसकी पत्नी राधा, बच्चे मोहन, भगवती और कल्याण तो घर के प्राणी थे। एक सेवक भी रखा हुआ था। जो यात्रियों को भोजन खिलाने-पिलाने में सहायक होता था। दो-तीन सहस्र रुपये वार्षिक की बचत होती थी और उसका अधिकांश रामकृष्ण सराय को अधिक और अधिक सुखप्रद तथा सुंदर बनाने में व्यय करता था। सराय के प्रांगण में छोटी-सी फुलवाड़ी भी लग गई थी। एक कमरा तो दरी, पलँग और बैठने की चौकियोंवाला बन गया था। इस कमरे के साथ पृथक् शौचालय भी बना दिया गया था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book