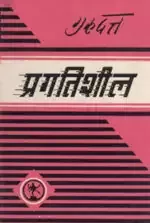|
सामाजिक >> प्रगतिशील प्रगतिशीलगुरुदत्त
|
409 पाठक हैं |
||||||
प्रगतिशील पुस्तक का कागजी संस्करण...
कागजी संस्करण
प्रथम उपन्यास ‘‘स्वाधीनता के पथ
पर’’ से ही ख्याति की सीढ़ियों पर जो चढ़ने लगे कि
फिर रुके नहीं।
विज्ञान की पृष्ठभूमि पर वेद, उपनिषद् दर्शन इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन आरम्भ किया तो उनको ज्ञान का अथाह सागर देख उसी में रम गये।
वेद, उपनिषद् तथा दर्शन शास्त्रों की विवेचना एवं अध्ययन अत्यन्त सरल भाषा में प्रस्तुत करना गुरुदत्त की ही विशेषता रही है।
उपन्यासों में भी शास्त्रों का निचोड़ तो मिलता ही है, रोचकता के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि उनका कोई भी उपन्यास पढ़ना आरम्भ करने पर समाप्त किये बिना छोड़ा नहीं जा सकता।
विज्ञान की पृष्ठभूमि पर वेद, उपनिषद् दर्शन इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन आरम्भ किया तो उनको ज्ञान का अथाह सागर देख उसी में रम गये।
वेद, उपनिषद् तथा दर्शन शास्त्रों की विवेचना एवं अध्ययन अत्यन्त सरल भाषा में प्रस्तुत करना गुरुदत्त की ही विशेषता रही है।
उपन्यासों में भी शास्त्रों का निचोड़ तो मिलता ही है, रोचकता के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि उनका कोई भी उपन्यास पढ़ना आरम्भ करने पर समाप्त किये बिना छोड़ा नहीं जा सकता।
भूमिका
वर्तमान युग में ‘प्रगतिशील’ एक पारिभाषिक शब्द हो
गया है।
इसका अर्थ है योरप के सोलहवीं शताब्दी और उसके परवर्ती मीमांसकों द्वारा
बताए हुए मार्ग पर अनुकरण करने वाला। इनमें से अधिकांश मीमांसक अनात्मवादी
थे। इनके अनात्मवाद के व्यापक प्रचार का कारण था ईसाईमत का अनर्गल
अनात्मवाद, जो केवल निष्ठा पर आधारित था। बुद्धिवाद के सम्मुख वह स्थिर
नहीं रह सका।
ईसाई मतावलम्बियों की अन्ध-निष्ठा ने प्राचीन यूनानी जीवन मीमांसा का विनाश कर दिया था। यूनानी जीवन मीमांसा में अनात्मवाद का विरोध करने की क्षमता थी। उस मीमांसा का संक्षिप्त स्वरूप सुकरात के इन शब्दों में दिखाई देगा, ‘‘सदाचार के अनुवर्तन (यम-नियम-पालन) से सम्यक्ज्ञान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान साधारण मनुष्य में उत्पन्न होने होने वाले सामान्य ज्ञान से भिन्न होता है...सम्यक्ज्ञान उत्कृष्ट गुणयुक्त है। व्यापक विचारों (विवेक) से उसकी उत्पत्ति होती है।’’
सुकरात से भिन्न विचार रखने वाले भी कुछ मीमांसक तो थे परन्तु उस समय चली सुकरात की ही। इनका मार्ग अति कठिन था। ईसाइयों के निष्ठा मार्ग के सामने सदाचार का कठिन मार्ग विलीन हो गया। ईसाई कहते थे, ‘‘ईमान लाओ, फल मिलेगा।’’ ‘बेकन’ इत्यादि भौतिकवादियों के सामने यह निष्ठा भी परास्त हो गई। यह निष्ठा टूटी गैलीलियो इत्यादि वैज्ञानिको के युक्ति तथा प्रमाण से। इस भौतिकवाद के सम्मुख ईसाईयत की निष्ठा थोथी सिद्ध हुई।
भौतिकवाद पनपने लगा और इसने वर्तमान युग के प्रगतिवाद को जन्म दिया। प्रगतिवाद की राजनीति में पराकाष्ठा हुई रूस के बोलशिविकिज़म में तथा अर्थनीति का अन्त हुआ मार्क्स और एंजिलवाद में। समाजशास्त्र में यथार्थ रूप निखरा स्टालिन तथा लेनिन के आचरण में और आचार-मीमांसा में इसने जन्म दिया फ्रायडिज़्म को।
भौतिकवाद से उद्भूत फ्रायडिज़्म का विशद् तथा व्यापक रूप दिखाई दे रहा है अमेरिका के युवक-युवतियों के आचरण में। संसार भोग-विलास का स्थान है, जितना हो सके भोगा जाय, यह प्रत्येक व्यक्ति का आधार बन गया है। इस विचार के साथ-साथ अमेरिका में विरली जनसृष्टि, भूमि की अधिक मात्रा और यन्त्र-युग आदि से भी इस आचार-संहिता की प्रगति-शीलता को प्रबल आश्रय मिला है। यहाँ तक कि वहाँ की समृद्धता का आधार भी इस प्रगतिशीलता को ही समझा जाने लगा है।
इस लघु उपन्यास में आचार-संहिता पर प्रगतिशीलता के आघात की ही झलक है। इसके राजनीति, अर्थनीति और समाजशास्त्र पर प्रभाव का कुछ दर्शन ‘विलोम गति’, ‘दासता के नये रूप’ और ‘छलना’ नामक उपन्यासों में कराया जा चुका है। प्रस्तुत उपन्यास में तो भौतिकवाद की सन्तान प्रगतिवाद का आचार-संहिता पर प्रभाव ही प्रकट करने का यत्न किया गया है।
वर्तमान प्रगतिवाद और इसकी जननी भौतिकता की टक्कर भारतीय आत्मवाद ही ले सकेगा। इतनी क्षमता इसमे ही है। इस आत्मवाद का अर्थ है परमात्मा तथा आत्मा का आस्तित्व, पुनर्जन्म और कर्म-मीमांसा, यम-नियम पर आचरण और परिष्कृत (ऋतम्भरा) प्रज्ञा द्वारा सत्य-ज्ञान का साक्षात्कार अर्थात् विवेक। वास्तविक प्रगति जिसके लिए मानव शताब्दियों से तरस रहा है, वह यूरोपीय भौतिकवादी मीमांसकों द्वारा प्रचारित ‘प्रगति’ नहीं।
ये हैं इस उपन्यास के भाव। पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी देश अथवा जातिविशेष की निन्दा अथवा प्रशंसा से किंचित् भी सम्बन्ध नहीं। यह तो विचारों की विश्लेषणात्मक व्याख्या-मात्र है।
ईसाई मतावलम्बियों की अन्ध-निष्ठा ने प्राचीन यूनानी जीवन मीमांसा का विनाश कर दिया था। यूनानी जीवन मीमांसा में अनात्मवाद का विरोध करने की क्षमता थी। उस मीमांसा का संक्षिप्त स्वरूप सुकरात के इन शब्दों में दिखाई देगा, ‘‘सदाचार के अनुवर्तन (यम-नियम-पालन) से सम्यक्ज्ञान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान साधारण मनुष्य में उत्पन्न होने होने वाले सामान्य ज्ञान से भिन्न होता है...सम्यक्ज्ञान उत्कृष्ट गुणयुक्त है। व्यापक विचारों (विवेक) से उसकी उत्पत्ति होती है।’’
सुकरात से भिन्न विचार रखने वाले भी कुछ मीमांसक तो थे परन्तु उस समय चली सुकरात की ही। इनका मार्ग अति कठिन था। ईसाइयों के निष्ठा मार्ग के सामने सदाचार का कठिन मार्ग विलीन हो गया। ईसाई कहते थे, ‘‘ईमान लाओ, फल मिलेगा।’’ ‘बेकन’ इत्यादि भौतिकवादियों के सामने यह निष्ठा भी परास्त हो गई। यह निष्ठा टूटी गैलीलियो इत्यादि वैज्ञानिको के युक्ति तथा प्रमाण से। इस भौतिकवाद के सम्मुख ईसाईयत की निष्ठा थोथी सिद्ध हुई।
भौतिकवाद पनपने लगा और इसने वर्तमान युग के प्रगतिवाद को जन्म दिया। प्रगतिवाद की राजनीति में पराकाष्ठा हुई रूस के बोलशिविकिज़म में तथा अर्थनीति का अन्त हुआ मार्क्स और एंजिलवाद में। समाजशास्त्र में यथार्थ रूप निखरा स्टालिन तथा लेनिन के आचरण में और आचार-मीमांसा में इसने जन्म दिया फ्रायडिज़्म को।
भौतिकवाद से उद्भूत फ्रायडिज़्म का विशद् तथा व्यापक रूप दिखाई दे रहा है अमेरिका के युवक-युवतियों के आचरण में। संसार भोग-विलास का स्थान है, जितना हो सके भोगा जाय, यह प्रत्येक व्यक्ति का आधार बन गया है। इस विचार के साथ-साथ अमेरिका में विरली जनसृष्टि, भूमि की अधिक मात्रा और यन्त्र-युग आदि से भी इस आचार-संहिता की प्रगति-शीलता को प्रबल आश्रय मिला है। यहाँ तक कि वहाँ की समृद्धता का आधार भी इस प्रगतिशीलता को ही समझा जाने लगा है।
इस लघु उपन्यास में आचार-संहिता पर प्रगतिशीलता के आघात की ही झलक है। इसके राजनीति, अर्थनीति और समाजशास्त्र पर प्रभाव का कुछ दर्शन ‘विलोम गति’, ‘दासता के नये रूप’ और ‘छलना’ नामक उपन्यासों में कराया जा चुका है। प्रस्तुत उपन्यास में तो भौतिकवाद की सन्तान प्रगतिवाद का आचार-संहिता पर प्रभाव ही प्रकट करने का यत्न किया गया है।
वर्तमान प्रगतिवाद और इसकी जननी भौतिकता की टक्कर भारतीय आत्मवाद ही ले सकेगा। इतनी क्षमता इसमे ही है। इस आत्मवाद का अर्थ है परमात्मा तथा आत्मा का आस्तित्व, पुनर्जन्म और कर्म-मीमांसा, यम-नियम पर आचरण और परिष्कृत (ऋतम्भरा) प्रज्ञा द्वारा सत्य-ज्ञान का साक्षात्कार अर्थात् विवेक। वास्तविक प्रगति जिसके लिए मानव शताब्दियों से तरस रहा है, वह यूरोपीय भौतिकवादी मीमांसकों द्वारा प्रचारित ‘प्रगति’ नहीं।
ये हैं इस उपन्यास के भाव। पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी देश अथवा जातिविशेष की निन्दा अथवा प्रशंसा से किंचित् भी सम्बन्ध नहीं। यह तो विचारों की विश्लेषणात्मक व्याख्या-मात्र है।
-गुरुदत्त
प्रथम परिच्छेद
::1::
‘‘बाबा, ये कौन हैं ?’’
‘‘बेटा ! बहुत बड़े लोग हैं।’’
‘‘बड़े क्या होते हैं बाबा ?’’
‘‘जो बड़े होते हैं।’’
बच्चा समझ नहीं सका। वह अपने बाबा का मुख देखता रह गया। प्रश्न पूछने वाला तीन-चार वर्ष का लड़का, तन-बदन से नंगा, मिट्टी से लथ-पथ, एक बहुत ही छोटे से, मैले-कुचैले मकान के बाहर खड़े एक प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति से पूछ रहा था। यह अकेला मकान दिल्ली से पांच मील के अन्तर पर शाहदरा के बाहर, ग्राण्डट्रंक रोड से कुछ दूर हटकर बना हुआ था। जिसके विषय में प्रश्न पूछा गया था वह एक बहुत बढ़िया मोटर में चमचमाते कपड़े पहन कर आया था और अपने साथ आई दो स्त्रियों को छोड़कर चला गया था। मोटर गाजियाबाद की ओर से आई थी और उस ओर ही लौट गई।
यह प्रौढ़वस्था का व्यक्ति, गोपीचन्द, जो मोटर में आने वालों का स्वागत करने के लिए अपने घर के द्वार पर खड़ा हुआ था, उस घर का स्वामी था। लड़का मकान से कुछ अन्तर पर, खुले में मिट्टी से खेल रहा था। मोटर आई हॉर्न बजा, उसे सुनकर गोपी घर से निकल आया। मोटर और उसमें आने वालों को देख लड़का अपना खेल छोड़ मोटर के समीप आ खड़ा हुआ। मोटर खड़ी हुई तो स्त्रियां उतरकर मकान के भीतर चली गईं। साथ में आया हुआ पुरुष भी भीतर चला गया। मकान में छोटे-छोटे तीन कमरे थे और उसके साथ ही एक छोटा-सा सेहन भी था। सेहन के एक ओर को कमरे थे और तीन ओर को सात-सात फुट ऊंची दीवार थी। मकान काफी गन्दा था, परन्तु एक कमरा पिछले दिन झाड़-फूंक और धो कर साफ कर दिया गया था।
उस लड़के की दादी मोटर में आई स्त्रियों को उस साफ किए हुए कमरे में ले गई और एक को, जो अभी युवा ही प्रतीत होती थी, एक खाट पर बैठा दिया।
यह सब-कुछ देख वह पुरुष, बाहर गया और मोटर में से बिस्तर, कुछ चादरें और एक छोटा-सा ट्रंक उठा लाया। ये वस्तुएं उसने चारपाई के समीप रख दीं। फिर मदन की दादी की ओर देखकर बोला, ‘‘हम सायंकाल समाचार जानने के लिए आवेंगे।’’
दूसरी औरत, जो अभी तक खड़ी ही थी, बोली, ‘‘बाबू ! आज सायंकाल नहीं। कल प्रातःकाल आना।’’
‘‘अच्छी बात है।’’
वह पुरुष बाहर निकला और मोटर में बैठकर चला गया। जब मदन अपने बाबा के उत्तर से कुछ समझ नहीं पाया तो उसने फिर पूछा, ‘‘यह औरत कौन है ?’’
‘‘बेटा ! बड़े घर की है।’’
‘‘ये भीतर क्या कर रहे हैं ?’’
‘‘कल बताऊंगा।’’
मदन ने इस प्रकार अपने बाबा को संक्षेप में और निर्रथक, जिनको वह समझ न सका, बातें करते पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो मदन जब भी कोई बात करता था तो उसका बाबा उसको बहुत विस्तार से और समझ सकने योग्य शब्दों में बताया करता था। आज सबका अन्त उसने ‘कल बताऊंगा’ कहकर कर दिया।
वह कुछ और पूछने का विचार कर रहा था, परन्तु इस समय उसकी दादी घर से निकल कर बोली, ‘‘तुम अब काम पर जाओ।’’
गोपी ने कमरे में घुस, अपनी झल्ली उठाई और शाहदरा शहर की ओर चल पड़ा। वह सामान ढोने का काम किया करता था। दिन-भर दो-ढाई रुपया कमा लेता था। इससे उसका निर्वाह हो जाता था। एक समय उसका लड़का राधेलाल भी उसके साथ ही काम किया करता था। मदन, राधेलाल का लड़का था। राधेलाल की बहू का देहान्त हुआ तो वह जीवन से निराश हो, घर छोड़कर कहीं चला गया। उस समय मदन की आयु एक वर्ष की थी और वह तब से अपने दादा-दादी के पास रहता था।
गोपी गया तो मदन की दादी ने लड़के को कहा, ‘‘मदन ! जाओ खेलो। भूख लगे तो चले आना।’’
मदन पुनः अपने उसी स्थान पर जा कर, जो वह मोटर के आने पर छोड़कर आया था, घर बनाने लगा। दो-ढाई घण्टे तक खेलने के उपरान्त वह खाने के लिए आया। घर आया तो उसने देखा कि जो कमरा कल साफ किया गया था, भीतर से बन्द था। उसकी दादी और वे दोनों औरतें भीतर बैठी हुई थीं। मदन ने अपनी दादी को आवाज दी—‘‘अम्मा ! ओ अम्मा ! !’’
मदन ने सुना भीतर से किसी के कराहने का शब्द आ रहा है। वह डर गया और वहीं उस कमरे के द्वार के समीप बैठ उत्सुक्ता से पुनः आवाज की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु फिर आवाज नहीं आई। भीतर उसकी दादी ने पुकार सुन ली थी। अतः वह द्वार खोलकर बाहर आ पूछने लगी, ‘‘क्या बात है ?’’
‘‘अम्मा ! भीतर क्या है ?’’
‘‘कुछ है, कल बतायेंगे। जाओ, बाल्टी में पानी भरा है। आज जरा अपने आप ही नहा लो। उसके बाद रोटी दूंगी।’’
मदन आंगन में चला गया। आंगन कच्चा ही था। उसके एक कोने में पानी से भरी एक बाल्टी रखी हुई थी और समीप एक पटरी भी रखी थी। उसके समीप ही एक तामचीनी का जग पड़ा था। मदन पटरी पर बैठ गया और जग से पानी भर-भरकर अपने शरीर पर उड़ेलने लगा। इस प्रकार आधा भीगा आधा सूखा-सा वह भागता हुआ भीतर आया। दादी ने उसे देखा तो कह दिया, ‘‘तुम तो पूरे भीगे भी नहीं। क्या इसी तरह नहाते हैं ?’’
इस समय भीतर के कमरे में से फिर कराहने का स्वर सुनाई दिया। मदन उस ओर देखने लगा। दादी ने उसकी बांह पकड़ी और नहलाने के लिए ले गई।
उसने उसके बदन की मिट्टी धोई। फिर एक सूखे वस्त्र से उसका शरीर पोंछकर, उसको कुरता तथा पायजामा, जिनको घर पर धोये हुए दो सप्ताह से भी अधिक हो गये होंगे, पहना दिये और उसको रसोईघर में ले गई। एक रोटी और बैंगन का साग उसके हाथ में रख दिया। मदन खाने लगा। इस समय उस कमरे से पुनः कराहने की आवाज आई। यह आवाज पहले से भी ज्यादा जोर से आई थी।
‘‘अम्मा ! यह क्या हो रहा है ?’’
‘‘वह जो मोटर में आई थीं न ! उसको पीड़ा हो रही है।’’
‘‘क्यों हो रही है ?’’
‘‘बेटा ! कल बताऊंगी। अब तुम चुपचाप खाना खा लो। ‘‘यह कौन है मां !’’
‘‘बहुत बड़े आदमी हैं।’’
‘‘बेटा ! बहुत बड़े लोग हैं।’’
‘‘बड़े क्या होते हैं बाबा ?’’
‘‘जो बड़े होते हैं।’’
बच्चा समझ नहीं सका। वह अपने बाबा का मुख देखता रह गया। प्रश्न पूछने वाला तीन-चार वर्ष का लड़का, तन-बदन से नंगा, मिट्टी से लथ-पथ, एक बहुत ही छोटे से, मैले-कुचैले मकान के बाहर खड़े एक प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति से पूछ रहा था। यह अकेला मकान दिल्ली से पांच मील के अन्तर पर शाहदरा के बाहर, ग्राण्डट्रंक रोड से कुछ दूर हटकर बना हुआ था। जिसके विषय में प्रश्न पूछा गया था वह एक बहुत बढ़िया मोटर में चमचमाते कपड़े पहन कर आया था और अपने साथ आई दो स्त्रियों को छोड़कर चला गया था। मोटर गाजियाबाद की ओर से आई थी और उस ओर ही लौट गई।
यह प्रौढ़वस्था का व्यक्ति, गोपीचन्द, जो मोटर में आने वालों का स्वागत करने के लिए अपने घर के द्वार पर खड़ा हुआ था, उस घर का स्वामी था। लड़का मकान से कुछ अन्तर पर, खुले में मिट्टी से खेल रहा था। मोटर आई हॉर्न बजा, उसे सुनकर गोपी घर से निकल आया। मोटर और उसमें आने वालों को देख लड़का अपना खेल छोड़ मोटर के समीप आ खड़ा हुआ। मोटर खड़ी हुई तो स्त्रियां उतरकर मकान के भीतर चली गईं। साथ में आया हुआ पुरुष भी भीतर चला गया। मकान में छोटे-छोटे तीन कमरे थे और उसके साथ ही एक छोटा-सा सेहन भी था। सेहन के एक ओर को कमरे थे और तीन ओर को सात-सात फुट ऊंची दीवार थी। मकान काफी गन्दा था, परन्तु एक कमरा पिछले दिन झाड़-फूंक और धो कर साफ कर दिया गया था।
उस लड़के की दादी मोटर में आई स्त्रियों को उस साफ किए हुए कमरे में ले गई और एक को, जो अभी युवा ही प्रतीत होती थी, एक खाट पर बैठा दिया।
यह सब-कुछ देख वह पुरुष, बाहर गया और मोटर में से बिस्तर, कुछ चादरें और एक छोटा-सा ट्रंक उठा लाया। ये वस्तुएं उसने चारपाई के समीप रख दीं। फिर मदन की दादी की ओर देखकर बोला, ‘‘हम सायंकाल समाचार जानने के लिए आवेंगे।’’
दूसरी औरत, जो अभी तक खड़ी ही थी, बोली, ‘‘बाबू ! आज सायंकाल नहीं। कल प्रातःकाल आना।’’
‘‘अच्छी बात है।’’
वह पुरुष बाहर निकला और मोटर में बैठकर चला गया। जब मदन अपने बाबा के उत्तर से कुछ समझ नहीं पाया तो उसने फिर पूछा, ‘‘यह औरत कौन है ?’’
‘‘बेटा ! बड़े घर की है।’’
‘‘ये भीतर क्या कर रहे हैं ?’’
‘‘कल बताऊंगा।’’
मदन ने इस प्रकार अपने बाबा को संक्षेप में और निर्रथक, जिनको वह समझ न सका, बातें करते पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो मदन जब भी कोई बात करता था तो उसका बाबा उसको बहुत विस्तार से और समझ सकने योग्य शब्दों में बताया करता था। आज सबका अन्त उसने ‘कल बताऊंगा’ कहकर कर दिया।
वह कुछ और पूछने का विचार कर रहा था, परन्तु इस समय उसकी दादी घर से निकल कर बोली, ‘‘तुम अब काम पर जाओ।’’
गोपी ने कमरे में घुस, अपनी झल्ली उठाई और शाहदरा शहर की ओर चल पड़ा। वह सामान ढोने का काम किया करता था। दिन-भर दो-ढाई रुपया कमा लेता था। इससे उसका निर्वाह हो जाता था। एक समय उसका लड़का राधेलाल भी उसके साथ ही काम किया करता था। मदन, राधेलाल का लड़का था। राधेलाल की बहू का देहान्त हुआ तो वह जीवन से निराश हो, घर छोड़कर कहीं चला गया। उस समय मदन की आयु एक वर्ष की थी और वह तब से अपने दादा-दादी के पास रहता था।
गोपी गया तो मदन की दादी ने लड़के को कहा, ‘‘मदन ! जाओ खेलो। भूख लगे तो चले आना।’’
मदन पुनः अपने उसी स्थान पर जा कर, जो वह मोटर के आने पर छोड़कर आया था, घर बनाने लगा। दो-ढाई घण्टे तक खेलने के उपरान्त वह खाने के लिए आया। घर आया तो उसने देखा कि जो कमरा कल साफ किया गया था, भीतर से बन्द था। उसकी दादी और वे दोनों औरतें भीतर बैठी हुई थीं। मदन ने अपनी दादी को आवाज दी—‘‘अम्मा ! ओ अम्मा ! !’’
मदन ने सुना भीतर से किसी के कराहने का शब्द आ रहा है। वह डर गया और वहीं उस कमरे के द्वार के समीप बैठ उत्सुक्ता से पुनः आवाज की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु फिर आवाज नहीं आई। भीतर उसकी दादी ने पुकार सुन ली थी। अतः वह द्वार खोलकर बाहर आ पूछने लगी, ‘‘क्या बात है ?’’
‘‘अम्मा ! भीतर क्या है ?’’
‘‘कुछ है, कल बतायेंगे। जाओ, बाल्टी में पानी भरा है। आज जरा अपने आप ही नहा लो। उसके बाद रोटी दूंगी।’’
मदन आंगन में चला गया। आंगन कच्चा ही था। उसके एक कोने में पानी से भरी एक बाल्टी रखी हुई थी और समीप एक पटरी भी रखी थी। उसके समीप ही एक तामचीनी का जग पड़ा था। मदन पटरी पर बैठ गया और जग से पानी भर-भरकर अपने शरीर पर उड़ेलने लगा। इस प्रकार आधा भीगा आधा सूखा-सा वह भागता हुआ भीतर आया। दादी ने उसे देखा तो कह दिया, ‘‘तुम तो पूरे भीगे भी नहीं। क्या इसी तरह नहाते हैं ?’’
इस समय भीतर के कमरे में से फिर कराहने का स्वर सुनाई दिया। मदन उस ओर देखने लगा। दादी ने उसकी बांह पकड़ी और नहलाने के लिए ले गई।
उसने उसके बदन की मिट्टी धोई। फिर एक सूखे वस्त्र से उसका शरीर पोंछकर, उसको कुरता तथा पायजामा, जिनको घर पर धोये हुए दो सप्ताह से भी अधिक हो गये होंगे, पहना दिये और उसको रसोईघर में ले गई। एक रोटी और बैंगन का साग उसके हाथ में रख दिया। मदन खाने लगा। इस समय उस कमरे से पुनः कराहने की आवाज आई। यह आवाज पहले से भी ज्यादा जोर से आई थी।
‘‘अम्मा ! यह क्या हो रहा है ?’’
‘‘वह जो मोटर में आई थीं न ! उसको पीड़ा हो रही है।’’
‘‘क्यों हो रही है ?’’
‘‘बेटा ! कल बताऊंगी। अब तुम चुपचाप खाना खा लो। ‘‘यह कौन है मां !’’
‘‘बहुत बड़े आदमी हैं।’’
:2:
मदन दो-ढाई घण्टे के खेल-कूद और पेट-भर रोटी खाने के बाद अपनी चारपाई पर
सो गया। जब जागा तो उसकी अम्मा उसके समीप ही बैठी थी और निश्चिन्त हो भोजन
कर रही थी। मदन ने अपनी चटाई पर से झांककर उस कमरे की ओर देखा, जिसमें से
कराहने का स्वर सुनाई दिया था। कमरे का द्वार अभी भी बन्द ही था। मदन ने
पूछा अम्मा ! वे गये ?’’
‘‘कौन ?’’
‘‘वही, जो बकरे की भांति चीख रही थी।’’
‘‘बकरे की भांति ?’’
‘‘हां अम्मा ! खेत के उस पार जो मियां रहता है न। उन्होंने एक दिन हलाल किया था। जब वे बकरे को काट रहे थे, तो वह ऐसे ही चीखता था जैसे वह उस कोठरी में चीख रही थी।’’
‘‘वह अब नहीं चीखेगी।’’
‘‘तो गई ?’’
‘‘नहीं, अभी नहीं। कल जावेगी।’’
‘‘यहां क्या कर रही है ?’’
‘‘कल बताऊंगी।’’
विवश मदन चुप रहा। वह फिर खेलने के लिए चला गया। उसके बाबा ने उसको दीवाली के दिन एक मिट्टी का घोड़ा ला दिया था। वह अब एक टूटी टांग से दीवार के सहारे खड़ा था। मदन वहां पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े तथा अन्य कंकड़-पत्थर उस पर लाद रहा था। अपने खेल में वह भूल गया था कि उनके घर में आज कोई विलक्षण बात भी हुई है।
अगले दिन मदन सोकर उठा तो वह कमरा खुला पड़ा था। उसकी दादी उस कमरे में उसी चारपाई पर बैठी थी, जिसपर पिछले दिन वह युवा स्त्री आकर बैठ गई थी।
मदन आंखें मलता हुआ भीतर गया तो उसका बाबा चारपाई के समीप झुककर दादी की गोदी में एक बच्चे को देख रहा था। बच्चा निश्चिन्त सो रहा था। मदन दादी की चारपाई के समीप खड़ा हो उस बच्चे को देखने लगा। दादी मुस्कराती हुई कभी बच्चे की ओर, कभी मदन की ओर देख रही थी।
गोपी ने पूछा, ‘‘कैसे रखोगी इसको ?’’
‘‘जैसे मदन को रखा था।’’
‘‘परन्तु जब उसकी मां मर गई थी, उस समय तो वह एक वर्ष का हो गया था ?’’
‘‘इससे क्या होता है। वे दूध दे गये हैं, दूछ बनाने का ढंग सिखा गये हैं। मैं समझती हूं यह काम हो जावेगा।
‘‘अम्मा ! यह क्या है ?’’
‘‘यह तुम्हारी छोटी-सी बहिन है।’’
‘‘बहिन ! कहां से आई है ?’’
‘‘जो औरत कल आई थीं, वे दे गई हैं।’’
‘‘क्यों दे गई हैं ?
‘‘तुम्हारी कोई बहिन नहीं थी, इसलिए दे गई हैं।’’
‘‘मैं इसको गोदी में लूंगा।’’
‘‘अभी नहीं, दस दिन के बाद।’’
‘‘पर बाबा ! कल तो उनके साथ यह लड़की नहीं थी ?’’
‘‘थी तो, शायद तुमने देखी नहीं होगी।’’
‘‘नहीं, नहीं थी। अच्छा वे हैं कहां ?’’
‘‘चली गई हैं।’’
‘‘कहां गई हैं ?’’
‘‘जहां से आई थीं।’’
‘‘कहां से आई थीं ?’’
‘‘बहुत दूर से।’’
दिन व्यतीत होने लगे। दस दिन बाद मदन ने लड़की को अपनी गोद में लिया। वह नरम-नरम बहुत ही हल्की-सी और लाल-गुलाल थी। मदन चटाई पर बैठा उसको गोद लिये, उसके हाथो की छोटी-छोटी अंगुलियां देख रहा था।
‘‘क्या देख रहे हो मदन ?’’ उसकी दादी ने पूछा।
‘‘इसके तो बहुत ही छोटे नाखून हैं।’’
‘‘हां।’’
‘‘और अम्मा ! इसके दांत तो हैं ही नहीं।’’
‘‘हां, नहीं हैं।’’
‘‘तो यह रोटी किस तरह खायेगी ?’’
‘‘यह रोटी नहीं खायेगी।’’
‘‘तो क्या खायेगी ?’’
‘‘वह देखो, वह रखा है इसके खाने के लिए।’ दादी ने सामने आलने में रखी दूध की बोतल की ओर संकेत कर दिया।
‘‘इसका नाम क्या है अम्मा !’’
‘‘जो तुम रख दो।’’
‘‘कैसे रख दूं !’’
‘‘कोई नाम बोल दो।’’
‘‘कौशल्या।’’
‘‘वह तो तुम्हारी मां का नाम है।
‘‘तो क्या यह नाम नहीं रखा जा सकता ?’’
‘‘ऊं-हूं’’ दादी ने मुस्कराते हुए कहा।
‘‘तो तुम बता दो।’’
‘‘अच्छा।’’ दादी ने कहा और फिर विचार कर बोली, ‘‘लक्ष्मी।’’
‘‘यह तो उस लड़की का नाम है जो उस...।’’ मदन ने हाथ उठाकर दूर दिशा की ओर संकेत कर दिया—‘‘घर में रहती है।’’
‘‘हां वह बड़ी लक्ष्मी है और यह हमारी छोटी लक्ष्मी होगी।’’
मदन पांच वर्ष का हुआ तो स्कूल जाने लगा। पिछले दो वर्षों में घर में परिवर्तन होने लगे थे। घर की मरम्मत हो गई थी। पहले केवल रसोई का फर्श पक्का था। अब सब घर के फर्श पक्के और दीवारों पर तथा घर के बाहर-भीतर पलस्तर सफेदी तथा दरवाजों पर रंगरोगन हो गया था। गोपीचन्द अब शाहदरा में फलों की छोटी-सी दुकान करता था। घर में फर्नीचर और कपड़े भी साफ-सुथरे दिखाई देने लगे थे। मदन सप्ताह में दो बार कपड़े बदलता था। लक्ष्मी के कपड़े तो मदन के कपड़ों से भी अधिक साफ-सुथरे होते थे।
लक्ष्मी को गोपी और उसकी पत्नी के हवाले करके जाने वाले उसके पालन-पोषण के लिए पचहत्तर रुपये मासिक देते थे। प्रति वर्ष मोटर आती थी और उसमें एक स्त्री और एक पुरुष होता था, वे लक्ष्मी को देखते, गोद में लेते, प्यार करते और एक सहस्र रुपया दे जाते थे। साथ ही लड़की के पहनने के लिए भांति-भांति के कपड़े और गले में डालने के लिए एक सोने की चैन दे गए थे।
‘‘कौन ?’’
‘‘वही, जो बकरे की भांति चीख रही थी।’’
‘‘बकरे की भांति ?’’
‘‘हां अम्मा ! खेत के उस पार जो मियां रहता है न। उन्होंने एक दिन हलाल किया था। जब वे बकरे को काट रहे थे, तो वह ऐसे ही चीखता था जैसे वह उस कोठरी में चीख रही थी।’’
‘‘वह अब नहीं चीखेगी।’’
‘‘तो गई ?’’
‘‘नहीं, अभी नहीं। कल जावेगी।’’
‘‘यहां क्या कर रही है ?’’
‘‘कल बताऊंगी।’’
विवश मदन चुप रहा। वह फिर खेलने के लिए चला गया। उसके बाबा ने उसको दीवाली के दिन एक मिट्टी का घोड़ा ला दिया था। वह अब एक टूटी टांग से दीवार के सहारे खड़ा था। मदन वहां पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े तथा अन्य कंकड़-पत्थर उस पर लाद रहा था। अपने खेल में वह भूल गया था कि उनके घर में आज कोई विलक्षण बात भी हुई है।
अगले दिन मदन सोकर उठा तो वह कमरा खुला पड़ा था। उसकी दादी उस कमरे में उसी चारपाई पर बैठी थी, जिसपर पिछले दिन वह युवा स्त्री आकर बैठ गई थी।
मदन आंखें मलता हुआ भीतर गया तो उसका बाबा चारपाई के समीप झुककर दादी की गोदी में एक बच्चे को देख रहा था। बच्चा निश्चिन्त सो रहा था। मदन दादी की चारपाई के समीप खड़ा हो उस बच्चे को देखने लगा। दादी मुस्कराती हुई कभी बच्चे की ओर, कभी मदन की ओर देख रही थी।
गोपी ने पूछा, ‘‘कैसे रखोगी इसको ?’’
‘‘जैसे मदन को रखा था।’’
‘‘परन्तु जब उसकी मां मर गई थी, उस समय तो वह एक वर्ष का हो गया था ?’’
‘‘इससे क्या होता है। वे दूध दे गये हैं, दूछ बनाने का ढंग सिखा गये हैं। मैं समझती हूं यह काम हो जावेगा।
‘‘अम्मा ! यह क्या है ?’’
‘‘यह तुम्हारी छोटी-सी बहिन है।’’
‘‘बहिन ! कहां से आई है ?’’
‘‘जो औरत कल आई थीं, वे दे गई हैं।’’
‘‘क्यों दे गई हैं ?
‘‘तुम्हारी कोई बहिन नहीं थी, इसलिए दे गई हैं।’’
‘‘मैं इसको गोदी में लूंगा।’’
‘‘अभी नहीं, दस दिन के बाद।’’
‘‘पर बाबा ! कल तो उनके साथ यह लड़की नहीं थी ?’’
‘‘थी तो, शायद तुमने देखी नहीं होगी।’’
‘‘नहीं, नहीं थी। अच्छा वे हैं कहां ?’’
‘‘चली गई हैं।’’
‘‘कहां गई हैं ?’’
‘‘जहां से आई थीं।’’
‘‘कहां से आई थीं ?’’
‘‘बहुत दूर से।’’
दिन व्यतीत होने लगे। दस दिन बाद मदन ने लड़की को अपनी गोद में लिया। वह नरम-नरम बहुत ही हल्की-सी और लाल-गुलाल थी। मदन चटाई पर बैठा उसको गोद लिये, उसके हाथो की छोटी-छोटी अंगुलियां देख रहा था।
‘‘क्या देख रहे हो मदन ?’’ उसकी दादी ने पूछा।
‘‘इसके तो बहुत ही छोटे नाखून हैं।’’
‘‘हां।’’
‘‘और अम्मा ! इसके दांत तो हैं ही नहीं।’’
‘‘हां, नहीं हैं।’’
‘‘तो यह रोटी किस तरह खायेगी ?’’
‘‘यह रोटी नहीं खायेगी।’’
‘‘तो क्या खायेगी ?’’
‘‘वह देखो, वह रखा है इसके खाने के लिए।’ दादी ने सामने आलने में रखी दूध की बोतल की ओर संकेत कर दिया।
‘‘इसका नाम क्या है अम्मा !’’
‘‘जो तुम रख दो।’’
‘‘कैसे रख दूं !’’
‘‘कोई नाम बोल दो।’’
‘‘कौशल्या।’’
‘‘वह तो तुम्हारी मां का नाम है।
‘‘तो क्या यह नाम नहीं रखा जा सकता ?’’
‘‘ऊं-हूं’’ दादी ने मुस्कराते हुए कहा।
‘‘तो तुम बता दो।’’
‘‘अच्छा।’’ दादी ने कहा और फिर विचार कर बोली, ‘‘लक्ष्मी।’’
‘‘यह तो उस लड़की का नाम है जो उस...।’’ मदन ने हाथ उठाकर दूर दिशा की ओर संकेत कर दिया—‘‘घर में रहती है।’’
‘‘हां वह बड़ी लक्ष्मी है और यह हमारी छोटी लक्ष्मी होगी।’’
मदन पांच वर्ष का हुआ तो स्कूल जाने लगा। पिछले दो वर्षों में घर में परिवर्तन होने लगे थे। घर की मरम्मत हो गई थी। पहले केवल रसोई का फर्श पक्का था। अब सब घर के फर्श पक्के और दीवारों पर तथा घर के बाहर-भीतर पलस्तर सफेदी तथा दरवाजों पर रंगरोगन हो गया था। गोपीचन्द अब शाहदरा में फलों की छोटी-सी दुकान करता था। घर में फर्नीचर और कपड़े भी साफ-सुथरे दिखाई देने लगे थे। मदन सप्ताह में दो बार कपड़े बदलता था। लक्ष्मी के कपड़े तो मदन के कपड़ों से भी अधिक साफ-सुथरे होते थे।
लक्ष्मी को गोपी और उसकी पत्नी के हवाले करके जाने वाले उसके पालन-पोषण के लिए पचहत्तर रुपये मासिक देते थे। प्रति वर्ष मोटर आती थी और उसमें एक स्त्री और एक पुरुष होता था, वे लक्ष्मी को देखते, गोद में लेते, प्यार करते और एक सहस्र रुपया दे जाते थे। साथ ही लड़की के पहनने के लिए भांति-भांति के कपड़े और गले में डालने के लिए एक सोने की चैन दे गए थे।
:3:
पांच वर्ष व्यतीत हो गये। लक्ष्मी अब सुन्दर चुलबुली और लम्बी-पतली लड़की
निकल आई थी। मदन इस समय तीसरी श्रेणी में पढ़ता था। इस बार वही स्त्री और
पुरुष आये तो गोपी की पत्नी से बोले, ‘‘अम्मा ! हम
इसको ले
जाना चाहते हैं।’’
‘‘तुम्हारी वस्तु है, जैसा मन में आए करो।’’
‘‘तो इसका सामान एकत्रित कर दो।’’
‘‘इस घर में जो कुछ है, वह सब इसी का ही है। यह इस घर की लक्ष्मी है। जो ले जाना चाहो और ले जा सको, ले जाओ।’’ यह कहते-कहते मदन की दादी के आंखों में आंसू छलक आये।
समीप बैठी औरत यह देख रही थी। उसने पूछा, ‘‘तुम्हें इसका सामान देने में दुःख होता है क्या ?’’
‘‘सामान देने में नहीं। यह सब कुछ इसी का ही तो है। आपके दिये रुपये से ही यह बना है। और उस रुपये के अतिरिक्त भी जो कुछ आया है, वह भी इसके भाग्य से ही आया है। इस कारण, अब जब यह जा रही है तो इस सामान के जाने में कोई सन्देह नहीं है। तुम नहीं ले जाओगी तो किसी और ढंग से चला जायेगा ?’’
‘‘कैसे चला जायेगा ?’’
‘‘जैसे किसी भाग्यवान के जाने से सौभाग्य चला जाता है। देखो बेटी ! हम सदा वैसे नहीं थे, जैसे तुमने हमें पांच वर्ष पूर्व देखा था। पंजाब में शेखुपुरा नगर की एक हवेली में हम रहा करते थे। पाकिस्तान बना तो हम वहां से चले आए किन्तु घर के पुरखा अर्थात् मेरे श्वसुर, जो उस समय सत्तर वर्ष के थे, मार्ग में उनका देहान्त हो गया। वे भाग्यवान थे। मैं, मेरे पति तथा मेरा पुत्र, हम तीनों को बेसरोसामान दिल्ली के स्टेशन पर उतार दिया गया।’’
फिर उसने उस स्थान की ओर इंगित करते हुए कहा, ‘‘हम तीनों इस स्थान को लावारिस देख, इधर-उधर से घास-फूस एकत्रित कर झोंपड़ा बना कर रहने लगे। उस समय मेरा पुत्र राधेलाल पाकिस्तान से आई हुई एक तेरह-चौदह वर्ष की लड़की ले आया था। लड़की के सभी परिवार वाले पाकिस्तान में मार डाले गये थे। एक दिन राधेलाल को शाहदरा स्टेशन पर वह परेशान-सी खड़ी दिखाई दी तो उसे वह अपने झोंपड़े में ले आया। मैंने उसे रख लिया। कुछ दिनों बाद उसका राधे से विवाह कर दिया और इस झोंपड़े के साथ ही एक अन्य झोंपड़ा बनाकर वे उसमें रहने लगे। बाप-बेटा मजदूरी करते थे। तीन-चार रुपये रोज लाते और हम औरतें ईंट-ईंट बटोरकर तथा खेत से मिट्टी खोदकर यह मकान बनाने लगे। कभी दस रुपये एकत्रित हो गये तो उससे नई ईंटें मोल ले आते। कभी कुछ ज्यादा रुपये बच जाते तो हम एक-दो दिन किसी राजगीर की सहायता ले लेते थे। दो वर्ष के कठोर परिश्रम से हमने वह कुछ निर्माण किया था, जो आपने आज से पांच वर्ष पूर्व देखा था।
‘‘तुम्हारी वस्तु है, जैसा मन में आए करो।’’
‘‘तो इसका सामान एकत्रित कर दो।’’
‘‘इस घर में जो कुछ है, वह सब इसी का ही है। यह इस घर की लक्ष्मी है। जो ले जाना चाहो और ले जा सको, ले जाओ।’’ यह कहते-कहते मदन की दादी के आंखों में आंसू छलक आये।
समीप बैठी औरत यह देख रही थी। उसने पूछा, ‘‘तुम्हें इसका सामान देने में दुःख होता है क्या ?’’
‘‘सामान देने में नहीं। यह सब कुछ इसी का ही तो है। आपके दिये रुपये से ही यह बना है। और उस रुपये के अतिरिक्त भी जो कुछ आया है, वह भी इसके भाग्य से ही आया है। इस कारण, अब जब यह जा रही है तो इस सामान के जाने में कोई सन्देह नहीं है। तुम नहीं ले जाओगी तो किसी और ढंग से चला जायेगा ?’’
‘‘कैसे चला जायेगा ?’’
‘‘जैसे किसी भाग्यवान के जाने से सौभाग्य चला जाता है। देखो बेटी ! हम सदा वैसे नहीं थे, जैसे तुमने हमें पांच वर्ष पूर्व देखा था। पंजाब में शेखुपुरा नगर की एक हवेली में हम रहा करते थे। पाकिस्तान बना तो हम वहां से चले आए किन्तु घर के पुरखा अर्थात् मेरे श्वसुर, जो उस समय सत्तर वर्ष के थे, मार्ग में उनका देहान्त हो गया। वे भाग्यवान थे। मैं, मेरे पति तथा मेरा पुत्र, हम तीनों को बेसरोसामान दिल्ली के स्टेशन पर उतार दिया गया।’’
फिर उसने उस स्थान की ओर इंगित करते हुए कहा, ‘‘हम तीनों इस स्थान को लावारिस देख, इधर-उधर से घास-फूस एकत्रित कर झोंपड़ा बना कर रहने लगे। उस समय मेरा पुत्र राधेलाल पाकिस्तान से आई हुई एक तेरह-चौदह वर्ष की लड़की ले आया था। लड़की के सभी परिवार वाले पाकिस्तान में मार डाले गये थे। एक दिन राधेलाल को शाहदरा स्टेशन पर वह परेशान-सी खड़ी दिखाई दी तो उसे वह अपने झोंपड़े में ले आया। मैंने उसे रख लिया। कुछ दिनों बाद उसका राधे से विवाह कर दिया और इस झोंपड़े के साथ ही एक अन्य झोंपड़ा बनाकर वे उसमें रहने लगे। बाप-बेटा मजदूरी करते थे। तीन-चार रुपये रोज लाते और हम औरतें ईंट-ईंट बटोरकर तथा खेत से मिट्टी खोदकर यह मकान बनाने लगे। कभी दस रुपये एकत्रित हो गये तो उससे नई ईंटें मोल ले आते। कभी कुछ ज्यादा रुपये बच जाते तो हम एक-दो दिन किसी राजगीर की सहायता ले लेते थे। दो वर्ष के कठोर परिश्रम से हमने वह कुछ निर्माण किया था, जो आपने आज से पांच वर्ष पूर्व देखा था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book